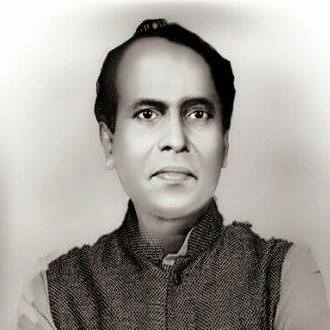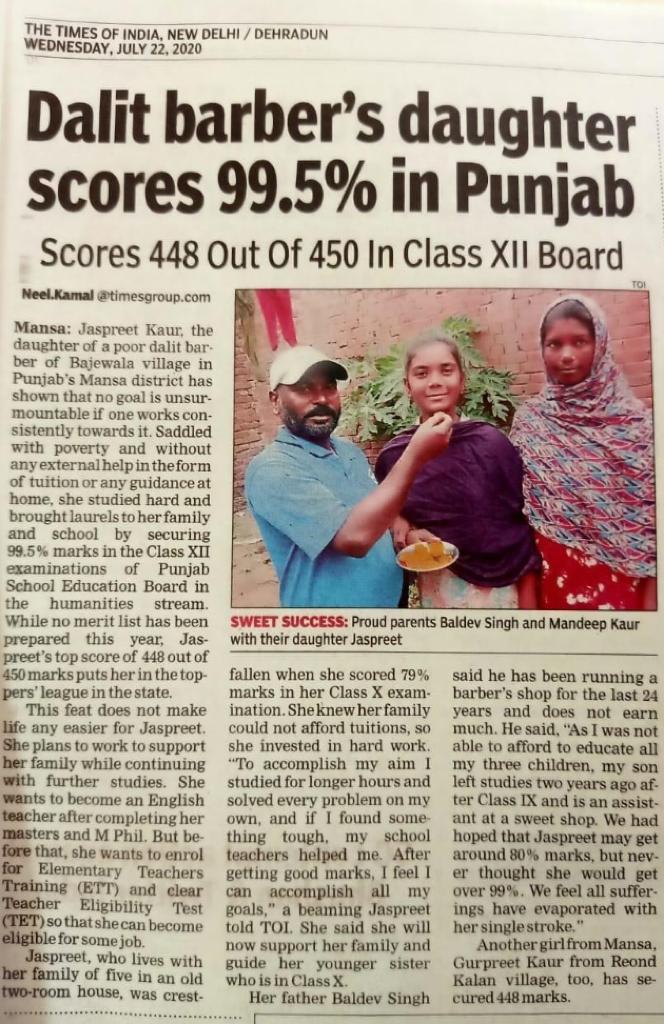विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।
इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।
इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। केंद्र सरकार के वह अध्यादेश, जिसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों उठा रहे हैं आवाज
 विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।
इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।
इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। अम्बेडकरवादी तैराक सत्येंन्द्र सिंह के हिस्से एक और बड़ा अवार्ड, बधाई सतेन्द्र
 अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक रखने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग तैराक सतेन्द्र सिंह लोहिया के पदकों की लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण सम्मान जुड़ गया है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने सतेन्द्र सिंह को तेनजिंग नौरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड (Tenzing Norgay National Award) 2019 देने की घोषणा की है। यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड के समकक्ष होता है। आमतौर पर यह अवार्ड सेना के जवानों (जल, थल और वायु) को दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी पैरा खिलाड़ी को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है।
अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक रखने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग तैराक सतेन्द्र सिंह लोहिया के पदकों की लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण सम्मान जुड़ गया है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने सतेन्द्र सिंह को तेनजिंग नौरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड (Tenzing Norgay National Award) 2019 देने की घोषणा की है। यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड के समकक्ष होता है। आमतौर पर यह अवार्ड सेना के जवानों (जल, थल और वायु) को दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी पैरा खिलाड़ी को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है।
इस अवार्ड की घोषणा 18 अगस्त को की गई। हर साल दिया जाने वाला यह अवार्ड खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद जयंती) के मौके पर 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा दरबार भवन में दिया जाता है। यह अवार्ड तीन कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स शामिल होता है। पहली बार यह पैरा खिलाड़ी को मिल रहा है। इस अवार्ड में अर्जुन अवार्ड की तरह ही पांच लाख रुपये नकद, एक शिल्ड और ब्लेजर दिया जाएगा। साथ ही प्रसस्ति पत्र भी दिया जाता है।
ये भी पढ़ें- इंग्लिश चैनल पार करने वाले सतेन्द्र बने एशिया के पहले दिव्यांग तैराक
गौरतलब है कि सतेन्द्र जाटव को इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार का सबसे प्रतिष्ठित विक्रम अवार्ड (2014) में और भारत सरकार द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर (दिव्यांग कैटेगरी) अवार्ड (2019) में मिल चुका है। विशेष बात यह है कि सतेन्द्र सिंह व्हीलचेयर पर रहते हैं और 70 फीसदी दिव्यांग हैं। ऐसे में सतेन्द्र का जीवन कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हालांकि सतेन्द्र सिंह अपना प्रेरणास्रोत कांशीराम जी को मानते हैं। सतेन्द्र सिंह का कहना है कि मान्यवर कांशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि जिसकी तमन्ना सच्ची हो उसे रास्ते मिल जाते हैं, और जिसकी तमन्ना सच्ची नहीं हो उसे बहाने मिल जाते हैं। इस वाक्य को जीवन में उतारते हुए सतेन्द्र सिंह ने दिव्यांगता को कभी अपनी कमी नहीं मानी और हर मुकाम हासिल किया। सतेन्द्र इसके पहले इंग्लिश चैनल और कैटलिना चैनल को भी पार कर चुके हैं। आप भी सतेन्द्र जी से प्रेरणा ले सकते हैं। बधाई सतेन्द्र।
बर्बाद हो रही है गांव की बहुजन युवा पीढ़ी
 गांव की पूरी की पूरी युवा आबादी, घोर लंपटई की गिरफ्त में है। पढ़ाई -लिखाई से नाता टूट चुका है। देश-दुनिया की कुल समझ व्हाट्सएप से बनी है। वहां पाकिस्तान माफ़ी मांगता है और चीन थरथर कांपता है। दहेज में बाइक मिली है, भले ही तेल महंगा हैं, धान-गेंहू बेच, एक लीटर भरा ही लेते हैं और गांव में एक बार फटाफटा लेते हैं। गांवई माफिया उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आखेट कर किसी न किसी धार्मिक सेनाओं के पदाधिकारी बना कर, अपनी गिरफ्त में रखते हैं।
हमारे गांव के उत्तर में बढ़ई टोला है। वहां से अक्सर कुछ युवाओं के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। उनकी हिस्ट्री देखिए तो सिर पर रंगीन कपड़ा बांधे , जयकारा लगाते, मूर्ति विसर्जन में दारू पीते फोटो मिलेगी। यह है नई पीढ़ी! इसी पर है देश का भविष्य। एक बीमार समाज। ऐसी पीढ़ी अपने बच्चों को कहां ले जा रही?जमीन-जायदाद इतनी नहीं कि ठीक से घर चला सकें या बीमारी पर इलाज हो। तो इनके लिए बेहतर जीवन क्या है? ये किसी औघड़ सेना के सचिव हैं तो किसी धार्मिक संगठनों में फंसा दिए गए हैं। इनकी पीढियां अब उबरने वाली नहीं। दास बनने को अभिशप्त हैं ये। इन्हें हम जैसों की बातें सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। इनका कोई स्वप्न नहीं।घमण्ड इतना कि IAS , PCS उनकी जेब में होते हैं। एक अपाहिज बाप के जवान बेटे को दिनभर चिलम और नशा करते देख कर टोका था तो उसकी मां बोली- हमार बेटा, जवन मन करी उ करी, केहू से मांग के त पिये ला ना? (मेरे बेटे के मन में जो होगा करेगा, किसी से मांग के तो नहीं पीता न?)
अब ऐसे मर रहे समाज में जान फूंकना आसान काम नहीं है? शिक्षा बिना बात का असर नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि जिस समाज को सचेतन ढंग से बर्बाद किया गया हो, शिक्षा से वंचित किया गया हो तो यह सचेतन गुलाम बनाने का कृत्य है। यह अमानवीय भी है और शातिराना भी। गुलाम बाहुल्य समाज, दुनियाभर में निम्न ही रहेगा, बेशक कुछ की कुंठाएं तृप्त हों। फिलहाल ये उबरने से रहे।
गांव की पूरी की पूरी युवा आबादी, घोर लंपटई की गिरफ्त में है। पढ़ाई -लिखाई से नाता टूट चुका है। देश-दुनिया की कुल समझ व्हाट्सएप से बनी है। वहां पाकिस्तान माफ़ी मांगता है और चीन थरथर कांपता है। दहेज में बाइक मिली है, भले ही तेल महंगा हैं, धान-गेंहू बेच, एक लीटर भरा ही लेते हैं और गांव में एक बार फटाफटा लेते हैं। गांवई माफिया उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आखेट कर किसी न किसी धार्मिक सेनाओं के पदाधिकारी बना कर, अपनी गिरफ्त में रखते हैं।
हमारे गांव के उत्तर में बढ़ई टोला है। वहां से अक्सर कुछ युवाओं के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। उनकी हिस्ट्री देखिए तो सिर पर रंगीन कपड़ा बांधे , जयकारा लगाते, मूर्ति विसर्जन में दारू पीते फोटो मिलेगी। यह है नई पीढ़ी! इसी पर है देश का भविष्य। एक बीमार समाज। ऐसी पीढ़ी अपने बच्चों को कहां ले जा रही?जमीन-जायदाद इतनी नहीं कि ठीक से घर चला सकें या बीमारी पर इलाज हो। तो इनके लिए बेहतर जीवन क्या है? ये किसी औघड़ सेना के सचिव हैं तो किसी धार्मिक संगठनों में फंसा दिए गए हैं। इनकी पीढियां अब उबरने वाली नहीं। दास बनने को अभिशप्त हैं ये। इन्हें हम जैसों की बातें सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। इनका कोई स्वप्न नहीं।घमण्ड इतना कि IAS , PCS उनकी जेब में होते हैं। एक अपाहिज बाप के जवान बेटे को दिनभर चिलम और नशा करते देख कर टोका था तो उसकी मां बोली- हमार बेटा, जवन मन करी उ करी, केहू से मांग के त पिये ला ना? (मेरे बेटे के मन में जो होगा करेगा, किसी से मांग के तो नहीं पीता न?)
अब ऐसे मर रहे समाज में जान फूंकना आसान काम नहीं है? शिक्षा बिना बात का असर नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि जिस समाज को सचेतन ढंग से बर्बाद किया गया हो, शिक्षा से वंचित किया गया हो तो यह सचेतन गुलाम बनाने का कृत्य है। यह अमानवीय भी है और शातिराना भी। गुलाम बाहुल्य समाज, दुनियाभर में निम्न ही रहेगा, बेशक कुछ की कुंठाएं तृप्त हों। फिलहाल ये उबरने से रहे।
- वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष चंद्र कुशवाहा जी के फेसबुक पेज से
जयंती विशेषः पिछड़े समाज को रामस्वरूप वर्मा के नायकत्व से सीख लेनी चाहिए
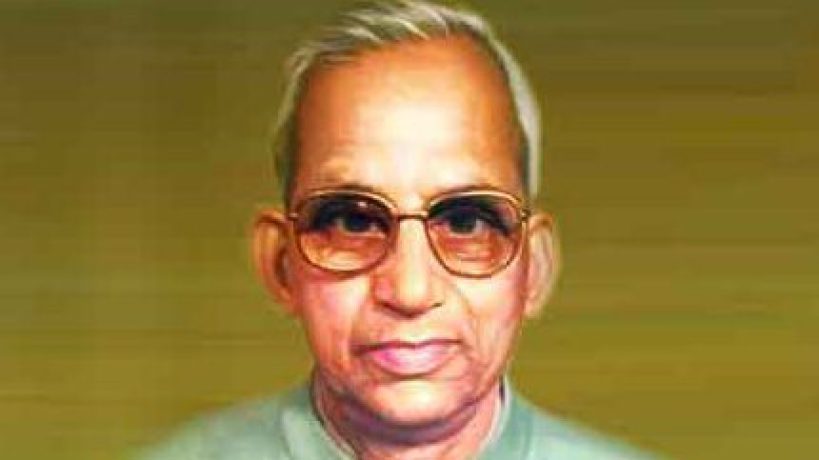 Written By- दयानाथ निगम
देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश ने कई नायकों को जन्म दिया। यही वह प्रदेश है, जहां से पिछड़े समाज को जगाने वाले नायक बड़ी संख्या में निकले। राम स्वरूप वर्मा का नाम उसमें प्रमुखता से शामिल है। यूपी के कानपुर देहात के गौरी करन गाँव में 22 अगस्त 1923 को एक साधारण कुर्मी किसान परिवार में रामस्वरूप वर्मा का जन्म हुआ। माता पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उच्च शिक्षा ग्रहण करे, सो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम०ए॰ और आगरा विश्विद्यालय से एल॰एल॰बी॰ की डिग्री प्राप्त की। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत के कारण शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हो रहा था जिसका लाभ माननीय रामस्वरूप वर्मा को मिला। रामस्वरूप वर्मा की जयंती और परिनिर्वाण की तारीख चार दिनों के भीतर ही आती है। उनकी जयंती 22 अगस्त को होती है, जबकि परिनिर्वाण दिवस 19 अगस्त को होता है। इस नाते यह हफ्ता रामस्वरूप वर्मा जी के नाम होता है।
Written By- दयानाथ निगम
देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश ने कई नायकों को जन्म दिया। यही वह प्रदेश है, जहां से पिछड़े समाज को जगाने वाले नायक बड़ी संख्या में निकले। राम स्वरूप वर्मा का नाम उसमें प्रमुखता से शामिल है। यूपी के कानपुर देहात के गौरी करन गाँव में 22 अगस्त 1923 को एक साधारण कुर्मी किसान परिवार में रामस्वरूप वर्मा का जन्म हुआ। माता पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उच्च शिक्षा ग्रहण करे, सो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम०ए॰ और आगरा विश्विद्यालय से एल॰एल॰बी॰ की डिग्री प्राप्त की। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत के कारण शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हो रहा था जिसका लाभ माननीय रामस्वरूप वर्मा को मिला। रामस्वरूप वर्मा की जयंती और परिनिर्वाण की तारीख चार दिनों के भीतर ही आती है। उनकी जयंती 22 अगस्त को होती है, जबकि परिनिर्वाण दिवस 19 अगस्त को होता है। इस नाते यह हफ्ता रामस्वरूप वर्मा जी के नाम होता है।
पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने तीन विकल्प थे। पहला विकल्प प्रशासनिक सेवा में जाना, दूसरा वकालत करना तथा तीसरा विकल्प था राजनीति के द्वारा मूलनिवासी बहुजनों व देश की सेवा करना। वर्मा जी ने आई॰ए॰एस॰ की लिखित परीक्षा भी उर्त्तीण कर ली थी किन्तु साक्षात्कार के पूर्व ही वे निर्णय ले चुके थे कि प्रशासनिक सेवा में रहकर वे ऐशो आराम की जिन्दगी तो व्यतीत कर सकते हैं पर मूलनिवासी बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते।
मा॰ रामस्वरूप वर्मा में राजनैतिक चेतना का प्रार्दुभाव डॉ॰ अम्बेडकर के उस भाषण से हुआ, जिसे उन्होंने मद्रास के पार्क टाउन मैदान में 1944 में शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था, ‘तुम अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें कल इस देश का शासक जमात बनना है जिसे आते जाते समय तुम्हें हमेशा याद रहे।’
माननीय रामस्वरूप वर्मा पर डॉ॰ अम्बेडकर के उस भाषण का भी बहुत ही प्रभाव पड़ा जिसे उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को बेगम हजरत महल पार्क में दिया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था, ‘जिस दिन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक मंच पर होंगे उस दिन वे सरदार बल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहर लाल नेहरू का स्थान ग्रहण कर सकते हैं।’ यही वजह रही कि एस॰सी॰, एस॰टी॰ एवं ओ॰बी॰सी॰ के बीच सामाजिक चेतना और जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने 1 जून 1968 को सामाजिक संगठन ‘अर्जक संघ’ की स्थापना की।
 मेरे लिये महामना रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लेना अक्सर भावुक कर जाता है। आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भी पहचान बनी है, उसका श्रेय महामना रामस्वरूप वर्मा जी को ही जाता है. मेरे सामाजिक जीवन के प्रारम्भ का किस्सा भी शानदार है। मुझे वर्मा जी द्वारा संपादित साप्ताहिक वैचारिक पत्र ‘‘अर्जक’’ एक गाँव में गोबर (खाद) के गढ्ढे में दिखा। मैंने उसे उठाया और किसी तरह से उसमें मिट्टी गोबर को साफ कर लेकर चल दिया। उसको पढ़ने के बाद सम्पादक/प्रकाशक का ढूंढ़ा तो लिखा था- रामस्वरूप वर्मा, बंगला नं. 3, दारूल सफा, लखनऊ। सामाचार पत्र पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आया कि अर्जक के सम्पादक/प्रकाशक से मिलना चाहिए। तब तक मैं कभी लखनऊ नहीं आया था। लेकिन वर्मा जी से मिलने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को रोक न पाया।
अपने गांव तमकुहीराज जो उस समय देवरिया जनपद के अंतर्गत (अब कुशीनगर) आता था, से लखनऊ जंक्शन के लिये 13 रूपये का टिकट लेकर निकल पड़ा। वह 1972 का साल था। बंगला नं. 3 दारूल सफा, जो कि वर्मा जी का निवास था, वहाँ पहुंच कर अपना परिचय दिया। जिला-जवार के बारे में बताया। वर्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो शरीर बुखार से तप रहा था। मेरी हालत देख वर्माजी ने मुझे अपने बिस्तर पर ही सोने के लिये कहा। मेरे कपड़े बेहद गन्दे थे और उनका बिस्तक एकदम साथ, ऐसे में मैं उस पर सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वर्माजी बार-बार मुझे बिस्तर पर सोने के लिये निर्देशित करते रहे। उनके दबाव के बाद मैं बिस्तर पर लेट तो गया परन्तु हमारी हिम्मत हार रही थी। इस बीच दो घण्टे के बाद वर्मा जी द्वारा प्रदत्त होमियो दवा के चलते मैं बुखार से मुक्त हो गया था। इस तरह मैं इस महान हस्ती के संपर्क में आया और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन अर्जक संघ से जुड़ गया। मुझे अर्जक संघ जनपद देवरिया का जिला मंत्री का कार्यभार मिल गया। उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया।
महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिये तमाम विचार प्रदान किये हैं। कुछ यूं है-
‘‘जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इन्सान नही’’
‘‘मानववाद की क्या पहचान ब्राह्मण-भंगी एक समान’’
मेरे लिये महामना रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लेना अक्सर भावुक कर जाता है। आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भी पहचान बनी है, उसका श्रेय महामना रामस्वरूप वर्मा जी को ही जाता है. मेरे सामाजिक जीवन के प्रारम्भ का किस्सा भी शानदार है। मुझे वर्मा जी द्वारा संपादित साप्ताहिक वैचारिक पत्र ‘‘अर्जक’’ एक गाँव में गोबर (खाद) के गढ्ढे में दिखा। मैंने उसे उठाया और किसी तरह से उसमें मिट्टी गोबर को साफ कर लेकर चल दिया। उसको पढ़ने के बाद सम्पादक/प्रकाशक का ढूंढ़ा तो लिखा था- रामस्वरूप वर्मा, बंगला नं. 3, दारूल सफा, लखनऊ। सामाचार पत्र पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आया कि अर्जक के सम्पादक/प्रकाशक से मिलना चाहिए। तब तक मैं कभी लखनऊ नहीं आया था। लेकिन वर्मा जी से मिलने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को रोक न पाया।
अपने गांव तमकुहीराज जो उस समय देवरिया जनपद के अंतर्गत (अब कुशीनगर) आता था, से लखनऊ जंक्शन के लिये 13 रूपये का टिकट लेकर निकल पड़ा। वह 1972 का साल था। बंगला नं. 3 दारूल सफा, जो कि वर्मा जी का निवास था, वहाँ पहुंच कर अपना परिचय दिया। जिला-जवार के बारे में बताया। वर्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो शरीर बुखार से तप रहा था। मेरी हालत देख वर्माजी ने मुझे अपने बिस्तर पर ही सोने के लिये कहा। मेरे कपड़े बेहद गन्दे थे और उनका बिस्तक एकदम साथ, ऐसे में मैं उस पर सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वर्माजी बार-बार मुझे बिस्तर पर सोने के लिये निर्देशित करते रहे। उनके दबाव के बाद मैं बिस्तर पर लेट तो गया परन्तु हमारी हिम्मत हार रही थी। इस बीच दो घण्टे के बाद वर्मा जी द्वारा प्रदत्त होमियो दवा के चलते मैं बुखार से मुक्त हो गया था। इस तरह मैं इस महान हस्ती के संपर्क में आया और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन अर्जक संघ से जुड़ गया। मुझे अर्जक संघ जनपद देवरिया का जिला मंत्री का कार्यभार मिल गया। उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया।
महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिये तमाम विचार प्रदान किये हैं। कुछ यूं है-
‘‘जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इन्सान नही’’
‘‘मानववाद की क्या पहचान ब्राह्मण-भंगी एक समान’’
इस तरह के नारे देकर उन्होंने समाज में ज्योति जलाई। महामना वर्मा जी ने वैचारिक क्रांति के लिये वैचारिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसमें क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे? ‘‘मानवतावाद बनाम ब्राह्मणवाद’’, ‘‘मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक’’ आदि पुस्तकें शामिल हैं। माननीय रामस्वरूप वर्मा सम्पूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। उनकी सम्पूर्ण क्रांति में भ्रांति का कोई स्थान नहीं था। वर्मा जी के अनुसार, जीवन के चार क्षेत्र होते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। उनका मानना था कि इन चारों क्षेत्रों में गैरबराबरी समाप्त करके ही हम सच्ची और वास्तविक क्रान्ति निरूपित कर सकते हैं। रामस्वरूप वर्मा निःसन्देह डॉ॰ राम मनोहर लोहिया के राजनैतिक दल संसोपा से जुड़े थे, किन्तु लोहिया जी के साथ वर्मा जी का वैचारिक मतभेद था। लोहिया गान्धीवादी थे, वर्मा जी अम्बेडकरवादी। लोहिया के आर्दश मर्यादा पुरूषोत्तम राम और मोहन दास करमचन्द गांधी थे, जबकि रामस्वरूप वर्मा के आदर्श भगवान बुद्ध, फूले, अम्बेडकर और पेरियार थे।
 रामस्वरूप वर्मा संसोपा से सन् 1957 में कानपुर के रामपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधान सभा के सदस्य चुने गये। इसके बाद 1967, 1969,1980,1989, और 1991 में सदस्य विधान सभा के चुनाव में विजयी रहे। माननीय वर्मा जी के तर्क के सामने विधान सभा में शासक जातियों की घिग्घी बंध जाती थी। सन 1967 की संबिदा सरकार में वर्मा जी डॉ॰ लोहिया की पार्टी संसोपा से जीतकर उ॰प्र॰ विधान सभा में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के मन्त्रीमण्डल के वह वित्त मन्त्री बनाये गये, जहां उन्होंने मुनाफे का बजट पेश किया। वर्मा जी ने उ॰प्र॰ विधानसभा में सभी धार्मिक स्थलों को सरकार के अधीन करने का बिल पेश किया। सवर्णों ने बिल का विरोध किया कि ऐसा करने से साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा,
“इस बिल में तो यह है कि जितने पूजा स्थल हैं उनको सरकार अपने नियन्त्रण में ले और हर पूजा स्थल पर जो चढ़ावा चढ़ेगा वह सरकार को मिलेगा। पुजारी रखने के बाद जो बचता है वह धर्म हित कार्यों में खर्च किया जाये। इसमें साम्प्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं हैं।”
रामस्वरूप वर्मा के तर्क सुनकर उनके विरोधी भी बंगले झांकने लगते थे। इतना ही नहीं वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैरसरकारी पुस्तकालयों में बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर का साहित्य रखवाया, जिसके कारण मूलनिवासी बहुजनों में स्वाभिमान जागने लगा। तत्पश्चात शासक जातियों ने बाबासाहब द्वारा लिखित- ‘जातिभेद का उच्छेद’ और ‘धर्म परिवर्तन करें’ दोनों पुस्तकों को जप्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों पुस्तकों को बहाल करवाया। इतना ही नहीं उन्होंने उ॰प्र॰ सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उ॰प्र॰ सरकार से पूरे मुकदमे का हर्जाना और खर्चा भी वसूल किया।
उनसे जुड़ा एक संस्मरण मुझे अक्सर भावुक बना देता है। लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित किया गया था। उस बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसी दौरान मैं पिता बनने वाला था और मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। बैठक में अनुपस्थिति के कारण मेरे बारे में महामना वर्मा जी ने जानना चाहा तब मैंने उन्हें बच्चे की बता बताई। मा. वर्मा जी ने यह सुनते ही तत्काल कहा “क्रांति पैदा हो गया.” इस तरह मेरे प्रथम पुत्र का नाम क्रांति कुमार, मा. वर्मा जी का दिया हुआ नाम है।
रामस्वरूप वर्मा संसोपा से सन् 1957 में कानपुर के रामपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधान सभा के सदस्य चुने गये। इसके बाद 1967, 1969,1980,1989, और 1991 में सदस्य विधान सभा के चुनाव में विजयी रहे। माननीय वर्मा जी के तर्क के सामने विधान सभा में शासक जातियों की घिग्घी बंध जाती थी। सन 1967 की संबिदा सरकार में वर्मा जी डॉ॰ लोहिया की पार्टी संसोपा से जीतकर उ॰प्र॰ विधान सभा में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के मन्त्रीमण्डल के वह वित्त मन्त्री बनाये गये, जहां उन्होंने मुनाफे का बजट पेश किया। वर्मा जी ने उ॰प्र॰ विधानसभा में सभी धार्मिक स्थलों को सरकार के अधीन करने का बिल पेश किया। सवर्णों ने बिल का विरोध किया कि ऐसा करने से साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा,
“इस बिल में तो यह है कि जितने पूजा स्थल हैं उनको सरकार अपने नियन्त्रण में ले और हर पूजा स्थल पर जो चढ़ावा चढ़ेगा वह सरकार को मिलेगा। पुजारी रखने के बाद जो बचता है वह धर्म हित कार्यों में खर्च किया जाये। इसमें साम्प्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं हैं।”
रामस्वरूप वर्मा के तर्क सुनकर उनके विरोधी भी बंगले झांकने लगते थे। इतना ही नहीं वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैरसरकारी पुस्तकालयों में बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर का साहित्य रखवाया, जिसके कारण मूलनिवासी बहुजनों में स्वाभिमान जागने लगा। तत्पश्चात शासक जातियों ने बाबासाहब द्वारा लिखित- ‘जातिभेद का उच्छेद’ और ‘धर्म परिवर्तन करें’ दोनों पुस्तकों को जप्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों पुस्तकों को बहाल करवाया। इतना ही नहीं उन्होंने उ॰प्र॰ सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उ॰प्र॰ सरकार से पूरे मुकदमे का हर्जाना और खर्चा भी वसूल किया।
उनसे जुड़ा एक संस्मरण मुझे अक्सर भावुक बना देता है। लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित किया गया था। उस बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसी दौरान मैं पिता बनने वाला था और मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। बैठक में अनुपस्थिति के कारण मेरे बारे में महामना वर्मा जी ने जानना चाहा तब मैंने उन्हें बच्चे की बता बताई। मा. वर्मा जी ने यह सुनते ही तत्काल कहा “क्रांति पैदा हो गया.” इस तरह मेरे प्रथम पुत्र का नाम क्रांति कुमार, मा. वर्मा जी का दिया हुआ नाम है।
 महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर के विचारों को प्रसारित करने का महान योगदान है ‘‘विचारों पर ताला और मूर्तियों पर माला’’ की चर्चा करते हुये बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक ले जाने का प्रयास किया। वर्मा जी ने नारा दिया था, ‘मारेंगे मर जायेंगे हिन्दू नहीं कहलायेंगे।’ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में रामस्वरूप वर्मा आजीवन संघर्ष करते रहे। लोहिया से वैचारिक मतभेद के कारण बाद के दिनों में उन्होंने संसोपा से अलविदा कर मूलनिवासी बहुजन समाज के शुभ चिन्तकों चौ॰ महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद, प्रो॰ जयराम प्रसाद सिंह, लक्ष्मण चौधरी, नन्द किशोर सिंह से सम्पर्क कर 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल की स्थापना की और नारा दिया-
”देश का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
सौ में नब्बे शोषित हैं नब्बे भाग हमारा है।“
शोषितों का राज, शोषितों के लिए शोषितों के द्वारा होगा।
महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर के विचारों को प्रसारित करने का महान योगदान है ‘‘विचारों पर ताला और मूर्तियों पर माला’’ की चर्चा करते हुये बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक ले जाने का प्रयास किया। वर्मा जी ने नारा दिया था, ‘मारेंगे मर जायेंगे हिन्दू नहीं कहलायेंगे।’ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में रामस्वरूप वर्मा आजीवन संघर्ष करते रहे। लोहिया से वैचारिक मतभेद के कारण बाद के दिनों में उन्होंने संसोपा से अलविदा कर मूलनिवासी बहुजन समाज के शुभ चिन्तकों चौ॰ महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद, प्रो॰ जयराम प्रसाद सिंह, लक्ष्मण चौधरी, नन्द किशोर सिंह से सम्पर्क कर 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल की स्थापना की और नारा दिया-
”देश का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
सौ में नब्बे शोषित हैं नब्बे भाग हमारा है।“
शोषितों का राज, शोषितों के लिए शोषितों के द्वारा होगा।
Video- मनुवाद को धूल चटाने वाले नायक थे रामस्वरूप वर्मा
मा॰ रामस्वरूप वर्मा का मानना था सामाजिक चेतना से ही सामाजिक परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनैतिक परिवर्तन सम्भव नहीं। अगर येन केन प्रकारेण राजनैतिक परिवर्तन हो भी गया तो वह ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं होगा। रामस्वरूप वर्मा सामाजिक सुधार के पक्षधर नहीं थे। वे सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। वे हमेशा समझाया करते थे जिस प्रकार दूध से भरे टब में यदि पोटेशियम साइनाइट का टुकड़ा पड़ जाये तो उस टुकड़े को दूध के टब से निकालने के बाद भी दूध का प्रयोग करना जानलेवा होगा। इसलिए ब्राह्मणवादी मूल्यों में सुधार की कोई गुंजाइश नही हैं। ब्राह्मणवाद सुधारा नहीं जा सकता बल्कि नकारा ही जा सकता है। माननीय रामस्वरूप वर्मा ने कभी भी सिद्धांतो से समझौता नहीं किया। रामस्वरूप वर्मा ने बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर की तरह 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म तो स्वीकार नहीं किया लेकिन उन्होंने विवाह संस्कार, यशाकायी दिवस, त्यौहार आदि को लेकर समाज में अपनी अर्जक पद्धति विकसित की। जैसे एक जून अर्जक संघ स्थापना दिवस को समता दिवस, बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल को चेतना दिवस, तथागत बुद्ध जयंती को मानवता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पूरे देश में जहां-जहां अर्जक संघ के कार्यकर्ता हैं वे बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर के जन्मदिन के दिन मूलनिवासी बहुजनों को जगाने के लिए 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे महीने रामायण और मनुस्मृति का दहन करें। अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप वर्मा के आदेशों का पालन करते हुए रामायण और मनुस्मृति को घोषणा के साथ जलाया। उन्होंने वैवाहिक संस्कार की भी पद्धति बनाकर अपनी संस्कृति स्थापित की। उन्होंने ताउम्र अपने सिद्धांतों की राजनीति की। 19 अगस्त 1998 को उनका परिनिर्वाण हो गया।- लेखक दयानाथ निगम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से प्रकाशित “अम्बेडकर इन इंडिया” मासिक पत्रिका के संपादक हैं। संपर्क- 9450469420
दलित उत्पीड़न और सवर्ण जातियों की चुप्पी
 – Written By- सुरेश कुमार
इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवर्णों की प्रताड़ना का बिंदु दलित समाज है। यह उच्च श्रेणी की मानसिकता वाला समाज दलितों पर अन्याय और जुल्म करने के मामले में इतिहास के पन्ने काले से काले करते आया है। अभी पिछले दिनों आगरा के अछनेरा तहसील के रायभा गांव में जिस तरह से एक दलित महिला के शव को उच्च जाति के सवर्णों ने श्मशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, उस से पता चलता है कि देश में जातिवाद की जड़े कितनी गहरी और अंदर तक धंसी हुई है। इस तरह की घटनाओं और सवर्णों का जातिगत भेदभाव दलितों को मनुकाल में ले जाकर धकेल देता हैं। उच्च श्रेणी के सवर्णों द्वारा दलितों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि इस देश में तुम्हारे लिये कोई जगह नहीं है। यहां तक दलितों लिये मरने के बाद दो गज जमीन उनकी नहीं है। कमाल की बात यह है कि संविधान और लोकतंत्रवादी व्यवस्था के भीतर भी सवर्णों का जातीय दंभ और उच्च श्रेणी की मानसिकता कमजोर होने के बजाय बलवती होती जा रही है।
दलितों को अपमानित करने वाली घटनायें समाज के सभी हलको में दिन प्रतिदिन घटती रहती है। अभी हाल में ही कानपुर देहात के मगतापुर गांव में दलित समाज के लोग सनातन कथा कराने के बजाय बौद्ध या भीम कथा करवा रहे थे। यह बात गांव के उच्च श्रेणी के लोगों को इतनी नगवार लगी कि उन्होंने पूरे गांव के दलितों की जमकर पिटाई कर दी थी। उच्च श्रेणी की मानसिकता और सामंती ठसक दलितों के संस्कृति क्षेत्र को भी नियंत्रण करने का उपक्रम करती आई है। बौद्ध कथा या बाबासाहब की कथा कराने से सवर्णों को लगता है की उनके वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है। और, उनके नायकों और प्रतिमानों के समक्ष दलित अपने नायक या प्रमिमान क्यों स्थापित कर रहें है? दलित के नायक और प्रमिमान स्थापित न हो जाये इसलिए उनके संस्कृतिक क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिस की जाती रही है। उच्च श्रेणी की मानसिकता और दंभ दलितों को मनुकाल की याद दिलाये रखने के लिये उनकों प्रताड़ित और अपमानित करने का उपक्रम करता रहता है।
– Written By- सुरेश कुमार
इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवर्णों की प्रताड़ना का बिंदु दलित समाज है। यह उच्च श्रेणी की मानसिकता वाला समाज दलितों पर अन्याय और जुल्म करने के मामले में इतिहास के पन्ने काले से काले करते आया है। अभी पिछले दिनों आगरा के अछनेरा तहसील के रायभा गांव में जिस तरह से एक दलित महिला के शव को उच्च जाति के सवर्णों ने श्मशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, उस से पता चलता है कि देश में जातिवाद की जड़े कितनी गहरी और अंदर तक धंसी हुई है। इस तरह की घटनाओं और सवर्णों का जातिगत भेदभाव दलितों को मनुकाल में ले जाकर धकेल देता हैं। उच्च श्रेणी के सवर्णों द्वारा दलितों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि इस देश में तुम्हारे लिये कोई जगह नहीं है। यहां तक दलितों लिये मरने के बाद दो गज जमीन उनकी नहीं है। कमाल की बात यह है कि संविधान और लोकतंत्रवादी व्यवस्था के भीतर भी सवर्णों का जातीय दंभ और उच्च श्रेणी की मानसिकता कमजोर होने के बजाय बलवती होती जा रही है।
दलितों को अपमानित करने वाली घटनायें समाज के सभी हलको में दिन प्रतिदिन घटती रहती है। अभी हाल में ही कानपुर देहात के मगतापुर गांव में दलित समाज के लोग सनातन कथा कराने के बजाय बौद्ध या भीम कथा करवा रहे थे। यह बात गांव के उच्च श्रेणी के लोगों को इतनी नगवार लगी कि उन्होंने पूरे गांव के दलितों की जमकर पिटाई कर दी थी। उच्च श्रेणी की मानसिकता और सामंती ठसक दलितों के संस्कृति क्षेत्र को भी नियंत्रण करने का उपक्रम करती आई है। बौद्ध कथा या बाबासाहब की कथा कराने से सवर्णों को लगता है की उनके वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है। और, उनके नायकों और प्रतिमानों के समक्ष दलित अपने नायक या प्रमिमान क्यों स्थापित कर रहें है? दलित के नायक और प्रमिमान स्थापित न हो जाये इसलिए उनके संस्कृतिक क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिस की जाती रही है। उच्च श्रेणी की मानसिकता और दंभ दलितों को मनुकाल की याद दिलाये रखने के लिये उनकों प्रताड़ित और अपमानित करने का उपक्रम करता रहता है।

बाबासाहब डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि दलित की कोई मातृभूमि नहीं है। इस कथन के पीछे उनकी गहरी चिंता और पीड़ा महसूस की जा सकती है। बाबासाहब के कहने का अर्थ था कि इस देश में दलितों का कुछ नहीं है। यहां के सवर्ण दलितों को देश का नागरिक नहीं बल्कि गुलाम और अछूत के सिवा कुछ नहीं समझते है। दलित न तो सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग कर सकते थे, और न तो मन्दिर जा सकते, और न ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। बाबासाहब ने यह भले यह बात बीसवीं सदी के तीसरे दशक में कही हो लेकिन सच्चाई यह है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी सवर्णों की मानसिकता में ज्याद बदलाव नहीं हुआ है। 21वीं सदी में भी दलितों के साथ वैसा ही सलूक देखने को मिल रहा है जैसा उनके साथ मनुकाल में होता था। आज भी सवर्ण मानसिकता के लोग दलितों के साथ बड़ी क्रूरता और निर्ममता से पेश आते हैं। यह कटु सच्चाई है कि दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार देखकर सवर्ण मानसिकता से भरे लोगों को खून खौल जाता है। सवर्णवादी संरचना दलितों को अछूत और बंधुवा गुलाम के तौर देखने की अभ्यस्त रही है। वर्णगत और सवर्णवादी व्यवस्था की ओर से तय की गयी परिभाषा पर जो दलित नहीं चलता है, उसको सवर्णों के द्वारा सबक सिखा दिया जाता है। दलितों के लिये इस से बड़ी त्रासदी और पीड़ा क्या हो सकती है कि वे जिस मिट्टी में पैदा हुये, जिसके लिये अपना खून पसीना एक कर दिया हो, और, मारने के बाद सवर्णों के द्वारा उनके शव को चिता से उठवा दिया जाये। डॉ. आंबेडकर की चिंता थीं कि हिन्दुओं के शासन में दलितों को प्रताड़ित और अपमानित किया जायेगा। आज बाबासाहब की बात शत प्रतिशत सही साबित हुई है। जहां जातिगत और वर्णगत व्यवस्था का ढांचा सवर्णों को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाता है, वहीं दलित और स्त्रियों को सम्मान और अधिकारों से वंचित करने का काम भी करता है। देखा जाय तो जातिगत संरचना दलितों और स्त्रियों के लिये मरण-व्यवस्था की तरह है। इसकी संरचना जहां दलितों के अधिकारों का दायरा सीमित कर देती है वहीं उच्च श्रेणी के हिंदुओं को विशेष अधिकारों का समर्थन करती है। वर्ण-व्यवस्था की संरचना दलितों को संसाधनों से भी वंचित कर देती है। संसाधनों से वंचित हो जाने पर दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की कमर टूट गई है। जमीन से लेकर संस्थाओं तक के सारे संसधानों पर सवर्णों का कब्जा है। दलित के पास जमा पूंजी के नाम पर भूख और सवर्णों की प्रताड़ना के सिवा और क्या है? भूमि विहीन दलित आखिर अपने मृत शरीर को कहां दफन करें। यदि दलितों के प्रति सवर्णों का रवैया नहीं बदल रहा है, और वे दलितों के शव को अपने शमशान में जलाने नहीं दे रहें है, तो सरकार बहादुर को दलितों के लिये अलग से श्मशान भूमि के आवंटन की ओर ध्यान देना चाहिये।

भारतीय समाज का सवर्ण तबका जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और रुढ़ियों का पोषक और रक्षक रहा है। यह समाज शास्त्रों और पुरोहितों के दिशा निर्देश में संचालित होता आ रहा है। पुरोहित और पोथाधारी शास्त्रों और स्मृतियों का हवाला देकर दलित विरोधी वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सवर्ण समाज का पढ़ा लिखा तपका भी जाति के जामे को पहना ओढ़ना और बिछना अब तक नहीं छोड़ सका है। संविधान और ज्ञान-विज्ञान की छत्रछाया में भी सवर्ण समाज जातिवाद और भेदभाव की संस्कृति का त्याग नहीं कर सका है। 21वीं सदी में भी दलितों के साथ यह समाज वैसे ही पेश आता है, जैसे मनुकाल में दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था। दलितों के प्रति घृणा का भाव चेतन और अवचेतन के स्तर पर हावी रहता है; जिसके फलस्वरुप दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। सवर्णों का श्रेष्ठता का भाव ही दलितों की गरिमा को लांक्षित और अपमानित करने का काम करता है। संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था किसी भी व्यक्ति और समाज को यह अधिकार नहीं देता है कि वह किसी मनुष्य के साथ भेदभाव और उसकी गरिमा को लांक्षित और अपमानित करने का उपक्रम करे। हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्चस्व रहा है। इनके वर्चस्व ने दलितों और स्त्रियों के साथ घोर सामाजिक अन्याय किया है। उच्च श्रेणी के लोगों की संवेदनायें दलितों के साथ नहीं बल्कि वर्णवादियों के साथ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने जातिगत वर्चस्व को कायम रखने के लिये दलितों के साथ बड़ी निर्ममता और संवेदनहीनता से पेश आते रहे हैं। जातिवादी वर्चस्व ने दलित शोषण और प्रताड़ना की एक अंतहीन जमीन तैयार की है। वर्णवादी शाक्तियां समाज का वातावरण दलितों के अनुकूल नहीं होने देती है।

सवर्णवादी मानसिकता के लोग संविधानवादी व्यवस्था को ताक पर रखकर दलितों को मनुकाल की याद तरोताजा कराने का कोई अवसर नहीं छोड़ते है। वर्णवादी लोग समता और सामाजिक न्याय की सदा धज्जिया उड़ाते आयें है। दलितों पर अत्याचार करने में संवदेनहीनता की सारे हदे पार कर जाते हैं। श्मशान भूमि से दलित स्त्री का शव चिता से उठवा देना, यह सवर्णवाद और सामन्ती ठसक की संवेदनहीनता की पराकष्ठा का उत्कर्ष नहीं तो और क्या है? सवर्णवादी मानसिकता दलितों और पिछड़ों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में सदैव अवरोध पैदा करती रही है। इसी मानसिकता के पक्षधर और समर्थकों ने दलितों को बुनियादी हकों से वंचित करने का काम किया है। यह तय है कि वर्णगत और जातिगत जुगलबंदी जब तक कायम है, तब तक दलितों को अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती है। दलितों के सर्वजानिक क्षेत्र के विकास के लिये जातिवाद और वर्णवाद का खात्मा होना निहायत ही जरुरी है। समाज के नियंताओं और बुद्धिजीवियों को वर्णगत और जातिगत संरचना के खि़लाफ विमर्श का माहौल तैयार करना होगा। सबसे पहले सवर्णो को जातीय दंभ और सामन्ती ठसक के खोल से मुक्त करना होगा। जब तक सवर्ण समाज के लोग अपने भीतर बैठे जातिवाद के दानव को नहीं खत्म करेगें, तब तक समाज के भीतर बदलाव की लहर नहीं आ सकती है। क्योंकि सवर्णवादी मानसिकता ही दलितों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में सर्वाधिक बाधा को तौर पर उपस्थिति होती है। सवर्ण समाज को अमेरिका के रंगभेद आंदोलन से सीख लेनी चाहिये। यदि वहां कोई स्वेत अस्वेतों के साथ भेदभाव करता है तो सबसे पहले मुखर विरोध स्वेतों की ओर से होता है। लेकिन भारत में दलितों के साथ जो अत्याचार और जुल्म होता उसको लेकर सवर्ण समाज के अधिकांश बु़द्धिजीवि चुप्पी साध लेते हैं। सवर्ण समाज के बुद्धिजीवियों को जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों के प्रति ‘गैर-आलोचनात्मक’ नहीं होना है। उन्हें दलित समाज पर अत्याचार और जुर्म करने वालों अपने स्वजातीय लोगों की सर्वजानिक तौर पर भर्स्ाना करने की पहल शुरु करनी होगी। सवर्ण बुद्धिजीवियों को जाति विरोधी गोलबंदी में दलितों का साथ देना होगा। मिल जुलकर दलित दलित शोषण के विरुद्ध विमर्श का माहौल तैयार करना होगा, तभी समाज समतावादी व्यवस्था कायम होगी।
लेखक सुरेश कुमार स्वतंत्र रूप से नियमित लेखन करते हैं। संपर्क- 8009824098
“सुप्रीम कोर्ट 2014 से ही संघ के आंगन में नाच रहा है”
 Written By- डॉ. सिद्धार्थ
Written By- डॉ. सिद्धार्थबहुजन शोधार्थियों के लिए बना मंच, पीएचडी में मदद करेंगे बहुजन विद्वान
 मेरी एक मित्र मुंबई मे रहती हैं। लॉकडाउन से ठीक एक हफ्ता पहले एक लड़की ने उन्हे महाराष्ट्र के किसी गाँव से फोन किया। वह लड़की लगभग रोते हुए उनसे बोली कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और बहुत परेशान हूँ। उसके पीएचडी गाइड ने बीते तीन सालों मे ना तो उसका प्रपोजल पढ़ा न पढ़ने के लिए कोई किताब या पेपर सजेस्ट किया ना ही मीटिंग के लिए टाइम दिया है। वह लड़की एक छोटे से गाँव से आती है, उसके माता पिता दूसरों के खेत पर मजदूरी करते हैं उसके सरनेम से ही पता चलता है कि वह तथाकथित नीचली जाति से आते है। गाइड महोदय इस बेचारी को तीन साल से टाल रहे हैं। अपने थीसिस चैप्टर के ड्राफ्ट लेकर उनके आगे पीछे डोलती रहती है लेकिन ‘महामहिम’ को देखने तक की फुरसत नहीं है।
यह लड़की आत्महत्या के विचारों से घिर गयी, बहुत उदास रहने लगी और फेसबुक पर उखड़ी-उखड़ी पोस्ट लिखने लगी। मेरी मित्र ने इस लड़की को हिम्मत बंधाई और आगे का रास्ता समझाया। यह लड़की ज्योतिबा फूले के विचारों पर पीएचडी कर रही है इसके गाइड महोदय ने अपने जमाने मे राजा राममोहन रॉय पर पीएचडी की है और वे ज्योतिबा या अंबेडकर को नहीं पढ़ना चाहते। रिसर्च कमेटी और पीएचडी गाइड समझाते रहे कि राममोहन रॉय पर शोध करो, लेकिन लड़की अड़ी रही। लेकिन अपने इस निर्णय का परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है।
Video- विदेशों में पढ़ाई और नौकरी कैसे हासिल करें, देखे यह वीडियो
मेरी मित्र ने इस लड़की को मेरा फोन नंबर दिया, वह जानती है कि मैंने ज्योतिबा पर किताब लिखी है। कुछ समय पहले इस लड़की ने मुझे फोन किया। उसकी बातें सुनकर लगा कि अगर इसके रिसर्च गाइड इसे सिर्फ आधा घंटा समय दे दें और सहानुभूति से इसकी बातें सुन लें तो ना सिर्फ यह अवसाद और आत्महत्या के विचारों से बाहर निकल जाएगी बल्कि उसकी पीएचडी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन गाइड को ना फुरसत है ना ही रुचि है।
बीते दस सालों मे मैंने ऐसी सैकड़ों कहानियाँ सुनीं है, पता चलता है कि न केवल छात्रों की उपेक्षा की जाती है बल्कि लड़कियों का शारीरिक शोषण भी पीएचडी गाइड द्वारा किया जाता है। लड़कों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके घर की साफ सफाई तक करवाई जाती है। ऐसी हालत मे ना केवल गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं बल्कि कई तो आत्महत्या के विचारों और अवसाद मे भी फस जाते हैं।
इस विषय मे मैंने कुछ अकादमिक मित्रों से बात की है, सभी मित्र यह महसूस करते हैं कि बहुजन बच्चों को तानाशाह और शोषक गाइड्स की तानाशाही से बचाने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक अलग से मंच बनाया जाए जहां कुछ मित्र इकट्ठे होकर सभी बच्चों की समस्याओं पर विचार किया जा सके। इसीलिए हम नालंदा पीएचडी कंसल्टेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके जरिए छात्रों को उनके विषय और पीएचडी की प्रक्रिया सहित विश्लेषण, लेखन, प्रकाशन आदि से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी।
यह मंच एक तरह से खुली चर्चा का मंच होगा जहां अनुभवी छात्र या शिक्षक नए लोगों से संवाद कर सकेंगे और जरूरी सलाह ले-दे सकेंगे।
इस बेहतरीन मंच के फेसबुक पेज को देखने के लिए आप इस लिंक पर जाएं- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/
संपर्क के लिए यह लिंक देखें- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/about/?ref=page_internal
मेरी एक मित्र मुंबई मे रहती हैं। लॉकडाउन से ठीक एक हफ्ता पहले एक लड़की ने उन्हे महाराष्ट्र के किसी गाँव से फोन किया। वह लड़की लगभग रोते हुए उनसे बोली कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और बहुत परेशान हूँ। उसके पीएचडी गाइड ने बीते तीन सालों मे ना तो उसका प्रपोजल पढ़ा न पढ़ने के लिए कोई किताब या पेपर सजेस्ट किया ना ही मीटिंग के लिए टाइम दिया है। वह लड़की एक छोटे से गाँव से आती है, उसके माता पिता दूसरों के खेत पर मजदूरी करते हैं उसके सरनेम से ही पता चलता है कि वह तथाकथित नीचली जाति से आते है। गाइड महोदय इस बेचारी को तीन साल से टाल रहे हैं। अपने थीसिस चैप्टर के ड्राफ्ट लेकर उनके आगे पीछे डोलती रहती है लेकिन ‘महामहिम’ को देखने तक की फुरसत नहीं है।
यह लड़की आत्महत्या के विचारों से घिर गयी, बहुत उदास रहने लगी और फेसबुक पर उखड़ी-उखड़ी पोस्ट लिखने लगी। मेरी मित्र ने इस लड़की को हिम्मत बंधाई और आगे का रास्ता समझाया। यह लड़की ज्योतिबा फूले के विचारों पर पीएचडी कर रही है इसके गाइड महोदय ने अपने जमाने मे राजा राममोहन रॉय पर पीएचडी की है और वे ज्योतिबा या अंबेडकर को नहीं पढ़ना चाहते। रिसर्च कमेटी और पीएचडी गाइड समझाते रहे कि राममोहन रॉय पर शोध करो, लेकिन लड़की अड़ी रही। लेकिन अपने इस निर्णय का परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है।
Video- विदेशों में पढ़ाई और नौकरी कैसे हासिल करें, देखे यह वीडियो
मेरी मित्र ने इस लड़की को मेरा फोन नंबर दिया, वह जानती है कि मैंने ज्योतिबा पर किताब लिखी है। कुछ समय पहले इस लड़की ने मुझे फोन किया। उसकी बातें सुनकर लगा कि अगर इसके रिसर्च गाइड इसे सिर्फ आधा घंटा समय दे दें और सहानुभूति से इसकी बातें सुन लें तो ना सिर्फ यह अवसाद और आत्महत्या के विचारों से बाहर निकल जाएगी बल्कि उसकी पीएचडी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन गाइड को ना फुरसत है ना ही रुचि है।
बीते दस सालों मे मैंने ऐसी सैकड़ों कहानियाँ सुनीं है, पता चलता है कि न केवल छात्रों की उपेक्षा की जाती है बल्कि लड़कियों का शारीरिक शोषण भी पीएचडी गाइड द्वारा किया जाता है। लड़कों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके घर की साफ सफाई तक करवाई जाती है। ऐसी हालत मे ना केवल गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं बल्कि कई तो आत्महत्या के विचारों और अवसाद मे भी फस जाते हैं।
इस विषय मे मैंने कुछ अकादमिक मित्रों से बात की है, सभी मित्र यह महसूस करते हैं कि बहुजन बच्चों को तानाशाह और शोषक गाइड्स की तानाशाही से बचाने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक अलग से मंच बनाया जाए जहां कुछ मित्र इकट्ठे होकर सभी बच्चों की समस्याओं पर विचार किया जा सके। इसीलिए हम नालंदा पीएचडी कंसल्टेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके जरिए छात्रों को उनके विषय और पीएचडी की प्रक्रिया सहित विश्लेषण, लेखन, प्रकाशन आदि से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी।
यह मंच एक तरह से खुली चर्चा का मंच होगा जहां अनुभवी छात्र या शिक्षक नए लोगों से संवाद कर सकेंगे और जरूरी सलाह ले-दे सकेंगे।
इस बेहतरीन मंच के फेसबुक पेज को देखने के लिए आप इस लिंक पर जाएं- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/
संपर्क के लिए यह लिंक देखें- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/about/?ref=page_internal राष्ट्र के रूप में भारत दलितों का कर्जदार है
 Written By- सूरज येंगड़े
आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछेक तरीकों में से एक थे। किन्तु ये बहुत ज़्यादा विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति का माध्यम सबसे व्यवहारिक तरीकों में से एक है।
एक राष्ट्र के रूप में भारत दलितों का कर्ज़दार है- जिनके कन्धों पर उसके सभ्यतागत स्तंभ खड़े किए गए हैं। दलित प्रतिभा, कौशल और आंतरिक-बल आदि भारत को अंग्रेजों सहित बाहरी लोगों के लिए सबसे वांछनीय स्थानों में से एक बनाता है। कला के विभिन्न स्वरुप, साहित्य, संगीत, कविता इत्यादि की उत्पत्ति दलित, आदिवासी और शूद्रों के जन-जीवन से हुई है। अपने आविष्कारशील प्रतिभा और प्रदर्शन के उत्साह में, दलितों ने अपनी त्रासदियों को एक लय में पिरोया है, तथा अस्पृश्यता की यातनाओं के बीच अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है। वे रोये हैं, और आग्रह किया, विरोध-प्रदर्शन किये और लड़ाई भी की है। इस सबके द्वारा उन्होंने संवेदी अनुभवों के नए स्वरूपों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
लगभग सभी “प्रतिष्ठित और शास्त्रीय” भारतीय कला के स्वरूपों का उद्गम दलितों के जन-जीवन में दिखता है। दलित कला की चोरी और उसके ब्रह्मणिकरण के बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। इसके बावजूद दलितों के दावों को रोकने के लिए, उन्हें विभिन्न कलाओं में भाग लेने और अभ्यास करने से रोक दिया गया। इसने दलित प्रतिभा की किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को समाप्त किया है। यही कारण है कि आज भी, कई उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित कलाओं में दलितों की भागीदारी नहीं है।
अन्य नयी खोजों में भी, दलितों ने विज्ञान को फलने-फूलने और तर्कवाद को तरजीह/प्रधानता हासिल करने में मदद की है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों और प्रार्थनाओं में, आत्मज्ञान के सार को सर्वशक्तिमान माना है। ऐसे में, हम दलित अस्मिता और अस्तित्व की हत्या करने की अपनी पिछली गलतियों को कैसे सुलझाएं ताकि भविष्य के लिए स्थिति को ठीक किया जा सके? इस सवाल का उत्तर, “जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता या किसी अन्य तरीके से सहयोग करके अपनी गलतियों को सुधार कर” भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति के बारे में सोचने का एक संभावित तरीका है। यह अतीत और आगे बढ़ने वाले अन्याय को ठीक करने का एक माध्यम है। भूल-सुधारों को तीन व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
नैतिक भूल-सुधार:- ज़ख़्मी दिलों और दिमागों के उपचार करने हेतु पिछली गलतियों को स्वीकारना और क्षमा माँगना।
आध्यात्मिक भूल-सुधार:- उन समुदायों को नेतृत्व और सम्मान देना, जिनके अध्यात्म के प्रति प्रयासों को अपराध घोषित कर दिया गया।
सशर्त भूल-सुधार:- यह धन और भौतिक सामग्री की अदायगी के रूप में एक मुआवज़ा/भूल-सुधार है। यह उन सामाजिक और आर्थिक कारकों से निकलता है जो एक पूरे समुदाय की भूमि, श्रम और मूल्य लूटते हैं।
क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार उपनिवेश देशों की एक अंतरराष्ट्रीय मांग है। “क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार और पुनर्वितरणवादी न्याय के विभिन्न वैश्विक दावों के लिए नैतिक, कानूनी, आर्थिक, ऐतिहासिक, और राजनीतिक साक्ष्यों” की जांच करने के लिए हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में लैंसेट कमीशन ऑन रेपरेशंस की स्थापना की गई जहाँ अफ्रीकी अमरीकियों, रोमन, कैरेबियन दासता के साथ साथ, भारत की जाति व्यवस्था के पीड़ितों को भी सुना गया। इसमें भारतीय सन्दर्भ को अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट और अमित थोरात ने पेश किया था।
क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का यह माध्यम, दलितों, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में खेत से लेकर उद्योगों तक अपना खून-पसीना एक किया, के अवैतनिक श्रम के भारी बोझ के बारे में चिंतन-मनन करने के लिए, देश के समक्ष अवसर मुहैया कराता है। देश की आत्मा लगातार नष्ट की जा रही है, जिसके पुनः जीर्णोद्धार के लिए पुनर्वितरणकारी न्याय और क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का ऐसा प्रावधान करना आवश्यक है। दलित महिलाओं के कोख-संबंधी कठोर श्रम को ध्यान में रखते हुए और भूमि पुनर्वितरण के रूप में पुनर्वितरणकारी न्याय करना ज़रूरी है।
विरोध-प्रदर्शनों और न्याय के आंदोलनों के पक्ष में, दलित अभी तक भूल-सुधार/मुआवज़े की मांग के करीब भी नहीं आये हैं। यह एक मौका है उस समाज को एक आईना दिखाने का, जो अपनी आंतरिक असुरक्षा की भावना के कारण दलितों के खिलाफ निरंतर हिंसा और उनसे घृणा करता है। असुरक्षा की ये भावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मित हुई हैं। क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार की यह प्रक्रिया हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में एक-साथ आने और स्वतंत्रता के खंडित वादों के पुनर्निर्माण में सहयोग का एक अवसर है।
इस देश का प्रत्येक संस्थान दलित हिंसा के इस अपराध में संलिप्त है। यह बहुत आसानी से, देश को एक रखने वाली संरचनाओं में स्थानांतरित हो गया है। आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व दलित जातियों, जिनका श्रम और सम्मान भारत की सत्तारूढ़ जातियों द्वारा शून्य कर दिया गया, को न्याय प्रदान करने का महज़ एक तरीका है।
एक राष्ट्र के रूप में, खुद को साबित करने के लिए हमें सामूहिक रूप से शोक मनाने या दुःखों को साझा करने में सक्षम होने की बहुत जरूरत है। यह देश नाज़ी नरसंहार के पीड़ितों, यहां तक कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के पीड़ितों के लिए शोक मना सकता है, लेकिन दलितों के खिलाफ अत्याचारों पर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है।
इस बड़ी उदासीनता को बदलने या खत्म करने के लिए, हमें नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछ तरीकों में से एक थे। लेकिन ये सर्वाधिक विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार सबसे व्यवहिरिक तरीकों में से एक
Written By- सूरज येंगड़े
आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछेक तरीकों में से एक थे। किन्तु ये बहुत ज़्यादा विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति का माध्यम सबसे व्यवहारिक तरीकों में से एक है।
एक राष्ट्र के रूप में भारत दलितों का कर्ज़दार है- जिनके कन्धों पर उसके सभ्यतागत स्तंभ खड़े किए गए हैं। दलित प्रतिभा, कौशल और आंतरिक-बल आदि भारत को अंग्रेजों सहित बाहरी लोगों के लिए सबसे वांछनीय स्थानों में से एक बनाता है। कला के विभिन्न स्वरुप, साहित्य, संगीत, कविता इत्यादि की उत्पत्ति दलित, आदिवासी और शूद्रों के जन-जीवन से हुई है। अपने आविष्कारशील प्रतिभा और प्रदर्शन के उत्साह में, दलितों ने अपनी त्रासदियों को एक लय में पिरोया है, तथा अस्पृश्यता की यातनाओं के बीच अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है। वे रोये हैं, और आग्रह किया, विरोध-प्रदर्शन किये और लड़ाई भी की है। इस सबके द्वारा उन्होंने संवेदी अनुभवों के नए स्वरूपों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
लगभग सभी “प्रतिष्ठित और शास्त्रीय” भारतीय कला के स्वरूपों का उद्गम दलितों के जन-जीवन में दिखता है। दलित कला की चोरी और उसके ब्रह्मणिकरण के बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। इसके बावजूद दलितों के दावों को रोकने के लिए, उन्हें विभिन्न कलाओं में भाग लेने और अभ्यास करने से रोक दिया गया। इसने दलित प्रतिभा की किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को समाप्त किया है। यही कारण है कि आज भी, कई उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित कलाओं में दलितों की भागीदारी नहीं है।
अन्य नयी खोजों में भी, दलितों ने विज्ञान को फलने-फूलने और तर्कवाद को तरजीह/प्रधानता हासिल करने में मदद की है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों और प्रार्थनाओं में, आत्मज्ञान के सार को सर्वशक्तिमान माना है। ऐसे में, हम दलित अस्मिता और अस्तित्व की हत्या करने की अपनी पिछली गलतियों को कैसे सुलझाएं ताकि भविष्य के लिए स्थिति को ठीक किया जा सके? इस सवाल का उत्तर, “जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता या किसी अन्य तरीके से सहयोग करके अपनी गलतियों को सुधार कर” भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति के बारे में सोचने का एक संभावित तरीका है। यह अतीत और आगे बढ़ने वाले अन्याय को ठीक करने का एक माध्यम है। भूल-सुधारों को तीन व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
नैतिक भूल-सुधार:- ज़ख़्मी दिलों और दिमागों के उपचार करने हेतु पिछली गलतियों को स्वीकारना और क्षमा माँगना।
आध्यात्मिक भूल-सुधार:- उन समुदायों को नेतृत्व और सम्मान देना, जिनके अध्यात्म के प्रति प्रयासों को अपराध घोषित कर दिया गया।
सशर्त भूल-सुधार:- यह धन और भौतिक सामग्री की अदायगी के रूप में एक मुआवज़ा/भूल-सुधार है। यह उन सामाजिक और आर्थिक कारकों से निकलता है जो एक पूरे समुदाय की भूमि, श्रम और मूल्य लूटते हैं।
क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार उपनिवेश देशों की एक अंतरराष्ट्रीय मांग है। “क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार और पुनर्वितरणवादी न्याय के विभिन्न वैश्विक दावों के लिए नैतिक, कानूनी, आर्थिक, ऐतिहासिक, और राजनीतिक साक्ष्यों” की जांच करने के लिए हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में लैंसेट कमीशन ऑन रेपरेशंस की स्थापना की गई जहाँ अफ्रीकी अमरीकियों, रोमन, कैरेबियन दासता के साथ साथ, भारत की जाति व्यवस्था के पीड़ितों को भी सुना गया। इसमें भारतीय सन्दर्भ को अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट और अमित थोरात ने पेश किया था।
क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का यह माध्यम, दलितों, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में खेत से लेकर उद्योगों तक अपना खून-पसीना एक किया, के अवैतनिक श्रम के भारी बोझ के बारे में चिंतन-मनन करने के लिए, देश के समक्ष अवसर मुहैया कराता है। देश की आत्मा लगातार नष्ट की जा रही है, जिसके पुनः जीर्णोद्धार के लिए पुनर्वितरणकारी न्याय और क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का ऐसा प्रावधान करना आवश्यक है। दलित महिलाओं के कोख-संबंधी कठोर श्रम को ध्यान में रखते हुए और भूमि पुनर्वितरण के रूप में पुनर्वितरणकारी न्याय करना ज़रूरी है।
विरोध-प्रदर्शनों और न्याय के आंदोलनों के पक्ष में, दलित अभी तक भूल-सुधार/मुआवज़े की मांग के करीब भी नहीं आये हैं। यह एक मौका है उस समाज को एक आईना दिखाने का, जो अपनी आंतरिक असुरक्षा की भावना के कारण दलितों के खिलाफ निरंतर हिंसा और उनसे घृणा करता है। असुरक्षा की ये भावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मित हुई हैं। क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार की यह प्रक्रिया हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में एक-साथ आने और स्वतंत्रता के खंडित वादों के पुनर्निर्माण में सहयोग का एक अवसर है।
इस देश का प्रत्येक संस्थान दलित हिंसा के इस अपराध में संलिप्त है। यह बहुत आसानी से, देश को एक रखने वाली संरचनाओं में स्थानांतरित हो गया है। आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व दलित जातियों, जिनका श्रम और सम्मान भारत की सत्तारूढ़ जातियों द्वारा शून्य कर दिया गया, को न्याय प्रदान करने का महज़ एक तरीका है।
एक राष्ट्र के रूप में, खुद को साबित करने के लिए हमें सामूहिक रूप से शोक मनाने या दुःखों को साझा करने में सक्षम होने की बहुत जरूरत है। यह देश नाज़ी नरसंहार के पीड़ितों, यहां तक कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के पीड़ितों के लिए शोक मना सकता है, लेकिन दलितों के खिलाफ अत्याचारों पर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है।
इस बड़ी उदासीनता को बदलने या खत्म करने के लिए, हमें नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछ तरीकों में से एक थे। लेकिन ये सर्वाधिक विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार सबसे व्यवहिरिक तरीकों में से एक  हैं।
हैं।
- लेखक सूरज येंगड़े अंबेडकरवादी युवा हैं। वर्तमान में हार्वर्ड युनिवर्सिटी में पोस्ट डाक्ट्रेट फेलो हैं। “कॉस्ट मैटर्स” किताब के लेखक हैं। हिन्दी अनुवाद- कोमल रजक (डॉक्टोरल स्कॉलर, दिल्ली विश्वविद्यालय)
कोरोना के दौर में डॉक्टरों की अग्निपरीक्षा
 देश भर में साढ़े तीन लाख डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय चिकित्सक संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों के खस्ता हाल का मुद्दा उठाया गया है। संस्था ने पत्र के साथ प्रधानमंत्री को एक सूची भेजी है। इसमें सात अगस्त 2020 तक कोविड का शिकार हो चुके 196 डॉक्टरों के नाम तथा अन्य विवरण हैं। एसोसिएशन ने पत्र में ध्यान दिलाया है, “कोविड से संक्रमित हुए डॉक्टरों और उनके परिजनों को बेड उपलब्ध न होने से उन्हें अस्पतालों में एडमिट नहीं किया जा रहा है, और अधिकांश डॉक्टरों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं।”
पत्र में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिजनों को संक्रमित होने के बाद समय से और मानक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। एसोसिएशन ने लिखा है, “प्रधानमंत्री जी, यह जरूरी है कि हम आपको ध्यान दिलाएं कि इन हालात का स्वास्थ्यकर्मियों के समुदाय पर बहुत ही हतोत्साहित करने वाला असर पड़ रहा है।” एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन शर्मा ने कहा है, “हम चाहते हैं कि महामारी में काम कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए।”
देश भर में साढ़े तीन लाख डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय चिकित्सक संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों के खस्ता हाल का मुद्दा उठाया गया है। संस्था ने पत्र के साथ प्रधानमंत्री को एक सूची भेजी है। इसमें सात अगस्त 2020 तक कोविड का शिकार हो चुके 196 डॉक्टरों के नाम तथा अन्य विवरण हैं। एसोसिएशन ने पत्र में ध्यान दिलाया है, “कोविड से संक्रमित हुए डॉक्टरों और उनके परिजनों को बेड उपलब्ध न होने से उन्हें अस्पतालों में एडमिट नहीं किया जा रहा है, और अधिकांश डॉक्टरों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं।”
पत्र में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिजनों को संक्रमित होने के बाद समय से और मानक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। एसोसिएशन ने लिखा है, “प्रधानमंत्री जी, यह जरूरी है कि हम आपको ध्यान दिलाएं कि इन हालात का स्वास्थ्यकर्मियों के समुदाय पर बहुत ही हतोत्साहित करने वाला असर पड़ रहा है।” एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन शर्मा ने कहा है, “हम चाहते हैं कि महामारी में काम कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए।”
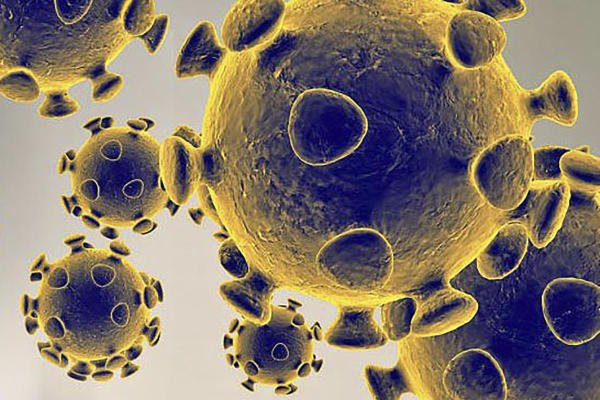 एसोसिएशन के मानद महासचिव आरवी अशोकन ने पत्र के माध्यम से कहा है, “डॉक्टरों को बीमार पड़ने पर अस्पताल में एडमिट किया जाना और बेड तथा दवाएं उपलब्ध कराया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह महामारी डॉक्टरों की जान लेने के मामले में एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अगली क़तार के योद्धा हैं, एक डॉक्टर की जान पर खतरे का मतलब उस पर निर्भर हजारों मरीजों को असुरक्षा में डाल देना है।”
हमारा आत्ममुग्ध शीर्ष नेतृत्व व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की कोई बात स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, लेकिन हालात यह हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने वाले लगभग सभी राजनेताओं और वीआईपी लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ही कराया है, और शायद इसीलिए उनके बीच मृत्युदर भी न के बराबर है, जबकि देश में अब तक लगभग 44 हजार गैर वीआईपी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
एसोसिएशन के मानद महासचिव आरवी अशोकन ने पत्र के माध्यम से कहा है, “डॉक्टरों को बीमार पड़ने पर अस्पताल में एडमिट किया जाना और बेड तथा दवाएं उपलब्ध कराया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह महामारी डॉक्टरों की जान लेने के मामले में एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अगली क़तार के योद्धा हैं, एक डॉक्टर की जान पर खतरे का मतलब उस पर निर्भर हजारों मरीजों को असुरक्षा में डाल देना है।”
हमारा आत्ममुग्ध शीर्ष नेतृत्व व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की कोई बात स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, लेकिन हालात यह हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने वाले लगभग सभी राजनेताओं और वीआईपी लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ही कराया है, और शायद इसीलिए उनके बीच मृत्युदर भी न के बराबर है, जबकि देश में अब तक लगभग 44 हजार गैर वीआईपी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
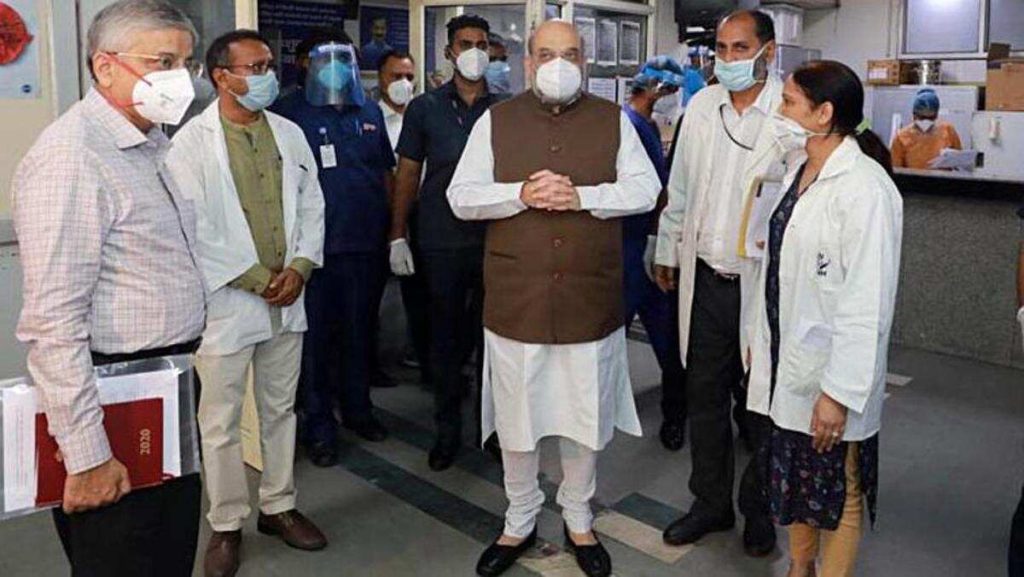 अभी हाल में ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी संक्रमित होने के बाद राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों के बजाय हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पांच सितारा निजी अस्पताल मेदांता का चुनाव किया और यहां तक कि मेदांता में भी उनकी देखरेख के लिए साथ ही साथ एम्स के डॉक्टरों की भी ड्यूटी लग रही है। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि खुद गृहमंत्री जी का अपनी ही व्यवस्था से विश्वास उठ गया?
एक अगस्त को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित का कोविड टेस्ट प्राइवेट कावेरी अस्पताल में हुआ और पॉजिटिव आने पर वे प्राइवेट अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए। इसी तरह से तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री पी थंगमानी, उच्चशिक्षा मंत्री केपी अनबालागन और सहकारिता मंत्री सेलुर के राजू ने भी कोविड होने के बाद सुख-सुविधाओं वाले प्राइवेट उस्पताल में ही भर्ती होना पसंद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कोविड का इलाज भोपाल के चिरायु प्राइवेट अस्पताल में और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने बंगलुरु के मणिपाल प्राइवेट अस्पताल में कराया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया ने भी अपने नेताजी का अनुसरण करते हुए अपना इलाज चिरायु अस्पताल में ही कराया। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाज भी गुड़गांव के मैक्स अस्पताल में हुआ।
सवाल है कि आखिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। सवाल यह भी है कि देश के भीतर आम और खास के लिए अलग-अलग स्वास्थ सुविधाएं कब तक चलती रहेगी। सवाल यह भी है कि कोविड को हराने में जुटे डाक्टरों की सुविधाओं का इंतजाम कब हो सकेगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि इस दौरान बीमार हो रहे डॉक्टरों के लिए सरकार विशेष इंतजाम कब करेगी।
अभी हाल में ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी संक्रमित होने के बाद राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों के बजाय हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पांच सितारा निजी अस्पताल मेदांता का चुनाव किया और यहां तक कि मेदांता में भी उनकी देखरेख के लिए साथ ही साथ एम्स के डॉक्टरों की भी ड्यूटी लग रही है। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि खुद गृहमंत्री जी का अपनी ही व्यवस्था से विश्वास उठ गया?
एक अगस्त को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित का कोविड टेस्ट प्राइवेट कावेरी अस्पताल में हुआ और पॉजिटिव आने पर वे प्राइवेट अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए। इसी तरह से तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री पी थंगमानी, उच्चशिक्षा मंत्री केपी अनबालागन और सहकारिता मंत्री सेलुर के राजू ने भी कोविड होने के बाद सुख-सुविधाओं वाले प्राइवेट उस्पताल में ही भर्ती होना पसंद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कोविड का इलाज भोपाल के चिरायु प्राइवेट अस्पताल में और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने बंगलुरु के मणिपाल प्राइवेट अस्पताल में कराया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया ने भी अपने नेताजी का अनुसरण करते हुए अपना इलाज चिरायु अस्पताल में ही कराया। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाज भी गुड़गांव के मैक्स अस्पताल में हुआ।
सवाल है कि आखिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। सवाल यह भी है कि देश के भीतर आम और खास के लिए अलग-अलग स्वास्थ सुविधाएं कब तक चलती रहेगी। सवाल यह भी है कि कोविड को हराने में जुटे डाक्टरों की सुविधाओं का इंतजाम कब हो सकेगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि इस दौरान बीमार हो रहे डॉक्टरों के लिए सरकार विशेष इंतजाम कब करेगी।
- By- डॉ. सिद्धार्थ
जब ब्राह्मण युवक ने फोन कर कहा, आपने दलित दरोगा कि ब्राह्मणों से मारपीट की खबर क्यों नहीं चलाई
 गाज़ीपुर जिले के ग्राम नूरपुर स्थित हाल्ट थाने की घटना परेशान करने वाली है। यहां आरोप है कि थाने के एक दारोगा ने जो कि दलित समाज का है, ब्राह्मण समाज के लोगों पर बर्बरता की है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वह किसी भी सभ्य इंसान को परेशान कर सकते हैं। दारोगा के इस मार-पीट का जमकर विरोध होना चाहिए।
कल मेरे पास इस संबंध में एक अपरिचित ब्राह्मण समाज के युवक का फोन भी आया। गुस्से में उसने कहा भी कि अब मैं इस पर खबर क्यों नहीं बना रहा? उसका आरोप था कि मैं सिर्फ दलित उत्पीड़न की खबरें ही बनाता हूं। हालांकि उसका यह आरोप ठीक नहीं था, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 18 मिनट में किसी न किसी रूप में दलित उत्पीड़न होता है, यानी एक घंटे में तकरीबन 3 घटनाएं। यानी कि 24 घंटे में तकरीबन 72 घटनाएं। और मैं हर दिन दलित उत्पीड़न की 72 घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्योंकि कईयों के पास उत्पीड़न का साक्ष्य नहीं होता, कईयों की FIR यही पुलिस महकमा नहीं लिखता। थाने में बैठे कथित ऊंची जाति के तमाम अधिकारी दलितों को गाली-गलौच कर थाने से भगा देते हैं। और बिना साक्ष्य के मैं खबर बनाने से बचता हूं। मेरे पास यह भी खबरें आती है कि कई लोगों के घरों की लड़कियों का अपहरण हुआ है और पुलिस मामले को दर्ज नहीं कर रही है, दर्ज कर भी लिया है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ज्यादा क्या कहूं आप भी इसी देश में रहते हैं, जानते ही होंगे।
तो ब्राह्मण युवक के फोन पर आते हैं। दलित पत्रकारिता से जुड़ने के बाद बीते आठ सालों में मुझे किसी ब्राह्मण या किसी भी ऊंची जाति या फिर मजबूत ओबीसी जाति के भी किसी व्यक्ति ने आज तक फोन कर के यह नहीं कहा कि फलां गांव या शहर में मेरे समाज के लोगों ने दलितों पर बहुत अत्याचार किया है, आप खबर बनाइए, या फिर फलां सवर्ण पुलिस अधिकारी दलितों की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, आप खबर बनाइए। आरोप लगाने वालों को खुद से यह भी पूछना चाहिए कि दलित/आदिवासी उत्पीड़न की तमाम बड़ी खबरें दबा जाने या फिर दलित/आदिवासी समाज के हितों से जुड़ी तमाम खबरें नहीं चलाने को लेकर उन्होंने अब तक कितने समाचार समूहों को फोन किया, या ई-मेल लिखा है। महाराष्ट्र के खैरलांजी से लेकर हरियाणा के मिर्चपुर या फिर गुजरात के ऊना जैसी घटनाओं में पुलिस और भारतीय मीडिया की अनदेखी के कारण पीड़ितों को इंसान न मिलने से वो कितने चिंतित हुए थे?
लेकिन मेरे पास गुस्से में यह फोन जरूर आता है कि आप दलितों द्वारा सवर्ण उत्पीड़न की खबरें नहीं चलातें। हालांकि इस तरह कि घटनाएं सालों में एकाध ही आती है। जिनको पता हो कि दलित आदतन सवर्णों पर अत्याचार करता है तो थेथरई से पहले मुझे साल में दस ऐसी घटनाओं के खबरों का लिंक साझा जरूर करे।
खैर, गाजीपुर की घटना पर आते हैं। दलित समाज के दारोगा ने जो भी किया, वह निंदनिय है। उसकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करे। मुझे ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक समुदाय विशेष के हाथ में कोई भी मांस हो, उसे गाय का मांस बताकर पीटकर अधमरा कर दिया जाए। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां गरीबों और कमजोरों को न्याय न मिले, चाहे वह किसी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्दोष पर अत्याचार कर बच जाए।
मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि जिस पुलिस अधिकारी पर यह आरोप हो कि उसने किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर जुल्म किया है, या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव किया है, उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ऐसी तमाम घटनाओं की निंदा करता हूं।
हालांकि इस खबर के संदर्भ में बाद में साफ हो गया कि दलित पुलिस अधिकारी को ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा फसाने की कोशिश हो रही थी। देखे लिंक
लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर दलितों के साथ अत्याचार पर सवर्णों के मुंह में दही क्यों जम जाता है। उन्हें तब दर्द क्यों नहीं होता??
गाज़ीपुर जिले के ग्राम नूरपुर स्थित हाल्ट थाने की घटना परेशान करने वाली है। यहां आरोप है कि थाने के एक दारोगा ने जो कि दलित समाज का है, ब्राह्मण समाज के लोगों पर बर्बरता की है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वह किसी भी सभ्य इंसान को परेशान कर सकते हैं। दारोगा के इस मार-पीट का जमकर विरोध होना चाहिए।
कल मेरे पास इस संबंध में एक अपरिचित ब्राह्मण समाज के युवक का फोन भी आया। गुस्से में उसने कहा भी कि अब मैं इस पर खबर क्यों नहीं बना रहा? उसका आरोप था कि मैं सिर्फ दलित उत्पीड़न की खबरें ही बनाता हूं। हालांकि उसका यह आरोप ठीक नहीं था, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 18 मिनट में किसी न किसी रूप में दलित उत्पीड़न होता है, यानी एक घंटे में तकरीबन 3 घटनाएं। यानी कि 24 घंटे में तकरीबन 72 घटनाएं। और मैं हर दिन दलित उत्पीड़न की 72 घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्योंकि कईयों के पास उत्पीड़न का साक्ष्य नहीं होता, कईयों की FIR यही पुलिस महकमा नहीं लिखता। थाने में बैठे कथित ऊंची जाति के तमाम अधिकारी दलितों को गाली-गलौच कर थाने से भगा देते हैं। और बिना साक्ष्य के मैं खबर बनाने से बचता हूं। मेरे पास यह भी खबरें आती है कि कई लोगों के घरों की लड़कियों का अपहरण हुआ है और पुलिस मामले को दर्ज नहीं कर रही है, दर्ज कर भी लिया है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ज्यादा क्या कहूं आप भी इसी देश में रहते हैं, जानते ही होंगे।
तो ब्राह्मण युवक के फोन पर आते हैं। दलित पत्रकारिता से जुड़ने के बाद बीते आठ सालों में मुझे किसी ब्राह्मण या किसी भी ऊंची जाति या फिर मजबूत ओबीसी जाति के भी किसी व्यक्ति ने आज तक फोन कर के यह नहीं कहा कि फलां गांव या शहर में मेरे समाज के लोगों ने दलितों पर बहुत अत्याचार किया है, आप खबर बनाइए, या फिर फलां सवर्ण पुलिस अधिकारी दलितों की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, आप खबर बनाइए। आरोप लगाने वालों को खुद से यह भी पूछना चाहिए कि दलित/आदिवासी उत्पीड़न की तमाम बड़ी खबरें दबा जाने या फिर दलित/आदिवासी समाज के हितों से जुड़ी तमाम खबरें नहीं चलाने को लेकर उन्होंने अब तक कितने समाचार समूहों को फोन किया, या ई-मेल लिखा है। महाराष्ट्र के खैरलांजी से लेकर हरियाणा के मिर्चपुर या फिर गुजरात के ऊना जैसी घटनाओं में पुलिस और भारतीय मीडिया की अनदेखी के कारण पीड़ितों को इंसान न मिलने से वो कितने चिंतित हुए थे?
लेकिन मेरे पास गुस्से में यह फोन जरूर आता है कि आप दलितों द्वारा सवर्ण उत्पीड़न की खबरें नहीं चलातें। हालांकि इस तरह कि घटनाएं सालों में एकाध ही आती है। जिनको पता हो कि दलित आदतन सवर्णों पर अत्याचार करता है तो थेथरई से पहले मुझे साल में दस ऐसी घटनाओं के खबरों का लिंक साझा जरूर करे।
खैर, गाजीपुर की घटना पर आते हैं। दलित समाज के दारोगा ने जो भी किया, वह निंदनिय है। उसकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करे। मुझे ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक समुदाय विशेष के हाथ में कोई भी मांस हो, उसे गाय का मांस बताकर पीटकर अधमरा कर दिया जाए। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां गरीबों और कमजोरों को न्याय न मिले, चाहे वह किसी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्दोष पर अत्याचार कर बच जाए।
मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि जिस पुलिस अधिकारी पर यह आरोप हो कि उसने किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर जुल्म किया है, या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव किया है, उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ऐसी तमाम घटनाओं की निंदा करता हूं।
हालांकि इस खबर के संदर्भ में बाद में साफ हो गया कि दलित पुलिस अधिकारी को ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा फसाने की कोशिश हो रही थी। देखे लिंक
लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर दलितों के साथ अत्याचार पर सवर्णों के मुंह में दही क्यों जम जाता है। उन्हें तब दर्द क्यों नहीं होता??
नई शिक्षा नीति से उठते सवाल
 Written By- प्रेमकुमार मणि
जुलाई महीने की 29 तारीख को केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसके पूर्व 1986 में राजीव गाँधी सरकार ने इस विभाग में एक बदलाव लाया था, जिसमे दिखने लायक बात यही थी कि शिक्षा विभाग का नाम बदल कर मानव संसाधन विभाग कर दिया गया था। कल की घोषणा में पुनर्मूसिको भव, अर्थात फिर से इस विभाग का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया।
कुछ बड़ी तब्दीलियां की गयी हैं। 10 +2 प्रणाली को ख़त्म कर के 5 +3 +3 +4 प्रणाली अपनायी गयी है। स्कूल से पहले ही बच्चों की शिक्षा आरम्भ हो जाएगी। इसे आंगनबाड़ियाँ अंजाम देंगी और यह फाउंडेशन कोर्स होगा। यह तीन साल को होगा। प्री -स्कूलिंग दो साल का होगा – कक्षा एक और दो। इस तरह फाउंडेशन और प्री मिल कर आरंभिक पांच। फिर कक्षा तीन से पांच तक का तीन वर्षीय मिडिल कोर्स। इसके बाद छह, सात,आठ का सेकंडरी और आखिर में नौ, दस, ग्यारह,बारह का हायर सेकंडरी कोर्स। खास बात यह है कि मिडिल कोर्स से ही कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा। उम्मीद की गयी है कि हर छात्र किसी न किसी हुनर के साथ, यानी हुनरमंद होकर ही स्कूल से बाहर निकलेगा। इस लक्ष्य की सराहना कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है।
वीडियो देखिए- बाबासाहेब की नई पीढ़ी का धमाल, देश, प्रदेश, जिलों में बने टॉपर
इस पूरे प्रयोग को समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस नीति को अंजाम देने के लिए सुब्रह्मण्यम और कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली अलग-अलग समितियों ने मिहनत की है। निचले स्तरों से भी काफी कुछ अध्ययन किये जाने की बात कही गयी है। फिर भी बहुत से सवाल उठते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी अभी भी बच्चों की देखभाल करती है। इस घोषणा ने उसे बाल कल्याण से उठा कर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ला दिया है। बाकी बारह कक्षाओं की व्यवस्था है ही। मेरी समझ से पुरानी व्यवस्था 10 +2 अधिक सही थी। दो सोपानीय की जगह चार सोपानीय का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। क्या सरकार चाहती है कि बच्चे बीच में पढाई का सिलसिला तोड़ें? यानी पहले, दूसरे या तीसरे सोपान पर भी स्कूल छोड़ सकते हैं।अनिवार्य शिक्षा के वातावरण को यह कमजोर करता प्रतीत होता है। ग़रीबों को शिक्षा से दूर रखने की छुपी और शातिर कोशिश के रूप में भी इसे देखा जायेगा।
उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स को चार साल का किया गया है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, यानि मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद बिना एम् फिल के पीएचडी। डिग्री कोर्स को ऐसा बनाया गया है कि छात्र बीच में भी यदि पढाई छोड़ते हैं, तो उन्हें सर्टिफ़िकेट मिलेगा। पहला साल पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे -चौथे साल के बाद डिग्री दे दिए जाने की व्यवस्था है। इसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम कहा गया है।
वीडियो- एक दलित कारसेवक से सुनिए अयोध्या आंदोलन की सच्चाई
आरंभिक शिक्षा में पहले भी मादरी-जुबानों पर जोर था। इस व्यवस्था में भी है। उच्च शिक्षा में निजी और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को एक ही शिक्षा नीति के तहत चलने की बात कही गयी है। यह सराहनीय है। लेकिन प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर यह नीति छात्रों को ड्रॉप-आउट के लिए उत्साहित करती प्रतीत होती हैं। इस लिए मैं इसकी सराहना करने में स्वयं को रोकना चाहूँगा।
प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर उत्साहित थे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनसे भी बढ़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहित थे। लेकिन मैंने इसे उलट -पुलट कर जो देखा उससे उत्साहित होने की जगह भयभीत हो रहा हूँ। यह पूरी तरह एक पाखंड सृजित करता है। उदाहरण देखिए। कहा गया है शिक्षा-बजट 4.43 फीसदी से बढ़ा कर 6 फीसदी किया जा रहा है। यानी 1.57 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। किसकी आँख में धूल झोंक रहे हो मोदी जी? आप पहले यह बतलाइये कि बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी का खर्च कितना है? आप उसे शिक्षा में जोड़ दे रहे हो। यह तो पहले ही खर्च हो रहा था। यदि इसके अलावा शिक्षा का व्यय बढ़ाया गया है, तब मैं आपकी थोड़ी -सी तारीफ़ करूँगा। अधिक नहीं, क्योंकि आज भी इस देश में शिक्षा का व्यय प्रतिरक्षा व्यय (15.5% )से बहुत कम है,और उसे उस से बहुत अधिक होना चाहिए।
वीडियो देखिए- वो दलित साहित्यकार, जिसके बारे में रूस के लोगों ने प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा था
यह शिक्षा नीति मेरी समझ से उलझावकारी है। नई सदी की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करने का इसके पास कोई विजन नहीं है। हमारा देश संस्कृति -बहुल और भाषा -बहुल है। इस बहुरंगेपन को एक इंद्रधनुषी राष्ट्रीयता में विकसित करना, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए एक वैश्विक चेतना सम्पन्न नागरिक का निर्माण और आर्थिक-सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुख इंसान बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह देखना होगा कि हम समान स्कूल प्रणाली को अपना रहे हैं या नहीं। देश में कई स्तर के स्कूल नहीं होने चाहिए, इसे सुनिश्चित करना होगा। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों का प्रवेश भले हो, स्कूल स्तर तक सभी तरह के प्राइवेट स्कूल को बंद करना होगा। यह नहीं होता है तब शिक्षा पर बात करना फिजूल है, बकवास है।
Written By- प्रेमकुमार मणि
जुलाई महीने की 29 तारीख को केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसके पूर्व 1986 में राजीव गाँधी सरकार ने इस विभाग में एक बदलाव लाया था, जिसमे दिखने लायक बात यही थी कि शिक्षा विभाग का नाम बदल कर मानव संसाधन विभाग कर दिया गया था। कल की घोषणा में पुनर्मूसिको भव, अर्थात फिर से इस विभाग का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया।
कुछ बड़ी तब्दीलियां की गयी हैं। 10 +2 प्रणाली को ख़त्म कर के 5 +3 +3 +4 प्रणाली अपनायी गयी है। स्कूल से पहले ही बच्चों की शिक्षा आरम्भ हो जाएगी। इसे आंगनबाड़ियाँ अंजाम देंगी और यह फाउंडेशन कोर्स होगा। यह तीन साल को होगा। प्री -स्कूलिंग दो साल का होगा – कक्षा एक और दो। इस तरह फाउंडेशन और प्री मिल कर आरंभिक पांच। फिर कक्षा तीन से पांच तक का तीन वर्षीय मिडिल कोर्स। इसके बाद छह, सात,आठ का सेकंडरी और आखिर में नौ, दस, ग्यारह,बारह का हायर सेकंडरी कोर्स। खास बात यह है कि मिडिल कोर्स से ही कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा। उम्मीद की गयी है कि हर छात्र किसी न किसी हुनर के साथ, यानी हुनरमंद होकर ही स्कूल से बाहर निकलेगा। इस लक्ष्य की सराहना कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है।
वीडियो देखिए- बाबासाहेब की नई पीढ़ी का धमाल, देश, प्रदेश, जिलों में बने टॉपर
इस पूरे प्रयोग को समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस नीति को अंजाम देने के लिए सुब्रह्मण्यम और कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली अलग-अलग समितियों ने मिहनत की है। निचले स्तरों से भी काफी कुछ अध्ययन किये जाने की बात कही गयी है। फिर भी बहुत से सवाल उठते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी अभी भी बच्चों की देखभाल करती है। इस घोषणा ने उसे बाल कल्याण से उठा कर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ला दिया है। बाकी बारह कक्षाओं की व्यवस्था है ही। मेरी समझ से पुरानी व्यवस्था 10 +2 अधिक सही थी। दो सोपानीय की जगह चार सोपानीय का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। क्या सरकार चाहती है कि बच्चे बीच में पढाई का सिलसिला तोड़ें? यानी पहले, दूसरे या तीसरे सोपान पर भी स्कूल छोड़ सकते हैं।अनिवार्य शिक्षा के वातावरण को यह कमजोर करता प्रतीत होता है। ग़रीबों को शिक्षा से दूर रखने की छुपी और शातिर कोशिश के रूप में भी इसे देखा जायेगा।
उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स को चार साल का किया गया है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, यानि मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद बिना एम् फिल के पीएचडी। डिग्री कोर्स को ऐसा बनाया गया है कि छात्र बीच में भी यदि पढाई छोड़ते हैं, तो उन्हें सर्टिफ़िकेट मिलेगा। पहला साल पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे -चौथे साल के बाद डिग्री दे दिए जाने की व्यवस्था है। इसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम कहा गया है।
वीडियो- एक दलित कारसेवक से सुनिए अयोध्या आंदोलन की सच्चाई
आरंभिक शिक्षा में पहले भी मादरी-जुबानों पर जोर था। इस व्यवस्था में भी है। उच्च शिक्षा में निजी और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को एक ही शिक्षा नीति के तहत चलने की बात कही गयी है। यह सराहनीय है। लेकिन प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर यह नीति छात्रों को ड्रॉप-आउट के लिए उत्साहित करती प्रतीत होती हैं। इस लिए मैं इसकी सराहना करने में स्वयं को रोकना चाहूँगा।
प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर उत्साहित थे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनसे भी बढ़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहित थे। लेकिन मैंने इसे उलट -पुलट कर जो देखा उससे उत्साहित होने की जगह भयभीत हो रहा हूँ। यह पूरी तरह एक पाखंड सृजित करता है। उदाहरण देखिए। कहा गया है शिक्षा-बजट 4.43 फीसदी से बढ़ा कर 6 फीसदी किया जा रहा है। यानी 1.57 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। किसकी आँख में धूल झोंक रहे हो मोदी जी? आप पहले यह बतलाइये कि बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी का खर्च कितना है? आप उसे शिक्षा में जोड़ दे रहे हो। यह तो पहले ही खर्च हो रहा था। यदि इसके अलावा शिक्षा का व्यय बढ़ाया गया है, तब मैं आपकी थोड़ी -सी तारीफ़ करूँगा। अधिक नहीं, क्योंकि आज भी इस देश में शिक्षा का व्यय प्रतिरक्षा व्यय (15.5% )से बहुत कम है,और उसे उस से बहुत अधिक होना चाहिए।
वीडियो देखिए- वो दलित साहित्यकार, जिसके बारे में रूस के लोगों ने प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा था
यह शिक्षा नीति मेरी समझ से उलझावकारी है। नई सदी की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करने का इसके पास कोई विजन नहीं है। हमारा देश संस्कृति -बहुल और भाषा -बहुल है। इस बहुरंगेपन को एक इंद्रधनुषी राष्ट्रीयता में विकसित करना, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए एक वैश्विक चेतना सम्पन्न नागरिक का निर्माण और आर्थिक-सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुख इंसान बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह देखना होगा कि हम समान स्कूल प्रणाली को अपना रहे हैं या नहीं। देश में कई स्तर के स्कूल नहीं होने चाहिए, इसे सुनिश्चित करना होगा। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों का प्रवेश भले हो, स्कूल स्तर तक सभी तरह के प्राइवेट स्कूल को बंद करना होगा। यह नहीं होता है तब शिक्षा पर बात करना फिजूल है, बकवास है। वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले हैनी बाबू की गिरफ्तारी के मायने
 Written By-प्रमोद रंजन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक हैनी बाबू मुसलीयारवेटिल थारायिल (हैनी बाबू, 54 वर्ष) को नेशनल इन्विस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने कहा है कि उन्हें भी भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार, वे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 12 वें बुद्धिजीवी हो गए हैं, जिनमें से कम से कम आधे पिछड़े अथवा दलित समुदाय से आते हैं।
इस मामले में पहले गिरफ़्तार होने वालों में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वरनोन गोंसालविस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और अरुण फेरेरा शामिल हैं।
उपरोक्त में से कई की तरह हैनी बाबू का भी भीमा-कोरेगांव में आयोजित यलगार परिषद के कार्यक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं था। न वे इसके आयोजकों में थे, न वहां आमंत्रित थे, न ही उनका इस आयोजन से कोई जुड़ाव था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस मामले में दिखाई गई है। हालांकि अगर ऐसा कोई जुड़ाव होता, तब भी वह कोई अपराध नहीं था।
भीमा-कोरे गांव में हर साल होने वाला वह आयोजन भारत की सबसे वंचित आबादी के आत्मसम्मान का आयोजन रहा है, जो हमारे देश में सामाजिक-लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया का संकेत है। लेकिन जिस तरह से उसे शहरी मध्यमवर्ग के समक्ष देशद्रोही गतिविधि के रूप में प्रसारित किया गया, वह अपने आप हैरतअंगेज़ और बहुत खौफनाक है।
हैनी बाबू को छह दिन लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने प्रेस को कहा है कि “आरोपी हैनी बाबू नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता थे।”
इससे पहले, जून 2018 में पुणे पुलिस ने कहा था कि भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन से एक पत्र (संभवत: पंपलेट) बरामद किया गया है, जिसमें “एक संदिग्ध अंडर कवर माओवादी नेता” कॉमरेड साई (जीएन साई बाबा) के लिए समर्थन जुटाने की अपील की गई है। पुलिस का कहना था कि चूंकि उस पत्र में एक जगह “कामरेड एच.बी.” का उल्लेख है, इसलिए उन्हें संदेह है कि वे एच.बी. – हैनी बाबू ही हैं। इसी सबूत के आधार पर सितंबर, 2019 में पुणे पुलिस ने हैनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापा मारा था तथा उनका लैपटॉप, पेन ड्राइव, ईमेल एकाउंट का पासवर्ड व दो किताबें और साई बाबा की रक्षा और रिहाई की मांग के लिए गठित समित द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकाएं जब्त की थीं। पुलिस द्वारा जब्त की गई दो किताबें थीं From Varna to Jati: Political Economy of Caste in Indian Social Formation (यलवर्थी नवीन बाबू) और Understanding Maoists: Notes of a Participant Observer from Andhra Pradesh (एन. वेणुगोपाल)। इनमें से पहली किताब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे यलवर्थी नवीन बाबू की एम.फिल. की थिसिस है, जिसे उन्होंने पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया है, जबकि दूसरी किताब आंध्रप्रदेश के माओवादी आंदोलन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है।
विभिन्न अखबारों में प्रकाशित एनआईए के बयानों से जाहिर है कि हैनी बाबू की गिरफ्तारी का आधार जीएन साई बाबा की रक्षा और रिहाई के लिए गठित समिति में सक्रियता के कारण हुई है, जिसका भीमा-कोरेगांव की घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में यह समझना आवश्यक है कि साई बाबा और हैनी बाबू का सामाजिक और बौद्धिक रिश्ता क्या है।
केरल के हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जबकि आंध्रप्रदेश के साईबाबा भी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने तक इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत अक्षम साई बाबा को 2014 में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मार्च, 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला न्यायालय ने साई बाबा, जेएनयू के शोधार्थी हेम मिश्र और पत्रकार प्रशांत राही को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। हैनी बाबू “राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए समिति” के प्रेस सचिव हैं। इस नाते वे साई बाबा की रिहाई के जारी होने वाली अपीलों, प्रदर्शनों आदि में भी सक्रिय रहते थे। इससे संबंधित उनके प्रेस नोट निरंतर मीडिया-संस्थानों को मिलते थे।
Written By-प्रमोद रंजन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक हैनी बाबू मुसलीयारवेटिल थारायिल (हैनी बाबू, 54 वर्ष) को नेशनल इन्विस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने कहा है कि उन्हें भी भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार, वे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 12 वें बुद्धिजीवी हो गए हैं, जिनमें से कम से कम आधे पिछड़े अथवा दलित समुदाय से आते हैं।
इस मामले में पहले गिरफ़्तार होने वालों में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वरनोन गोंसालविस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और अरुण फेरेरा शामिल हैं।
उपरोक्त में से कई की तरह हैनी बाबू का भी भीमा-कोरेगांव में आयोजित यलगार परिषद के कार्यक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं था। न वे इसके आयोजकों में थे, न वहां आमंत्रित थे, न ही उनका इस आयोजन से कोई जुड़ाव था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस मामले में दिखाई गई है। हालांकि अगर ऐसा कोई जुड़ाव होता, तब भी वह कोई अपराध नहीं था।
भीमा-कोरे गांव में हर साल होने वाला वह आयोजन भारत की सबसे वंचित आबादी के आत्मसम्मान का आयोजन रहा है, जो हमारे देश में सामाजिक-लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया का संकेत है। लेकिन जिस तरह से उसे शहरी मध्यमवर्ग के समक्ष देशद्रोही गतिविधि के रूप में प्रसारित किया गया, वह अपने आप हैरतअंगेज़ और बहुत खौफनाक है।
हैनी बाबू को छह दिन लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने प्रेस को कहा है कि “आरोपी हैनी बाबू नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता थे।”
इससे पहले, जून 2018 में पुणे पुलिस ने कहा था कि भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन से एक पत्र (संभवत: पंपलेट) बरामद किया गया है, जिसमें “एक संदिग्ध अंडर कवर माओवादी नेता” कॉमरेड साई (जीएन साई बाबा) के लिए समर्थन जुटाने की अपील की गई है। पुलिस का कहना था कि चूंकि उस पत्र में एक जगह “कामरेड एच.बी.” का उल्लेख है, इसलिए उन्हें संदेह है कि वे एच.बी. – हैनी बाबू ही हैं। इसी सबूत के आधार पर सितंबर, 2019 में पुणे पुलिस ने हैनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापा मारा था तथा उनका लैपटॉप, पेन ड्राइव, ईमेल एकाउंट का पासवर्ड व दो किताबें और साई बाबा की रक्षा और रिहाई की मांग के लिए गठित समित द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकाएं जब्त की थीं। पुलिस द्वारा जब्त की गई दो किताबें थीं From Varna to Jati: Political Economy of Caste in Indian Social Formation (यलवर्थी नवीन बाबू) और Understanding Maoists: Notes of a Participant Observer from Andhra Pradesh (एन. वेणुगोपाल)। इनमें से पहली किताब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे यलवर्थी नवीन बाबू की एम.फिल. की थिसिस है, जिसे उन्होंने पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया है, जबकि दूसरी किताब आंध्रप्रदेश के माओवादी आंदोलन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है।
विभिन्न अखबारों में प्रकाशित एनआईए के बयानों से जाहिर है कि हैनी बाबू की गिरफ्तारी का आधार जीएन साई बाबा की रक्षा और रिहाई के लिए गठित समिति में सक्रियता के कारण हुई है, जिसका भीमा-कोरेगांव की घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में यह समझना आवश्यक है कि साई बाबा और हैनी बाबू का सामाजिक और बौद्धिक रिश्ता क्या है।
केरल के हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जबकि आंध्रप्रदेश के साईबाबा भी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने तक इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत अक्षम साई बाबा को 2014 में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मार्च, 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला न्यायालय ने साई बाबा, जेएनयू के शोधार्थी हेम मिश्र और पत्रकार प्रशांत राही को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। हैनी बाबू “राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए समिति” के प्रेस सचिव हैं। इस नाते वे साई बाबा की रिहाई के जारी होने वाली अपीलों, प्रदर्शनों आदि में भी सक्रिय रहते थे। इससे संबंधित उनके प्रेस नोट निरंतर मीडिया-संस्थानों को मिलते थे।
 मार्च, 2019 में साई बाबा की रक्षा और बचाव के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर एके रामकृष्णन, अमित भादुड़ी, आनंद तेलतुंबडे, अरुंधति राय, अशोक भौमिक, जी. हरगोपाल, जगमोहन सिंह, करेन गेब्रियल, एन रघुराम, नंदिता नारायण, पीके विजयन, संजय काक, सीमा आजाद, कृष्णदेव राव, सुधीर ढवले, सुमित चक्रवर्ती और विकास गुप्ता थे। हालांकि इस समिति के सदस्यों में हैनी बाबू का नाम नहीं था, लेकिन यह सच है कि वे साई बाबा के बिगड़ते स्वास्थ्य और उन्हें जेल में दी जा रही प्रताड़ना से लगातार चिंतित थे। संभवत: इसी समिति ने साई बाबा के मामले से संबंधित जानकारी देने वाली वे पुस्तकाएं प्रकाशित की थीं, जिन्हें हैनी बाबू के घर पर छापे के दौरान पुलिस ने जब्त किया था।
दक्षिण भारत से आने के नाते, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही विषय का शिक्षक होने के नाते भी हैनी बाबू का साई बाबा के पक्ष में खड़ा होना होना अनूठी बात नहीं थी। लेकिन उनके बीच एक और रिश्ता था, जिस पर एनआईए की नजर भले ही रही हो, लेकिन जिस तबके के लिए वे काम करते रहे हैं, उनमें से अधिकांश को इससे कोई लेना-देना नहीं है। साई बाबा और हैनी बाबू अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं तथा इस तबके को उसका जायज हक दिलाने के लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है।
आंध्रप्रदेश के अमलापुरम् में जन्मे जीएन साई बाबा का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था, उनके घर में बिजली तक नहीं थी। छुटपन में उनके पिता के पास तीन एकड़ जमीन थी, जिसमें धान की फसल लहलहाया करती थी, लेकिन साई बाबा के 10 वीं कक्षा में पहुंचने से पहले ही वे खेत कर्ज देने वाले साहूकार की भेंट चढ़ गए थे। विलक्षण मेधा के धनी साई बाबा ने अपनी पढ़ाई फ़ेलोशिप और पत्नी वसंथा (उस समय मित्र) के सहयोग से पूरी की थी। वसंथा से उनकी मित्रता 10 वीं कक्षा में ही गणित का होम-वर्क करते समय हुई थी। साई बाबा कॉलेज में नामांकन के लिए वसंथा द्वारा उपलब्ध करवाए गए टिकट के पैसे से जब पहली बार हैदराबाद गए तो उन्होंने पहली बार ट्रेन देखी। बचपन से लेकर युवावस्था का एक लंबा चरण पार हो जाने तक उनके पास व्हील चेयर तक नहीं थी और वे घुटनों के बल पर जमीन पर घिसट कर चला करते थे। 2003 में दिल्ली आने के बाद उन्होंने पहली बार व्हील चेयर खरीदी। दिल्ली ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उनकी प्रतिभा पर देश-विदेश के अध्येताओं की नजर गई और उनके शोध-पत्रों को विश्व के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर जगह मिली। उन्होंने इस दौरान पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाना जारी रखा तथा कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जारी विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी की।
एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में साई बाबा ने बताया था कि हैदराबाद में “मेरा राजनीतिक जीवन मंडल आयोग और आरक्षण की लड़ाई से शुरू हुआ।” जिसमें वसंथा भी उनके साथ शामिल थीं। उसी दौरान मार्च, 1991 में उन्होंने विवाह भी किया। वह लड़ाई वे आजीवन लड़ते रहे।
इसी प्रकार हैनी बाबू ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की अनेक बड़ी लड़ाईयां, जिस प्रकार बिना किसी आत्मप्रचार के, बहुत धैर्य और परिश्रम से लड़ीं और जीतीं वह अपने आप में एक मिसाल है।
उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 में ही 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन 2016 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करने के लिए अघोषित रूप से तरह-तरह के नियम बना रखे थे। नतीजा यह होता था कि सामान्य वर्ग में ओबीसी के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का नामांकन तो दूर, 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों में आधी से अधिक सीटें भी खाली रह जाती थीं तथा उन पर बाद में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन कर लिया जाता था।
हैनी बाबू ने इसे रोकने के लिए दलित एवं पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के फोरम “एकैडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस” के तहत सक्रिय रहते हुए अथक परिश्रम किया। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सैकड़ों आवेदन किए, अपील पर अपीलें की और उन आंकड़ों का संधान कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण की स्थिति की वह तस्वीर पेश की, जिसे देखकर हम सब हैरान रह गए। उन दिनों मैं बहुजन मुद्दों पर केंद्रित एक मासिक पत्रिका का संपादन किया करता था। हमने अपनी पत्रिका में उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया था – “ओबीसी सीटों की लूट”! ओबीसी आरक्षण के नाम पर केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सरकार ने विद्यार्थियों की भर्ती 54 प्रतिशत बढ़ा दी थी, ताकि अनारक्षित वर्ग को जाने वाली सीटों में कमी न हो और उन्हें इसके लिए सैकड़ों करोड़ रूपए का अनुदान भी मिला था, लेकिन हैनी बाबू द्वारा जमा किए गए आंकड़े साफ तौर पर बता रहे थे इसका फायदा वास्तव में द्विज समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को हो रहा था और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों विद्यार्थियों को साल दर साल उनके वाजिब हक से वंचित किया जा रहा था।
हैनी बाबू द्वारा जमा किए गए इन आंकड़ों को उनके संगठन ने ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं तक पहुंचाया, जिससे उसकी गूंज संसद में भी पहुंची। हैनी बाबू की इस मुहिम में उनके संगठन के एक और पिछड़े वर्ग से आने वाले शिक्षक केदार मंडल निरंतर शामिल रहते थे। केदार भी साई बाबा की तरह शारीरिक रूप से अक्षम हैं। दो वर्ष पहले उन पर भी हिंदू भावनाओं के अपमान के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था तथा उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया था।
हैनी बाबू द्वारा संकलित उन आंकड़ों के प्रकाश में आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के लिए ओबीसी सीटों की लूट जारी रखना संभव नहीं रह गया। 2016 के बाद से हर साल दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों अतिरिक्त विद्यार्थी देश के दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में नामांकन पाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम को ही हैनी बाबू के नाम की भी जानकारी होगी।
मार्च, 2019 में साई बाबा की रक्षा और बचाव के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर एके रामकृष्णन, अमित भादुड़ी, आनंद तेलतुंबडे, अरुंधति राय, अशोक भौमिक, जी. हरगोपाल, जगमोहन सिंह, करेन गेब्रियल, एन रघुराम, नंदिता नारायण, पीके विजयन, संजय काक, सीमा आजाद, कृष्णदेव राव, सुधीर ढवले, सुमित चक्रवर्ती और विकास गुप्ता थे। हालांकि इस समिति के सदस्यों में हैनी बाबू का नाम नहीं था, लेकिन यह सच है कि वे साई बाबा के बिगड़ते स्वास्थ्य और उन्हें जेल में दी जा रही प्रताड़ना से लगातार चिंतित थे। संभवत: इसी समिति ने साई बाबा के मामले से संबंधित जानकारी देने वाली वे पुस्तकाएं प्रकाशित की थीं, जिन्हें हैनी बाबू के घर पर छापे के दौरान पुलिस ने जब्त किया था।
दक्षिण भारत से आने के नाते, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही विषय का शिक्षक होने के नाते भी हैनी बाबू का साई बाबा के पक्ष में खड़ा होना होना अनूठी बात नहीं थी। लेकिन उनके बीच एक और रिश्ता था, जिस पर एनआईए की नजर भले ही रही हो, लेकिन जिस तबके के लिए वे काम करते रहे हैं, उनमें से अधिकांश को इससे कोई लेना-देना नहीं है। साई बाबा और हैनी बाबू अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं तथा इस तबके को उसका जायज हक दिलाने के लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है।
आंध्रप्रदेश के अमलापुरम् में जन्मे जीएन साई बाबा का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था, उनके घर में बिजली तक नहीं थी। छुटपन में उनके पिता के पास तीन एकड़ जमीन थी, जिसमें धान की फसल लहलहाया करती थी, लेकिन साई बाबा के 10 वीं कक्षा में पहुंचने से पहले ही वे खेत कर्ज देने वाले साहूकार की भेंट चढ़ गए थे। विलक्षण मेधा के धनी साई बाबा ने अपनी पढ़ाई फ़ेलोशिप और पत्नी वसंथा (उस समय मित्र) के सहयोग से पूरी की थी। वसंथा से उनकी मित्रता 10 वीं कक्षा में ही गणित का होम-वर्क करते समय हुई थी। साई बाबा कॉलेज में नामांकन के लिए वसंथा द्वारा उपलब्ध करवाए गए टिकट के पैसे से जब पहली बार हैदराबाद गए तो उन्होंने पहली बार ट्रेन देखी। बचपन से लेकर युवावस्था का एक लंबा चरण पार हो जाने तक उनके पास व्हील चेयर तक नहीं थी और वे घुटनों के बल पर जमीन पर घिसट कर चला करते थे। 2003 में दिल्ली आने के बाद उन्होंने पहली बार व्हील चेयर खरीदी। दिल्ली ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उनकी प्रतिभा पर देश-विदेश के अध्येताओं की नजर गई और उनके शोध-पत्रों को विश्व के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर जगह मिली। उन्होंने इस दौरान पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाना जारी रखा तथा कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जारी विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी की।
एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में साई बाबा ने बताया था कि हैदराबाद में “मेरा राजनीतिक जीवन मंडल आयोग और आरक्षण की लड़ाई से शुरू हुआ।” जिसमें वसंथा भी उनके साथ शामिल थीं। उसी दौरान मार्च, 1991 में उन्होंने विवाह भी किया। वह लड़ाई वे आजीवन लड़ते रहे।
इसी प्रकार हैनी बाबू ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की अनेक बड़ी लड़ाईयां, जिस प्रकार बिना किसी आत्मप्रचार के, बहुत धैर्य और परिश्रम से लड़ीं और जीतीं वह अपने आप में एक मिसाल है।
उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 में ही 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन 2016 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करने के लिए अघोषित रूप से तरह-तरह के नियम बना रखे थे। नतीजा यह होता था कि सामान्य वर्ग में ओबीसी के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का नामांकन तो दूर, 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों में आधी से अधिक सीटें भी खाली रह जाती थीं तथा उन पर बाद में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन कर लिया जाता था।
हैनी बाबू ने इसे रोकने के लिए दलित एवं पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के फोरम “एकैडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस” के तहत सक्रिय रहते हुए अथक परिश्रम किया। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सैकड़ों आवेदन किए, अपील पर अपीलें की और उन आंकड़ों का संधान कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण की स्थिति की वह तस्वीर पेश की, जिसे देखकर हम सब हैरान रह गए। उन दिनों मैं बहुजन मुद्दों पर केंद्रित एक मासिक पत्रिका का संपादन किया करता था। हमने अपनी पत्रिका में उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया था – “ओबीसी सीटों की लूट”! ओबीसी आरक्षण के नाम पर केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सरकार ने विद्यार्थियों की भर्ती 54 प्रतिशत बढ़ा दी थी, ताकि अनारक्षित वर्ग को जाने वाली सीटों में कमी न हो और उन्हें इसके लिए सैकड़ों करोड़ रूपए का अनुदान भी मिला था, लेकिन हैनी बाबू द्वारा जमा किए गए आंकड़े साफ तौर पर बता रहे थे इसका फायदा वास्तव में द्विज समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को हो रहा था और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों विद्यार्थियों को साल दर साल उनके वाजिब हक से वंचित किया जा रहा था।
हैनी बाबू द्वारा जमा किए गए इन आंकड़ों को उनके संगठन ने ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं तक पहुंचाया, जिससे उसकी गूंज संसद में भी पहुंची। हैनी बाबू की इस मुहिम में उनके संगठन के एक और पिछड़े वर्ग से आने वाले शिक्षक केदार मंडल निरंतर शामिल रहते थे। केदार भी साई बाबा की तरह शारीरिक रूप से अक्षम हैं। दो वर्ष पहले उन पर भी हिंदू भावनाओं के अपमान के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था तथा उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया था।
हैनी बाबू द्वारा संकलित उन आंकड़ों के प्रकाश में आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के लिए ओबीसी सीटों की लूट जारी रखना संभव नहीं रह गया। 2016 के बाद से हर साल दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों अतिरिक्त विद्यार्थी देश के दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में नामांकन पाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम को ही हैनी बाबू के नाम की भी जानकारी होगी।
 इसी प्रकार 2018 में जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर दिया गया, जिससे दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग की हजारों सीटें कम हो गईं तो उसके विरोध को व्यवस्थित करने में हैनी बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। इन संघर्षों ने उन्हें आरक्षण संबंधी जटिल नियमों का इनसाक्लोपीडिया बना दिया था। जिसे भी इससे कोई भी जानकारी चाहिए होती, वह उन्हें ही फोन लगाता और वे हरसंभव जानकारी देते। उन्होंने उस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जारी विज्ञापनों में दलित, ओबीसी और आदिवासी सीटों की गणना करके बताया कि किस प्रकार रोस्टर में होने वाला यह परिवर्तन इन वर्गों के हितों पर भारी कुठराघात है। उस लड़ाई में भी बहुजन तबक़ों की जीत हुई और सरकार को आरक्षण बहाल करने के लिए नए नियम बनाने पड़े।
बहरहाल, हैनी बाबू और साई बाबा जैसे लोगों द्वारा किए गए संघर्ष और उनकी प्रताड़ना का एक और ऐसा पहलू है, जिस पर प्राय: नजर नहीं जाती। साई बाबा के मामले पर नजर रखने वाले अनेक पत्रकारों ने लिखा है कि उन्हें जिस प्रकार आजीवन कारावास की सजा हुई वह अपने आप में न्यायपालिक का एक “इतिहास” है। ऐसा संभवत: पहली बार हुआ था कि किसी मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई सभी की सभी धाराओं को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले में आरोपित सभी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साई बाबा जैसे लोग उस कमजोर सामाजिक समुदाय का हिस्सा थे, जिसमें इस प्रकार की लड़ाइयों में अपने लोगों के साथ खड़ा होने की क्षमता नहीं है।
साई बाबा के मामले को नजदीक से देखने वाले पी. विक्टर विजय ने अपने एक लेख में लिखा है कि प्रोफेसर साई बाबा ने अपने श्रम और मेधा से बहुत मूल्यवान बौद्धिक पूंजी का निर्माण किया, लेकिन वह उनकी लुटी-पिटी सामाजिक पूंजी से मेल नहीं खाती थी। वे देशी-विदेशी अकादमिक दायरे में सबसे संतुलित और तीक्ष्ण विचारों वाले बौद्धिक के रूप में जाने जाने लगे थे। लेकिन उनके समुदाय के पास वास्तव में उतनी सामाजिक पूंजी थी ही नहीं, जितनी कि इस प्रकार की सक्रियता के लिए आवश्यक होती है। यही कारण था कि वे समान आरोपों में समय-समय पर फंसाए जाते रहे द्विज बौद्धिकों की तुलना में उन्हें अपनी जनपक्षधर सक्रियता की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी।
साई बाबा को मुकदमे के दौरान कानूनी-परामर्श की कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके प्रयास एक सीमा से आगे जाने में असमर्थ थे। हैनी बाबू की गिरफ्तारी पर विचार करते हुए हमें इन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बहुजन तबके से आने वाले अन्य लोगों की ही तरह उन्हें भी समान आरोपों से घिरे अनेक लोगों की तुलना में अधिक आर्थिक, नैतिक और कानूनी संबल की आवश्यकता होगी।
इसी प्रकार 2018 में जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर दिया गया, जिससे दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग की हजारों सीटें कम हो गईं तो उसके विरोध को व्यवस्थित करने में हैनी बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। इन संघर्षों ने उन्हें आरक्षण संबंधी जटिल नियमों का इनसाक्लोपीडिया बना दिया था। जिसे भी इससे कोई भी जानकारी चाहिए होती, वह उन्हें ही फोन लगाता और वे हरसंभव जानकारी देते। उन्होंने उस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जारी विज्ञापनों में दलित, ओबीसी और आदिवासी सीटों की गणना करके बताया कि किस प्रकार रोस्टर में होने वाला यह परिवर्तन इन वर्गों के हितों पर भारी कुठराघात है। उस लड़ाई में भी बहुजन तबक़ों की जीत हुई और सरकार को आरक्षण बहाल करने के लिए नए नियम बनाने पड़े।
बहरहाल, हैनी बाबू और साई बाबा जैसे लोगों द्वारा किए गए संघर्ष और उनकी प्रताड़ना का एक और ऐसा पहलू है, जिस पर प्राय: नजर नहीं जाती। साई बाबा के मामले पर नजर रखने वाले अनेक पत्रकारों ने लिखा है कि उन्हें जिस प्रकार आजीवन कारावास की सजा हुई वह अपने आप में न्यायपालिक का एक “इतिहास” है। ऐसा संभवत: पहली बार हुआ था कि किसी मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई सभी की सभी धाराओं को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले में आरोपित सभी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साई बाबा जैसे लोग उस कमजोर सामाजिक समुदाय का हिस्सा थे, जिसमें इस प्रकार की लड़ाइयों में अपने लोगों के साथ खड़ा होने की क्षमता नहीं है।
साई बाबा के मामले को नजदीक से देखने वाले पी. विक्टर विजय ने अपने एक लेख में लिखा है कि प्रोफेसर साई बाबा ने अपने श्रम और मेधा से बहुत मूल्यवान बौद्धिक पूंजी का निर्माण किया, लेकिन वह उनकी लुटी-पिटी सामाजिक पूंजी से मेल नहीं खाती थी। वे देशी-विदेशी अकादमिक दायरे में सबसे संतुलित और तीक्ष्ण विचारों वाले बौद्धिक के रूप में जाने जाने लगे थे। लेकिन उनके समुदाय के पास वास्तव में उतनी सामाजिक पूंजी थी ही नहीं, जितनी कि इस प्रकार की सक्रियता के लिए आवश्यक होती है। यही कारण था कि वे समान आरोपों में समय-समय पर फंसाए जाते रहे द्विज बौद्धिकों की तुलना में उन्हें अपनी जनपक्षधर सक्रियता की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी।
साई बाबा को मुकदमे के दौरान कानूनी-परामर्श की कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके प्रयास एक सीमा से आगे जाने में असमर्थ थे। हैनी बाबू की गिरफ्तारी पर विचार करते हुए हमें इन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बहुजन तबके से आने वाले अन्य लोगों की ही तरह उन्हें भी समान आरोपों से घिरे अनेक लोगों की तुलना में अधिक आर्थिक, नैतिक और कानूनी संबल की आवश्यकता होगी।
[फारवर्ड प्रेस नामक पत्रिका के प्रबंध संपादक रहे प्रमोद रंजन की दिलचस्पी सबाल्टर्न अध्ययन और आधुनिकता के विकास में रही है। पेरियार के लेखन और भाषणों का उनके द्वारा संपादित संकलन तीन खंड में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। संपर्क: 9811884495, janvikalp@gmail.com
टॉपर है डॉ. आंबेडकर की नई पीढ़ी
 पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर घूमती कुछ तस्वीरों को देख रहे होंगे। देश के तमाम राज्यों और जिले से टॉपरों की सूची में शामिल ये नाम गर्व करने वाले हैं। ये वो नाम हैं, जिन्होंने हाल ही में आए दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप किया है। कुछ ने अपने राज्य में तो कईयों ने अपने जिलों में। खास बात यह है कि इसमें कुछ नाम ऐसे भी शामिल हैं, जिन्होंने तमाम अभाव और गरीबी के बावजूद लाखों मेरिटधारियों को पछाड़ दिया है।
पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर घूमती कुछ तस्वीरों को देख रहे होंगे। देश के तमाम राज्यों और जिले से टॉपरों की सूची में शामिल ये नाम गर्व करने वाले हैं। ये वो नाम हैं, जिन्होंने हाल ही में आए दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप किया है। कुछ ने अपने राज्य में तो कईयों ने अपने जिलों में। खास बात यह है कि इसमें कुछ नाम ऐसे भी शामिल हैं, जिन्होंने तमाम अभाव और गरीबी के बावजूद लाखों मेरिटधारियों को पछाड़ दिया है।
 अब आपको झारखंड ले चलते हैं। झारखंड में लीजा उरांव सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में पूरे झारखंड में टॉपर बनी हैं। उन्होंने 99 फीसद अंक हासिल किया हैं। लीजा को इंग्लिश में 99, हिदी में 100, मैथ में 98, साइंस में 99, सोशल साइंस में 98 और आइटी में 100 अंक मिले हैं। कटहल मोड़ की रहने वाली लीजा उरांव के पिता दशरथ उरांव और माता संयुक्त कच्छप दोनों टीचर हैं। माता-पिता और नानी लीजा के प्रेरणास्रोत हैं। लीजा के दिल में अपने समाज के लिए काफी दर्द है, और वह उसकी बेहतरी के लिए काफी कुछ करना चाहती हैं। परिणाम आने के बाद स्थानीय मीडिया से बातचीत में लीजा ने कहा कि वह आगे चलकर आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती हैं। लीजा भी तुषार की तरह सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। झारखंड बनने के बाद यह पहला मौका है जब आदिवासी समाज का कोई बच्चा स्टेट टॉपर बना है।
अब पंजाब चलिए। पंजाब में इन दिनों जसप्रीत कौर का नाम चर्चा का विषय है। जसप्रीत ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। जसप्रीत ने अपनी मेहनत के बूते 99.5 प्रतिशत अंक हासिल किया है। जसप्रीत ने 450 अंकों में से 448 अंक हासिल किया है।
अब आपको झारखंड ले चलते हैं। झारखंड में लीजा उरांव सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में पूरे झारखंड में टॉपर बनी हैं। उन्होंने 99 फीसद अंक हासिल किया हैं। लीजा को इंग्लिश में 99, हिदी में 100, मैथ में 98, साइंस में 99, सोशल साइंस में 98 और आइटी में 100 अंक मिले हैं। कटहल मोड़ की रहने वाली लीजा उरांव के पिता दशरथ उरांव और माता संयुक्त कच्छप दोनों टीचर हैं। माता-पिता और नानी लीजा के प्रेरणास्रोत हैं। लीजा के दिल में अपने समाज के लिए काफी दर्द है, और वह उसकी बेहतरी के लिए काफी कुछ करना चाहती हैं। परिणाम आने के बाद स्थानीय मीडिया से बातचीत में लीजा ने कहा कि वह आगे चलकर आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती हैं। लीजा भी तुषार की तरह सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। झारखंड बनने के बाद यह पहला मौका है जब आदिवासी समाज का कोई बच्चा स्टेट टॉपर बना है।
अब पंजाब चलिए। पंजाब में इन दिनों जसप्रीत कौर का नाम चर्चा का विषय है। जसप्रीत ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। जसप्रीत ने अपनी मेहनत के बूते 99.5 प्रतिशत अंक हासिल किया है। जसप्रीत ने 450 अंकों में से 448 अंक हासिल किया है।
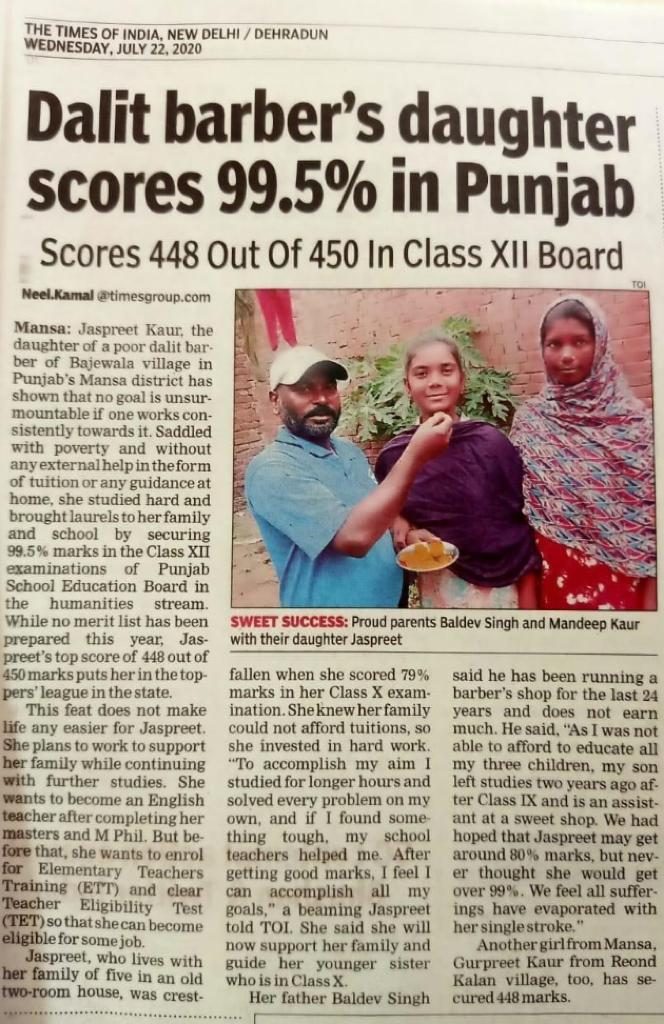 बेहद गरीबी में पलने वाली जसप्रीत के पिता एक नाई हैं, और लोगों के बाल काटते हैं। जसप्रीत ने न तो कोई ट्यूशन किया और न ही उन्हें गाईड करने वाला ही कोई था, बावजूद इसके कड़ी मेहनत के बूते जसप्रीत ने यह मुकाम हासिल किया और बता दिया की नामुमकिन कुछ भी नहीं। जसप्रीत का सपना उच्च शिक्षा का है। वह एम.ए और एम.फिल के बाद इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हैं।
जसप्रीत के पिता बलदेव सिंह पिछले 24 साल से नाई का काम करते हैं। मां मनदीप कौर गृहणी हैं। परिवार गरीबी में जीता है। जसप्रीत ने 10वीं में 79 प्रतिशत अंक हासिल किया था। तब उन्हें पता था कि उनके पिता ट्यूशन कराने में सक्षम नहीं हैं, सो उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद पर भरोसा रखा और 12वीं में अव्वल आईँ।
पंजाब के बाद राजस्थान में भी एससी समाज के युवा ने परचम लहराया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी 12वीं के परिणाम में प्रकाश फुलवारिया टॉपर बने हैं। प्रकाश 99.20 प्रतिशत लाते हुए 500 नंबरों में 496 अंक हासिल कर टॉपर बने हैं। प्रकाश की तैयारी इतनी शानदार थी कि 496 अंक आने के बावजूद वो असमंजस में हैं कि उनके 4 नंबर क्यों कट गए। उनके पिता का नाम चन्ना राम और मां का नाम संतोष देवी है।
अब प्रकाश के नंबरों पर नजर डालते हैं। अपनी मेहनत के बूते प्रकाश ने हिन्दी में 100 अंक, इंग्लिश में 99 अंक,
बेहद गरीबी में पलने वाली जसप्रीत के पिता एक नाई हैं, और लोगों के बाल काटते हैं। जसप्रीत ने न तो कोई ट्यूशन किया और न ही उन्हें गाईड करने वाला ही कोई था, बावजूद इसके कड़ी मेहनत के बूते जसप्रीत ने यह मुकाम हासिल किया और बता दिया की नामुमकिन कुछ भी नहीं। जसप्रीत का सपना उच्च शिक्षा का है। वह एम.ए और एम.फिल के बाद इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हैं।
जसप्रीत के पिता बलदेव सिंह पिछले 24 साल से नाई का काम करते हैं। मां मनदीप कौर गृहणी हैं। परिवार गरीबी में जीता है। जसप्रीत ने 10वीं में 79 प्रतिशत अंक हासिल किया था। तब उन्हें पता था कि उनके पिता ट्यूशन कराने में सक्षम नहीं हैं, सो उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद पर भरोसा रखा और 12वीं में अव्वल आईँ।
पंजाब के बाद राजस्थान में भी एससी समाज के युवा ने परचम लहराया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी 12वीं के परिणाम में प्रकाश फुलवारिया टॉपर बने हैं। प्रकाश 99.20 प्रतिशत लाते हुए 500 नंबरों में 496 अंक हासिल कर टॉपर बने हैं। प्रकाश की तैयारी इतनी शानदार थी कि 496 अंक आने के बावजूद वो असमंजस में हैं कि उनके 4 नंबर क्यों कट गए। उनके पिता का नाम चन्ना राम और मां का नाम संतोष देवी है।
अब प्रकाश के नंबरों पर नजर डालते हैं। अपनी मेहनत के बूते प्रकाश ने हिन्दी में 100 अंक, इंग्लिश में 99 अंक, 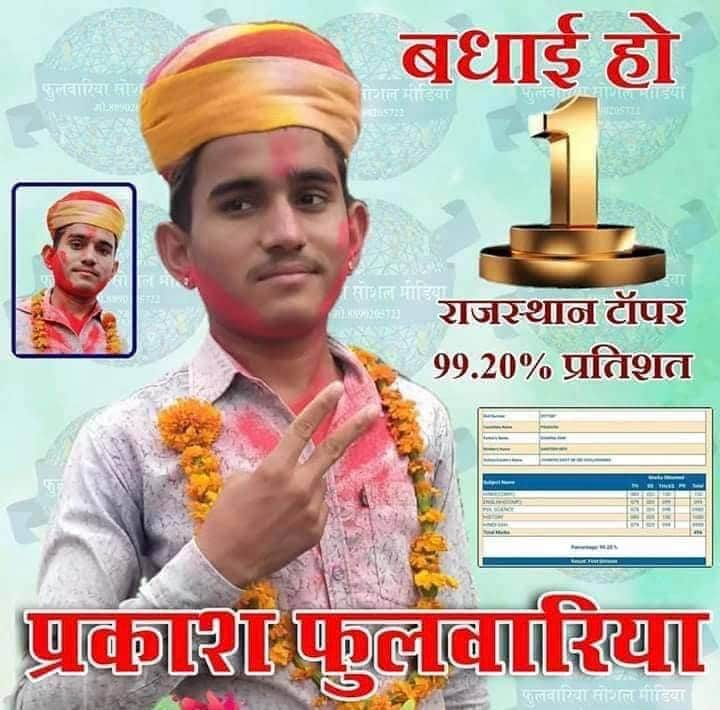 पोलिटिकल साइंस में 98, हिस्ट्री में 100 और हिन्दी साहित्य में 99 अंक हासिल किया है। प्रकाश के पिता चनणाराम कमठा एक मजदूर हैं। प्रकाश आईएएस बनना चाहते हैं।
जिलों में भी बाबासाहेब के बच्चों ने शानदार सफलता हासिल की है।
हरियाणा की प्रेरणा दयाल ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में गुरुग्राम जिले की टापर बनी हैं। प्रदेश में उनका स्थान पांचवा है। प्रेरणा ने 500 अंकों में से 493 अंक हासिल किए हैं। प्रेरणा का परिवार अंबेडकरवादी है। प्रेरणा आगे कानून की पढ़ाई कर जज बनना चाहती हैं। प्रेरणा के आदर्श बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रेरणा देशहित में और महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करना चाहती हैं। प्रेरणा के पिता राम किशोर दयाल और मां सीमा दयाल हैं। प्रेरणा के बड़े पिता आर. के दयाल तो अम्बेडकरी आंदोलन में खासे सक्रिय हैं। गुरुग्राम जिले में ही साईकिल रिपेयर करने वाले पिता की बेटी मीनू ने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है।
तो दूसरी ओर यूपी के मेरठ जिले में आयुषि राज 99.2 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉपर बनी हैं।
पोलिटिकल साइंस में 98, हिस्ट्री में 100 और हिन्दी साहित्य में 99 अंक हासिल किया है। प्रकाश के पिता चनणाराम कमठा एक मजदूर हैं। प्रकाश आईएएस बनना चाहते हैं।
जिलों में भी बाबासाहेब के बच्चों ने शानदार सफलता हासिल की है।
हरियाणा की प्रेरणा दयाल ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में गुरुग्राम जिले की टापर बनी हैं। प्रदेश में उनका स्थान पांचवा है। प्रेरणा ने 500 अंकों में से 493 अंक हासिल किए हैं। प्रेरणा का परिवार अंबेडकरवादी है। प्रेरणा आगे कानून की पढ़ाई कर जज बनना चाहती हैं। प्रेरणा के आदर्श बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रेरणा देशहित में और महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करना चाहती हैं। प्रेरणा के पिता राम किशोर दयाल और मां सीमा दयाल हैं। प्रेरणा के बड़े पिता आर. के दयाल तो अम्बेडकरी आंदोलन में खासे सक्रिय हैं। गुरुग्राम जिले में ही साईकिल रिपेयर करने वाले पिता की बेटी मीनू ने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है।
तो दूसरी ओर यूपी के मेरठ जिले में आयुषि राज 99.2 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉपर बनी हैं।
 मैंने जिन बच्चों का भी जिक्र किया, उनमें दो बातें कॉमन है। पहली बात सभी टॉपर हैं। किसी ने प्रदेश में तो किसी ने अपने जिले में टॉप किया है। दूसरी बात सब के सब एससी-एसटी समाज के बच्चे हैं, जिन्हें आमतौर पर अंडरमेरिट मान कर खारिज कर देने का रिवाज रहा है। लेकिन इन बच्चों में कईयों ने अभाव के बीच सफलता हासिल कर बता दिया है कि वो बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के वंशज हैं, जिन्हें दुनिया विद्वान मानती है। वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, जिन्होंने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा था। खासबात यह भी है कि इन टॉपर्स में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। और तमाम युवा बाबासाहेब सहित बहुजन नायकों को अपना आदर्श मानते हैं। साफ है कि यह बाबासाहेब आंबेडकर के समाज की नई पीढ़ी है, जिसने मौका मिलते ही साबित कर दिया है कि मेरिट किसी के घर की बपौती नहीं होती, बस मौका मिलना चाहिए।
मैंने जिन बच्चों का भी जिक्र किया, उनमें दो बातें कॉमन है। पहली बात सभी टॉपर हैं। किसी ने प्रदेश में तो किसी ने अपने जिले में टॉप किया है। दूसरी बात सब के सब एससी-एसटी समाज के बच्चे हैं, जिन्हें आमतौर पर अंडरमेरिट मान कर खारिज कर देने का रिवाज रहा है। लेकिन इन बच्चों में कईयों ने अभाव के बीच सफलता हासिल कर बता दिया है कि वो बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के वंशज हैं, जिन्हें दुनिया विद्वान मानती है। वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, जिन्होंने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा था। खासबात यह भी है कि इन टॉपर्स में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। और तमाम युवा बाबासाहेब सहित बहुजन नायकों को अपना आदर्श मानते हैं। साफ है कि यह बाबासाहेब आंबेडकर के समाज की नई पीढ़ी है, जिसने मौका मिलते ही साबित कर दिया है कि मेरिट किसी के घर की बपौती नहीं होती, बस मौका मिलना चाहिए।
हिंदी पट्टी में पेरियार
 पेरियार के मूल तमिल लेखन का हिंदी अनुवाद अभी तक उपलब्ध नहीं था, इस कारण उनकी वैचारिकी से हिंदी क्षेत्रों के दलित-बहुजन आंदोलन का उस तरह का सघन और सक्रिय रिश्ता विकसित नहीं हो पाया, जैसा कि डॉ. आम्बेडकर और बहुत हद तक जोतिराव फुले से हो सका है। इस कमी को बहुजन साहित्य के अध्येता प्रमोद रंजन ने पेरियार पर केंद्रित तीन पुस्तकों की ऋंखला का संपादन कर पूरा किया है, जिन्हें राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है।
5 अगस्त को अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण के लिए भूमि-पूजन होना है। उससे ठीक पहले आई इन किताबों, विशेषकर पेरियार की “सच्ची-रामायण” के प्रकाशन को सांप्रदायिक शक्तियों को प्रगतिशील व दलित-बहुजन समाज के एक सशक्त उत्तर के रूप में भी देखा जा रहा है।
यही कारण है कि इन किताबों के बाजार में आते ही हिंदी की द्विजवादी बौद्धिक दुनिया भड़क उठी है। हम यहां ‘दलित-दस्तक’ के पाठकों के लिए पुस्तक श्रृंखला के संपादक प्रमोद रंजन की एक इससे संंबंधित टिप्पणी और पुस्तक का संपादकीय उपलब्ध करवा रहे हैं। रंजन ने अपनी टिप्पणी में हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पेरियार संबंधी अज्ञान पर प्रकाश डाला है तथा पेरियार का विरोध करने वाले लेखकों की खबर ली है।
– संपादक, दलित-दस्तक
पेरियार के मूल तमिल लेखन का हिंदी अनुवाद अभी तक उपलब्ध नहीं था, इस कारण उनकी वैचारिकी से हिंदी क्षेत्रों के दलित-बहुजन आंदोलन का उस तरह का सघन और सक्रिय रिश्ता विकसित नहीं हो पाया, जैसा कि डॉ. आम्बेडकर और बहुत हद तक जोतिराव फुले से हो सका है। इस कमी को बहुजन साहित्य के अध्येता प्रमोद रंजन ने पेरियार पर केंद्रित तीन पुस्तकों की ऋंखला का संपादन कर पूरा किया है, जिन्हें राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है।
5 अगस्त को अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण के लिए भूमि-पूजन होना है। उससे ठीक पहले आई इन किताबों, विशेषकर पेरियार की “सच्ची-रामायण” के प्रकाशन को सांप्रदायिक शक्तियों को प्रगतिशील व दलित-बहुजन समाज के एक सशक्त उत्तर के रूप में भी देखा जा रहा है।
यही कारण है कि इन किताबों के बाजार में आते ही हिंदी की द्विजवादी बौद्धिक दुनिया भड़क उठी है। हम यहां ‘दलित-दस्तक’ के पाठकों के लिए पुस्तक श्रृंखला के संपादक प्रमोद रंजन की एक इससे संंबंधित टिप्पणी और पुस्तक का संपादकीय उपलब्ध करवा रहे हैं। रंजन ने अपनी टिप्पणी में हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पेरियार संबंधी अज्ञान पर प्रकाश डाला है तथा पेरियार का विरोध करने वाले लेखकों की खबर ली है।
– संपादक, दलित-दस्तक
Written By- प्रमोद रंजन ‘हिंदी पट्टी में पेरियार’ विषय पर बात करनी हो तो, एक चालू वाक्य को उलट कर कहने पर बात अधिक तथ्यगत होगी। वह यह कि पेरियार के विचार हिंदी की दुनिया में परिचय के मोहताज हैं! उत्तर भारत, दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी, दार्शनिक और देश एक बड़े हिस्से में सामाजिक-संतुलन की विधियों और राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले ईवी रामासामी पेरियार (17 सितम्बर, 1879-24 दिसम्बर, 1973) के बौद्धिक योगदान के विविध आयामों से अपरिचित हैं। यह सुनने में अजीब है, लेकिन सच है। जबकि स्वयं पेरियार चाहते थे कि उनके विचार उत्तर भारत के प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अपने जीवनकाल में उत्तर भारत के कई दौरे किए और विभिन्न जगहों पर भाषण दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ लेखों व एक पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख बहुजन कार्यकर्ताओं, क्रमशः चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और ललई सिंह को दिए थे। लेकिन वह बात न हो सकी, जो पेरियार चाहते थे।
 उत्तर भारत में आज भी पेरियार को मुख्य रूप से नास्तिक और हिंदी विरोधी के रूप में जाना जाता है। यह गलत तो नहीं, लेकिन उनका एकांगी चित्रण अवश्य है। उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की, लेकिन उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया। डॉ. आंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उन्होंने स्वागत किया और उसे ऐतिहासिक दिन बताया। इसी तरह उनका हिंदी-विरोध सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का विरोध था, जिसने बाद के वर्षों में दक्षिण और उत्तर भारत में राजनीतिक संतुलन बनाया और देश की अखंडता को संभव किया। वे हिंदी भाषा के विरोधी नहीं थे। इन चीजों से इतर पेरियार ने विवाह संस्था, स्त्रियों की आजादी, साहित्य के महत्ता और उपयोग, भारतीय मार्क्सवाद की कमजोरियों, गांधीवाद और उदारवाद की असली मंशा और पाखंड आदि पर जिस मौलिकता से विचार किया है, उसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। वे अपने काल तक ही सीमित नहीं थे, उनसे दृष्टि निरंतर भविष्य पर बनी रही। विज्ञान और तकनीक भी उनके प्रिय विषय थे। यही कारण है कि आज के उत्तर सूचना-युग में भी हम उनकी भविष्यवाणियों को फलीभूत होते देख रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों में हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आन्दोलनों व अकादमियों में समाज के वंचित तबकों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वे सिर्फ ‘नास्तिक पेरियार’ से परिचित हैं। हालांकि उनके इस रूप के प्रति नई पीढ़ी में जबरदस्त आकर्षण भी है। लेकिन उसने वस्तुत: पेरियार को पढ़ा नहीं है। इस पीढ़ी के पास पेरियार के विचारों के बारे में कुछ सुनी-सुनाई, आधी-अधूरी बातें ही हैं। यह स्वभाविक है क्योंकि हिंदी में अब तक पेरियार का साहित्य उपलब्ध नहीं था।
सकते में डाल देने वाली इस कमी का अहसास मुझे वर्ष 2011 में हुआ था। उन दिनाें मैं नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। अपने एक लेख के लिए मुझे ई.वी. रामासामी पेरियार के विचारों को जानने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन, यह जानकर हैरानी हुई कि ‘सच्ची रामायण’ के अतिरिक्त उनका कोई भी साहित्य हिंदी में उपलब्ध ही नहीं है। 1970 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ‘ई.वी. रामासामी पेरियार नायकर’ नाम पेरियार के कुछ लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था। वह भी अनुपलब्ध था।
उत्तर भारत में आज भी पेरियार को मुख्य रूप से नास्तिक और हिंदी विरोधी के रूप में जाना जाता है। यह गलत तो नहीं, लेकिन उनका एकांगी चित्रण अवश्य है। उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की, लेकिन उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया। डॉ. आंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उन्होंने स्वागत किया और उसे ऐतिहासिक दिन बताया। इसी तरह उनका हिंदी-विरोध सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का विरोध था, जिसने बाद के वर्षों में दक्षिण और उत्तर भारत में राजनीतिक संतुलन बनाया और देश की अखंडता को संभव किया। वे हिंदी भाषा के विरोधी नहीं थे। इन चीजों से इतर पेरियार ने विवाह संस्था, स्त्रियों की आजादी, साहित्य के महत्ता और उपयोग, भारतीय मार्क्सवाद की कमजोरियों, गांधीवाद और उदारवाद की असली मंशा और पाखंड आदि पर जिस मौलिकता से विचार किया है, उसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। वे अपने काल तक ही सीमित नहीं थे, उनसे दृष्टि निरंतर भविष्य पर बनी रही। विज्ञान और तकनीक भी उनके प्रिय विषय थे। यही कारण है कि आज के उत्तर सूचना-युग में भी हम उनकी भविष्यवाणियों को फलीभूत होते देख रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों में हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आन्दोलनों व अकादमियों में समाज के वंचित तबकों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वे सिर्फ ‘नास्तिक पेरियार’ से परिचित हैं। हालांकि उनके इस रूप के प्रति नई पीढ़ी में जबरदस्त आकर्षण भी है। लेकिन उसने वस्तुत: पेरियार को पढ़ा नहीं है। इस पीढ़ी के पास पेरियार के विचारों के बारे में कुछ सुनी-सुनाई, आधी-अधूरी बातें ही हैं। यह स्वभाविक है क्योंकि हिंदी में अब तक पेरियार का साहित्य उपलब्ध नहीं था।
सकते में डाल देने वाली इस कमी का अहसास मुझे वर्ष 2011 में हुआ था। उन दिनाें मैं नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। अपने एक लेख के लिए मुझे ई.वी. रामासामी पेरियार के विचारों को जानने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन, यह जानकर हैरानी हुई कि ‘सच्ची रामायण’ के अतिरिक्त उनका कोई भी साहित्य हिंदी में उपलब्ध ही नहीं है। 1970 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ‘ई.वी. रामासामी पेरियार नायकर’ नाम पेरियार के कुछ लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था। वह भी अनुपलब्ध था।
 ‘सच्ची रामायण’ का जो अनुवाद उपलब्ध था, वह भी शुद्ध नहीं था। अंग्रेजी से मिलान करने पर साफ पता चल रहा था कि कई हिस्सों का अनुवाद ही नहीं किया गया है तथा कई स्थानों पर अनुवादक/प्रकाशक ने अपनी भावनाओं का समावेश कर दिया है। इस दिशा में खोजबीन करने पर सच्ची रामायण के हिंदी में प्रचार-प्रसार और राजनीतिक उपयोग-उपेक्षा के बारे कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी मिलीं।
राम-कथा की व्याख्या पर केन्द्रित पेरियार की रामायण मूल रूप से तमिल में 1944 में छपी थी। तमिल में इसका नाम था – ‘रामायण पातिरंगल (रामायण के चरित्र)’ अंग्रेजी में यह 1959 में ‘द रामायण : अ ट्रू रीडिंग’ शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद ‘सच्ची रामायण’ शीर्षक से किन्हीं रामाधार ने किया था; जो 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक ललई सिंह (1 सितंबर, 1911- 7 फरवरी, 1993) ने प्रकाशित किया था। बाद के वर्षों में वे स्वयं भी अपने प्रशंसकों के बीच ‘पेरियार ललई सिंह’ और उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने गए।
उन्होंने सिर्फ इसे प्रकाशित ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार-प्रसार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे राम-पूजक उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिसंबर, 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को (सिर्फ हिंदी अनुवाद नहीं) हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया और हिंदी अनुवाद की प्रतियां जब्त कर ली। ललई सिंह यादव ने इसके खिलाफ लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 1976 के अपने फैसले में इस किताब पर प्रतिबंध को गलत बताया एवं जब्त की गई प्रतियां ललई सिंह को लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन, कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘सच्ची रामायण’ से प्रतिबंध नहीं हटाया। 1995 में प्रदेश में पेरियार को अपने प्रमुख आदर्शों में गिनने वाले कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सत्ता में आई, तब जाकर इससे प्रतिबंध हटा। उस समय बसपा कांशीराम के हाथ में थी और वे दलित-ओबीसी नायकों का राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहे थे।
‘सच्ची रामायण’ का जो अनुवाद उपलब्ध था, वह भी शुद्ध नहीं था। अंग्रेजी से मिलान करने पर साफ पता चल रहा था कि कई हिस्सों का अनुवाद ही नहीं किया गया है तथा कई स्थानों पर अनुवादक/प्रकाशक ने अपनी भावनाओं का समावेश कर दिया है। इस दिशा में खोजबीन करने पर सच्ची रामायण के हिंदी में प्रचार-प्रसार और राजनीतिक उपयोग-उपेक्षा के बारे कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी मिलीं।
राम-कथा की व्याख्या पर केन्द्रित पेरियार की रामायण मूल रूप से तमिल में 1944 में छपी थी। तमिल में इसका नाम था – ‘रामायण पातिरंगल (रामायण के चरित्र)’ अंग्रेजी में यह 1959 में ‘द रामायण : अ ट्रू रीडिंग’ शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद ‘सच्ची रामायण’ शीर्षक से किन्हीं रामाधार ने किया था; जो 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक ललई सिंह (1 सितंबर, 1911- 7 फरवरी, 1993) ने प्रकाशित किया था। बाद के वर्षों में वे स्वयं भी अपने प्रशंसकों के बीच ‘पेरियार ललई सिंह’ और उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने गए।
उन्होंने सिर्फ इसे प्रकाशित ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार-प्रसार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे राम-पूजक उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिसंबर, 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को (सिर्फ हिंदी अनुवाद नहीं) हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया और हिंदी अनुवाद की प्रतियां जब्त कर ली। ललई सिंह यादव ने इसके खिलाफ लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 1976 के अपने फैसले में इस किताब पर प्रतिबंध को गलत बताया एवं जब्त की गई प्रतियां ललई सिंह को लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन, कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘सच्ची रामायण’ से प्रतिबंध नहीं हटाया। 1995 में प्रदेश में पेरियार को अपने प्रमुख आदर्शों में गिनने वाले कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सत्ता में आई, तब जाकर इससे प्रतिबंध हटा। उस समय बसपा कांशीराम के हाथ में थी और वे दलित-ओबीसी नायकों का राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहे थे।
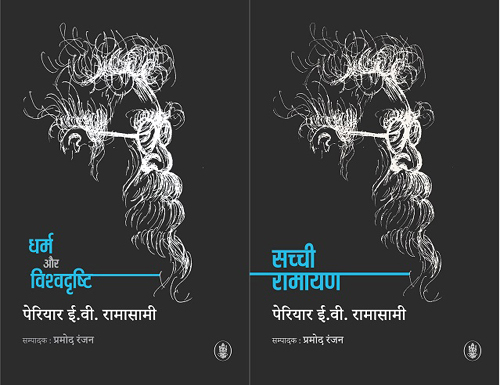 लेकिन पेरियार के विचार तब भी हिंदी भाषी जनता तक नहीं पहुंच सके। कांशीराम की मुख्य प्रतिबद्धता दलित समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति थी। उन्होंने पेरियार मेला का भी आयोजन किया। नायकों की मूर्तियों की स्थापना, मेलों का आयोजन आदि शीघ्र फल देने वाले बहुत महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन कांशीराम से इन नायकों के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने की उम्मीद करना अतिरेक ही कहा जाएगा। यह बीड़ा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे समतावादी कार्यकर्ताओं को उठाना चाहिए था। लेकिन यह नहीं हुआ।
यही कारण था कि, 2007 में जब उत्तर प्रदेश में ‘सच्ची रामायण’ का एक बार फिर जोरदार विरोध हुआ था, तब बसपा को पेरियार से कन्नी काटनी पड़ी। विरोधियों के प्रश्नों का उसके पास सैद्धांतिक उत्तर नहीं था। उस समय भी बसपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और मायावती ही मुख्यमंत्री थीं।
अक्टूबर, 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया कि वह सरकार के सहयोग से ‘सच्ची रामायण’ का प्रचार-प्रसार कर रही है तथा बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री की जा रही है। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। इसलिए यह मामला मीडिया में भी खूब गूंजा। भाजपा विधानमंडल दल के नेता ओमप्रकाश सिंह का कहना था कि “हिंदू देवी-देवताओं के विरोधी तथा द्रविड़िस्तान की मांग करने वाले अलगाववादी पेरियार रामासामी की सरकार निंदा करे तथा उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में न माने।“ इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का उत्तर अप्रत्याशित था। मायावती ने कहा कि ‘‘बसपा तथा सरकार का पेरियार की सच्ची रामायण की बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है।’’
लेकिन पेरियार के विचार तब भी हिंदी भाषी जनता तक नहीं पहुंच सके। कांशीराम की मुख्य प्रतिबद्धता दलित समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति थी। उन्होंने पेरियार मेला का भी आयोजन किया। नायकों की मूर्तियों की स्थापना, मेलों का आयोजन आदि शीघ्र फल देने वाले बहुत महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन कांशीराम से इन नायकों के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने की उम्मीद करना अतिरेक ही कहा जाएगा। यह बीड़ा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे समतावादी कार्यकर्ताओं को उठाना चाहिए था। लेकिन यह नहीं हुआ।
यही कारण था कि, 2007 में जब उत्तर प्रदेश में ‘सच्ची रामायण’ का एक बार फिर जोरदार विरोध हुआ था, तब बसपा को पेरियार से कन्नी काटनी पड़ी। विरोधियों के प्रश्नों का उसके पास सैद्धांतिक उत्तर नहीं था। उस समय भी बसपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और मायावती ही मुख्यमंत्री थीं।
अक्टूबर, 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया कि वह सरकार के सहयोग से ‘सच्ची रामायण’ का प्रचार-प्रसार कर रही है तथा बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री की जा रही है। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। इसलिए यह मामला मीडिया में भी खूब गूंजा। भाजपा विधानमंडल दल के नेता ओमप्रकाश सिंह का कहना था कि “हिंदू देवी-देवताओं के विरोधी तथा द्रविड़िस्तान की मांग करने वाले अलगाववादी पेरियार रामासामी की सरकार निंदा करे तथा उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में न माने।“ इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का उत्तर अप्रत्याशित था। मायावती ने कहा कि ‘‘बसपा तथा सरकार का पेरियार की सच्ची रामायण की बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है।’’
 भाजपा के विरोध और बसपा द्वारा पेरियार से रणनीतिक दूरी बना लेने की इस घटना का एक आश्चर्यजनक पक्ष भी था; जिसका पता इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर से लगता है।
पत्रकार अलका पांडेय ने 7 नवंबर, 2007 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपनी खोजी रिपोर्ट में लिखा कि, “जिस ‘सच्ची रामायण’ के लिए भाजपा और बसपा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही थीं उसकी प्रति न भाजपा के पास उपलब्ध है, न ही बसपा के पास। बसपा का सारा साहित्य बेचने वाले ‘बहुजन चेतना मंडप’ के पास भी यह किताब उपलब्ध नहीं है।’’ भाजपा इस दौरान कई जगहों पर ‘सच्ची रामायण’ के दहन का आयोजन कर रही थी। लेकिन, “जलाने के लिए भी पार्टी के पास किताब की प्रति नहीं थी। उसने जिस किताब का दहन किया, वह किताब के कथित आपत्तिजनक अंशों की फोटोकॉपी थी।”
अखबार ने अपनी पड़ताल में पाया कि “सिर्फ बसपा से जुड़े स्टॉलों पर ही नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ में किसी भी दुकान पर ‘सच्ची रामायण’ उपलब्ध नहीं है।’’ लखनऊ के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता ‘यूनिवर्सल बुक सेलर’ ने भी अखबार को बताया कि “‘सच्ची रामायण’ कभी बिक्री के लिए उपलब्ध ही नहीं थी।“
वस्तुत: ‘बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंप्लाइज फेडरेशन’ (बामसेफ) से जुड़े ‘मूलनिवासी प्रचार-प्रसार केंद्र’ तथा ‘आंबेडकर प्रचार समिति’ आदि ने ‘सच्ची रामायण’ की लाखों प्रतियां अपने समर्थकों-कार्यकर्ताओं के बीच वितरित की थीं। लेकिन, इसकी पहुंच न तो विश्वविद्यालयों तक हो सकी थी, न ही उन दुकानों तक, जहां कथित ‘मुख्यधारा’ की किताबें पढ़ने वाले लोग जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। एक ओर बहुजन तबकों को ज्ञान की कथित मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिश की जाती है, दूसरी ओर इन तबकों के पास उपलब्ध ज्ञान और उनके नायकों की यह सचेत उपेक्षा की जाती है।
बहरहाल, इन स्थितियों से चिंतित होकर मैंने वर्ष 2014 में ही तमिलनाडु निवासी विश्वविद्यालय में अपने सहपाठी मनीवन्नन मुरुगेसन और तमिल पत्रिका कत्तारू के सदस्य टी. थमराईकन्नन के साथ मिलकर पेरियार ग्रंथावली हिंदी में लाने की योजना बनाई थी।
थोड़े विषयांतर का खतरा मोल लेते हुए भी, उपरोक्त तमिल पत्रिका की विशिष्टता का उल्लेख कर देना यहां प्रासंगिक होगा।
कोयंबटूर से प्रकाशित ‘कात्तारू’अपने कलेवर, विषयों के चुनाव आदि में यह एक श्रेष्ठ और गंभीर मासिक पत्रिका है, जो आज भी नियमित प्रकाशित हो रही है। उत्तर भारत से जो साहित्यिक – वैचारिक अथवा दलित-बहुजन मुद्दों पर केंद्रित लघु पत्रिकाएँ निकलती हैं, उनमें से अधिकांश के पीछे प्राय: कोई एक व्यक्ति मिशनरी भाव से जुड़ा होता है। कुछ मामलों में तो पत्रिका के माध्यम से स्वनामधन्य हो जाने की ख्वाहिश भी काम कर रही होती है। लेकिन, कोयंबटूर में ‘कात्तारू’ की युवा टीम इससे बिलकुल अलग है।
भाजपा के विरोध और बसपा द्वारा पेरियार से रणनीतिक दूरी बना लेने की इस घटना का एक आश्चर्यजनक पक्ष भी था; जिसका पता इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर से लगता है।
पत्रकार अलका पांडेय ने 7 नवंबर, 2007 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपनी खोजी रिपोर्ट में लिखा कि, “जिस ‘सच्ची रामायण’ के लिए भाजपा और बसपा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही थीं उसकी प्रति न भाजपा के पास उपलब्ध है, न ही बसपा के पास। बसपा का सारा साहित्य बेचने वाले ‘बहुजन चेतना मंडप’ के पास भी यह किताब उपलब्ध नहीं है।’’ भाजपा इस दौरान कई जगहों पर ‘सच्ची रामायण’ के दहन का आयोजन कर रही थी। लेकिन, “जलाने के लिए भी पार्टी के पास किताब की प्रति नहीं थी। उसने जिस किताब का दहन किया, वह किताब के कथित आपत्तिजनक अंशों की फोटोकॉपी थी।”
अखबार ने अपनी पड़ताल में पाया कि “सिर्फ बसपा से जुड़े स्टॉलों पर ही नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ में किसी भी दुकान पर ‘सच्ची रामायण’ उपलब्ध नहीं है।’’ लखनऊ के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता ‘यूनिवर्सल बुक सेलर’ ने भी अखबार को बताया कि “‘सच्ची रामायण’ कभी बिक्री के लिए उपलब्ध ही नहीं थी।“
वस्तुत: ‘बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंप्लाइज फेडरेशन’ (बामसेफ) से जुड़े ‘मूलनिवासी प्रचार-प्रसार केंद्र’ तथा ‘आंबेडकर प्रचार समिति’ आदि ने ‘सच्ची रामायण’ की लाखों प्रतियां अपने समर्थकों-कार्यकर्ताओं के बीच वितरित की थीं। लेकिन, इसकी पहुंच न तो विश्वविद्यालयों तक हो सकी थी, न ही उन दुकानों तक, जहां कथित ‘मुख्यधारा’ की किताबें पढ़ने वाले लोग जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। एक ओर बहुजन तबकों को ज्ञान की कथित मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिश की जाती है, दूसरी ओर इन तबकों के पास उपलब्ध ज्ञान और उनके नायकों की यह सचेत उपेक्षा की जाती है।
बहरहाल, इन स्थितियों से चिंतित होकर मैंने वर्ष 2014 में ही तमिलनाडु निवासी विश्वविद्यालय में अपने सहपाठी मनीवन्नन मुरुगेसन और तमिल पत्रिका कत्तारू के सदस्य टी. थमराईकन्नन के साथ मिलकर पेरियार ग्रंथावली हिंदी में लाने की योजना बनाई थी।
थोड़े विषयांतर का खतरा मोल लेते हुए भी, उपरोक्त तमिल पत्रिका की विशिष्टता का उल्लेख कर देना यहां प्रासंगिक होगा।
कोयंबटूर से प्रकाशित ‘कात्तारू’अपने कलेवर, विषयों के चुनाव आदि में यह एक श्रेष्ठ और गंभीर मासिक पत्रिका है, जो आज भी नियमित प्रकाशित हो रही है। उत्तर भारत से जो साहित्यिक – वैचारिक अथवा दलित-बहुजन मुद्दों पर केंद्रित लघु पत्रिकाएँ निकलती हैं, उनमें से अधिकांश के पीछे प्राय: कोई एक व्यक्ति मिशनरी भाव से जुड़ा होता है। कुछ मामलों में तो पत्रिका के माध्यम से स्वनामधन्य हो जाने की ख्वाहिश भी काम कर रही होती है। लेकिन, कोयंबटूर में ‘कात्तारू’ की युवा टीम इससे बिलकुल अलग है।
 ‘कात्तारू’ में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं प्रकाशित होता है। सारा काम ‘टीम’ की ओर से किया जाता है। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात है पत्रिका के प्रकाशन स्थल के निकटवर्ती गांव-कस्बों के परिवारों का इससे जुड़ाव। उस वार्षिकोत्सव के दौरान ‘टीम कात्तारू’ ने मुझे बताया कि इससे आसपास के गांवों के लगभग 500 परिवार जुड़े हैं, जिनके अनुदान से यह चलती है। सम-सामयिक मुद्दों की इस पत्रिका में कुछ पृष्ठ इन परिवारों में होने वाले जन्मदिन, विवाह व अन्य छोटी-बड़ी उपलब्धियों, शोक समाचार आदि के संक्षिप्त समाचारों व तस्वीरों के लिए सुरक्षित हैं। हिंदी की लघु पत्रिकाओं में इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पत्रिका के जिस समारोह में मैं शामिल हुआ था, उसमें पुरुषों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में किशोरियां, युवतियां, बहुएं, बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी कर रहीं थीं। वे विविध वैचारिक मुद्दों पर सवाल पूछ रहीं थीं और वक्ताओं के भाषणों के बाद हस्तक्षेप कर रहीं थीं।
पेरियार ने अपने आन्दोलन को महिलाओं से जोड़ने पर बहुत बल दिया था, जिसका असर उस समारोह में दिख रहा था। इसके विपरीत, आज उत्तर भारत के सारे जातिवाद-विरोधी आन्दोलन मुख्य रूप से सिर्फ पुरुषों के आन्दोलन हैं। जो महिलाएं इन आन्दोलनों में हमारे कंधे-से-कंधा मिला सकती थीं, उन्हें भी हमने विवश कर दिया है कि वे हमारे पुरुषवाद के विरोध में अपना अलग आन्दोलन चलाएँ। उत्तर भारत का ‘दलित स्त्रीवाद’ इसी का परिणाम है।
बहरहाल, पेरियार को हिंदी में लाना इतना आसान नहीं था। धारा के खिलाफ जाने वाले कामों में ऐसे अप्रत्याशित विघ्न आ खड़े होते हैं, जिनसे पार पाना बहुत कठिन होता है।
अंतत: कोविड:19 के इस दौर में पेरियार के विचार हिंदी में तीन पुस्तकों की ऋंखला के रूप में प्रकाशित हो गए हैं। इनमें संबंधित विषयों पर पेरियार के लेख और भाषण हैं। इसके अतिरिक्त सभी खंडों में संबंधित विषय के अध्येताओं के आलोचनात्मक लेख तथा पेरियार के जीवन का वर्ष वार लेखाजोखा दिया गया है।
आज ये किताबों जिस रूप में प्रकाशित हो रही है, उसमें कई लोगों की भूमिका रही है। ललई सिंह द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का अंग्रेजी संस्करण से मिलान और पुनः पूरी पुस्तक का नया और सटीक अनुवाद, तमिल भाषा के शब्दों के सही भावार्थ को समझने के लिए तमिल भाषी साथियों से निरंतर संपर्क एक बहुत श्रम साध्य काम था, जिसे मित्र अशोक झा ने अपनी अनेक व्यस्तताओं के बीच पूरी प्रतिबद्धता से पूर्ण किया।
कंवल भारती, ओमप्रकाश कश्यप युवा शोधार्थी धर्मवीर गगन के परामर्शों ने इस किताब को समृद्ध किया है। पेरियार की विलक्षण अध्येता व्ही.गीता, ब्रजरंजन मणि, टी मार्क्स, ललिता धारा, विद्याभूषण रावत, देवीना अक्षयवर, पूजा सिंह, संजय जोठे और ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन’ के निदेशक मित्र संजीव चंदन ने न सिर्फ इसमें अपना रचनात्मक योगदान दिया, बल्कि इसके प्रकाशन के दौरान आई बाधाओं को दूर करने में भी साथ खड़े रहें। इन मित्रों के लिए आभार शब्द तो पर्याप्त नहीं ही होगा।
उम्मीद करता हूं कि अनेकानेक मित्रों के सहयोग से तैयार यह पुस्तक हिंदी पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी और हम अब कह सकेंगे कि पेरियार हिंदी पट्टी में भी परिचय के मोहताज नहीं हैं!
‘कात्तारू’ में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं प्रकाशित होता है। सारा काम ‘टीम’ की ओर से किया जाता है। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात है पत्रिका के प्रकाशन स्थल के निकटवर्ती गांव-कस्बों के परिवारों का इससे जुड़ाव। उस वार्षिकोत्सव के दौरान ‘टीम कात्तारू’ ने मुझे बताया कि इससे आसपास के गांवों के लगभग 500 परिवार जुड़े हैं, जिनके अनुदान से यह चलती है। सम-सामयिक मुद्दों की इस पत्रिका में कुछ पृष्ठ इन परिवारों में होने वाले जन्मदिन, विवाह व अन्य छोटी-बड़ी उपलब्धियों, शोक समाचार आदि के संक्षिप्त समाचारों व तस्वीरों के लिए सुरक्षित हैं। हिंदी की लघु पत्रिकाओं में इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पत्रिका के जिस समारोह में मैं शामिल हुआ था, उसमें पुरुषों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में किशोरियां, युवतियां, बहुएं, बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी कर रहीं थीं। वे विविध वैचारिक मुद्दों पर सवाल पूछ रहीं थीं और वक्ताओं के भाषणों के बाद हस्तक्षेप कर रहीं थीं।
पेरियार ने अपने आन्दोलन को महिलाओं से जोड़ने पर बहुत बल दिया था, जिसका असर उस समारोह में दिख रहा था। इसके विपरीत, आज उत्तर भारत के सारे जातिवाद-विरोधी आन्दोलन मुख्य रूप से सिर्फ पुरुषों के आन्दोलन हैं। जो महिलाएं इन आन्दोलनों में हमारे कंधे-से-कंधा मिला सकती थीं, उन्हें भी हमने विवश कर दिया है कि वे हमारे पुरुषवाद के विरोध में अपना अलग आन्दोलन चलाएँ। उत्तर भारत का ‘दलित स्त्रीवाद’ इसी का परिणाम है।
बहरहाल, पेरियार को हिंदी में लाना इतना आसान नहीं था। धारा के खिलाफ जाने वाले कामों में ऐसे अप्रत्याशित विघ्न आ खड़े होते हैं, जिनसे पार पाना बहुत कठिन होता है।
अंतत: कोविड:19 के इस दौर में पेरियार के विचार हिंदी में तीन पुस्तकों की ऋंखला के रूप में प्रकाशित हो गए हैं। इनमें संबंधित विषयों पर पेरियार के लेख और भाषण हैं। इसके अतिरिक्त सभी खंडों में संबंधित विषय के अध्येताओं के आलोचनात्मक लेख तथा पेरियार के जीवन का वर्ष वार लेखाजोखा दिया गया है।
आज ये किताबों जिस रूप में प्रकाशित हो रही है, उसमें कई लोगों की भूमिका रही है। ललई सिंह द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का अंग्रेजी संस्करण से मिलान और पुनः पूरी पुस्तक का नया और सटीक अनुवाद, तमिल भाषा के शब्दों के सही भावार्थ को समझने के लिए तमिल भाषी साथियों से निरंतर संपर्क एक बहुत श्रम साध्य काम था, जिसे मित्र अशोक झा ने अपनी अनेक व्यस्तताओं के बीच पूरी प्रतिबद्धता से पूर्ण किया।
कंवल भारती, ओमप्रकाश कश्यप युवा शोधार्थी धर्मवीर गगन के परामर्शों ने इस किताब को समृद्ध किया है। पेरियार की विलक्षण अध्येता व्ही.गीता, ब्रजरंजन मणि, टी मार्क्स, ललिता धारा, विद्याभूषण रावत, देवीना अक्षयवर, पूजा सिंह, संजय जोठे और ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन’ के निदेशक मित्र संजीव चंदन ने न सिर्फ इसमें अपना रचनात्मक योगदान दिया, बल्कि इसके प्रकाशन के दौरान आई बाधाओं को दूर करने में भी साथ खड़े रहें। इन मित्रों के लिए आभार शब्द तो पर्याप्त नहीं ही होगा।
उम्मीद करता हूं कि अनेकानेक मित्रों के सहयोग से तैयार यह पुस्तक हिंदी पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी और हम अब कह सकेंगे कि पेरियार हिंदी पट्टी में भी परिचय के मोहताज नहीं हैं!
(राजकमल समूह द्वारा प्रकाशित पेरियार पुस्तक ऋंखला के संपादकीय का संपादित अंश) राजकमल समूह द्वारा प्रकाशित पेरियार पुस्तक श्रंखला की तीन पुस्तकें

- धर्म और विश्वदृष्टि
- जाति व्यवस्था और पितृसत्ता
- सच्ची रामायणसंपादक : प्रमोद रंजन
(यह दोनों किताब आप बहुजन बुक्स की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। सच्ची रामायण एवं धर्म और विश्व दृष्टि पुस्तक बुक करने के लिए किताबों के नाम पर क्लिक करिए।
कोरोना काल में विस्थापित मज़दूरों के बच्चे
 Written By- पूजा मारवाह
जब कोविड-19 से संबंधित काम करने वाली एक सहायता समूह के सदस्य ने सात साल की बच्ची आशा (बदला हुआ नाम) से मुलाकात की तो उस समय वह अपने चार साल के भाई की सुरक्षा कर रही थी। क्योंकि उसके माता पिता कहीं खाने की व्यवस्था करने गए हुए थे और वह बच्ची बहुत ही धैर्य के साथ उनके लौटने का इंतज़ार कर रही थी। उस बच्ची ने सहायता समूह के सदस्य को बताया कि वह लोग बिहार के किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले मज़दूर हैं। सड़क निर्माण करने वाले मज़दूरों का यह छोटा सा समूह अब उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक कच्ची आबादी में अस्थाई रूप से निवास कर रहा है, जहां कोरोना के बाद उन्हें दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से उपलब्ध पा रही है। उन्हें अपने गांव वापस लौटने की भी उम्मीद नहीं है। “हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं हैं, हम गांव कैसे जा सकते हैं?” सात साल की इस बच्ची का बहुत आसान जवाब था, लेकिन इसके पीछे कई गंभीर सवाल छुपे हुए थे। जिसका जवाब उस सहायता समूह के सदस्य के पास नहीं था।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉक डाउन और उसके बाद की परिस्थितियों ने बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को इसने सबसे अधिक प्रभावित किया है। लॉक डाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को राशन और स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही संस्था ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ ऐसी बहुत सी कहानियों की गवाह बनी, जो सुनने वालों के दिल को झकझोर कर रख देती है। हम सभी जानते हैं कि लॉक डाउन के दौरान अस्थाई और विस्थापित मज़दूरों के पास जीवन यापन का कोई माध्यम नहीं बचा था। काम बंद हो जाने के कारण उनके पास एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में उनके बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इसका शायद ही किसी ने अंदाज़ा लगाने का प्रयास किया होगा।
माता पिता के साथ विस्थापन के दौरान बच्चों को सबसे अधिक खाने पीने की जद्दोजहद करनी पर रही है। उनके सामने न केवल भूख और प्यास का मसला था बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को संभालने की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ रही थी। इस दौरान उन्हें उनकी उम्र और क्षमता के अनुरूप भोजन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लॉक डाउन के कारण स्कूलों के बंद होने से गरीब बच्चों को दोपहर का मिलने वाला पौष्टिक भोजन भी बंद हो गया। जिससे इस अवधि में कुपोषण के बढ़ने की संभावनाओं ने भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं कोरोना की अफरातफरी में बच्चों को समय पर लगने वाले टीके भी नहीं मिल सके हैं जो भविष्य में उन्हें खतरनाक बिमारियों से बचा सकता था।
समेकित बाल विकास कार्यक्रम योजना (आईसीडीएस) और स्वास्थ्य केंद्र कोरोना की रोकथाम के नाम पर पिछले कुछ महीनों से बंद पड़े हैं। जिसके कारण पोलियो वैक्सीन, समय पर लगने वाले टीके, आयरन की गोलियां तथा गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं तथा उनके बच्चों को दिए जाने वाले पोषण योजना जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम ठप्प हो गए हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और खून की कमी तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या पर काबू पाने की मुहिम को झटका लग सकता है। इससे भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य और भी दूर हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लॉक डाउन के कारण गरीब बस्तियों में सामाजिक स्तर पर साफ़ सफाई नहीं होने से टायफायड तथा पानी से होने वाली अधिकतर बिमारियों के बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है।
बहुत अफ़सोस की बात है कि बच्चों को भी काम के लिए विस्थापित होना पड़ता है। पढ़ने लिखने की उम्र में इन्हें बाल मज़दूरी करनी पड़ती है। लेकिन काम के बाद अक्सर इन बच्चों को उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बल्कि कई बार इन्हें काम पर लगाने वाले ठेकेदार और बिचौलिए इनका पैसा हड़प जाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में इन बच्चों की सुरक्षा को सबसे अधिक खतरा रहता है। क्योंकि इनसे काम करवाने वाले मालिक बाल श्रम कानून से बचने के लिए इनका नाम मज़दूरों की लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। यही कारण है कि अक्सर इन तक पहुँचना और उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना किसी भी संस्था के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
अपने परिवार के दुखों को देख कर इस परिवेश में रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व और स्वभाव में सामान्य बच्चों की तुलना में काफी अंतर होता है। कई बार ऐसे बच्चे यौन शोषण का भी आसानी से शिकार हो जाते हैं। वहीँ मानव तस्कर के चुंगल में भी इनके फंसने की संभावनाएं बहुत अधिक बनी रहती है। लगातार विस्थापन के कारण इन बच्चों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होती है। ज़्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है। ऐसे में या तो परिवार वालों के साथ मज़दूरी की आग में झोंक दिए जाते हैं या फिर गलत संगत में आकर अपराध और नशे की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। मानसिक रूप से अत्यधिक दबाब के कारण ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे बहुत जल्द कमज़ोर और विपक्षित अवस्था में भी पहुँच जाते हैं।
बार बार विस्थापन के कारण मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित होती है। बहुत सारे बच्चों का स्कूलों में नामांकन तो होता है लेकिन माता पिता के विस्थापन के कारण अधिकतर बच्चे स्कूल का मुंह तक देख नहीं पाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉक डाउन के बाद विस्थापित मज़दूरों के बच्चों की स्कूल से दूरी और भी बढ़ गई है। लॉक डाउन के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब होने तथा ऑनलाइन क्लास की सुविधा से वंचित होने के कारण यह बच्चे मज़दूरी की अंधेरी दुनिया में धकेल दिए जायेंगे। इसमें सबसे अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे प्रभावित होंगे। लॉक डाउन के सबब ऑनलाइन सुविधा नहीं होने के कारण गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इनमें विस्थापित मज़दूरों के बच्चों की संख्या लगभग शत प्रतिशत है। हालांकि लॉक डाउन के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की प्रभावित होती शिक्षा को सामान्य स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रकार की योजनाओं पर काम कर रही हैं। इनमें कम्युनिटी रेडियो और संचार के दूसरे अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार विस्थापित होने वाले बच्चों तक इन माध्यमों की पहुँच बहुत कम मुमकिन हो पाती है।
वर्तमान में बच्चों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके साथ साथ उनके पोषण और शारीरिक विकास के लिए भी ठोस योजनाओं पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें हर तरह से स्वस्थ्य और विकार रहित जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसे में मदद के दौरान उन तक पहुँचाए जा रहे राहत सामग्रियों में दूध, प्रोटीन और अन्य पौष्टिक आहारों को अधिक से अधिक उपलब्ध कराये जाने की ज़रूरत है। हमें इस बात को समझना होगा कि बिना पका हुआ खाना उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित नहीं होगा क्योंकि विस्थापितों के लिए आसानी से रसोई घर की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाना मुमकिन नहीं है।
इसके अतिरिक्त विस्थापित मज़दूरों और उनके बच्चों के लिए साफ़ सफ़ाई तथा शौचालयों की व्यवस्था भी ज़रूरी है। इसके लिए राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक और पंचायत स्तर तक विस्थापित मज़दूरों के लिए बनाये गए अस्थाई बस्तियों में विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत है। विशेष रूप से इस मामले में लड़कियों के लिए ख़ास इंतज़ाम करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के यौन शोषण से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, युवावस्था में प्रवेश करने वाली विस्थापित मज़दूरों की बच्चियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ख़ास ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें न केवल माहवारी संबंधी सही मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है बल्कि कम उम्र में शादी करने से बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है।
अब समय आ गया है कि विस्थापित होने वाले बच्चों के जीवन में भी रौशनी फैलाई जाये। उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त हो। उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध हो तथा समय पर स्वास्थ्य के टीके मिल सकें। यह बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे कोई भी संस्था अकेले पूरा नहीं कर सकती है। इसके लिए सरकार और प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मिल कर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि एक आम बच्चों की तरह लगातार विस्थापन का दंश झेल रहे मज़दूरों के बच्चों को भी सभी सुविधाएं पाने का हक़ है और यह हक़ उन्हें हमारा संविधान देता है।
Written By- पूजा मारवाह
जब कोविड-19 से संबंधित काम करने वाली एक सहायता समूह के सदस्य ने सात साल की बच्ची आशा (बदला हुआ नाम) से मुलाकात की तो उस समय वह अपने चार साल के भाई की सुरक्षा कर रही थी। क्योंकि उसके माता पिता कहीं खाने की व्यवस्था करने गए हुए थे और वह बच्ची बहुत ही धैर्य के साथ उनके लौटने का इंतज़ार कर रही थी। उस बच्ची ने सहायता समूह के सदस्य को बताया कि वह लोग बिहार के किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले मज़दूर हैं। सड़क निर्माण करने वाले मज़दूरों का यह छोटा सा समूह अब उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक कच्ची आबादी में अस्थाई रूप से निवास कर रहा है, जहां कोरोना के बाद उन्हें दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से उपलब्ध पा रही है। उन्हें अपने गांव वापस लौटने की भी उम्मीद नहीं है। “हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं हैं, हम गांव कैसे जा सकते हैं?” सात साल की इस बच्ची का बहुत आसान जवाब था, लेकिन इसके पीछे कई गंभीर सवाल छुपे हुए थे। जिसका जवाब उस सहायता समूह के सदस्य के पास नहीं था।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉक डाउन और उसके बाद की परिस्थितियों ने बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को इसने सबसे अधिक प्रभावित किया है। लॉक डाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को राशन और स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही संस्था ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ ऐसी बहुत सी कहानियों की गवाह बनी, जो सुनने वालों के दिल को झकझोर कर रख देती है। हम सभी जानते हैं कि लॉक डाउन के दौरान अस्थाई और विस्थापित मज़दूरों के पास जीवन यापन का कोई माध्यम नहीं बचा था। काम बंद हो जाने के कारण उनके पास एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में उनके बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इसका शायद ही किसी ने अंदाज़ा लगाने का प्रयास किया होगा।
माता पिता के साथ विस्थापन के दौरान बच्चों को सबसे अधिक खाने पीने की जद्दोजहद करनी पर रही है। उनके सामने न केवल भूख और प्यास का मसला था बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को संभालने की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ रही थी। इस दौरान उन्हें उनकी उम्र और क्षमता के अनुरूप भोजन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लॉक डाउन के कारण स्कूलों के बंद होने से गरीब बच्चों को दोपहर का मिलने वाला पौष्टिक भोजन भी बंद हो गया। जिससे इस अवधि में कुपोषण के बढ़ने की संभावनाओं ने भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं कोरोना की अफरातफरी में बच्चों को समय पर लगने वाले टीके भी नहीं मिल सके हैं जो भविष्य में उन्हें खतरनाक बिमारियों से बचा सकता था।
समेकित बाल विकास कार्यक्रम योजना (आईसीडीएस) और स्वास्थ्य केंद्र कोरोना की रोकथाम के नाम पर पिछले कुछ महीनों से बंद पड़े हैं। जिसके कारण पोलियो वैक्सीन, समय पर लगने वाले टीके, आयरन की गोलियां तथा गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं तथा उनके बच्चों को दिए जाने वाले पोषण योजना जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम ठप्प हो गए हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और खून की कमी तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या पर काबू पाने की मुहिम को झटका लग सकता है। इससे भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य और भी दूर हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लॉक डाउन के कारण गरीब बस्तियों में सामाजिक स्तर पर साफ़ सफाई नहीं होने से टायफायड तथा पानी से होने वाली अधिकतर बिमारियों के बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है।
बहुत अफ़सोस की बात है कि बच्चों को भी काम के लिए विस्थापित होना पड़ता है। पढ़ने लिखने की उम्र में इन्हें बाल मज़दूरी करनी पड़ती है। लेकिन काम के बाद अक्सर इन बच्चों को उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बल्कि कई बार इन्हें काम पर लगाने वाले ठेकेदार और बिचौलिए इनका पैसा हड़प जाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में इन बच्चों की सुरक्षा को सबसे अधिक खतरा रहता है। क्योंकि इनसे काम करवाने वाले मालिक बाल श्रम कानून से बचने के लिए इनका नाम मज़दूरों की लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। यही कारण है कि अक्सर इन तक पहुँचना और उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना किसी भी संस्था के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
अपने परिवार के दुखों को देख कर इस परिवेश में रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व और स्वभाव में सामान्य बच्चों की तुलना में काफी अंतर होता है। कई बार ऐसे बच्चे यौन शोषण का भी आसानी से शिकार हो जाते हैं। वहीँ मानव तस्कर के चुंगल में भी इनके फंसने की संभावनाएं बहुत अधिक बनी रहती है। लगातार विस्थापन के कारण इन बच्चों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होती है। ज़्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है। ऐसे में या तो परिवार वालों के साथ मज़दूरी की आग में झोंक दिए जाते हैं या फिर गलत संगत में आकर अपराध और नशे की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। मानसिक रूप से अत्यधिक दबाब के कारण ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे बहुत जल्द कमज़ोर और विपक्षित अवस्था में भी पहुँच जाते हैं।
बार बार विस्थापन के कारण मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित होती है। बहुत सारे बच्चों का स्कूलों में नामांकन तो होता है लेकिन माता पिता के विस्थापन के कारण अधिकतर बच्चे स्कूल का मुंह तक देख नहीं पाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉक डाउन के बाद विस्थापित मज़दूरों के बच्चों की स्कूल से दूरी और भी बढ़ गई है। लॉक डाउन के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब होने तथा ऑनलाइन क्लास की सुविधा से वंचित होने के कारण यह बच्चे मज़दूरी की अंधेरी दुनिया में धकेल दिए जायेंगे। इसमें सबसे अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे प्रभावित होंगे। लॉक डाउन के सबब ऑनलाइन सुविधा नहीं होने के कारण गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इनमें विस्थापित मज़दूरों के बच्चों की संख्या लगभग शत प्रतिशत है। हालांकि लॉक डाउन के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की प्रभावित होती शिक्षा को सामान्य स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रकार की योजनाओं पर काम कर रही हैं। इनमें कम्युनिटी रेडियो और संचार के दूसरे अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार विस्थापित होने वाले बच्चों तक इन माध्यमों की पहुँच बहुत कम मुमकिन हो पाती है।
वर्तमान में बच्चों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके साथ साथ उनके पोषण और शारीरिक विकास के लिए भी ठोस योजनाओं पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें हर तरह से स्वस्थ्य और विकार रहित जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसे में मदद के दौरान उन तक पहुँचाए जा रहे राहत सामग्रियों में दूध, प्रोटीन और अन्य पौष्टिक आहारों को अधिक से अधिक उपलब्ध कराये जाने की ज़रूरत है। हमें इस बात को समझना होगा कि बिना पका हुआ खाना उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित नहीं होगा क्योंकि विस्थापितों के लिए आसानी से रसोई घर की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाना मुमकिन नहीं है।
इसके अतिरिक्त विस्थापित मज़दूरों और उनके बच्चों के लिए साफ़ सफ़ाई तथा शौचालयों की व्यवस्था भी ज़रूरी है। इसके लिए राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक और पंचायत स्तर तक विस्थापित मज़दूरों के लिए बनाये गए अस्थाई बस्तियों में विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत है। विशेष रूप से इस मामले में लड़कियों के लिए ख़ास इंतज़ाम करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के यौन शोषण से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, युवावस्था में प्रवेश करने वाली विस्थापित मज़दूरों की बच्चियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ख़ास ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें न केवल माहवारी संबंधी सही मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है बल्कि कम उम्र में शादी करने से बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है।
अब समय आ गया है कि विस्थापित होने वाले बच्चों के जीवन में भी रौशनी फैलाई जाये। उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त हो। उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध हो तथा समय पर स्वास्थ्य के टीके मिल सकें। यह बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे कोई भी संस्था अकेले पूरा नहीं कर सकती है। इसके लिए सरकार और प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मिल कर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि एक आम बच्चों की तरह लगातार विस्थापन का दंश झेल रहे मज़दूरों के बच्चों को भी सभी सुविधाएं पाने का हक़ है और यह हक़ उन्हें हमारा संविधान देता है।
लेखिका पूजा मारवाह चाइल्ड राइट्स एंड यू “क्राई” की सीईओ हैं।
No End to Humiliation of Dalits Even After Death
 Written By- Subhash Gatade
Does anybody still remember the Dalits of Chakwara, a village around 50km from Jaipur in Rajasthan, who had launched a struggle to gain access to the pond in their village? It is more than 18 years since the Dalits, supported by human rights organisations, won that fight for water. Their undertaking had echoes with the historic struggle launched by Dr BR Ambedkar in March 1927 at Chavdar tank at Mahad to assert the equal rights of Dalits to water. It is well known to most people that while animals were allowed to use the water of this tank in present-day Raigad district of the state, the Dalits were not. Anand Teltumbde has described the events of this satyagraha in his book, Mahad: The Making of the First Dalit Revolt, published by Navayana in 2016.
But what happened at Chakwara after the Dalits started using the village pond is hardly known: the upper castes slowly stopped using the water from the pond once the Dalits gained access to it, saying it had become “impure”. Enraged by the assertion of the Dalits and keen to humiliate them for it, they dug up the village sewer and directed the waste water to their own village pond. There is no change in the status quo there.
Read Full Story
Written By- Subhash Gatade
Does anybody still remember the Dalits of Chakwara, a village around 50km from Jaipur in Rajasthan, who had launched a struggle to gain access to the pond in their village? It is more than 18 years since the Dalits, supported by human rights organisations, won that fight for water. Their undertaking had echoes with the historic struggle launched by Dr BR Ambedkar in March 1927 at Chavdar tank at Mahad to assert the equal rights of Dalits to water. It is well known to most people that while animals were allowed to use the water of this tank in present-day Raigad district of the state, the Dalits were not. Anand Teltumbde has described the events of this satyagraha in his book, Mahad: The Making of the First Dalit Revolt, published by Navayana in 2016.
But what happened at Chakwara after the Dalits started using the village pond is hardly known: the upper castes slowly stopped using the water from the pond once the Dalits gained access to it, saying it had become “impure”. Enraged by the assertion of the Dalits and keen to humiliate them for it, they dug up the village sewer and directed the waste water to their own village pond. There is no change in the status quo there.
Read Full Story यूपी में 2007 का करिश्मा दोहरा सकती है बसपा, बशर्ते…
 क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बार फिर जमीन तैयार हो रही है। क्या आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा को एक बार फिर से ब्राह्मण समाज का साथ मिल सकता है। यह सवाल उत्तर प्रदेश की हालिया घटनाओं के कारण उठ रहा है। विकास दूबे मामले में एक नाबालिक युवक का एनकाउंटर और अब गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है।
कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के बहाने जब पूरे ब्राह्मण समाज को कठघरे में खड़ा किया जा रहा था, बसपा प्रमुख मायावती ने पूरे ब्राह्मण समाज पर निशाना साधने वालों की आलोचना की थी। इन दोनों घटनाओं से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में योगी सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। जहां तक पत्रकार हत्याकांड की बात है तो पुलिस से शिकायत के बावजूद पुलिस ने अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इससे उत्साहित गुंडों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। इसको लेकर योगी सरकार की काफी आलोचना हो रही है। लखनऊ में तो पत्रकारों ने मीडियाकर्मियों पर बढ़ती हिंसा के मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तो दूसरी ओर विकास दूबे के मामले में 14 साल के एक नाबालिग युवक के इनकाउंटर को भी ब्राह्मण समाज अन्याय बता रहा है।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के लोगों के बीच भी योगी सरकार को लेकर तेजी से गुस्सा फैलता जा रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से ठाकुरवाद को बढ़ा रहे हैं, और ब्राह्मणों को दरकिनार कर रहे हैं, उससे ब्राह्मण समाज में रोष है। ऐसे में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है।
क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बार फिर जमीन तैयार हो रही है। क्या आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा को एक बार फिर से ब्राह्मण समाज का साथ मिल सकता है। यह सवाल उत्तर प्रदेश की हालिया घटनाओं के कारण उठ रहा है। विकास दूबे मामले में एक नाबालिक युवक का एनकाउंटर और अब गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है।
कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के बहाने जब पूरे ब्राह्मण समाज को कठघरे में खड़ा किया जा रहा था, बसपा प्रमुख मायावती ने पूरे ब्राह्मण समाज पर निशाना साधने वालों की आलोचना की थी। इन दोनों घटनाओं से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में योगी सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। जहां तक पत्रकार हत्याकांड की बात है तो पुलिस से शिकायत के बावजूद पुलिस ने अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इससे उत्साहित गुंडों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। इसको लेकर योगी सरकार की काफी आलोचना हो रही है। लखनऊ में तो पत्रकारों ने मीडियाकर्मियों पर बढ़ती हिंसा के मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तो दूसरी ओर विकास दूबे के मामले में 14 साल के एक नाबालिग युवक के इनकाउंटर को भी ब्राह्मण समाज अन्याय बता रहा है।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के लोगों के बीच भी योगी सरकार को लेकर तेजी से गुस्सा फैलता जा रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से ठाकुरवाद को बढ़ा रहे हैं, और ब्राह्मणों को दरकिनार कर रहे हैं, उससे ब्राह्मण समाज में रोष है। ऐसे में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है।
 अब जरा पीछे आते हैं तो वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बिना गठबंधन चुनाव लड़ा था और अपने बलबूते सत्ता हासिल की थी। इसके पीछे अनुसूचित जातियों व जनजातियों के साथ सर्वसमाज को जोड़ने का प्रयोग माना जाता रहा है। हालिया घटनाक्रम के बाद प्रदेश में एक बार फिर से 2007 जैसी स्थिति बनने की पूरी संभवना है। हालांकि यहां एक बात साफ है कि ब्राह्मण वोटर योगी सरकार से नाराज हैं, न कि भाजपा से। लेकिन लोकतंत्र में हर राज्य का चुनावी गणित अलग होता है। और यूपी के चुनावी गणित में योगी ब्राह्मण समाज के निशाने पर हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि योगी से नाराज वोटर किस ओर जाएंगे। क्या वह बिना कोशिश के ही खुद बसपा के पीछे खड़े हो जाएंगे? जाहिर है नहीं। क्योंकि जमीनी हकीकत से समाजवादी पार्टी भी वाकिफ है और अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं। यही नहीं सपा के कई अन्य नेता भी सोशल मीडिया पर ब्राह्मण अत्याचार की बात को जोर-शोर से उठा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कितनी गंभीर कोशिश करती है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इसकी संभावना जताई जा रही है कि अगर बसपा ने ईमानदारी से कोशिश की और ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया तो प्रदेश में एक बार फिर से 2007 की स्थिति दोहराई जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि बसपा को कोशिश करनी होगी, और कोशिश में ईमानदारी होनी चाहिए।
अब जरा पीछे आते हैं तो वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बिना गठबंधन चुनाव लड़ा था और अपने बलबूते सत्ता हासिल की थी। इसके पीछे अनुसूचित जातियों व जनजातियों के साथ सर्वसमाज को जोड़ने का प्रयोग माना जाता रहा है। हालिया घटनाक्रम के बाद प्रदेश में एक बार फिर से 2007 जैसी स्थिति बनने की पूरी संभवना है। हालांकि यहां एक बात साफ है कि ब्राह्मण वोटर योगी सरकार से नाराज हैं, न कि भाजपा से। लेकिन लोकतंत्र में हर राज्य का चुनावी गणित अलग होता है। और यूपी के चुनावी गणित में योगी ब्राह्मण समाज के निशाने पर हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि योगी से नाराज वोटर किस ओर जाएंगे। क्या वह बिना कोशिश के ही खुद बसपा के पीछे खड़े हो जाएंगे? जाहिर है नहीं। क्योंकि जमीनी हकीकत से समाजवादी पार्टी भी वाकिफ है और अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं। यही नहीं सपा के कई अन्य नेता भी सोशल मीडिया पर ब्राह्मण अत्याचार की बात को जोर-शोर से उठा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कितनी गंभीर कोशिश करती है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इसकी संभावना जताई जा रही है कि अगर बसपा ने ईमानदारी से कोशिश की और ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया तो प्रदेश में एक बार फिर से 2007 की स्थिति दोहराई जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि बसपा को कोशिश करनी होगी, और कोशिश में ईमानदारी होनी चाहिए। अयोध्या में बौद्ध पक्ष को अदालत की फटकार कितनी जायज
 देश की अदालत सबके लिए है। शायद यही वजह है कि अदालतों को भी तीन स्तरों पर बांटा गया है, ताकि एक जगह न्याय मिलने से रह जाए और अदालत से ही कोई गलती हो जाए तो दूसरी या तीसरी जगह न्याय हासिल किया जा सके। लेकिन न्याय पाने के लिए अपील दो लोगों को भारी पर गई। जब शीर्ष अदालत ने उनकी जनहित याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि उसे बेकार और बकवास तक कह दिया और तो और याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।
मामला अयोध्या के रामजन्मभूमि स्थल से जुड़ा है। आप सबको याद होगा पिछले दिनों रामजन्म भूमि के समतलीकरण के दौरान तमाम अवशेष सामने आए थे। खुदाई में जो अवशेष मिले थे, वो तमाम बौद्ध धर्म से मिलते-जुलते थे। बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखने वाले अशोक धम्म चक्र और कमल का फूल जैसे अवशेष की तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद तमाम बौद्ध विद्वान इसे बौद्ध धर्म का अवशेष बताते हुए एक बार फिर से अयोध्या को बौद्ध नगरी साकेत बताने लगे।
देश की अदालत सबके लिए है। शायद यही वजह है कि अदालतों को भी तीन स्तरों पर बांटा गया है, ताकि एक जगह न्याय मिलने से रह जाए और अदालत से ही कोई गलती हो जाए तो दूसरी या तीसरी जगह न्याय हासिल किया जा सके। लेकिन न्याय पाने के लिए अपील दो लोगों को भारी पर गई। जब शीर्ष अदालत ने उनकी जनहित याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि उसे बेकार और बकवास तक कह दिया और तो और याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।
मामला अयोध्या के रामजन्मभूमि स्थल से जुड़ा है। आप सबको याद होगा पिछले दिनों रामजन्म भूमि के समतलीकरण के दौरान तमाम अवशेष सामने आए थे। खुदाई में जो अवशेष मिले थे, वो तमाम बौद्ध धर्म से मिलते-जुलते थे। बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखने वाले अशोक धम्म चक्र और कमल का फूल जैसे अवशेष की तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद तमाम बौद्ध विद्वान इसे बौद्ध धर्म का अवशेष बताते हुए एक बार फिर से अयोध्या को बौद्ध नगरी साकेत बताने लगे।
 पिछले कई वर्षों से अयोध्या के बौद्ध स्थल होने का दावा बौद्ध धम्म को मानने वाले करते रहे हैं। इस खुदाई में मिले अवशेष के बाद मामले ने फिर से जोर पकड़ा। इसके बाद बिहार के दो बौद्ध भिक्खुओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और रामजन्मभूमि को खोदने और खुदाई के दौरान सामने आने वाली कलाकृतियों की सुरक्षा करने की मांग की। अवशेषों की सुरक्षा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में किए जाने की मांग थी।
इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानि कि 20 जुलाई को सुनवाई हुई। जिस पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने लगभग भड़कते हुए न सिर्फ इस याचिका को बेकार, तुच्छ तक कहा, बल्कि बिल्कुल कठोर रुख अपनाते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। और इस रकम को एक महीने के भीतर जमा करने का फरमान सुना दिया। दोनों को यह कह कर भी डांट लगाई गई कि अदालत याचिकाकर्ता संगठनों की सीबीआई जांच के आदेश देगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि आप जनहित के नाम पर ऐसी बेकार याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं। आप दंड के भागी हैं। आप पर इसलिए जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि ऐसी गलती आप दोबारा न करें। दरअसल कोर्ट इस मामले में पहले से ही याचिका होने के बावजूद नई याचिका लाए जाने से नाराज थी। तीन जजों की इस खंडपीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी थे।
दरअसल हुआ यह कि रामजन्मभूमि स्थल के समतलीकरण के दौरान कई अवशेष मिले थे। इसके बाद बिहार से आये दो बौद्ध मतावलंबियों ने राम जन्मभूमि पर अपना दावा बताया था। इसमें से एक भंते बुद्धशरण केसरिया भी थे।
पिछले कई वर्षों से अयोध्या के बौद्ध स्थल होने का दावा बौद्ध धम्म को मानने वाले करते रहे हैं। इस खुदाई में मिले अवशेष के बाद मामले ने फिर से जोर पकड़ा। इसके बाद बिहार के दो बौद्ध भिक्खुओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और रामजन्मभूमि को खोदने और खुदाई के दौरान सामने आने वाली कलाकृतियों की सुरक्षा करने की मांग की। अवशेषों की सुरक्षा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में किए जाने की मांग थी।
इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानि कि 20 जुलाई को सुनवाई हुई। जिस पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने लगभग भड़कते हुए न सिर्फ इस याचिका को बेकार, तुच्छ तक कहा, बल्कि बिल्कुल कठोर रुख अपनाते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। और इस रकम को एक महीने के भीतर जमा करने का फरमान सुना दिया। दोनों को यह कह कर भी डांट लगाई गई कि अदालत याचिकाकर्ता संगठनों की सीबीआई जांच के आदेश देगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि आप जनहित के नाम पर ऐसी बेकार याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं। आप दंड के भागी हैं। आप पर इसलिए जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि ऐसी गलती आप दोबारा न करें। दरअसल कोर्ट इस मामले में पहले से ही याचिका होने के बावजूद नई याचिका लाए जाने से नाराज थी। तीन जजों की इस खंडपीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी थे।
दरअसल हुआ यह कि रामजन्मभूमि स्थल के समतलीकरण के दौरान कई अवशेष मिले थे। इसके बाद बिहार से आये दो बौद्ध मतावलंबियों ने राम जन्मभूमि पर अपना दावा बताया था। इसमें से एक भंते बुद्धशरण केसरिया भी थे।
 बुद्धशरण केसरिया का कहना है कि “अयोध्या में बन रहे राममंदिर निर्माण के लिए हुए समतलीकरण के दौरान बौद्ध संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी मूर्तियां, अशोक धम्म चक्र, कमल का फूल एवं अन्य अवशेष मिलने से स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान अयोध्या बोधिसत्व लोमश ऋषि की बुद्ध नगरी साकेत है। अयोध्या मसले पर हिंदु मुस्लिम और बौद्ध तीनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी लेकिन सारे सबूतों को दरकिनार कर एकतरफा फैसला हिंदुओं के पक्ष में राम जन्मभूमि के लिए दे दिया गया। इसके लिए हमारे संगठन ने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट समेत कई संस्थाओं को पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया।’
अब फिर मूल सवाल पर आते हैं। सवाल है कि क्या यह मामला इतना छोटा था कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से अदालत का ध्यान आकर्षित करना अपराध हो गया। क्या भारत और दुनिया भर में मौजूद बौद्ध धम्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। क्या अवशेष की तस्वीरें सामने आने के बाद और उसके बौद्ध धम्म से संबंधित होने के बाद भी बौद्ध धम्म में आस्था रखने वालों को अपने ही देश की अदालत से न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए थी। सवाल कई हैं। आप भी इस बारे में जरूर सोचिएगा।
बुद्धशरण केसरिया का कहना है कि “अयोध्या में बन रहे राममंदिर निर्माण के लिए हुए समतलीकरण के दौरान बौद्ध संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी मूर्तियां, अशोक धम्म चक्र, कमल का फूल एवं अन्य अवशेष मिलने से स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान अयोध्या बोधिसत्व लोमश ऋषि की बुद्ध नगरी साकेत है। अयोध्या मसले पर हिंदु मुस्लिम और बौद्ध तीनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी लेकिन सारे सबूतों को दरकिनार कर एकतरफा फैसला हिंदुओं के पक्ष में राम जन्मभूमि के लिए दे दिया गया। इसके लिए हमारे संगठन ने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट समेत कई संस्थाओं को पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया।’
अब फिर मूल सवाल पर आते हैं। सवाल है कि क्या यह मामला इतना छोटा था कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से अदालत का ध्यान आकर्षित करना अपराध हो गया। क्या भारत और दुनिया भर में मौजूद बौद्ध धम्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। क्या अवशेष की तस्वीरें सामने आने के बाद और उसके बौद्ध धम्म से संबंधित होने के बाद भी बौद्ध धम्म में आस्था रखने वालों को अपने ही देश की अदालत से न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए थी। सवाल कई हैं। आप भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। अन्नाभाऊ साठेः ऐसे दलित साहित्यकार, जिनकी रचनाओं का 27 भाषाओं में हुआ अनुवाद
 दलित समाज में जन्में बहुत से ऐसे रत्न हैं, जिनके बारे में देश को नहीं पता। या तो वह क्षेत्र विशेष तक सीमट कर रह गए हैं या फिर समाज के हीरो बनकर। जबकि उनकी काबिलियत ऐसी है कि बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी उनके सामने धाराशायी हो जाए। उनकी प्रसिद्धी सीमट कर रह गई तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति की वजह से। अन्नाभाऊ साठे ऐसे ही साहित्यकार हैं, जिनको देश के भीतर उनके कद के मुताबिक मान-सम्मान नहीं मिला। आज भी देश तो क्या खुद दलित-बहुजन समाज के ज्यादातर लोग उनकी महानता से अनभिज्ञ हैं।
18 जुलाई (1969)को उनकी पुण्यतिथि यानी परिनिर्वाण दिवस है। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के वाटेगांव में हुआ था। वह महज 48 साल जिए, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने इतना शानदार साहित्य रचा कि उसकी धमक दुनिया के 27 देशों तक में पहुंची। जी हां, अन्नभाऊ साठे की रचनाओं का दुनिया की 27 भाषाओं में अनुवाद हुआ। वह सबसे ज्यादा रुस में प्रचलित थे। कहा जाता है कि उनकी वजह से भारत और रुस के संबंध बेहतर हुए।
दलित समाज में जन्में बहुत से ऐसे रत्न हैं, जिनके बारे में देश को नहीं पता। या तो वह क्षेत्र विशेष तक सीमट कर रह गए हैं या फिर समाज के हीरो बनकर। जबकि उनकी काबिलियत ऐसी है कि बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी उनके सामने धाराशायी हो जाए। उनकी प्रसिद्धी सीमट कर रह गई तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति की वजह से। अन्नाभाऊ साठे ऐसे ही साहित्यकार हैं, जिनको देश के भीतर उनके कद के मुताबिक मान-सम्मान नहीं मिला। आज भी देश तो क्या खुद दलित-बहुजन समाज के ज्यादातर लोग उनकी महानता से अनभिज्ञ हैं।
18 जुलाई (1969)को उनकी पुण्यतिथि यानी परिनिर्वाण दिवस है। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के वाटेगांव में हुआ था। वह महज 48 साल जिए, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने इतना शानदार साहित्य रचा कि उसकी धमक दुनिया के 27 देशों तक में पहुंची। जी हां, अन्नभाऊ साठे की रचनाओं का दुनिया की 27 भाषाओं में अनुवाद हुआ। वह सबसे ज्यादा रुस में प्रचलित थे। कहा जाता है कि उनकी वजह से भारत और रुस के संबंध बेहतर हुए।