 झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”
मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.
इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.
घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है.
झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”
मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.
इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.
घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है. मंदिर में दलित ने झुकाया सिर तो पड़े डंडे, कुशवाहा समाज के लोगों ने कहा- तूने भगवान को भगा दिया
 झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”
मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.
इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.
घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है.
झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”
मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.
इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.
घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है. कौन कहता है बच्चों को जाति का ज्ञान नहीं होता
 मैं मुजफ्फरपुर (बिहार) का रहने वाला हूँ, मेरी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड में नहीं बल्कि मुज़फ्फरपुर में ही हुई. दिवंगत रघुनाथ पांडे द्वारा बनवाए गए- विद्या बिहार स्कूल में. दसवीं तक वहीँ पढ़ा. जाहिर है, उम्र नाबालिग थी और मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र भी नाबालिग थे. लेकिन ज्यादातर नाबालिग छात्रों में जातिगत सोच कूट-कूट कर भरी हुई थी. आखिर नाबालिग उम्र के बच्चों को कौन सिखलाता है कि किस (जाति) के लोगों के साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ बैठना है इत्यादि .. जाहिर है यह ट्रेनिंग घर से ही मिलती होगी. कई बार मैंने कई अभिवावकों को यह भी कहते सुना कि फलां छोटी जात का है, उसके साथ मत रहो इत्यादि.
मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज का छात्र हुआ, जातिवाद का एक खूुनी, भयावह कॉलेज. बचपन से विद्रोही प्रवृति का था, आप समझ ही गए होंगे. इसलिए पिताजी नाम कटवाकर मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज ले गए, वहां भी कमोबेश वही आलम. उबकर दिल्ली चला आया, देशबंधु कॉलेज, यहाँ भी पहले दिन जाति पूछी गई. यही नहीं सवर्णों की आपसी जातिगत गुटबंदी भी थी. फिर एम. ए. और उससे आगे, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर, हॉस्टल भी सवर्ण जातियों ने आपस में बाँट लिया था और बिहार की तरह ही गुंडई का केंद्र. कौन कहता है, बच्चों को जाति का ज्ञान नहीं होता ? स्कूल से लेकर बी.ए., कितनी उम्र होती है, सोलह से अठारह साल, कहाँ से सीखता है बच्चा जातीय ज्ञान, नफरत और भेदभाव? – निः संदेह परिवार ही पहली पाठशाला है. कहानी और भी है, धीरे-धीरे विस्तार से बयां करेंगे….
मैं मुजफ्फरपुर (बिहार) का रहने वाला हूँ, मेरी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड में नहीं बल्कि मुज़फ्फरपुर में ही हुई. दिवंगत रघुनाथ पांडे द्वारा बनवाए गए- विद्या बिहार स्कूल में. दसवीं तक वहीँ पढ़ा. जाहिर है, उम्र नाबालिग थी और मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र भी नाबालिग थे. लेकिन ज्यादातर नाबालिग छात्रों में जातिगत सोच कूट-कूट कर भरी हुई थी. आखिर नाबालिग उम्र के बच्चों को कौन सिखलाता है कि किस (जाति) के लोगों के साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ बैठना है इत्यादि .. जाहिर है यह ट्रेनिंग घर से ही मिलती होगी. कई बार मैंने कई अभिवावकों को यह भी कहते सुना कि फलां छोटी जात का है, उसके साथ मत रहो इत्यादि.
मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज का छात्र हुआ, जातिवाद का एक खूुनी, भयावह कॉलेज. बचपन से विद्रोही प्रवृति का था, आप समझ ही गए होंगे. इसलिए पिताजी नाम कटवाकर मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज ले गए, वहां भी कमोबेश वही आलम. उबकर दिल्ली चला आया, देशबंधु कॉलेज, यहाँ भी पहले दिन जाति पूछी गई. यही नहीं सवर्णों की आपसी जातिगत गुटबंदी भी थी. फिर एम. ए. और उससे आगे, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर, हॉस्टल भी सवर्ण जातियों ने आपस में बाँट लिया था और बिहार की तरह ही गुंडई का केंद्र. कौन कहता है, बच्चों को जाति का ज्ञान नहीं होता ? स्कूल से लेकर बी.ए., कितनी उम्र होती है, सोलह से अठारह साल, कहाँ से सीखता है बच्चा जातीय ज्ञान, नफरत और भेदभाव? – निः संदेह परिवार ही पहली पाठशाला है. कहानी और भी है, धीरे-धीरे विस्तार से बयां करेंगे….
भारतीय समाज में दलित साहित्य और राजनीति
 भारतीय समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का आधार मानी जाती है. परन्तु दलित समाज के लिए एक सामान संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही. चतुर्वर्ण व्यवस्था से अधिक निकृष्ट और कोई सामाजिक संगठन कभी नहीं पनप पाया, बल्कि इस व्यवस्था ने तो दलित समाज के लोगों को मृत, पंगु तथा अशक्त बनाकर अच्छा कर्म करने से रोकने का आधार तैयार किया. हिन्दू धर्म ने तो दलितों को युगों से गुलाम बनाकर रौंदा है. एक वर्ग दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठतम के अहंकार से लिप्त हिन्दू धर्म सभ्यता की झूठी आडम्बरी संस्कृति ने दलितों को हाशिए पर धकेलकर बहिष्कृतों की तरह जीने के लिए मजबूर किया है. ब्राह्मणवादी सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दलितों का प्रवेश निषेध कर दिया गया. उसे उत्पादनों के तमाम संसाधनों के हकों से वंचित कर दिया गया. जिस कारण से उसके लिए आर्थिक सत्ता को प्राप्त करने के सब सुलभ रास्ते बंद कर दिए गए. केवल बाकी बचा अस्पृश्यता का अदृश्य अदद शरीर. लेकिन उस अदद शरीर को भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी कब्जा कर लिया गया. कब्जा करके गुलामी की बेड़ियों से जकड़कर सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके आज भी ताजा उदाहरण हमारे ग्रामीण परिवेश में नज़र आते हैं.
हिन्दू समाज ने दलित समाज को अपने में समेटता हुआ अधिकारहीन, अपवित्र करार दिया, जो राजसत्ता की मोहर की तरह जिन्दा और आज तक कायम है. समाज में जातिगत अपमान और उत्पीड़न की जड़ें गहरी हैं. एक लम्बे ऐतिहासिक काल से सामाजिक संरचना में इसकी मौजूदगी की निरन्तरता के कारण उसकी जटिल संश्लिष्ट प्रकृति सामने आती है. उसे देखकर इसके अस्तित्व का कभी खात्मा हो पाएगा, यह बात असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि बहिष्कृत समाज गांव, कस्बों एवं नगरों की दक्षिण दिशा में अंधकारमय बस्तियों में सिसकता रहा है. ऐसी गुमनाम जिन्दगी, जिसमें अभाव, अपमान, अवहेलना, पीड़ा और तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं. इसको तो जन्म से ही अपवित्र माना जाता रहा है. अपवित्रता का अभिशाप झेलने की विवशता और उत्पीड़न के साथ जी रहा है.
सर्वप्रथम इस जातिवादी-ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कट्टर प्रहार तथागत गौतम बौद्ध ने किया. समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया. दलितों एव स्त्रियों के लिए बौद्ध विहारों में प्रवेश के माध्यम से ज्ञान का मार्ग प्रस्शत किया. थेर और थेरी गाथाओं में रचित साहित्य दलितों और स्त्रियों के दुख दर्द की अभिव्यक्ति दिखायी देती है जिसे सर्वप्रथम दलित साहित्य (काव्य) की श्रेणी में रखा जाता है. बौद्ध काल को स्वर्णकाल कहा गया परन्तु भारतीय हिन्दूवादी संकीर्ण राजनीति ने अपने कपटतापूर्ण व्यव्हार से बौद्ध-विहारों को नष्ट कर वैदिक संस्कृति की नींव रखने में सफलता प्राप्त की. शंकराचार्य जैसे लोगों ने बौद्ध विहारों को नष्ट करने के लिए उनमें प्रवेश कर गंदी राजनीति का खेल खेला और बौद्धों के विहारों को नष्ट करने के लिए एकजुट होकर उनके द्वारा रचित साहित्य को खत्म कर दिया. तक्षशीला जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को तीन दिन तक जलाकर विपुल बौद्ध साहित्य को खत्म कर दिया गया. यही वजह रही कि आज हमे बौद्ध साहित्य प्राप्त नहीं होता जो बचा वह विदेशों में मिलता है. इस समय ही दलित साहित्य की नींव पड़ गयी थी जिसे आगे चलकर दलित संत-परम्परा ने जिंदा रखा. उन्होंने उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की जिसकी नींव तथागत बुद्ध ने डाली थी.
संत कबीर, संत रैदास, संत सवता माली ने अपनी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की स्थापना की. भारतीय मुख्यधारा के साहित्य में इनकी रचनाओं और संदेश को भक्तिवादी साहित्य ही माना गया. उन्हे एक युगंतकारी मूलगामी परिवर्तक के तौर पर न देखना राजनीति का ही परिणाम रहा. संत सविता माली जो नामदेव के समकालीन थे, इसी परंपरा से महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए जिनको सारा राष्ट्र आदर, श्रद्धा सम्मान और स्नेह से ज्योतिबा कहता है. हिन्दू समाज में अछूत”” मानी जाने वाली जातियों के लिए सम्भवतः सबसे पहले उन्नीसवी सदी में जोतिराव फुले ने ‘दलित’ शब्द का प्रयोग किया. उन्हें जाति विरोधी आन्दोलनों का अग्रदूत कहा जा सकता है. 1840 में उन्होंने मुम्बई में खास तौर पर अछूतों”” के लिए एक स्कूल खोला और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ‘शूद्र और अतिशूद्र”” कही जाने वाली जातियों को अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ब्राह्मण धर्मशास्त्रा में प्रतिपादित विचारधारा के प्रभाव से मुक्त कराना था. महात्मा फूले ने हिन्दू विधवा स्त्रियों के लिए, उनके बाल काटने का विरोध करने के लिए नाइयों की हड़ताल करवा दी थी जो भारतीय ढांचे का एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था. उन्होंने गुलामगिरी के माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया. शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया और सबसे पहले अपनी पत्नी को पढाया जो कालान्तर में भारत की पहली शिक्षिका बनी. मुक्ता बाई जैसे महिलाएं उनकी छात्राएं बनी. मुक्ता बाई जब 14 साल की थी तब उसने महार जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर एक निबंध लिखा जो अहमनगर से प्रकाशित एक अखबार में विस्तार से छपा. यह दलित छात्रा की पहली रचना थी जो स्त्रियों के दयनीय जीवन पर आधारित रचना थी. ये सब भी उसी राजनीति का शिकार हुए और एक युग का अन्त हुआ.
तथागत बुद्ध से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्री बाई फुले के कार्यों को आगे बढाते हुए डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलित एकता, समानता, स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आजीवन संघर्ष किया. राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने पूना-पैक्ट किया और संविधान के माध्यम से सभी अधिकारों में सामानता दी. स्त्रियों के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया जो संसद में उस रूप में पारित नहीं हो पाया जिस रूप में बाबासाहेब ने इसे बनाया था. इसके कारण उन्होंने संसद में कानून मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था. मनुस्मृति जो दलितों और स्त्रियों के लिए हिन्दू कानून के रूप में काम करती थी उसका दहन कर उस व्यवस्था को खत्म किया जो सदियों से दलितों को गुलाम बनाने के लिए बनी थी. उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार हो रहे इस सामाजिक उत्पीड़न को एक के ऊपर एक रखे उन मटकों के समान माना है, जिनमे सबसे नीचे के मटके में दलित और आदिवासी है. वर्ण व जाति के इस मानव निर्मित जाल की बुनतर को बाबासाहेब बखूबी समझते थे इसलिए उन्होंने जाति-व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने का बीड़ा उठाया. उन्होंने कहा- “मैं हिन्दू समाज में पैदा हुआ पर इसमे मरुंगा नही”. सन 1956 में दस लाख लोगों के साथ बाबासाहेब ने नागपुर में हिन्दू धर्म का त्याग कर और बौद्ध धर्म ग्रहण कर दलितों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया था. लोकतंत्र के माध्यम से सता प्राप्ति का अधिकार दलितों और आदिवासियों के लिए दिया. बाबासाहेब शिक्षा को शेरनी का दूध कहते थे. इसलिए उन्होंने हमेशा पैन और प्रैस पर जोर दिया. दलितों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अपने अनुभव अपनी कलम से लिखो ताकि आने वाली पीढ़ियां उस साहित्य को पढे. उस दौर में लिखा गया साहित्य दलित साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. दलित महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने दुख-दर्द एक दूसरे से सांझा किये .
उस दौर से प्रेरणा लेकर अम्बेडकरी साहित्य आज विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है. दलित, जिसमें दलित महिलाएं भी शामिल हैं, आज मुख्यधारा के साहित्य को टक्कर देकर भूमंडलीकरण साहित्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए है. आज दलित साहित्य को स्कूलों और कालेज तथा विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में पढाया जाना इस साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. फिर भी इतने संघर्षों और कुर्बानियों के बावजूद भी आज दलितों और आदिवासियों के साहित्य को मूल रूप से नहीं पढाया जाता बल्कि उसमें राजनीति एक अहं रोल अदा करती दिखाई देती है. राजनीति उस दलित काव्य को नजरादंज करती है जो उस व्यवस्था पर चोट करती है जो मूलगामी परिवर्तन व दलित तथा बहुजन एकता की बात करते हैं. राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज की एकता स्थापित हो जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था .
भारतीय समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का आधार मानी जाती है. परन्तु दलित समाज के लिए एक सामान संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही. चतुर्वर्ण व्यवस्था से अधिक निकृष्ट और कोई सामाजिक संगठन कभी नहीं पनप पाया, बल्कि इस व्यवस्था ने तो दलित समाज के लोगों को मृत, पंगु तथा अशक्त बनाकर अच्छा कर्म करने से रोकने का आधार तैयार किया. हिन्दू धर्म ने तो दलितों को युगों से गुलाम बनाकर रौंदा है. एक वर्ग दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठतम के अहंकार से लिप्त हिन्दू धर्म सभ्यता की झूठी आडम्बरी संस्कृति ने दलितों को हाशिए पर धकेलकर बहिष्कृतों की तरह जीने के लिए मजबूर किया है. ब्राह्मणवादी सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दलितों का प्रवेश निषेध कर दिया गया. उसे उत्पादनों के तमाम संसाधनों के हकों से वंचित कर दिया गया. जिस कारण से उसके लिए आर्थिक सत्ता को प्राप्त करने के सब सुलभ रास्ते बंद कर दिए गए. केवल बाकी बचा अस्पृश्यता का अदृश्य अदद शरीर. लेकिन उस अदद शरीर को भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी कब्जा कर लिया गया. कब्जा करके गुलामी की बेड़ियों से जकड़कर सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके आज भी ताजा उदाहरण हमारे ग्रामीण परिवेश में नज़र आते हैं.
हिन्दू समाज ने दलित समाज को अपने में समेटता हुआ अधिकारहीन, अपवित्र करार दिया, जो राजसत्ता की मोहर की तरह जिन्दा और आज तक कायम है. समाज में जातिगत अपमान और उत्पीड़न की जड़ें गहरी हैं. एक लम्बे ऐतिहासिक काल से सामाजिक संरचना में इसकी मौजूदगी की निरन्तरता के कारण उसकी जटिल संश्लिष्ट प्रकृति सामने आती है. उसे देखकर इसके अस्तित्व का कभी खात्मा हो पाएगा, यह बात असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि बहिष्कृत समाज गांव, कस्बों एवं नगरों की दक्षिण दिशा में अंधकारमय बस्तियों में सिसकता रहा है. ऐसी गुमनाम जिन्दगी, जिसमें अभाव, अपमान, अवहेलना, पीड़ा और तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं. इसको तो जन्म से ही अपवित्र माना जाता रहा है. अपवित्रता का अभिशाप झेलने की विवशता और उत्पीड़न के साथ जी रहा है.
सर्वप्रथम इस जातिवादी-ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कट्टर प्रहार तथागत गौतम बौद्ध ने किया. समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया. दलितों एव स्त्रियों के लिए बौद्ध विहारों में प्रवेश के माध्यम से ज्ञान का मार्ग प्रस्शत किया. थेर और थेरी गाथाओं में रचित साहित्य दलितों और स्त्रियों के दुख दर्द की अभिव्यक्ति दिखायी देती है जिसे सर्वप्रथम दलित साहित्य (काव्य) की श्रेणी में रखा जाता है. बौद्ध काल को स्वर्णकाल कहा गया परन्तु भारतीय हिन्दूवादी संकीर्ण राजनीति ने अपने कपटतापूर्ण व्यव्हार से बौद्ध-विहारों को नष्ट कर वैदिक संस्कृति की नींव रखने में सफलता प्राप्त की. शंकराचार्य जैसे लोगों ने बौद्ध विहारों को नष्ट करने के लिए उनमें प्रवेश कर गंदी राजनीति का खेल खेला और बौद्धों के विहारों को नष्ट करने के लिए एकजुट होकर उनके द्वारा रचित साहित्य को खत्म कर दिया. तक्षशीला जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को तीन दिन तक जलाकर विपुल बौद्ध साहित्य को खत्म कर दिया गया. यही वजह रही कि आज हमे बौद्ध साहित्य प्राप्त नहीं होता जो बचा वह विदेशों में मिलता है. इस समय ही दलित साहित्य की नींव पड़ गयी थी जिसे आगे चलकर दलित संत-परम्परा ने जिंदा रखा. उन्होंने उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की जिसकी नींव तथागत बुद्ध ने डाली थी.
संत कबीर, संत रैदास, संत सवता माली ने अपनी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की स्थापना की. भारतीय मुख्यधारा के साहित्य में इनकी रचनाओं और संदेश को भक्तिवादी साहित्य ही माना गया. उन्हे एक युगंतकारी मूलगामी परिवर्तक के तौर पर न देखना राजनीति का ही परिणाम रहा. संत सविता माली जो नामदेव के समकालीन थे, इसी परंपरा से महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए जिनको सारा राष्ट्र आदर, श्रद्धा सम्मान और स्नेह से ज्योतिबा कहता है. हिन्दू समाज में अछूत”” मानी जाने वाली जातियों के लिए सम्भवतः सबसे पहले उन्नीसवी सदी में जोतिराव फुले ने ‘दलित’ शब्द का प्रयोग किया. उन्हें जाति विरोधी आन्दोलनों का अग्रदूत कहा जा सकता है. 1840 में उन्होंने मुम्बई में खास तौर पर अछूतों”” के लिए एक स्कूल खोला और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ‘शूद्र और अतिशूद्र”” कही जाने वाली जातियों को अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ब्राह्मण धर्मशास्त्रा में प्रतिपादित विचारधारा के प्रभाव से मुक्त कराना था. महात्मा फूले ने हिन्दू विधवा स्त्रियों के लिए, उनके बाल काटने का विरोध करने के लिए नाइयों की हड़ताल करवा दी थी जो भारतीय ढांचे का एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था. उन्होंने गुलामगिरी के माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया. शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया और सबसे पहले अपनी पत्नी को पढाया जो कालान्तर में भारत की पहली शिक्षिका बनी. मुक्ता बाई जैसे महिलाएं उनकी छात्राएं बनी. मुक्ता बाई जब 14 साल की थी तब उसने महार जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर एक निबंध लिखा जो अहमनगर से प्रकाशित एक अखबार में विस्तार से छपा. यह दलित छात्रा की पहली रचना थी जो स्त्रियों के दयनीय जीवन पर आधारित रचना थी. ये सब भी उसी राजनीति का शिकार हुए और एक युग का अन्त हुआ.
तथागत बुद्ध से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्री बाई फुले के कार्यों को आगे बढाते हुए डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलित एकता, समानता, स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आजीवन संघर्ष किया. राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने पूना-पैक्ट किया और संविधान के माध्यम से सभी अधिकारों में सामानता दी. स्त्रियों के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया जो संसद में उस रूप में पारित नहीं हो पाया जिस रूप में बाबासाहेब ने इसे बनाया था. इसके कारण उन्होंने संसद में कानून मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था. मनुस्मृति जो दलितों और स्त्रियों के लिए हिन्दू कानून के रूप में काम करती थी उसका दहन कर उस व्यवस्था को खत्म किया जो सदियों से दलितों को गुलाम बनाने के लिए बनी थी. उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार हो रहे इस सामाजिक उत्पीड़न को एक के ऊपर एक रखे उन मटकों के समान माना है, जिनमे सबसे नीचे के मटके में दलित और आदिवासी है. वर्ण व जाति के इस मानव निर्मित जाल की बुनतर को बाबासाहेब बखूबी समझते थे इसलिए उन्होंने जाति-व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने का बीड़ा उठाया. उन्होंने कहा- “मैं हिन्दू समाज में पैदा हुआ पर इसमे मरुंगा नही”. सन 1956 में दस लाख लोगों के साथ बाबासाहेब ने नागपुर में हिन्दू धर्म का त्याग कर और बौद्ध धर्म ग्रहण कर दलितों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया था. लोकतंत्र के माध्यम से सता प्राप्ति का अधिकार दलितों और आदिवासियों के लिए दिया. बाबासाहेब शिक्षा को शेरनी का दूध कहते थे. इसलिए उन्होंने हमेशा पैन और प्रैस पर जोर दिया. दलितों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अपने अनुभव अपनी कलम से लिखो ताकि आने वाली पीढ़ियां उस साहित्य को पढे. उस दौर में लिखा गया साहित्य दलित साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. दलित महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने दुख-दर्द एक दूसरे से सांझा किये .
उस दौर से प्रेरणा लेकर अम्बेडकरी साहित्य आज विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है. दलित, जिसमें दलित महिलाएं भी शामिल हैं, आज मुख्यधारा के साहित्य को टक्कर देकर भूमंडलीकरण साहित्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए है. आज दलित साहित्य को स्कूलों और कालेज तथा विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में पढाया जाना इस साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. फिर भी इतने संघर्षों और कुर्बानियों के बावजूद भी आज दलितों और आदिवासियों के साहित्य को मूल रूप से नहीं पढाया जाता बल्कि उसमें राजनीति एक अहं रोल अदा करती दिखाई देती है. राजनीति उस दलित काव्य को नजरादंज करती है जो उस व्यवस्था पर चोट करती है जो मूलगामी परिवर्तन व दलित तथा बहुजन एकता की बात करते हैं. राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज की एकता स्थापित हो जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था .
नहीं दिया दलित बच्चों को दाखिला, स्कूलों ने हड़पी 100 करोड़ की स्कॉलरशिप
 चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की निगरानी में दलित छात्रों के नाम पर हो रहे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. आप की पंजाब इकाई के संयोजक गुरप्रीत सिंह वडैच ने आज यहां कहा कि शिक्षा माफिया इस फर्जीवाड़े के जरिये सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए डकार रहा है.
पार्टी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है. निजी शिक्षा संस्थाओं में वर्ष 2014-15 के लिए 30 हजार फर्जी दाखिले दिखाकर सरकार से 100 करोड़ रुपए हड़पे गए. उन्होंने कहा कि यह राशि दलित छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए थी. वडैच ने कहा कि करोड़ों के इस घोटाले के लिये अकाली भाजपा गठबंधन सरकार जिम्मेदार है.
सरकार की शह पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा है. कांग्रेस ने भी मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई क्योंकि निजी शिक्षा माफिया में अकाली-भाजपा नेताओं के साथ कांग्रेसी भी शामिल हैं. आप नेता के अनुसार इस घोटाले के कारण दलित छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा. दलितों के अलावा गरीब छात्रों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं.
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की निगरानी में दलित छात्रों के नाम पर हो रहे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. आप की पंजाब इकाई के संयोजक गुरप्रीत सिंह वडैच ने आज यहां कहा कि शिक्षा माफिया इस फर्जीवाड़े के जरिये सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए डकार रहा है.
पार्टी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है. निजी शिक्षा संस्थाओं में वर्ष 2014-15 के लिए 30 हजार फर्जी दाखिले दिखाकर सरकार से 100 करोड़ रुपए हड़पे गए. उन्होंने कहा कि यह राशि दलित छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए थी. वडैच ने कहा कि करोड़ों के इस घोटाले के लिये अकाली भाजपा गठबंधन सरकार जिम्मेदार है.
सरकार की शह पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा है. कांग्रेस ने भी मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई क्योंकि निजी शिक्षा माफिया में अकाली-भाजपा नेताओं के साथ कांग्रेसी भी शामिल हैं. आप नेता के अनुसार इस घोटाले के कारण दलित छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा. दलितों के अलावा गरीब छात्रों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. भारत में जानवर हत्या पाप है और दलित हत्या पुण्य !
 जिस समाज में हम रहते हैं वह उत्सव प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, पशु प्रेमी तो है मगर मानवता प्रेमी नहीं है. ऐसा इसलिए कि मरे हुए पशु की खाल को रोजी-रोटी का साधन बनाने वाले गुजरात के ऊना शहर में दलित युवकों की तालीबानी अंदाज में खाल उधेड़ दी गयी, जो ब्रिटिश हूकूमत की दमन की नीति को ताजा कर देती है. आज विश्व में 90 प्रतिशत चमड़ा उद्योग गोवंशीय पशुओं की खाल पर ही निर्भर है. चमड़े के उत्पादों की विश्व बाजार में बड़ी मांग है. इन उद्योंगों/फैक्टरियों में क्या गाय की खाल नहीं जाती होगी पशु प्रेमियों से यही प्रश्न है कि आपने अभी तक कितने चमड़े की फैक्टरियों को बंद कराया है?
दलित जो आजादी के 70 वर्ष बाद भी शोषण और प्रताड़नाओं, छुआछूत, हिन्दू धर्म की आंतरिक संरचना की गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो पाया है. इसमें दोष किसका माना जाये धर्म का या राजनीति का? दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मरी हुई गाय की खाल ले जाने पर गरीब दलित युवको की खाल उधेड़ दी जाती है और आटा छूने पर उत्तराखण्ड में एक ब्राह्मण शिक्षक द्धारा दलित युवक की गर्दन काट दी जाती है आखिर क्यों? हल जोतकर दिन रात पसीना बहाकर जो दलित ब्राहमण के घर में अनाज का ढेर लगाता है और खुद भूखा-प्यासा रहता है, तब वो ब्राह्मण क्यों उसकी पैदा की गयी फसल और अनाज को अपवित्र नहीं मानता? इतना ही नहीं जो शिल्पकार उनके मकानों को बनाता है तब उनके बनाये मकानों में क्यों निवास करते हैं?
वंचितों को उत्पीड़ित करने का यह नया तरीका हिन्दुस्तान के सामाजिक ताने-बाने को अवश्य ही बिगाड़ने का काम कर रहा है, जिसकी कटु से कटु शब्दों में निंदा की जानी चाहिए. गौरक्षा अच्छी पहल है शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, मगर एक दलित युवक का सरेआम हलाल किया गया तब अहिंसा के पुजारी और मानवता के पुजारी तथा सनातन धर्म के ठेकेदार चुप क्यों?
आज हकीकत मालूम हो गयी कि भारत में जानवर हत्या पाप है और दलित हत्या पुण्य है. भारत की विडंबना ही कही जायेगी कि वेदों से लेकर मनुस्मृति तक सभी धर्म ग्रंथ दलितों के खिलाफ हैं. भारतीय शास्त्र और धर्म इंसान को अछूत मानता है. जबकि संविधान सभी ग्रंथों से ऊपर है संविधान की मर्यादा को लांघकर किया गया अमानवीय कृत्य देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर धकेल देगा! गौरक्षा ही क्यों प्राणी मात्र की रक्षा और सेवा करना सच्चे मानव धर्म की पहचान होनी चाहिए. धर्म और जाति के नाम पर उन्माद और गुंडा गर्दी, कानून की अवहेलना करना सब संविधान के विरूद्ध किया गया आचरण है. भारत ने मंगल ग्रह की दूरी तो नाप दी है जो गर्व की बात है मगर देश को जिन बातों पर अभिमान है उनमें जातपांत भी एक है. जातिवाद की खाई को मिटाने या कम करने में समाज और देश की राजनीति और देश का धर्म अवश्य ही विफल रहा है.
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में भाषण देते हैं तो भारत को बुद्ध की धरती कहकर संबोधित करते है मगर अमेरिका, जापान, फ्रांस सब जानता है कि भारत प्राचीन काल में बुद्ध की भूमि अवश्य थी मगर अफसोस अब अगड़ों और पिछड़ों की युद्ध भूमि बनती जा रही है. सबका साथ सबका विकास नहीं वरन देश में अगड़ों का सम्मान और दलितों का अपमान हो रहा है जो चिंता का विषय है. गाय से मंदिर तक, नल से जल तक, स्कूल से कॉलेज तक, गांव से श्मशान तक, शिक्षक से डॉक्टर तक, चपरासी से अफसर तक बच्चे से बूढ़े तक, बेटी-बहन से मां तक हर रोज देश का वंचित समाज दलित होने का दंश झेल रहा हैं और उत्पीडन का शिकार हो रहा और अपमानित हो रहा है. दलितों के वोट तो कीमती हैं मगर उनका लहू पानी से भी सस्ता.
बागेश्वर जनपद के भेटा गांव (उत्तराखण्ड) की घटना ने देश को शर्मसार तो किया ही है लेकिन इस घटना ने एक क्रांतिकारी संदेश भी दिया है कि अब देश का दलित अपने ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण को सहन नहीं करेगा. जिस तरह 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था जिसमें कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में बहा दिया गया था उसी प्रकार 12 अक्टूबर 2016 को उत्तराखण्ड के शिल्पकार समाज ने जिसकी अगुवाई शिक्षक संगठन ने की, ब्राह्मणवाद के प्रतीक टीका चंदन को त्यागने का संकल्प लिया और मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाये और डा. अम्बेडकर के नीले रंग को धारण करने की भीम प्रतिज्ञा की. संगठित होकर पूरे उत्तराखण्ड के दलित समुदाय विरोध प्रदर्शिन करने सड़कों पर उतर आया और डॉ. अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मार्ग पर चलने लगा है जिसके दूरगामी परिणाम अवश्य ही दिखाई देंगे.
जिस समाज में हम रहते हैं वह उत्सव प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, पशु प्रेमी तो है मगर मानवता प्रेमी नहीं है. ऐसा इसलिए कि मरे हुए पशु की खाल को रोजी-रोटी का साधन बनाने वाले गुजरात के ऊना शहर में दलित युवकों की तालीबानी अंदाज में खाल उधेड़ दी गयी, जो ब्रिटिश हूकूमत की दमन की नीति को ताजा कर देती है. आज विश्व में 90 प्रतिशत चमड़ा उद्योग गोवंशीय पशुओं की खाल पर ही निर्भर है. चमड़े के उत्पादों की विश्व बाजार में बड़ी मांग है. इन उद्योंगों/फैक्टरियों में क्या गाय की खाल नहीं जाती होगी पशु प्रेमियों से यही प्रश्न है कि आपने अभी तक कितने चमड़े की फैक्टरियों को बंद कराया है?
दलित जो आजादी के 70 वर्ष बाद भी शोषण और प्रताड़नाओं, छुआछूत, हिन्दू धर्म की आंतरिक संरचना की गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो पाया है. इसमें दोष किसका माना जाये धर्म का या राजनीति का? दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मरी हुई गाय की खाल ले जाने पर गरीब दलित युवको की खाल उधेड़ दी जाती है और आटा छूने पर उत्तराखण्ड में एक ब्राह्मण शिक्षक द्धारा दलित युवक की गर्दन काट दी जाती है आखिर क्यों? हल जोतकर दिन रात पसीना बहाकर जो दलित ब्राहमण के घर में अनाज का ढेर लगाता है और खुद भूखा-प्यासा रहता है, तब वो ब्राह्मण क्यों उसकी पैदा की गयी फसल और अनाज को अपवित्र नहीं मानता? इतना ही नहीं जो शिल्पकार उनके मकानों को बनाता है तब उनके बनाये मकानों में क्यों निवास करते हैं?
वंचितों को उत्पीड़ित करने का यह नया तरीका हिन्दुस्तान के सामाजिक ताने-बाने को अवश्य ही बिगाड़ने का काम कर रहा है, जिसकी कटु से कटु शब्दों में निंदा की जानी चाहिए. गौरक्षा अच्छी पहल है शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, मगर एक दलित युवक का सरेआम हलाल किया गया तब अहिंसा के पुजारी और मानवता के पुजारी तथा सनातन धर्म के ठेकेदार चुप क्यों?
आज हकीकत मालूम हो गयी कि भारत में जानवर हत्या पाप है और दलित हत्या पुण्य है. भारत की विडंबना ही कही जायेगी कि वेदों से लेकर मनुस्मृति तक सभी धर्म ग्रंथ दलितों के खिलाफ हैं. भारतीय शास्त्र और धर्म इंसान को अछूत मानता है. जबकि संविधान सभी ग्रंथों से ऊपर है संविधान की मर्यादा को लांघकर किया गया अमानवीय कृत्य देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर धकेल देगा! गौरक्षा ही क्यों प्राणी मात्र की रक्षा और सेवा करना सच्चे मानव धर्म की पहचान होनी चाहिए. धर्म और जाति के नाम पर उन्माद और गुंडा गर्दी, कानून की अवहेलना करना सब संविधान के विरूद्ध किया गया आचरण है. भारत ने मंगल ग्रह की दूरी तो नाप दी है जो गर्व की बात है मगर देश को जिन बातों पर अभिमान है उनमें जातपांत भी एक है. जातिवाद की खाई को मिटाने या कम करने में समाज और देश की राजनीति और देश का धर्म अवश्य ही विफल रहा है.
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में भाषण देते हैं तो भारत को बुद्ध की धरती कहकर संबोधित करते है मगर अमेरिका, जापान, फ्रांस सब जानता है कि भारत प्राचीन काल में बुद्ध की भूमि अवश्य थी मगर अफसोस अब अगड़ों और पिछड़ों की युद्ध भूमि बनती जा रही है. सबका साथ सबका विकास नहीं वरन देश में अगड़ों का सम्मान और दलितों का अपमान हो रहा है जो चिंता का विषय है. गाय से मंदिर तक, नल से जल तक, स्कूल से कॉलेज तक, गांव से श्मशान तक, शिक्षक से डॉक्टर तक, चपरासी से अफसर तक बच्चे से बूढ़े तक, बेटी-बहन से मां तक हर रोज देश का वंचित समाज दलित होने का दंश झेल रहा हैं और उत्पीडन का शिकार हो रहा और अपमानित हो रहा है. दलितों के वोट तो कीमती हैं मगर उनका लहू पानी से भी सस्ता.
बागेश्वर जनपद के भेटा गांव (उत्तराखण्ड) की घटना ने देश को शर्मसार तो किया ही है लेकिन इस घटना ने एक क्रांतिकारी संदेश भी दिया है कि अब देश का दलित अपने ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण को सहन नहीं करेगा. जिस तरह 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था जिसमें कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में बहा दिया गया था उसी प्रकार 12 अक्टूबर 2016 को उत्तराखण्ड के शिल्पकार समाज ने जिसकी अगुवाई शिक्षक संगठन ने की, ब्राह्मणवाद के प्रतीक टीका चंदन को त्यागने का संकल्प लिया और मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाये और डा. अम्बेडकर के नीले रंग को धारण करने की भीम प्रतिज्ञा की. संगठित होकर पूरे उत्तराखण्ड के दलित समुदाय विरोध प्रदर्शिन करने सड़कों पर उतर आया और डॉ. अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मार्ग पर चलने लगा है जिसके दूरगामी परिणाम अवश्य ही दिखाई देंगे.
दीक्षाभूमि पर उमड़ा भीम सैलाब, 20 हजार लोगों ने ली बौद्ध धम्म की दीक्षा
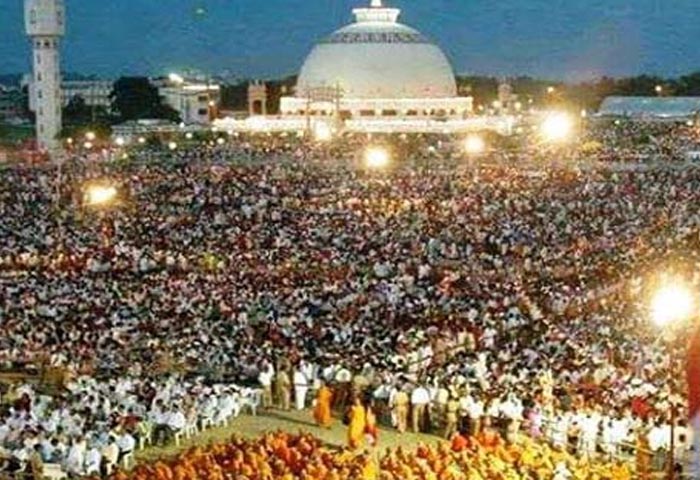 नागपुर। बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर की धम्मक्रांति भूमि नागपुर की पवित्र दीक्षाभूमि पर 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन लाखों बौद्ध अनुयायियों ने तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. अशोक विजयदशमी 14 अक्तूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह मनाया गया. बाबासाहेब ने 14 अक्तूबर 1956 को बौद्ध धम्म अपनाया था. इस दिन लाखों अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर महामानव को नमन किया. भारत और विश्व के बौद्धों के लिए दीक्षाभूमि आधुनिक तीर्थ स्थल है. भारत में बौद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुंबिनी की तरह ही दीक्षाभूमि भी पूजनीय है.
हाथ में पंचशील और नीले झंडे लेकर देशभर से लाखों लोग इस वर्ष भी दीक्षाभूमि पहुंचे थे. धर्मांतरण की यह 60वीं वर्षगांठ होने के कारण पहले से भी अधिक संख्या में अम्बेडकरी अनुयायी इस वर्ष नागपुर आये थे. उनमें कुछ विदेशी मेहमान भी थे. बौद्ध देश के लोग तो दीक्षाभूमि पर आते ही है. अब पश्चिमी देशों के लोग भी इस समारोह को देखने के लिए आने लगे है. धम्मचक्र प्रवर्तन समारोह में उमड़े भीम सैलाब को देखकर उन्हें (विदेशियों को) बाबासाहेब अम्बेडकर के महान कार्य की महत्ता ज्ञात हुई.
डॉ. अम्बेडकर के साथ पांच लाख लोगों ने हिंदू धर्म त्यागकर समता, करुणा, शांति का संदेश देने वाले महान बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी. विश्व में शांतिपूर्वक हुए इस धम्म क्रांति ने इतिहास रच दिया है. 1956 के धर्मांतरण समारोह के बाद से हर वर्ष अशोक विजयदशमी को लाखों अम्बेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमि पर पहुंचकर तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को स्मरण कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं. यह परंपरा 60 वर्षों से लगातार जारी है.
हर वर्ष इस भूमि पर बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम भी होता है. आयोजकों ने दावा किया है कि इस वर्ष करीब 20 हजार लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है. त्रिशरण-पंचशील ग्रहण कर तथा 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने की शपथ लेकर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर दीक्षाभूमि के साथ ही पूरा नागपुर नमो बुद्धाय-जय भीम के नारों से गुंज उठा था. नीले झंडे, पंचशील झंडे, बैनर, होर्डिंग से शहर भीममय हो गया था. शहर के हर रास्ते केवल और केवल दीक्षाभूमि की ओर जाते हुए प्रतित हो रहे थे. विभिन्न राज्यों के अम्बेडकरी अनुयायी अपनी परंपरागत वेषभूशा और वाद्यों के साथ भीम-बुद्ध का जयघोष करते और गीत गाते हुए दीक्षाभूमि पहुंच रहे थे. शहर के कोनो-कोनो से जुलूस निकालकर लोग जय भीम करते दीक्षाभूमि पर पहुंचे. समता सैनिक दल की विभिन्न प्रदेश शाखाओं ने दीक्षाभूमि तक मार्च निकाले.
दीक्षाभूमि पर चारों और से भीम सैलाब उमडा था. जगह-जगह भीम-बुद्ध गीतों के स्वर गुंज रहे थे. दीक्षाभूमि स्मारक पर तथागत बुद्ध की मूर्ति को नमन कर बाबासाहेब की अस्थियां और प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर लाखों लोग धन्य महसूस कर रहे थे. लाखों लोग केवल तथागत बुद्ध और महामानव डा. अम्बेडकर को नमन करने के लिए ही इस ऐतिहासिक दिन दीक्षाभूमि पर आते हैं. इस भूमि पर पहुंचकर नमन करना और लौटते वक्त विचार, पुस्तकों के साथ ज्ञानामृत साथ ले जाना ही अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य होता है.
दीक्षाभूमि पर डॉ.अम्बेडकर की किताबें, ग्रंथ, उनके विचारों के संग्रह, भाषण संग्रह, बुद्ध विचार, ग्रंथ, संविधान के साथ ही विभिन्न विषयों पर पुस्तकों के विविध प्रकाशकों के स्टॉल लगते है. इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल लगे थे. बुद्ध और अम्बेडकर की मूर्तियों की खूब बिक्री हुई. गीत- नाटकों की सीडी भी हर वर्ष की तरह बिके.
दीक्षाभूमिपर आनेवाले लोगों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इस वर्ष भी सामाजिक संगठनों ने की थी. करिब 500 संस्थाओं ने भोजनदान किया था. हर वर्ष की तरह अत्यधिक शांतिपूर्ण तरीके से यह समारोह संपन्न हुआ.
नागपुर। बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर की धम्मक्रांति भूमि नागपुर की पवित्र दीक्षाभूमि पर 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन लाखों बौद्ध अनुयायियों ने तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. अशोक विजयदशमी 14 अक्तूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह मनाया गया. बाबासाहेब ने 14 अक्तूबर 1956 को बौद्ध धम्म अपनाया था. इस दिन लाखों अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर महामानव को नमन किया. भारत और विश्व के बौद्धों के लिए दीक्षाभूमि आधुनिक तीर्थ स्थल है. भारत में बौद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुंबिनी की तरह ही दीक्षाभूमि भी पूजनीय है.
हाथ में पंचशील और नीले झंडे लेकर देशभर से लाखों लोग इस वर्ष भी दीक्षाभूमि पहुंचे थे. धर्मांतरण की यह 60वीं वर्षगांठ होने के कारण पहले से भी अधिक संख्या में अम्बेडकरी अनुयायी इस वर्ष नागपुर आये थे. उनमें कुछ विदेशी मेहमान भी थे. बौद्ध देश के लोग तो दीक्षाभूमि पर आते ही है. अब पश्चिमी देशों के लोग भी इस समारोह को देखने के लिए आने लगे है. धम्मचक्र प्रवर्तन समारोह में उमड़े भीम सैलाब को देखकर उन्हें (विदेशियों को) बाबासाहेब अम्बेडकर के महान कार्य की महत्ता ज्ञात हुई.
डॉ. अम्बेडकर के साथ पांच लाख लोगों ने हिंदू धर्म त्यागकर समता, करुणा, शांति का संदेश देने वाले महान बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी. विश्व में शांतिपूर्वक हुए इस धम्म क्रांति ने इतिहास रच दिया है. 1956 के धर्मांतरण समारोह के बाद से हर वर्ष अशोक विजयदशमी को लाखों अम्बेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमि पर पहुंचकर तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को स्मरण कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं. यह परंपरा 60 वर्षों से लगातार जारी है.
हर वर्ष इस भूमि पर बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम भी होता है. आयोजकों ने दावा किया है कि इस वर्ष करीब 20 हजार लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है. त्रिशरण-पंचशील ग्रहण कर तथा 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने की शपथ लेकर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर दीक्षाभूमि के साथ ही पूरा नागपुर नमो बुद्धाय-जय भीम के नारों से गुंज उठा था. नीले झंडे, पंचशील झंडे, बैनर, होर्डिंग से शहर भीममय हो गया था. शहर के हर रास्ते केवल और केवल दीक्षाभूमि की ओर जाते हुए प्रतित हो रहे थे. विभिन्न राज्यों के अम्बेडकरी अनुयायी अपनी परंपरागत वेषभूशा और वाद्यों के साथ भीम-बुद्ध का जयघोष करते और गीत गाते हुए दीक्षाभूमि पहुंच रहे थे. शहर के कोनो-कोनो से जुलूस निकालकर लोग जय भीम करते दीक्षाभूमि पर पहुंचे. समता सैनिक दल की विभिन्न प्रदेश शाखाओं ने दीक्षाभूमि तक मार्च निकाले.
दीक्षाभूमि पर चारों और से भीम सैलाब उमडा था. जगह-जगह भीम-बुद्ध गीतों के स्वर गुंज रहे थे. दीक्षाभूमि स्मारक पर तथागत बुद्ध की मूर्ति को नमन कर बाबासाहेब की अस्थियां और प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर लाखों लोग धन्य महसूस कर रहे थे. लाखों लोग केवल तथागत बुद्ध और महामानव डा. अम्बेडकर को नमन करने के लिए ही इस ऐतिहासिक दिन दीक्षाभूमि पर आते हैं. इस भूमि पर पहुंचकर नमन करना और लौटते वक्त विचार, पुस्तकों के साथ ज्ञानामृत साथ ले जाना ही अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य होता है.
दीक्षाभूमि पर डॉ.अम्बेडकर की किताबें, ग्रंथ, उनके विचारों के संग्रह, भाषण संग्रह, बुद्ध विचार, ग्रंथ, संविधान के साथ ही विभिन्न विषयों पर पुस्तकों के विविध प्रकाशकों के स्टॉल लगते है. इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल लगे थे. बुद्ध और अम्बेडकर की मूर्तियों की खूब बिक्री हुई. गीत- नाटकों की सीडी भी हर वर्ष की तरह बिके.
दीक्षाभूमिपर आनेवाले लोगों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इस वर्ष भी सामाजिक संगठनों ने की थी. करिब 500 संस्थाओं ने भोजनदान किया था. हर वर्ष की तरह अत्यधिक शांतिपूर्ण तरीके से यह समारोह संपन्न हुआ. सर्वेक्षणों पर संदेह का घेरा
 बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा की सदस्या एडवोकेट मायावती ने अपने समर्थकों को समाचार पत्रों एवं निजी टीवी चैनलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वेक्षणों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. उनका मानना है कि ये समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों का स्वामित्य पूंजीपतियों के पास है और वे बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के चुनाव के संदर्भ में नकारात्मक वातावरण पैदा कर रहे हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को जोर देकर यह समझाया है कि चुनाव के पहले ये सर्वेक्षण बहुजन समाज का मनोबल तोड़ने की पूंजीपतियों की साजिश का नतीजा है.
बसपा सुप्रीमो के उपरोक्त संदेह पर एक समाजशास्त्री के रूप में मेरा यह मानना है कि पद्धति शास्त्र, ज्ञान मिमांसा एवं सत्ता मिमांसा के आधार पर भारत में चुनाव सर्वेक्षणों ने अभी वह वैज्ञानिक तटस्थता नहीं प्राप्त की है, जैसा कि अमेरिकी और यूरोपिय देशों ने. इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय सामाजिक संरचना में जाति के आधार पर भेदभाव. यही भेदभाव चुनाव सर्वेक्षण की वैज्ञानिक तटस्थता को प्रमाणित करता है. सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने वाले तथा सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर किस समाज से कैसे प्रश्न पूछे जाए और जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे उत्तर देंगे, यह सब का सब तथ्य जाति अस्मिता द्वारा ही निर्धारित होते हैं. उदाहरण के लिए ज्यादातर सर्वेक्षण करने वाले सवर्ण समाज के शहरी क्षेत्र के रहने वाले युवा और युवती होते हैं, जिनकी चेतना में दलित, पिछड़े एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बस्ती में जाकर कैसे प्रश्नों का उत्तर लिया जाए, इसका नितांत अभाव होता है. बहुत से प्रश्नकर्ता दलितों एवं मलिन बस्ती में जाने से ही घिन्न महसूस करते हैं. और इसलिए वे उधर का रुख ही नहीं करते.
दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में दलित एवं अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति सामंतों एवं उच्च जातियों से भयभीत रहता है. इसलिए वह सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों का जानबूझ कर सही-सही उत्तर नहीं देता. ऐसी स्थिति में प्रश्नकर्ता एवं चुनाव अनुसंधानकर्ता के पास ऐसी कोई पद्धति नहीं होती; जिससे वह इस भोली-भाली सहमी एवं डरी जनता के अंदर की सत्यता को निकाल कर अपने परिणाम में शामिल कर सके. ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण की वैद्यता अपने आप ही संदिग्ध हो जाती है.
वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र के आधार पर चुनाव सर्वेक्षणों की दूसरी बड़ी संदिग्धता; एक अन्य तथ्य के आधार पर प्रमाणित की जा सकती है. वह तथ्य है, सर्वेक्षण के दौरान किसी भी दल को मिले मत प्रतिशतों को उस दल को मिलने वाली सीटों में तब्दील करना. यह स्थापित सत्य है कि किसी राजनैतिक दल द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त मत प्रतिशत को सीट में बदलने का कोई भी वैज्ञानिक फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया है. विशेष कर विविधता भरे इस भारतीय समाज में कोई भी यह सही-सही नहीं बता सकता कि अगर एक राजनैतिक दल को इतने मत मिलेंगे तो उसको इतनी सीट मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर यह देखने में आया है कि कम प्रतिशत वोट पाने वाले दलों को ज्यादा सीट मिल जाती है और ज्यादा मत पाने वाले को कम.
उदाहरण के लिए 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बसपा को यद्यति 27.5 प्रतिशत वोट मिले थे, परंतु उसको सीट मिली थी बीस. इसके समानान्तर कांग्रेस को 2009 में 18.3 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन उसने 21 सीटों पर चुनाव जीता था. इसी कड़ी में अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा को 19.8 प्रतिशत वोट मिले, परंतु उसको कोई भी सीट नहीं मिली. दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ 7.5 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद उसने दो सीटों पर चुनाव जीत लिया. अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी दल को सर्वेक्षण में मिले मतों के आधार पर उसको कितनी सीटें मिलेंगी, यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. शायद इसीलिए बसपा को अक्सर सर्वेक्षणों में पीछे दिखाया जाता है और उसको सर्वेक्षणों में कम मत प्रतिशत और सीटें मिलती दिखायी जाती हैं. यद्यपि वास्तविकता में परिणाम इससे बिल्कुल अलग और बेहतर होते हैं. 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं.
सर्वेक्षणों में मिले मत प्रतिशत के आधार पर उसे सीटों में कैसे बदला जाता है, और उसका क्या वैज्ञानिक फार्मूला है इसका खबरिया चैनल आज भी रहस्योदघाटन नहीं करते. वे किस पद्धति शास्त्र से यह गणना करते हैं कि कितने प्रतिशत वोट पर व्यक्ति एक सीट जीत जाएगा, वे इसका कोई भी आंकलन अपने दर्शकों को नहीं बतातें. शायद इसके पास कोई फार्मूला है ही नहीं. और इसीलिए सर्वेक्षण संदेह के घेरे में आ जाता है. चुनाव सर्वेक्षण केवल व्यापारिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें राजनीति के गरीब राजनैतिक दल पिछड़ जाते हैं और धनाढ्य राजनैतिक दल अपने पक्ष में निर्णय लाकर जनता के निर्णय को प्रभावित करते हैं. शायद इसीलिए पाश्चात्य देशों में मत प्रतिशत को सीटों में परिवर्तित करने की परंपरा नहीं है. जो कि एक साधारण अनुसंधानिक प्रक्रिया लगती है. और यही प्रक्रिया भारत में भी अपनायी जानी चाहिए. तब कहीं जाकर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण संदेह के घेरे से कुछ बाहर निकल पाएंगे.
बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा की सदस्या एडवोकेट मायावती ने अपने समर्थकों को समाचार पत्रों एवं निजी टीवी चैनलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वेक्षणों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. उनका मानना है कि ये समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों का स्वामित्य पूंजीपतियों के पास है और वे बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के चुनाव के संदर्भ में नकारात्मक वातावरण पैदा कर रहे हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को जोर देकर यह समझाया है कि चुनाव के पहले ये सर्वेक्षण बहुजन समाज का मनोबल तोड़ने की पूंजीपतियों की साजिश का नतीजा है.
बसपा सुप्रीमो के उपरोक्त संदेह पर एक समाजशास्त्री के रूप में मेरा यह मानना है कि पद्धति शास्त्र, ज्ञान मिमांसा एवं सत्ता मिमांसा के आधार पर भारत में चुनाव सर्वेक्षणों ने अभी वह वैज्ञानिक तटस्थता नहीं प्राप्त की है, जैसा कि अमेरिकी और यूरोपिय देशों ने. इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय सामाजिक संरचना में जाति के आधार पर भेदभाव. यही भेदभाव चुनाव सर्वेक्षण की वैज्ञानिक तटस्थता को प्रमाणित करता है. सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने वाले तथा सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर किस समाज से कैसे प्रश्न पूछे जाए और जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे उत्तर देंगे, यह सब का सब तथ्य जाति अस्मिता द्वारा ही निर्धारित होते हैं. उदाहरण के लिए ज्यादातर सर्वेक्षण करने वाले सवर्ण समाज के शहरी क्षेत्र के रहने वाले युवा और युवती होते हैं, जिनकी चेतना में दलित, पिछड़े एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बस्ती में जाकर कैसे प्रश्नों का उत्तर लिया जाए, इसका नितांत अभाव होता है. बहुत से प्रश्नकर्ता दलितों एवं मलिन बस्ती में जाने से ही घिन्न महसूस करते हैं. और इसलिए वे उधर का रुख ही नहीं करते.
दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में दलित एवं अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति सामंतों एवं उच्च जातियों से भयभीत रहता है. इसलिए वह सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों का जानबूझ कर सही-सही उत्तर नहीं देता. ऐसी स्थिति में प्रश्नकर्ता एवं चुनाव अनुसंधानकर्ता के पास ऐसी कोई पद्धति नहीं होती; जिससे वह इस भोली-भाली सहमी एवं डरी जनता के अंदर की सत्यता को निकाल कर अपने परिणाम में शामिल कर सके. ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण की वैद्यता अपने आप ही संदिग्ध हो जाती है.
वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र के आधार पर चुनाव सर्वेक्षणों की दूसरी बड़ी संदिग्धता; एक अन्य तथ्य के आधार पर प्रमाणित की जा सकती है. वह तथ्य है, सर्वेक्षण के दौरान किसी भी दल को मिले मत प्रतिशतों को उस दल को मिलने वाली सीटों में तब्दील करना. यह स्थापित सत्य है कि किसी राजनैतिक दल द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त मत प्रतिशत को सीट में बदलने का कोई भी वैज्ञानिक फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया है. विशेष कर विविधता भरे इस भारतीय समाज में कोई भी यह सही-सही नहीं बता सकता कि अगर एक राजनैतिक दल को इतने मत मिलेंगे तो उसको इतनी सीट मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर यह देखने में आया है कि कम प्रतिशत वोट पाने वाले दलों को ज्यादा सीट मिल जाती है और ज्यादा मत पाने वाले को कम.
उदाहरण के लिए 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बसपा को यद्यति 27.5 प्रतिशत वोट मिले थे, परंतु उसको सीट मिली थी बीस. इसके समानान्तर कांग्रेस को 2009 में 18.3 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन उसने 21 सीटों पर चुनाव जीता था. इसी कड़ी में अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा को 19.8 प्रतिशत वोट मिले, परंतु उसको कोई भी सीट नहीं मिली. दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ 7.5 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद उसने दो सीटों पर चुनाव जीत लिया. अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी दल को सर्वेक्षण में मिले मतों के आधार पर उसको कितनी सीटें मिलेंगी, यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. शायद इसीलिए बसपा को अक्सर सर्वेक्षणों में पीछे दिखाया जाता है और उसको सर्वेक्षणों में कम मत प्रतिशत और सीटें मिलती दिखायी जाती हैं. यद्यपि वास्तविकता में परिणाम इससे बिल्कुल अलग और बेहतर होते हैं. 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं.
सर्वेक्षणों में मिले मत प्रतिशत के आधार पर उसे सीटों में कैसे बदला जाता है, और उसका क्या वैज्ञानिक फार्मूला है इसका खबरिया चैनल आज भी रहस्योदघाटन नहीं करते. वे किस पद्धति शास्त्र से यह गणना करते हैं कि कितने प्रतिशत वोट पर व्यक्ति एक सीट जीत जाएगा, वे इसका कोई भी आंकलन अपने दर्शकों को नहीं बतातें. शायद इसके पास कोई फार्मूला है ही नहीं. और इसीलिए सर्वेक्षण संदेह के घेरे में आ जाता है. चुनाव सर्वेक्षण केवल व्यापारिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें राजनीति के गरीब राजनैतिक दल पिछड़ जाते हैं और धनाढ्य राजनैतिक दल अपने पक्ष में निर्णय लाकर जनता के निर्णय को प्रभावित करते हैं. शायद इसीलिए पाश्चात्य देशों में मत प्रतिशत को सीटों में परिवर्तित करने की परंपरा नहीं है. जो कि एक साधारण अनुसंधानिक प्रक्रिया लगती है. और यही प्रक्रिया भारत में भी अपनायी जानी चाहिए. तब कहीं जाकर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण संदेह के घेरे से कुछ बाहर निकल पाएंगे. नास्तिक सम्मेलन पर हिंदू संगठनों ने की पत्थरबाजी, महिला पत्रकार को भी थप्पड़ मारे
 मथुरा। वृन्दावन में आज से शुरू हुआ नास्तिक सम्मेलन हिन्दू संगठनों के विरोध की भेंट चढ़ गया. हिन्दू समुदाय के कुछ लोगों ने इस सम्मेलन का विरोध किया और सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी की. स्वामी बालेन्दु ने इस सम्मेलन का आयोजन अपने घर पर किया था, जहां देश के 18 राज्यों से करीब 500 लोग जुटे थे. कई साधू हाथों में झण्डा लेकर आयोजन स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए और सम्मेलन करने वालों पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया.
हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों से भी मारपीट शुरू कर दी. देश की एक वरिष्ठ महिला फोटो पत्रकार को बीच सड़क पर घेर कर थप्पड़ मारे गए. महिला पत्रकार के मुताबिक पुलिस वालों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की. एबीपी न्यूज के पत्रकार सुमित चौहान के साथ भी बदसलूकी की गई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. प्रदर्शन के कारण प्रशासन के आग्रह पर इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है. लेकिन देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये नास्तिक और प्रगतिशील लोग अभी भी आश्रम में डटे हुए हैं. देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नास्तिक लोग एक साथ जुटे हैं.
वृंदावन सिटी के एसपी ने सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है लेकिन किसी हमले की आशंका के कारण कई लोग अभी भी आश्रम में ही हैं. प्रदर्शनकारियों ने आयोजकर्ता के घर और रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी भी की जिसमें रेस्टोरेंट को काफी नुकसान पहुंचा है. स्वामी बालेन्दु का कहना है कि नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है और उन्होंने प्रशासन से भी लिखित अनुमति ली थी. ऐसे में इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना हमारे वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है. देश का संविधान हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है और हम शांतिपूर्ण ढंग से ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे.
आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 14 से 15 अक्टूबर तक चलने वाला था. सम्मेलन में आये लोगों ने इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को लोकतंत्र पर हमला बताया है.
मथुरा। वृन्दावन में आज से शुरू हुआ नास्तिक सम्मेलन हिन्दू संगठनों के विरोध की भेंट चढ़ गया. हिन्दू समुदाय के कुछ लोगों ने इस सम्मेलन का विरोध किया और सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी की. स्वामी बालेन्दु ने इस सम्मेलन का आयोजन अपने घर पर किया था, जहां देश के 18 राज्यों से करीब 500 लोग जुटे थे. कई साधू हाथों में झण्डा लेकर आयोजन स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए और सम्मेलन करने वालों पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया.
हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों से भी मारपीट शुरू कर दी. देश की एक वरिष्ठ महिला फोटो पत्रकार को बीच सड़क पर घेर कर थप्पड़ मारे गए. महिला पत्रकार के मुताबिक पुलिस वालों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की. एबीपी न्यूज के पत्रकार सुमित चौहान के साथ भी बदसलूकी की गई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. प्रदर्शन के कारण प्रशासन के आग्रह पर इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है. लेकिन देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये नास्तिक और प्रगतिशील लोग अभी भी आश्रम में डटे हुए हैं. देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नास्तिक लोग एक साथ जुटे हैं.
वृंदावन सिटी के एसपी ने सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है लेकिन किसी हमले की आशंका के कारण कई लोग अभी भी आश्रम में ही हैं. प्रदर्शनकारियों ने आयोजकर्ता के घर और रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी भी की जिसमें रेस्टोरेंट को काफी नुकसान पहुंचा है. स्वामी बालेन्दु का कहना है कि नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है और उन्होंने प्रशासन से भी लिखित अनुमति ली थी. ऐसे में इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना हमारे वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है. देश का संविधान हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है और हम शांतिपूर्ण ढंग से ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे.
आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 14 से 15 अक्टूबर तक चलने वाला था. सम्मेलन में आये लोगों ने इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को लोकतंत्र पर हमला बताया है. मायावती की रैली के लिए बुक ट्रेनें समय से छोड़ने वाले अधिकारी पर कार्रवाई
 लखनऊ। भाजपा भले ही बसपा को कमजोर पार्टी होने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा बसपा की ताकत से इस हद तक डरी हुई है कि बसपा की रैली में मुरादाबाद से सही समय पर ट्रैनें छोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. इसको लेकर रेलवे अधिकारियों में खासी गहमागहमी भी है.
दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली का आयोजन किया था. इस रैली में हर क्षेत्र से लोगों की लाने की जिम्मेदारी स्थानीय पदाधिकारियों और बसपा के विधानसभा उम्मीदवारों को दी गई थी. बसपा ने मुरादाबाद से सात ट्रेनें लखनऊ के लिए बुक कराई थी. ये स्पेशल ट्रेनें मुरादाबाद के अधिकारियों ने सही समय से छोड़ दी और अन्य यात्री ट्रेनों को काफी देर तक रोके रखा. उस दिन तो इस घटना को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया.
बसपा की रैली की सफलता की सूचना जब उच्च स्तर तक पहुंची तो पूरा रेलवे विभाग सकते में आ गया. सभी अधिकारी सक्रिय हो गए. यह पता लगाया जाने लगा कि बसपा के लिए बुक रेलगाड़ियां सही समय पर क्यों चलाई गई? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? छानबीन में पता चला कि रेलवे के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल प्रबंधक हंसराज ने गाड़ियां छोड़ने के आदेश दिए थे. फिर क्या था कि रेल विभाग ने उन्हें वहां तत्काल प्रभाव से उनके अधीनस्थ की पोस्ट पर भेज दिया और अधीनस्थ को हंसराज की जगह पर. इलाहाबाद-झांसी मंडल के अधिकारियों ने से भी इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी गई थी.
सूत्रों का कहना है कि बसपा की रैली में अप्रत्याशित भीड़ आने से भाजपा हाईकमान चितिंत हो उठा है. वह यह पता करने में जुट गया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्य में लोग कैसे पहुंचे. जांच में पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के माध्यम से रैली में गए थे. इसके बाद यह पता किया जा रहा है कि और कहां-कहां से सही समय से रवाना की गई. अब वहां भी कार्रवाई किए जाने के संकेत है.
लखनऊ। भाजपा भले ही बसपा को कमजोर पार्टी होने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा बसपा की ताकत से इस हद तक डरी हुई है कि बसपा की रैली में मुरादाबाद से सही समय पर ट्रैनें छोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. इसको लेकर रेलवे अधिकारियों में खासी गहमागहमी भी है.
दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली का आयोजन किया था. इस रैली में हर क्षेत्र से लोगों की लाने की जिम्मेदारी स्थानीय पदाधिकारियों और बसपा के विधानसभा उम्मीदवारों को दी गई थी. बसपा ने मुरादाबाद से सात ट्रेनें लखनऊ के लिए बुक कराई थी. ये स्पेशल ट्रेनें मुरादाबाद के अधिकारियों ने सही समय से छोड़ दी और अन्य यात्री ट्रेनों को काफी देर तक रोके रखा. उस दिन तो इस घटना को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया.
बसपा की रैली की सफलता की सूचना जब उच्च स्तर तक पहुंची तो पूरा रेलवे विभाग सकते में आ गया. सभी अधिकारी सक्रिय हो गए. यह पता लगाया जाने लगा कि बसपा के लिए बुक रेलगाड़ियां सही समय पर क्यों चलाई गई? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? छानबीन में पता चला कि रेलवे के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल प्रबंधक हंसराज ने गाड़ियां छोड़ने के आदेश दिए थे. फिर क्या था कि रेल विभाग ने उन्हें वहां तत्काल प्रभाव से उनके अधीनस्थ की पोस्ट पर भेज दिया और अधीनस्थ को हंसराज की जगह पर. इलाहाबाद-झांसी मंडल के अधिकारियों ने से भी इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी गई थी.
सूत्रों का कहना है कि बसपा की रैली में अप्रत्याशित भीड़ आने से भाजपा हाईकमान चितिंत हो उठा है. वह यह पता करने में जुट गया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्य में लोग कैसे पहुंचे. जांच में पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के माध्यम से रैली में गए थे. इसके बाद यह पता किया जा रहा है कि और कहां-कहां से सही समय से रवाना की गई. अब वहां भी कार्रवाई किए जाने के संकेत है. बड़ा संदेश था डॉ. अम्बेडकर का बौद्ध बनना
 मेरा प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल अब नहीं है. 1910 में इसकी स्थापना एक राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी. यह बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध था, जब बंबई (अब मुंबई) रहने और काम करने के लिहाज से रोमांचक शहर माना जाता था. बंबई ब्रिटिश भारत की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही फिल्म उद्योग और राष्ट्रवादी राजनीति की धुरी भी थी. बॉम्बे क्रॉनिकल समाज की नब्ज पर जबर्दस्त पकड़ वाला अखबार था. अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने पर लिखने का ख्याल आया, तो मैंने सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल की पुरानी फाइलें ही पलटीं. इस अखबार ने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से अम्बेडकर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी थी और मेरे लिए यह जानना रोचक था कि बाबासाहेब के जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर इस अखबार ने क्या लिखा होगा? अंबेडकर ने आज से ठीक 60 साल पहले, यानी 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था. यह बताने से पहले कि बॉम्बे क्रॉनिकल ने उस पूरे आयोजन को किस तरह कवर किया, संदर्भवश कुछ जानकारियां जरूरी हैं-
अक्तूबर 1935 की बात है. गुजरात के गांव कविथा में सवर्ण हिंदुओं ने ‘अछूतों’ का इसलिए बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने स्थानीय स्कूलों में अपने बच्चों को भी पढ़ाने की मंशा जाहिर करने का ‘दुस्साहस’ किया था. अम्बेडकर ने घटना पर टिप्पणी की, ‘यदि हम किसी और धर्म के अनुयायी होते, तो कोई ऐसी हिम्मत न कर पाता’. उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा,‘कोई ऐसा धर्म चुन लें, जो आपको समानता का अधिकार और दर्जा देता हो’. अम्बेडकर की सलाह पर ही दलित वर्ग के तमाम लोगों ने नासिक बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि वे हिंदू धर्म छोड़कर कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे, जो अपने धर्मावलंबियों के साथ उन्हें भी बराबरी का दर्जा व अधिकार दे.
अक्तूबर 1935 में अम्बेडकर ने स्वयं भी हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी. हालांकि इसे अमलीजामा पहनाने में उन्हें 21 वर्ष और लगे. क्यों? पहली बात यह कि वह सभी विकल्पों पर पूरी सावधानी के साथ सोच-विचार लेना चाहते थे. दूसरी बात, सुधारों व प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी सवालों पर भी वह रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर सोच-विचार करना जरूरी मानते थे. हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते ही मुस्लिम समाज और ईसाई मिशनरियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन अम्बेडकर ने दोनों को इस सोच के साथ दरकिनार कर दिया कि ये धर्म भारतीय मूल के नहीं हैं. थोड़ी देर के लिए ही सही, उन्होंने सिख धर्म अपनाने के बारे में जरूर सोचा, लेकिन यह पता चलते ही कि सिखों के सामाजिक ताने-बाने में भी हिंदू धर्म जैसी जाति व्यवस्था हावी है, इरादा त्याग दिया.
अम्बेडकर की तलाश जारी रही. उनका आकर्षण तो 1940 से ही बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ने लगा था, जब वह बुद्ध और उनकी विरासत पर पढ़-लिख रहे थे. वह दिसंबर 1954 में रंगून के विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और तभी बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया. यह अलग बात है कि राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता और खराब स्वास्थ्य के चलते क्रियान्वयन में थोड़ा वक्त लगा. मई 1956 में अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध ऐंड द धर्म पूरी करने के साथ ही अपने इरादे की औपचारिक घोषणा कर दी. इसके लिए अपने अनुयायियों की बड़ी फौज वाले शहर नागपुर को चुना. तारीख रविवार 14 अक्तूबर की तय की, जिस दिन देश में विजयदशमी मनाई जा रही थी.
बॉम्बे क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले ही अम्बेडकर के नागपुर स्थित ‘शिड्यूल कास्ट फेडरेशन’ के दफ्तर के भारी जुटान शुरू हो चुका था. 12 अक्तूबर तक तो हालात ऐसे हो गए कि नागपुर आने वाली हर ट्रेन या बस अम्बेडकर के अनुयायियों से अटी दिख रही थी. 14 अक्तूबर को सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ. बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्ट बताती है कि धर्म परिवर्तन स्थल पर तड़के से ही लगी हजारों लोगों की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं. सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी. उस दिन अंबेडकर के तीन लाख से भी ज्यादा अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया.
रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले अम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता बाई ने बौद्ध धर्म अपनाया. बर्मा से आए 83 वर्षीय बौद्ध भिक्षु भिखू चंद्रमणि ने उन्हें नए धर्म में स्वीकार किया. इसके बाद बिल्कुल झक सफेद परिधान पहने अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को मराठी भाषा में सामूहिक शपथ दिलाई. अगले दिन यानी 15 अक्तूबर को अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों की एक विशाल रैली में धर्मांतरण के पीछे के कारण बताए. उन्होंने कहा कि जिस तरह जीवन स्तर में आर्थिक बेहतरी और विधायिका में प्रतिनिधित्व जरूरी है, उसी तरह ‘धर्म हमारी आस्था का मामला है और चहुंमुखी विकास के लिए यह भी बहुत जरूरी है’. उन्होंने आगे जोड़ा कि यह हिंदू धर्म की हठधर्मिता ही थी, जो अब तक हरिजनों की मुक्ति में बाधक बनी हुई थी (क्रॉनिकल ने ‘हरिजन’ शब्द का ही इस्तेमाल किया है, हालांकि अम्बेडकर ने निश्चित तौर पर मराठी में किसी और शब्द का इस्तेमाल किया होगा).
रिपोर्ट के अनुसार, अम्बेडकर आगे कहते हैं, ‘हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलावा किसी और को चमत्कृत करे. यही कारण है कि हमें दूसरा धर्म अपनाने का बड़ा फैसला लेना पड़ा.’उन्होंने अपने अनुयायियों को आश्वस्त किया कि उनकी आने वाली किताब हर उस सवाल का जवाब देगी, जो उनके मन में उठ रहे हैं.
अम्बेडकर ने धर्मांतरण के लिए 14 अक्तूबर की तारीख ही क्यों चुनी? क्या सिर्फ इसलिए कि यह रविवार था या हिंदू कैलेंडर में उस वर्ष महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज था. यदि दूसरी बात को ही लें, तो क्या अपने फैसले को वह बड़ी जीत या ‘विजय’ के रूप में ले रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाकर वह और उनके अनुयायी हिंदू धर्म की जातिवादी जकड़न से खुद को आजाद कर रहे थे?
इन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते. लेकिन एक दिलचस्प सवाल या अटकल मन में जरूर उठती है- धर्मांतरण के बाद इतने कम समय के अंदर यदि उनका निधन न हुआ होता, तब क्या होता? नागपुर कार्यक्रम के सात सप्ताह बाद ही जब उनका निधन हुआ, तब वह 65 साल के थे. अंबेडकर यदि एक दशक और जीवित रहते, तो कोई शक नहीं कि इस अभिशाप को झेलते आए न जाने कितने और लोग बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए होते. तब शायद यह संख्या लाखों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती और यह देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी और परिवर्तनकारी घटना के रूप में दर्ज होती. एक महान मुक्तिदाता असमय जा चुका था और हमारा हिंदू समाज बहुत जल्द ही अपने पुरातन और गहरे पूर्वाग्रहों की ओर लौट चुका था.
मेरा प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल अब नहीं है. 1910 में इसकी स्थापना एक राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी. यह बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध था, जब बंबई (अब मुंबई) रहने और काम करने के लिहाज से रोमांचक शहर माना जाता था. बंबई ब्रिटिश भारत की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही फिल्म उद्योग और राष्ट्रवादी राजनीति की धुरी भी थी. बॉम्बे क्रॉनिकल समाज की नब्ज पर जबर्दस्त पकड़ वाला अखबार था. अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने पर लिखने का ख्याल आया, तो मैंने सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल की पुरानी फाइलें ही पलटीं. इस अखबार ने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से अम्बेडकर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी थी और मेरे लिए यह जानना रोचक था कि बाबासाहेब के जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर इस अखबार ने क्या लिखा होगा? अंबेडकर ने आज से ठीक 60 साल पहले, यानी 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था. यह बताने से पहले कि बॉम्बे क्रॉनिकल ने उस पूरे आयोजन को किस तरह कवर किया, संदर्भवश कुछ जानकारियां जरूरी हैं-
अक्तूबर 1935 की बात है. गुजरात के गांव कविथा में सवर्ण हिंदुओं ने ‘अछूतों’ का इसलिए बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने स्थानीय स्कूलों में अपने बच्चों को भी पढ़ाने की मंशा जाहिर करने का ‘दुस्साहस’ किया था. अम्बेडकर ने घटना पर टिप्पणी की, ‘यदि हम किसी और धर्म के अनुयायी होते, तो कोई ऐसी हिम्मत न कर पाता’. उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा,‘कोई ऐसा धर्म चुन लें, जो आपको समानता का अधिकार और दर्जा देता हो’. अम्बेडकर की सलाह पर ही दलित वर्ग के तमाम लोगों ने नासिक बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि वे हिंदू धर्म छोड़कर कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे, जो अपने धर्मावलंबियों के साथ उन्हें भी बराबरी का दर्जा व अधिकार दे.
अक्तूबर 1935 में अम्बेडकर ने स्वयं भी हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी. हालांकि इसे अमलीजामा पहनाने में उन्हें 21 वर्ष और लगे. क्यों? पहली बात यह कि वह सभी विकल्पों पर पूरी सावधानी के साथ सोच-विचार लेना चाहते थे. दूसरी बात, सुधारों व प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी सवालों पर भी वह रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर सोच-विचार करना जरूरी मानते थे. हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते ही मुस्लिम समाज और ईसाई मिशनरियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन अम्बेडकर ने दोनों को इस सोच के साथ दरकिनार कर दिया कि ये धर्म भारतीय मूल के नहीं हैं. थोड़ी देर के लिए ही सही, उन्होंने सिख धर्म अपनाने के बारे में जरूर सोचा, लेकिन यह पता चलते ही कि सिखों के सामाजिक ताने-बाने में भी हिंदू धर्म जैसी जाति व्यवस्था हावी है, इरादा त्याग दिया.
अम्बेडकर की तलाश जारी रही. उनका आकर्षण तो 1940 से ही बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ने लगा था, जब वह बुद्ध और उनकी विरासत पर पढ़-लिख रहे थे. वह दिसंबर 1954 में रंगून के विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और तभी बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया. यह अलग बात है कि राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता और खराब स्वास्थ्य के चलते क्रियान्वयन में थोड़ा वक्त लगा. मई 1956 में अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध ऐंड द धर्म पूरी करने के साथ ही अपने इरादे की औपचारिक घोषणा कर दी. इसके लिए अपने अनुयायियों की बड़ी फौज वाले शहर नागपुर को चुना. तारीख रविवार 14 अक्तूबर की तय की, जिस दिन देश में विजयदशमी मनाई जा रही थी.
बॉम्बे क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले ही अम्बेडकर के नागपुर स्थित ‘शिड्यूल कास्ट फेडरेशन’ के दफ्तर के भारी जुटान शुरू हो चुका था. 12 अक्तूबर तक तो हालात ऐसे हो गए कि नागपुर आने वाली हर ट्रेन या बस अम्बेडकर के अनुयायियों से अटी दिख रही थी. 14 अक्तूबर को सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ. बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्ट बताती है कि धर्म परिवर्तन स्थल पर तड़के से ही लगी हजारों लोगों की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं. सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी. उस दिन अंबेडकर के तीन लाख से भी ज्यादा अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया.
रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले अम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता बाई ने बौद्ध धर्म अपनाया. बर्मा से आए 83 वर्षीय बौद्ध भिक्षु भिखू चंद्रमणि ने उन्हें नए धर्म में स्वीकार किया. इसके बाद बिल्कुल झक सफेद परिधान पहने अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को मराठी भाषा में सामूहिक शपथ दिलाई. अगले दिन यानी 15 अक्तूबर को अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों की एक विशाल रैली में धर्मांतरण के पीछे के कारण बताए. उन्होंने कहा कि जिस तरह जीवन स्तर में आर्थिक बेहतरी और विधायिका में प्रतिनिधित्व जरूरी है, उसी तरह ‘धर्म हमारी आस्था का मामला है और चहुंमुखी विकास के लिए यह भी बहुत जरूरी है’. उन्होंने आगे जोड़ा कि यह हिंदू धर्म की हठधर्मिता ही थी, जो अब तक हरिजनों की मुक्ति में बाधक बनी हुई थी (क्रॉनिकल ने ‘हरिजन’ शब्द का ही इस्तेमाल किया है, हालांकि अम्बेडकर ने निश्चित तौर पर मराठी में किसी और शब्द का इस्तेमाल किया होगा).
रिपोर्ट के अनुसार, अम्बेडकर आगे कहते हैं, ‘हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलावा किसी और को चमत्कृत करे. यही कारण है कि हमें दूसरा धर्म अपनाने का बड़ा फैसला लेना पड़ा.’उन्होंने अपने अनुयायियों को आश्वस्त किया कि उनकी आने वाली किताब हर उस सवाल का जवाब देगी, जो उनके मन में उठ रहे हैं.
अम्बेडकर ने धर्मांतरण के लिए 14 अक्तूबर की तारीख ही क्यों चुनी? क्या सिर्फ इसलिए कि यह रविवार था या हिंदू कैलेंडर में उस वर्ष महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज था. यदि दूसरी बात को ही लें, तो क्या अपने फैसले को वह बड़ी जीत या ‘विजय’ के रूप में ले रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाकर वह और उनके अनुयायी हिंदू धर्म की जातिवादी जकड़न से खुद को आजाद कर रहे थे?
इन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते. लेकिन एक दिलचस्प सवाल या अटकल मन में जरूर उठती है- धर्मांतरण के बाद इतने कम समय के अंदर यदि उनका निधन न हुआ होता, तब क्या होता? नागपुर कार्यक्रम के सात सप्ताह बाद ही जब उनका निधन हुआ, तब वह 65 साल के थे. अंबेडकर यदि एक दशक और जीवित रहते, तो कोई शक नहीं कि इस अभिशाप को झेलते आए न जाने कितने और लोग बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए होते. तब शायद यह संख्या लाखों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती और यह देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी और परिवर्तनकारी घटना के रूप में दर्ज होती. एक महान मुक्तिदाता असमय जा चुका था और हमारा हिंदू समाज बहुत जल्द ही अपने पुरातन और गहरे पूर्वाग्रहों की ओर लौट चुका था.
धम्म दीक्षा विशेषः 1956 के बाद बौद्ध धम्म
 बोधिसत्व भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी. यह वह तारीख थी, जब भारत में धम्म कारवां को नयी गति और दिशा मिली थी. अब उस तारीख के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में इन 57 सालों में धम्म कारवां की प्रगति, उसकी दशा, दिशा और भविष्य का अवलोकन करने की आवश्यकता है. लेकिन इन तमाम अवलोकनों की बुनियाद में पहला सवाल यह खड़ा है कि आखिर बाबासाहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया और धम्म कारवां क्यों आरंभ किया?
असल में डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि भारत में प्रचलित जातिगत असमानता दलितों के पिछड़े होने का मुख्य कारण है. 9 मई, 1916 को कोलम्बिया विश्वविद्यालय में आयोजित एक सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर ‘भारत में जातियां-उनकी संरचना, उद्भव एवं विकास’ के जरिए डॉ. अम्बेडकर ने यह साबित कर दिया था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने जातिगत असमानता की व्यवस्था को शास्त्र सम्मत दिखाने की कोशिश की है और ये धारणा फैलाई है कि शास्त्र गलत नहीं हो सकते. भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों के मानवाधिकारों के लिए अलग-अलग मोर्चे पर प्रयास करना शुरू कर दिया. महाड सत्याग्रह द्वारा सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के अधिकार, कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार, अंग्रेजी सरकार के सामने दलितों के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार, गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन के अधिकार की लड़ाई ऐसी ही कोशिश थी. 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा भी कर दी थी लेकिन महात्मा गांधी द्वारा आमरण-अनशन करने के कारण डॉ़. अम्बेडकर को तरह-तरह की धमकियां मिली. तब डॉ. अम्बेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट स्वीकार करना पड़ा और दलितों के लिए आरक्षण के बदले में पृथक निर्वाचन का हक छोड़ना पड़ा. इस संघर्ष के दौरान डॉ. अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हिन्दू धर्म में रहकर दलितों को राजनैतिक आजादी का अधिकार भले ही मिल जाए लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक बराबरी का हक नहीं मिल सकता. इसलिए 1935 में येवला (नाशिक) में डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वह हिन्दू धर्म में पैदा हुए थे यह उनके वश की बात नहीं थी लेकिन हिन्दू रहकर वह मरेंगे नहीं, यह उनके वश में है. डॉ. अम्बेडकर ने धर्म-परिवर्तन का निश्चय येवला की सभा में ही कर लिया था.
धर्म परिवर्तन पर विचार करने के लिए 30 एवं 31 मई 1936 को बंबई में आयोजित महार परिषद को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा थाः -‘धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है. यह ‘मनुष्य के जीवन को सफल कैसे बनाया जाय’ इस सरोकार से जुड़ा प्रश्न है… इसको समझे बिना आप धर्म परिवर्तन के संबंध में मेरी घोषणा के वास्तविक निहितार्थ का अहसास कर पाने में समर्थ नहीं होंगे. छुआछूत की स्पष्ट समझ और वास्तविक जीवन में इसके अमल का अहसास कराने के लिए मैं आप लोगों के खिलाफ किये जाने वाले अन्याय और अत्याचारों की दास्तान का स्मरण कराना चाहता हूं. सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने का हक जताने पर या सार्वजनिक कुंओं से पानी भरने का अधिकार जताने पर या घोड़ी पर दूल्हे को बैठाकर बारात को जुलूस की शक्ल में सार्वजनिक रास्तों से घुमाने के अधिकार आदि का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को सवर्ण हिन्दुओं द्वारा मारे-पीटे जाने के उदाहरण तो बहुत आम हैं. लेकिन ऐसी और भी अनेक वजहें हैं जिनके कारण दलितों पर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न का कहर ढाया जाता है… खरी बात पूछूं तो बताइये कि इस समय हिन्दुओं और आप लोगों के बीच क्या किसी प्रकार के समाजिक संबंध हैं?
जिस तरह मुसलमान हिन्दुओं से भिन्न हैं; उसी तरह दलित लोग भी हिन्दुओं से नितान्त भिन्न हैं. जिस तरह मुसलमानों और ईसाइयों के साथ हिन्दुओं का रोटी-बेटी का कोई सम्बन्ध नहीं होता है उसी तरह आप लोगों के साथ भी हिन्दुओं का किसी भी प्रकार का रोटी-बेटी का कोई संबंध नहीं है… आपका समाज और उनका समाज दो बिल्कुल अलग-अलग समूह हैं… हालांकि आप लोगों ने धर्मांतरण के महत्व को नहीं समझा है लेकिन निस्संदेह रूप से आप लोगों ने नामान्तरण यानि नाम परिवर्तन के महत्व को समझ ही लिया है. अगर आप लोगों में से किसी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में सवाल कर दिया जाता है कि वह किस जाति का है तो वह दलित होने के रूप में अपना उत्तर देता है, लेकिन वह महार है या भंगी है, ऐसा बताने में संकोच करता है. जब तक कुछ विशेष परिस्थितियों की मजबूरी न हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम नहीं बदल सकता. ऐसे नाम परिवर्तन का कारण यह है कि एक अनजान आदमी तो दलित और सवर्ण के बीच कोई अन्तर कर नहीं सकता. और जब तक एक हिन्दू को किसी व्यक्ति की जाति का पता नहीं चल जाता तब तक उस व्यक्ति के दलित होने के कारण वह हिन्दू उस व्यक्ति के खिलाफ अपने मन में नफरत का भाव नहीं भर सकता. सवर्ण हिन्दुओं को जब तक साथ यात्रा कर रहे दलितों की जातियों की जानकारी नहीं होती है तब तक तो यात्रा के दौरान वे बड़े दोस्ताना अंदाज में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी हिन्दू को यह पता चलता है कि वह जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहा है वह दलित है; तो उसका मुंह और मन तुरंत कसैला हो जाता है. आप लोगों के लिए इस तरह के अनुभव नये नहीं हैं.
आखिर ऐसा क्यों होता है? आप महार कहने के बजाय स्वयं को चोखामेला बता कर या भंगी कहने के बजाय वाल्मीकि बता कर दूसरों को चकमा देने की कोशिश करते हैं. लेकिन आप लोग यह तो जानते ही हैं कि दूसरे लोग इस तरह के झांसे में नहीं आते. आप लोग अपने को चाहे चोखामेला कहें या दलित कहें; लोग तो जान ही जाते हैं कि आप क्या हैं. आप लोगों ने अपनी छुपा-छुपी की ऐसी कारगुजारियों से ही नाम-परिवर्तन की आवश्यकता को स्वयं ही सिद्ध कर दिया है. तो फिर धर्म-परिवर्तन करने में आखिर क्या ऐतराज होना चाहिए? धर्म-परिवर्तन करना नाम परिवर्तन करने जैसा ही है. धर्म-परिवर्तन करने के पश्चात ही नाम-परिवर्तन आप लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा. अपने को एक मुसलमान, एक ईसाई, एक बौद्ध या एक सिक्ख कहना एक धर्म का परिवर्तन मात्र नहीं है बल्कि एक नाम का भी परिवर्तन है. यही सच्चा नाम परिवर्तन है… जब तक आप हिन्दू धर्म में बने रहेंगे तब तक आपको अपने जाति नाम को छिपा कर नाम-परिवर्तन करते रहने पर निरन्तर मजबूर होना पड़ेगा… इसलिए मैं आप लोगों से यह पूछता हूं कि बजाय इसके कि आप आज एक नाम बदलें, कल दूसरा नाम बदलें और पेंडुलम की तरह लगातार ढुलमुल हालत में बने रहें, आप लोगों को धर्म परिवर्तन करके अपना नाम स्थाई रूप से क्यों नहीं बदल लेना चाहिये?’ डॉ. अम्बेडकर द्वारा कही गई उपरोक्त बातें कमोबेश आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि सन् 1935 में थी.
इसी सभा में धर्म परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा:
‘मुझे उस प्रश्न पर बस आश्चर्य ही होता है जिसे कुछ हिन्दू कुछ इस तरह उठाते हैं कि केवल धर्म-परिवर्तन से क्या होने वाला है? भारत में वर्तमान समय के सिक्खों, मुसलमानों और ईसाईयों में से अधिसंख्य लोग तो पहले हिन्दू ही थे और उन में भी शूद्रों और दलितों की तादाद ही सबसे ज्यादा है…अगर ऐसा है भी तो धर्म-परिवर्तन के बाद उनकी स्थिति में एक स्पष्ट प्रगति साफ दिखती है… समस्या पर गहन चिंतन-मनन करने के बाद हर किसी को यह मानना पड़ेगा कि दलितों के लिये धर्म-परिवर्तन उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार भारत के लिए स्वराज जरूरी है. दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक जैसा ही है, दोनों के लक्ष्य में कोई फर्क नहीं है और वह अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता प्राप्त करना.
20 वर्षों तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद डॉ. अम्बेडकर इस निश्चय पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ है और बौद्ध धर्म समानता, करूणा, मैत्री, अहिंसा और भाई-चारे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है. इसमें ऊंच-नीच और छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है. जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात डॉ. आंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर बौद्धधम्म के प्रचार-प्रसार को नई गति प्रदान की. उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का एक नया फार्मूला दिया.
वर्तमान में धम्म
भगवान बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले अषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन करके धम्म कारवां की शुरूआत की थी. डॉ. अम्बेडकर ने सन 1956 में विजयदशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लेकर धम्म चक्र का अनुपर्वतन किया. धम्म कारवां आज काफी फल-फूल चुका है. 1956 में पांच लाख लोगों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच गई है. अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली संस्करण,10 नवंबर 2006) में प्रकाशित एक रपट के अनुसार भारत वर्ष में सन 2006 में 30 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. 2001 की जनगणना के वक्त बढ़कर यह लगभग 81 लाख हो चुकी थी. जो कि 2011 की आखिरी जनगणना के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 97 लाख पहुंच गई हैं. हालांकि कुछ विशेषज्ञ भारत में बौद्धों की संख्या 3 करोड़ 50 लाख से भी अधिक मानते हैं. उनका मानना है कि जनगणना में वास्तविक संख्या इसलिए सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि काफी लोग बौद्ध होते हुए भी अपने को आधिकारिक दस्तावेजों में बौद्ध नहीं घोषित करते.
सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो लगभग सभी प्रदेशों में बौद्ध अनुयायियों ने अनेकों बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया है. पंजाब में 22 बुद्ध विहार निर्मित किए गए हैं. गुजरात में कई जगहों पर बुद्ध अनुयायियों ने बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया है. यू.पी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के तमाम प्रदेशों में अनेकों बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया जा चुका है. अमेरिका और यूरोप में भी बौद्ध धम्म बहुत तेजी से बढ़ती हुई जीवनशैली बनता जा रहा है. डॉ. आंबेडकर ने धम्म दीक्षा लेते हुए कहा था कि वो एक नए किस्म का धम्म कारवां आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु शील सदाचार का पालन करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य करेंगे. इससे प्रभावित होकर एशिया के अन्य देशों में भी बौद्ध पुनर्जागरण तेजी से हुआ. जिनेवा आधारित ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व आध्यात्मिक संगठन’ ने 2009 का ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म का सम्मान’ बौद्ध धम्म को प्रदान किया.
धम्म कारवां की दिशा
आज के वक्त में यह सोचना भी जरूरी है कि धम्म कारवां की दिशा क्या हो और उसमें हमारी भूमिका क्या हो?
बौद्धों का जीवन- बौद्धों को अपना जीवन और दैनिक क्रियाकलाप बौद्धधम्म की शिक्षाओं के अनुरूप जीना चाहिए. इसके लिए सबसे आवश्यक है कि देवी-देवताओं की पूजा का मोह त्यागना होगा. धम्म वंदना और दीक्षा प्रतिज्ञा गाथा के उस पालि सुत्त की बातें जीवन में उतारनी होगी जिसमें कहा गया है कि… ‘मैं भगवान बुद्ध के अलावा (बुद्ध मार्ग) अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा. इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. मैं धम्म के अलावा अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा. धम्म ही मेरा श्रद्धा स्थान है, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. भिक्खु संघ के अलावा मैं अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा; इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो.’
संस्कृति- बौद्धों को एक ऐसी संस्कृति का विकास करना चाहिए जिसमें प्रत्येक देशवासी को एक सम्मानित नागरिक माना जाए और प्रत्येक नागरिक की मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर सुनिश्चित हो. देश में परस्पर भाईचारे के साथ प्रेम और सौहार्द की भावना हो. डॉ. आंबेडकर का कहना था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक-भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए… लेकिन इस भावना के विकास में जाति सबसे बड़ी बाधा है. डॉ आंबेडकर का निष्कर्ष था कि जाति की प्रकृति ही विखण्डन और विभाजन करना है. जाति का यह अभिशाप है. जाति भावनाओं से आर्थिक विकास रूकता है. इसलिए डॉ. अंबेडकर का लगातार यह प्रयत्न रहा कि भारत में एक ऐसी सांझी संस्कृति का निर्माण हो जिसमें जात-पात के आधार पर लोगों के साथ अन्याय और शोषण न हो और हर नागरिक अपनी क्षमताओं के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके. आपस में उपजातिवाद छोड़कर एक साझा पहचान जो बौद्ध पहचान है उसको अपनाना चाहिए और आपस में रोटी-बेटी का संबंध कायम करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता मिले. डॉ. आंबेडकर चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों में खान-पान का संबंध विकसित हो. जो लोग धम्म दीक्षा लेने के बाद भी जाति और उप-जाति बनाए रखना चाहते हैं या जाति-पात में विश्वास करते हैं वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं क्योंकि इससे बौद्ध धर्म में भी जाति का जहर फैल जाएगा.
विपस्सना- एक अन्य चर्चा विपस्सना को लेकर है. बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि विपस्सना लोगों को निष्क्रिय कर देती हैं, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है जबकि दलित समाज को आंदोलित रखने के लिए क्रोध की आवश्यकता है और विपस्सना से समाज सेवा की भावना कम हो जाती है. इन सब मिथ्या प्रचार को हमें दूर करना होगा. गौतम बुद्ध ने छः वर्षों तक ध्यान साधना किया और विपस्सना का आविष्कार किया. विपस्सना करते-करते 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व को प्राप्त किया. बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात 45 वर्षो तक शहरों, गांवों, कस्बों में जा-जाकर धम्म का प्रसार किया. यदि भगवान बुद्ध निष्क्रिय नहीं हुए तो फिर उनकी खोजी हुई विपस्सना करने से उनके अनुयायी कैसे निष्क्रिय हो सकते हैं?
भिक्खुओं द्वारा खुद पहल कर लोगों से नहीं मिलना भी एक समस्या है. बहुत से भिक्खु इस आशा में रहते हैं कि जब कोई बुद्ध विहार में आएगा तभी वो धम्म दीक्षा की बात करेंगे. इस बारे में भगवान बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है. भगवान बुद्ध बोधगया से चलकर सारनाथ आए थे और धम्मचक्र प्रवर्तन किया था. वह इस भरोसे में नहीं बैठे रहे कि लोग बोधगया आए और तब वो उनको धम्म सिखाएं. इसीलिए डॉं. आंबेडकर ने ‘इंगेज्ड बुद्धिज्म’ की परिकल्पना की थी. इस परिकल्पना को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है. वियतनाम में भिक्खु संघ ने अमेरिका के आक्रमण के खिलाफ पूरी ताकत से विरोध किया और लोगों के बीच जाकर धर्म का प्रचार-प्रसार किया. ताईवान में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में वहां के भिक्खुनी संघ ने अहम भूमिका अदा की है. ताईवान में भिक्खुनी संघ स्कूल भी चलाता है, अस्पताल भी चलाता है और लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं का निदान भी करता है. ताईवान के उदाहरण को भारत वर्ष में भी दोहराने की आवश्यकता है.
बौद्ध संस्कृति विकसित करना जरूरी – हर सिक्ख रविवार को अनिवार्य रूप से गुरूद्वारा जाता है, ईसाई चर्च जाते है. हर मुसलमान शुक्रवार की नमाज मस्जिद जाकर अता करता है. बौद्ध समाज के लोगों को भी ऐसी परंपरा डालनी होगी. प्रत्येक रविवार को अपने नजदीकी बौद्ध विहार में जाएं. जहां बौद्ध विहार नहीं है, वहां किसी के घर में और यदि वो भी संभव नहीं है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर कोई संगोष्ठी करें. ऐसी कोशिश भी की जा सकती है कि जीवन के उत्सव चाहे जन्मदिन का कार्यक्रम हो या सालगिरह, उसे बौद्ध विहार में मनाए. इसके साथ ही अपना जीवन पंचशीलों के अनुसार जीने की कोशिश करें. डॉ. आंबेडकर ने स्वयं बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने आवास को सजाना आरंभ किया और उत्सव मनाने की परंपरा आरंभ की. विवाह के लिए विवाह विधि का प्रतिपादन किया और बौद्ध चर्या पद्धति तैयार की. बौद्धों में शील और सदाचार का जीवन विकसित करने के लिए ‘बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया’ की स्थापना की जिसकी शाखाएं हर प्रदेश में स्थापित की गई. डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1956 को सारनाथ के मृगदाय वन में 150 भिक्खुओं के समक्ष भाषण दिया था कि प्रत्येक बौद्ध के लिए अनिवार्य है कि वह हर रविवार को बौद्ध विहार में जाए और वहां उपदेश सुने. यदि ऐसा नहीं होगा तो नव दीक्षित बौद्ध को धम्म की जानकारी नहीं हो सकेगी. प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए जिसमें सभा करने के लिए काफी स्थान रहे. बौद्ध विहारों को सभामंदिर होना चाहिए.
बाल साहित्य और बौद्ध साहित्य- सुरूचिपूर्ण बाल साहित्य और जनभाषा में बौद्ध साहित्य की भी काफी आवश्यकता है. इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय लोक भाषा में छोटी-छोटी पुस्तकें बड़े अक्षरों में छपवाई जाए और सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि साहित्य के बगैर धर्म का प्रचार-प्रसार कठिन होगा. जो भी बौद्ध साहित्य लिखा गया है, उसको और सरल और सुगम बनाकर कम से कम शब्दों में तैयार कर जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है जिससे कि किसान, मजदूर, गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सभी लोग समझ सकें और उसको जीवन में उतार सकें. बुद्ध की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शीलवान और पढ़े-लिखे भिक्खुओं की जरूरत है. इसके साथ ही, हमें एक समानांतर प्रचार व्यवस्था को विकसित करना होगा जिसमें नुक्कड़ नाटक, भजन मंडली, स्वांग मंडली, लोकगीत शामिल हैं जो लोगों तक आपकी बात पहुंचा सके.
पर्सनल लॉ की जरूरत- लगभग सभी अल्पसंख्यकों के अपने-अपने Personal Low हैं. ईसाईयों का Personal Low उनका बाईबिल है, मुसलमानों का Personal Low कुरान शरीफ द्वारा निर्धारित होता है. सिक्खों में आनंद कारज विवाह प्रथा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन बौद्धों का अपना कोई Personal Low नहीं है. इसलिए जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बन जाती, बौद्धों का भी अपना Personal Low होना चाहिए.
चारों महत्वपूर्ण अंगों को सामने आना होगा- बौद्ध धम्म के सामाजिक संगठन के चार महत्वपूर्ण अंग हैं. ये हैं भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ. धम्म कारवां के आगे बढ़ने के लिए इन चारों संघों का शील-सदाचार पूर्ण जीवन जीना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है. लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में अकेले भिक्षु संघ काम कर रहा है. अभी तक न तो भिक्षुणी संघ बन पाया है, न ही उपासक संघ और न ही उपासिका संघ. इसलिए आवश्यक है कि बौद्ध अनुयायियों को इन संघों का निर्माण करना चाहिए और उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए.
धम्म कारवां का भविष्य
धम्म के आम आदमी के जीवन में पड़ते प्रभाव और इसकी वैज्ञानिक जीवन पद्धति को देखकर यह कहा जा सकता है कि धम्म कारवां का भविष्य अत्यंत उज्जवल है. धम्म दीक्षा लेने वालों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और उनका चहुमुंखी विकास हुआ है.मशहूर समाजशास्त्री डी. एस. जनबन्धू और गौतम गावली द्वारा महाराष्ट्र में किए गए समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली उनमें एक नई पहचान और आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई, जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर में काफी सुधार आया. इन नवदीक्षित लोगों ने राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसी प्रकार का एक शोध भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. संजय चहांडे ने किया और वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धम्म दीक्षा लेने वालों का विकास धम्म दीक्षा न लेने वालों की तुलना में अधिक हुआ है. डॉ. संजय चहांडे ने इस विषय पर पीएचडी की है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दलितों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में काफी अच्छे बदलाव आए हैं. उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसके कारण उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है.
एक सर्वे के अनुसार ताईवान में बौद्ध अनुयायियों की संख्या सन् 1980 में 8 लाख थी जो 2001 में बढ़कर 55 लाख और 2006 में बढ़कर 80 लाख हो गई. इस तरह 26 सालों में ताईवान में बौद्ध अनुयायियों की संख्या दस गुणा बढ़ी है. इसी अवधि में ताईवान में बुद्ध विहारों की संख्या 1157 से बढ़कर 4500 और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 3470 से बढ़कर 10 हजार पहुंच गई. ताईवान में भिक्षु और भिक्षुनियां अनेक प्रकार के समाजिक कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसे व्यक्ति विकास के काम कर रहे हैं. इसी तरह चीन में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो गई है. थाईलैंड में 90 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है. यही स्थिति श्रीलंका, म्यामांर और भूटान जैसे देशों की है. भगवान बुद्ध के कारण एशिया के अधिकतर देश भारत को बहुत पवित्र मानते हैं और भारत की यात्रा करना अपना धर्म समझते हैं. जापान, कोरिया, थाईलैंड, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, ताईवान सहित अनेकों देशों के करोड़ों लोगों के मन में एक लालसा रहती है कि जीवन में कम से कम एक बार बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिशा और सांची के दर्शन कर पाएं. इसलिए भारतवर्ष के लिए बुद्ध और उनकी शिक्षाओं द्वारा पूरे एशिया का अगुवा बनने का सुनहरा अवसर है.
भ्रम फैलाने की कोशिश
धम्म कारवां की लोकप्रियता से डरे कुछ लोगों और संगठनों द्वारा अनेकों दुष्प्रचार करने की घटना भी सामने आई हैं. इसमें एक दुष्प्रचार यह किया जा रहा है कि बौद्धधर्म केवल दलित अपना रहे हैं. जबकि हकीकत इससे अलग है. भगवान बुद्ध दलित नहीं थे. उनके प्रथम पांचों शिष्य ब्राह्मण थे. उसके बाद यश और उसके 54 साथी व्यापारी वर्ग से थे. उसके बाद धम्मदीक्षा लेने वाले उरूवेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप और उनके 1000 शिष्य सभी ब्राह्मण थे. राजा बिबिंसार और राजा प्रसेनजित तथा शाक्य संघ के लोग सभी के सभी क्षत्रिय थे. वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मानंद कौशाम्बी, डी डी कौशाम्बी पूर्व में ब्राह्मण थे. इसी तरह भदन्त आनंद कौशलायन, आचार्य सत्यनारायण गोयनका, भन्तेसुरई सशई, अमेरिका के मशहूर फिल्म अभिनेता रिचर्ड गेरे, फिल्म प्रोड्यूसर टीना टर्नर कोई भी दलित वर्ग से नहीं है. इसलिए बौद्ध धर्म के विरोधियों के इस मिथ्या प्रचार को कि बौद्ध धर्म दलितो का धर्म होता जा रहा रोका जाना चाहिए.
इसी तरह एक प्रचार और किया जा रहा है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे. ऐसा प्रचार पहले भी होता रहा है. बुद्ध को अवतार मानने की बात सबसे पहले संभवतः छठी सदी के दौरान मत्स्यपुराण में की गई, मत्स्य पुराण का एक चरण 700 ईसवीं में महाबलीपुरम में, जहां मध्यकालीन ब्राह्मण पुस्तकों में 10 अवतारों की संकल्पना की गई है, पल्लव स्मारकों में उत्कीर्ण हैं. इस बिषय में नॉरमन कौसिन्स लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का निर्माण होने पर हिन्दू धर्म ने उसके साथ होड़ नहीं लगाई, बल्कि उसे सोख लिया. बुद्ध को अवतार के रूप में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धम्म को अवशोषित (सोख) कर उसका ब्राह्मणीकरण करना था, जिसे ब्राह्मण विरोध करके भी दबा नहीं पाए. इस प्रक्रिया में उन्होंने पशु-हिंसा छोड़कर, शाकाहार के आदर्श को अपना लिया. इस प्रक्रिया की अत्यंत चतुर चाल यह थी कि भगवान बुद्ध को वैदिक साहित्य में विष्णु के नवें अवतार के रूप में जबरन शामिल करना. निश्चित ही इस परिकल्पना ने बौद्ध धम्म की जड़ों को आघात पहुंचाया. बुद्ध को अवतार के रूप में स्थापित करने का काम एक राजनैतिक चाल के तहत किया गया. यह इस बात से स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि हिन्दू साहित्य में बुद्ध को स्थान देने के बावजूद पुराणों और अन्य हिन्दू धर्म ग्रंथों में निरंतर बुद्ध और बौद्ध धम्म के प्रति एक विरोधात्मक एवं विद्रोहात्मक स्वर देखने को मिलता है.
ऐसे प्रचार को ध्यान में रखकर ही डॉ. आंबेडकर ने प्रतिज्ञा संख्या 5 में लिखा है कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताना धोखा और झूठ प्रचार है. डॉ. आंबेडकर के अनुसार बौद्ध अनुयायी इस सिद्धांत को सिरे से नकारते हैं कि बुद्ध विष्णु के एक अवतार थे. भगवान बुद्ध ने स्वयं ही अवतार के सिद्धांत को नकारा था. बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने यह उल्हास भरी घोषणा की थी-
‘अयं अन्तिमा जाति’ (अर्थातः यह मेरा अंतिम जन्म है),
‘नत्थिदानि पुनब्भवोति’ (अर्थात अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा)
डॉ. एम. एल. जोशी ने कहा है कि बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में प्रचारित करने का सटीक कारण यह है कि बुद्ध का व्यक्तित्व इतना महान था कि उसे नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में संभव नहीं था. डॉ. जोशी के मुताबिक, ‘बुद्ध की भारतीय जनमानस में इतनी गहरी पैठ है कि पूरे देश में असंख्य विहारों के हजारों स्तंभों, दीवारों और दरवाजों पर उत्कीर्ण की गई. उनकी शिक्षाएं लगभग न समाप्त होने वाले पालि और संस्कृत साहित्य के अकूत खजाने के माध्यम से फैलाकर लोकप्रिय की गईं. अनेकों राजाओं और महान चिंतकों ने उनके युक्तिवादी व मानवतावादी मिशन को अत्यधिक ससम्मान से अपनाया. असंख्य भारतीय सदियों से उनकी प्रशंसा का गुणगान करते आ रहे हैं. वह सचमुच इतने महान थे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी. स्वाभाविक रूप से वे उच्च स्थान प्राप्त सदस्य के रूप में अवतारों के तारामंडल में आ गए.’ बुद्ध को अवतारों की श्रेणी में रखने की दुर्भावनापूर्ण सोच इस बात से भी स्पष्ट होती है कि पौराणिक लोगों ने उनके सम्मान में किसी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, इसलिए तार्किक दृष्टि से बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने का सिद्धांत दुर्भावनापूर्ण है. अगर बुद्ध को श्रद्धावश विष्णु का अवतार माना गया होता तो यह कैसे संभव है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हजारों हिन्दू मंदिरों में किसी में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होती? एक और तथ्य जानने योग्य है. बुद्ध का अर्थ ही होता है कि जन्म-मरण के संसार चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना. अगर कोई दुबारा जन्म लेता है, तो फिर बुद्ध कैसे हुआ? इसलिए बुद्ध को अवतार बताना उनके बुद्धत्व को नकारना है. 19 नबवंर, 1999 को सारनाथ में विपस्सना के प्रधानाचार्य सत्यनारायण गोयन्का और कांचीकामकोटि पीठम के तत्कालीन शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके घोषणा की थी कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे.
एक टी. वी धारावाहिक में यह दिखाया गया है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के बाद हुआ था. बौद्ध विद्वानों का कहना है कि पूरे पालि साहित्य और बौद्धों के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटकों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है. इसलिए बौद्ध अनुयायियों को इस प्रकार के प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए. बुद्ध और बौद्ध धर्म से द्वेष रखने वाले कुछ लोग यह भी प्रचार करते हैं कि बौद्धों में कई पंथ है जैसे कि हीनयान, महायान और तंत्रयान. यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित मूल सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है. सभी बौद्ध गौतम बुद्ध को अपना शास्ता मानते हैं, सभी बौद्ध चार आर्य सत्य मानते हैं. सभी बौद्ध आर्य आष्टांगिक मार्ग मानते हैं. बौद्ध धर्म का सार शील, समाधि और प्रज्ञा है. जो अंतर है वो केवल बाहरी कपड़ों और पूजा विधि को लेकर है. इसलिए ऐसे दुष्प्रचार से बचने की आवश्यकता है.
डॉ. अम्बेडकर सिर्फ नाममात्र का धर्मांतरण नहीं चाहते थे, बल्कि वे लोगों की सोच और जीवन में एक आमूलचुल परिवर्तन लाना चाहते थे. अब यह बौद्ध अनुयायियों पर निर्भर करता है कि वो धम्म कारवां को कहां ले जाना चाहते हैं. भिक्षु संघ इस बात को लेकर बेहद सजग है. यही कारण है कि भारतीय बौद्ध अब अपनी विशेष पहचान और अलग संस्कृति का विकास करने में जुटे हैं. 22 जुलाई, 2013 को सारनाथ में भन्ते पी. सिवली महाथेरा की अध्यक्षता में धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और उपासक-उपासिका शामिल हुए. इस मौके पर भारतीय चीवर पेश किया गया. अभी तक भारतीय चीवर नहीं था और इसका आयात श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड से किया जाता था. लेकिन अब भारतीय चीवर बनने के बाद चीवर की उपलब्धता आसान हो जाएगी. धम्म दीक्षा के समय डॉ. आंबेडकर ने कहा था ‘मैं आपलोगों के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूं. आप ऐसा जीवन जीएं जिससे आप सम्मान के पात्र बन सकें. ऐसा मत सोचें कि यह धम्म आपके गले में जंजीर की तरह बांध दिया गया है. जहां तक बुद्ध धम्म का सवाल है, अपना देश तो इसमें रेगिस्तान हो चुका है. अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस धम्म को उत्साह और पूरी ईमानदारी से निबाहें और ध्यान रखें कि किसी समय यह धम्म कितना वैभवशाली था. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग इस धर्मांतरण पर हंसेंगे. यह धर्म न केवल इस देश की अपितु दुनिया की सेवा कर सकता है. वैश्विक गतिविधियों के इन क्षणों में दुनिया में शांति के लिए बुद्ध धम्म अपरिहार्य है. धर्म परिवर्तन के बाद मुझे उस असीम संतुष्टि और खुशी का अनुभव हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. मुझे लगता है कि जैसे मुझे एक नरक से छुटकारा मिल गया है. जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है. आप निज केंद्रित न हों. अपने विचारों से स्वार्थी न बनें. आप लोग संकल्प लें कि अपनी आय का 1/2 भाग धम्म के प्रसार में खर्च करेंगे. बुद्ध ने अपने धम्म के प्रसार के लिए उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे उपयुक्त तरीका चुना. उसी तरह से हमें भी वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त तरीका चुनना होगा. बौद्धों को कोशिश करनी चाहिए कि जहां-जहां भी बौद्ध विहार हैं, उनके सामने बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाए जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को जैसे कि चार आर्य सत्य, आर्य आष्टांगिक मार्ग, पंचशील, बुद्ध से संबंधित धर्म स्थल, बौद्ध के त्योहार इत्यादि को मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा जाए जिससे कि आम जनता और कम पढ़े-लिखे लोग भी इसको समझ सकें. जहां-जहां भी संभव हो, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया जाए और उसमें गांव और कस्बों के सभी लोगों को शामिल किया जाए क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत सिर्फ दलितों को ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस व्यक्ति को है, जो अपना कल्याण चाहते हैं और जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं.
बौद्ध अनुयायी यदि डॉ. अम्बेडकर के सुझावों पर चलते रहेंगे तो धम्म कारवां का भविष्य उज्जवल ही रहेगा और धम्म कारवां इसी तरह बढ़ता जाएगा. वैसे भी भूमंडलीकरण के कारण लोगों में आर्थिक समृद्धि आने के साथ मानसिक तनाव बढ़ेगा और दुनिया में अशांति भी बढ़ेगी. इन सबसे निपटने में बुद्धआनंद श्रीकृष्ण की शील-समाधि और प्रज्ञा पर आधारित शिक्षाएं बहुत काम आएगी क्योंकि दुनिया को ‘युद्ध’ की नहीं ‘बुद्ध’ की आवश्यकता है.
लेखक एक बौद्ध विचारक, साहित्यकार और सामाजिक चिंतक हैं. उनसे संपर्क उनकी E-mail- anand622009@hotmail.com पर किया जा सकता है.
बोधिसत्व भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी. यह वह तारीख थी, जब भारत में धम्म कारवां को नयी गति और दिशा मिली थी. अब उस तारीख के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में इन 57 सालों में धम्म कारवां की प्रगति, उसकी दशा, दिशा और भविष्य का अवलोकन करने की आवश्यकता है. लेकिन इन तमाम अवलोकनों की बुनियाद में पहला सवाल यह खड़ा है कि आखिर बाबासाहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया और धम्म कारवां क्यों आरंभ किया?
असल में डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि भारत में प्रचलित जातिगत असमानता दलितों के पिछड़े होने का मुख्य कारण है. 9 मई, 1916 को कोलम्बिया विश्वविद्यालय में आयोजित एक सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर ‘भारत में जातियां-उनकी संरचना, उद्भव एवं विकास’ के जरिए डॉ. अम्बेडकर ने यह साबित कर दिया था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने जातिगत असमानता की व्यवस्था को शास्त्र सम्मत दिखाने की कोशिश की है और ये धारणा फैलाई है कि शास्त्र गलत नहीं हो सकते. भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों के मानवाधिकारों के लिए अलग-अलग मोर्चे पर प्रयास करना शुरू कर दिया. महाड सत्याग्रह द्वारा सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के अधिकार, कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार, अंग्रेजी सरकार के सामने दलितों के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार, गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन के अधिकार की लड़ाई ऐसी ही कोशिश थी. 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा भी कर दी थी लेकिन महात्मा गांधी द्वारा आमरण-अनशन करने के कारण डॉ़. अम्बेडकर को तरह-तरह की धमकियां मिली. तब डॉ. अम्बेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट स्वीकार करना पड़ा और दलितों के लिए आरक्षण के बदले में पृथक निर्वाचन का हक छोड़ना पड़ा. इस संघर्ष के दौरान डॉ. अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हिन्दू धर्म में रहकर दलितों को राजनैतिक आजादी का अधिकार भले ही मिल जाए लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक बराबरी का हक नहीं मिल सकता. इसलिए 1935 में येवला (नाशिक) में डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वह हिन्दू धर्म में पैदा हुए थे यह उनके वश की बात नहीं थी लेकिन हिन्दू रहकर वह मरेंगे नहीं, यह उनके वश में है. डॉ. अम्बेडकर ने धर्म-परिवर्तन का निश्चय येवला की सभा में ही कर लिया था.
धर्म परिवर्तन पर विचार करने के लिए 30 एवं 31 मई 1936 को बंबई में आयोजित महार परिषद को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा थाः -‘धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है. यह ‘मनुष्य के जीवन को सफल कैसे बनाया जाय’ इस सरोकार से जुड़ा प्रश्न है… इसको समझे बिना आप धर्म परिवर्तन के संबंध में मेरी घोषणा के वास्तविक निहितार्थ का अहसास कर पाने में समर्थ नहीं होंगे. छुआछूत की स्पष्ट समझ और वास्तविक जीवन में इसके अमल का अहसास कराने के लिए मैं आप लोगों के खिलाफ किये जाने वाले अन्याय और अत्याचारों की दास्तान का स्मरण कराना चाहता हूं. सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने का हक जताने पर या सार्वजनिक कुंओं से पानी भरने का अधिकार जताने पर या घोड़ी पर दूल्हे को बैठाकर बारात को जुलूस की शक्ल में सार्वजनिक रास्तों से घुमाने के अधिकार आदि का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को सवर्ण हिन्दुओं द्वारा मारे-पीटे जाने के उदाहरण तो बहुत आम हैं. लेकिन ऐसी और भी अनेक वजहें हैं जिनके कारण दलितों पर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न का कहर ढाया जाता है… खरी बात पूछूं तो बताइये कि इस समय हिन्दुओं और आप लोगों के बीच क्या किसी प्रकार के समाजिक संबंध हैं?
जिस तरह मुसलमान हिन्दुओं से भिन्न हैं; उसी तरह दलित लोग भी हिन्दुओं से नितान्त भिन्न हैं. जिस तरह मुसलमानों और ईसाइयों के साथ हिन्दुओं का रोटी-बेटी का कोई सम्बन्ध नहीं होता है उसी तरह आप लोगों के साथ भी हिन्दुओं का किसी भी प्रकार का रोटी-बेटी का कोई संबंध नहीं है… आपका समाज और उनका समाज दो बिल्कुल अलग-अलग समूह हैं… हालांकि आप लोगों ने धर्मांतरण के महत्व को नहीं समझा है लेकिन निस्संदेह रूप से आप लोगों ने नामान्तरण यानि नाम परिवर्तन के महत्व को समझ ही लिया है. अगर आप लोगों में से किसी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में सवाल कर दिया जाता है कि वह किस जाति का है तो वह दलित होने के रूप में अपना उत्तर देता है, लेकिन वह महार है या भंगी है, ऐसा बताने में संकोच करता है. जब तक कुछ विशेष परिस्थितियों की मजबूरी न हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम नहीं बदल सकता. ऐसे नाम परिवर्तन का कारण यह है कि एक अनजान आदमी तो दलित और सवर्ण के बीच कोई अन्तर कर नहीं सकता. और जब तक एक हिन्दू को किसी व्यक्ति की जाति का पता नहीं चल जाता तब तक उस व्यक्ति के दलित होने के कारण वह हिन्दू उस व्यक्ति के खिलाफ अपने मन में नफरत का भाव नहीं भर सकता. सवर्ण हिन्दुओं को जब तक साथ यात्रा कर रहे दलितों की जातियों की जानकारी नहीं होती है तब तक तो यात्रा के दौरान वे बड़े दोस्ताना अंदाज में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी हिन्दू को यह पता चलता है कि वह जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहा है वह दलित है; तो उसका मुंह और मन तुरंत कसैला हो जाता है. आप लोगों के लिए इस तरह के अनुभव नये नहीं हैं.
आखिर ऐसा क्यों होता है? आप महार कहने के बजाय स्वयं को चोखामेला बता कर या भंगी कहने के बजाय वाल्मीकि बता कर दूसरों को चकमा देने की कोशिश करते हैं. लेकिन आप लोग यह तो जानते ही हैं कि दूसरे लोग इस तरह के झांसे में नहीं आते. आप लोग अपने को चाहे चोखामेला कहें या दलित कहें; लोग तो जान ही जाते हैं कि आप क्या हैं. आप लोगों ने अपनी छुपा-छुपी की ऐसी कारगुजारियों से ही नाम-परिवर्तन की आवश्यकता को स्वयं ही सिद्ध कर दिया है. तो फिर धर्म-परिवर्तन करने में आखिर क्या ऐतराज होना चाहिए? धर्म-परिवर्तन करना नाम परिवर्तन करने जैसा ही है. धर्म-परिवर्तन करने के पश्चात ही नाम-परिवर्तन आप लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा. अपने को एक मुसलमान, एक ईसाई, एक बौद्ध या एक सिक्ख कहना एक धर्म का परिवर्तन मात्र नहीं है बल्कि एक नाम का भी परिवर्तन है. यही सच्चा नाम परिवर्तन है… जब तक आप हिन्दू धर्म में बने रहेंगे तब तक आपको अपने जाति नाम को छिपा कर नाम-परिवर्तन करते रहने पर निरन्तर मजबूर होना पड़ेगा… इसलिए मैं आप लोगों से यह पूछता हूं कि बजाय इसके कि आप आज एक नाम बदलें, कल दूसरा नाम बदलें और पेंडुलम की तरह लगातार ढुलमुल हालत में बने रहें, आप लोगों को धर्म परिवर्तन करके अपना नाम स्थाई रूप से क्यों नहीं बदल लेना चाहिये?’ डॉ. अम्बेडकर द्वारा कही गई उपरोक्त बातें कमोबेश आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि सन् 1935 में थी.
इसी सभा में धर्म परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा:
‘मुझे उस प्रश्न पर बस आश्चर्य ही होता है जिसे कुछ हिन्दू कुछ इस तरह उठाते हैं कि केवल धर्म-परिवर्तन से क्या होने वाला है? भारत में वर्तमान समय के सिक्खों, मुसलमानों और ईसाईयों में से अधिसंख्य लोग तो पहले हिन्दू ही थे और उन में भी शूद्रों और दलितों की तादाद ही सबसे ज्यादा है…अगर ऐसा है भी तो धर्म-परिवर्तन के बाद उनकी स्थिति में एक स्पष्ट प्रगति साफ दिखती है… समस्या पर गहन चिंतन-मनन करने के बाद हर किसी को यह मानना पड़ेगा कि दलितों के लिये धर्म-परिवर्तन उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार भारत के लिए स्वराज जरूरी है. दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक जैसा ही है, दोनों के लक्ष्य में कोई फर्क नहीं है और वह अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता प्राप्त करना.
20 वर्षों तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद डॉ. अम्बेडकर इस निश्चय पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ है और बौद्ध धर्म समानता, करूणा, मैत्री, अहिंसा और भाई-चारे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है. इसमें ऊंच-नीच और छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है. जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात डॉ. आंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर बौद्धधम्म के प्रचार-प्रसार को नई गति प्रदान की. उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का एक नया फार्मूला दिया.
वर्तमान में धम्म
भगवान बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले अषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन करके धम्म कारवां की शुरूआत की थी. डॉ. अम्बेडकर ने सन 1956 में विजयदशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लेकर धम्म चक्र का अनुपर्वतन किया. धम्म कारवां आज काफी फल-फूल चुका है. 1956 में पांच लाख लोगों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच गई है. अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली संस्करण,10 नवंबर 2006) में प्रकाशित एक रपट के अनुसार भारत वर्ष में सन 2006 में 30 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. 2001 की जनगणना के वक्त बढ़कर यह लगभग 81 लाख हो चुकी थी. जो कि 2011 की आखिरी जनगणना के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 97 लाख पहुंच गई हैं. हालांकि कुछ विशेषज्ञ भारत में बौद्धों की संख्या 3 करोड़ 50 लाख से भी अधिक मानते हैं. उनका मानना है कि जनगणना में वास्तविक संख्या इसलिए सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि काफी लोग बौद्ध होते हुए भी अपने को आधिकारिक दस्तावेजों में बौद्ध नहीं घोषित करते.
सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो लगभग सभी प्रदेशों में बौद्ध अनुयायियों ने अनेकों बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया है. पंजाब में 22 बुद्ध विहार निर्मित किए गए हैं. गुजरात में कई जगहों पर बुद्ध अनुयायियों ने बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया है. यू.पी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के तमाम प्रदेशों में अनेकों बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया जा चुका है. अमेरिका और यूरोप में भी बौद्ध धम्म बहुत तेजी से बढ़ती हुई जीवनशैली बनता जा रहा है. डॉ. आंबेडकर ने धम्म दीक्षा लेते हुए कहा था कि वो एक नए किस्म का धम्म कारवां आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु शील सदाचार का पालन करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य करेंगे. इससे प्रभावित होकर एशिया के अन्य देशों में भी बौद्ध पुनर्जागरण तेजी से हुआ. जिनेवा आधारित ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व आध्यात्मिक संगठन’ ने 2009 का ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म का सम्मान’ बौद्ध धम्म को प्रदान किया.
धम्म कारवां की दिशा
आज के वक्त में यह सोचना भी जरूरी है कि धम्म कारवां की दिशा क्या हो और उसमें हमारी भूमिका क्या हो?
बौद्धों का जीवन- बौद्धों को अपना जीवन और दैनिक क्रियाकलाप बौद्धधम्म की शिक्षाओं के अनुरूप जीना चाहिए. इसके लिए सबसे आवश्यक है कि देवी-देवताओं की पूजा का मोह त्यागना होगा. धम्म वंदना और दीक्षा प्रतिज्ञा गाथा के उस पालि सुत्त की बातें जीवन में उतारनी होगी जिसमें कहा गया है कि… ‘मैं भगवान बुद्ध के अलावा (बुद्ध मार्ग) अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा. इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. मैं धम्म के अलावा अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा. धम्म ही मेरा श्रद्धा स्थान है, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. भिक्खु संघ के अलावा मैं अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा; इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो.’
संस्कृति- बौद्धों को एक ऐसी संस्कृति का विकास करना चाहिए जिसमें प्रत्येक देशवासी को एक सम्मानित नागरिक माना जाए और प्रत्येक नागरिक की मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर सुनिश्चित हो. देश में परस्पर भाईचारे के साथ प्रेम और सौहार्द की भावना हो. डॉ. आंबेडकर का कहना था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक-भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए… लेकिन इस भावना के विकास में जाति सबसे बड़ी बाधा है. डॉ आंबेडकर का निष्कर्ष था कि जाति की प्रकृति ही विखण्डन और विभाजन करना है. जाति का यह अभिशाप है. जाति भावनाओं से आर्थिक विकास रूकता है. इसलिए डॉ. अंबेडकर का लगातार यह प्रयत्न रहा कि भारत में एक ऐसी सांझी संस्कृति का निर्माण हो जिसमें जात-पात के आधार पर लोगों के साथ अन्याय और शोषण न हो और हर नागरिक अपनी क्षमताओं के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके. आपस में उपजातिवाद छोड़कर एक साझा पहचान जो बौद्ध पहचान है उसको अपनाना चाहिए और आपस में रोटी-बेटी का संबंध कायम करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता मिले. डॉ. आंबेडकर चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों में खान-पान का संबंध विकसित हो. जो लोग धम्म दीक्षा लेने के बाद भी जाति और उप-जाति बनाए रखना चाहते हैं या जाति-पात में विश्वास करते हैं वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं क्योंकि इससे बौद्ध धर्म में भी जाति का जहर फैल जाएगा.
विपस्सना- एक अन्य चर्चा विपस्सना को लेकर है. बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि विपस्सना लोगों को निष्क्रिय कर देती हैं, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है जबकि दलित समाज को आंदोलित रखने के लिए क्रोध की आवश्यकता है और विपस्सना से समाज सेवा की भावना कम हो जाती है. इन सब मिथ्या प्रचार को हमें दूर करना होगा. गौतम बुद्ध ने छः वर्षों तक ध्यान साधना किया और विपस्सना का आविष्कार किया. विपस्सना करते-करते 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व को प्राप्त किया. बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात 45 वर्षो तक शहरों, गांवों, कस्बों में जा-जाकर धम्म का प्रसार किया. यदि भगवान बुद्ध निष्क्रिय नहीं हुए तो फिर उनकी खोजी हुई विपस्सना करने से उनके अनुयायी कैसे निष्क्रिय हो सकते हैं?
भिक्खुओं द्वारा खुद पहल कर लोगों से नहीं मिलना भी एक समस्या है. बहुत से भिक्खु इस आशा में रहते हैं कि जब कोई बुद्ध विहार में आएगा तभी वो धम्म दीक्षा की बात करेंगे. इस बारे में भगवान बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है. भगवान बुद्ध बोधगया से चलकर सारनाथ आए थे और धम्मचक्र प्रवर्तन किया था. वह इस भरोसे में नहीं बैठे रहे कि लोग बोधगया आए और तब वो उनको धम्म सिखाएं. इसीलिए डॉं. आंबेडकर ने ‘इंगेज्ड बुद्धिज्म’ की परिकल्पना की थी. इस परिकल्पना को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है. वियतनाम में भिक्खु संघ ने अमेरिका के आक्रमण के खिलाफ पूरी ताकत से विरोध किया और लोगों के बीच जाकर धर्म का प्रचार-प्रसार किया. ताईवान में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में वहां के भिक्खुनी संघ ने अहम भूमिका अदा की है. ताईवान में भिक्खुनी संघ स्कूल भी चलाता है, अस्पताल भी चलाता है और लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं का निदान भी करता है. ताईवान के उदाहरण को भारत वर्ष में भी दोहराने की आवश्यकता है.
बौद्ध संस्कृति विकसित करना जरूरी – हर सिक्ख रविवार को अनिवार्य रूप से गुरूद्वारा जाता है, ईसाई चर्च जाते है. हर मुसलमान शुक्रवार की नमाज मस्जिद जाकर अता करता है. बौद्ध समाज के लोगों को भी ऐसी परंपरा डालनी होगी. प्रत्येक रविवार को अपने नजदीकी बौद्ध विहार में जाएं. जहां बौद्ध विहार नहीं है, वहां किसी के घर में और यदि वो भी संभव नहीं है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर कोई संगोष्ठी करें. ऐसी कोशिश भी की जा सकती है कि जीवन के उत्सव चाहे जन्मदिन का कार्यक्रम हो या सालगिरह, उसे बौद्ध विहार में मनाए. इसके साथ ही अपना जीवन पंचशीलों के अनुसार जीने की कोशिश करें. डॉ. आंबेडकर ने स्वयं बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने आवास को सजाना आरंभ किया और उत्सव मनाने की परंपरा आरंभ की. विवाह के लिए विवाह विधि का प्रतिपादन किया और बौद्ध चर्या पद्धति तैयार की. बौद्धों में शील और सदाचार का जीवन विकसित करने के लिए ‘बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया’ की स्थापना की जिसकी शाखाएं हर प्रदेश में स्थापित की गई. डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1956 को सारनाथ के मृगदाय वन में 150 भिक्खुओं के समक्ष भाषण दिया था कि प्रत्येक बौद्ध के लिए अनिवार्य है कि वह हर रविवार को बौद्ध विहार में जाए और वहां उपदेश सुने. यदि ऐसा नहीं होगा तो नव दीक्षित बौद्ध को धम्म की जानकारी नहीं हो सकेगी. प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए जिसमें सभा करने के लिए काफी स्थान रहे. बौद्ध विहारों को सभामंदिर होना चाहिए.
बाल साहित्य और बौद्ध साहित्य- सुरूचिपूर्ण बाल साहित्य और जनभाषा में बौद्ध साहित्य की भी काफी आवश्यकता है. इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय लोक भाषा में छोटी-छोटी पुस्तकें बड़े अक्षरों में छपवाई जाए और सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि साहित्य के बगैर धर्म का प्रचार-प्रसार कठिन होगा. जो भी बौद्ध साहित्य लिखा गया है, उसको और सरल और सुगम बनाकर कम से कम शब्दों में तैयार कर जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है जिससे कि किसान, मजदूर, गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सभी लोग समझ सकें और उसको जीवन में उतार सकें. बुद्ध की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शीलवान और पढ़े-लिखे भिक्खुओं की जरूरत है. इसके साथ ही, हमें एक समानांतर प्रचार व्यवस्था को विकसित करना होगा जिसमें नुक्कड़ नाटक, भजन मंडली, स्वांग मंडली, लोकगीत शामिल हैं जो लोगों तक आपकी बात पहुंचा सके.
पर्सनल लॉ की जरूरत- लगभग सभी अल्पसंख्यकों के अपने-अपने Personal Low हैं. ईसाईयों का Personal Low उनका बाईबिल है, मुसलमानों का Personal Low कुरान शरीफ द्वारा निर्धारित होता है. सिक्खों में आनंद कारज विवाह प्रथा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन बौद्धों का अपना कोई Personal Low नहीं है. इसलिए जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बन जाती, बौद्धों का भी अपना Personal Low होना चाहिए.
चारों महत्वपूर्ण अंगों को सामने आना होगा- बौद्ध धम्म के सामाजिक संगठन के चार महत्वपूर्ण अंग हैं. ये हैं भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ. धम्म कारवां के आगे बढ़ने के लिए इन चारों संघों का शील-सदाचार पूर्ण जीवन जीना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है. लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में अकेले भिक्षु संघ काम कर रहा है. अभी तक न तो भिक्षुणी संघ बन पाया है, न ही उपासक संघ और न ही उपासिका संघ. इसलिए आवश्यक है कि बौद्ध अनुयायियों को इन संघों का निर्माण करना चाहिए और उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए.
धम्म कारवां का भविष्य
धम्म के आम आदमी के जीवन में पड़ते प्रभाव और इसकी वैज्ञानिक जीवन पद्धति को देखकर यह कहा जा सकता है कि धम्म कारवां का भविष्य अत्यंत उज्जवल है. धम्म दीक्षा लेने वालों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और उनका चहुमुंखी विकास हुआ है.मशहूर समाजशास्त्री डी. एस. जनबन्धू और गौतम गावली द्वारा महाराष्ट्र में किए गए समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली उनमें एक नई पहचान और आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई, जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर में काफी सुधार आया. इन नवदीक्षित लोगों ने राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसी प्रकार का एक शोध भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. संजय चहांडे ने किया और वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धम्म दीक्षा लेने वालों का विकास धम्म दीक्षा न लेने वालों की तुलना में अधिक हुआ है. डॉ. संजय चहांडे ने इस विषय पर पीएचडी की है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दलितों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में काफी अच्छे बदलाव आए हैं. उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसके कारण उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है.
एक सर्वे के अनुसार ताईवान में बौद्ध अनुयायियों की संख्या सन् 1980 में 8 लाख थी जो 2001 में बढ़कर 55 लाख और 2006 में बढ़कर 80 लाख हो गई. इस तरह 26 सालों में ताईवान में बौद्ध अनुयायियों की संख्या दस गुणा बढ़ी है. इसी अवधि में ताईवान में बुद्ध विहारों की संख्या 1157 से बढ़कर 4500 और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 3470 से बढ़कर 10 हजार पहुंच गई. ताईवान में भिक्षु और भिक्षुनियां अनेक प्रकार के समाजिक कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसे व्यक्ति विकास के काम कर रहे हैं. इसी तरह चीन में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो गई है. थाईलैंड में 90 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है. यही स्थिति श्रीलंका, म्यामांर और भूटान जैसे देशों की है. भगवान बुद्ध के कारण एशिया के अधिकतर देश भारत को बहुत पवित्र मानते हैं और भारत की यात्रा करना अपना धर्म समझते हैं. जापान, कोरिया, थाईलैंड, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, ताईवान सहित अनेकों देशों के करोड़ों लोगों के मन में एक लालसा रहती है कि जीवन में कम से कम एक बार बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिशा और सांची के दर्शन कर पाएं. इसलिए भारतवर्ष के लिए बुद्ध और उनकी शिक्षाओं द्वारा पूरे एशिया का अगुवा बनने का सुनहरा अवसर है.
भ्रम फैलाने की कोशिश
धम्म कारवां की लोकप्रियता से डरे कुछ लोगों और संगठनों द्वारा अनेकों दुष्प्रचार करने की घटना भी सामने आई हैं. इसमें एक दुष्प्रचार यह किया जा रहा है कि बौद्धधर्म केवल दलित अपना रहे हैं. जबकि हकीकत इससे अलग है. भगवान बुद्ध दलित नहीं थे. उनके प्रथम पांचों शिष्य ब्राह्मण थे. उसके बाद यश और उसके 54 साथी व्यापारी वर्ग से थे. उसके बाद धम्मदीक्षा लेने वाले उरूवेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप और उनके 1000 शिष्य सभी ब्राह्मण थे. राजा बिबिंसार और राजा प्रसेनजित तथा शाक्य संघ के लोग सभी के सभी क्षत्रिय थे. वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मानंद कौशाम्बी, डी डी कौशाम्बी पूर्व में ब्राह्मण थे. इसी तरह भदन्त आनंद कौशलायन, आचार्य सत्यनारायण गोयनका, भन्तेसुरई सशई, अमेरिका के मशहूर फिल्म अभिनेता रिचर्ड गेरे, फिल्म प्रोड्यूसर टीना टर्नर कोई भी दलित वर्ग से नहीं है. इसलिए बौद्ध धर्म के विरोधियों के इस मिथ्या प्रचार को कि बौद्ध धर्म दलितो का धर्म होता जा रहा रोका जाना चाहिए.
इसी तरह एक प्रचार और किया जा रहा है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे. ऐसा प्रचार पहले भी होता रहा है. बुद्ध को अवतार मानने की बात सबसे पहले संभवतः छठी सदी के दौरान मत्स्यपुराण में की गई, मत्स्य पुराण का एक चरण 700 ईसवीं में महाबलीपुरम में, जहां मध्यकालीन ब्राह्मण पुस्तकों में 10 अवतारों की संकल्पना की गई है, पल्लव स्मारकों में उत्कीर्ण हैं. इस बिषय में नॉरमन कौसिन्स लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का निर्माण होने पर हिन्दू धर्म ने उसके साथ होड़ नहीं लगाई, बल्कि उसे सोख लिया. बुद्ध को अवतार के रूप में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धम्म को अवशोषित (सोख) कर उसका ब्राह्मणीकरण करना था, जिसे ब्राह्मण विरोध करके भी दबा नहीं पाए. इस प्रक्रिया में उन्होंने पशु-हिंसा छोड़कर, शाकाहार के आदर्श को अपना लिया. इस प्रक्रिया की अत्यंत चतुर चाल यह थी कि भगवान बुद्ध को वैदिक साहित्य में विष्णु के नवें अवतार के रूप में जबरन शामिल करना. निश्चित ही इस परिकल्पना ने बौद्ध धम्म की जड़ों को आघात पहुंचाया. बुद्ध को अवतार के रूप में स्थापित करने का काम एक राजनैतिक चाल के तहत किया गया. यह इस बात से स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि हिन्दू साहित्य में बुद्ध को स्थान देने के बावजूद पुराणों और अन्य हिन्दू धर्म ग्रंथों में निरंतर बुद्ध और बौद्ध धम्म के प्रति एक विरोधात्मक एवं विद्रोहात्मक स्वर देखने को मिलता है.
ऐसे प्रचार को ध्यान में रखकर ही डॉ. आंबेडकर ने प्रतिज्ञा संख्या 5 में लिखा है कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताना धोखा और झूठ प्रचार है. डॉ. आंबेडकर के अनुसार बौद्ध अनुयायी इस सिद्धांत को सिरे से नकारते हैं कि बुद्ध विष्णु के एक अवतार थे. भगवान बुद्ध ने स्वयं ही अवतार के सिद्धांत को नकारा था. बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने यह उल्हास भरी घोषणा की थी-
‘अयं अन्तिमा जाति’ (अर्थातः यह मेरा अंतिम जन्म है),
‘नत्थिदानि पुनब्भवोति’ (अर्थात अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा)
डॉ. एम. एल. जोशी ने कहा है कि बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में प्रचारित करने का सटीक कारण यह है कि बुद्ध का व्यक्तित्व इतना महान था कि उसे नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में संभव नहीं था. डॉ. जोशी के मुताबिक, ‘बुद्ध की भारतीय जनमानस में इतनी गहरी पैठ है कि पूरे देश में असंख्य विहारों के हजारों स्तंभों, दीवारों और दरवाजों पर उत्कीर्ण की गई. उनकी शिक्षाएं लगभग न समाप्त होने वाले पालि और संस्कृत साहित्य के अकूत खजाने के माध्यम से फैलाकर लोकप्रिय की गईं. अनेकों राजाओं और महान चिंतकों ने उनके युक्तिवादी व मानवतावादी मिशन को अत्यधिक ससम्मान से अपनाया. असंख्य भारतीय सदियों से उनकी प्रशंसा का गुणगान करते आ रहे हैं. वह सचमुच इतने महान थे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी. स्वाभाविक रूप से वे उच्च स्थान प्राप्त सदस्य के रूप में अवतारों के तारामंडल में आ गए.’ बुद्ध को अवतारों की श्रेणी में रखने की दुर्भावनापूर्ण सोच इस बात से भी स्पष्ट होती है कि पौराणिक लोगों ने उनके सम्मान में किसी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, इसलिए तार्किक दृष्टि से बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने का सिद्धांत दुर्भावनापूर्ण है. अगर बुद्ध को श्रद्धावश विष्णु का अवतार माना गया होता तो यह कैसे संभव है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हजारों हिन्दू मंदिरों में किसी में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होती? एक और तथ्य जानने योग्य है. बुद्ध का अर्थ ही होता है कि जन्म-मरण के संसार चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना. अगर कोई दुबारा जन्म लेता है, तो फिर बुद्ध कैसे हुआ? इसलिए बुद्ध को अवतार बताना उनके बुद्धत्व को नकारना है. 19 नबवंर, 1999 को सारनाथ में विपस्सना के प्रधानाचार्य सत्यनारायण गोयन्का और कांचीकामकोटि पीठम के तत्कालीन शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके घोषणा की थी कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे.
एक टी. वी धारावाहिक में यह दिखाया गया है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के बाद हुआ था. बौद्ध विद्वानों का कहना है कि पूरे पालि साहित्य और बौद्धों के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटकों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है. इसलिए बौद्ध अनुयायियों को इस प्रकार के प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए. बुद्ध और बौद्ध धर्म से द्वेष रखने वाले कुछ लोग यह भी प्रचार करते हैं कि बौद्धों में कई पंथ है जैसे कि हीनयान, महायान और तंत्रयान. यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित मूल सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है. सभी बौद्ध गौतम बुद्ध को अपना शास्ता मानते हैं, सभी बौद्ध चार आर्य सत्य मानते हैं. सभी बौद्ध आर्य आष्टांगिक मार्ग मानते हैं. बौद्ध धर्म का सार शील, समाधि और प्रज्ञा है. जो अंतर है वो केवल बाहरी कपड़ों और पूजा विधि को लेकर है. इसलिए ऐसे दुष्प्रचार से बचने की आवश्यकता है.
डॉ. अम्बेडकर सिर्फ नाममात्र का धर्मांतरण नहीं चाहते थे, बल्कि वे लोगों की सोच और जीवन में एक आमूलचुल परिवर्तन लाना चाहते थे. अब यह बौद्ध अनुयायियों पर निर्भर करता है कि वो धम्म कारवां को कहां ले जाना चाहते हैं. भिक्षु संघ इस बात को लेकर बेहद सजग है. यही कारण है कि भारतीय बौद्ध अब अपनी विशेष पहचान और अलग संस्कृति का विकास करने में जुटे हैं. 22 जुलाई, 2013 को सारनाथ में भन्ते पी. सिवली महाथेरा की अध्यक्षता में धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और उपासक-उपासिका शामिल हुए. इस मौके पर भारतीय चीवर पेश किया गया. अभी तक भारतीय चीवर नहीं था और इसका आयात श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड से किया जाता था. लेकिन अब भारतीय चीवर बनने के बाद चीवर की उपलब्धता आसान हो जाएगी. धम्म दीक्षा के समय डॉ. आंबेडकर ने कहा था ‘मैं आपलोगों के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूं. आप ऐसा जीवन जीएं जिससे आप सम्मान के पात्र बन सकें. ऐसा मत सोचें कि यह धम्म आपके गले में जंजीर की तरह बांध दिया गया है. जहां तक बुद्ध धम्म का सवाल है, अपना देश तो इसमें रेगिस्तान हो चुका है. अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस धम्म को उत्साह और पूरी ईमानदारी से निबाहें और ध्यान रखें कि किसी समय यह धम्म कितना वैभवशाली था. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग इस धर्मांतरण पर हंसेंगे. यह धर्म न केवल इस देश की अपितु दुनिया की सेवा कर सकता है. वैश्विक गतिविधियों के इन क्षणों में दुनिया में शांति के लिए बुद्ध धम्म अपरिहार्य है. धर्म परिवर्तन के बाद मुझे उस असीम संतुष्टि और खुशी का अनुभव हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. मुझे लगता है कि जैसे मुझे एक नरक से छुटकारा मिल गया है. जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है. आप निज केंद्रित न हों. अपने विचारों से स्वार्थी न बनें. आप लोग संकल्प लें कि अपनी आय का 1/2 भाग धम्म के प्रसार में खर्च करेंगे. बुद्ध ने अपने धम्म के प्रसार के लिए उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे उपयुक्त तरीका चुना. उसी तरह से हमें भी वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त तरीका चुनना होगा. बौद्धों को कोशिश करनी चाहिए कि जहां-जहां भी बौद्ध विहार हैं, उनके सामने बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाए जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को जैसे कि चार आर्य सत्य, आर्य आष्टांगिक मार्ग, पंचशील, बुद्ध से संबंधित धर्म स्थल, बौद्ध के त्योहार इत्यादि को मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा जाए जिससे कि आम जनता और कम पढ़े-लिखे लोग भी इसको समझ सकें. जहां-जहां भी संभव हो, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया जाए और उसमें गांव और कस्बों के सभी लोगों को शामिल किया जाए क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत सिर्फ दलितों को ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस व्यक्ति को है, जो अपना कल्याण चाहते हैं और जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं.
बौद्ध अनुयायी यदि डॉ. अम्बेडकर के सुझावों पर चलते रहेंगे तो धम्म कारवां का भविष्य उज्जवल ही रहेगा और धम्म कारवां इसी तरह बढ़ता जाएगा. वैसे भी भूमंडलीकरण के कारण लोगों में आर्थिक समृद्धि आने के साथ मानसिक तनाव बढ़ेगा और दुनिया में अशांति भी बढ़ेगी. इन सबसे निपटने में बुद्धआनंद श्रीकृष्ण की शील-समाधि और प्रज्ञा पर आधारित शिक्षाएं बहुत काम आएगी क्योंकि दुनिया को ‘युद्ध’ की नहीं ‘बुद्ध’ की आवश्यकता है.
लेखक एक बौद्ध विचारक, साहित्यकार और सामाजिक चिंतक हैं. उनसे संपर्क उनकी E-mail- anand622009@hotmail.com पर किया जा सकता है. धम्म दीक्षा विशेषः धर्मांतरण से परिवर्तन
 बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म ग्रहण कर भारत में तथागत बुद्ध के धम्म चक्र को पुनः गतिमान ही नहीं किया, बल्कि विश्व में नई धम्म क्रांति की. पांच लाख से अधिक दलितों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और हिंदू धर्म के सभी बंधन तोड़कर सदियों से दलितों-अछूतों पर लादी गयी गुलामगिरी से मुक्ति दिलाई.
चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद यदि किसी के कारण बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मांतरण हुआ तो वे बाबासाहेब अम्बेडकर ही एकमात्र महापुरुष है. उन्होंने ही भारत से लुप्तप्राय हो चुके बौद्ध धम्म को पुर्नस्थापित किया. लाखों दलितों ने बाबासाहेब पर विश्वास रखकर एक क्षण में अपने पुराने हिंदू धर्म की सभी धारणा और कुरीतियों को त्यागकर बौद्ध धम्म अपना लिया. हिंदू संस्कृति का बोझ फेंककर नयी बौद्ध संस्कृति में दीक्षा ली. डॉ. अम्बेडकर ने परंपरावादी मूल्यों से नाता तोड़कर बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दलितों को अवगतकर उनके जीवन में आमूल परिवर्तन का मार्ग दिखाया.
बौद्ध धर्मांतरण समारोह में बाबासाहेब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाऐं दी थी. जो की दलितों के लिऐ पथ प्रदर्शक सिद्ध हुई. इन प्रतिज्ञाओं से उन्होने अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म की सभी मान्यताओं से मुक्त होने की शपथ दिलायी. उन्होने हिंदू देवता ब्रम्हा, विष्णू, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणपती को ईश्वर नही मानने की और बुद्ध को अवतार नहीं मानने की प्रतिज्ञा दिलाकर दलितों को हिंदू परंपरा से पूरी तरह बाहर निकाला. साथ ही धर्मांतरण की प्रतिज्ञा में ‘मै यह मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है’ की शपथ दिलाकर डॉ. अम्बेडकर ने दलितों का धर्मांतरणही नही तो सामाजिक और मानसिक परिवर्तन भी किया. इस परिवर्तन के दृष्य परिणाम दलितों मे जल्द ही दिखने लगे.
डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिखाया बौद्ध धर्मांतरण का मार्ग ही दलितो, अछूतों के मुक्ति के लिए पथ प्रदर्शक साबित हुआ. शताब्दियों की जाति व्यवस्था से उन्हे स्वतंत्रता प्राप्त हुई. समता, बंधुता, न्याय पर आधारित बुद्ध के वैज्ञानिक विचारों को अपनाने से कतिपय दलितों के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन कर दिया. दीक्षा भूमि पर 14 अक्तूबर 1956 को धर्मांतरण समारोह के अपने ऐतिहासिक संबोधन में बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था कि ‘‘ 13 अक्तूबर 1936 को नाशिक जिले के येवला में हमने निर्णय लिया था कि हमे हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए. मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी. ‘मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, यह मेरे वश में नही था. लेकिन मै हिंदू रहकर मरूंगा नहीं’ मेरी यह 21 वर्ष की प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है. मैं आज हर्ष से प्रफुल्लीत हूं. मुझे प्रतीत होता है, आज मुझे हिंदू धर्म के नरक से छुटकारा मिल गया है.
बाबासाहेब ने कहा था कि ‘बौद्ध धम्म अभ्युदय और उत्कर्ष का मार्ग है. यह कोई बाहर का धर्म नहीं है. यह इसी भारत का है. इस देशमे 2000 वर्षो तक बौद्ध धम्म रहा है. सच कहे तो हमे अफसोस है कि हम इससे पहले ही बौद्ध धर्म में शामिल क्यो नही हुए. तथागत बुद्ध के तत्व अजर-अमर है. इतनी उदारता किसी अन्य धर्म में नही है. कालानुरूप बदलाव करने की सुविधा इसमें है. तथागत बुद्ध के धम्म को ब्राम्हणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी. उन सभी भिक्खुओं को आदेश देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा था कि ‘हे भिक्खुओ! आप लोग कई देशों और जातियों से आये है, किंन्तु, यहां आप सब एक हो गये है. जिस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों में अनेक नदियां बहती हैं और उनका अलग-अलग अस्तित्व दिखाई देता है. किन्तु, सब नदियां जब सागर में मिलती है, तब अपने पृथक अस्तित्व को खो देती है और सब समंदर में समा जाती है. बौद्ध संघ भी समंदर की भांति है. इस संघ में सभी एक है और सभी बराबर है. समुंदर में गंगा और यमुना के मिल जाने पर उनके पानी को पहचानना कठिन है. इसी प्रकार आप लोगों के बौद्ध संघ में आ जाने पर आप सभी एक हैं. सभी समान हैं. यही उदाहरण देकर बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था की ‘दुखों और शोषण से मुक्ति का एकमात्र विकल्प बुद्ध का धम्म है.’ यही मार्ग अपनाकर बाबासाहेब के अनुयायियों ने भारतमे नया इतिहास रच डाला.
दलितों के बौद्ध धर्मांतरण के संदर्भ में बौद्ध विद्वान और साहित्यकार डॉ. भदंत आनंद कौशल्यायन ने कहा था कि ‘मेरे विचार में धर्मांतर से सबसे बड़ा परिवर्तन दिमागी परिवर्तन होता है. बौद्ध धम्म ग्रहण करने से पहले यह लोग अछूत बनें रहना अपना धर्म मानते थे. वे हर तरह का अत्याचार सहने के लिए ही पैदा हुए है. बौद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद वे अछूतपन से लड़ने और अत्याचारियों से संघर्ष करने को अपना धर्म मानने लगे है.’ डॉ. कौशल्यायन की यह टिप्पणी बौद्ध धर्मांतरित दलितों पर सटीक तथा यथार्थ बयां करती है.
बौद्ध धम्म एक वैज्ञानिक जीवन पथ है. जिसका केंद्र बिंदू इन्सान है. यह धम्म मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रारंभ से लेकर अन्त तक मानवीय भावना से ओतप्रोत है. बाबासाहेब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया और दलितों में उसी ज्ञान प्रकाश की मानव ज्योति प्रज्ज्वलित की. जिससे उनका जीवन ही संवरा नहीं जगमगा उठा.
बौद्ध धर्मांतरण करने के बाद दलितों मे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरपर कई बदलाव देखे गये. हिंदू सामाजिक वर्ण-व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए दलितों ने बौद्ध धम्म का मार्ग चुना है. सनातन हिंदू धर्म के आडम्बर और कर्मकांडो को त्यागकर जिन दलितों ने धर्मांतरण किया उनका जीवनस्तर हिंदू दलितों से कहीं अधिक सुधरा है. बौद्ध धर्मांतरण करनेवाले दलितों में जागरूकता भी अधिक है. उन्होंने सामाजिक-आर्थिक रूप से भी अधिक तरक्की की है. वे ही राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अन्यों से आगे हैं.
बौद्ध धर्मांतरण से दलितों में आत्मविश्वास जगा. उनमें आशावान और संभावनात्मक परिवर्तन हुआ है. बाबासाहेब अम्बेडकर इनके धर्मांतरण के पीछे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि है. उन्होंने एक नये समतामूलक समाज निर्माण की परिकल्पना की थी. जो नवबौद्ध समाज के रूप में आज दिखता है. प्रस्थापित वर्ण-व्यवस्था की परंपराओं, रूढ़ी, विषमता को त्यागकर इस समाज ने नवीन मूल्यों, परम्परा और आधुनिक मान्यताओं को स्वीकार किया है. डॉ. अम्बेडकर का अनुकरण कर रहे दलितों ने जाति की जंजीरो से मुक्ति ही नहीं पायी, जिस देश में शताब्दियों से अछूत का दंश झेला है, उसी भारत के हर क्षेत्र में अव्वल रहकर अपना लोहा मनवाया है.
डॉ. अम्बेडकर का आंदोलन भारत से जातिव्यवस्था, चातुर्वण्य व्यवस्था, अछूतपन के विनाश का था. यह आंदोलन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित अछूत, दलितों के स्वतंत्रता का था. ब्राह्मणवाद, हिंदुत्ववाद, ब्राह्मणी धर्म के खिलाफ यह परिवर्तन का संघर्ष था. अस्पृश्यता, दासता से मुक्ति और मूलभूत अधिकारों से वंचित दलितों को एक मानव के नाते उनके मूलभूत अधिकारों को दिलाकर उनमें अस्मिता जगाने के कार्य अम्बेडकरी आंदोलन ने ही किया. डॉ. अम्बेडकर इनके विचार और जीवन-संघर्ष ने ही दलितों में नई चेतना जगाई. अस्मिता और आत्म सन्मान से दलित जाग उठा. उनकी ही प्रेरणा से दलित आंदोलन सशक्त हुआ है.
बाबासाहेब ने सामाजिक परिवर्तन के साथ ही धार्मिक क्रांति की भी बात कही थी. इसी लिए उन्होंने समतावादी बौद्ध धम्म को चुना. डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म पर कड़े प्रहार किये हैं. उन्होंने हिंदू धर्म को शोषण पर आधारित धर्म कहा है. इस धर्म में एक वर्ग या वर्णद्वारा दूसरे वर्ग का शोषण होता है. इस शोषण व्यवस्था से मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया. दलितों को मुक्ति के लिए उन्होने परम्परागत-जातिगत धन्धों को छोड़ने का आवाह्न किया. गावों से शहरों में आकर बसने का आवाह्न किया. दलितों को शिक्षित होने की सीख दी. शिक्षा से स्वाभिमान, स्व-सम्मान, आधुनिकता अपनाने को कहा. हिंदुत्व को पूरी तरह नकार कर धर्म-परिवर्तन की बात की. जाति-व्यवस्था से मुक्ति के लिए धर्मांतरण का मार्ग दिखाया.
धर्मांतरण घोषणा पर चर्चा हेतू डॉ. अम्बेडकर ने 30 और 31 मई 1936 को मुंबई में महार जाति का सम्मेलन बुलाया था. इस सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्मपर कड़े प्रहार कर धर्मांतरण के कारण भी गिनाये थे. उन्होंने कहा था ‘‘ जब तक अस्पृश्य वर्ग हिंदू समाज का हिस्सा रहेंगा, तब तक उनकी जुल्मों से मुक्ति और उन्नति नहीं हो सकती. स्वतंत्रता पाने के लिये उनको हिंदू धर्म छोड़ना होगा. जब तक वे हिंदू बने रहेंगे, तब तक उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, नौकरी, शिक्षा के अधिकार से वंचित ही रहना होगा. हिंदू धर्म में अधूतों के विकास के लिए विद्या, वित्त, और शस्त्र का अधिकार, वैयक्तिक स्वतंत्रता नकारी गयी है. जो धर्म इसलिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करेगा, उसे हमे अपनाना होगा.
अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें सही जीवन, सम्मान और प्रतिष्ठा से वंचित किया है. तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बेड़ियों के. हिंदुस्तान को जितनी स्वराज की आवश्यकता है, उतनी ही अस्पृश्योंको धर्मांतरण की. धर्मांतरण और स्वराज का अंतिम लक्ष्य स्वातंत्रता प्राप्ती ही है. धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं. तुम्हें यदि उन्नति करना है, तो हिंदू धर्म का त्याग करो. जो धर्म तुम्हे मनुष्य नहीं समझता, जो तुम्हे पानी नहीं देता. वह धर्म संज्ञा के लिए भी अपात्र है. जो धर्म तुम्हे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नकारता है. तुम्हारी प्रगती के मार्ग में बाधा डालता है. वह धर्म संज्ञा के लिए पात्र नहीं है. जो धर्म अपने अनुयायियों को अपने ही धर्म बांधवों के साथ इन्सानियत से बर्ताव करना नहीं सिखाता, मनुष्य का स्पर्श अमंगल मानता है. वह धर्म न होकर रोग है. जिस धर्म में जानवरों का स्पर्श सहज है, जनावरों ने छुआ पानी भी चलता हो, लेकिन अस्पृश्य मनुष्य का स्पर्श होने से पानी अपवित्र हो जाता हो. वह धर्म नहीं, पागलपन है. जो धर्म कुछ वर्गों को शिक्षा से दूर रखता है, उन्हें धन संचय नहीं करने देता. शस्त्र हाथ में लेने से मना करता है, वह धर्म न होकर मनुष्य जीवन की विडम्बना मात्र है. जो धर्म अज्ञानियों को अज्ञानी, निर्धनों को निर्धन रहने को बाध्य करता है, वह धर्म नहीं सजा है.’’ डॉ. अम्बेडकर ने इसी सम्मेलन में अपने धर्मांतरण की संकल्पना स्पष्ट की थी.
इसी सम्मेलन मे उन्होंने दलितों से मरे हुए जानवर ना उठाने, उनकी खाल उधड़ने जैसे घृणित काम त्यागने की तथा अन्य काम करने की अपील की थी. बच्चों को शिक्षित करने की, साफ-सुथरे-धुले हुए अच्छे कपड़े पहनने की अपील की थी. हिंदू देवी-देवताओं की पूजा ना करने की, हिंदू धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा ना करने की और हिंदू त्यौहार ना मनाने की भी अपील उन्होंने की थी. डॉ. अम्बेडकर के इसी अपील के बाद हजारों दलितों ने महाराष्ट्र में मरे जानवर उठाना और उनकी खाल उधेड़ने जैसे परम्परागत- जातिगत काम छोड़ दिये थे.
14 अक्तूबर 1956 के धर्मांतरण के बाद डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों ने पूरी तौर पर हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धम्म पथ पर मार्गक्रमण किया. हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ती, प्रतिमा और प्रतीकों को लाखों दलितों ने अपने घर से बहार निकालकर हिंदू धर्म को अपने जीवन और मन से भी बाहर कर दिया था. बौद्ध धर्मांतरण के बाद विगत 60 वर्षों में दलितों के जीवन और स्थिती में आमूल परिवर्तन हुआ है. जिन दलितों ने बौद्ध धम्म अपनाया वे बहुत हद तक हिंदू धर्म के अछूतपन से मुक्त हो चुके हैं. उनकी आज अलग पहचान है.
अम्बेडकरवादी दलितों के एक बहुत बड़े वर्ग ने बौद्ध धर्म अपनाया है. वो अपने आपको बौद्ध होने से सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करते है. विश्व के बौद्ध अनुयायियों मे से एक समझते है. उन्होंने विश्व के बौद्धों से अपने आपको जोड़ लिया है. अब उनकी नई बौद्ध संस्कृति है. धम्म पद से लेकर ‘बुद्ध और उनका धम्म’ जैसे धम्म ग्रंथ है. वे ही नये धम्म ग्रंथों के रचियता है. सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी है.
दलितों ने जातिव्यवस्था को ही नहीं नकारा बल्कि जातिवाचक नाम भी छोड़ दिये है. उत्तर और मध्य भारत में अनेक बौद्ध धर्मांतरित दलित अपने नाम के साथ बौद्ध या गौतम शब्द जोड़ृकर आत्मसम्मान से जी रहे है. हिंदू धर्म के अवतारवाद, आत्मा, परमात्मा, पुरोहितवाद को उन्होंने खारिज कर दिया है. उन्होंने सभी देवी- देवताओं को नकार दिया है. उनको जीवन में अब हिंदू देवी-देवताओं का आज कोई महत्व नहीं है. तथागत बुद्ध और बाबासाहेब अम्बेडकर ही उनके लिए महापुरुष है.
जिन दलितों को मंदिरो में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. भगवान का बहार से ही दर्शन करना पडता था. उनके स्पर्श मात्र से मंदिर के देवता अपवित्र हो जाते थे. उन्हीं दलितों ने बौद्ध धर्मांतरण के बाद अपने अलग प्रार्थना स्थल बना डाले. बुद्ध विहार यह उनके लिए प्रेरणा स्थल है. जहां भी नव बौद्ध रहते है, उस शहर, कस्बो, गावों में उन्होंने विहार बनाये है. विहारों में तथागत बुद्ध के साथ ही प्रेरणास्त्रोत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर भी विराजमान है. हिंदू मंदिरो से कही अधिक और विशाल बुद्ध विहार देश में जगह-जगह दिखते है. हर गांव में विहार बौद्ध अस्मिता के प्रतीक है. नवबौद्धों के लिए दीक्षा भूमी, चैत्य भूमी तीर्थस्थल है. बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुंबिनी परम पूजनीय धार्मिक स्थल है. हजारों नव बौद्ध म्यांमार, थाईलेंड, श्रीलंका, हॉंगकॉंग, सिंगापुर के बौद्ध स्थलों के दर्शन और पर्यटन के लिए जाते है. युवा इन देशों के साथ ही जपान, कोरिया, अमरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, युरोप में पढ़ते हैं, नौकरी के लिए जाते है. आज पूरे विश्व में नवबौद्ध संचार करते हैं. एकदम नयी सोच और संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है.
यह परिवर्तन यकायक नहीं हुआ. महाराष्ट्र में दलितों को धर्मांतरण करने के बाद भी अनेक जगहों पर हिंदुओं के जुल्मों सितम सहने पड़े थे. धर्मांतरित दलितों की बस्तियों का बहिष्कार कर दिया गया. सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाई की गयी. आटे की चक्की पर गेंहूं नहीं पीसकर दिया जाता था. किराना दुकानदार सामान देने से मना करते थे. डॉ. अम्बेडकरके साथ बौद्ध धर्मांतरण करने की सजा उन्हें दी जा रही थी. लेकिन धर्मांतरित दलितों के हौसले बुलंद थे. पूरे आत्मविश्वास के साथ वे सभी संकटों का सामना करने के लिए तैयार थे. आत्मस्वाभिमान की ज्योत प्रज्वलित हो गयी थी.
उन्होंने परम्परागत सभी धु्रणास्पद काम करना बंद कर दिया था. मरे हुए जनावर उठाना, उनकी खाल निकालने का काम छोड़ दिया. अछूतपन के सभी कामों से उन्होंने मना कर दिया था. धर्मांतरण के बाद पहला परिवर्तन यह था. गांवो-कस्बों में दलितों ने घर की देवी-देवताओं की मूर्ती, प्रतिमाओं को नदी मे प्रवाहित कर दिया. दलित बस्ती में हिंदू मंदिरों को या तो ताले लग गये या वहां की हिंदू देवता की मूर्ती हटाकर बुद्ध विहार बना दिये गये. बस्ती के मैदानों में पंचशील झेंडे लहराने लगे. जगह-जगह बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमायें खड़ी की गयी. तथागत बुद्ध की मूर्ती बैठायी गयी. दलित बस्तियों में बुद्ध वंदना के स्वर गुंजने लगे.
कुछ दलित बस्तियों में व्यायाम शाला, अखाडों को बुद्ध विहार में परिवर्तित किया गया. हजारों दलितों ने जाति त्यागकर धर्म बौद्ध लिखना प्रारंभ किया. अनेकों ने पुराने नाम बदल डाले. बच्चों के, घरों के, बस्ती के, रास्ते के, संस्था के नाम परिवर्तित कर डाले. हिंदू धर्म के सभी प्रतीक त्याग दिये गये, गुलामी के सभी अवशेष नष्ट किए गये. बुद्ध कालीन इतिहास, संस्कृति और नाम स्वीकार किए गये. बस्तियों में डॉ. अम्बेडकर और बुद्ध जयंती हर्षोल्हास से त्योंहार के तौर पर मनाई जाने लगी. लोगों ने स्वयं स्फूर्तता से शराबबंदी-नशाबंदी को अपनाया. अलग बौद्ध विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार स्वीकार किए गये. शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार के समय डफली बजाने की प्रथा बंद हुई. सभी जगह परिवर्तन प्रारंभ हुआ. नयी अस्मिता के संचार से धर्मांतरित दलितों ने नया इतिहास गढ़ा.
बाबासाहेब ने दलितों को गावों को छोड़कर शहरों में आकर बसने का आवाहन किया था. उनका अनुकरण करके हजारो लोक शहरों में आकर बसे. ‘शिक्षित बनो, संघटित हो, संघर्ष करो’ का मूलमंत्र धर्मांतरित दलितों ने आत्मसात किया. बच्चों को पढ़ाने का पहला लक्ष्य हर दलित ने रखा. मजदूरी करेंगे, सड़क पर काम करेंगे, रिक्शा चलायेंगे लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षित करने का संकल्प लिया. यही कारण है, कि आज धर्मांतरित दलितों में साक्षरता का प्रमाण सर्वाधिक है. इस समाज के हजारों डॉक्टर, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, अधिकारी है. कलेक्टर, कमीश्नर, पुलिस अधिकारी, प्रोफेसर, कुलपति, आई.ए.एस., आई.पी.एस., सचिव, अधिकारी है. आई.ए.एस., आई.पी.एस., यू.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी, की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक प्रथम स्थान पर ब्राम्हण तो दूसरे स्थान पर धर्मांतरित बौद्ध, दलित रहते. अब तो यू.पी.एस.सी. में प्रथम स्थान भी इसी समाज की छात्रा ने हासिल कर लिया है. अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र इसी समाज से आगे आ रहे है. विद्वत्ता में, प्रतियोगीता में ब्राम्हणों की बराबरी बौद्ध, दलित कर रहे है. एक बड़ा उच्च और मध्यवर्ग का इस समाज में निर्माण हुआ है. हर क्षेत्र में इस समाज ने अपना लोहा मनवाया है.
व्यापार-उद्योग में भी कुछ लोगों ने अपना स्थान बनाया है. साहित्य-लेखन में दलित, बौद्ध अग्रणी है. दलित साहित्य ने समूची भारतीय साहित्य विश्व को झकझोरकर रख दिया. पत्रकारिता में, मीडिया में भी यह समाज सक्रिय है. मासिक, साप्ताहिक पत्र ही नहीं दैनिक अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की भी मालकियत है. गायक, कलाकार समाज की आवाज बनकर उभरे है. धर्मांतरीत दलितों ने प्रगती के हर क्षेत्र को छुआ है .डॉ. अम्बेडकर के धर्मांतरण के साथ जुड़े दलितों ने अपनी अलग पहचान नहीं बनाई बल्कि नया इतिहास भी रचा है.
महाराष्ट्र में हिंदू धर्म आस्था रखकर बने रहने वाले दलित इस विकास प्रक्रिया काफी पिछे छूट गये है. उनके लिए दलित मुक्ति के कोई मायने नहीं है. हिंदू होने के बावजूद उच्चवर्णियों के अत्याचार और शोषण के वे ही अधिक शिकार हो रहे है. महार समाज ने डॉ.आंबेडकर का अनुकरण कर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. लेकिन जिन अन्य अनुसूचित जातियों ने इससे बाहर रहकर हिंदुत्व में आस्था रखी वे जातियां पिछड़ गयी है. महारों ने धर्मांतरण के बाद जो घृणीत काम-धंधे छोड़ दिये उन्हें अन्य जातियों पर थोप दिया गया. उन्होंने नियती समझकर इसे स्वीकार कर लिया. मातंग, चमार, ढोर इन जातियों में शिक्षा का प्रतिशत आज भी कम है. वे हिंदू देव -देवताओं को पूजते और बैन्ड-डफली बजाने को ही कर्तव्य समझते है. इसके बावजूद अनेक हिंदू मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित है. सार्वजनिक कुंओं पर पानी भरने की मनाही है. गांव के बाहर रहने को वे बाध्य है. हिंदुत्व में उन्हें सबसे निचले पायदान पर समझा जाता है. हिंदू दलित जातियों में कुछ डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, वकील, प्रोफेसर जरूर है, किंतु उनकी संख्या बहुत ही कम है. गावों में अत्याचार की शिकार भी अधिकतर यही जातियों होती है. मातंग समाज का डफली बजाने का परम्परागत काम है. हिंदू के त्यौहार, शादी, ब्याह समारोह में वे ही वाद्य बजाते है. मंदिर के सामने वाद्य बजाने के बावजूद अनेक मंदिरों में उनके प्रवेश पर आज भी पाबंदी है. शिक्षा और प्रशासन में उनकी कोई पूछ नहीं. हिंदू धर्म की जातिव्यवस्था में वे अभिशिप्त है.
महाराष्ट्र के साथ ही देश के जिन भागों में दलितों ने बौद्ध धम्म अपनाया, धर्मांतरण किया. उनकी स्थिती में विगत 60 बरसों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. बौद्धों की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में हैं. इस राज्य में 52 लाख से अधिक बौद्ध है. उत्तर प्रदेश में भी तीन लाख से अधिक नवबौद्ध है. उनमें से अधिकतर लोगों ने हिंदू कर्मकांड छोड़ दिये है. पूरे देश में 1991 से 2001 के बीच बौद्धों की आबादी में 24 प्रतिशत की वृद्धी हुई थी. 2011 में भी बौद्धों की आबादी बढ़ी है, लेकिन वह एक करोड़ से थोड़ी कम है.
नवबौद्धों में स्त्री-पुरुष अनुपात 943 प्रति हजार है. जबकी हिंदू दलितों में यह 936 है. दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमान, सिक्ख और जैनियों की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है. छह वर्ष तक के बच्चो में लड़कियों और लडकों का लिंग अनुपात 952 है. हिंदू से धर्म बदलकर बौद्ध हुए दलितों मे शिक्षा का दर 72.7 प्रतिशत है. जबकी हिंदू दलितों मे सिर्फ 55 प्रतिशत है. महिलाओं की शिक्षा दर क्रमशः 62 और 52 प्रतिशत है. एक अध्ययन के मुताबिक नवबौद्धों में अपार जागरुकता और शिक्षा के कारण रोजगार का प्रतिशत भी बेहतर हुआ है और वे अपेक्षाकृत संपन्न हुए है. यह उपलब्धि धर्मांतरण के 60 बरसों की है.
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नागपुर में रहते हैं. संपर्क- 09823286373
बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म ग्रहण कर भारत में तथागत बुद्ध के धम्म चक्र को पुनः गतिमान ही नहीं किया, बल्कि विश्व में नई धम्म क्रांति की. पांच लाख से अधिक दलितों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और हिंदू धर्म के सभी बंधन तोड़कर सदियों से दलितों-अछूतों पर लादी गयी गुलामगिरी से मुक्ति दिलाई.
चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद यदि किसी के कारण बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मांतरण हुआ तो वे बाबासाहेब अम्बेडकर ही एकमात्र महापुरुष है. उन्होंने ही भारत से लुप्तप्राय हो चुके बौद्ध धम्म को पुर्नस्थापित किया. लाखों दलितों ने बाबासाहेब पर विश्वास रखकर एक क्षण में अपने पुराने हिंदू धर्म की सभी धारणा और कुरीतियों को त्यागकर बौद्ध धम्म अपना लिया. हिंदू संस्कृति का बोझ फेंककर नयी बौद्ध संस्कृति में दीक्षा ली. डॉ. अम्बेडकर ने परंपरावादी मूल्यों से नाता तोड़कर बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दलितों को अवगतकर उनके जीवन में आमूल परिवर्तन का मार्ग दिखाया.
बौद्ध धर्मांतरण समारोह में बाबासाहेब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाऐं दी थी. जो की दलितों के लिऐ पथ प्रदर्शक सिद्ध हुई. इन प्रतिज्ञाओं से उन्होने अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म की सभी मान्यताओं से मुक्त होने की शपथ दिलायी. उन्होने हिंदू देवता ब्रम्हा, विष्णू, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणपती को ईश्वर नही मानने की और बुद्ध को अवतार नहीं मानने की प्रतिज्ञा दिलाकर दलितों को हिंदू परंपरा से पूरी तरह बाहर निकाला. साथ ही धर्मांतरण की प्रतिज्ञा में ‘मै यह मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है’ की शपथ दिलाकर डॉ. अम्बेडकर ने दलितों का धर्मांतरणही नही तो सामाजिक और मानसिक परिवर्तन भी किया. इस परिवर्तन के दृष्य परिणाम दलितों मे जल्द ही दिखने लगे.
डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिखाया बौद्ध धर्मांतरण का मार्ग ही दलितो, अछूतों के मुक्ति के लिए पथ प्रदर्शक साबित हुआ. शताब्दियों की जाति व्यवस्था से उन्हे स्वतंत्रता प्राप्त हुई. समता, बंधुता, न्याय पर आधारित बुद्ध के वैज्ञानिक विचारों को अपनाने से कतिपय दलितों के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन कर दिया. दीक्षा भूमि पर 14 अक्तूबर 1956 को धर्मांतरण समारोह के अपने ऐतिहासिक संबोधन में बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था कि ‘‘ 13 अक्तूबर 1936 को नाशिक जिले के येवला में हमने निर्णय लिया था कि हमे हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए. मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी. ‘मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, यह मेरे वश में नही था. लेकिन मै हिंदू रहकर मरूंगा नहीं’ मेरी यह 21 वर्ष की प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है. मैं आज हर्ष से प्रफुल्लीत हूं. मुझे प्रतीत होता है, आज मुझे हिंदू धर्म के नरक से छुटकारा मिल गया है.
बाबासाहेब ने कहा था कि ‘बौद्ध धम्म अभ्युदय और उत्कर्ष का मार्ग है. यह कोई बाहर का धर्म नहीं है. यह इसी भारत का है. इस देशमे 2000 वर्षो तक बौद्ध धम्म रहा है. सच कहे तो हमे अफसोस है कि हम इससे पहले ही बौद्ध धर्म में शामिल क्यो नही हुए. तथागत बुद्ध के तत्व अजर-अमर है. इतनी उदारता किसी अन्य धर्म में नही है. कालानुरूप बदलाव करने की सुविधा इसमें है. तथागत बुद्ध के धम्म को ब्राम्हणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी. उन सभी भिक्खुओं को आदेश देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा था कि ‘हे भिक्खुओ! आप लोग कई देशों और जातियों से आये है, किंन्तु, यहां आप सब एक हो गये है. जिस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों में अनेक नदियां बहती हैं और उनका अलग-अलग अस्तित्व दिखाई देता है. किन्तु, सब नदियां जब सागर में मिलती है, तब अपने पृथक अस्तित्व को खो देती है और सब समंदर में समा जाती है. बौद्ध संघ भी समंदर की भांति है. इस संघ में सभी एक है और सभी बराबर है. समुंदर में गंगा और यमुना के मिल जाने पर उनके पानी को पहचानना कठिन है. इसी प्रकार आप लोगों के बौद्ध संघ में आ जाने पर आप सभी एक हैं. सभी समान हैं. यही उदाहरण देकर बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था की ‘दुखों और शोषण से मुक्ति का एकमात्र विकल्प बुद्ध का धम्म है.’ यही मार्ग अपनाकर बाबासाहेब के अनुयायियों ने भारतमे नया इतिहास रच डाला.
दलितों के बौद्ध धर्मांतरण के संदर्भ में बौद्ध विद्वान और साहित्यकार डॉ. भदंत आनंद कौशल्यायन ने कहा था कि ‘मेरे विचार में धर्मांतर से सबसे बड़ा परिवर्तन दिमागी परिवर्तन होता है. बौद्ध धम्म ग्रहण करने से पहले यह लोग अछूत बनें रहना अपना धर्म मानते थे. वे हर तरह का अत्याचार सहने के लिए ही पैदा हुए है. बौद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद वे अछूतपन से लड़ने और अत्याचारियों से संघर्ष करने को अपना धर्म मानने लगे है.’ डॉ. कौशल्यायन की यह टिप्पणी बौद्ध धर्मांतरित दलितों पर सटीक तथा यथार्थ बयां करती है.
बौद्ध धम्म एक वैज्ञानिक जीवन पथ है. जिसका केंद्र बिंदू इन्सान है. यह धम्म मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रारंभ से लेकर अन्त तक मानवीय भावना से ओतप्रोत है. बाबासाहेब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया और दलितों में उसी ज्ञान प्रकाश की मानव ज्योति प्रज्ज्वलित की. जिससे उनका जीवन ही संवरा नहीं जगमगा उठा.
बौद्ध धर्मांतरण करने के बाद दलितों मे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरपर कई बदलाव देखे गये. हिंदू सामाजिक वर्ण-व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए दलितों ने बौद्ध धम्म का मार्ग चुना है. सनातन हिंदू धर्म के आडम्बर और कर्मकांडो को त्यागकर जिन दलितों ने धर्मांतरण किया उनका जीवनस्तर हिंदू दलितों से कहीं अधिक सुधरा है. बौद्ध धर्मांतरण करनेवाले दलितों में जागरूकता भी अधिक है. उन्होंने सामाजिक-आर्थिक रूप से भी अधिक तरक्की की है. वे ही राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अन्यों से आगे हैं.
बौद्ध धर्मांतरण से दलितों में आत्मविश्वास जगा. उनमें आशावान और संभावनात्मक परिवर्तन हुआ है. बाबासाहेब अम्बेडकर इनके धर्मांतरण के पीछे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि है. उन्होंने एक नये समतामूलक समाज निर्माण की परिकल्पना की थी. जो नवबौद्ध समाज के रूप में आज दिखता है. प्रस्थापित वर्ण-व्यवस्था की परंपराओं, रूढ़ी, विषमता को त्यागकर इस समाज ने नवीन मूल्यों, परम्परा और आधुनिक मान्यताओं को स्वीकार किया है. डॉ. अम्बेडकर का अनुकरण कर रहे दलितों ने जाति की जंजीरो से मुक्ति ही नहीं पायी, जिस देश में शताब्दियों से अछूत का दंश झेला है, उसी भारत के हर क्षेत्र में अव्वल रहकर अपना लोहा मनवाया है.
डॉ. अम्बेडकर का आंदोलन भारत से जातिव्यवस्था, चातुर्वण्य व्यवस्था, अछूतपन के विनाश का था. यह आंदोलन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित अछूत, दलितों के स्वतंत्रता का था. ब्राह्मणवाद, हिंदुत्ववाद, ब्राह्मणी धर्म के खिलाफ यह परिवर्तन का संघर्ष था. अस्पृश्यता, दासता से मुक्ति और मूलभूत अधिकारों से वंचित दलितों को एक मानव के नाते उनके मूलभूत अधिकारों को दिलाकर उनमें अस्मिता जगाने के कार्य अम्बेडकरी आंदोलन ने ही किया. डॉ. अम्बेडकर इनके विचार और जीवन-संघर्ष ने ही दलितों में नई चेतना जगाई. अस्मिता और आत्म सन्मान से दलित जाग उठा. उनकी ही प्रेरणा से दलित आंदोलन सशक्त हुआ है.
बाबासाहेब ने सामाजिक परिवर्तन के साथ ही धार्मिक क्रांति की भी बात कही थी. इसी लिए उन्होंने समतावादी बौद्ध धम्म को चुना. डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म पर कड़े प्रहार किये हैं. उन्होंने हिंदू धर्म को शोषण पर आधारित धर्म कहा है. इस धर्म में एक वर्ग या वर्णद्वारा दूसरे वर्ग का शोषण होता है. इस शोषण व्यवस्था से मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया. दलितों को मुक्ति के लिए उन्होने परम्परागत-जातिगत धन्धों को छोड़ने का आवाह्न किया. गावों से शहरों में आकर बसने का आवाह्न किया. दलितों को शिक्षित होने की सीख दी. शिक्षा से स्वाभिमान, स्व-सम्मान, आधुनिकता अपनाने को कहा. हिंदुत्व को पूरी तरह नकार कर धर्म-परिवर्तन की बात की. जाति-व्यवस्था से मुक्ति के लिए धर्मांतरण का मार्ग दिखाया.
धर्मांतरण घोषणा पर चर्चा हेतू डॉ. अम्बेडकर ने 30 और 31 मई 1936 को मुंबई में महार जाति का सम्मेलन बुलाया था. इस सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्मपर कड़े प्रहार कर धर्मांतरण के कारण भी गिनाये थे. उन्होंने कहा था ‘‘ जब तक अस्पृश्य वर्ग हिंदू समाज का हिस्सा रहेंगा, तब तक उनकी जुल्मों से मुक्ति और उन्नति नहीं हो सकती. स्वतंत्रता पाने के लिये उनको हिंदू धर्म छोड़ना होगा. जब तक वे हिंदू बने रहेंगे, तब तक उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, नौकरी, शिक्षा के अधिकार से वंचित ही रहना होगा. हिंदू धर्म में अधूतों के विकास के लिए विद्या, वित्त, और शस्त्र का अधिकार, वैयक्तिक स्वतंत्रता नकारी गयी है. जो धर्म इसलिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करेगा, उसे हमे अपनाना होगा.
अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें सही जीवन, सम्मान और प्रतिष्ठा से वंचित किया है. तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बेड़ियों के. हिंदुस्तान को जितनी स्वराज की आवश्यकता है, उतनी ही अस्पृश्योंको धर्मांतरण की. धर्मांतरण और स्वराज का अंतिम लक्ष्य स्वातंत्रता प्राप्ती ही है. धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं. तुम्हें यदि उन्नति करना है, तो हिंदू धर्म का त्याग करो. जो धर्म तुम्हे मनुष्य नहीं समझता, जो तुम्हे पानी नहीं देता. वह धर्म संज्ञा के लिए भी अपात्र है. जो धर्म तुम्हे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नकारता है. तुम्हारी प्रगती के मार्ग में बाधा डालता है. वह धर्म संज्ञा के लिए पात्र नहीं है. जो धर्म अपने अनुयायियों को अपने ही धर्म बांधवों के साथ इन्सानियत से बर्ताव करना नहीं सिखाता, मनुष्य का स्पर्श अमंगल मानता है. वह धर्म न होकर रोग है. जिस धर्म में जानवरों का स्पर्श सहज है, जनावरों ने छुआ पानी भी चलता हो, लेकिन अस्पृश्य मनुष्य का स्पर्श होने से पानी अपवित्र हो जाता हो. वह धर्म नहीं, पागलपन है. जो धर्म कुछ वर्गों को शिक्षा से दूर रखता है, उन्हें धन संचय नहीं करने देता. शस्त्र हाथ में लेने से मना करता है, वह धर्म न होकर मनुष्य जीवन की विडम्बना मात्र है. जो धर्म अज्ञानियों को अज्ञानी, निर्धनों को निर्धन रहने को बाध्य करता है, वह धर्म नहीं सजा है.’’ डॉ. अम्बेडकर ने इसी सम्मेलन में अपने धर्मांतरण की संकल्पना स्पष्ट की थी.
इसी सम्मेलन मे उन्होंने दलितों से मरे हुए जानवर ना उठाने, उनकी खाल उधड़ने जैसे घृणित काम त्यागने की तथा अन्य काम करने की अपील की थी. बच्चों को शिक्षित करने की, साफ-सुथरे-धुले हुए अच्छे कपड़े पहनने की अपील की थी. हिंदू देवी-देवताओं की पूजा ना करने की, हिंदू धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा ना करने की और हिंदू त्यौहार ना मनाने की भी अपील उन्होंने की थी. डॉ. अम्बेडकर के इसी अपील के बाद हजारों दलितों ने महाराष्ट्र में मरे जानवर उठाना और उनकी खाल उधेड़ने जैसे परम्परागत- जातिगत काम छोड़ दिये थे.
14 अक्तूबर 1956 के धर्मांतरण के बाद डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों ने पूरी तौर पर हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धम्म पथ पर मार्गक्रमण किया. हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ती, प्रतिमा और प्रतीकों को लाखों दलितों ने अपने घर से बहार निकालकर हिंदू धर्म को अपने जीवन और मन से भी बाहर कर दिया था. बौद्ध धर्मांतरण के बाद विगत 60 वर्षों में दलितों के जीवन और स्थिती में आमूल परिवर्तन हुआ है. जिन दलितों ने बौद्ध धम्म अपनाया वे बहुत हद तक हिंदू धर्म के अछूतपन से मुक्त हो चुके हैं. उनकी आज अलग पहचान है.
अम्बेडकरवादी दलितों के एक बहुत बड़े वर्ग ने बौद्ध धर्म अपनाया है. वो अपने आपको बौद्ध होने से सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करते है. विश्व के बौद्ध अनुयायियों मे से एक समझते है. उन्होंने विश्व के बौद्धों से अपने आपको जोड़ लिया है. अब उनकी नई बौद्ध संस्कृति है. धम्म पद से लेकर ‘बुद्ध और उनका धम्म’ जैसे धम्म ग्रंथ है. वे ही नये धम्म ग्रंथों के रचियता है. सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी है.
दलितों ने जातिव्यवस्था को ही नहीं नकारा बल्कि जातिवाचक नाम भी छोड़ दिये है. उत्तर और मध्य भारत में अनेक बौद्ध धर्मांतरित दलित अपने नाम के साथ बौद्ध या गौतम शब्द जोड़ृकर आत्मसम्मान से जी रहे है. हिंदू धर्म के अवतारवाद, आत्मा, परमात्मा, पुरोहितवाद को उन्होंने खारिज कर दिया है. उन्होंने सभी देवी- देवताओं को नकार दिया है. उनको जीवन में अब हिंदू देवी-देवताओं का आज कोई महत्व नहीं है. तथागत बुद्ध और बाबासाहेब अम्बेडकर ही उनके लिए महापुरुष है.
जिन दलितों को मंदिरो में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. भगवान का बहार से ही दर्शन करना पडता था. उनके स्पर्श मात्र से मंदिर के देवता अपवित्र हो जाते थे. उन्हीं दलितों ने बौद्ध धर्मांतरण के बाद अपने अलग प्रार्थना स्थल बना डाले. बुद्ध विहार यह उनके लिए प्रेरणा स्थल है. जहां भी नव बौद्ध रहते है, उस शहर, कस्बो, गावों में उन्होंने विहार बनाये है. विहारों में तथागत बुद्ध के साथ ही प्रेरणास्त्रोत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर भी विराजमान है. हिंदू मंदिरो से कही अधिक और विशाल बुद्ध विहार देश में जगह-जगह दिखते है. हर गांव में विहार बौद्ध अस्मिता के प्रतीक है. नवबौद्धों के लिए दीक्षा भूमी, चैत्य भूमी तीर्थस्थल है. बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुंबिनी परम पूजनीय धार्मिक स्थल है. हजारों नव बौद्ध म्यांमार, थाईलेंड, श्रीलंका, हॉंगकॉंग, सिंगापुर के बौद्ध स्थलों के दर्शन और पर्यटन के लिए जाते है. युवा इन देशों के साथ ही जपान, कोरिया, अमरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, युरोप में पढ़ते हैं, नौकरी के लिए जाते है. आज पूरे विश्व में नवबौद्ध संचार करते हैं. एकदम नयी सोच और संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है.
यह परिवर्तन यकायक नहीं हुआ. महाराष्ट्र में दलितों को धर्मांतरण करने के बाद भी अनेक जगहों पर हिंदुओं के जुल्मों सितम सहने पड़े थे. धर्मांतरित दलितों की बस्तियों का बहिष्कार कर दिया गया. सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाई की गयी. आटे की चक्की पर गेंहूं नहीं पीसकर दिया जाता था. किराना दुकानदार सामान देने से मना करते थे. डॉ. अम्बेडकरके साथ बौद्ध धर्मांतरण करने की सजा उन्हें दी जा रही थी. लेकिन धर्मांतरित दलितों के हौसले बुलंद थे. पूरे आत्मविश्वास के साथ वे सभी संकटों का सामना करने के लिए तैयार थे. आत्मस्वाभिमान की ज्योत प्रज्वलित हो गयी थी.
उन्होंने परम्परागत सभी धु्रणास्पद काम करना बंद कर दिया था. मरे हुए जनावर उठाना, उनकी खाल निकालने का काम छोड़ दिया. अछूतपन के सभी कामों से उन्होंने मना कर दिया था. धर्मांतरण के बाद पहला परिवर्तन यह था. गांवो-कस्बों में दलितों ने घर की देवी-देवताओं की मूर्ती, प्रतिमाओं को नदी मे प्रवाहित कर दिया. दलित बस्ती में हिंदू मंदिरों को या तो ताले लग गये या वहां की हिंदू देवता की मूर्ती हटाकर बुद्ध विहार बना दिये गये. बस्ती के मैदानों में पंचशील झेंडे लहराने लगे. जगह-जगह बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमायें खड़ी की गयी. तथागत बुद्ध की मूर्ती बैठायी गयी. दलित बस्तियों में बुद्ध वंदना के स्वर गुंजने लगे.
कुछ दलित बस्तियों में व्यायाम शाला, अखाडों को बुद्ध विहार में परिवर्तित किया गया. हजारों दलितों ने जाति त्यागकर धर्म बौद्ध लिखना प्रारंभ किया. अनेकों ने पुराने नाम बदल डाले. बच्चों के, घरों के, बस्ती के, रास्ते के, संस्था के नाम परिवर्तित कर डाले. हिंदू धर्म के सभी प्रतीक त्याग दिये गये, गुलामी के सभी अवशेष नष्ट किए गये. बुद्ध कालीन इतिहास, संस्कृति और नाम स्वीकार किए गये. बस्तियों में डॉ. अम्बेडकर और बुद्ध जयंती हर्षोल्हास से त्योंहार के तौर पर मनाई जाने लगी. लोगों ने स्वयं स्फूर्तता से शराबबंदी-नशाबंदी को अपनाया. अलग बौद्ध विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार स्वीकार किए गये. शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार के समय डफली बजाने की प्रथा बंद हुई. सभी जगह परिवर्तन प्रारंभ हुआ. नयी अस्मिता के संचार से धर्मांतरित दलितों ने नया इतिहास गढ़ा.
बाबासाहेब ने दलितों को गावों को छोड़कर शहरों में आकर बसने का आवाहन किया था. उनका अनुकरण करके हजारो लोक शहरों में आकर बसे. ‘शिक्षित बनो, संघटित हो, संघर्ष करो’ का मूलमंत्र धर्मांतरित दलितों ने आत्मसात किया. बच्चों को पढ़ाने का पहला लक्ष्य हर दलित ने रखा. मजदूरी करेंगे, सड़क पर काम करेंगे, रिक्शा चलायेंगे लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षित करने का संकल्प लिया. यही कारण है, कि आज धर्मांतरित दलितों में साक्षरता का प्रमाण सर्वाधिक है. इस समाज के हजारों डॉक्टर, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, अधिकारी है. कलेक्टर, कमीश्नर, पुलिस अधिकारी, प्रोफेसर, कुलपति, आई.ए.एस., आई.पी.एस., सचिव, अधिकारी है. आई.ए.एस., आई.पी.एस., यू.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी, की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक प्रथम स्थान पर ब्राम्हण तो दूसरे स्थान पर धर्मांतरित बौद्ध, दलित रहते. अब तो यू.पी.एस.सी. में प्रथम स्थान भी इसी समाज की छात्रा ने हासिल कर लिया है. अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र इसी समाज से आगे आ रहे है. विद्वत्ता में, प्रतियोगीता में ब्राम्हणों की बराबरी बौद्ध, दलित कर रहे है. एक बड़ा उच्च और मध्यवर्ग का इस समाज में निर्माण हुआ है. हर क्षेत्र में इस समाज ने अपना लोहा मनवाया है.
व्यापार-उद्योग में भी कुछ लोगों ने अपना स्थान बनाया है. साहित्य-लेखन में दलित, बौद्ध अग्रणी है. दलित साहित्य ने समूची भारतीय साहित्य विश्व को झकझोरकर रख दिया. पत्रकारिता में, मीडिया में भी यह समाज सक्रिय है. मासिक, साप्ताहिक पत्र ही नहीं दैनिक अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की भी मालकियत है. गायक, कलाकार समाज की आवाज बनकर उभरे है. धर्मांतरीत दलितों ने प्रगती के हर क्षेत्र को छुआ है .डॉ. अम्बेडकर के धर्मांतरण के साथ जुड़े दलितों ने अपनी अलग पहचान नहीं बनाई बल्कि नया इतिहास भी रचा है.
महाराष्ट्र में हिंदू धर्म आस्था रखकर बने रहने वाले दलित इस विकास प्रक्रिया काफी पिछे छूट गये है. उनके लिए दलित मुक्ति के कोई मायने नहीं है. हिंदू होने के बावजूद उच्चवर्णियों के अत्याचार और शोषण के वे ही अधिक शिकार हो रहे है. महार समाज ने डॉ.आंबेडकर का अनुकरण कर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. लेकिन जिन अन्य अनुसूचित जातियों ने इससे बाहर रहकर हिंदुत्व में आस्था रखी वे जातियां पिछड़ गयी है. महारों ने धर्मांतरण के बाद जो घृणीत काम-धंधे छोड़ दिये उन्हें अन्य जातियों पर थोप दिया गया. उन्होंने नियती समझकर इसे स्वीकार कर लिया. मातंग, चमार, ढोर इन जातियों में शिक्षा का प्रतिशत आज भी कम है. वे हिंदू देव -देवताओं को पूजते और बैन्ड-डफली बजाने को ही कर्तव्य समझते है. इसके बावजूद अनेक हिंदू मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित है. सार्वजनिक कुंओं पर पानी भरने की मनाही है. गांव के बाहर रहने को वे बाध्य है. हिंदुत्व में उन्हें सबसे निचले पायदान पर समझा जाता है. हिंदू दलित जातियों में कुछ डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, वकील, प्रोफेसर जरूर है, किंतु उनकी संख्या बहुत ही कम है. गावों में अत्याचार की शिकार भी अधिकतर यही जातियों होती है. मातंग समाज का डफली बजाने का परम्परागत काम है. हिंदू के त्यौहार, शादी, ब्याह समारोह में वे ही वाद्य बजाते है. मंदिर के सामने वाद्य बजाने के बावजूद अनेक मंदिरों में उनके प्रवेश पर आज भी पाबंदी है. शिक्षा और प्रशासन में उनकी कोई पूछ नहीं. हिंदू धर्म की जातिव्यवस्था में वे अभिशिप्त है.
महाराष्ट्र के साथ ही देश के जिन भागों में दलितों ने बौद्ध धम्म अपनाया, धर्मांतरण किया. उनकी स्थिती में विगत 60 बरसों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. बौद्धों की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में हैं. इस राज्य में 52 लाख से अधिक बौद्ध है. उत्तर प्रदेश में भी तीन लाख से अधिक नवबौद्ध है. उनमें से अधिकतर लोगों ने हिंदू कर्मकांड छोड़ दिये है. पूरे देश में 1991 से 2001 के बीच बौद्धों की आबादी में 24 प्रतिशत की वृद्धी हुई थी. 2011 में भी बौद्धों की आबादी बढ़ी है, लेकिन वह एक करोड़ से थोड़ी कम है.
नवबौद्धों में स्त्री-पुरुष अनुपात 943 प्रति हजार है. जबकी हिंदू दलितों में यह 936 है. दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमान, सिक्ख और जैनियों की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है. छह वर्ष तक के बच्चो में लड़कियों और लडकों का लिंग अनुपात 952 है. हिंदू से धर्म बदलकर बौद्ध हुए दलितों मे शिक्षा का दर 72.7 प्रतिशत है. जबकी हिंदू दलितों मे सिर्फ 55 प्रतिशत है. महिलाओं की शिक्षा दर क्रमशः 62 और 52 प्रतिशत है. एक अध्ययन के मुताबिक नवबौद्धों में अपार जागरुकता और शिक्षा के कारण रोजगार का प्रतिशत भी बेहतर हुआ है और वे अपेक्षाकृत संपन्न हुए है. यह उपलब्धि धर्मांतरण के 60 बरसों की है.
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नागपुर में रहते हैं. संपर्क- 09823286373 सवर्णों ने की बाबासाहेब का पुतला जलाने की कोशिश, बवाल
 ग्वालियर। भितरवार के चरखा गांव में दशहरे की रात डॉ. भीमराव अम्बेडकर का पुतला लेकर फेरी लगाए जाने पर बुधवार को हंगामा हो गया. सुबह 11 बजे 96 गांव जाटव समाज सुधारक समिति के आह्वान पर दलित लामबंद होकर भितरवार थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया. डबरा नगर पालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेड़िया के साथ कई दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डबरा-भितरवार रोड पर विरोध प्रदर्शन किया. करीब तीन घंटे बाद दोपहर दो बजे पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज कर लिया.
प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि चरखा गांव में कुछ लोगों ने रावण के पुतले की तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पुतले को लेकर गांव में फेरी लगाई और अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए. इसी बीच गांव में ऐसी अफवाह फैली कि इन लोगों द्वारा अम्बेडकर के पुतले को जलाने की तैयारी की जा रही है. इसे लेकर जनपद सदस्य रामहेत जाटव, बलवीर सिंह, अजीत, जगदीश सिंह, भूपेन्द्र सिंह, कोक सिंह, कप्तान सिंह ने उनके साथ मारपीट कर दी.
बुधवार की सुबह यह मामला तूल पकड़ गया और 96 गांव जाटव समाज सुधार समिति के कार्यकर्ता और डबरा नगर पालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेड़िया के नेतृत्व में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने का घेराव करने पहुंच गए. तनाव बढ़ता देख पुलिस ने दोपहर में सीताराम जाटव की रिपोर्ट पर 30 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 294, 336, 452, 506, 124 ए और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है.
आरोपियों के नाम चन्द्रमोहन शर्मा, हरनाम सिंह, प्रदीप सिंह, राजेन्द्र, हरबल्लभ योगी, रामहेत, अवधेश, संदीप, मुकेश पवैया, राजू, शेख सिंह पवैया, मजबूत सिंह, किल्लू, राहुल योगी, बंटी ठाकुर, सूरज, राजवीर सिंह, अंकित, अजय, दलवीर सिंह, सोनू, महेश शर्मा, माखन सिंह, शिवकुमार, पिंकू, आकाश, सुनील योगी, माखन योगी, सुनील, कल्लू योगी हैं.
पुलिस ने 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. इसमें धारा 124 ए भी शामिल है. अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि 124 ए धारा राष्ट्रद्रोह की है. साथ ही पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें यह अंकित किया गया है कि इन लोगों ने बाबासाहेब का पुतला लेकर फेरी लगाई और अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. साथ ही दलित समाज के कुछ लोगों से मारपीट भी की. इस संबंध में देहात एएसपी योगेश्वर शर्मा ने बताया कि चरखा गांव में जो विवाद हुआ है, उस संबंध में बलबा, मारपीट का मामला दर्ज किया है. राष्ट्रद्रोह जैसा कुछ नहीं है. यदि कोई देश के खिलाफ टिप्पणी करता है या देश को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ ही राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है.
चरखा के जनपद सदस्य रामहेत जाटव ने कहा कि सवर्ण समाज के लोगों की ओर से डॉ. अम्बेडकर का पुतला लेकर गांव में फेरी लगाई गई. साथ ही अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी.
ग्वालियर। भितरवार के चरखा गांव में दशहरे की रात डॉ. भीमराव अम्बेडकर का पुतला लेकर फेरी लगाए जाने पर बुधवार को हंगामा हो गया. सुबह 11 बजे 96 गांव जाटव समाज सुधारक समिति के आह्वान पर दलित लामबंद होकर भितरवार थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया. डबरा नगर पालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेड़िया के साथ कई दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डबरा-भितरवार रोड पर विरोध प्रदर्शन किया. करीब तीन घंटे बाद दोपहर दो बजे पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज कर लिया.
प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि चरखा गांव में कुछ लोगों ने रावण के पुतले की तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पुतले को लेकर गांव में फेरी लगाई और अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए. इसी बीच गांव में ऐसी अफवाह फैली कि इन लोगों द्वारा अम्बेडकर के पुतले को जलाने की तैयारी की जा रही है. इसे लेकर जनपद सदस्य रामहेत जाटव, बलवीर सिंह, अजीत, जगदीश सिंह, भूपेन्द्र सिंह, कोक सिंह, कप्तान सिंह ने उनके साथ मारपीट कर दी.
बुधवार की सुबह यह मामला तूल पकड़ गया और 96 गांव जाटव समाज सुधार समिति के कार्यकर्ता और डबरा नगर पालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेड़िया के नेतृत्व में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने का घेराव करने पहुंच गए. तनाव बढ़ता देख पुलिस ने दोपहर में सीताराम जाटव की रिपोर्ट पर 30 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 294, 336, 452, 506, 124 ए और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है.
आरोपियों के नाम चन्द्रमोहन शर्मा, हरनाम सिंह, प्रदीप सिंह, राजेन्द्र, हरबल्लभ योगी, रामहेत, अवधेश, संदीप, मुकेश पवैया, राजू, शेख सिंह पवैया, मजबूत सिंह, किल्लू, राहुल योगी, बंटी ठाकुर, सूरज, राजवीर सिंह, अंकित, अजय, दलवीर सिंह, सोनू, महेश शर्मा, माखन सिंह, शिवकुमार, पिंकू, आकाश, सुनील योगी, माखन योगी, सुनील, कल्लू योगी हैं.
पुलिस ने 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. इसमें धारा 124 ए भी शामिल है. अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि 124 ए धारा राष्ट्रद्रोह की है. साथ ही पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें यह अंकित किया गया है कि इन लोगों ने बाबासाहेब का पुतला लेकर फेरी लगाई और अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. साथ ही दलित समाज के कुछ लोगों से मारपीट भी की. इस संबंध में देहात एएसपी योगेश्वर शर्मा ने बताया कि चरखा गांव में जो विवाद हुआ है, उस संबंध में बलबा, मारपीट का मामला दर्ज किया है. राष्ट्रद्रोह जैसा कुछ नहीं है. यदि कोई देश के खिलाफ टिप्पणी करता है या देश को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ ही राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है.
चरखा के जनपद सदस्य रामहेत जाटव ने कहा कि सवर्ण समाज के लोगों की ओर से डॉ. अम्बेडकर का पुतला लेकर गांव में फेरी लगाई गई. साथ ही अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी. ”जय भीम लगे जब नारा” एल्बम को अम्बेकरवादी-बौद्ध विचारकों ने किया रिलीज
 नई दिल्ली। मिशनरी गायक तरन्नुम बौद्ध और हेमंत कुमार बौद्ध के आठ गानों के संग्रह वाली वीडियों डीवीडी ”जय भीम लगे जब नारा” का विमोचन प्रोफेसर विवेक कुमार, आनंद श्रीकृष्णा और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने किया. इस एल्बम को प्रसिद्ध कंपनी टी-सीरीज ने निर्मित किया है.
इस अवसर पर प्रो. विवेक कुमार ने कहा कि देश में बहुआयामी दलित आंदोलन 8-9 रूप में चल रहे हैं जोकि दलित समाज में जागृति लाने का काम कर रहे हैं. उसी कड़ी में दलितों में सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन तरन्नुम बौद्ध और हेमन्त कुमार बौद्ध जैसे युवा कर रहे हैं. यह युवा जयभीम के नारे को निर्भीकता के साथ क्रांतिकारी रूप से पूरे भारत में गुंजायमान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब हमें मनुवादियों को अपशब्द कहने की जगह अपनी संस्कृति के निर्माण की ओर कार्य करना चाहिए. प्रो. विवेक कुमार ने इस मौके पर एक मोटिवेशनल गीत “जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने” भी सुनाया.
बौद्ध विद्वान आनन्द श्रीकृष्णा और बौद्धाचार्य शांति स्वरुप बौद्ध ने भी इस अवसर पर अपने ओजस्वी धम्म गर्भित विचार रखे. इसी कार्यक्रम में छमाही पत्रिका (स्मारिका) “समता युग” का विमोचन भी मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया, जिसे उपस्थित उपासक-उपासिकाओं को “समता बुद्ध विहार प्रबंधक संघ” द्वारा वितरित भी किया गया.
महोपासक आरपी राष्ट्रपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 18 उपासक और उपासिकाओं ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की. इस अवसर पर बहुजन समाज के 5 विद्वानों एवं समाज सेवियों जिनमें प्रसिद्द साहित्यकार बी. एस. भगत, धम्मसेवक रामरतन बौद्ध, समाजसेविका श्रद्धेया शकुन बौद्ध, दलित दस्तक पत्रिका के सम्पादक अशोक दास और भवतु सब्ब मंगल संघ की टीम से सर्वेश कुमार गौतम शामिल है. इन सभी को “भारतीय त्रिरत्न सम्मान-2016” के द्वारा सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में युवा कवियों बाल गंगाधर ”बागी”, प्रदीप कुमार बौद्ध और संजय गौतम ”मन्थन” ने मिशनरी कविताओं से उपस्थित उपासक-उपासिकाओं का ज्ञानरंजन किया. इस कार्यक्रम का मंच संचालन उपासक सुधीर भास्कर ने किया. गोवर्धन दास गौतम ने आये हुए सभी उपासक-उपासिकाओं का साधूवाद किया और कार्यक्रम का समापन “सब्बे सत्ता सुखी होन्तु” मंगल कामना के साथ हुआ.
नई दिल्ली। मिशनरी गायक तरन्नुम बौद्ध और हेमंत कुमार बौद्ध के आठ गानों के संग्रह वाली वीडियों डीवीडी ”जय भीम लगे जब नारा” का विमोचन प्रोफेसर विवेक कुमार, आनंद श्रीकृष्णा और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने किया. इस एल्बम को प्रसिद्ध कंपनी टी-सीरीज ने निर्मित किया है.
इस अवसर पर प्रो. विवेक कुमार ने कहा कि देश में बहुआयामी दलित आंदोलन 8-9 रूप में चल रहे हैं जोकि दलित समाज में जागृति लाने का काम कर रहे हैं. उसी कड़ी में दलितों में सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन तरन्नुम बौद्ध और हेमन्त कुमार बौद्ध जैसे युवा कर रहे हैं. यह युवा जयभीम के नारे को निर्भीकता के साथ क्रांतिकारी रूप से पूरे भारत में गुंजायमान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब हमें मनुवादियों को अपशब्द कहने की जगह अपनी संस्कृति के निर्माण की ओर कार्य करना चाहिए. प्रो. विवेक कुमार ने इस मौके पर एक मोटिवेशनल गीत “जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने” भी सुनाया.
बौद्ध विद्वान आनन्द श्रीकृष्णा और बौद्धाचार्य शांति स्वरुप बौद्ध ने भी इस अवसर पर अपने ओजस्वी धम्म गर्भित विचार रखे. इसी कार्यक्रम में छमाही पत्रिका (स्मारिका) “समता युग” का विमोचन भी मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया, जिसे उपस्थित उपासक-उपासिकाओं को “समता बुद्ध विहार प्रबंधक संघ” द्वारा वितरित भी किया गया.
महोपासक आरपी राष्ट्रपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 18 उपासक और उपासिकाओं ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की. इस अवसर पर बहुजन समाज के 5 विद्वानों एवं समाज सेवियों जिनमें प्रसिद्द साहित्यकार बी. एस. भगत, धम्मसेवक रामरतन बौद्ध, समाजसेविका श्रद्धेया शकुन बौद्ध, दलित दस्तक पत्रिका के सम्पादक अशोक दास और भवतु सब्ब मंगल संघ की टीम से सर्वेश कुमार गौतम शामिल है. इन सभी को “भारतीय त्रिरत्न सम्मान-2016” के द्वारा सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में युवा कवियों बाल गंगाधर ”बागी”, प्रदीप कुमार बौद्ध और संजय गौतम ”मन्थन” ने मिशनरी कविताओं से उपस्थित उपासक-उपासिकाओं का ज्ञानरंजन किया. इस कार्यक्रम का मंच संचालन उपासक सुधीर भास्कर ने किया. गोवर्धन दास गौतम ने आये हुए सभी उपासक-उपासिकाओं का साधूवाद किया और कार्यक्रम का समापन “सब्बे सत्ता सुखी होन्तु” मंगल कामना के साथ हुआ. हरियाणाः दलित दूल्हे को घुड़चढ़ी के दौरान घोड़ी से उतारा, मारपीट कर डीजे भी तोड़ा
 यमुनानगर। हरियाणा के कनालसी गांव में सोमवार देर रात घुड़चढ़ी रस्म के दौरान दलित समुदाय के दूल्हे को गांव के ही दूसरी जाति के लोगों ने घोड़ी से नीचे उतार दिया. आरोप है कि दूल्हे के परिजनों से मारपीट भी की गई. जिस वाहन पर डीजे लगा हुआ था, उसका शीशा भी तोड़ दिया गया. सूचना मिलने पर रात को ही थाना बूड़िया एसएचओ हरदीपेंद्र सिंह गांव में गए.
सोमवार रात कनालसी निवासी पालाराम के बेटे कर्मचंद की शादी थी. रात को गांव में घुड़चढ़ी की रस्म की जा रही थी. कर्मचंद की मां लीला देवी ने बताया कि घुड़चढ़ी के दौरान उन्होंने गांव में बने सभी चार धार्मिक स्थानों पर बेटे के साथ मत्था टेका. जब वे गांव में बनी घोड़ा गाड़ी पर जा रहे थे तो एक परिवार ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि वे घोड़ी पर चढ़ने की रस्म अदा क्यों कर रहे हैं. यह अधिकार उसको नहीं है. इस रस्म पर सिर्फ उनका ही अधिकार है, दलित का नहीं.
लीला देवी ने बताया कि जब उनके परिजनों और रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने उसके साथ झगड़ा किया. इसी बीच कुछ युवकों ने उसके डीजे वाली गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. उसके रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी. कर्मचंद की मौसी माया, गांव की रितु, संतोष, मीना आदि ने बताया कि रात को उन पर गलत तरीके से हमला किया गया. वे तो शांतिपूर्वक मत्था टेकने जा रहे थे, लेकिन दूल्हे को घोड़े से उतार दिया गया. वे इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करेंगे.
गांव की सरपंच मंजू देवी के पति राजकुमार और पूर्व सरपंच मेघ सिंह का कहना है कि मारपीट और घोड़ी से नीचे उतारने के आरोप निराधार हैं. दलित जाति के लोग रात 11 बजे शराब के नशे में धुत होकर डीजे बजा रहे थे. इसकी जानकारी उन्हें पंडित सोमपाल ने दी. उन्होंने देखा कि वे लोग आपस में लड़ रहे हैं. वे उन्हें समझाने के लिए गए थे. पालाराम का परिवार घर जाने के बाद दोबारा उनके पास आए और उन पर हमला कर दिया. गांव में आपसी माहौल न बिगड़े इसलिए वे चुप रहे. राजकुमार का कहना है कि वे सरपंच एक विशेष बिरादरी के नहीं हैं, वे सभी का नेतृत्व कर रहे हैं. अब यह मामला बुधवार पंचायत में रखा जाएगा.
बूड़िया एसएचओ हरदीपेंद्र सिह ने बताया कि सोमवार रात घुड़चढ़ी रोकने की सूचना आई थी. उसके बाद वे मौके पर पहुंचे. सरपंच और पुलिस के प्रयास से मामला सुलझ गया था. मंगलवार शाम तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है.
यमुनानगर। हरियाणा के कनालसी गांव में सोमवार देर रात घुड़चढ़ी रस्म के दौरान दलित समुदाय के दूल्हे को गांव के ही दूसरी जाति के लोगों ने घोड़ी से नीचे उतार दिया. आरोप है कि दूल्हे के परिजनों से मारपीट भी की गई. जिस वाहन पर डीजे लगा हुआ था, उसका शीशा भी तोड़ दिया गया. सूचना मिलने पर रात को ही थाना बूड़िया एसएचओ हरदीपेंद्र सिंह गांव में गए.
सोमवार रात कनालसी निवासी पालाराम के बेटे कर्मचंद की शादी थी. रात को गांव में घुड़चढ़ी की रस्म की जा रही थी. कर्मचंद की मां लीला देवी ने बताया कि घुड़चढ़ी के दौरान उन्होंने गांव में बने सभी चार धार्मिक स्थानों पर बेटे के साथ मत्था टेका. जब वे गांव में बनी घोड़ा गाड़ी पर जा रहे थे तो एक परिवार ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि वे घोड़ी पर चढ़ने की रस्म अदा क्यों कर रहे हैं. यह अधिकार उसको नहीं है. इस रस्म पर सिर्फ उनका ही अधिकार है, दलित का नहीं.
लीला देवी ने बताया कि जब उनके परिजनों और रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने उसके साथ झगड़ा किया. इसी बीच कुछ युवकों ने उसके डीजे वाली गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. उसके रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी. कर्मचंद की मौसी माया, गांव की रितु, संतोष, मीना आदि ने बताया कि रात को उन पर गलत तरीके से हमला किया गया. वे तो शांतिपूर्वक मत्था टेकने जा रहे थे, लेकिन दूल्हे को घोड़े से उतार दिया गया. वे इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करेंगे.
गांव की सरपंच मंजू देवी के पति राजकुमार और पूर्व सरपंच मेघ सिंह का कहना है कि मारपीट और घोड़ी से नीचे उतारने के आरोप निराधार हैं. दलित जाति के लोग रात 11 बजे शराब के नशे में धुत होकर डीजे बजा रहे थे. इसकी जानकारी उन्हें पंडित सोमपाल ने दी. उन्होंने देखा कि वे लोग आपस में लड़ रहे हैं. वे उन्हें समझाने के लिए गए थे. पालाराम का परिवार घर जाने के बाद दोबारा उनके पास आए और उन पर हमला कर दिया. गांव में आपसी माहौल न बिगड़े इसलिए वे चुप रहे. राजकुमार का कहना है कि वे सरपंच एक विशेष बिरादरी के नहीं हैं, वे सभी का नेतृत्व कर रहे हैं. अब यह मामला बुधवार पंचायत में रखा जाएगा.
बूड़िया एसएचओ हरदीपेंद्र सिह ने बताया कि सोमवार रात घुड़चढ़ी रोकने की सूचना आई थी. उसके बाद वे मौके पर पहुंचे. सरपंच और पुलिस के प्रयास से मामला सुलझ गया था. मंगलवार शाम तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है. अशोक विजयदशमी : दशहरा
 दशहरा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है. मुख्यतःइस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावन का वध और अयोध्या पति राम की जीत के रूप में मनाया जाता है. ये बात और है कि कौन बुरा था और कौन अच्छा इस पर सभ्य समाज में एक लम्बी बहस की जरुरत है.
जब पूरा देश रावण को जलाए जाने पर ढोल ताशे बजा-बजा कर खुशी मनाता है तब एक शहर इस उत्सव से दूर दीक्षाभूमि में लाखों लोग बौद्ध धम्म प्रवर्तन हेतु अपनी दस्तक देते है. महाराष्ट्र के विशाल नगर नागपुर में हर वर्ष दशहरा के उपलक्ष में अपने ऐतिहासिक दिन को याद करने और बौद्ध धर्म अपनाने हेतु लाखों की संख्या में एकत्र होते है. माना जाता है कि इस दिन मोर्यवंशीय सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की विजय के बाद हुए रक्तपात से खिन्न हो कर शान्ति और विकास के लिए बौद्ध धम्म स्वीकार किया और दस दिन तक राज्य की ओर से भोजन दान एवं दीपोत्सव किया.
14 अक्तूबर 1956 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने पांच लाख अनुयायियों के साथ हिन्दू धर्म को त्याग कर, बौद्ध धम्म में विश्वास करने वाले पूर्वज नागो की जमीन नागपुर में बौद्ध धम्म स्वीकार किया. आधुनिक भारत के इतिहास में दुबारा से बौद्ध धम्म की पताका फहराई गयी. बौद्ध धम्म को मानने वाले देश चीन, जापान, थाईलैंड से प्रति वर्ष हजारो की संख्या में अक्तूबर के महीने में सैलानी नागपुर की दीक्षाभूमि में दर्शन के लिए आते है.
डॉ. अम्बेडकर ने दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसका सार था ईश्वरवाद-अवतारवाद, आत्मा स्वर्ग- नर्क, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड से मुक्ति और जीवन में सादगीपूर्ण सदव्यवहार का संचार. हिन्दू धर्म की मान्यताओं से दूर जाति-उपजातियो से उपजे भेदभाव को समाप्त करके बाबासाहेब ने एक प्रबुद्ध भारत की ओर एक कदम उठाया था. नागपुर स्थित दीक्षाभूमि में तीन दिन बड़ा उत्सव होता है. महाराष्ट्र के दूर दराज जिलों, गावो कस्बों से नंगे पांव लाखों लोग दीक्षा भूमि के दर्शन करने आते है, न केवल महाराष्ट्र से बल्कि पुरे भारत के कोने-कोने से लाखों लोग दीक्षाभूमि में धम्म की वंदना करने आते है. इस उत्सव में सबसे खुबसूरत चीज जो देखने को मिलती है की भीड़भाड़ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती न ही कोई फसाद.
दलित आन्दोलन की झलक पल-पल पर देखने को मिलती है. महिलाओं के मंडप, छात्रों के मंडप, पुस्तकों के मंडप, अंधविश्वास निवारण मंडप, बुद्धिस्ट विचारों के कैम्प, कर्मचारियों के कैम्प, पत्रिकाओं के स्टाल, समता सैनिक दल का मार्च, आरपीआई का मार्च, महिलाओं का मार्च, युवाओं का मार्च नारे लगाते लोग दिखते हैं, तो नागपुर की सड़कों पर जहां-जहां से लोग गुजरते है. उनके लिए भोजन की व्यवस्था वहीं के लोग करते है. महिलाएं भोजन दान करती हैं. जितना विशाल उत्सव होता है, उतना ही विशाल पुस्तकों, पोस्टर, बिल्लो का बाजार होता है जो अपनी विशिष्ट छाप छोड़ता है.
यह उत्सव अब पूरे देश में मनाया जाता है. अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले संगठन, संस्थाएं, पार्टी, समूह दल अपने-अपने राज्यों में दशहरा के दिन अशोक विजयदशमी मनाते है. बनारस, आगरा, दिल्ली , हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कानपुर, लखनऊ में धूमधाम से मनाया जाता है. अफसोसजनक बात है कि लाखों कि संख्या में दस्तक लेनेवाले उत्सव के बारे में मिडिया, टीवी चैनल में कोई उत्साह नहीं है न ही उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग ही होती है. मुख्यधारा के अखबार दुर्गा पूजा, रावणदहन से भरे हुए मिलेंगे लेकिन हमारी मूल सभ्यता और विचारधारा पर कोई लेख टिप्पणी भी देखने को नहीं मिलेगी. अशोक विजयदशमी की याद में आज हम बौद्ध, दलित आदिवासी, घुमंतू जातीय लोगों और उनकी महिलाओं की अस्मिताओं के प्रति सजग हो कर पितृसत्तात्मक पर्व और मिथकों पर बहस चलानी होगी, बहस हमें इस बात पर भी चलानी चाहिए एक लोकतान्त्रिक देश में त्योहारों के नाम पर हम हिंसात्मक अभिव्यक्तियों को क्यों अभ्यास करे?
दशहरा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है. मुख्यतःइस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावन का वध और अयोध्या पति राम की जीत के रूप में मनाया जाता है. ये बात और है कि कौन बुरा था और कौन अच्छा इस पर सभ्य समाज में एक लम्बी बहस की जरुरत है.
जब पूरा देश रावण को जलाए जाने पर ढोल ताशे बजा-बजा कर खुशी मनाता है तब एक शहर इस उत्सव से दूर दीक्षाभूमि में लाखों लोग बौद्ध धम्म प्रवर्तन हेतु अपनी दस्तक देते है. महाराष्ट्र के विशाल नगर नागपुर में हर वर्ष दशहरा के उपलक्ष में अपने ऐतिहासिक दिन को याद करने और बौद्ध धर्म अपनाने हेतु लाखों की संख्या में एकत्र होते है. माना जाता है कि इस दिन मोर्यवंशीय सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की विजय के बाद हुए रक्तपात से खिन्न हो कर शान्ति और विकास के लिए बौद्ध धम्म स्वीकार किया और दस दिन तक राज्य की ओर से भोजन दान एवं दीपोत्सव किया.
14 अक्तूबर 1956 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने पांच लाख अनुयायियों के साथ हिन्दू धर्म को त्याग कर, बौद्ध धम्म में विश्वास करने वाले पूर्वज नागो की जमीन नागपुर में बौद्ध धम्म स्वीकार किया. आधुनिक भारत के इतिहास में दुबारा से बौद्ध धम्म की पताका फहराई गयी. बौद्ध धम्म को मानने वाले देश चीन, जापान, थाईलैंड से प्रति वर्ष हजारो की संख्या में अक्तूबर के महीने में सैलानी नागपुर की दीक्षाभूमि में दर्शन के लिए आते है.
डॉ. अम्बेडकर ने दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसका सार था ईश्वरवाद-अवतारवाद, आत्मा स्वर्ग- नर्क, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड से मुक्ति और जीवन में सादगीपूर्ण सदव्यवहार का संचार. हिन्दू धर्म की मान्यताओं से दूर जाति-उपजातियो से उपजे भेदभाव को समाप्त करके बाबासाहेब ने एक प्रबुद्ध भारत की ओर एक कदम उठाया था. नागपुर स्थित दीक्षाभूमि में तीन दिन बड़ा उत्सव होता है. महाराष्ट्र के दूर दराज जिलों, गावो कस्बों से नंगे पांव लाखों लोग दीक्षा भूमि के दर्शन करने आते है, न केवल महाराष्ट्र से बल्कि पुरे भारत के कोने-कोने से लाखों लोग दीक्षाभूमि में धम्म की वंदना करने आते है. इस उत्सव में सबसे खुबसूरत चीज जो देखने को मिलती है की भीड़भाड़ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती न ही कोई फसाद.
दलित आन्दोलन की झलक पल-पल पर देखने को मिलती है. महिलाओं के मंडप, छात्रों के मंडप, पुस्तकों के मंडप, अंधविश्वास निवारण मंडप, बुद्धिस्ट विचारों के कैम्प, कर्मचारियों के कैम्प, पत्रिकाओं के स्टाल, समता सैनिक दल का मार्च, आरपीआई का मार्च, महिलाओं का मार्च, युवाओं का मार्च नारे लगाते लोग दिखते हैं, तो नागपुर की सड़कों पर जहां-जहां से लोग गुजरते है. उनके लिए भोजन की व्यवस्था वहीं के लोग करते है. महिलाएं भोजन दान करती हैं. जितना विशाल उत्सव होता है, उतना ही विशाल पुस्तकों, पोस्टर, बिल्लो का बाजार होता है जो अपनी विशिष्ट छाप छोड़ता है.
यह उत्सव अब पूरे देश में मनाया जाता है. अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले संगठन, संस्थाएं, पार्टी, समूह दल अपने-अपने राज्यों में दशहरा के दिन अशोक विजयदशमी मनाते है. बनारस, आगरा, दिल्ली , हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कानपुर, लखनऊ में धूमधाम से मनाया जाता है. अफसोसजनक बात है कि लाखों कि संख्या में दस्तक लेनेवाले उत्सव के बारे में मिडिया, टीवी चैनल में कोई उत्साह नहीं है न ही उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग ही होती है. मुख्यधारा के अखबार दुर्गा पूजा, रावणदहन से भरे हुए मिलेंगे लेकिन हमारी मूल सभ्यता और विचारधारा पर कोई लेख टिप्पणी भी देखने को नहीं मिलेगी. अशोक विजयदशमी की याद में आज हम बौद्ध, दलित आदिवासी, घुमंतू जातीय लोगों और उनकी महिलाओं की अस्मिताओं के प्रति सजग हो कर पितृसत्तात्मक पर्व और मिथकों पर बहस चलानी होगी, बहस हमें इस बात पर भी चलानी चाहिए एक लोकतान्त्रिक देश में त्योहारों के नाम पर हम हिंसात्मक अभिव्यक्तियों को क्यों अभ्यास करे? भुखमरी और कुपोषण के दौर में परमाणु युद्ध की सोच!
 भूख के ग्लोबल सूचकांक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर तीन बच्चे में से एक बच्चे का विकास बाधित है. इस देश में अब भी आबादी के पंद्रह फीसद लोग कुपोषण के शिकार है. दुनिया के जिन 118 देशों में भुखमरी सबसे बड़ी समस्या है, उनमें भारत का स्थान 97वां है. दुनियाभर में जिन सैंतालीस देशों में भूख का लेवल अत्यंत गंभीर है, उनमें भारत शामिल है. इनमें हमारा जानी दुश्मन पाकिस्तान भी शामिल है. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीच्युट ने ये आंकडें जारी किये हैं.
इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के लिए दुनियाभर की ताकतें जुगत लगा रही हैं. युद्ध और हथियारों के काराबर का सारा दांव इस संभावित परमाणु युद्ध पर लगे हैं तो पाकिस्तान में फौजी हुकूमत पर फौज का भारी दबाव है. वह युद्ध का मौका बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. दूसरी ओर, भारतीय फौज भरातीय मजहबी सियासत के मुताबिक केंद्र सरकार की कमान में है जिसपर काबिज सत्ता के राजनीतिक समीकरण इसी युद्धोन्माद के राष्ट्रवाद से बनते हैं.
विकास का जो फर्जीवाड़ा है और अच्छे दिनों के जो ख्वाब है, उसकी हकीकत यह है कि खेती चौपट करके जल-जंगल-जमीन से किसानों को बेदखल किया जा रहा है. अंधाधुंध औद्योगीकीकरण हो रहा है. हकीकत यह है कि पिछले दस सालों में औद्योगिक उत्पादन दर इस वित्तीय वर्ष में सबसे कम हुई है. जो लगातार कम होती जा रही है. मसलन औद्योगिक उत्पादन के आकंड़ों में लगातार दूसरे महीने यानी अगस्त में भी गिरावट आई. अगस्त में ये आर्थिक उत्पादन -0.7 फीसदी घटा. जुलाई में ये गिरावट -2.5 फीसदी रही थी. गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में इसमें 6.3 फीसदी की तेजी देखने को मिली थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) आंकड़ों में बताया गया है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण कारखाना क्षेत्र के उत्पादन में 0.3 फीसदी की गिरावट है. इस क्षेत्र की पूरे आईआईपी इंडेक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है.
किसानों और खेती की तबाही से अनाज की पैदावर कम से कम होती जा रही है और भूख का भूगोल लगातार सीमाओं के आरपार विस्तृत होता जा रहा है और हमारा ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा है. हालत यह है कि भुखमरी से निपटने में हम चीन से तो पीछे हैं ही, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे कहीं आगे हैं. दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान में भुखमरी और कुपोषण संकट सबसे भारी है, जहां कश्मीर को लेकर हमेशा युद्ध का माहौल है. नेपाल और श्रीलंका में लगातार राजनीतिक उथल पुथल है. म्यांमार में भी फौजी हुकूमत है, तो बांग्लादेश भी लहूलुहान है. वहां भी आतंकवाद ने जड़ें गहरा जमा ली है और लोकतंत्र के लिए लगातार लड़ाई जारी है.
इन समस्याओं के बावजूद हमसे कम विकसित इन देशों में औद्योगीकीकरण और शहरीकरण अंधाधुंध नहीं हैं. ना ही यहां व्यापक पैमाने पर किसानों की बेदखली हुई है. यहां भुखमरी और कुपोषण से बेहतर ढंग से निपटने की तैयारी है. दूसरी ओेर, हमारे यहां विकास का मतलब किसानों की बेदखली और प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट है. दुनिया का तापमान करीब दो डिग्री सेल्सियस बढ़ने को हैं और हरियाली आहिस्ते-आहिस्ते खत्म होती जा रही है. ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं. नदियां सूखने लगी हैं और जंगलों का सफाया हो रहा है. समुद्रतटों को भी हमने रेडियोएक्टिव बना दिया है. ऐसे में बचे-खुचे खेत कब तक उपजाऊ रहेंगे, कहना मुश्किल है.
जल संसाधन नहीं रहेंगे तो हम फिर खेती के लिए मानसून के भरोसे होंगे. हमारे आधुनिक महानगरीय सभ्यता ने भूगर्भीय जल का भी काम तमाम कर दिया है. हिमालय से अबाध जलधारा को हम बांधकर बिजली बना रहे हैं. लेकिन हिमालय से पानी आना बंद हो गया तो बिजली पानी का क्या होगा, हमने अभी सोचा नहीं है. खेती चौपट करके प्राकृतिक संसाधनों को तबाह करके अंधाधुंध जो शहरीकरण हो रहा है, उसे भी बहुत जल्द बिजली पानी से मोहताज होना होगा. अनाज और सब्जियों की मंहगाई आसमान छूने लगी हैं. जिनके पास पैसे हैं वे खरीद पा रहे हैं. बहुत जल्द ऐसे दिन भी आने वाले हैं जब जेब में पैसे होंगे लेकिन बाजार में ऩ अनाज मिलने वाला है और न सब्जियां मिलने वाली है. न पीने को पानी होगा और न कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन चलाने के लिए बिजली होगी. दूसरी तरफ, औद्योगिक उत्पादन भी लगातार घट रहा है. ये हमारे सबसे अच्छे दिन हैं.
जिस कश्मीर को लेकर यह हंगामा कायम है, उसकी जनता की परवाह न तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को है और न ही भारत के हुक्मरानों को. लगातार डेढ़ महीने से कश्मीर में युद्ध के हालात है. लगातार डेढ़ महीने से कश्मीर में नागरिक और मानवाधिकारों पर अंकुश है. हालात यहां तक है कि कश्मीर में बहुसंख्य मुसलमान आबादी को मुहर्रम की आजादी भी नसीब नहीं है. ऐसा पाक फौजी हुकूमत की हरकतों की वजह से हो रहा है. तो भारत की सरकार और भारत की जनता को कश्मीर की जनता की रोजमर्रा की तकलीफों की कोई परवाह नहीं है. इन्हीं युद्ध परिस्थितियों में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत पाक सीमाएं सीलबंद हैं. सीमावर्ती तमाम गांवों से किसान जनता को उनके घर बार, खेती बाड़ी छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर किया जा रहा है. पंजाब में खेती सबसे समृद्ध है. हम अपने अनाज के भंडार को युद्ध की आग में झोंकने पर अमादा हैं.
भूख के ग्लोबल सूचकांक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर तीन बच्चे में से एक बच्चे का विकास बाधित है. इस देश में अब भी आबादी के पंद्रह फीसद लोग कुपोषण के शिकार है. दुनिया के जिन 118 देशों में भुखमरी सबसे बड़ी समस्या है, उनमें भारत का स्थान 97वां है. दुनियाभर में जिन सैंतालीस देशों में भूख का लेवल अत्यंत गंभीर है, उनमें भारत शामिल है. इनमें हमारा जानी दुश्मन पाकिस्तान भी शामिल है. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीच्युट ने ये आंकडें जारी किये हैं.
इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के लिए दुनियाभर की ताकतें जुगत लगा रही हैं. युद्ध और हथियारों के काराबर का सारा दांव इस संभावित परमाणु युद्ध पर लगे हैं तो पाकिस्तान में फौजी हुकूमत पर फौज का भारी दबाव है. वह युद्ध का मौका बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. दूसरी ओर, भारतीय फौज भरातीय मजहबी सियासत के मुताबिक केंद्र सरकार की कमान में है जिसपर काबिज सत्ता के राजनीतिक समीकरण इसी युद्धोन्माद के राष्ट्रवाद से बनते हैं.
विकास का जो फर्जीवाड़ा है और अच्छे दिनों के जो ख्वाब है, उसकी हकीकत यह है कि खेती चौपट करके जल-जंगल-जमीन से किसानों को बेदखल किया जा रहा है. अंधाधुंध औद्योगीकीकरण हो रहा है. हकीकत यह है कि पिछले दस सालों में औद्योगिक उत्पादन दर इस वित्तीय वर्ष में सबसे कम हुई है. जो लगातार कम होती जा रही है. मसलन औद्योगिक उत्पादन के आकंड़ों में लगातार दूसरे महीने यानी अगस्त में भी गिरावट आई. अगस्त में ये आर्थिक उत्पादन -0.7 फीसदी घटा. जुलाई में ये गिरावट -2.5 फीसदी रही थी. गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में इसमें 6.3 फीसदी की तेजी देखने को मिली थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) आंकड़ों में बताया गया है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण कारखाना क्षेत्र के उत्पादन में 0.3 फीसदी की गिरावट है. इस क्षेत्र की पूरे आईआईपी इंडेक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है.
किसानों और खेती की तबाही से अनाज की पैदावर कम से कम होती जा रही है और भूख का भूगोल लगातार सीमाओं के आरपार विस्तृत होता जा रहा है और हमारा ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा है. हालत यह है कि भुखमरी से निपटने में हम चीन से तो पीछे हैं ही, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे कहीं आगे हैं. दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान में भुखमरी और कुपोषण संकट सबसे भारी है, जहां कश्मीर को लेकर हमेशा युद्ध का माहौल है. नेपाल और श्रीलंका में लगातार राजनीतिक उथल पुथल है. म्यांमार में भी फौजी हुकूमत है, तो बांग्लादेश भी लहूलुहान है. वहां भी आतंकवाद ने जड़ें गहरा जमा ली है और लोकतंत्र के लिए लगातार लड़ाई जारी है.
इन समस्याओं के बावजूद हमसे कम विकसित इन देशों में औद्योगीकीकरण और शहरीकरण अंधाधुंध नहीं हैं. ना ही यहां व्यापक पैमाने पर किसानों की बेदखली हुई है. यहां भुखमरी और कुपोषण से बेहतर ढंग से निपटने की तैयारी है. दूसरी ओेर, हमारे यहां विकास का मतलब किसानों की बेदखली और प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट है. दुनिया का तापमान करीब दो डिग्री सेल्सियस बढ़ने को हैं और हरियाली आहिस्ते-आहिस्ते खत्म होती जा रही है. ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं. नदियां सूखने लगी हैं और जंगलों का सफाया हो रहा है. समुद्रतटों को भी हमने रेडियोएक्टिव बना दिया है. ऐसे में बचे-खुचे खेत कब तक उपजाऊ रहेंगे, कहना मुश्किल है.
जल संसाधन नहीं रहेंगे तो हम फिर खेती के लिए मानसून के भरोसे होंगे. हमारे आधुनिक महानगरीय सभ्यता ने भूगर्भीय जल का भी काम तमाम कर दिया है. हिमालय से अबाध जलधारा को हम बांधकर बिजली बना रहे हैं. लेकिन हिमालय से पानी आना बंद हो गया तो बिजली पानी का क्या होगा, हमने अभी सोचा नहीं है. खेती चौपट करके प्राकृतिक संसाधनों को तबाह करके अंधाधुंध जो शहरीकरण हो रहा है, उसे भी बहुत जल्द बिजली पानी से मोहताज होना होगा. अनाज और सब्जियों की मंहगाई आसमान छूने लगी हैं. जिनके पास पैसे हैं वे खरीद पा रहे हैं. बहुत जल्द ऐसे दिन भी आने वाले हैं जब जेब में पैसे होंगे लेकिन बाजार में ऩ अनाज मिलने वाला है और न सब्जियां मिलने वाली है. न पीने को पानी होगा और न कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन चलाने के लिए बिजली होगी. दूसरी तरफ, औद्योगिक उत्पादन भी लगातार घट रहा है. ये हमारे सबसे अच्छे दिन हैं.
जिस कश्मीर को लेकर यह हंगामा कायम है, उसकी जनता की परवाह न तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को है और न ही भारत के हुक्मरानों को. लगातार डेढ़ महीने से कश्मीर में युद्ध के हालात है. लगातार डेढ़ महीने से कश्मीर में नागरिक और मानवाधिकारों पर अंकुश है. हालात यहां तक है कि कश्मीर में बहुसंख्य मुसलमान आबादी को मुहर्रम की आजादी भी नसीब नहीं है. ऐसा पाक फौजी हुकूमत की हरकतों की वजह से हो रहा है. तो भारत की सरकार और भारत की जनता को कश्मीर की जनता की रोजमर्रा की तकलीफों की कोई परवाह नहीं है. इन्हीं युद्ध परिस्थितियों में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत पाक सीमाएं सीलबंद हैं. सीमावर्ती तमाम गांवों से किसान जनता को उनके घर बार, खेती बाड़ी छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर किया जा रहा है. पंजाब में खेती सबसे समृद्ध है. हम अपने अनाज के भंडार को युद्ध की आग में झोंकने पर अमादा हैं. आवासीय स्कूल में हर साल होती है 71 आदिवासी छात्रों की मौत
 मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, बीते दस वर्षों में महाराष्ट्र के आवासीय स्कूलों में पढ़ रहे 740 से अधिक छात्रों की कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य कारणों से मौत हुई. विभाग द्वारा राज्य में आदिवासी बच्चों के लिए कुल 552 आवासीय स्कूल संचालित किए जाते हैं.
आदिवासी जनसंख्या मुख्य रूप से धुले, नांदुरबार, जलगांव, नासिक, पालघर, रायगढ़, अहमदनगर, पुणे (सहयाद्रि क्षेत्र) जैसे क्षेत्रों और चंद्रपुर, गढचिरौली, गोंदिया, नागपुर, अमरावती, यवतमाल तथा नांदेड (गोंडवाना क्षेत्र) जैसे पूर्वी वन्य जिलों में केन्द्रित हैं. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में पाया गया कि औसत रूप से आदिवासी आवासीय स्कूलों के 70.80 छात्रों की हर साल मौत होती है और बीते 10 साल में 740 से अधिक की मौत हुई.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर गौर करने और स्थिति सुधारने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति बनाई है. इस रिपोर्ट का इंतजार है. आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत चीजों की कमी इन मौतों का मुख्य कारण है.
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, बीते दस वर्षों में महाराष्ट्र के आवासीय स्कूलों में पढ़ रहे 740 से अधिक छात्रों की कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य कारणों से मौत हुई. विभाग द्वारा राज्य में आदिवासी बच्चों के लिए कुल 552 आवासीय स्कूल संचालित किए जाते हैं.
आदिवासी जनसंख्या मुख्य रूप से धुले, नांदुरबार, जलगांव, नासिक, पालघर, रायगढ़, अहमदनगर, पुणे (सहयाद्रि क्षेत्र) जैसे क्षेत्रों और चंद्रपुर, गढचिरौली, गोंदिया, नागपुर, अमरावती, यवतमाल तथा नांदेड (गोंडवाना क्षेत्र) जैसे पूर्वी वन्य जिलों में केन्द्रित हैं. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में पाया गया कि औसत रूप से आदिवासी आवासीय स्कूलों के 70.80 छात्रों की हर साल मौत होती है और बीते 10 साल में 740 से अधिक की मौत हुई.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर गौर करने और स्थिति सुधारने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति बनाई है. इस रिपोर्ट का इंतजार है. आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत चीजों की कमी इन मौतों का मुख्य कारण है. …क्योंकि रावण अपना चरित्र जानता है
 रामचरितमानस मध्ययुग की रचना है. कथा का तानाबाना तुलसीबाबा ने कुछ ऐसा बुना की रावण रावण बन गया. हर युग के देशकाल का प्रभाव तत्कालीन समय की रचनाओं में सहज ही परीलक्षित होता है. रावण के पतन का मूल कारण सीताहरण है. पर सीताहरण की मूल वजह क्या है? गंभीरता से विचार करें. कई लेखक, विचारक रावण का पक्ष उठाते रहे हैं. बुरी पृवत्तियों वाले ढेरों रावण आज भी जिंदा हैं. कागज के रावण फूंकने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर जिस पौराणिक पात्र वाले रावण की बात की जा रही है, उसे ईमानदार नजरिये से देखे. विचार करें. यदि कोई किसी के बहन का नाक काट दे तो भाई क्या करेगा. आज 21वीं सदी में ऐसी घटना किसी भी सच्चे भाई के साथ होगी, तो निश्चय ही प्रतिशोध की आग में धधक उठेगा. फिर मध्य युग में सुर्पनखा के नाम का बदला रामण क्यों नहीं लेता. संभवत्त मध्ययुग के अराजक समाज में तो यह और भी समान्य बात रही होगी.
अपहृत नारी पर अपहरणकर्ता का वश चलता है. रावण ने बलात्कार नहीं किया. सीता की गरिमा का ध्यान रखा. उसे मालूम था कि सीता वनवासी बन पति के साथ सास-ससुर के बचनों का पालन कर रही है. इसलिए वैभवशाली लंका में रावण ने सीता को रखने के लिए अशोक बाटिका में रखा. सीता को पटरानी बनाने का प्रस्ताव दिया. लेकिन इसके लिए जबरदस्ती नहीं की. दरअसल मध्य युग पूरी तरह से सत्ता संघर्ष और नारी के भोगी प्रवृत्ति का युग है. इसी आलोक में तो राजेंद्र यादव हनुमान को पहला आतंकवादी की संज्ञा देते हैं. निश्चय ही कोई किसी के महल में रात में जाये और रात में सबसे खूबसूरत वाटिका को उजाड़े तो उसे क्यों नहीं दंडित किया जाए. रावण ने भी तो यहीं किया. सत्ता संघर्ष का पूरा जंजाल रामायण में दिखता है. ऋषि-मुनि दंडाकारण्य में तपत्या कर रहे थे या जासूसी.
रघुकुल के प्रति निष्ठा दिखानेवाले तपस्वी दंडाकारण्य अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह क्यों करते थे. उनका कार्य तो तप का है. जैसे ही योद्धा राम यहां आते हैं, उन्हें अस्त्र-शस्त्रों की शक्ति प्रदान करते हैं. उन्हीं अस्त्र-शस्त्रों से राम आगे बढ़ते हैं. मध्ययुग में सत्ता का जो संघर्ष था, वह किसी न किसी रूप में आज भी है. सत्ताधारी और संघर्षी बदले हुए हैं. छल और प्रपंच किसी न किसी रूप में आज भी चल रहे हैं. सत्ता की हमेशा जय होती रही है. राम की सत्ता प्रभावी हुई, तो किसी ने उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला. लेकिन जनता के मन से राम के प्रति संदेह नहीं गया. तभी एक धोबी के लांछन पर सीता को महल से निकाल देते हैं. वह भी उस सीता को जो गर्भवती थी. यह विवाद पारिवारिक मसला था.
आज भी ऐसा हो रहा है. आपसी रिश्ते के संदेह में आज भी कई महिलाओं को घर से बेघर कर दिया जाता है. फिर राम के इस प्रवृत्ति को रावण की तरह क्यों नहीं देखा जाता है. जबकि इस तरह घर से निकालने के लिए आधुनिक युग में घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा दे दी गई है. बहन की रक्षा, उनकी मर्यादा हनन करने वालों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा, पराई नारी को हाथ नहीं लगाने का उज्ज्वल चरित्र तो रावण में दिखता है. लोग कहते भी है कि रावण प्रकांड पंडित था. फिर भी उसका गुणगणान नहीं होता. विभीषण सदाचारी थे. रामभक्त थे. पर उसे कोई सम्मान कहां देता है. सत्ता की लालच में रावण की मृत्यु का राज बताने की सजा मिली. सत्ता के प्रभाव में चाहे जैसा भी साहित्य रचा जाए, इतिहास लिखा जाए, हकीकत को जानने वाला जनमानस उसे कभी मान्यता नहीं देता है. तभी तो उज्ज्वल चरित्र वाले विभीषण आज भी समाज में प्रतिष्ठा के लिए तरस रहे हैं.
सत्ता का प्रभाव था, राम महिमा मंडित हो गए. पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाने तक राम के चरित्र पर संदेह नहीं. लेकिन इसके पीछे सत्ता विस्तार की नीति जनहित में नहीं थी. राम राजा थे. मध्य युग में सत्ता का विस्तार राजा के लक्षण थे. पर प्रकांड पंडित रावण ने सत्ता का विस्तार का प्रयास नहीं किया. हालांकि दूसरे रामायण में देवताओं के साथ युद्ध की बात आती है. पर देवताओं के छल-प्रपंच के किस्से कम नहीं हैं.
काश, कागज के रावण फूंकने वाले कम से कम उसके उदत्ता चरित्र से सबक लेते. बहन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हिम्मत दिखाते. उसकी रक्षा करते. परायी नारी के साथ जबरदस्ती नहीं करते. ऐसी सीख नई पीढ़ी को देते. समाज बदलता. मुझे लगता है कि राम चरित्र की असंतुलित शिक्षा का ही प्रभाव है कि 21वीं सदी में भी अनेक महिलाएं जिस पति को देवता मानती है, वहीं उन पर शक करता है, घर से निकालता है. संभवत: यहीं कारण है कि आज धूं-धूं कर जलता हुए रावण के मुंह से चीख निकलने के बजाय हंसी निकलती है. क्योंकि वह जानता है कि जिस लिए उसे जलाया जा रहा है, वह चरित्र उसका नहीं आज के मानव रूपी राम का है.
रामचरितमानस मध्ययुग की रचना है. कथा का तानाबाना तुलसीबाबा ने कुछ ऐसा बुना की रावण रावण बन गया. हर युग के देशकाल का प्रभाव तत्कालीन समय की रचनाओं में सहज ही परीलक्षित होता है. रावण के पतन का मूल कारण सीताहरण है. पर सीताहरण की मूल वजह क्या है? गंभीरता से विचार करें. कई लेखक, विचारक रावण का पक्ष उठाते रहे हैं. बुरी पृवत्तियों वाले ढेरों रावण आज भी जिंदा हैं. कागज के रावण फूंकने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर जिस पौराणिक पात्र वाले रावण की बात की जा रही है, उसे ईमानदार नजरिये से देखे. विचार करें. यदि कोई किसी के बहन का नाक काट दे तो भाई क्या करेगा. आज 21वीं सदी में ऐसी घटना किसी भी सच्चे भाई के साथ होगी, तो निश्चय ही प्रतिशोध की आग में धधक उठेगा. फिर मध्य युग में सुर्पनखा के नाम का बदला रामण क्यों नहीं लेता. संभवत्त मध्ययुग के अराजक समाज में तो यह और भी समान्य बात रही होगी.
अपहृत नारी पर अपहरणकर्ता का वश चलता है. रावण ने बलात्कार नहीं किया. सीता की गरिमा का ध्यान रखा. उसे मालूम था कि सीता वनवासी बन पति के साथ सास-ससुर के बचनों का पालन कर रही है. इसलिए वैभवशाली लंका में रावण ने सीता को रखने के लिए अशोक बाटिका में रखा. सीता को पटरानी बनाने का प्रस्ताव दिया. लेकिन इसके लिए जबरदस्ती नहीं की. दरअसल मध्य युग पूरी तरह से सत्ता संघर्ष और नारी के भोगी प्रवृत्ति का युग है. इसी आलोक में तो राजेंद्र यादव हनुमान को पहला आतंकवादी की संज्ञा देते हैं. निश्चय ही कोई किसी के महल में रात में जाये और रात में सबसे खूबसूरत वाटिका को उजाड़े तो उसे क्यों नहीं दंडित किया जाए. रावण ने भी तो यहीं किया. सत्ता संघर्ष का पूरा जंजाल रामायण में दिखता है. ऋषि-मुनि दंडाकारण्य में तपत्या कर रहे थे या जासूसी.
रघुकुल के प्रति निष्ठा दिखानेवाले तपस्वी दंडाकारण्य अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह क्यों करते थे. उनका कार्य तो तप का है. जैसे ही योद्धा राम यहां आते हैं, उन्हें अस्त्र-शस्त्रों की शक्ति प्रदान करते हैं. उन्हीं अस्त्र-शस्त्रों से राम आगे बढ़ते हैं. मध्ययुग में सत्ता का जो संघर्ष था, वह किसी न किसी रूप में आज भी है. सत्ताधारी और संघर्षी बदले हुए हैं. छल और प्रपंच किसी न किसी रूप में आज भी चल रहे हैं. सत्ता की हमेशा जय होती रही है. राम की सत्ता प्रभावी हुई, तो किसी ने उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला. लेकिन जनता के मन से राम के प्रति संदेह नहीं गया. तभी एक धोबी के लांछन पर सीता को महल से निकाल देते हैं. वह भी उस सीता को जो गर्भवती थी. यह विवाद पारिवारिक मसला था.
आज भी ऐसा हो रहा है. आपसी रिश्ते के संदेह में आज भी कई महिलाओं को घर से बेघर कर दिया जाता है. फिर राम के इस प्रवृत्ति को रावण की तरह क्यों नहीं देखा जाता है. जबकि इस तरह घर से निकालने के लिए आधुनिक युग में घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा दे दी गई है. बहन की रक्षा, उनकी मर्यादा हनन करने वालों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा, पराई नारी को हाथ नहीं लगाने का उज्ज्वल चरित्र तो रावण में दिखता है. लोग कहते भी है कि रावण प्रकांड पंडित था. फिर भी उसका गुणगणान नहीं होता. विभीषण सदाचारी थे. रामभक्त थे. पर उसे कोई सम्मान कहां देता है. सत्ता की लालच में रावण की मृत्यु का राज बताने की सजा मिली. सत्ता के प्रभाव में चाहे जैसा भी साहित्य रचा जाए, इतिहास लिखा जाए, हकीकत को जानने वाला जनमानस उसे कभी मान्यता नहीं देता है. तभी तो उज्ज्वल चरित्र वाले विभीषण आज भी समाज में प्रतिष्ठा के लिए तरस रहे हैं.
सत्ता का प्रभाव था, राम महिमा मंडित हो गए. पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाने तक राम के चरित्र पर संदेह नहीं. लेकिन इसके पीछे सत्ता विस्तार की नीति जनहित में नहीं थी. राम राजा थे. मध्य युग में सत्ता का विस्तार राजा के लक्षण थे. पर प्रकांड पंडित रावण ने सत्ता का विस्तार का प्रयास नहीं किया. हालांकि दूसरे रामायण में देवताओं के साथ युद्ध की बात आती है. पर देवताओं के छल-प्रपंच के किस्से कम नहीं हैं.
काश, कागज के रावण फूंकने वाले कम से कम उसके उदत्ता चरित्र से सबक लेते. बहन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हिम्मत दिखाते. उसकी रक्षा करते. परायी नारी के साथ जबरदस्ती नहीं करते. ऐसी सीख नई पीढ़ी को देते. समाज बदलता. मुझे लगता है कि राम चरित्र की असंतुलित शिक्षा का ही प्रभाव है कि 21वीं सदी में भी अनेक महिलाएं जिस पति को देवता मानती है, वहीं उन पर शक करता है, घर से निकालता है. संभवत: यहीं कारण है कि आज धूं-धूं कर जलता हुए रावण के मुंह से चीख निकलने के बजाय हंसी निकलती है. क्योंकि वह जानता है कि जिस लिए उसे जलाया जा रहा है, वह चरित्र उसका नहीं आज के मानव रूपी राम का है. 

