 बाबासाहेब ने कहा था कि हम किसी भी दिशा में मुड़े जातिवाद का राक्षस आगे खड़ा मिलेगा. समाज में व्याप्त जातिवाद आज एक नये रूप-रंग में हमारे सामने आ गया है. जातिवाद ने अपना चेहरा समय के साथ साथ बदल लिया है, अगर गांव देहात को एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाये तो शहरी संस्कृति में यह एक नये रूप में हमारे सामने हैं. लगता है कि सुरसा के मुख की तरह बढते जा रहे बाजारवाद का यह भी अहम हिस्सा बन गया है. देखने में यह साफ-सुथरा नजर आता है पर अंदर से पहले से ज्यादा घिनौना और खतरनाक है. खासकर शिक्षण संस्थाओं में यह सीधे तौर पर नजर नहीं आता परंतु यह अन्दर ही अंदर इनकी गरिमा को खोखला करने पर तुला है. जब से उदारीकरण व निजीकरण के रंग में यह ढला है तब से इसने ब्राह्मणवाद का एक ओर नया चौला पहन लिया है.
अब यह संविधान के तहत दिये प्रतिनिधित्व पर हमला नहीं करता बल्कि उनको ही खत्म करने पर तुला है जो प्रतिनिधित्व लेने के योग्य बन चुके है. यह हमाला अब उन पर काम कर रहा है जो योग्य नहीं है. इनका निशाना अब सीधे योग्यता पर ही है. ना बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. इसकी चिर्ताथता नजर आ रही है. चाहे वह हरियाणा में मिर्चपुर में जिन्दा जलाने वाली लड़की हो, रोहित वेमुला हो, या फ़िर अब लखनऊ विश्वविधायलय से निष्कासित छात्र हो या इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले दलित शिक्षक हो. अब यह ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकना चाहता.
बार-बार छात्रों की प्रतिभा और अध्यापकों की योग्यता पर प्रश्न खड़े कर उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वह इन शिक्षण संस्थाओं से अपने आप मुंह मोड़ ले या फिर उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को अपना ले, उनके साथ खड़े हो जाये. अगर उनकी अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति है तो वह उनके बर्दास्त के बाहर है. यह न सिर्फ़ मेरे साथ एक शिक्षक होने के नाते हो रहा है बल्कि शायद हर उस शिक्षक के साथ है जो अपनी बात रखने का हौंसला रखते है. उन्हें इतना टोर्चर किया जाता है कि वह खुद पर ही संदेह करना शुरु कर देता है कि कहीं ये सब ही तो ठीक नहीं है, शायद मैं ही गलत होंऊ. पर इस ब्राह्मणवाद को समझना ज्यादा कठीन भी नहीं है. यह ब्राह्मणवाद उस कछुए की तरह है जो सामने खतरा देख अपने पैर और गर्दन को सिकोड़ लेता है पर जैसे ही खतरा निकल जाता है यह फिर से अपने पर निकाल लेता है, और आगे बढ़ता है. इसे हम भारतीय प्राचीन समाज के नजरिये से जांच-परख सकते है.
मेरे महाविद्यालय में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जाना माना महाविद्यालय है. शोषण और अपनाम करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है. पिछले वर्ष मैने अपने संस्कृत विभाग की सबजैक्ट सोसायटी की संयोजिका होने के नाते अन्तर्महाविद्यालयीय श्लोकोच्चारण और प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की थी. संयोजिका होने के नाते वितरीत किये जाने वाले सर्टिफ़िकेट पर मेरे हस्तक्षार होने थे और साथ में ही प्रींसिपल जे.पी. मिश्र के होने थे. मैने सभी सर्टिफ़िकेट पर साइन किये थे और उसके बाद प्राचार्य के कक्ष मे साइन करने के लिए मैं खुद लेकर गयी. उन्होने कहा मैं सेमिनार कक्ष में ही साइन करके भेज दूंगा. मैं वापिस प्रोग्राम स्थल जो महाविद्यालय का सेमिनार हाल था आ गयी थी.
प्रोग्राम चल रहा था. मैं सर्टिफ़िकेट मुझ तक पंहुचने का इन्तजार कर रही थी. उस वक्त मेरे ही कुलिग श्री. वत्स माइक पर बोल रहे थे कि अचानक उनका फोन बज उठा. हम सब मंच पर थे और हमारे सामने हमारे संस्कृत के सभी छात्र-छात्राएं. उन्होने वहीं पर खड़े ही खड़े फोन उठा लिया. सबको सुन रहा था कि प्राचार्य क्या बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सर्टिफ़िकेट पर साइन कर दूं. मैं सुनकर दंग रह गयी. क्या मेरे साइन देखकर उन्हे साइन नहीं करनी चाहिए. मेरा अपमान किया उन्होने. जबकि मैं ही नहीं सबने सुना. क्या इज्जत रही मेरी. पल नहीं लगा उनको मेरी औकात दिखाने में. श्री वत्स ने क्या कहा- “कर दिजिए साइन, मैडम ने तो किया हुआ है, उसमें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है” ये माइक से ही बोला जा रहा था. मंच पर विभाग के सभी अध्यापक और बाहर से आये हुए तीन निर्णायक भी थे. मैं आंखे नीची करके बैठी रही. मन तो किया की प्रोग्राम छोड़कर सीधा आफिस में जाऊं और इसका जवाब मांगू. पर वे यही तो चाहते थे कि हम अपनी सारी अनर्जी जलते भुनते निकाल लें और छात्र भी ये समझे कि हम कोई प्रोग्राम ही नहीं करवा सकते. गुस्से में या तश में आकर हम विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी हीं न ले और इनको ये ही मौका मिलता रहे कि हम केवल आरक्षण लेकर नौकरी पा जाते है और तो हमे कुछ आता जाता नहीं. इसलिए मन मसोस कर रह गयी. क्या जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उस पर साइन किसी ओर व्यक्ति से पूछकर वे करते है? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है. फिर क्युं उन्हें मेरे साइन को देखकर भी किसी ओर से पूंछकर साइन किये. इसमें ब्राह्मणवाद काम कर रहा था, जातिवाद का जहर इनके दिमागों में कूट-कूट कर भरा है. ये कभी मौका नहीं छोड़ते कि कोई बिना अपमान के छूट जाये. इसमें खास बात यह भी थी कि वे मेरे ही विभाग के भी थे.
ऐसी बहुत सी घटनायें शिक्षण संस्थाओं में घटती है जो उनके लिए बहुत छोटी-छोटी होती है परन्तु हमारे लिए हमारी अस्मिता का प्रश्न. मुझे एक दिन प्राचार्य ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि अब के एग्जाम वर्ष 2016-2017 में आपको कोरडिनेट करना है. उस समय प्राचार्य के पी.ए. दिनेशा जी भी वहीं थे और हमारे स्टाफ कॉन्सिल के अध्यापक और अध्यापकों के साथ सभी बैठे थे. मैने हां की.
आज दिनांक 9/11/2016 को स्टाफ रूम में प्राचार्य महोदय आये तो मेरी ही एक कुलिग राधिका ने उनसे एग्जाम कोरडिनेट करने के बारे में पूछा तो मैने भी उनकी बात पूरी होने के बाद पूछ लिया कि मुझे अभी तक लैटर नहीं मिला है और न हीं कोई ऑफिस से फोन आया कोरडिनेट करने के लिए. प्राचार्य ने कहा-“ तुम्हे नहीं रखा उसमें”, मैने पूछा क्यूं नहीं रखा तो उन्होंने बताया की तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स है इसलिए नहीं लगाया, सबने मना किया कि तुम्हे न रखा जाये”, मैने पूछा फ्रेंड्स यहां पर किसके नहीं है, सबके हैं, मैं जानती हुं कि आपने क्य़ू किया. आपको क्या लगता है कि मुझे इस तरह रोकने से मैं रुक सकती हूं. वे अच्छी तरह जानते है कि प्रमोशन में कोरडिनेट करने के प्वाईंट मिलते है. कहीं मुझे मिल न जाये इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज मे रहते हुए कोई प्रमोशन पा लूं.
प्रमोशन रोक देने के लिए वे क्या इस स्तर पर जाकर भी सोच सकते हैं, या जो बेगारी हम दलितों से वे एग्जाम में ड्यूटी लगवा लगवाकर करवाते हैं और दूसरे सो कॉल्ड अपर कास्ट के टीचर मौज उड़ाते हैं, इस पर कहीं मेरे एग्जाम कंडक्ट करवाने से तो उनको कोई प्रोब्लम नहीं हो जायेगी, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया. वे और कुछ नहीं बोले. पर मेरी लिए उनकी चुप्पी भी तीर की तह से लग रही थी, पर आज मैने अपने आपको इतना मजबूत कर लिया था कि मेरी आंख से पानी न निकले, वे इसी का इन्तजार कर रहे थे. मैं इस अपमान का घूंट पिये वही सीट पर बैठी रही. ये उन घटनाओं में एक ओर शोषण की घटना थी मेरे लिए, मेरे काम पर, मेरी जिम्मेदारी पर प्रश्नचिहन कि हम अभी भी रिलायबल नहीं है, हम पर विश्वास नहीं किया जा सकता. क्यों?
उतर साफ है, धुंधला नहीं, कोई कोहरा नहीं कि हम दलित अभी इतने उनके विश्वास से पात्र नहीं है कि हम इस जिम्मेदारी को सम्भालने के लिए तैयार हो. नौकरी तो उन्होंने देने दी क्योंकि बाबासाहेब ने आरक्षण के प्रावधान दिये है. संविधान में पर इसे व्यवहारिकता में लाना और असल जामा पहनाना अभी भी ब्राह्मणवाद के हाथ में ही है. इन सब पर सवाल उठना अब भी बाकि है. वे अब हम जैसे जागरुक शिक्षकों को भी हांकना चाहते है पर वे अब नहीं हांक पायेंगे. आज कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि मैने उनके सामने कभी उनके अपनों के सामने आंख में आंख मिलाकर कह दिया कि मैं सब जानती हूं कि आपने ऐसा क्यूं किया. आप मुझे रोक नहीं पायेंगे. कम से कम अपनी बात कहने के इस साहस को मैं उनके मुंह पर लगा तमाचा मानती हुं. ये शिक्षण संस्थाओं के पहले भी इसके दरवाजे हमारे लिए सदियों तक बंद रहे, और आज भी शोषण के गढ़ बन रहे हैं परंतु कब तक वे इसे स्थिर कर पायेंगे.
पिसती रहेगी मानवता, समय की धार से कब तक
अंधियारे को चीरकर, उजाला होगा कब तक.
बाबासाहेब ने कहा था कि हम किसी भी दिशा में मुड़े जातिवाद का राक्षस आगे खड़ा मिलेगा. समाज में व्याप्त जातिवाद आज एक नये रूप-रंग में हमारे सामने आ गया है. जातिवाद ने अपना चेहरा समय के साथ साथ बदल लिया है, अगर गांव देहात को एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाये तो शहरी संस्कृति में यह एक नये रूप में हमारे सामने हैं. लगता है कि सुरसा के मुख की तरह बढते जा रहे बाजारवाद का यह भी अहम हिस्सा बन गया है. देखने में यह साफ-सुथरा नजर आता है पर अंदर से पहले से ज्यादा घिनौना और खतरनाक है. खासकर शिक्षण संस्थाओं में यह सीधे तौर पर नजर नहीं आता परंतु यह अन्दर ही अंदर इनकी गरिमा को खोखला करने पर तुला है. जब से उदारीकरण व निजीकरण के रंग में यह ढला है तब से इसने ब्राह्मणवाद का एक ओर नया चौला पहन लिया है.
अब यह संविधान के तहत दिये प्रतिनिधित्व पर हमला नहीं करता बल्कि उनको ही खत्म करने पर तुला है जो प्रतिनिधित्व लेने के योग्य बन चुके है. यह हमाला अब उन पर काम कर रहा है जो योग्य नहीं है. इनका निशाना अब सीधे योग्यता पर ही है. ना बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. इसकी चिर्ताथता नजर आ रही है. चाहे वह हरियाणा में मिर्चपुर में जिन्दा जलाने वाली लड़की हो, रोहित वेमुला हो, या फ़िर अब लखनऊ विश्वविधायलय से निष्कासित छात्र हो या इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले दलित शिक्षक हो. अब यह ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकना चाहता.
बार-बार छात्रों की प्रतिभा और अध्यापकों की योग्यता पर प्रश्न खड़े कर उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वह इन शिक्षण संस्थाओं से अपने आप मुंह मोड़ ले या फिर उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को अपना ले, उनके साथ खड़े हो जाये. अगर उनकी अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति है तो वह उनके बर्दास्त के बाहर है. यह न सिर्फ़ मेरे साथ एक शिक्षक होने के नाते हो रहा है बल्कि शायद हर उस शिक्षक के साथ है जो अपनी बात रखने का हौंसला रखते है. उन्हें इतना टोर्चर किया जाता है कि वह खुद पर ही संदेह करना शुरु कर देता है कि कहीं ये सब ही तो ठीक नहीं है, शायद मैं ही गलत होंऊ. पर इस ब्राह्मणवाद को समझना ज्यादा कठीन भी नहीं है. यह ब्राह्मणवाद उस कछुए की तरह है जो सामने खतरा देख अपने पैर और गर्दन को सिकोड़ लेता है पर जैसे ही खतरा निकल जाता है यह फिर से अपने पर निकाल लेता है, और आगे बढ़ता है. इसे हम भारतीय प्राचीन समाज के नजरिये से जांच-परख सकते है.
मेरे महाविद्यालय में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जाना माना महाविद्यालय है. शोषण और अपनाम करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है. पिछले वर्ष मैने अपने संस्कृत विभाग की सबजैक्ट सोसायटी की संयोजिका होने के नाते अन्तर्महाविद्यालयीय श्लोकोच्चारण और प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की थी. संयोजिका होने के नाते वितरीत किये जाने वाले सर्टिफ़िकेट पर मेरे हस्तक्षार होने थे और साथ में ही प्रींसिपल जे.पी. मिश्र के होने थे. मैने सभी सर्टिफ़िकेट पर साइन किये थे और उसके बाद प्राचार्य के कक्ष मे साइन करने के लिए मैं खुद लेकर गयी. उन्होने कहा मैं सेमिनार कक्ष में ही साइन करके भेज दूंगा. मैं वापिस प्रोग्राम स्थल जो महाविद्यालय का सेमिनार हाल था आ गयी थी.
प्रोग्राम चल रहा था. मैं सर्टिफ़िकेट मुझ तक पंहुचने का इन्तजार कर रही थी. उस वक्त मेरे ही कुलिग श्री. वत्स माइक पर बोल रहे थे कि अचानक उनका फोन बज उठा. हम सब मंच पर थे और हमारे सामने हमारे संस्कृत के सभी छात्र-छात्राएं. उन्होने वहीं पर खड़े ही खड़े फोन उठा लिया. सबको सुन रहा था कि प्राचार्य क्या बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सर्टिफ़िकेट पर साइन कर दूं. मैं सुनकर दंग रह गयी. क्या मेरे साइन देखकर उन्हे साइन नहीं करनी चाहिए. मेरा अपमान किया उन्होने. जबकि मैं ही नहीं सबने सुना. क्या इज्जत रही मेरी. पल नहीं लगा उनको मेरी औकात दिखाने में. श्री वत्स ने क्या कहा- “कर दिजिए साइन, मैडम ने तो किया हुआ है, उसमें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है” ये माइक से ही बोला जा रहा था. मंच पर विभाग के सभी अध्यापक और बाहर से आये हुए तीन निर्णायक भी थे. मैं आंखे नीची करके बैठी रही. मन तो किया की प्रोग्राम छोड़कर सीधा आफिस में जाऊं और इसका जवाब मांगू. पर वे यही तो चाहते थे कि हम अपनी सारी अनर्जी जलते भुनते निकाल लें और छात्र भी ये समझे कि हम कोई प्रोग्राम ही नहीं करवा सकते. गुस्से में या तश में आकर हम विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी हीं न ले और इनको ये ही मौका मिलता रहे कि हम केवल आरक्षण लेकर नौकरी पा जाते है और तो हमे कुछ आता जाता नहीं. इसलिए मन मसोस कर रह गयी. क्या जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उस पर साइन किसी ओर व्यक्ति से पूछकर वे करते है? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है. फिर क्युं उन्हें मेरे साइन को देखकर भी किसी ओर से पूंछकर साइन किये. इसमें ब्राह्मणवाद काम कर रहा था, जातिवाद का जहर इनके दिमागों में कूट-कूट कर भरा है. ये कभी मौका नहीं छोड़ते कि कोई बिना अपमान के छूट जाये. इसमें खास बात यह भी थी कि वे मेरे ही विभाग के भी थे.
ऐसी बहुत सी घटनायें शिक्षण संस्थाओं में घटती है जो उनके लिए बहुत छोटी-छोटी होती है परन्तु हमारे लिए हमारी अस्मिता का प्रश्न. मुझे एक दिन प्राचार्य ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि अब के एग्जाम वर्ष 2016-2017 में आपको कोरडिनेट करना है. उस समय प्राचार्य के पी.ए. दिनेशा जी भी वहीं थे और हमारे स्टाफ कॉन्सिल के अध्यापक और अध्यापकों के साथ सभी बैठे थे. मैने हां की.
आज दिनांक 9/11/2016 को स्टाफ रूम में प्राचार्य महोदय आये तो मेरी ही एक कुलिग राधिका ने उनसे एग्जाम कोरडिनेट करने के बारे में पूछा तो मैने भी उनकी बात पूरी होने के बाद पूछ लिया कि मुझे अभी तक लैटर नहीं मिला है और न हीं कोई ऑफिस से फोन आया कोरडिनेट करने के लिए. प्राचार्य ने कहा-“ तुम्हे नहीं रखा उसमें”, मैने पूछा क्यूं नहीं रखा तो उन्होंने बताया की तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स है इसलिए नहीं लगाया, सबने मना किया कि तुम्हे न रखा जाये”, मैने पूछा फ्रेंड्स यहां पर किसके नहीं है, सबके हैं, मैं जानती हुं कि आपने क्य़ू किया. आपको क्या लगता है कि मुझे इस तरह रोकने से मैं रुक सकती हूं. वे अच्छी तरह जानते है कि प्रमोशन में कोरडिनेट करने के प्वाईंट मिलते है. कहीं मुझे मिल न जाये इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज मे रहते हुए कोई प्रमोशन पा लूं.
प्रमोशन रोक देने के लिए वे क्या इस स्तर पर जाकर भी सोच सकते हैं, या जो बेगारी हम दलितों से वे एग्जाम में ड्यूटी लगवा लगवाकर करवाते हैं और दूसरे सो कॉल्ड अपर कास्ट के टीचर मौज उड़ाते हैं, इस पर कहीं मेरे एग्जाम कंडक्ट करवाने से तो उनको कोई प्रोब्लम नहीं हो जायेगी, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया. वे और कुछ नहीं बोले. पर मेरी लिए उनकी चुप्पी भी तीर की तह से लग रही थी, पर आज मैने अपने आपको इतना मजबूत कर लिया था कि मेरी आंख से पानी न निकले, वे इसी का इन्तजार कर रहे थे. मैं इस अपमान का घूंट पिये वही सीट पर बैठी रही. ये उन घटनाओं में एक ओर शोषण की घटना थी मेरे लिए, मेरे काम पर, मेरी जिम्मेदारी पर प्रश्नचिहन कि हम अभी भी रिलायबल नहीं है, हम पर विश्वास नहीं किया जा सकता. क्यों?
उतर साफ है, धुंधला नहीं, कोई कोहरा नहीं कि हम दलित अभी इतने उनके विश्वास से पात्र नहीं है कि हम इस जिम्मेदारी को सम्भालने के लिए तैयार हो. नौकरी तो उन्होंने देने दी क्योंकि बाबासाहेब ने आरक्षण के प्रावधान दिये है. संविधान में पर इसे व्यवहारिकता में लाना और असल जामा पहनाना अभी भी ब्राह्मणवाद के हाथ में ही है. इन सब पर सवाल उठना अब भी बाकि है. वे अब हम जैसे जागरुक शिक्षकों को भी हांकना चाहते है पर वे अब नहीं हांक पायेंगे. आज कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि मैने उनके सामने कभी उनके अपनों के सामने आंख में आंख मिलाकर कह दिया कि मैं सब जानती हूं कि आपने ऐसा क्यूं किया. आप मुझे रोक नहीं पायेंगे. कम से कम अपनी बात कहने के इस साहस को मैं उनके मुंह पर लगा तमाचा मानती हुं. ये शिक्षण संस्थाओं के पहले भी इसके दरवाजे हमारे लिए सदियों तक बंद रहे, और आज भी शोषण के गढ़ बन रहे हैं परंतु कब तक वे इसे स्थिर कर पायेंगे.
पिसती रहेगी मानवता, समय की धार से कब तक
अंधियारे को चीरकर, उजाला होगा कब तक.
शोषण के गढ़ हैं भारत के शैक्षिक संस्थान
 बाबासाहेब ने कहा था कि हम किसी भी दिशा में मुड़े जातिवाद का राक्षस आगे खड़ा मिलेगा. समाज में व्याप्त जातिवाद आज एक नये रूप-रंग में हमारे सामने आ गया है. जातिवाद ने अपना चेहरा समय के साथ साथ बदल लिया है, अगर गांव देहात को एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाये तो शहरी संस्कृति में यह एक नये रूप में हमारे सामने हैं. लगता है कि सुरसा के मुख की तरह बढते जा रहे बाजारवाद का यह भी अहम हिस्सा बन गया है. देखने में यह साफ-सुथरा नजर आता है पर अंदर से पहले से ज्यादा घिनौना और खतरनाक है. खासकर शिक्षण संस्थाओं में यह सीधे तौर पर नजर नहीं आता परंतु यह अन्दर ही अंदर इनकी गरिमा को खोखला करने पर तुला है. जब से उदारीकरण व निजीकरण के रंग में यह ढला है तब से इसने ब्राह्मणवाद का एक ओर नया चौला पहन लिया है.
अब यह संविधान के तहत दिये प्रतिनिधित्व पर हमला नहीं करता बल्कि उनको ही खत्म करने पर तुला है जो प्रतिनिधित्व लेने के योग्य बन चुके है. यह हमाला अब उन पर काम कर रहा है जो योग्य नहीं है. इनका निशाना अब सीधे योग्यता पर ही है. ना बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. इसकी चिर्ताथता नजर आ रही है. चाहे वह हरियाणा में मिर्चपुर में जिन्दा जलाने वाली लड़की हो, रोहित वेमुला हो, या फ़िर अब लखनऊ विश्वविधायलय से निष्कासित छात्र हो या इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले दलित शिक्षक हो. अब यह ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकना चाहता.
बार-बार छात्रों की प्रतिभा और अध्यापकों की योग्यता पर प्रश्न खड़े कर उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वह इन शिक्षण संस्थाओं से अपने आप मुंह मोड़ ले या फिर उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को अपना ले, उनके साथ खड़े हो जाये. अगर उनकी अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति है तो वह उनके बर्दास्त के बाहर है. यह न सिर्फ़ मेरे साथ एक शिक्षक होने के नाते हो रहा है बल्कि शायद हर उस शिक्षक के साथ है जो अपनी बात रखने का हौंसला रखते है. उन्हें इतना टोर्चर किया जाता है कि वह खुद पर ही संदेह करना शुरु कर देता है कि कहीं ये सब ही तो ठीक नहीं है, शायद मैं ही गलत होंऊ. पर इस ब्राह्मणवाद को समझना ज्यादा कठीन भी नहीं है. यह ब्राह्मणवाद उस कछुए की तरह है जो सामने खतरा देख अपने पैर और गर्दन को सिकोड़ लेता है पर जैसे ही खतरा निकल जाता है यह फिर से अपने पर निकाल लेता है, और आगे बढ़ता है. इसे हम भारतीय प्राचीन समाज के नजरिये से जांच-परख सकते है.
मेरे महाविद्यालय में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जाना माना महाविद्यालय है. शोषण और अपनाम करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है. पिछले वर्ष मैने अपने संस्कृत विभाग की सबजैक्ट सोसायटी की संयोजिका होने के नाते अन्तर्महाविद्यालयीय श्लोकोच्चारण और प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की थी. संयोजिका होने के नाते वितरीत किये जाने वाले सर्टिफ़िकेट पर मेरे हस्तक्षार होने थे और साथ में ही प्रींसिपल जे.पी. मिश्र के होने थे. मैने सभी सर्टिफ़िकेट पर साइन किये थे और उसके बाद प्राचार्य के कक्ष मे साइन करने के लिए मैं खुद लेकर गयी. उन्होने कहा मैं सेमिनार कक्ष में ही साइन करके भेज दूंगा. मैं वापिस प्रोग्राम स्थल जो महाविद्यालय का सेमिनार हाल था आ गयी थी.
प्रोग्राम चल रहा था. मैं सर्टिफ़िकेट मुझ तक पंहुचने का इन्तजार कर रही थी. उस वक्त मेरे ही कुलिग श्री. वत्स माइक पर बोल रहे थे कि अचानक उनका फोन बज उठा. हम सब मंच पर थे और हमारे सामने हमारे संस्कृत के सभी छात्र-छात्राएं. उन्होने वहीं पर खड़े ही खड़े फोन उठा लिया. सबको सुन रहा था कि प्राचार्य क्या बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सर्टिफ़िकेट पर साइन कर दूं. मैं सुनकर दंग रह गयी. क्या मेरे साइन देखकर उन्हे साइन नहीं करनी चाहिए. मेरा अपमान किया उन्होने. जबकि मैं ही नहीं सबने सुना. क्या इज्जत रही मेरी. पल नहीं लगा उनको मेरी औकात दिखाने में. श्री वत्स ने क्या कहा- “कर दिजिए साइन, मैडम ने तो किया हुआ है, उसमें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है” ये माइक से ही बोला जा रहा था. मंच पर विभाग के सभी अध्यापक और बाहर से आये हुए तीन निर्णायक भी थे. मैं आंखे नीची करके बैठी रही. मन तो किया की प्रोग्राम छोड़कर सीधा आफिस में जाऊं और इसका जवाब मांगू. पर वे यही तो चाहते थे कि हम अपनी सारी अनर्जी जलते भुनते निकाल लें और छात्र भी ये समझे कि हम कोई प्रोग्राम ही नहीं करवा सकते. गुस्से में या तश में आकर हम विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी हीं न ले और इनको ये ही मौका मिलता रहे कि हम केवल आरक्षण लेकर नौकरी पा जाते है और तो हमे कुछ आता जाता नहीं. इसलिए मन मसोस कर रह गयी. क्या जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उस पर साइन किसी ओर व्यक्ति से पूछकर वे करते है? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है. फिर क्युं उन्हें मेरे साइन को देखकर भी किसी ओर से पूंछकर साइन किये. इसमें ब्राह्मणवाद काम कर रहा था, जातिवाद का जहर इनके दिमागों में कूट-कूट कर भरा है. ये कभी मौका नहीं छोड़ते कि कोई बिना अपमान के छूट जाये. इसमें खास बात यह भी थी कि वे मेरे ही विभाग के भी थे.
ऐसी बहुत सी घटनायें शिक्षण संस्थाओं में घटती है जो उनके लिए बहुत छोटी-छोटी होती है परन्तु हमारे लिए हमारी अस्मिता का प्रश्न. मुझे एक दिन प्राचार्य ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि अब के एग्जाम वर्ष 2016-2017 में आपको कोरडिनेट करना है. उस समय प्राचार्य के पी.ए. दिनेशा जी भी वहीं थे और हमारे स्टाफ कॉन्सिल के अध्यापक और अध्यापकों के साथ सभी बैठे थे. मैने हां की.
आज दिनांक 9/11/2016 को स्टाफ रूम में प्राचार्य महोदय आये तो मेरी ही एक कुलिग राधिका ने उनसे एग्जाम कोरडिनेट करने के बारे में पूछा तो मैने भी उनकी बात पूरी होने के बाद पूछ लिया कि मुझे अभी तक लैटर नहीं मिला है और न हीं कोई ऑफिस से फोन आया कोरडिनेट करने के लिए. प्राचार्य ने कहा-“ तुम्हे नहीं रखा उसमें”, मैने पूछा क्यूं नहीं रखा तो उन्होंने बताया की तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स है इसलिए नहीं लगाया, सबने मना किया कि तुम्हे न रखा जाये”, मैने पूछा फ्रेंड्स यहां पर किसके नहीं है, सबके हैं, मैं जानती हुं कि आपने क्य़ू किया. आपको क्या लगता है कि मुझे इस तरह रोकने से मैं रुक सकती हूं. वे अच्छी तरह जानते है कि प्रमोशन में कोरडिनेट करने के प्वाईंट मिलते है. कहीं मुझे मिल न जाये इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज मे रहते हुए कोई प्रमोशन पा लूं.
प्रमोशन रोक देने के लिए वे क्या इस स्तर पर जाकर भी सोच सकते हैं, या जो बेगारी हम दलितों से वे एग्जाम में ड्यूटी लगवा लगवाकर करवाते हैं और दूसरे सो कॉल्ड अपर कास्ट के टीचर मौज उड़ाते हैं, इस पर कहीं मेरे एग्जाम कंडक्ट करवाने से तो उनको कोई प्रोब्लम नहीं हो जायेगी, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया. वे और कुछ नहीं बोले. पर मेरी लिए उनकी चुप्पी भी तीर की तह से लग रही थी, पर आज मैने अपने आपको इतना मजबूत कर लिया था कि मेरी आंख से पानी न निकले, वे इसी का इन्तजार कर रहे थे. मैं इस अपमान का घूंट पिये वही सीट पर बैठी रही. ये उन घटनाओं में एक ओर शोषण की घटना थी मेरे लिए, मेरे काम पर, मेरी जिम्मेदारी पर प्रश्नचिहन कि हम अभी भी रिलायबल नहीं है, हम पर विश्वास नहीं किया जा सकता. क्यों?
उतर साफ है, धुंधला नहीं, कोई कोहरा नहीं कि हम दलित अभी इतने उनके विश्वास से पात्र नहीं है कि हम इस जिम्मेदारी को सम्भालने के लिए तैयार हो. नौकरी तो उन्होंने देने दी क्योंकि बाबासाहेब ने आरक्षण के प्रावधान दिये है. संविधान में पर इसे व्यवहारिकता में लाना और असल जामा पहनाना अभी भी ब्राह्मणवाद के हाथ में ही है. इन सब पर सवाल उठना अब भी बाकि है. वे अब हम जैसे जागरुक शिक्षकों को भी हांकना चाहते है पर वे अब नहीं हांक पायेंगे. आज कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि मैने उनके सामने कभी उनके अपनों के सामने आंख में आंख मिलाकर कह दिया कि मैं सब जानती हूं कि आपने ऐसा क्यूं किया. आप मुझे रोक नहीं पायेंगे. कम से कम अपनी बात कहने के इस साहस को मैं उनके मुंह पर लगा तमाचा मानती हुं. ये शिक्षण संस्थाओं के पहले भी इसके दरवाजे हमारे लिए सदियों तक बंद रहे, और आज भी शोषण के गढ़ बन रहे हैं परंतु कब तक वे इसे स्थिर कर पायेंगे.
पिसती रहेगी मानवता, समय की धार से कब तक
अंधियारे को चीरकर, उजाला होगा कब तक.
बाबासाहेब ने कहा था कि हम किसी भी दिशा में मुड़े जातिवाद का राक्षस आगे खड़ा मिलेगा. समाज में व्याप्त जातिवाद आज एक नये रूप-रंग में हमारे सामने आ गया है. जातिवाद ने अपना चेहरा समय के साथ साथ बदल लिया है, अगर गांव देहात को एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाये तो शहरी संस्कृति में यह एक नये रूप में हमारे सामने हैं. लगता है कि सुरसा के मुख की तरह बढते जा रहे बाजारवाद का यह भी अहम हिस्सा बन गया है. देखने में यह साफ-सुथरा नजर आता है पर अंदर से पहले से ज्यादा घिनौना और खतरनाक है. खासकर शिक्षण संस्थाओं में यह सीधे तौर पर नजर नहीं आता परंतु यह अन्दर ही अंदर इनकी गरिमा को खोखला करने पर तुला है. जब से उदारीकरण व निजीकरण के रंग में यह ढला है तब से इसने ब्राह्मणवाद का एक ओर नया चौला पहन लिया है.
अब यह संविधान के तहत दिये प्रतिनिधित्व पर हमला नहीं करता बल्कि उनको ही खत्म करने पर तुला है जो प्रतिनिधित्व लेने के योग्य बन चुके है. यह हमाला अब उन पर काम कर रहा है जो योग्य नहीं है. इनका निशाना अब सीधे योग्यता पर ही है. ना बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. इसकी चिर्ताथता नजर आ रही है. चाहे वह हरियाणा में मिर्चपुर में जिन्दा जलाने वाली लड़की हो, रोहित वेमुला हो, या फ़िर अब लखनऊ विश्वविधायलय से निष्कासित छात्र हो या इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले दलित शिक्षक हो. अब यह ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकना चाहता.
बार-बार छात्रों की प्रतिभा और अध्यापकों की योग्यता पर प्रश्न खड़े कर उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वह इन शिक्षण संस्थाओं से अपने आप मुंह मोड़ ले या फिर उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को अपना ले, उनके साथ खड़े हो जाये. अगर उनकी अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति है तो वह उनके बर्दास्त के बाहर है. यह न सिर्फ़ मेरे साथ एक शिक्षक होने के नाते हो रहा है बल्कि शायद हर उस शिक्षक के साथ है जो अपनी बात रखने का हौंसला रखते है. उन्हें इतना टोर्चर किया जाता है कि वह खुद पर ही संदेह करना शुरु कर देता है कि कहीं ये सब ही तो ठीक नहीं है, शायद मैं ही गलत होंऊ. पर इस ब्राह्मणवाद को समझना ज्यादा कठीन भी नहीं है. यह ब्राह्मणवाद उस कछुए की तरह है जो सामने खतरा देख अपने पैर और गर्दन को सिकोड़ लेता है पर जैसे ही खतरा निकल जाता है यह फिर से अपने पर निकाल लेता है, और आगे बढ़ता है. इसे हम भारतीय प्राचीन समाज के नजरिये से जांच-परख सकते है.
मेरे महाविद्यालय में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जाना माना महाविद्यालय है. शोषण और अपनाम करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है. पिछले वर्ष मैने अपने संस्कृत विभाग की सबजैक्ट सोसायटी की संयोजिका होने के नाते अन्तर्महाविद्यालयीय श्लोकोच्चारण और प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की थी. संयोजिका होने के नाते वितरीत किये जाने वाले सर्टिफ़िकेट पर मेरे हस्तक्षार होने थे और साथ में ही प्रींसिपल जे.पी. मिश्र के होने थे. मैने सभी सर्टिफ़िकेट पर साइन किये थे और उसके बाद प्राचार्य के कक्ष मे साइन करने के लिए मैं खुद लेकर गयी. उन्होने कहा मैं सेमिनार कक्ष में ही साइन करके भेज दूंगा. मैं वापिस प्रोग्राम स्थल जो महाविद्यालय का सेमिनार हाल था आ गयी थी.
प्रोग्राम चल रहा था. मैं सर्टिफ़िकेट मुझ तक पंहुचने का इन्तजार कर रही थी. उस वक्त मेरे ही कुलिग श्री. वत्स माइक पर बोल रहे थे कि अचानक उनका फोन बज उठा. हम सब मंच पर थे और हमारे सामने हमारे संस्कृत के सभी छात्र-छात्राएं. उन्होने वहीं पर खड़े ही खड़े फोन उठा लिया. सबको सुन रहा था कि प्राचार्य क्या बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सर्टिफ़िकेट पर साइन कर दूं. मैं सुनकर दंग रह गयी. क्या मेरे साइन देखकर उन्हे साइन नहीं करनी चाहिए. मेरा अपमान किया उन्होने. जबकि मैं ही नहीं सबने सुना. क्या इज्जत रही मेरी. पल नहीं लगा उनको मेरी औकात दिखाने में. श्री वत्स ने क्या कहा- “कर दिजिए साइन, मैडम ने तो किया हुआ है, उसमें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है” ये माइक से ही बोला जा रहा था. मंच पर विभाग के सभी अध्यापक और बाहर से आये हुए तीन निर्णायक भी थे. मैं आंखे नीची करके बैठी रही. मन तो किया की प्रोग्राम छोड़कर सीधा आफिस में जाऊं और इसका जवाब मांगू. पर वे यही तो चाहते थे कि हम अपनी सारी अनर्जी जलते भुनते निकाल लें और छात्र भी ये समझे कि हम कोई प्रोग्राम ही नहीं करवा सकते. गुस्से में या तश में आकर हम विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी हीं न ले और इनको ये ही मौका मिलता रहे कि हम केवल आरक्षण लेकर नौकरी पा जाते है और तो हमे कुछ आता जाता नहीं. इसलिए मन मसोस कर रह गयी. क्या जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उस पर साइन किसी ओर व्यक्ति से पूछकर वे करते है? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है. फिर क्युं उन्हें मेरे साइन को देखकर भी किसी ओर से पूंछकर साइन किये. इसमें ब्राह्मणवाद काम कर रहा था, जातिवाद का जहर इनके दिमागों में कूट-कूट कर भरा है. ये कभी मौका नहीं छोड़ते कि कोई बिना अपमान के छूट जाये. इसमें खास बात यह भी थी कि वे मेरे ही विभाग के भी थे.
ऐसी बहुत सी घटनायें शिक्षण संस्थाओं में घटती है जो उनके लिए बहुत छोटी-छोटी होती है परन्तु हमारे लिए हमारी अस्मिता का प्रश्न. मुझे एक दिन प्राचार्य ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि अब के एग्जाम वर्ष 2016-2017 में आपको कोरडिनेट करना है. उस समय प्राचार्य के पी.ए. दिनेशा जी भी वहीं थे और हमारे स्टाफ कॉन्सिल के अध्यापक और अध्यापकों के साथ सभी बैठे थे. मैने हां की.
आज दिनांक 9/11/2016 को स्टाफ रूम में प्राचार्य महोदय आये तो मेरी ही एक कुलिग राधिका ने उनसे एग्जाम कोरडिनेट करने के बारे में पूछा तो मैने भी उनकी बात पूरी होने के बाद पूछ लिया कि मुझे अभी तक लैटर नहीं मिला है और न हीं कोई ऑफिस से फोन आया कोरडिनेट करने के लिए. प्राचार्य ने कहा-“ तुम्हे नहीं रखा उसमें”, मैने पूछा क्यूं नहीं रखा तो उन्होंने बताया की तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स है इसलिए नहीं लगाया, सबने मना किया कि तुम्हे न रखा जाये”, मैने पूछा फ्रेंड्स यहां पर किसके नहीं है, सबके हैं, मैं जानती हुं कि आपने क्य़ू किया. आपको क्या लगता है कि मुझे इस तरह रोकने से मैं रुक सकती हूं. वे अच्छी तरह जानते है कि प्रमोशन में कोरडिनेट करने के प्वाईंट मिलते है. कहीं मुझे मिल न जाये इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज मे रहते हुए कोई प्रमोशन पा लूं.
प्रमोशन रोक देने के लिए वे क्या इस स्तर पर जाकर भी सोच सकते हैं, या जो बेगारी हम दलितों से वे एग्जाम में ड्यूटी लगवा लगवाकर करवाते हैं और दूसरे सो कॉल्ड अपर कास्ट के टीचर मौज उड़ाते हैं, इस पर कहीं मेरे एग्जाम कंडक्ट करवाने से तो उनको कोई प्रोब्लम नहीं हो जायेगी, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया. वे और कुछ नहीं बोले. पर मेरी लिए उनकी चुप्पी भी तीर की तह से लग रही थी, पर आज मैने अपने आपको इतना मजबूत कर लिया था कि मेरी आंख से पानी न निकले, वे इसी का इन्तजार कर रहे थे. मैं इस अपमान का घूंट पिये वही सीट पर बैठी रही. ये उन घटनाओं में एक ओर शोषण की घटना थी मेरे लिए, मेरे काम पर, मेरी जिम्मेदारी पर प्रश्नचिहन कि हम अभी भी रिलायबल नहीं है, हम पर विश्वास नहीं किया जा सकता. क्यों?
उतर साफ है, धुंधला नहीं, कोई कोहरा नहीं कि हम दलित अभी इतने उनके विश्वास से पात्र नहीं है कि हम इस जिम्मेदारी को सम्भालने के लिए तैयार हो. नौकरी तो उन्होंने देने दी क्योंकि बाबासाहेब ने आरक्षण के प्रावधान दिये है. संविधान में पर इसे व्यवहारिकता में लाना और असल जामा पहनाना अभी भी ब्राह्मणवाद के हाथ में ही है. इन सब पर सवाल उठना अब भी बाकि है. वे अब हम जैसे जागरुक शिक्षकों को भी हांकना चाहते है पर वे अब नहीं हांक पायेंगे. आज कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि मैने उनके सामने कभी उनके अपनों के सामने आंख में आंख मिलाकर कह दिया कि मैं सब जानती हूं कि आपने ऐसा क्यूं किया. आप मुझे रोक नहीं पायेंगे. कम से कम अपनी बात कहने के इस साहस को मैं उनके मुंह पर लगा तमाचा मानती हुं. ये शिक्षण संस्थाओं के पहले भी इसके दरवाजे हमारे लिए सदियों तक बंद रहे, और आज भी शोषण के गढ़ बन रहे हैं परंतु कब तक वे इसे स्थिर कर पायेंगे.
पिसती रहेगी मानवता, समय की धार से कब तक
अंधियारे को चीरकर, उजाला होगा कब तक.
डॉ. अम्बेडकर की राजनीति
 डॉ. अम्बेडकर दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दलितों के लिए राजनैतिक अधिकारों की लडाई लड़ी थी. उन्होंने ही भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में लंदन में 1930-32 में हुए गोलमेज़ सम्मलेन में दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था. 1932 में जब “कम्युनल अवार्ड” के अंतर्गत दलितों को भी अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग मताधिकार मिला तो गांधीजी ने उसके विरोध में यह कहते हुए कि इससे हिन्दू समाज टूट जायेगा, आमरण अनशन की धमकी दे डाली. जबकि उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी. अंत में अनुचित दबाव में मजबूर होकर डॉ. आम्बेडकर को गांधीजी की जान बचाने के लिए “पूना पैकट” करना पड़ा और मजबूरन दलितों के राजनैतिक स्वतंत्रता के अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्वीकार करनी पड़ीं.
गोलमेज़ कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार नया कानून “गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट” 1936 में लागू हुआ. इसके अंतर्गत 1937 में पहला चुनाव कराने की घोषणा की गयी. इस चुनाव में भाग लेने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (स्वतंत्र मजदूर पार्टी) की स्थापना की और बम्बई प्रेज़ीडैन्सी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीतीं. इसके बाद उन्होंने 19 जुलाई, 1942 को आल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन बनायी. इस पार्टी से उन्होंने 1946 और 1952 में चुनाव लड़े परन्तु इसमें पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव के कारण उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली. फलस्वरूप 1952 और 1954 के चुनाव में डॉ. अम्बेडकर स्वयं हार गए. अंत में उन्होंने 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में आल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को भंग करके रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआई) नाम से नयी पार्टी बनाने की घोषणा की. इसके लिए उन्होंने इस पार्टी का संविधान भी बनाया. वास्तव में यह पार्टी उनके परिनिर्वाण के बाद 3 अक्तूबर, 1957 को अस्तित्व में आई. इस विवरण के अनुसार बाबासाहेब ने अपने जीवन काल में तीन राजनैतिक पार्टियां बनायीं. इनमें से वर्तमान में आरपीआई अलग-अलग गुटों के रूप में मौजूद है. वर्तमान संदर्भ में यह देखना ज़रूरी है कि बाबासाहेब ने जिन राजनैतिक पार्टियों के माध्यम से राजनीति की क्या वह जाति की राजनीति थी या विभिन्न वर्गों के मुद्दों की राजनीति थी. इसके लिए उनके द्वारा स्थापित पार्टियों के एजेंडा का विश्लेषण ज़रूरी है.
सबसे पहले बाबासाहेब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी को देखें. डॉ. अम्बेडकर ने अपने बयान में पार्टी के बनाने के कारणों और उसके काम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था- “’इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज पार्टियों को सम्प्रदाय के आधार पर संगठित करने का समय नहीं है, मैंने अपने मित्रों की इच्छाओं से सहमति रखते हुए पार्टी का नाम तथा इसके प्रोग्राम को विशाल बना दिया है ताकि अन्य वर्ग के लोगों के साथ राजनीतिक सहयोग संभव हो सके. पार्टी का मुख्य केंद्रबिंदु तो दलित जातियों के 15 सदस्य ही रहेंगे परन्तु अन्य वर्ग के लोग भी पार्टी में शामिल हो सकेंगे.’” पार्टी के घोषणापत्र में भूमिहीन, गरीब किसानों और पट्टेदारों और मजदूरों की ज़रूरतों और समस्याओं का निवारण, पुराने उद्योगों की पुनर्स्थापना और नए उद्योगों की स्थापना, छोटी जोतों की चकबंदी, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, भूमि के पट्टेदारों का ज़मीदारों द्वारा शोषण और बेदखली, औद्योगिक मजदूरों के संरक्षण के लिए कानून, सभी प्रकार की कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावाद को दण्डित करने, दान में मिले पैसे से शिक्षा प्रसार, गांव के नजरिये को आधुनिक बनाने के लिए सफाई और मकानों का नियोजन और गांव के लिए हाल, पुस्तकालय और सिनेमा घर आदि का प्रावधान करना था. पार्टी ने मुख्यतया किसानों और गरीब मजदूरों के कल्याण पर बल दिया था. पार्टी की कोशिश लोगों को लोकतंत्र के तरीकों से शिक्षित करना, उनके सामने सही विचारधारा रखना और उन्हें कानून द्वारा राजनीतिक कार्रवाही के लिए संगठित करना आदि था. इससे स्पष्ट है कि इस पार्टी की राजनीति जातिवादी न होकर वर्ग और मुद्दा आधारित थी और इसके केंद्र में मुख्यतया दलित थे. यह पार्टी बम्बई विधान सभा में सत्ताधारी कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी. इस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत जनोपयोगी कानून बनवाये थे. इस पार्टी के विरोध के कारण ही फैक्टरियों में हड़ताल पर रोक लगाने संबंधी औद्योगिक विवाद बिल पास नहीं हो सका था.
अब बाबासाहेब द्वारा 1942 में स्थापित आल इंडिया शिडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उद्देश्य और एजेंडा को देखा जाये. डॉ. अम्बेडकर ने इसे सत्ताधारी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात कही थी. पार्टी के मैनिफिस्टो में कुछ मुख्य मुद्दे थे. मसलन, सभी भारतीय समानता के अधिकारी हैं, सभी भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता की पक्षधरता, सभी भारतीयों को अभाव और भय से मुक्त रखना राज्य की जिम्मेवारी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संरक्षण, आदमी का आदमी द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा तथा राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति और सरकार की संसदीय व्यवस्था का संरक्षण, आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत बीमा का राष्ट्रीयकरण और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना और नशेबंदी का निषेध था. यद्यपि यह पार्टी पूना पैक्ट के कारण शक्तिशाली कांग्रेस के सामने चुनाव में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परन्तु पार्टी के एजेंडे और जन आंदोलन जैसे भूमि आन्दोलन आदि के कारण अछूत एक राजनीतिक झंडे के तले जमा होने लगे जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा. फेडरेशन के प्रोग्राम से स्पष्ट है कि यदपि इस पार्टी के केंद्र में दलित थे परन्तु पार्टी जाति की राजनीति की जगह मुद्दों पर राजनीति करती थी और इसका फलक व्यापक था.
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबासाहेब ने बदलती परिस्थितियों और लोगों की ज़रुरत को ध्यान में रख कर एक नयी राजनीतिक पार्टी “रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया” की स्थापना की घोषणा 14 अक्तूबर, 1956 को की थी और इसका संविधान भी उन्होंने ही बनाया था. इस पार्टी को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पार्टी बनाना था जो संविधान में किये गए वादों के अनुसार हो और उन्हें पूरा करना उसका उद्देश्य हो. वे इसे केवल अछूतों की पार्टी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि एक जाति या वर्ग के नाम पर बनायी गयी पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती. वह केवल दबाव डालने वाला ग्रुप ही बन सकती है. आरपीआई की स्थापना के पीछे कुछ मुख्य ध्येय था. जैसे-
(1) समाज व्यवस्था से विषमतायें हटाई जाएं ताकि कोई विशेषाधिकार प्राप्त तथा वंचित वर्ग न रहे.
(2) दो पार्टी सिस्टम हो एक सत्ता में दूसरा विरोधी पक्ष
(3) कानून के सामने समानता और सबके लिए एक जैसा कानून हो
(4) समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना
(5) अल्पसंख्यक लोगों के साथ सामान व्यवहार
(6) मानवता की भावना जिसका भारतीय समाज में अभाव रहा है
पार्टी के संविधान की प्रस्तावना में पार्टी का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता” को प्राप्त करना था. पार्टी का कार्यक्रम बहुत व्यापक था. पार्टी की स्थापना के पीछे बाबासाहेब का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब मुस्लिम, गरीब ईसाई, गरीब तथा निचली जाति के सिक्ख तथा कमज़ोर वर्ग के अछूत, पिछड़ी जातियों के लोग, आदिम जातियों के लोग, शोषण का अंत, न्याय और प्रगति चाहने वाले सभी लोग एक झंडे के तले संगठित हो सकें और पूंजीपतियों के मुकाबले में खड़े होकर संविधान तथा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें. (दलित राजनीति और संगठन – भगवान दास)
आरपीआई की विधिवत स्थापना बाबासाहेब के परिनिर्वाण के बाद 1957 में हुई और पार्टी ने नए एजेंडे के साथ 1957 व 1962 का चुनाव लड़ा. पार्टी को महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी सफलता मिली. शुरू में पार्टी ने ज़मीन के बंटवारे, नौकरियों में आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी, दलितों से बौद्ध बने लोगों लिए आरक्षण आदि के लिए संघर्ष किया. पार्टी में मुसलमान, सिक्ख और जैन आदि धर्मों के लोग शामिल हुए. उनमें पंजाब के जनरल राजिंदर सिंह स्पैरो, दिल्ली में डॉ. अब्बास मलिक, उत्तर प्रदेश में राहत मोलाई, डॉ. छेदी लाल साथी, नासिर अहमद, बंगाल में श्री एस. एच. घोष आदि प्रसिद्ध व्यक्ति और कार्यकर्ता हुए. 1964 में 6 दिसंबर से फरवरी 1965 तक पार्टी ने स्वतंत्र भारत में ज़मीन के मुद्दे को लेकर पहला जेल भरो आन्दोलन चलाया जिसमें तीन लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जेल गए. सरकार को मजबूर होकर भूमि आवंटन और कुछ अन्य मांगें माननी पड़ीं.
इस दौर में आरपीआई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मज़बूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई. परन्तु 1962 के बाद यह पार्टी टूटने लगी. इसका मुख्य कारण था कि इस पार्टी से उस समय की सब से मज़बूत राजनैतिक पार्टी कांग्रेस को महाराष्ट्र में खतरा पैदा हो रहा था. इस पार्टी की एक बड़ी कमजोरी थी कि इसकी सदस्यता केवल महारों तक ही सीमित थी. कांग्रेस के नेताओं ने इस पार्टी के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठा कर पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी. सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता दादा साहेब गायकवाड़ को पटाया और उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना दिया. इस पर पार्टी दो गुटों में बंट गयी. गायकवाड का एक गुट कांग्रेस के साथ था जबकि दूसरा बी.डी.खोब्रागडे गुट विरोध में था. इसके बाद अलग नेताओं के नाम पर अलग गुट बनते गए और वर्तमान में यह कई गुटों में बंट कर बेअसर हो चुकी है. इन गुटों के नेता रिपब्लिकन नाम का इस्तेमाल तो करते हैं परन्तु उनका इस पार्टी के मूल एजेंडे से कुछ भी लेना देना नहीं है. वे अपने-अपने फायदे के लिए अलग पार्टियों से समझौते करते हैं और यदा-कदा लाभ भी उठाते हैं.
एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
डॉ. अम्बेडकर दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दलितों के लिए राजनैतिक अधिकारों की लडाई लड़ी थी. उन्होंने ही भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में लंदन में 1930-32 में हुए गोलमेज़ सम्मलेन में दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था. 1932 में जब “कम्युनल अवार्ड” के अंतर्गत दलितों को भी अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग मताधिकार मिला तो गांधीजी ने उसके विरोध में यह कहते हुए कि इससे हिन्दू समाज टूट जायेगा, आमरण अनशन की धमकी दे डाली. जबकि उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी. अंत में अनुचित दबाव में मजबूर होकर डॉ. आम्बेडकर को गांधीजी की जान बचाने के लिए “पूना पैकट” करना पड़ा और मजबूरन दलितों के राजनैतिक स्वतंत्रता के अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्वीकार करनी पड़ीं.
गोलमेज़ कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार नया कानून “गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट” 1936 में लागू हुआ. इसके अंतर्गत 1937 में पहला चुनाव कराने की घोषणा की गयी. इस चुनाव में भाग लेने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (स्वतंत्र मजदूर पार्टी) की स्थापना की और बम्बई प्रेज़ीडैन्सी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीतीं. इसके बाद उन्होंने 19 जुलाई, 1942 को आल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन बनायी. इस पार्टी से उन्होंने 1946 और 1952 में चुनाव लड़े परन्तु इसमें पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव के कारण उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली. फलस्वरूप 1952 और 1954 के चुनाव में डॉ. अम्बेडकर स्वयं हार गए. अंत में उन्होंने 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में आल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को भंग करके रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआई) नाम से नयी पार्टी बनाने की घोषणा की. इसके लिए उन्होंने इस पार्टी का संविधान भी बनाया. वास्तव में यह पार्टी उनके परिनिर्वाण के बाद 3 अक्तूबर, 1957 को अस्तित्व में आई. इस विवरण के अनुसार बाबासाहेब ने अपने जीवन काल में तीन राजनैतिक पार्टियां बनायीं. इनमें से वर्तमान में आरपीआई अलग-अलग गुटों के रूप में मौजूद है. वर्तमान संदर्भ में यह देखना ज़रूरी है कि बाबासाहेब ने जिन राजनैतिक पार्टियों के माध्यम से राजनीति की क्या वह जाति की राजनीति थी या विभिन्न वर्गों के मुद्दों की राजनीति थी. इसके लिए उनके द्वारा स्थापित पार्टियों के एजेंडा का विश्लेषण ज़रूरी है.
सबसे पहले बाबासाहेब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी को देखें. डॉ. अम्बेडकर ने अपने बयान में पार्टी के बनाने के कारणों और उसके काम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था- “’इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज पार्टियों को सम्प्रदाय के आधार पर संगठित करने का समय नहीं है, मैंने अपने मित्रों की इच्छाओं से सहमति रखते हुए पार्टी का नाम तथा इसके प्रोग्राम को विशाल बना दिया है ताकि अन्य वर्ग के लोगों के साथ राजनीतिक सहयोग संभव हो सके. पार्टी का मुख्य केंद्रबिंदु तो दलित जातियों के 15 सदस्य ही रहेंगे परन्तु अन्य वर्ग के लोग भी पार्टी में शामिल हो सकेंगे.’” पार्टी के घोषणापत्र में भूमिहीन, गरीब किसानों और पट्टेदारों और मजदूरों की ज़रूरतों और समस्याओं का निवारण, पुराने उद्योगों की पुनर्स्थापना और नए उद्योगों की स्थापना, छोटी जोतों की चकबंदी, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, भूमि के पट्टेदारों का ज़मीदारों द्वारा शोषण और बेदखली, औद्योगिक मजदूरों के संरक्षण के लिए कानून, सभी प्रकार की कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावाद को दण्डित करने, दान में मिले पैसे से शिक्षा प्रसार, गांव के नजरिये को आधुनिक बनाने के लिए सफाई और मकानों का नियोजन और गांव के लिए हाल, पुस्तकालय और सिनेमा घर आदि का प्रावधान करना था. पार्टी ने मुख्यतया किसानों और गरीब मजदूरों के कल्याण पर बल दिया था. पार्टी की कोशिश लोगों को लोकतंत्र के तरीकों से शिक्षित करना, उनके सामने सही विचारधारा रखना और उन्हें कानून द्वारा राजनीतिक कार्रवाही के लिए संगठित करना आदि था. इससे स्पष्ट है कि इस पार्टी की राजनीति जातिवादी न होकर वर्ग और मुद्दा आधारित थी और इसके केंद्र में मुख्यतया दलित थे. यह पार्टी बम्बई विधान सभा में सत्ताधारी कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी. इस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत जनोपयोगी कानून बनवाये थे. इस पार्टी के विरोध के कारण ही फैक्टरियों में हड़ताल पर रोक लगाने संबंधी औद्योगिक विवाद बिल पास नहीं हो सका था.
अब बाबासाहेब द्वारा 1942 में स्थापित आल इंडिया शिडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उद्देश्य और एजेंडा को देखा जाये. डॉ. अम्बेडकर ने इसे सत्ताधारी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात कही थी. पार्टी के मैनिफिस्टो में कुछ मुख्य मुद्दे थे. मसलन, सभी भारतीय समानता के अधिकारी हैं, सभी भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता की पक्षधरता, सभी भारतीयों को अभाव और भय से मुक्त रखना राज्य की जिम्मेवारी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संरक्षण, आदमी का आदमी द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा तथा राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति और सरकार की संसदीय व्यवस्था का संरक्षण, आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत बीमा का राष्ट्रीयकरण और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना और नशेबंदी का निषेध था. यद्यपि यह पार्टी पूना पैक्ट के कारण शक्तिशाली कांग्रेस के सामने चुनाव में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परन्तु पार्टी के एजेंडे और जन आंदोलन जैसे भूमि आन्दोलन आदि के कारण अछूत एक राजनीतिक झंडे के तले जमा होने लगे जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा. फेडरेशन के प्रोग्राम से स्पष्ट है कि यदपि इस पार्टी के केंद्र में दलित थे परन्तु पार्टी जाति की राजनीति की जगह मुद्दों पर राजनीति करती थी और इसका फलक व्यापक था.
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबासाहेब ने बदलती परिस्थितियों और लोगों की ज़रुरत को ध्यान में रख कर एक नयी राजनीतिक पार्टी “रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया” की स्थापना की घोषणा 14 अक्तूबर, 1956 को की थी और इसका संविधान भी उन्होंने ही बनाया था. इस पार्टी को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पार्टी बनाना था जो संविधान में किये गए वादों के अनुसार हो और उन्हें पूरा करना उसका उद्देश्य हो. वे इसे केवल अछूतों की पार्टी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि एक जाति या वर्ग के नाम पर बनायी गयी पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती. वह केवल दबाव डालने वाला ग्रुप ही बन सकती है. आरपीआई की स्थापना के पीछे कुछ मुख्य ध्येय था. जैसे-
(1) समाज व्यवस्था से विषमतायें हटाई जाएं ताकि कोई विशेषाधिकार प्राप्त तथा वंचित वर्ग न रहे.
(2) दो पार्टी सिस्टम हो एक सत्ता में दूसरा विरोधी पक्ष
(3) कानून के सामने समानता और सबके लिए एक जैसा कानून हो
(4) समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना
(5) अल्पसंख्यक लोगों के साथ सामान व्यवहार
(6) मानवता की भावना जिसका भारतीय समाज में अभाव रहा है
पार्टी के संविधान की प्रस्तावना में पार्टी का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता” को प्राप्त करना था. पार्टी का कार्यक्रम बहुत व्यापक था. पार्टी की स्थापना के पीछे बाबासाहेब का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब मुस्लिम, गरीब ईसाई, गरीब तथा निचली जाति के सिक्ख तथा कमज़ोर वर्ग के अछूत, पिछड़ी जातियों के लोग, आदिम जातियों के लोग, शोषण का अंत, न्याय और प्रगति चाहने वाले सभी लोग एक झंडे के तले संगठित हो सकें और पूंजीपतियों के मुकाबले में खड़े होकर संविधान तथा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें. (दलित राजनीति और संगठन – भगवान दास)
आरपीआई की विधिवत स्थापना बाबासाहेब के परिनिर्वाण के बाद 1957 में हुई और पार्टी ने नए एजेंडे के साथ 1957 व 1962 का चुनाव लड़ा. पार्टी को महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी सफलता मिली. शुरू में पार्टी ने ज़मीन के बंटवारे, नौकरियों में आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी, दलितों से बौद्ध बने लोगों लिए आरक्षण आदि के लिए संघर्ष किया. पार्टी में मुसलमान, सिक्ख और जैन आदि धर्मों के लोग शामिल हुए. उनमें पंजाब के जनरल राजिंदर सिंह स्पैरो, दिल्ली में डॉ. अब्बास मलिक, उत्तर प्रदेश में राहत मोलाई, डॉ. छेदी लाल साथी, नासिर अहमद, बंगाल में श्री एस. एच. घोष आदि प्रसिद्ध व्यक्ति और कार्यकर्ता हुए. 1964 में 6 दिसंबर से फरवरी 1965 तक पार्टी ने स्वतंत्र भारत में ज़मीन के मुद्दे को लेकर पहला जेल भरो आन्दोलन चलाया जिसमें तीन लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जेल गए. सरकार को मजबूर होकर भूमि आवंटन और कुछ अन्य मांगें माननी पड़ीं.
इस दौर में आरपीआई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मज़बूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई. परन्तु 1962 के बाद यह पार्टी टूटने लगी. इसका मुख्य कारण था कि इस पार्टी से उस समय की सब से मज़बूत राजनैतिक पार्टी कांग्रेस को महाराष्ट्र में खतरा पैदा हो रहा था. इस पार्टी की एक बड़ी कमजोरी थी कि इसकी सदस्यता केवल महारों तक ही सीमित थी. कांग्रेस के नेताओं ने इस पार्टी के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठा कर पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी. सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता दादा साहेब गायकवाड़ को पटाया और उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना दिया. इस पर पार्टी दो गुटों में बंट गयी. गायकवाड का एक गुट कांग्रेस के साथ था जबकि दूसरा बी.डी.खोब्रागडे गुट विरोध में था. इसके बाद अलग नेताओं के नाम पर अलग गुट बनते गए और वर्तमान में यह कई गुटों में बंट कर बेअसर हो चुकी है. इन गुटों के नेता रिपब्लिकन नाम का इस्तेमाल तो करते हैं परन्तु उनका इस पार्टी के मूल एजेंडे से कुछ भी लेना देना नहीं है. वे अपने-अपने फायदे के लिए अलग पार्टियों से समझौते करते हैं और यदा-कदा लाभ भी उठाते हैं.
एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट केंद्र सरकार चाहती है न पढ़ें दलित छात्र, इसलिए रोकी छात्रवृत्तिः टम्टा
 नई टिहरी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के अंदर कांग्रेस ही दलितों की हितैषी है. टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो साल से अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली एक अरब 27 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति जारी नहीं की है. अगर भाजपा दलित हितैशी होती तो दलित छात्रों की छात्रवृति को नहीं रोकती. प्रदीप टम्टा ने कहा कि भाजपा दलितों के बीच जाकर गलत बयानबाजी कर रही है.
बीते रविवार को कांग्रेस के प्रतापनगर विधानसभा के अनुसूचित जाति सम्मेलन में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा केंद्र सरकार दलित छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहती. इतना ही नहीं भाजपा के लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट की राजनीति करते है, जिससे पूरे समाज की सामाजिक समरसता एवं विकास की गति को नुकसान होता है.
विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा है. जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारीलाल खंडवाल ने केंद्र सरकार पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एससीपी की योजनाओं हेतु जिलास्तर पर बजट आवंटन करने समेत कई समस्याओं को रखा.
नई टिहरी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के अंदर कांग्रेस ही दलितों की हितैषी है. टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो साल से अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली एक अरब 27 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति जारी नहीं की है. अगर भाजपा दलित हितैशी होती तो दलित छात्रों की छात्रवृति को नहीं रोकती. प्रदीप टम्टा ने कहा कि भाजपा दलितों के बीच जाकर गलत बयानबाजी कर रही है.
बीते रविवार को कांग्रेस के प्रतापनगर विधानसभा के अनुसूचित जाति सम्मेलन में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा केंद्र सरकार दलित छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहती. इतना ही नहीं भाजपा के लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट की राजनीति करते है, जिससे पूरे समाज की सामाजिक समरसता एवं विकास की गति को नुकसान होता है.
विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा है. जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारीलाल खंडवाल ने केंद्र सरकार पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एससीपी की योजनाओं हेतु जिलास्तर पर बजट आवंटन करने समेत कई समस्याओं को रखा. जाति: भारत से ब्रिटेन तक
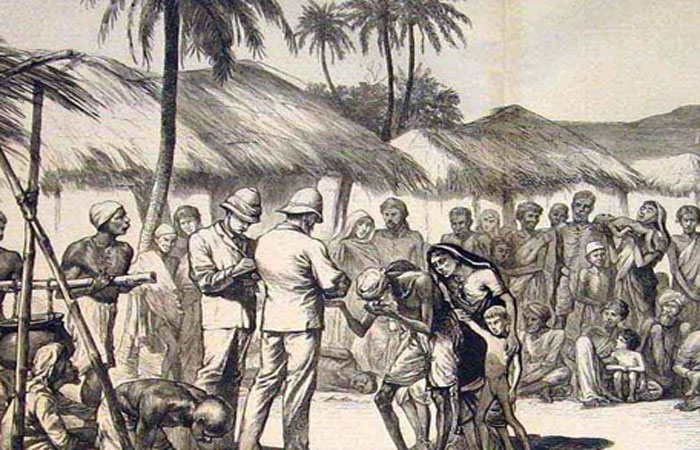 रिटेन में जातिगत भेदभाव के विरूद्ध कानून बनाने की मांग और इसकी कोशिशों के विरोध ने एक बार फिर जाति-व्यवस्था और इसके पोषकों, समर्थकों के बारे में सोचने को विवश किया है. भारतीय, विशेष रूप से हिंदू समाज में जाति, जातिवाद, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के अस्तित्व के बावजूद देश में यह कहने या दावा करने वालों की कमी नहीं है कि समाज में आज जाति की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है. जाति और तदजनित ऊंच-नीच का भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी कोई बात अब समाज में नहीं रह गयी है. यह केवल दूर-दराज गांवों में अशिक्षित, अर्द्ध-शिक्षित लोगों में ही थोड़ी बहुत जीवित है. शिक्षा और आर्थिक विकास के साथ-साथ यह वहां पर भी समाप्त हो जाएगी. उनके तर्क का आधार यह है कि भारतीय समाज में जाति की बुराई का कारण शिक्षा की कमी के कारण रही. जहां-जहां तक शिक्षा का प्रसार हो रहा है जाति अपना अस्तित्व खोती जा रही है. इसके समर्थन में कई उदाहरण भी दिए जाते हैं. इस प्रकार के दावे और कथन प्राय: सवर्ण हिंदुओं द्वारा किए जाते हैं.
समाज से जाति के उन्मूलन का दावा करने वाले लोग गर्व के साथ यह बताना भी नहीं भूलते कि हम दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, उनके घर जाते हैं, उनके साथ उठते-बैठते और खाते-पीते हैं. दलितों को अपने घरों में वे कितना बुलाते हैं, कितना खिलाते-पिलाते हैं. दलितों के घरों में जाकर मांस और मदिरा सेवन का सुख प्राप्त करने वाले सवर्ण क्या अपने घरों में भी उसी प्रकार दलितों को मांस और मदिरा का सेवन कराते हैं. प्रश्न यह है कि जितने अधिकार और स्वतंत्रता से सवर्ण लोग दलितों के घरों में जाते हैं और जितना सम्मान पाते हैं क्या उतने ही अधिकार और स्वतंत्रता से दलित उनके घरों में आते-जाते हैं या आ-जा सकते हैं. क्या सवर्णों द्वारा अपने घरों में दलितों को उतना ही सम्मान दिया जाता है, जितना वे दलितों के घरों में पाते हैं. यदि ऐसा नहीं है तो फिर उनके बीच समानता कैसी है. फिर किस आधार पर कहा जा सकता है कि जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है. सवर्णों द्वारा दलितों के घर जाकर उनके साथ बैठकर खाने-पीने मात्र से जातिगत भेदभाव को समाप्त हुआ नहीं माना जा सकता.
जहां तक अशिक्षा को जातिगत भेदभाव का आधार मानने का प्रश्न है, यह एक निहायत खोखला तर्क है. भारत से इंग्लैण्ड, अमेरिका और अन्य देशों में उच्च शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए जाने वाले लोग प्राय: शिक्षित हैं. और इन देशों में काले-गोरे रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव भले ही है, किंतु एक ही जैसे रंग रूप वाले लोगों के बीच जाति जैसा कोई भेदभाव और अस्पृश्यता वहां पर नहीं है. यह भी एक सच है कि भारत से विदेशों में जाकर नौकरी, व्यापार करने वाले अधिकांश लोग उच्च जातीय हैं. प्रारम्भ में तो सब के सब वही जाते थे. बाबासाहेब आम्बेडकर के लम्बे और कठिन संघर्ष के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दलितों को शिक्षा के अवसर मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो कुछ दलित भी दूसरों की देखादेखी अब विदेशों में जाने लगे हैं. सदियों से जातिगत घृणा, अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न की मार झेलने वाले दलित समाज का कोई भी व्यक्ति जाति को अपनाना नहीं चाहता, अपितु वह इससे मुक्त होना चाहता है. समाज में इस बात के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां दलितों ने अपनी जाति छिपायी है. कई दलित लेखकों ने इस तथ्य को अपनी आत्मकथाओं या आत्म-कथ्यों में अभिव्यक्त किया है. बाबासाहेब आम्बेडकर को बड़ौदा राज्य की नौकरी के दौरान रहने के लिए मकान नहीं मिलने के कारण अपनी जाति छिपाकर रहना पड़ा था. यह स्थिति आज भी है. दलितों के लिए अपनी जाति छिपाकर सवर्णों के बीच रहना सरल नहीं है, क्योंकि बाद में सच्चाई पता चलने पर उनको जिस अपमान और जिल्लत का सामना करना पड़ता है वह कष्टपूर्ण मौत से भी बढकर है. और प्राय: ऐसा होता है. बाबासाहेब आम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही हुआ था.
ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून की मांग और कोशिश इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव है और यह भेदभाव किन्हीं अन्य समुदायों के बीच नहीं भारत से वहां पर गए सवर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ किया जाता है. क्योंकि ब्रिटिश समाज में जाति-भेद और अस्पृश्यता नहीं है. नस्ल भेद के आधार पर समस्त भारतीय उनके लिए हीन हैं, क्योंकि वे गोरे नहीं, काले या गेहुंए हैं. नस्ल भेदीय दृष्टि से सवर्ण और दलित में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों एक ही रंग के हैं. हालांकि जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन में शुरू हुई है, किंतु अमेरिका, जर्मनी, कनाडा आदि अनेक देशों में, जहां पर भारतीय काफी संख्या में हैं, भी सवर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ इसी प्रकार का जातिगत भेदभाव किया जाता है. जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा प्रमाण अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रवासी टाइम्स है, जिसमें अन्य सामग्री के साथ वैवाहिक विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं. एकाध अपवाद को छोड़कर ये समस्त विज्ञापन उसी प्रकार जाति आधारित होते हैं जिस प्रकार भारत में होते हैं. यह देखना आश्चर्यजनक है कि ब्रिटेन, अमेरिका आदि खुले समाजों में रहते हुए भी तथाकथित सवर्ण हिंदू जातीय संकीर्णता में क्यों बंधे रहते हैं. नए देश और समाज में वहां की व्यवस्था और कानून के अनुसार ही चला जाता है. विदेशों में रहने वाले भारतीय (तथाकथित सवर्ण हिंदू) उन देशों के कानूनों का तो पालन करते हैं, उनके रहन-सहन, खान-पान, भाषा और पहनावे को भी सहज अपना लेते हैं. किंतु अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखते हैं, या कहिए अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं. हिंदू समाज के लिए वर्ण-जाति-व्यवस्था उनके धर्म का आधार है. यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के द्वारा बाल्यावस्था से ही व्यक्ति को श्रेष्ठता और हीनता का पाठ सिखाया जाता है. जातिगत भेदभाव के विषाणु यहीं से उसके मानस को विषाक्त बनाना शुरू कर देते हैं. वर्ण-जाति व्यवस्था यदि समानता की शत्रु और मनुष्यता के लिए विष है तो हिंदू धर्म विष उत्पादन का कारखाना और सवर्ण हिंदू समाज विष का रक्षक, प्रचारक और विक्रेता है. सवर्ण हिंदू जहां भी जाता है अपने साथ वर्ण-व्यवस्था और जातिवाद के विषाणु अपने साथ लेकर जाता है तथा वहां के समाज को भी जाति के इस जहर से विषाक्त बनाता है. जाति हिंदू धर्म की विशेषता है और सवर्ण हिंदुओं ने कसम खायी हुई है कि कहीं भी रहेंगे अपनी विशेषता को नहीं छोड़ेंगे. वर्ण-जाति व्यवस्था के रूप में हिंदू धर्म का पढाया हुए असमानता के पाठ का प्रभाव ही है कि तथाकथित सवर्ण हिंदू या तो किसी की अधीनता में रहेगा या किसी को अपने अधीन बनाकर रखेगा. वह समानता और सदभाव के साथ मिल-जुलकर नहीं सकता. यह उसकी नैतिकता, सैद्धांतिकी या आचार संहिता में ही नहीं है.
भारत देश और समाज का कितना अहित शताब्दियों से वर्ण-जाति व्यवस्था ने किया है, यह एक इतिहास है. ब्रिटेन का समाज और राजनेता इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे. ब्रिटिश सरकार को सशक्त कानून बनाकर जातिगत भेदभाव को यहीं पर रोकना चाहिए, यही ब्रिटिश और विश्व मानव समाज के हित में है. अन्यथा ब्रिटिश समाज का ताना बाना भी जातिगत भेदभाव से अप्रभावित नहीं रहेगा. जाति का जहर जितना फैलता जाएगा समाज और राजनीति यह सबको प्रभावित करेगा और इससे ब्रिटेन भारत की तरह देश और समाज दोनों ही रूप में विभाजित और कमजोर ही बनेगा सशक्त नहीं.
लेखक जाने-माने साहित्यकार और स्तंभकार हैं.
रिटेन में जातिगत भेदभाव के विरूद्ध कानून बनाने की मांग और इसकी कोशिशों के विरोध ने एक बार फिर जाति-व्यवस्था और इसके पोषकों, समर्थकों के बारे में सोचने को विवश किया है. भारतीय, विशेष रूप से हिंदू समाज में जाति, जातिवाद, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के अस्तित्व के बावजूद देश में यह कहने या दावा करने वालों की कमी नहीं है कि समाज में आज जाति की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है. जाति और तदजनित ऊंच-नीच का भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी कोई बात अब समाज में नहीं रह गयी है. यह केवल दूर-दराज गांवों में अशिक्षित, अर्द्ध-शिक्षित लोगों में ही थोड़ी बहुत जीवित है. शिक्षा और आर्थिक विकास के साथ-साथ यह वहां पर भी समाप्त हो जाएगी. उनके तर्क का आधार यह है कि भारतीय समाज में जाति की बुराई का कारण शिक्षा की कमी के कारण रही. जहां-जहां तक शिक्षा का प्रसार हो रहा है जाति अपना अस्तित्व खोती जा रही है. इसके समर्थन में कई उदाहरण भी दिए जाते हैं. इस प्रकार के दावे और कथन प्राय: सवर्ण हिंदुओं द्वारा किए जाते हैं.
समाज से जाति के उन्मूलन का दावा करने वाले लोग गर्व के साथ यह बताना भी नहीं भूलते कि हम दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, उनके घर जाते हैं, उनके साथ उठते-बैठते और खाते-पीते हैं. दलितों को अपने घरों में वे कितना बुलाते हैं, कितना खिलाते-पिलाते हैं. दलितों के घरों में जाकर मांस और मदिरा सेवन का सुख प्राप्त करने वाले सवर्ण क्या अपने घरों में भी उसी प्रकार दलितों को मांस और मदिरा का सेवन कराते हैं. प्रश्न यह है कि जितने अधिकार और स्वतंत्रता से सवर्ण लोग दलितों के घरों में जाते हैं और जितना सम्मान पाते हैं क्या उतने ही अधिकार और स्वतंत्रता से दलित उनके घरों में आते-जाते हैं या आ-जा सकते हैं. क्या सवर्णों द्वारा अपने घरों में दलितों को उतना ही सम्मान दिया जाता है, जितना वे दलितों के घरों में पाते हैं. यदि ऐसा नहीं है तो फिर उनके बीच समानता कैसी है. फिर किस आधार पर कहा जा सकता है कि जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है. सवर्णों द्वारा दलितों के घर जाकर उनके साथ बैठकर खाने-पीने मात्र से जातिगत भेदभाव को समाप्त हुआ नहीं माना जा सकता.
जहां तक अशिक्षा को जातिगत भेदभाव का आधार मानने का प्रश्न है, यह एक निहायत खोखला तर्क है. भारत से इंग्लैण्ड, अमेरिका और अन्य देशों में उच्च शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए जाने वाले लोग प्राय: शिक्षित हैं. और इन देशों में काले-गोरे रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव भले ही है, किंतु एक ही जैसे रंग रूप वाले लोगों के बीच जाति जैसा कोई भेदभाव और अस्पृश्यता वहां पर नहीं है. यह भी एक सच है कि भारत से विदेशों में जाकर नौकरी, व्यापार करने वाले अधिकांश लोग उच्च जातीय हैं. प्रारम्भ में तो सब के सब वही जाते थे. बाबासाहेब आम्बेडकर के लम्बे और कठिन संघर्ष के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दलितों को शिक्षा के अवसर मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो कुछ दलित भी दूसरों की देखादेखी अब विदेशों में जाने लगे हैं. सदियों से जातिगत घृणा, अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न की मार झेलने वाले दलित समाज का कोई भी व्यक्ति जाति को अपनाना नहीं चाहता, अपितु वह इससे मुक्त होना चाहता है. समाज में इस बात के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां दलितों ने अपनी जाति छिपायी है. कई दलित लेखकों ने इस तथ्य को अपनी आत्मकथाओं या आत्म-कथ्यों में अभिव्यक्त किया है. बाबासाहेब आम्बेडकर को बड़ौदा राज्य की नौकरी के दौरान रहने के लिए मकान नहीं मिलने के कारण अपनी जाति छिपाकर रहना पड़ा था. यह स्थिति आज भी है. दलितों के लिए अपनी जाति छिपाकर सवर्णों के बीच रहना सरल नहीं है, क्योंकि बाद में सच्चाई पता चलने पर उनको जिस अपमान और जिल्लत का सामना करना पड़ता है वह कष्टपूर्ण मौत से भी बढकर है. और प्राय: ऐसा होता है. बाबासाहेब आम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही हुआ था.
ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून की मांग और कोशिश इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव है और यह भेदभाव किन्हीं अन्य समुदायों के बीच नहीं भारत से वहां पर गए सवर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ किया जाता है. क्योंकि ब्रिटिश समाज में जाति-भेद और अस्पृश्यता नहीं है. नस्ल भेद के आधार पर समस्त भारतीय उनके लिए हीन हैं, क्योंकि वे गोरे नहीं, काले या गेहुंए हैं. नस्ल भेदीय दृष्टि से सवर्ण और दलित में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों एक ही रंग के हैं. हालांकि जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन में शुरू हुई है, किंतु अमेरिका, जर्मनी, कनाडा आदि अनेक देशों में, जहां पर भारतीय काफी संख्या में हैं, भी सवर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ इसी प्रकार का जातिगत भेदभाव किया जाता है. जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा प्रमाण अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रवासी टाइम्स है, जिसमें अन्य सामग्री के साथ वैवाहिक विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं. एकाध अपवाद को छोड़कर ये समस्त विज्ञापन उसी प्रकार जाति आधारित होते हैं जिस प्रकार भारत में होते हैं. यह देखना आश्चर्यजनक है कि ब्रिटेन, अमेरिका आदि खुले समाजों में रहते हुए भी तथाकथित सवर्ण हिंदू जातीय संकीर्णता में क्यों बंधे रहते हैं. नए देश और समाज में वहां की व्यवस्था और कानून के अनुसार ही चला जाता है. विदेशों में रहने वाले भारतीय (तथाकथित सवर्ण हिंदू) उन देशों के कानूनों का तो पालन करते हैं, उनके रहन-सहन, खान-पान, भाषा और पहनावे को भी सहज अपना लेते हैं. किंतु अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखते हैं, या कहिए अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं. हिंदू समाज के लिए वर्ण-जाति-व्यवस्था उनके धर्म का आधार है. यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के द्वारा बाल्यावस्था से ही व्यक्ति को श्रेष्ठता और हीनता का पाठ सिखाया जाता है. जातिगत भेदभाव के विषाणु यहीं से उसके मानस को विषाक्त बनाना शुरू कर देते हैं. वर्ण-जाति व्यवस्था यदि समानता की शत्रु और मनुष्यता के लिए विष है तो हिंदू धर्म विष उत्पादन का कारखाना और सवर्ण हिंदू समाज विष का रक्षक, प्रचारक और विक्रेता है. सवर्ण हिंदू जहां भी जाता है अपने साथ वर्ण-व्यवस्था और जातिवाद के विषाणु अपने साथ लेकर जाता है तथा वहां के समाज को भी जाति के इस जहर से विषाक्त बनाता है. जाति हिंदू धर्म की विशेषता है और सवर्ण हिंदुओं ने कसम खायी हुई है कि कहीं भी रहेंगे अपनी विशेषता को नहीं छोड़ेंगे. वर्ण-जाति व्यवस्था के रूप में हिंदू धर्म का पढाया हुए असमानता के पाठ का प्रभाव ही है कि तथाकथित सवर्ण हिंदू या तो किसी की अधीनता में रहेगा या किसी को अपने अधीन बनाकर रखेगा. वह समानता और सदभाव के साथ मिल-जुलकर नहीं सकता. यह उसकी नैतिकता, सैद्धांतिकी या आचार संहिता में ही नहीं है.
भारत देश और समाज का कितना अहित शताब्दियों से वर्ण-जाति व्यवस्था ने किया है, यह एक इतिहास है. ब्रिटेन का समाज और राजनेता इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे. ब्रिटिश सरकार को सशक्त कानून बनाकर जातिगत भेदभाव को यहीं पर रोकना चाहिए, यही ब्रिटिश और विश्व मानव समाज के हित में है. अन्यथा ब्रिटिश समाज का ताना बाना भी जातिगत भेदभाव से अप्रभावित नहीं रहेगा. जाति का जहर जितना फैलता जाएगा समाज और राजनीति यह सबको प्रभावित करेगा और इससे ब्रिटेन भारत की तरह देश और समाज दोनों ही रूप में विभाजित और कमजोर ही बनेगा सशक्त नहीं.
लेखक जाने-माने साहित्यकार और स्तंभकार हैं. जब हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, तो क्या करेंगे?
 दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है. गुड़गांव के भी कुछ स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है. हवा ही कुछ ऐसी है कि अब जाने क्या क्या बंद करने का फैसला किया जाएगा. हम जागरूक हैं. हम जानते भी हैं. आज बच्चा बच्चा पीएम के साथ साथ पीएम 2.5 के बारे में जानने लगा है. मगर हो क्या रहा है. इस सवाल को ऐसे भी पूछिये कि हो क्या सकता है.
अभी अभी तो रिपोर्ट आई थी कि कार्बन का भाई डाई आक्साईड का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब वो कभी पीछे नहीं हटेगा. दिल्ली की हवा आने वाले साल में ख़राब नहीं होगी बल्कि हो चुकी है. अब जो हो रहा है वो ये कि ये हवा पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. दरअसल जवाब तो तब मिलेगा जब सवाल पूछा जाएगा, सवाल तो तब पूछा जाएगा जब नोटिस लिया जाएगा, नोटिस दिया नहीं जाएगा.
आपने नचिकेता की कहानी तो सुनी ही होगी. बालक नचिकेता की कहानी हमें क्यों पढ़ाई गई. नचिकेता के सवालों ने उसके पिता वाजश्रवा को कितना क्रोधित कर दिया. क्रोध में वाजश्रवा ने नचिकेता को यमराज को ही दान कर दिया. नचिकेता ने देख लिया कि पिता सब कुछ दान देने के नाम पर अपने लोभ पर काबू नहीं पा रहे हैं. अच्छी गायों की जगह मरियल और बूढ़ी गायें दान में दे रहे हैं. नचिकेता हैरान रह जाता है. सोचता है कि पिता ने दुनिया को कहा कुछ, और कर कुछ रहे हैं. यह भ्रम नहीं टूटता अगर नचिकेता सवाल नहीं करता. नचिकेता पिता से बुनियादी सवाल करता है कि मुझे दान करना होगो तो किसे करोगे. ताम कस्मै माम दास्यसि? यानी पिता मुझे किसे दान करेंगे. वाजश्रवा को गुस्सा आता है और कहते हैं कि मृत्युव त्वाम दास्यामि. यानी जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं. याद रखियेगा, हज़ारों साल पहले की यह कहानी नचिकेता के बाप के दानवीर होने के कारण नहीं जानी जाती है, नचिकेता के नाम से जानी जाती है.
अथॉरिटी और पुलिस कब सवाल से मुक्त हो गए. अथॉरिटी का मतलब है जवाबदेही. बगैर जवाबदेही के अथॉरिटी या पुलिस कुछ और होती होगी. जब हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, कुछ बता नहीं पायेंगे तो क्या करेंगे.
मूक अभिनय को अंग्रेज़ी में माइम कहते हैं. इसकी अथॉरिटी कला की दुनिया में कितनी है मैं नहीं जानता लेकिन हम सबको माइम आर्ट के बारे में जानना चाहिए. यूपीएससी नहीं तो बीपीएससी में तो आ ही जाएगा कि भारत में माइम कला के उदभव और विकास की यात्रा पर लघु निबंध लिखें. कोलकाता के निरंजन गोस्वामी ने बताया कि 2500 साल पुराने नाट्य शास्त्र में भी मूक अभिनय का उल्लेख मिलता है. भारतीय मूक कलाकारों ने सब कुछ यूरोप से नहीं लिया है बल्कि बहुत कुछ अपनी परंपराओं से भी विकसित किया है. बल्कि दुनिया में जो टेकनिक अपनाई जाती है उसमें भारतीय असर ही ज्यादा है. बीबीसी के अनुसार कोलकाता से चुप्पी की आवाज़ नाम की एक पत्रिका भी छपती है जो कई देशों में पढ़ी जाती है. मूक अभिनय में आप संवाद मन में बोलते हैं ताकि दर्शक सुनाई देते हैं. मन की बात नहीं करने पर चेहरे पर भाव नहीं आता है. इस वक्त भारत में माइम की कई रिपोर्टरी कंपनी खुल गई है. कोलकाता में हर साल बीस पचीस टीमें आती हैं. आम तौर पर आप चार्ली चैपलिन के ज़रिये मूक अभियन को याद रखते हैं. आम तौर पर दुख और सुख को ही इसके ज़रिये व्यक्त किया जाता है. जैसे आप जब चार्ली चैपलिन को देखते हैं तो हंसी आती है मगर कलाकार के मन का भाव दुखी है.
आमतौर पर शुक्रवार के रोज़ फिल्मों की ही बात होती है, लेकिन माइम यानी मूक अभिनय की हम बात करेंगे. आज के माहौल में जब हवा ख़राब है, कार्बन कणों की मात्रा काफी बढ़ गई है तो क्यों न इन कलाकारों की सोहबत में हम आज की शाम गुज़ारें और महसूस करें कि जब हमारा बोलना बंद हो जाएगा तो मन में तैरते हुए भाव चेहरे पर कैसे आएंगे. आप क्या करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या बोलना चाहते हैं. बोलने से याद आया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजा है कि 9 नवंबर के दिन एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण एक दिन के लिए स्थगित करना होगा. एनडीटीवी का जवाब है कि ये दुखद है कि सिर्फ़ एनडीटीवी को इस तरह निशाना बनाया गया. सभी चैनलों और अख़बारों में (पठानकोट हमले की) ऐसी ही कवरेज थी. (पठानकोट हमले पर) एनडीटीवी की कवरेज ख़ास तौर पर संतुलित रही. प्रेस को ज़ंजीरों में जकड़ने वाले आपातकाल के काले दिनों के बाद एनडीटीवी पर इस तरह की कार्रवाई असाधारण है. एनडीटीवी सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है.
देश भर से हमें समर्थन मिल रहा है. आप सभी का शुक्रिया. नोटिस की सर्वत्र निंदा हो रही है. एनडीटीवी जल्द ही सूचित करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा. हम अपना काम उसी बुलंदी और इकबाल से करते रहेंगे. ख़ैर वैसे भी सवालों से घबरा कर बहुत लोग मुझसे दूर जा चुके हैं. तभी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें सवालों का डर न रहे. दिन ढले न ढले दिल ज़रूर बहले. इससे पहले कि आप घर में भी मास्क पहनकर टीवी देखने लगें, हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं. रामनाथ गोयनका पुरस्कार के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण के बाद धन्यवाद भाषण देते हुए इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने एक बात कही थी. अगर कोई पत्रकार इस वक्त प्राइम टाइम देख रहा है तो राजकमल झा की इस बात को लिखकर पर्स में रख ले. अगर किसी पॉकेटमार ने उसका कभी पर्स उड़ा भी लिया तो राजकमल झा की इस बात को पढ़ कर हमेशा के लिए बदल जाएगा और एक अच्छा नागरिक बन जाएगा. वो बात ये है, ”इस साल मैं 50 का हो रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं, जो रिट्वीट और लाइक के ज़माने में जवान हो रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्ज़त की बात है.”
साभारः एनडीटीवी से लिया गया है. यह प्राइम टाइम का लिखित रूप है.
दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है. गुड़गांव के भी कुछ स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है. हवा ही कुछ ऐसी है कि अब जाने क्या क्या बंद करने का फैसला किया जाएगा. हम जागरूक हैं. हम जानते भी हैं. आज बच्चा बच्चा पीएम के साथ साथ पीएम 2.5 के बारे में जानने लगा है. मगर हो क्या रहा है. इस सवाल को ऐसे भी पूछिये कि हो क्या सकता है.
अभी अभी तो रिपोर्ट आई थी कि कार्बन का भाई डाई आक्साईड का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब वो कभी पीछे नहीं हटेगा. दिल्ली की हवा आने वाले साल में ख़राब नहीं होगी बल्कि हो चुकी है. अब जो हो रहा है वो ये कि ये हवा पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. दरअसल जवाब तो तब मिलेगा जब सवाल पूछा जाएगा, सवाल तो तब पूछा जाएगा जब नोटिस लिया जाएगा, नोटिस दिया नहीं जाएगा.
आपने नचिकेता की कहानी तो सुनी ही होगी. बालक नचिकेता की कहानी हमें क्यों पढ़ाई गई. नचिकेता के सवालों ने उसके पिता वाजश्रवा को कितना क्रोधित कर दिया. क्रोध में वाजश्रवा ने नचिकेता को यमराज को ही दान कर दिया. नचिकेता ने देख लिया कि पिता सब कुछ दान देने के नाम पर अपने लोभ पर काबू नहीं पा रहे हैं. अच्छी गायों की जगह मरियल और बूढ़ी गायें दान में दे रहे हैं. नचिकेता हैरान रह जाता है. सोचता है कि पिता ने दुनिया को कहा कुछ, और कर कुछ रहे हैं. यह भ्रम नहीं टूटता अगर नचिकेता सवाल नहीं करता. नचिकेता पिता से बुनियादी सवाल करता है कि मुझे दान करना होगो तो किसे करोगे. ताम कस्मै माम दास्यसि? यानी पिता मुझे किसे दान करेंगे. वाजश्रवा को गुस्सा आता है और कहते हैं कि मृत्युव त्वाम दास्यामि. यानी जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं. याद रखियेगा, हज़ारों साल पहले की यह कहानी नचिकेता के बाप के दानवीर होने के कारण नहीं जानी जाती है, नचिकेता के नाम से जानी जाती है.
अथॉरिटी और पुलिस कब सवाल से मुक्त हो गए. अथॉरिटी का मतलब है जवाबदेही. बगैर जवाबदेही के अथॉरिटी या पुलिस कुछ और होती होगी. जब हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, कुछ बता नहीं पायेंगे तो क्या करेंगे.
मूक अभिनय को अंग्रेज़ी में माइम कहते हैं. इसकी अथॉरिटी कला की दुनिया में कितनी है मैं नहीं जानता लेकिन हम सबको माइम आर्ट के बारे में जानना चाहिए. यूपीएससी नहीं तो बीपीएससी में तो आ ही जाएगा कि भारत में माइम कला के उदभव और विकास की यात्रा पर लघु निबंध लिखें. कोलकाता के निरंजन गोस्वामी ने बताया कि 2500 साल पुराने नाट्य शास्त्र में भी मूक अभिनय का उल्लेख मिलता है. भारतीय मूक कलाकारों ने सब कुछ यूरोप से नहीं लिया है बल्कि बहुत कुछ अपनी परंपराओं से भी विकसित किया है. बल्कि दुनिया में जो टेकनिक अपनाई जाती है उसमें भारतीय असर ही ज्यादा है. बीबीसी के अनुसार कोलकाता से चुप्पी की आवाज़ नाम की एक पत्रिका भी छपती है जो कई देशों में पढ़ी जाती है. मूक अभिनय में आप संवाद मन में बोलते हैं ताकि दर्शक सुनाई देते हैं. मन की बात नहीं करने पर चेहरे पर भाव नहीं आता है. इस वक्त भारत में माइम की कई रिपोर्टरी कंपनी खुल गई है. कोलकाता में हर साल बीस पचीस टीमें आती हैं. आम तौर पर आप चार्ली चैपलिन के ज़रिये मूक अभियन को याद रखते हैं. आम तौर पर दुख और सुख को ही इसके ज़रिये व्यक्त किया जाता है. जैसे आप जब चार्ली चैपलिन को देखते हैं तो हंसी आती है मगर कलाकार के मन का भाव दुखी है.
आमतौर पर शुक्रवार के रोज़ फिल्मों की ही बात होती है, लेकिन माइम यानी मूक अभिनय की हम बात करेंगे. आज के माहौल में जब हवा ख़राब है, कार्बन कणों की मात्रा काफी बढ़ गई है तो क्यों न इन कलाकारों की सोहबत में हम आज की शाम गुज़ारें और महसूस करें कि जब हमारा बोलना बंद हो जाएगा तो मन में तैरते हुए भाव चेहरे पर कैसे आएंगे. आप क्या करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या बोलना चाहते हैं. बोलने से याद आया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजा है कि 9 नवंबर के दिन एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण एक दिन के लिए स्थगित करना होगा. एनडीटीवी का जवाब है कि ये दुखद है कि सिर्फ़ एनडीटीवी को इस तरह निशाना बनाया गया. सभी चैनलों और अख़बारों में (पठानकोट हमले की) ऐसी ही कवरेज थी. (पठानकोट हमले पर) एनडीटीवी की कवरेज ख़ास तौर पर संतुलित रही. प्रेस को ज़ंजीरों में जकड़ने वाले आपातकाल के काले दिनों के बाद एनडीटीवी पर इस तरह की कार्रवाई असाधारण है. एनडीटीवी सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है.
देश भर से हमें समर्थन मिल रहा है. आप सभी का शुक्रिया. नोटिस की सर्वत्र निंदा हो रही है. एनडीटीवी जल्द ही सूचित करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा. हम अपना काम उसी बुलंदी और इकबाल से करते रहेंगे. ख़ैर वैसे भी सवालों से घबरा कर बहुत लोग मुझसे दूर जा चुके हैं. तभी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें सवालों का डर न रहे. दिन ढले न ढले दिल ज़रूर बहले. इससे पहले कि आप घर में भी मास्क पहनकर टीवी देखने लगें, हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं. रामनाथ गोयनका पुरस्कार के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण के बाद धन्यवाद भाषण देते हुए इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने एक बात कही थी. अगर कोई पत्रकार इस वक्त प्राइम टाइम देख रहा है तो राजकमल झा की इस बात को लिखकर पर्स में रख ले. अगर किसी पॉकेटमार ने उसका कभी पर्स उड़ा भी लिया तो राजकमल झा की इस बात को पढ़ कर हमेशा के लिए बदल जाएगा और एक अच्छा नागरिक बन जाएगा. वो बात ये है, ”इस साल मैं 50 का हो रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं, जो रिट्वीट और लाइक के ज़माने में जवान हो रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्ज़त की बात है.”
साभारः एनडीटीवी से लिया गया है. यह प्राइम टाइम का लिखित रूप है. प्रिंसिपल ने दलित छात्र से जबरन साफ कराया स्कूल का शौचालय
 नई दिल्ली। कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय भैरवा में एक दलित छात्र से शौचालय साफ कराने की शर्मनाक घटना सामने आई है. आरोप विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर है. घटना के बाद बच्चे ने घर पहुंचकर अपनी नानी को पूरी बात बताई. प्रधानाध्यापक के खिलाफ नानी ने कौशाम्बी थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. बीते गुरूवार को नानी छात्र को लेकर जिला मुख्यालय जा रही थीं, लेकिन कुछ लोगों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और अफसरों तक नहीं पहुंचने दिया.
प्राथमिक विद्यालय भैरवा में कक्षा एक में पढ़ने वाला पांच वर्षीय छात्र भैरवा गांव में ही अपनी नानी मालती देवी के साथ रहता है. 24 अक्तूबर को वह स्कूल गया तो प्रधानाध्यापक रावेंद्र सिंह ने उसे स्कूल का शौचालय साफ करने को कहा. शिवा ने मना किया तो उसे डांटा गया और ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया. शौचालय साफ होने के बाद शिवा पर पानी डालकर भीगे कपड़ों में उसे घर भेज दिया गया.
ठिठुरते और रोते हुए वह घर पहुंचा तो नानी मालती देवी उसकी हालत देख सन्न रह गईं. पूछने पर उसने अपनी नानी को घटना की जानकारी दी, जिस पर मालती देवी आगबबूला हो गईं. वह शिवा को लेकर सीधे कौशाम्बी थाने पहुंच गईं. उन्होंने थाने में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत दी.
हफ्ते भर बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मालती देवी गुरूवार को अफसरों से मिलने जिला मुख्यालय की ओर से चल पड़ीं लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. सुलह-समझौते के लिए काफी देर तक पंचायत चली लेकिन मालती देवी अपने नाती को न्याय दिलाने के लिए अड़ी रहीं. वह अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और प्रधानाध्यापक के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई चाहती हैं.
कौशाम्बी थाने के एसओ ने कहा कि ‘मामले की तहरीर मिली है. त्योहार होने के कारण स्कूल बंद हो गए थे, इसलिए जांच नहीं हो पाई है. जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.’
नई दिल्ली। कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय भैरवा में एक दलित छात्र से शौचालय साफ कराने की शर्मनाक घटना सामने आई है. आरोप विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर है. घटना के बाद बच्चे ने घर पहुंचकर अपनी नानी को पूरी बात बताई. प्रधानाध्यापक के खिलाफ नानी ने कौशाम्बी थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. बीते गुरूवार को नानी छात्र को लेकर जिला मुख्यालय जा रही थीं, लेकिन कुछ लोगों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और अफसरों तक नहीं पहुंचने दिया.
प्राथमिक विद्यालय भैरवा में कक्षा एक में पढ़ने वाला पांच वर्षीय छात्र भैरवा गांव में ही अपनी नानी मालती देवी के साथ रहता है. 24 अक्तूबर को वह स्कूल गया तो प्रधानाध्यापक रावेंद्र सिंह ने उसे स्कूल का शौचालय साफ करने को कहा. शिवा ने मना किया तो उसे डांटा गया और ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया. शौचालय साफ होने के बाद शिवा पर पानी डालकर भीगे कपड़ों में उसे घर भेज दिया गया.
ठिठुरते और रोते हुए वह घर पहुंचा तो नानी मालती देवी उसकी हालत देख सन्न रह गईं. पूछने पर उसने अपनी नानी को घटना की जानकारी दी, जिस पर मालती देवी आगबबूला हो गईं. वह शिवा को लेकर सीधे कौशाम्बी थाने पहुंच गईं. उन्होंने थाने में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत दी.
हफ्ते भर बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मालती देवी गुरूवार को अफसरों से मिलने जिला मुख्यालय की ओर से चल पड़ीं लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. सुलह-समझौते के लिए काफी देर तक पंचायत चली लेकिन मालती देवी अपने नाती को न्याय दिलाने के लिए अड़ी रहीं. वह अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और प्रधानाध्यापक के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई चाहती हैं.
कौशाम्बी थाने के एसओ ने कहा कि ‘मामले की तहरीर मिली है. त्योहार होने के कारण स्कूल बंद हो गए थे, इसलिए जांच नहीं हो पाई है. जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.’ झाड़ू लगानेवाली मां की सेवानिवृत्ति पर पहुंचे आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर पुत्र
 रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ में पानी टंकी परिसर में झाडू लगाने का काम करनेवाली चतुर्थ वर्गीय कर्मी सुमित्रा देवी की सेवानिवृत्ति कई मायनों में सबसे अलग रही. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) रजरप्पा स्थित टाउनशिप में बीते सोमवार शाम सुमित्रा देवी के विदाई समारोह में उनके तीनों पुत्र शामिल हुए. सबसे बड़े पुत्र विरेंद्र कुमार रेलवे में इंजीनियर है, उनसे छोटे धीरेंद्र कुमार डॉक्टर और सबसे छोटे महेंद्र कुमार आईएएस और बिहार के सिवान में जिलाधिकारी है.
विदाई समारोह में अपने तीनों अफसर बेटों को अपने पास देख सुमित्रा देवी जहां भावुक हो गई, वहीं सहकर्मी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे. तीनों बेटों के लिए भी यह भावुक पल था. कारण जिस परिश्रम की बदौलत उनकी मां ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर सभी साथ-साथ थे. सीसीएल कर्मी सुमित्रा देवी लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई. विदाई समारोह में मुख्य अतिथि स्टाफ ऑफिसर ईएंडएम धीरेंद्र बिहारी ने गुलदस्ता देकर और शॉल भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी. साथ ही कार्यकाल में सुमित्रा देवी द्वारा किए गए बेहतर कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का अहम हिस्सा है, यह पल सभी के जीवनकाल में एक बार आता है. विदाई के पल भावुक होते हैं. लेकिन सुमित्रा देवी ने जिस ईमानदारीपूर्वक काम किया वह कंपनी एवं समाज के लिए प्रेरणा है. मौके पर तीनों पुत्रों ने भी बारी-बारी से अपनी कामयाबी की बातें टाउनशिप के कर्मियों के समक्ष रखी.
उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने कठिन परिश्रम कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. उनके मुताबिक मां ने काफी संघर्ष कर सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई. उनका संघर्ष देख हमलोगों ने भी कुछ करने और कुछ बनकर दिखाने का ठान ली. उन्हीं की बदौलत आज हम तीनों अपनी-अपनी जगह पर खड़ें है. सिवान के डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि कोई काम जीवन में कठिन नहीं होता है. मेहनत करने से हर कार्य संभव हो जाता है. बस, काम ईमानदारी से करना चाहिए.
रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ में पानी टंकी परिसर में झाडू लगाने का काम करनेवाली चतुर्थ वर्गीय कर्मी सुमित्रा देवी की सेवानिवृत्ति कई मायनों में सबसे अलग रही. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) रजरप्पा स्थित टाउनशिप में बीते सोमवार शाम सुमित्रा देवी के विदाई समारोह में उनके तीनों पुत्र शामिल हुए. सबसे बड़े पुत्र विरेंद्र कुमार रेलवे में इंजीनियर है, उनसे छोटे धीरेंद्र कुमार डॉक्टर और सबसे छोटे महेंद्र कुमार आईएएस और बिहार के सिवान में जिलाधिकारी है.
विदाई समारोह में अपने तीनों अफसर बेटों को अपने पास देख सुमित्रा देवी जहां भावुक हो गई, वहीं सहकर्मी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे. तीनों बेटों के लिए भी यह भावुक पल था. कारण जिस परिश्रम की बदौलत उनकी मां ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर सभी साथ-साथ थे. सीसीएल कर्मी सुमित्रा देवी लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई. विदाई समारोह में मुख्य अतिथि स्टाफ ऑफिसर ईएंडएम धीरेंद्र बिहारी ने गुलदस्ता देकर और शॉल भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी. साथ ही कार्यकाल में सुमित्रा देवी द्वारा किए गए बेहतर कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का अहम हिस्सा है, यह पल सभी के जीवनकाल में एक बार आता है. विदाई के पल भावुक होते हैं. लेकिन सुमित्रा देवी ने जिस ईमानदारीपूर्वक काम किया वह कंपनी एवं समाज के लिए प्रेरणा है. मौके पर तीनों पुत्रों ने भी बारी-बारी से अपनी कामयाबी की बातें टाउनशिप के कर्मियों के समक्ष रखी.
उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने कठिन परिश्रम कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. उनके मुताबिक मां ने काफी संघर्ष कर सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई. उनका संघर्ष देख हमलोगों ने भी कुछ करने और कुछ बनकर दिखाने का ठान ली. उन्हीं की बदौलत आज हम तीनों अपनी-अपनी जगह पर खड़ें है. सिवान के डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि कोई काम जीवन में कठिन नहीं होता है. मेहनत करने से हर कार्य संभव हो जाता है. बस, काम ईमानदारी से करना चाहिए. पहले दलित के घर में आग लगाई, फिर पंचायत ने जबरन समझौता कराया
 फरीदाबाद। सदर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बीते मंगलवार तड़के अज्ञात लोगों ने दलित के घर में आग लगा दी. आग के दौरान कुत्तों के भौंकने पर परिवार के लोग जाग गए. इस वजह से उन्होंने आग पर काबू पा लिया. आग से 2 चारपाई व भूसा जल गया. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. दोपहर बाद गांव के लोगों की पंचायत हुई. जिसमें आरोपी व पीड़ित पक्ष के लोग शामिल हुए. पंचायत में हुए फैसले के बाद दलित परिवार ने अपना केस वापस लेने के लिए पुलिस को शपथ पत्र दे दिया. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई रोक दी.
पुलिस के अनुसार नवादा गांव निवासी मामचंद की बेटी सपना ने दी शिकायत में बताया कि सोमवार रात को वह अपनी बहन शकुंत और उसके बच्चों के साथ घर में सोई हुई थी. परिवार के अन्य लोग अस्पताल गए थे. दिवाली के दिन गांव के कुछ लोगों ने उनके परिवार के लोगों को पीटकर घायल कर दिया था. सभी घायल अस्पताल में दाखिल हैं. सपना ने बताया कि मंगलवार तड़के करीब 3 बजे घर के बाहर बने चौक में जोर-जोर से कुत्ते भौंक रहे थे. इस पर सपना की नींद खुल गई और वह कुत्तों को हड़काने के लिए बाहर आ गई. तभी उसने देखा कि मकान के पास बने भूसे के कमरे में आग लगी हुई थी. आग से कमरे में रखी दो चारपाई जल चुकी थी.
सपना ने पुलिस को बताया कि घटनास्थल के पास से 3 युवक भाग रहे थे. आग लगने पर उसने शोर मचा दिया. जिस पर परिवार के लोग जाग गए और उन्होंने पानी आदि डालकर आग पर काबू पा लिया. सपना का कहना है कि 30 अक्टूबर को दिवाली के दिन नवादा गांव में रहने वाले भुप्पी, महेश, भारत, भीम, बिरन, हंसराज, बलराज व नफेसिंह आदि ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी. आरोप है कि इसी रंजिश में आरोपियों ने आग लगाई. रात को घटनास्थल पर दिखने वाले 3 लोग इन्हीं आरोपियों में से हैं. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर एसीपी विष्णु दयाल व एसएचओ राजदीप मोर पुलिस बल के साथ पहुंच गए और घटना की गहनता से जांच की.
एसएचओ राजदीप मोर ने बताया कि सपना के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया, मगर मंगलवार दोपहर के समय गांव में एक पंचायत हुई. पंचायत में गांव के सभी लोगों के अलावा पीड़ित और आरोपी पक्ष के लोग भी शामिल हुए. इस पंचायत के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को दर्ज मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई न कराने के लिए शपथ पत्र दे दिया. इस वजह से कार्रवाई रोक दी गई है.
फरीदाबाद। सदर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बीते मंगलवार तड़के अज्ञात लोगों ने दलित के घर में आग लगा दी. आग के दौरान कुत्तों के भौंकने पर परिवार के लोग जाग गए. इस वजह से उन्होंने आग पर काबू पा लिया. आग से 2 चारपाई व भूसा जल गया. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. दोपहर बाद गांव के लोगों की पंचायत हुई. जिसमें आरोपी व पीड़ित पक्ष के लोग शामिल हुए. पंचायत में हुए फैसले के बाद दलित परिवार ने अपना केस वापस लेने के लिए पुलिस को शपथ पत्र दे दिया. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई रोक दी.
पुलिस के अनुसार नवादा गांव निवासी मामचंद की बेटी सपना ने दी शिकायत में बताया कि सोमवार रात को वह अपनी बहन शकुंत और उसके बच्चों के साथ घर में सोई हुई थी. परिवार के अन्य लोग अस्पताल गए थे. दिवाली के दिन गांव के कुछ लोगों ने उनके परिवार के लोगों को पीटकर घायल कर दिया था. सभी घायल अस्पताल में दाखिल हैं. सपना ने बताया कि मंगलवार तड़के करीब 3 बजे घर के बाहर बने चौक में जोर-जोर से कुत्ते भौंक रहे थे. इस पर सपना की नींद खुल गई और वह कुत्तों को हड़काने के लिए बाहर आ गई. तभी उसने देखा कि मकान के पास बने भूसे के कमरे में आग लगी हुई थी. आग से कमरे में रखी दो चारपाई जल चुकी थी.
सपना ने पुलिस को बताया कि घटनास्थल के पास से 3 युवक भाग रहे थे. आग लगने पर उसने शोर मचा दिया. जिस पर परिवार के लोग जाग गए और उन्होंने पानी आदि डालकर आग पर काबू पा लिया. सपना का कहना है कि 30 अक्टूबर को दिवाली के दिन नवादा गांव में रहने वाले भुप्पी, महेश, भारत, भीम, बिरन, हंसराज, बलराज व नफेसिंह आदि ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी. आरोप है कि इसी रंजिश में आरोपियों ने आग लगाई. रात को घटनास्थल पर दिखने वाले 3 लोग इन्हीं आरोपियों में से हैं. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर एसीपी विष्णु दयाल व एसएचओ राजदीप मोर पुलिस बल के साथ पहुंच गए और घटना की गहनता से जांच की.
एसएचओ राजदीप मोर ने बताया कि सपना के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया, मगर मंगलवार दोपहर के समय गांव में एक पंचायत हुई. पंचायत में गांव के सभी लोगों के अलावा पीड़ित और आरोपी पक्ष के लोग भी शामिल हुए. इस पंचायत के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को दर्ज मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई न कराने के लिए शपथ पत्र दे दिया. इस वजह से कार्रवाई रोक दी गई है. कॉलेजियम सिस्टमः 85 प्रतिशत लोगों को न्याय से वंचित रखने का षडयंत्र
 हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों द्वारा बनायी गयी 3-4 हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों की कमिटी का नाम ही कॉलेजियम है. शुरू में सोचा गया कि यह व्यवस्था ”मोहि ले चल” की बिमारी से भिन्न होगी. लेकिन इसने भी ऐसा करना शुरू किया कि लोग कहने लगे ”चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास”. कलक्टर ही कलक्टर की बहाली, एसपी ही एसपी की बहाली और जज ही जज की बहाली करने लगेगा तो सुनने में तो बड़ा अजूबा लगेगा ही और यह न्यायसंगत और संविधान सम्मत भी नहीं है. बाबासाहेब का लिखा हुआ संविधान है जिसमें हर समस्याओं का समाधान है तो फिर कॉलेजियम ही क्यों?
संविधान से ऊपर कोई नहीं. न्यायपालिका भी नहीं. जब से पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिलने की व्यवस्था की गयी तब से जजों ने ही जजों की एक कॉलेजियम बनाकर हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम प्रारम्भ कर दिया. भारत जैसे जाति प्रधान डैमोक्रेटिक देश में जजों की नियुक्ति के लिए मनमाने तौर से कॉलेजियम जैसी व्यवस्था देश के माथे पर कलंक का एक काला धब्बा है. डॉ. लोहिया कहते थे सभी डैमोक्रेटिक संस्थाओं में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होना सबके हित में है. संविधान के अनुच्छेद 312 में IAS , IPS और IFS की तरह ऑल इन्डिया ज्यूडिशियल सर्विस (AIJS) की स्थापना का उपबंध करने की भी बात कही गयी है और इसके लिए 1976 में संविधान का 42वां संशोधन भी किया गया है. लेकिन आज तक AIJS का गठन नहीं किया गया. यह अच्छी बात है कि 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने हाईकोर्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर विज्ञान भवन दिल्ली के स्वर्णजयंती समारोह में सिविल सेवा की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने पर विचार करने को कहा है. देखिये क्या होता है?
अन्य सेवाओं की तरह अगर इसका भी गठन हो जाए तो जजों का भी मेरिट के आधार पर चयन होने लगेगा और सभी वर्गों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा जिससे हमारी ज्यूडिशियरी को भी विवाद रहित योग्य जज उपलबध होने लगेंगे. फिर कोई हमारी ज्यूडिशियरी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी उंगली नहीं उठाएगा. जनमानस को भी ज्यूडिशियरी की पारदर्शिता दिखने लगेगी. लेकिन विगत 70 वर्षों से इस सम्बन्ध में सवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और ना हीं होने दिया.
जहां तक मेरिट का सवाल है तो मेरिट किसी ख़ास वर्ग या जाति की जागीर नहीं. यह कहना और समझना विल्कुल बेईमानी है कि 85 प्रतिशत पिछड़ों में जज बनने की योग्यता नहीं है. अंग्रेज तो काफी योग्य थे. योग्यता ही सब कुछ है तो फिर अंग्रेजों को हटाने के लिये लाखों नागरिकों ने लहू क्यों बहाया? जबकि उनका किया गया कोई काम आज भी आपके काम से लाख गुना बेहतर है. आरक्षण का सम्बन्ध योग्यता से नहीं बल्कि शासन-प्रशासन में सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व से है और अब यह मामला हिस्सेदारी का भी बन गया है.
अगर मेरिट केवल ऊंची जाति की जागीर होती तो दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के किसी विश्वविद्यालय के नाम का नहीं होना, जबकि सभी विश्वविद्यालयों में 95 प्रतिशत ऊंची जाति के लोग ही व्याख्याता के साथ-साथ कुलपति भी हैं, यह प्रमाणित करता है कि ये लोग योग्य नहीं हैं. अगर ये योग्य ही होते और सारे जगत की बुद्धि का भण्डार इन्हीं के पास होता तो बच्चों के खिलौनों एवं इनके देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर सभी युद्धक हथियार तक विदेशों से आयात नहीं किये जाते और इसके लिये उनके चरणों में जाकर दांत नहीं निपोरने पड़ते. यही नहीं विश्वविद्यालयों में छात्रों-शिक्षकों को कानून की पुस्तकों सहित हर विषयों के अध्ययन-अध्यापन तक के लिए विदेशी पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता है. कहां चला गया इनका अपना ज्ञान? किसी विषय पर इनकी कोई पुस्तक नहीं जिसकी किसी एक पंक्ति को अपनी पुस्तकों में कोट करके दुनियावाले अपनी बात आगे बढ़ाते हों लेकिन ठीक इसके उलट ये लोग दुनियावालों को कोट किये वगैर कोई पुस्तक लिख ही नहीं सकते. मतलब किसी भी विषय पर इनकी कोई अपनी ओरिजीनालिटी नहीं है. न्यायपालिका में भी 95 प्रतिशत ऊंची जाति के ही योग्य जजों, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर आये दिन न्यायपालिका की हो रही किरकिरी से हम शर्मसार होते रहे हैं. फिर भी ये गर्व से कहते हैं, ढूंढने पर भी इन SC /ST और OBC वर्ग में जज बनने के लायक कोई योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं है.
संवैधानिक पदों पर बैठे ये जब इतना भी नहीं समझते कि ये क्या कह रहे हैं तो हमें तरस आता है. इनके द्वारा बहिष्कृत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को आज दुनिया पढ़ती और मानती है. विश्वविख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को विदेशों में पढ़ा जा रहा है. रेल मैनेजमेंट पर लालूजी दुनिया में सराहे जाते हैं और इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों में लेक्चर देने के लिये बुलाये जाते हैं, तो बहन मायावती को भारत में दलित समस्या और समाधान आदि विषयों पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है. कल “भारत में शराब मुक्त बिहार” विषय पर विदेशों के लोग आकर रिसर्च करेंगे. फिर भी इन्हें 85 प्रतिशत पिछड़ों में कोई जज बनने के लायक मिलता ही नहीं है. बिल्कुल गलत होते हुए भी अगर इनकी ही बात कुछ क्षण के लिए सही मान भी लें तो 60-70 वर्षों की आजादी के बाद भी देश की 85 प्रतिशत पिछड़ों को अयोग्य कहकर ये सम्राट अशोक के इस महान भारत देश का अपमान तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही अपनी योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं. क्योंकि आजादी के बाद हम 85 प्रतिशत अनपढ़, गंवार और अयोग्य पिछड़ों को योग्य बनाने की जिम्मेदारी भी तो बड़ी ही चालाकी से इन्होंने ही अपने माथे पर ले ली थी.
फिर भी इन्होंने 70 वर्षों के आजाद भारत में भी अपनी इस जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया और स्वयं को भी अपने बल-बुते खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाये कि विदेशों में जा-जाकर गिड़गिड़ाना ना पड़े. ये तो केवल मनुवादी व्यवस्था को ही मजबूत करने में उलझे रहे और आस्था और अंधविश्वास के मकड़जाल में 85 प्रतिशत पिछड़ों को फंसाये रखने की पूरी व्यवस्था कर डाली, जिससे करोड़ों इंसान भूमिहीन, गृहविहीन, बुद्धिहीन और कंगाल होता चला गया तो दूसरी तरफ इनके मंदिर-मठ मालामाल होते गए. समता, स्वतन्त्रता, भाईचारा और न्याय का युग समाप्त हो गया और हमारा भारत जो महात्मा बुद्ध के समय में दुनिया का विश्वगुरु कहलाता था. आज हर समस्याओं से जूझ रहा है और दुनियावालों की कतार में निचले पायदान पर भी झिलमिलाते हुए दिखता है. चीन और पाकिस्तान ये दोनों भी आंखे तरेर कर बातें करते हैं. रूस और अमेरिका भी अपने जंग लगे हथियारों की खपत के लिए भारत को अच्छा मार्केट समझकर हमारी पीठ थपथपाते रहते हैं और हम इसी में फुले नहीं समाते कि चलो ये हमसे हंस कर बोले और गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया. ठीक उसी तरह जैसे किसी छात्र से गुरूजी नाम पुकार कर पानी वगैरह कुछ मांगते तो वह बालक अति प्रसन्न होता कि गुरूजी उसे ही अधिक जानते-मानते हैं.
लेकिन वर्ण और जाति के घेरे में बुरी तरह से जकड़े ये समझने को तैयार हीं नहीं कि जिस देश की 85-90 प्रतिशत आबादी लुल्ही, लंगड़ी, अज्ञानी और हर तरह से कुंठित रहेगी तो देश कभी भी दुनियावालों के सामने सीना तानकर खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पायेगा. उसी तरह जब इस वर्ण और जाति प्रधान देश के न्यायालयों में भी सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिखेगा तो सबको समुचित न्याय नहीं मिल पायेगा और समुचित न्याय के अभाव में समाज कुंठित और अपाहिज बना रहेगा. इसलिए जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बिच का द्वन्द किसी भी ख्याल से न उचित है न संविधान सम्मत है, बल्कि संविधान को ठेंगा दिखाने जैसा है.
कॉलेजियम व्यवस्था से न्यायालयों में भी भाई-भतीजावाद बढ़ा है. अयोग्य और जातिवादी लोग जज बन रहे हैं. भ्रष्टाचार भी बढ़ते जा रहा है जिससे देश और दुनिया में हमारी पवित्र न्याय व्यवस्था की भी किरकिरी होने लगी है. इसलिये जरुरत है संविधान के अनुच्छेद 312 के आलोक में AIJS का गठन कर जितना जल्दी हो सके जजों की नियुक्ति प्रारम्भ कर दी जाय ताकि हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में भी योग्य जजों की नियुकि हो और सबको समुचित न्याय मिले तो दूसरी तरफ हमारी महान न्यायपालिका भी किरकिरी से बचे. इस काम में जितना विलम्ब हो रहा है और जिनकी वजह से हो रहा है वे लोग ही इस देश की महान जनता को न्याय देने में विलंब के दोषी हैं.
हमारी डेमोक्रेसी में हमारा पवित्र संविधान भी किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान, बलवान, धनवान, जज, कलक्टर और मंत्री ही क्यों न हो, उसे राजशाही के राजा और उसके अधिकारियों की तरह अहम और अहंकार के साथ कुछ बोलने या कुछ करने की इजाजत नहीं देता. यह अशोभनीय है कि आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के वकील से यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पांच सदस्यीय खंडपीठ का गठन कर कहा जाएगा कि सरकार को नया एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस) बनाने के आधार पर न्यायिक नियुक्तियों को बाधित करने का अधिकार नहीं है. क्या आप ऐसा चाहते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराज होकर कहा ” You may now as well close court rooms down and lock justice out… We don”t want to clash with you. But if you go on like this, we will form a ”Five-Judge Bench” and say you are scuttling appointments .” यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पक्ष या संस्थाएं अपनी संवैधानिक मार्यादाओं का ख्याल किये वगैर अपनी -अपनी जिद्द का ज्यादा ख्याल रख रही हैं. यहां जनता को न्याय देने की बात गौण दिखती हैं.
असल में हुआ यह है कि हाईकोर्ट में 86 नए जज, सुप्रीमकोर्ट में 04 जज और 14 हाईकोर्टों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं 4 मुख्य न्यायाधीशों और 33 हाईकोर्टों के जजों के तबादलों के मामलों को लेकर जो नाम सीजेआई की अध्यक्षतावाली कॉलेजियम द्वारा सरकार के पास भेजे गए थे. उसे सरकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके चयन के सम्बन्ध में विगत वर्ष दिसंबर 2015 में जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षतावाली पांच जजों की बेंच ने स्वीकार किया था. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिये चयन में जो प्रक्रिया CJI की अध्यक्षतावाली कॉलेजियम द्वारा अपनायी गयी थी उसमें बहुत सारी कमियां थीं. इसलिए जस्टिस खेहर की अध्यक्षतावाली बेंच ने सरकार को कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नया एमओपी बनाने का निर्देश दिया था. निर्देश के आलोक में सरकार ने नया एमओपी बनाकर 07 अगस्त 2016 को ही कॉलेजियम को भेज दिया था. लेकिन कॉलेजियम द्वारा शायद ढाई माह के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. क्यों? अगर यह बात सही है तो हम प्रबुद्ध जनों के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है. इसी बीच पांच जजों के संवैधानिक बेंच के निर्णय का उल्लंघन करते हुए सरकार द्वारा पुराने MOP के आधार पर ही 18 में 08 जजों के नामों की मंजूरी दे देने और 02 नामों को मंजूर करने पर विचार करने की भी बात प्रकाश में आई है. अगर यह भी सत्य है तो माना जाएगा कि सरकार ने ब्लंडर किया है. लेकिन क्यों अब आगे सरकार उस पुराने पैटर्न पर बहाली करना नहीं चाहती और क्यों 3 जजों की बेंच द्वारा औरों की तरह उसी गलत चयन प्रक्रिया के आधार पर कॉलेजियम द्वारा भेजे गए बाकी जजों के नामों को मंजूर करने पर जोर दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह तो और ब्लंडर है. सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच वर्तमान विवाद का यही कारण है. मेरी समझ से अगर मामले की तह में जाया जाय तो मिलेगा कि विवाद का मूल कारण कॉलेजियम द्वारा गलत प्रक्रिया के तहत तैयार कर सरकार को भेजी गयी सूची में से ही अपने-अपने मन मुताबिक जजों की नियुक्ति का है, जिसमें कुछ को सरकार ने कर लिया है और बाकी को सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है. लेकिन सचमुच में ऐसा हुआ है और आगे भी होनेवाला है, जो हाई लेवल जांच से ही पता चलेगा तो यह समाज और राष्ट्रहित के लिए घातक और निराशाजनक है.
विवाद के हल के लिए जरुरी है कि सबका साथ और सबके साथ न्याय के लिए AIJS का गठन कर ही जजों की बहाली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए और यदि इसमें कुछ बिलंब नजर आये तो एक समय सीमा तय की जाए तब तक के लिए संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत ही नियुक्ति और तबादला की कार्रवाई की जाए. क्योंकि कॉलेजियम से नियुक्ति जनता के लिए अन्यायपूर्ण, अहितकर और असंवैधानिक है.
लेखक वकील हैं. इनसे 9430574723 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों द्वारा बनायी गयी 3-4 हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों की कमिटी का नाम ही कॉलेजियम है. शुरू में सोचा गया कि यह व्यवस्था ”मोहि ले चल” की बिमारी से भिन्न होगी. लेकिन इसने भी ऐसा करना शुरू किया कि लोग कहने लगे ”चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास”. कलक्टर ही कलक्टर की बहाली, एसपी ही एसपी की बहाली और जज ही जज की बहाली करने लगेगा तो सुनने में तो बड़ा अजूबा लगेगा ही और यह न्यायसंगत और संविधान सम्मत भी नहीं है. बाबासाहेब का लिखा हुआ संविधान है जिसमें हर समस्याओं का समाधान है तो फिर कॉलेजियम ही क्यों?
संविधान से ऊपर कोई नहीं. न्यायपालिका भी नहीं. जब से पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिलने की व्यवस्था की गयी तब से जजों ने ही जजों की एक कॉलेजियम बनाकर हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम प्रारम्भ कर दिया. भारत जैसे जाति प्रधान डैमोक्रेटिक देश में जजों की नियुक्ति के लिए मनमाने तौर से कॉलेजियम जैसी व्यवस्था देश के माथे पर कलंक का एक काला धब्बा है. डॉ. लोहिया कहते थे सभी डैमोक्रेटिक संस्थाओं में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होना सबके हित में है. संविधान के अनुच्छेद 312 में IAS , IPS और IFS की तरह ऑल इन्डिया ज्यूडिशियल सर्विस (AIJS) की स्थापना का उपबंध करने की भी बात कही गयी है और इसके लिए 1976 में संविधान का 42वां संशोधन भी किया गया है. लेकिन आज तक AIJS का गठन नहीं किया गया. यह अच्छी बात है कि 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने हाईकोर्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर विज्ञान भवन दिल्ली के स्वर्णजयंती समारोह में सिविल सेवा की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने पर विचार करने को कहा है. देखिये क्या होता है?
अन्य सेवाओं की तरह अगर इसका भी गठन हो जाए तो जजों का भी मेरिट के आधार पर चयन होने लगेगा और सभी वर्गों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा जिससे हमारी ज्यूडिशियरी को भी विवाद रहित योग्य जज उपलबध होने लगेंगे. फिर कोई हमारी ज्यूडिशियरी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी उंगली नहीं उठाएगा. जनमानस को भी ज्यूडिशियरी की पारदर्शिता दिखने लगेगी. लेकिन विगत 70 वर्षों से इस सम्बन्ध में सवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और ना हीं होने दिया.
जहां तक मेरिट का सवाल है तो मेरिट किसी ख़ास वर्ग या जाति की जागीर नहीं. यह कहना और समझना विल्कुल बेईमानी है कि 85 प्रतिशत पिछड़ों में जज बनने की योग्यता नहीं है. अंग्रेज तो काफी योग्य थे. योग्यता ही सब कुछ है तो फिर अंग्रेजों को हटाने के लिये लाखों नागरिकों ने लहू क्यों बहाया? जबकि उनका किया गया कोई काम आज भी आपके काम से लाख गुना बेहतर है. आरक्षण का सम्बन्ध योग्यता से नहीं बल्कि शासन-प्रशासन में सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व से है और अब यह मामला हिस्सेदारी का भी बन गया है.
अगर मेरिट केवल ऊंची जाति की जागीर होती तो दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के किसी विश्वविद्यालय के नाम का नहीं होना, जबकि सभी विश्वविद्यालयों में 95 प्रतिशत ऊंची जाति के लोग ही व्याख्याता के साथ-साथ कुलपति भी हैं, यह प्रमाणित करता है कि ये लोग योग्य नहीं हैं. अगर ये योग्य ही होते और सारे जगत की बुद्धि का भण्डार इन्हीं के पास होता तो बच्चों के खिलौनों एवं इनके देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर सभी युद्धक हथियार तक विदेशों से आयात नहीं किये जाते और इसके लिये उनके चरणों में जाकर दांत नहीं निपोरने पड़ते. यही नहीं विश्वविद्यालयों में छात्रों-शिक्षकों को कानून की पुस्तकों सहित हर विषयों के अध्ययन-अध्यापन तक के लिए विदेशी पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता है. कहां चला गया इनका अपना ज्ञान? किसी विषय पर इनकी कोई पुस्तक नहीं जिसकी किसी एक पंक्ति को अपनी पुस्तकों में कोट करके दुनियावाले अपनी बात आगे बढ़ाते हों लेकिन ठीक इसके उलट ये लोग दुनियावालों को कोट किये वगैर कोई पुस्तक लिख ही नहीं सकते. मतलब किसी भी विषय पर इनकी कोई अपनी ओरिजीनालिटी नहीं है. न्यायपालिका में भी 95 प्रतिशत ऊंची जाति के ही योग्य जजों, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर आये दिन न्यायपालिका की हो रही किरकिरी से हम शर्मसार होते रहे हैं. फिर भी ये गर्व से कहते हैं, ढूंढने पर भी इन SC /ST और OBC वर्ग में जज बनने के लायक कोई योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं है.
संवैधानिक पदों पर बैठे ये जब इतना भी नहीं समझते कि ये क्या कह रहे हैं तो हमें तरस आता है. इनके द्वारा बहिष्कृत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को आज दुनिया पढ़ती और मानती है. विश्वविख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को विदेशों में पढ़ा जा रहा है. रेल मैनेजमेंट पर लालूजी दुनिया में सराहे जाते हैं और इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों में लेक्चर देने के लिये बुलाये जाते हैं, तो बहन मायावती को भारत में दलित समस्या और समाधान आदि विषयों पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है. कल “भारत में शराब मुक्त बिहार” विषय पर विदेशों के लोग आकर रिसर्च करेंगे. फिर भी इन्हें 85 प्रतिशत पिछड़ों में कोई जज बनने के लायक मिलता ही नहीं है. बिल्कुल गलत होते हुए भी अगर इनकी ही बात कुछ क्षण के लिए सही मान भी लें तो 60-70 वर्षों की आजादी के बाद भी देश की 85 प्रतिशत पिछड़ों को अयोग्य कहकर ये सम्राट अशोक के इस महान भारत देश का अपमान तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही अपनी योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं. क्योंकि आजादी के बाद हम 85 प्रतिशत अनपढ़, गंवार और अयोग्य पिछड़ों को योग्य बनाने की जिम्मेदारी भी तो बड़ी ही चालाकी से इन्होंने ही अपने माथे पर ले ली थी.
फिर भी इन्होंने 70 वर्षों के आजाद भारत में भी अपनी इस जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया और स्वयं को भी अपने बल-बुते खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाये कि विदेशों में जा-जाकर गिड़गिड़ाना ना पड़े. ये तो केवल मनुवादी व्यवस्था को ही मजबूत करने में उलझे रहे और आस्था और अंधविश्वास के मकड़जाल में 85 प्रतिशत पिछड़ों को फंसाये रखने की पूरी व्यवस्था कर डाली, जिससे करोड़ों इंसान भूमिहीन, गृहविहीन, बुद्धिहीन और कंगाल होता चला गया तो दूसरी तरफ इनके मंदिर-मठ मालामाल होते गए. समता, स्वतन्त्रता, भाईचारा और न्याय का युग समाप्त हो गया और हमारा भारत जो महात्मा बुद्ध के समय में दुनिया का विश्वगुरु कहलाता था. आज हर समस्याओं से जूझ रहा है और दुनियावालों की कतार में निचले पायदान पर भी झिलमिलाते हुए दिखता है. चीन और पाकिस्तान ये दोनों भी आंखे तरेर कर बातें करते हैं. रूस और अमेरिका भी अपने जंग लगे हथियारों की खपत के लिए भारत को अच्छा मार्केट समझकर हमारी पीठ थपथपाते रहते हैं और हम इसी में फुले नहीं समाते कि चलो ये हमसे हंस कर बोले और गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया. ठीक उसी तरह जैसे किसी छात्र से गुरूजी नाम पुकार कर पानी वगैरह कुछ मांगते तो वह बालक अति प्रसन्न होता कि गुरूजी उसे ही अधिक जानते-मानते हैं.
लेकिन वर्ण और जाति के घेरे में बुरी तरह से जकड़े ये समझने को तैयार हीं नहीं कि जिस देश की 85-90 प्रतिशत आबादी लुल्ही, लंगड़ी, अज्ञानी और हर तरह से कुंठित रहेगी तो देश कभी भी दुनियावालों के सामने सीना तानकर खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पायेगा. उसी तरह जब इस वर्ण और जाति प्रधान देश के न्यायालयों में भी सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिखेगा तो सबको समुचित न्याय नहीं मिल पायेगा और समुचित न्याय के अभाव में समाज कुंठित और अपाहिज बना रहेगा. इसलिए जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बिच का द्वन्द किसी भी ख्याल से न उचित है न संविधान सम्मत है, बल्कि संविधान को ठेंगा दिखाने जैसा है.
कॉलेजियम व्यवस्था से न्यायालयों में भी भाई-भतीजावाद बढ़ा है. अयोग्य और जातिवादी लोग जज बन रहे हैं. भ्रष्टाचार भी बढ़ते जा रहा है जिससे देश और दुनिया में हमारी पवित्र न्याय व्यवस्था की भी किरकिरी होने लगी है. इसलिये जरुरत है संविधान के अनुच्छेद 312 के आलोक में AIJS का गठन कर जितना जल्दी हो सके जजों की नियुक्ति प्रारम्भ कर दी जाय ताकि हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में भी योग्य जजों की नियुकि हो और सबको समुचित न्याय मिले तो दूसरी तरफ हमारी महान न्यायपालिका भी किरकिरी से बचे. इस काम में जितना विलम्ब हो रहा है और जिनकी वजह से हो रहा है वे लोग ही इस देश की महान जनता को न्याय देने में विलंब के दोषी हैं.
हमारी डेमोक्रेसी में हमारा पवित्र संविधान भी किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान, बलवान, धनवान, जज, कलक्टर और मंत्री ही क्यों न हो, उसे राजशाही के राजा और उसके अधिकारियों की तरह अहम और अहंकार के साथ कुछ बोलने या कुछ करने की इजाजत नहीं देता. यह अशोभनीय है कि आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के वकील से यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पांच सदस्यीय खंडपीठ का गठन कर कहा जाएगा कि सरकार को नया एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस) बनाने के आधार पर न्यायिक नियुक्तियों को बाधित करने का अधिकार नहीं है. क्या आप ऐसा चाहते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराज होकर कहा ” You may now as well close court rooms down and lock justice out… We don”t want to clash with you. But if you go on like this, we will form a ”Five-Judge Bench” and say you are scuttling appointments .” यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पक्ष या संस्थाएं अपनी संवैधानिक मार्यादाओं का ख्याल किये वगैर अपनी -अपनी जिद्द का ज्यादा ख्याल रख रही हैं. यहां जनता को न्याय देने की बात गौण दिखती हैं.
असल में हुआ यह है कि हाईकोर्ट में 86 नए जज, सुप्रीमकोर्ट में 04 जज और 14 हाईकोर्टों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं 4 मुख्य न्यायाधीशों और 33 हाईकोर्टों के जजों के तबादलों के मामलों को लेकर जो नाम सीजेआई की अध्यक्षतावाली कॉलेजियम द्वारा सरकार के पास भेजे गए थे. उसे सरकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके चयन के सम्बन्ध में विगत वर्ष दिसंबर 2015 में जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षतावाली पांच जजों की बेंच ने स्वीकार किया था. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिये चयन में जो प्रक्रिया CJI की अध्यक्षतावाली कॉलेजियम द्वारा अपनायी गयी थी उसमें बहुत सारी कमियां थीं. इसलिए जस्टिस खेहर की अध्यक्षतावाली बेंच ने सरकार को कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नया एमओपी बनाने का निर्देश दिया था. निर्देश के आलोक में सरकार ने नया एमओपी बनाकर 07 अगस्त 2016 को ही कॉलेजियम को भेज दिया था. लेकिन कॉलेजियम द्वारा शायद ढाई माह के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. क्यों? अगर यह बात सही है तो हम प्रबुद्ध जनों के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है. इसी बीच पांच जजों के संवैधानिक बेंच के निर्णय का उल्लंघन करते हुए सरकार द्वारा पुराने MOP के आधार पर ही 18 में 08 जजों के नामों की मंजूरी दे देने और 02 नामों को मंजूर करने पर विचार करने की भी बात प्रकाश में आई है. अगर यह भी सत्य है तो माना जाएगा कि सरकार ने ब्लंडर किया है. लेकिन क्यों अब आगे सरकार उस पुराने पैटर्न पर बहाली करना नहीं चाहती और क्यों 3 जजों की बेंच द्वारा औरों की तरह उसी गलत चयन प्रक्रिया के आधार पर कॉलेजियम द्वारा भेजे गए बाकी जजों के नामों को मंजूर करने पर जोर दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह तो और ब्लंडर है. सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच वर्तमान विवाद का यही कारण है. मेरी समझ से अगर मामले की तह में जाया जाय तो मिलेगा कि विवाद का मूल कारण कॉलेजियम द्वारा गलत प्रक्रिया के तहत तैयार कर सरकार को भेजी गयी सूची में से ही अपने-अपने मन मुताबिक जजों की नियुक्ति का है, जिसमें कुछ को सरकार ने कर लिया है और बाकी को सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है. लेकिन सचमुच में ऐसा हुआ है और आगे भी होनेवाला है, जो हाई लेवल जांच से ही पता चलेगा तो यह समाज और राष्ट्रहित के लिए घातक और निराशाजनक है.
विवाद के हल के लिए जरुरी है कि सबका साथ और सबके साथ न्याय के लिए AIJS का गठन कर ही जजों की बहाली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए और यदि इसमें कुछ बिलंब नजर आये तो एक समय सीमा तय की जाए तब तक के लिए संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत ही नियुक्ति और तबादला की कार्रवाई की जाए. क्योंकि कॉलेजियम से नियुक्ति जनता के लिए अन्यायपूर्ण, अहितकर और असंवैधानिक है.
लेखक वकील हैं. इनसे 9430574723 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. महादलितों के पूजा करने पर उच्च जाति के लोगों ने पीटा और घरों पर किया पथराव
 बिहार शरीफ। बिहार में लक्ष्मी पूजा करने पर उच्च जाति के लोगों ने रविवार को महादलितों को रोका. विरोध करने पर पिटाई की. उनके घरों पर पथराव किया. इससे गांव में तनाव बढ़ गया है. इसमें महादलितों के छह से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना के चलते पुलिस छावनी में गांव तब्दील हो गया है.
पुलिस के मुताबिक रविवार को महादलित लक्ष्मी पूजा के बाद प्रसाद वितरण कर रहे थे. इस दौरान गांव के दबंगों ने उन्हें रोका. इस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. उच्च जाति के लोगों ने महादलितों को पीटा और उनके घरों पर पथराव किया. इसमें महादलित परिवार की सुशीला देवी, बुलेटन पासवान, धर्मवीर कुमार, अजीत कुमार और लवली कुमारी घायल हो गए. इनका इलाज गांव के निजी क्लीनिक में कराया जा रहा है. विवाद बढ़ने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.
गांव में परंपरा चली रही थी कि मूर्ति स्थापित होने के बाद गांव में उसे घुमाया जाता है उसके बाद मूर्ति को मंदिर में स्थापित की जाती है. तनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित करा दिया और आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है.
पुत्र की नौकरी लगने पर दिया था मूर्ति का चंदा
महादलित परिवार की सुशीला देवी के पुत्र संतोष कुमार की सिपाही की नौकरी लगी थी. महिला ने मन्नत मांगी थी कि पुत्र की नौकरी होने पर वह लक्ष्मी की मूर्ति का खर्च देगी. महिला के पैसे से गांव में मूर्ति बिठाई गई. महिला जब अपने परिवार के साथ पूजा-अर्चना करने गई तो उच्च जाति के लोगों ने उसे पूजा करने और प्रसाद बांटने से मना कर दिया. इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को मार-पीटकर वहां से खदेड़ दिया गया.
पंचायत ने 2002 से लगा रखी थी पूजा पर रोक: महादलित परिवार के रविन्द्र रविदास ने बताया कि वर्ष 2002 में पूजा करने को लेकर उच्च जाति के लोगों ने गोलीबारी की थी. वे महादलित और दलित परिवारों को मंदिर में पूजा करने नहीं देते हैं. बवाल के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया था कि कोई भी महादलित परिवार मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होगा.
कायम रहेगी परंपरा, नहीं पूजा करने दूंगा: उच्च जाति के दिनेश सिंह, रविन्द्र यादव समेत अन्य ने बताया कि पूर्वजों के जमाने से गांव में यह परंपरा चली रही है कि महादलित को गांव के लक्ष्मी स्थान में पूजा नहीं करने दिया जाएगा. यह परंपरा कायम रहेगी. किसी के चंदा देने से क्या होता है. वे लोग महादलित को पूजा करने नहीं देंगे.
बिहार शरीफ। बिहार में लक्ष्मी पूजा करने पर उच्च जाति के लोगों ने रविवार को महादलितों को रोका. विरोध करने पर पिटाई की. उनके घरों पर पथराव किया. इससे गांव में तनाव बढ़ गया है. इसमें महादलितों के छह से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना के चलते पुलिस छावनी में गांव तब्दील हो गया है.
पुलिस के मुताबिक रविवार को महादलित लक्ष्मी पूजा के बाद प्रसाद वितरण कर रहे थे. इस दौरान गांव के दबंगों ने उन्हें रोका. इस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. उच्च जाति के लोगों ने महादलितों को पीटा और उनके घरों पर पथराव किया. इसमें महादलित परिवार की सुशीला देवी, बुलेटन पासवान, धर्मवीर कुमार, अजीत कुमार और लवली कुमारी घायल हो गए. इनका इलाज गांव के निजी क्लीनिक में कराया जा रहा है. विवाद बढ़ने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.
गांव में परंपरा चली रही थी कि मूर्ति स्थापित होने के बाद गांव में उसे घुमाया जाता है उसके बाद मूर्ति को मंदिर में स्थापित की जाती है. तनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित करा दिया और आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है.
पुत्र की नौकरी लगने पर दिया था मूर्ति का चंदा
महादलित परिवार की सुशीला देवी के पुत्र संतोष कुमार की सिपाही की नौकरी लगी थी. महिला ने मन्नत मांगी थी कि पुत्र की नौकरी होने पर वह लक्ष्मी की मूर्ति का खर्च देगी. महिला के पैसे से गांव में मूर्ति बिठाई गई. महिला जब अपने परिवार के साथ पूजा-अर्चना करने गई तो उच्च जाति के लोगों ने उसे पूजा करने और प्रसाद बांटने से मना कर दिया. इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को मार-पीटकर वहां से खदेड़ दिया गया.
पंचायत ने 2002 से लगा रखी थी पूजा पर रोक: महादलित परिवार के रविन्द्र रविदास ने बताया कि वर्ष 2002 में पूजा करने को लेकर उच्च जाति के लोगों ने गोलीबारी की थी. वे महादलित और दलित परिवारों को मंदिर में पूजा करने नहीं देते हैं. बवाल के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया था कि कोई भी महादलित परिवार मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होगा.
कायम रहेगी परंपरा, नहीं पूजा करने दूंगा: उच्च जाति के दिनेश सिंह, रविन्द्र यादव समेत अन्य ने बताया कि पूर्वजों के जमाने से गांव में यह परंपरा चली रही है कि महादलित को गांव के लक्ष्मी स्थान में पूजा नहीं करने दिया जाएगा. यह परंपरा कायम रहेगी. किसी के चंदा देने से क्या होता है. वे लोग महादलित को पूजा करने नहीं देंगे. महिलाओं को हर कदम पर देेनी पड़ती है अग्निपरीक्षा!
 इस महान देश में विवाह के माध्यम से पितृसत्ता का वर्चस्व तमाम रीति रिवाज, कायदा कानून से लेकर साहित्य और संस्कृति, धर्म कर्म में संस्थागत है. तो अब लगता है कि बलात्कार भी बहुत तेजी से विवाह की तरह संस्थागत है. अभी हाल में प्रदर्शित फिल्म पिंक में सामाजिक अनुशासन और मान्यताओं की धज्जियां उधेड़कर देहमुक्ति के जो कानूनी तर्क गढ़े गये हैं, वे सिरे से इस महादेश की औरतों की रोजमर्रे की जिंदगी में अप्रासंगिक हैं. ना कहने का अधिकार स्त्री को नहीं है. विवाह और बलात्कार दोनों स्थितियों में स्त्री की अग्निपरीक्षा होती है. मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम अंध-राष्ट्रवाद के आवाहन के मध्य अब हर औरत सीता है.
फिल्म में जितनी आसानी से मीनल ने अदालत में अपने मुक्त यौन संबंधों को स्वीकार किया है हकीकत की जमीन पर न समाज, न कानून व्यवस्था और न न्यापालिका के नजरिये में स्त्री की देह पर उसका कोई अधिकार स्वीकृत है. जिस महानायक ने मीनल के ना कहने के हक के बचाव में चीख चीखकर दलीलें दी हैं, उनके ही परिवार की बहू को भी बतौर अभिनेत्री फिल्मी चुंबन को लेकर उठे विवाद में मीनल की तरह दुनियाभर में सफाई देनी पड़ रही है. उसका परिवार उसके साथ नहीं है. महानायक इस मामले में मौन है, यही समाजिक यथार्थ है और रिअल और रील लाइफ का फर्क है, जहां स्त्री की छवि डर्टी पिक्चर है.
स्त्री के यौन संबंधों से लेकर ऑनरकीलिंग तक पंचायती और मजहबी सजा अदालत के दायरे से बाहर का किस्सा है. जहां मीनल की कोई सुनवाई असंभव है. परिवार, समाज और राष्ट्र का अनुशासन विशुद्ध मनुस्मृति राज है. उसका देह नीलामी पर है और विनिमय प्रचलित मुद्रा में हो, जरुरी नहीं है. विनियम अस्मिता और पहचान है तो कर्मकांड भी है. जो हमारी लोकसंस्कृति के राधा-कृष्ण प्रेम का जैसा तो कतई नहीं है और न कोई वैष्णव जीवनशैली है. हैसियत चाहे कुछ हो, जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. स्त्री को पल-पल अपना सतीत्व साबित करना पड़ता है. पीड़ित हो या शिकार, हर हाल में कटघरे में वही है. सारे गवाह उसके खिलाफ हैं. बलात्कार का रसायन शास्त्र यही है.
बलात्कार के मामलों में मर्द के चरित्र पर सवाल नहीं उठता है. बलात्कार के अभियोग के मामले में स्त्री का चरित्र सती सावित्री जैसा है या नहीं, अपराध साबित करने से पहले यह साबित करना जरुरी है. कोलकाता के पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड में पीड़ित स्त्री सुजेट मर गयी है, जिसे कानून और व्यवस्था ने लगातार चरित्रहीन ठहराने की कोशिश की. इसी दलील की आड़ में बलात्कारियों का बचाव होता रहा. मरने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला और बलात्कारी को लेकर मुंबई के होटल में रहकर उसके बचाव का रास्ता बताने वाली एक दूसरी स्त्री इस वक्त बांग्ला फिल्मों की टाप हिरोइन है, जिससे पूछताछ भी नहीं हुई है.
पूरा देश अब पिंक का सूरजकुंड थाना है. इंचार्ज महिला हो या मुख्यमंत्री महिला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. महिला सांसदों की हालत पति के लिए पंचायत प्रधानी से बेहतर नहीं है क्योंकि ज्यादातर स्त्रियां पति, पिता के राजनीतिक संबंधों और उनकी हैसियत के आधार पर संसद और विधानसभा में पहुंचती है. जिन्हें हम बखूब जानते हैं. संसद से सड़क तक स्त्री की नियति वहीं है जो जनमदुखिनी सीता की नियति रही है. हर हालात में वह गांधारी माता है. आंखें सही सलामत पर आंखों पर पितृसत्ता की अनिवार्य पट्टी काली पूजा की अमावस्या है. रक्तबीज की तरह तेजी से फल-फूल रहे बलात्कारियों को वह मां काली बनकर मार तो नहीं सकती लेकिन महिषासुर वध संभव है लेकिन इस पितृसत्ता के खिलाफ दसप्रहारधारिणी भी निशस्त्र बलिप्रदत्त है.
स्त्रीविरोधी इस पितृसत्ता को शरतचंद्र ने अपने उपन्यासों में खासकर चरित्रहीन और गृहदाह में बेनकाब किया है तो हाल में उत्पीड़न की शिकार स्त्री के चरित्र को लेकर दहन जैसी फिल्म भी बनी है. जिसमें उसका पति उसके खिलाफ है. यह एसिड हमलों का असल रसायन है. उदारता भी धार्मिक पाखंड है. सत्यजीत राय की फिल्म प्रतिद्वंद्वी में धंधा करती एक नर्स को दिखाने पर तमाम नर्सें शक के घेरे में आ गयी थीं तो मृणाल सेन की फिल्म एकदिन प्रतिदिन के बाद बंगाल में हर कामकाजी स्त्री का चरित्र पर सवाल उठने लगा था.
बांग्ला के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र एई समय की महिला क्राइम रिपोर्टर ने कालीपूजा के नाम जो तांडव चलाया है, उसमें से खुद के किसी तरह बच निकलने की आपबीती लिखी है. पत्रकार होने की वजह से टॉप के पुलिस प्रशासन के अफसरान के संपर्क के जरिये उन्हें फोन करके जिस तरह वह रात को अपने घर वापस लौटी, उसका ब्यौरा दिया है. फिर लिखा है कि किसी आम स्त्री या लड़की के लिए ऐसे नंबरों से संपर्क साधकर बचाव की कोई सूरत नहीं है तो उनकी हालत क्या होगी जबकि बलात्कार कार्निवाल धर्म और संस्कृति के नाम अखंड है. जिस पर कानून व्यवस्था का अंकिश नहीं है. यह विशिष्ट श्रेणी की कामकाजी महिलाओं की सार्वभौम आपबीती है.
बाकी स्त्री उत्पीड़न की वारदातों की जो बाढ़ है, वह अखबारों में सुर्खियां हैं. कोई संदेह नहीं है कि मीनल की जिरह के आधार पर पितृसत्ता स्त्री के ना कहने के अधिकार को मंजूर करें या नहीं, लेकिन इससे कामकाजी, परिवार से अलग रहने वाली औरतों की जीवनशैली को लेकर बलात्कारी पितृसत्ता के नजरिये के मुताबिक ऐसी हर स्त्री को मीनल की तरह जिरह का सामना देर सवेर करना ही होगा. यह मुक्तबाजार में पितृसत्ता का नया बलात्कारी तेवर है. जिसे हम अपनी सामंती सोच से देख ही नहीं पाते. राम ने रावण वध के बाद जिस सीता को जीता, वह अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अपने को सती साबित नहीं कर पायी और मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसे वनवास भेज दिया.
बलात्कार न थमने का कारण यही है कि बलात्कारी के बच निकलने के हजार रास्ते हैं. बलात्कार साबित हो तभी न सजा होगी. यहां तो मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है. बलात्कार की शिकार दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी स्त्रियों की आपबीती किसी भी तरह सामने नहीं आती, सुनवाई नहीं होती चीखों की और मामला तक दर्ज नहीं होता, तफतीश का सवाल ही नहीं होता. गायपट्टी और दक्षिणपंथी पितृसत्ता के शिकंजे में फंसे भूगोल का सच हम जानते हैं. जहां न्याय के रास्ते जाति, धर्म भी बहुत बड़ा अवरोध है. जाति और धर्म देखकर न्याय का रास्ता बनता बिगड़ता है. ऐसा किस्सा फेसबुक पर पल दर पल देस के कोने-कोने से दर्ज होता रहता है. किस किसको फर्क पड़ता है यह बताना मुश्किल है. स्त्री चेहरे और उसकी नर्म गोरी त्वचा का यह सबसे बड़ा खुला बाजार है.
इसके विपरीत तीन राज्यों में लंबे समय तक वामपंथी शासन रहा है. केरल में 1952 में कामरेड नंबूदरीपाद की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसे जवाहर लाल नेहरु ने बर्खास्त करवा दिया था. तबसे लेकर अब तक केरल में कम्युलिस्टों की सरकार बीच-बीच के अंतराल के बावजूद बनतकी रही है. बंगाल में 35 साल तक वाम शासन रहा है और त्रिपुरा में वाम दुर्ग अभी अटूट है. पितृसत्ता का वर्चस्व इन राज्यों में भी नहीं टूटा है. हमारी विचारधारा का यह सारा पाखंड भी स्त्रीविरोधी है.
स्त्री के हकूक के मामलों में जाति धर्म हैसियत के आर-पार राजनीतिक गोलबंदी के पीछे भी यह मर्दबादी सोच है. विचारधारा के नाम पर फिर कठमुल्लातंत्र को अखंड समर्थन है. यह सारी की सारी राजनीति मनुस्मृति का विस्तार है. बहरहाल, इस साल बंगाल में दुर्गापूजा से पहले से जो स्त्री आखेट जारी है. उसका सिलसिला दिवाली के बाद भी जारी है. धार्मिक कर्मकांड और उत्सव बलात्कार कार्निवाल में तब्दील है. 2011 को वामपंथी शासन खत्म होने के बाद बंगाल में स्त्री-उत्पीड़न बढ़ा है लेकिन नारीदेह की सीमा के आर-पार कुटीर उद्योग बने रहने का सिलसिला तो भारत विभाजन से लगातार जारी है. पार्टीबद्ध बलात्कार उत्सव का कैडरतंत्र सर्वदलीय है. जिसे सर्वदलीय राजनीतिक संरक्षण है. तो दूसरी ओर वामशासित केरल में कड़े कानूनों एवं जागरुकता अभियानों के बावजूद इस साल पिछले छह महीनों में बलात्कार के 910 मामले सामने आए हैं जो राज्य में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का संकेत हैं.
केरल पुलिस के अपराध आंकड़ों के अनुसार जुलाई तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 7909 मामले सामने आए. कुल मामलों में बलात्कार के 910 मामलों के अलावा छेड़खानी के 2332 मामले और बाकी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अन्य मामले थे. पिछले साल बलात्कार के 1263 मामले सामने आए थे. विडंबना यह कि वाम शासन में भी सामाजिक बदलाव कुछ नहीं हो रहा है. वैदिकी साहित्य में स्त्री को ना कहने पर देवताओं और ऋषियों को श्राप लगता था. उर्वशी को ना कहने के अपराध में अर्जुन को कुछ समय के लिए किन्नर भी बनना पड़ा. उसी वैदिकी संस्कृति के नाम पर स्त्री की इच्छा अनिच्छा का अब सर्वथा निषेध है.
मुक्त बाजार और पश्चिम की तरह लिव इन और फ्रीसेक्स की वातानुकूलित जीवनशैली में स्त्री उपभोक्ता सामग्री जरुर बनी है, गोरेपन का सौंदर्यबाजार आयुर्वेदिक विस्तार भी हुआ है. लेकिन स्त्री को इस सत्तावर्गीय विशेषाधिकार और जीवन के हर क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व के बावजूद विवाह और बलात्कार दोनों स्थितियों में न कहने का कोई अधिकार नहीं है. दहेज उत्पीड़न भी इसी पितृसत्ता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है.
हमारी प्रगतिशील विचारधारा भी उतनी ही सामंती है जितनी कि दक्षिणपंथी खाप पंचायतों की निरंतरता हर क्षेत्र में है. मनुस्मृति कि सिद्धांतो के तहत वाम दक्षिण किसी भी खेमे में स्त्री के हक हकूक के लिए कोई जगह नहीं है. सत्ता, राजनीति और कानून व्यवस्था बलात्कारी पितृसत्ता के पक्ष में है. केरल, बंगाल और त्रिपुरा में लंबे समय तक वाम शासन के दौरान यह पितृसत्ता ही मजबूत होती रही है, केरल और बंगाल में जारी बलात्कार कार्निवाल यही साबित करते हैं.
इस महान देश में विवाह के माध्यम से पितृसत्ता का वर्चस्व तमाम रीति रिवाज, कायदा कानून से लेकर साहित्य और संस्कृति, धर्म कर्म में संस्थागत है. तो अब लगता है कि बलात्कार भी बहुत तेजी से विवाह की तरह संस्थागत है. अभी हाल में प्रदर्शित फिल्म पिंक में सामाजिक अनुशासन और मान्यताओं की धज्जियां उधेड़कर देहमुक्ति के जो कानूनी तर्क गढ़े गये हैं, वे सिरे से इस महादेश की औरतों की रोजमर्रे की जिंदगी में अप्रासंगिक हैं. ना कहने का अधिकार स्त्री को नहीं है. विवाह और बलात्कार दोनों स्थितियों में स्त्री की अग्निपरीक्षा होती है. मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम अंध-राष्ट्रवाद के आवाहन के मध्य अब हर औरत सीता है.
फिल्म में जितनी आसानी से मीनल ने अदालत में अपने मुक्त यौन संबंधों को स्वीकार किया है हकीकत की जमीन पर न समाज, न कानून व्यवस्था और न न्यापालिका के नजरिये में स्त्री की देह पर उसका कोई अधिकार स्वीकृत है. जिस महानायक ने मीनल के ना कहने के हक के बचाव में चीख चीखकर दलीलें दी हैं, उनके ही परिवार की बहू को भी बतौर अभिनेत्री फिल्मी चुंबन को लेकर उठे विवाद में मीनल की तरह दुनियाभर में सफाई देनी पड़ रही है. उसका परिवार उसके साथ नहीं है. महानायक इस मामले में मौन है, यही समाजिक यथार्थ है और रिअल और रील लाइफ का फर्क है, जहां स्त्री की छवि डर्टी पिक्चर है.
स्त्री के यौन संबंधों से लेकर ऑनरकीलिंग तक पंचायती और मजहबी सजा अदालत के दायरे से बाहर का किस्सा है. जहां मीनल की कोई सुनवाई असंभव है. परिवार, समाज और राष्ट्र का अनुशासन विशुद्ध मनुस्मृति राज है. उसका देह नीलामी पर है और विनिमय प्रचलित मुद्रा में हो, जरुरी नहीं है. विनियम अस्मिता और पहचान है तो कर्मकांड भी है. जो हमारी लोकसंस्कृति के राधा-कृष्ण प्रेम का जैसा तो कतई नहीं है और न कोई वैष्णव जीवनशैली है. हैसियत चाहे कुछ हो, जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. स्त्री को पल-पल अपना सतीत्व साबित करना पड़ता है. पीड़ित हो या शिकार, हर हाल में कटघरे में वही है. सारे गवाह उसके खिलाफ हैं. बलात्कार का रसायन शास्त्र यही है.
बलात्कार के मामलों में मर्द के चरित्र पर सवाल नहीं उठता है. बलात्कार के अभियोग के मामले में स्त्री का चरित्र सती सावित्री जैसा है या नहीं, अपराध साबित करने से पहले यह साबित करना जरुरी है. कोलकाता के पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड में पीड़ित स्त्री सुजेट मर गयी है, जिसे कानून और व्यवस्था ने लगातार चरित्रहीन ठहराने की कोशिश की. इसी दलील की आड़ में बलात्कारियों का बचाव होता रहा. मरने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला और बलात्कारी को लेकर मुंबई के होटल में रहकर उसके बचाव का रास्ता बताने वाली एक दूसरी स्त्री इस वक्त बांग्ला फिल्मों की टाप हिरोइन है, जिससे पूछताछ भी नहीं हुई है.
पूरा देश अब पिंक का सूरजकुंड थाना है. इंचार्ज महिला हो या मुख्यमंत्री महिला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. महिला सांसदों की हालत पति के लिए पंचायत प्रधानी से बेहतर नहीं है क्योंकि ज्यादातर स्त्रियां पति, पिता के राजनीतिक संबंधों और उनकी हैसियत के आधार पर संसद और विधानसभा में पहुंचती है. जिन्हें हम बखूब जानते हैं. संसद से सड़क तक स्त्री की नियति वहीं है जो जनमदुखिनी सीता की नियति रही है. हर हालात में वह गांधारी माता है. आंखें सही सलामत पर आंखों पर पितृसत्ता की अनिवार्य पट्टी काली पूजा की अमावस्या है. रक्तबीज की तरह तेजी से फल-फूल रहे बलात्कारियों को वह मां काली बनकर मार तो नहीं सकती लेकिन महिषासुर वध संभव है लेकिन इस पितृसत्ता के खिलाफ दसप्रहारधारिणी भी निशस्त्र बलिप्रदत्त है.
स्त्रीविरोधी इस पितृसत्ता को शरतचंद्र ने अपने उपन्यासों में खासकर चरित्रहीन और गृहदाह में बेनकाब किया है तो हाल में उत्पीड़न की शिकार स्त्री के चरित्र को लेकर दहन जैसी फिल्म भी बनी है. जिसमें उसका पति उसके खिलाफ है. यह एसिड हमलों का असल रसायन है. उदारता भी धार्मिक पाखंड है. सत्यजीत राय की फिल्म प्रतिद्वंद्वी में धंधा करती एक नर्स को दिखाने पर तमाम नर्सें शक के घेरे में आ गयी थीं तो मृणाल सेन की फिल्म एकदिन प्रतिदिन के बाद बंगाल में हर कामकाजी स्त्री का चरित्र पर सवाल उठने लगा था.
बांग्ला के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र एई समय की महिला क्राइम रिपोर्टर ने कालीपूजा के नाम जो तांडव चलाया है, उसमें से खुद के किसी तरह बच निकलने की आपबीती लिखी है. पत्रकार होने की वजह से टॉप के पुलिस प्रशासन के अफसरान के संपर्क के जरिये उन्हें फोन करके जिस तरह वह रात को अपने घर वापस लौटी, उसका ब्यौरा दिया है. फिर लिखा है कि किसी आम स्त्री या लड़की के लिए ऐसे नंबरों से संपर्क साधकर बचाव की कोई सूरत नहीं है तो उनकी हालत क्या होगी जबकि बलात्कार कार्निवाल धर्म और संस्कृति के नाम अखंड है. जिस पर कानून व्यवस्था का अंकिश नहीं है. यह विशिष्ट श्रेणी की कामकाजी महिलाओं की सार्वभौम आपबीती है.
बाकी स्त्री उत्पीड़न की वारदातों की जो बाढ़ है, वह अखबारों में सुर्खियां हैं. कोई संदेह नहीं है कि मीनल की जिरह के आधार पर पितृसत्ता स्त्री के ना कहने के अधिकार को मंजूर करें या नहीं, लेकिन इससे कामकाजी, परिवार से अलग रहने वाली औरतों की जीवनशैली को लेकर बलात्कारी पितृसत्ता के नजरिये के मुताबिक ऐसी हर स्त्री को मीनल की तरह जिरह का सामना देर सवेर करना ही होगा. यह मुक्तबाजार में पितृसत्ता का नया बलात्कारी तेवर है. जिसे हम अपनी सामंती सोच से देख ही नहीं पाते. राम ने रावण वध के बाद जिस सीता को जीता, वह अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अपने को सती साबित नहीं कर पायी और मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसे वनवास भेज दिया.
बलात्कार न थमने का कारण यही है कि बलात्कारी के बच निकलने के हजार रास्ते हैं. बलात्कार साबित हो तभी न सजा होगी. यहां तो मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है. बलात्कार की शिकार दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी स्त्रियों की आपबीती किसी भी तरह सामने नहीं आती, सुनवाई नहीं होती चीखों की और मामला तक दर्ज नहीं होता, तफतीश का सवाल ही नहीं होता. गायपट्टी और दक्षिणपंथी पितृसत्ता के शिकंजे में फंसे भूगोल का सच हम जानते हैं. जहां न्याय के रास्ते जाति, धर्म भी बहुत बड़ा अवरोध है. जाति और धर्म देखकर न्याय का रास्ता बनता बिगड़ता है. ऐसा किस्सा फेसबुक पर पल दर पल देस के कोने-कोने से दर्ज होता रहता है. किस किसको फर्क पड़ता है यह बताना मुश्किल है. स्त्री चेहरे और उसकी नर्म गोरी त्वचा का यह सबसे बड़ा खुला बाजार है.
इसके विपरीत तीन राज्यों में लंबे समय तक वामपंथी शासन रहा है. केरल में 1952 में कामरेड नंबूदरीपाद की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसे जवाहर लाल नेहरु ने बर्खास्त करवा दिया था. तबसे लेकर अब तक केरल में कम्युलिस्टों की सरकार बीच-बीच के अंतराल के बावजूद बनतकी रही है. बंगाल में 35 साल तक वाम शासन रहा है और त्रिपुरा में वाम दुर्ग अभी अटूट है. पितृसत्ता का वर्चस्व इन राज्यों में भी नहीं टूटा है. हमारी विचारधारा का यह सारा पाखंड भी स्त्रीविरोधी है.
स्त्री के हकूक के मामलों में जाति धर्म हैसियत के आर-पार राजनीतिक गोलबंदी के पीछे भी यह मर्दबादी सोच है. विचारधारा के नाम पर फिर कठमुल्लातंत्र को अखंड समर्थन है. यह सारी की सारी राजनीति मनुस्मृति का विस्तार है. बहरहाल, इस साल बंगाल में दुर्गापूजा से पहले से जो स्त्री आखेट जारी है. उसका सिलसिला दिवाली के बाद भी जारी है. धार्मिक कर्मकांड और उत्सव बलात्कार कार्निवाल में तब्दील है. 2011 को वामपंथी शासन खत्म होने के बाद बंगाल में स्त्री-उत्पीड़न बढ़ा है लेकिन नारीदेह की सीमा के आर-पार कुटीर उद्योग बने रहने का सिलसिला तो भारत विभाजन से लगातार जारी है. पार्टीबद्ध बलात्कार उत्सव का कैडरतंत्र सर्वदलीय है. जिसे सर्वदलीय राजनीतिक संरक्षण है. तो दूसरी ओर वामशासित केरल में कड़े कानूनों एवं जागरुकता अभियानों के बावजूद इस साल पिछले छह महीनों में बलात्कार के 910 मामले सामने आए हैं जो राज्य में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का संकेत हैं.
केरल पुलिस के अपराध आंकड़ों के अनुसार जुलाई तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 7909 मामले सामने आए. कुल मामलों में बलात्कार के 910 मामलों के अलावा छेड़खानी के 2332 मामले और बाकी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अन्य मामले थे. पिछले साल बलात्कार के 1263 मामले सामने आए थे. विडंबना यह कि वाम शासन में भी सामाजिक बदलाव कुछ नहीं हो रहा है. वैदिकी साहित्य में स्त्री को ना कहने पर देवताओं और ऋषियों को श्राप लगता था. उर्वशी को ना कहने के अपराध में अर्जुन को कुछ समय के लिए किन्नर भी बनना पड़ा. उसी वैदिकी संस्कृति के नाम पर स्त्री की इच्छा अनिच्छा का अब सर्वथा निषेध है.
मुक्त बाजार और पश्चिम की तरह लिव इन और फ्रीसेक्स की वातानुकूलित जीवनशैली में स्त्री उपभोक्ता सामग्री जरुर बनी है, गोरेपन का सौंदर्यबाजार आयुर्वेदिक विस्तार भी हुआ है. लेकिन स्त्री को इस सत्तावर्गीय विशेषाधिकार और जीवन के हर क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व के बावजूद विवाह और बलात्कार दोनों स्थितियों में न कहने का कोई अधिकार नहीं है. दहेज उत्पीड़न भी इसी पितृसत्ता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है.
हमारी प्रगतिशील विचारधारा भी उतनी ही सामंती है जितनी कि दक्षिणपंथी खाप पंचायतों की निरंतरता हर क्षेत्र में है. मनुस्मृति कि सिद्धांतो के तहत वाम दक्षिण किसी भी खेमे में स्त्री के हक हकूक के लिए कोई जगह नहीं है. सत्ता, राजनीति और कानून व्यवस्था बलात्कारी पितृसत्ता के पक्ष में है. केरल, बंगाल और त्रिपुरा में लंबे समय तक वाम शासन के दौरान यह पितृसत्ता ही मजबूत होती रही है, केरल और बंगाल में जारी बलात्कार कार्निवाल यही साबित करते हैं. हिंदू त्यौहार और बहुजन समाज
 अभी-अभी दस दिनों का दशहरा बीता है. मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि दुर्गा कौन थीं और उनका महिषासुर के साथ क्या संबंध था और राजा महिषासुर ने दुर्गा का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसे मार डाला. और मार भी डाला तो नौ दिनों का वह क्रम क्या था और उन नौ दिनों में क्या हुआ था? क्योंकि समाज के एक बड़े हिस्से से अब यह सवाल भी उटने लगा है. मैं यह भी नहीं समझ पाता कि दशहरे में रामलीला क्यों दिखाते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि दुर्गा और महिषासुर के बीच नौ दिनों में जो हुआ था उसे लोगों को बतातें, तब जाकर दशहरा ज्यादा सार्थक होता.
मैं तो महज यह पूछना चाहता हूं कि जो ”भक्तजन” इन दस दिनों तक धूनी रमाए रहें आखिर उन्हें मिला क्या? क्या आपका धन बढ़ा, या फिर यश में वृद्धि हो गई या फिर रातों रात आपके सभी कष्ट दूर हो गए. यह सवाल इसलिए है क्योंकि हर काम करने के पीछे इंसान की कुछ मंशा, कोई चाहत तो रहती ही है. उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या हासिल हो गया. मैं यह सवाल इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों से इन नौ दिनों भक्ति में आकंठ डूबते रहे हैं लेकिन आज भी वहीं हैं, जहा एक दशक पहले तक थे. जाहिर है कि इंसान की उन्नति मेहनत से होती है ना कि किसी औऱ तरीके से.
ऐेसे ही आने वाले दिनों में दीपावली है. हिंदू धर्म के मुताबिक कथित तौर पर राम उस दिन अयोध्या लौटे थे तो दिपावली का पर्व मनाया जाता है. ठीक. मान लिया कि राम लौटे थे तो फिर लक्ष्मी को क्यों पूजते हो? वह अचानक से कहां से बीच में आ जाती है. तर्क करने पर लोग इसे साफ-सफाई से जोड़ कर देखने लगते हैं कि इसी बहाने घरों की ठीक से सफाई हो जाती है. इस तर्क पर बड़ी हंसी आती है; क्योंकि भारत इस मायने में अनोखा देश है जहां घरों की सफाई के लिए ”दीपावली” और ठीक से नहाने के लिए ”होली” का इंतजार किया जाता है. खैर, यह आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपकी इच्छा है, लेकिन यह बताओ कि उस एक रात में कथित तौर पर ”धन की देवी” के आगे रखे नोट दोगुने हुए या नहीं हुए?
अजब देश है भारत. यहां हर काम के लिए अलग देवता है. शक्ति के लिए अलग, धन के लिए अलग, ब्रह्मचर्य के लिए अलग, शादी कराने (अच्छा वर दिलाने) के लिए अगल, बारिश कराने के लिए अलग, पढ़ाई-लिखाई के लिए अलग, शुभ वाले अलग, अशुभ वाले अलग और तो और यहां भोग के लिए भी कामदेव जैसे देव हैं. और इतने सारे देवों के होने के बावजूद भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सूखा और बीमारी से बेहाल है. सवाल है कि जो लोग लाचार, बेरोजगार और बीमार है, क्या वो इस भगवान को नहीं मानते होंगे, फिर क्या आखिर इनके दुख क्यों नहीं दूर होते? सूखे से बर्बाद हुई फसलों को देख किसान रोज पेड़ों पर टंग जा रहे है फिर आखिर यह भगवान उन पर रहम कर उनके लिए बारिश क्यों नहीं कराता? शहीद भगत सिंह ने समाज में फैली इसी विषमता और गैरबराबरी को देखते हुए ईश्वर को मानने से इंकार कर दिया था और खुद को नास्तिक घोषित कर दिया था.
एक सवाल दलित/पिछड़े/आदिवासी समाज से है कि मंदिरों से लतिया कर भगा दिए जाने के बावजूद भी आप इसी ईश्वर को सालो से गोहराते रहे लेकिन देश का संविधान लागू होने से पहले करोड़ों भगवानों के इस देश में किसी इृकलौते ईश्वर ने भी आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ क्यों नहीं किया? आप गांवो के दक्षिण में पड़े सड़ते रहे, चमड़ा छीलते रहे, मैला, ढोते रहे, हल चलाते रहे, बेगार करते रहे, जूठन खाते रहे, बिन कपड़ों के रहे, बिना छत और बिस्तर के सोए, और यहां तक की गुलामी करते रहे तब चौरासी करोड़ ईश्वरों की यह फौज कहां थी? टीवी, बीवी, व्हाट्सएप और फेसबुक से वक्त नहीं मिले तो एक बार सोचिएगा जरूर और ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल नए हैं और आप लोग जानते नहीं हैं बल्कि आपलोग शतुर्मुग हो गए हैं जो अपने सर को रेत में धंसा कर ऑल इज वेल के मुगालत में जी रहे हैं.
बात बस इतनी भर है कि आपका भला किसमें है? तीर्थ करने में या फिर पढ़ाई कर नौकरी हासिल कर लेने में. क्योंकि आपकी जमीनों पर हजारों साल पहले किसी और ने कब्जा कर लिया है और आपके पास खाने भर का अनाज उगा लेने तक की जमीन नहीं है. दलित/पिछड़े/आदिवासी समाज में आपको सैकड़ों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनकी पिछली पीढ़ी के सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वर्तमान पीढ़ी वापस उसी अंधकार की ओर लौटने लगी है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मेहनत के जरिए खुद को सबल बनाने की बजाय ज्यादातर युवा धर्म और देवताओं पर निर्भर हो आर्शिवाद के जुगाड़ में लगे हैं. बंधु, आपको न तो आर्शिवाद मिला है और न ही आगे मिलने वाला है. इसलिए बेहतर यह होगा कि किसी धाम की ट्रेन पकड़िए. आपका उद्धार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ कर नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के माध्य से नौकरी हासिल कर के होगा. और नौकरी मंदिरों में नहीं बंटती, शायद इसीलिए बनाने वालों ने ”नौकरी दिलाने वाले” को ईश्वर को नहीं बनाया.
अभी-अभी दस दिनों का दशहरा बीता है. मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि दुर्गा कौन थीं और उनका महिषासुर के साथ क्या संबंध था और राजा महिषासुर ने दुर्गा का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसे मार डाला. और मार भी डाला तो नौ दिनों का वह क्रम क्या था और उन नौ दिनों में क्या हुआ था? क्योंकि समाज के एक बड़े हिस्से से अब यह सवाल भी उटने लगा है. मैं यह भी नहीं समझ पाता कि दशहरे में रामलीला क्यों दिखाते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि दुर्गा और महिषासुर के बीच नौ दिनों में जो हुआ था उसे लोगों को बतातें, तब जाकर दशहरा ज्यादा सार्थक होता.
मैं तो महज यह पूछना चाहता हूं कि जो ”भक्तजन” इन दस दिनों तक धूनी रमाए रहें आखिर उन्हें मिला क्या? क्या आपका धन बढ़ा, या फिर यश में वृद्धि हो गई या फिर रातों रात आपके सभी कष्ट दूर हो गए. यह सवाल इसलिए है क्योंकि हर काम करने के पीछे इंसान की कुछ मंशा, कोई चाहत तो रहती ही है. उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या हासिल हो गया. मैं यह सवाल इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों से इन नौ दिनों भक्ति में आकंठ डूबते रहे हैं लेकिन आज भी वहीं हैं, जहा एक दशक पहले तक थे. जाहिर है कि इंसान की उन्नति मेहनत से होती है ना कि किसी औऱ तरीके से.
ऐेसे ही आने वाले दिनों में दीपावली है. हिंदू धर्म के मुताबिक कथित तौर पर राम उस दिन अयोध्या लौटे थे तो दिपावली का पर्व मनाया जाता है. ठीक. मान लिया कि राम लौटे थे तो फिर लक्ष्मी को क्यों पूजते हो? वह अचानक से कहां से बीच में आ जाती है. तर्क करने पर लोग इसे साफ-सफाई से जोड़ कर देखने लगते हैं कि इसी बहाने घरों की ठीक से सफाई हो जाती है. इस तर्क पर बड़ी हंसी आती है; क्योंकि भारत इस मायने में अनोखा देश है जहां घरों की सफाई के लिए ”दीपावली” और ठीक से नहाने के लिए ”होली” का इंतजार किया जाता है. खैर, यह आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपकी इच्छा है, लेकिन यह बताओ कि उस एक रात में कथित तौर पर ”धन की देवी” के आगे रखे नोट दोगुने हुए या नहीं हुए?
अजब देश है भारत. यहां हर काम के लिए अलग देवता है. शक्ति के लिए अलग, धन के लिए अलग, ब्रह्मचर्य के लिए अलग, शादी कराने (अच्छा वर दिलाने) के लिए अगल, बारिश कराने के लिए अलग, पढ़ाई-लिखाई के लिए अलग, शुभ वाले अलग, अशुभ वाले अलग और तो और यहां भोग के लिए भी कामदेव जैसे देव हैं. और इतने सारे देवों के होने के बावजूद भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सूखा और बीमारी से बेहाल है. सवाल है कि जो लोग लाचार, बेरोजगार और बीमार है, क्या वो इस भगवान को नहीं मानते होंगे, फिर क्या आखिर इनके दुख क्यों नहीं दूर होते? सूखे से बर्बाद हुई फसलों को देख किसान रोज पेड़ों पर टंग जा रहे है फिर आखिर यह भगवान उन पर रहम कर उनके लिए बारिश क्यों नहीं कराता? शहीद भगत सिंह ने समाज में फैली इसी विषमता और गैरबराबरी को देखते हुए ईश्वर को मानने से इंकार कर दिया था और खुद को नास्तिक घोषित कर दिया था.
एक सवाल दलित/पिछड़े/आदिवासी समाज से है कि मंदिरों से लतिया कर भगा दिए जाने के बावजूद भी आप इसी ईश्वर को सालो से गोहराते रहे लेकिन देश का संविधान लागू होने से पहले करोड़ों भगवानों के इस देश में किसी इृकलौते ईश्वर ने भी आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ क्यों नहीं किया? आप गांवो के दक्षिण में पड़े सड़ते रहे, चमड़ा छीलते रहे, मैला, ढोते रहे, हल चलाते रहे, बेगार करते रहे, जूठन खाते रहे, बिन कपड़ों के रहे, बिना छत और बिस्तर के सोए, और यहां तक की गुलामी करते रहे तब चौरासी करोड़ ईश्वरों की यह फौज कहां थी? टीवी, बीवी, व्हाट्सएप और फेसबुक से वक्त नहीं मिले तो एक बार सोचिएगा जरूर और ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल नए हैं और आप लोग जानते नहीं हैं बल्कि आपलोग शतुर्मुग हो गए हैं जो अपने सर को रेत में धंसा कर ऑल इज वेल के मुगालत में जी रहे हैं.
बात बस इतनी भर है कि आपका भला किसमें है? तीर्थ करने में या फिर पढ़ाई कर नौकरी हासिल कर लेने में. क्योंकि आपकी जमीनों पर हजारों साल पहले किसी और ने कब्जा कर लिया है और आपके पास खाने भर का अनाज उगा लेने तक की जमीन नहीं है. दलित/पिछड़े/आदिवासी समाज में आपको सैकड़ों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनकी पिछली पीढ़ी के सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वर्तमान पीढ़ी वापस उसी अंधकार की ओर लौटने लगी है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मेहनत के जरिए खुद को सबल बनाने की बजाय ज्यादातर युवा धर्म और देवताओं पर निर्भर हो आर्शिवाद के जुगाड़ में लगे हैं. बंधु, आपको न तो आर्शिवाद मिला है और न ही आगे मिलने वाला है. इसलिए बेहतर यह होगा कि किसी धाम की ट्रेन पकड़िए. आपका उद्धार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ कर नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के माध्य से नौकरी हासिल कर के होगा. और नौकरी मंदिरों में नहीं बंटती, शायद इसीलिए बनाने वालों ने ”नौकरी दिलाने वाले” को ईश्वर को नहीं बनाया. केसरिया बौद्ध स्तूप की अनदेखी को लेकर बौद्ध संगठनों ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र
 चम्पारण। बिहार के चम्पारण में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप सुरक्षा एवं संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहा है. बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति, बुद्धगया के राष्ट्रीय संगठक आशाराम गौतम ने केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर भारत के राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री, जनशिकायत मंत्री, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और कई संबंधित विभागों को याचिका पत्र भेजी गई है.
इस याचिका पत्र में समिति ने 6 सदस्यी भ्रमण रिपोर्ट को आधार बनाकर केसरिया बौद्ध की कुछ तस्वीरों भी भेजी हैं. इन तस्वीरों में केसरिया बौद्ध स्तूप की दुर्दशा का साफ पता चला रहा है. अपने भ्रमण में बौद्ध प्रतिनिधिमंडल ने देखा कि दुनिया के सबसे ऊंचे केसरिया बौद्ध स्तूप के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है. तेज बारिश एवं धूप के कारण केसरिया बौद्ध स्तूप की दीवारें एवं ईंटें गिर रही हैं. केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा व संरक्षण में तैनात भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, असंवेदनशीलता के कारण केसरिया स्तूप के दक्षिणी हिस्से में जंगल एवं झाड़ियां उग आई हैं जिससे बारिश का पानी स्तूप में जा रहा है, जो कि स्तूप की दीवारों को कमजोर करता जा रहा है, जिससे मिट्टी ढह रही है और केसरिया बौद्ध स्तूप नष्ट हो रहा है. देश की प्राचीन विरासत केसरिया बौद्ध स्तूप के अस्तित्व को भयंकर खतरा पैदा हो गया है.
गौतम ने याचिका में कहा है कि बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले के गन्डक नदी के तट पर मोतिहारी से 35 किलोमीटर दूर ‘साहेबगंज-चकिया मार्ग’ पर केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है. बौद्ध धर्म के इतिहास में केसरिया बौद्ध स्तूप का प्रमुख स्थान है. कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर जाते समय एक रात केसरिया में गुजारी थी और लिच्छवियों को अपना भिक्षापात्र प्रदान किया था.
पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार केसरिया बौद्ध स्तूप दुनिया में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है. यह स्थान बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर और वैशाली से 30 किलोमीटर दूर है. मूलरूप से 150 फीट ऊंचे इस स्तूप की ऊंचाई सन् 1934 में आये भयानक भूकम्प से पहले 123 फीट थी, किन्तु वर्तमान समय में केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊँचाई 104 फीट है. बौद्ध जातक कथाओं में केसरिया बौद्ध स्तूप का वर्णन मिलता है. पर्यटन के साथ-साथ बौद्ध धम्म के इतिहास में केसरिया बौद्ध स्तूप का प्रमुख स्थान है. यहां आज भी प्रतिवर्ष लाखों बौद्ध तीर्थयात्री विश्व भर से दर्शन के लिए आते हैं
संगठन याचिका में विभिन्न सरकारी संस्थानों से अपी की है कि बौद्ध स्तूप के अस्तित्व को बचाने एवं स्थायी संरक्षण करने के लिए चारों तरफ “छायादार फाईबर शीट का प्लेटफार्म“ बनाकर केसरिया बौद्ध स्तूप को तेज बारिश एवं धूप से बचाया जाये. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन का गैरकानूनी अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण किया गया है, उसको तत्काल रद्द किया जाये और आगे जो भू-अतिक्रमण किया जा रहा है उसे तत्काल रोका जाये. केसरिया बौद्ध स्तूप के दर्शन करने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों, बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुलभ शौचालय, पीने के पानी की फिल्टर मशीन, खान-पान व्यवस्था एवं ‘पर्यटक गैस्ट हाऊस’ बनवाया जाये. देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए बिहार राज्य के अन्दर सभी प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थलों विशेषकर तथागत बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि महाविहार बुद्धगया, नालंदा, राजगीर, पाटलीपुत्र (पटना), वैशाली, केसरिया बौद्ध स्तूप आदि पर्यटन स्थलों के दर्शन के लिए “वातानुकूलित पर्यटक बस सेवा” शुरू की जाये.
चम्पारण। बिहार के चम्पारण में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप सुरक्षा एवं संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहा है. बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति, बुद्धगया के राष्ट्रीय संगठक आशाराम गौतम ने केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर भारत के राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री, जनशिकायत मंत्री, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और कई संबंधित विभागों को याचिका पत्र भेजी गई है.
इस याचिका पत्र में समिति ने 6 सदस्यी भ्रमण रिपोर्ट को आधार बनाकर केसरिया बौद्ध की कुछ तस्वीरों भी भेजी हैं. इन तस्वीरों में केसरिया बौद्ध स्तूप की दुर्दशा का साफ पता चला रहा है. अपने भ्रमण में बौद्ध प्रतिनिधिमंडल ने देखा कि दुनिया के सबसे ऊंचे केसरिया बौद्ध स्तूप के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है. तेज बारिश एवं धूप के कारण केसरिया बौद्ध स्तूप की दीवारें एवं ईंटें गिर रही हैं. केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा व संरक्षण में तैनात भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, असंवेदनशीलता के कारण केसरिया स्तूप के दक्षिणी हिस्से में जंगल एवं झाड़ियां उग आई हैं जिससे बारिश का पानी स्तूप में जा रहा है, जो कि स्तूप की दीवारों को कमजोर करता जा रहा है, जिससे मिट्टी ढह रही है और केसरिया बौद्ध स्तूप नष्ट हो रहा है. देश की प्राचीन विरासत केसरिया बौद्ध स्तूप के अस्तित्व को भयंकर खतरा पैदा हो गया है.
गौतम ने याचिका में कहा है कि बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले के गन्डक नदी के तट पर मोतिहारी से 35 किलोमीटर दूर ‘साहेबगंज-चकिया मार्ग’ पर केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है. बौद्ध धर्म के इतिहास में केसरिया बौद्ध स्तूप का प्रमुख स्थान है. कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर जाते समय एक रात केसरिया में गुजारी थी और लिच्छवियों को अपना भिक्षापात्र प्रदान किया था.
पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार केसरिया बौद्ध स्तूप दुनिया में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है. यह स्थान बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर और वैशाली से 30 किलोमीटर दूर है. मूलरूप से 150 फीट ऊंचे इस स्तूप की ऊंचाई सन् 1934 में आये भयानक भूकम्प से पहले 123 फीट थी, किन्तु वर्तमान समय में केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊँचाई 104 फीट है. बौद्ध जातक कथाओं में केसरिया बौद्ध स्तूप का वर्णन मिलता है. पर्यटन के साथ-साथ बौद्ध धम्म के इतिहास में केसरिया बौद्ध स्तूप का प्रमुख स्थान है. यहां आज भी प्रतिवर्ष लाखों बौद्ध तीर्थयात्री विश्व भर से दर्शन के लिए आते हैं
संगठन याचिका में विभिन्न सरकारी संस्थानों से अपी की है कि बौद्ध स्तूप के अस्तित्व को बचाने एवं स्थायी संरक्षण करने के लिए चारों तरफ “छायादार फाईबर शीट का प्लेटफार्म“ बनाकर केसरिया बौद्ध स्तूप को तेज बारिश एवं धूप से बचाया जाये. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन का गैरकानूनी अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण किया गया है, उसको तत्काल रद्द किया जाये और आगे जो भू-अतिक्रमण किया जा रहा है उसे तत्काल रोका जाये. केसरिया बौद्ध स्तूप के दर्शन करने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों, बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुलभ शौचालय, पीने के पानी की फिल्टर मशीन, खान-पान व्यवस्था एवं ‘पर्यटक गैस्ट हाऊस’ बनवाया जाये. देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए बिहार राज्य के अन्दर सभी प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थलों विशेषकर तथागत बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि महाविहार बुद्धगया, नालंदा, राजगीर, पाटलीपुत्र (पटना), वैशाली, केसरिया बौद्ध स्तूप आदि पर्यटन स्थलों के दर्शन के लिए “वातानुकूलित पर्यटक बस सेवा” शुरू की जाये. 1998 क्रिकेट विश्वकप का ये ”तेंदुलकर”आज चरा रहा हैं भैंस
 नई दिल्ली। हमारे देश में क्रिकेट का जुनून लगभग हर किसी के सिर चढ़ कर बोलता है. किसी भी क्रिकेटर के लिए विश्वकप में देश का प्रतिनिधित्व करना एक सपने का साकार होने जैसा होता है. ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं भालाजी डामोर. विश्वकप खेल कर भी ये आज भैंस चराने को मजबूर हैं.
इनका भी एक सपना था कि वह देश के लिए विश्वकप खेलें. 1998 के विश्वकप में उनका यह सपना सिर्फ पूरा हीं नहीं हुआ, बल्कि वह इस टुर्नामेंट के हीरो भी रहे. लेकिन, दुर्भाग्य से वह आज भैंस चराने के साथ-साथ कुछ छोटे-मोटे काम कर रहे हैं.
दरअसल, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप-1998 में इस ऑलराउंडर खिलाड़ी की बदौलत भारत सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब हो सका था. गुजरात के एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नेत्रहीन भालाजी को उम्मीद थी कि विश्वकप के बाद उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आयेगा, लेकिन दुर्भाग्य से विश्वकप 1998 के 18 वर्षो बाद आज यह होनहार एक-एक रुपये के लिये तरस रहा है.
अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भालाजी डामोर
अरावली जिले के पिपराणा गांव में भालाजी और उनके भाई की एक एकड़ जमीन है, लेकिन इतनी सी जमीन पर हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनका परिवार महीने के केवल 3000 रुपए कमा पाता है. एक कमरे के घर में परिवार के साथ रह रहे इस स्टार क्रिकेटर के करियर में मिले पुरस्कार और सर्टिफिकेट घर में जगह-जगह बिखरे पड़े हैं.
भालाजी डामोर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें…
– 38 वर्षीय इस ब्लाइंड क्रिकेटर का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. भालाजी के नाम आज भी भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.
– 125 मैचो में इस ऑलराउंडर ने 3,125 रन और 150 विकेट लिए हैं.
– पूरी तरह से दृष्टिबाधित इस क्रिकेटर ने भारत की तरफ से 8 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.
– भालाजी केवल एक कमरे वाले घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं. घर खर्च में उनका हाथ बंटाने के लिए उनकी पत्नी भी खेत में काम करती हैं.
एक अदद नौकरी की दरकार
भालाजी डामोर कहते हैं कि विश्वकप के बाद उम्मीद थी कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी. पर, कहीं नौकरी नहीं मिल सकी. स्पोर्ट्स कोटा और विकलांग कोटा मेरे किसी काम नहीं आ सके. भालाजी बेहद भारी मन से कहते हैं कि कई सालों बाद गुजरात सरकार ने उनका प्रशंसात्मक उल्लेख जरूर किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं है.
टीम के तेंदुलकर थे भालाजी
नेशनल एशोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर मेहता कहते हैं कि ””इंडियन ब्लाइंड टीम को भालाजी जैसा प्रतिभावान खिलाड़ी फिर नहीं मिला. विश्वकप के दौरान उसके साथी खिलाड़ी उसे सचिन तेंदुलकर कहकर बुलाते थे.””
बहरहाल, जिस देश में जहां एक तरफ रेगुलर क्रिकेटर्स को खूब सारी दौलत और शोहरत मिलती है, वहीं भालाजी जैसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर को अपनी तमाम प्रतिभाओं के बावजूद करियर समाप्त होने के बाद एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है.
(साभारः ईनाडू इंडिया)
नई दिल्ली। हमारे देश में क्रिकेट का जुनून लगभग हर किसी के सिर चढ़ कर बोलता है. किसी भी क्रिकेटर के लिए विश्वकप में देश का प्रतिनिधित्व करना एक सपने का साकार होने जैसा होता है. ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं भालाजी डामोर. विश्वकप खेल कर भी ये आज भैंस चराने को मजबूर हैं.
इनका भी एक सपना था कि वह देश के लिए विश्वकप खेलें. 1998 के विश्वकप में उनका यह सपना सिर्फ पूरा हीं नहीं हुआ, बल्कि वह इस टुर्नामेंट के हीरो भी रहे. लेकिन, दुर्भाग्य से वह आज भैंस चराने के साथ-साथ कुछ छोटे-मोटे काम कर रहे हैं.
दरअसल, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप-1998 में इस ऑलराउंडर खिलाड़ी की बदौलत भारत सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब हो सका था. गुजरात के एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नेत्रहीन भालाजी को उम्मीद थी कि विश्वकप के बाद उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आयेगा, लेकिन दुर्भाग्य से विश्वकप 1998 के 18 वर्षो बाद आज यह होनहार एक-एक रुपये के लिये तरस रहा है.
अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भालाजी डामोर
अरावली जिले के पिपराणा गांव में भालाजी और उनके भाई की एक एकड़ जमीन है, लेकिन इतनी सी जमीन पर हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनका परिवार महीने के केवल 3000 रुपए कमा पाता है. एक कमरे के घर में परिवार के साथ रह रहे इस स्टार क्रिकेटर के करियर में मिले पुरस्कार और सर्टिफिकेट घर में जगह-जगह बिखरे पड़े हैं.
भालाजी डामोर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें…
– 38 वर्षीय इस ब्लाइंड क्रिकेटर का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. भालाजी के नाम आज भी भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.
– 125 मैचो में इस ऑलराउंडर ने 3,125 रन और 150 विकेट लिए हैं.
– पूरी तरह से दृष्टिबाधित इस क्रिकेटर ने भारत की तरफ से 8 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.
– भालाजी केवल एक कमरे वाले घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं. घर खर्च में उनका हाथ बंटाने के लिए उनकी पत्नी भी खेत में काम करती हैं.
एक अदद नौकरी की दरकार
भालाजी डामोर कहते हैं कि विश्वकप के बाद उम्मीद थी कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी. पर, कहीं नौकरी नहीं मिल सकी. स्पोर्ट्स कोटा और विकलांग कोटा मेरे किसी काम नहीं आ सके. भालाजी बेहद भारी मन से कहते हैं कि कई सालों बाद गुजरात सरकार ने उनका प्रशंसात्मक उल्लेख जरूर किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं है.
टीम के तेंदुलकर थे भालाजी
नेशनल एशोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर मेहता कहते हैं कि ””इंडियन ब्लाइंड टीम को भालाजी जैसा प्रतिभावान खिलाड़ी फिर नहीं मिला. विश्वकप के दौरान उसके साथी खिलाड़ी उसे सचिन तेंदुलकर कहकर बुलाते थे.””
बहरहाल, जिस देश में जहां एक तरफ रेगुलर क्रिकेटर्स को खूब सारी दौलत और शोहरत मिलती है, वहीं भालाजी जैसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर को अपनी तमाम प्रतिभाओं के बावजूद करियर समाप्त होने के बाद एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है.
(साभारः ईनाडू इंडिया) बेकसूर दलित को पुलिस ने थाने में 6 दिनों तक दिया थर्ड डिग्री, ईलाज के दौरान मौत
 सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस के थर्ड डिग्री के कारण एक दलित की मौत हो जाने का मामला सामने आया है. मृतक के परिजन अब दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ये पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के हाहुर गांव का है. जहां 11 अक्टूबर को दलित परिवार के मुखिया गणेश साकेत नाम के वृद्ध की हत्या कर दी गई. जांच करने पर मामला जमीन का निकला.
दरअसल, गणेश की सिर्फ एक ही बेटी थी, ऐसे में उसकी मौत के बाद उसके नाम की पूरी जमीन बेटी कमसिलिया की हो जाती. इस जमीन पर पड़ोसी कल्लू साकेत और उसकी पत्नी की भी नजर थी, जिसके लिए उन्होंने गणेश की हत्या कर दी. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस बीच पुलिस ने कमसिलिया के पति रामसिया पर भी शक जाहिर किया और उसे छह दिनों की रिमांड पर ले लिया.
छह दिनों तक पुलिस ने उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोप है कि कमसिलिया ने जब अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाई तो टीआई आजाद खान ने उससे 30 हजार रुपए रिश्वत मांगी. अपने सुहाग को बचाने के लिए महिला ने ये राशि दे दी. रामसिया को जब छोड़ा गया तब तक पुलिस के थर्ड डिग्री से उसे काफी गंभीर चोटें आ चुकी थी. हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पति की मौत के बाद अब कमसिलिया टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है. दलित की मौत का मामला सामने आने के बाद रेगांव विधायक ऊषा चौधरी और अन्य दलित नेता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी पुलिसकर्मियों से जमकर बहस हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सतना एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को 10 हजार की राहत राशि देते हुए उनके बयान लिए. साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस के थर्ड डिग्री के कारण एक दलित की मौत हो जाने का मामला सामने आया है. मृतक के परिजन अब दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ये पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के हाहुर गांव का है. जहां 11 अक्टूबर को दलित परिवार के मुखिया गणेश साकेत नाम के वृद्ध की हत्या कर दी गई. जांच करने पर मामला जमीन का निकला.
दरअसल, गणेश की सिर्फ एक ही बेटी थी, ऐसे में उसकी मौत के बाद उसके नाम की पूरी जमीन बेटी कमसिलिया की हो जाती. इस जमीन पर पड़ोसी कल्लू साकेत और उसकी पत्नी की भी नजर थी, जिसके लिए उन्होंने गणेश की हत्या कर दी. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस बीच पुलिस ने कमसिलिया के पति रामसिया पर भी शक जाहिर किया और उसे छह दिनों की रिमांड पर ले लिया.
छह दिनों तक पुलिस ने उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोप है कि कमसिलिया ने जब अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाई तो टीआई आजाद खान ने उससे 30 हजार रुपए रिश्वत मांगी. अपने सुहाग को बचाने के लिए महिला ने ये राशि दे दी. रामसिया को जब छोड़ा गया तब तक पुलिस के थर्ड डिग्री से उसे काफी गंभीर चोटें आ चुकी थी. हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पति की मौत के बाद अब कमसिलिया टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है. दलित की मौत का मामला सामने आने के बाद रेगांव विधायक ऊषा चौधरी और अन्य दलित नेता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी पुलिसकर्मियों से जमकर बहस हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सतना एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को 10 हजार की राहत राशि देते हुए उनके बयान लिए. साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया. मनु की मूर्ति के विरोध में आंदोलन शुरू
 राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति स्थापित है, जबकि संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट के बाहर एक चौराहे के कोने में लगी हुई है. समाज में आज भी मनुस्मृति का शासन चलता दिखाई पड़ता है, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि मनु की मूर्ति हटाने और मनु स्मृति दहन जैसे प्रतीकात्मक कार्यवाहियों को पुन: हाथ में लिया जाये. इसी क्रम में 26 अक्टूबर को गुजरात उना दलित अत्याचार लड़त समिति के संयोजक जिग्नेश मेवाणी की मौजूदगी में जयपुर में जुटे मानवतावादी लोगों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है कि या तो मनुवाद रहेगा या मानवतावाद.
मेवाणी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अगर 56 इंच का सीना है और वह खुद को अम्बेडकर भक्त मानते है तो स्वयं मनु की मूर्ति को तोड़ें और उसका विरोध करें. उन्होंने कहा कि हम मनु की मूर्ति को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे. यह विरोध प्रदर्शन जयपुर में होगा. इस बैठक में फैसला लिया है कि अगामी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा. राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में लोग मनुस्मृति का दहन करेंगे और इसी दिन मनुस्मृति के खिलाफ यात्रा निकालेंगे. यह यात्रा 3 जनवरी 2017 को सावित्री बाई फुले जयंती के अवसर पर जयपुर पहुंचेगी. जहां पर मनु की मूर्ति के विरोध में महासम्मेलन और आक्रोश रैली आयोजित होगी.
गौरतलब है कि जिग्नेश मेवाणी नें उना आन्दोलन के दौरान मनु के पुतले के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की घोषणा की थी. जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि तमाम प्रगतिशील और अम्बेडकराइट ताकतों को दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होना चाहिये. इसी एकजुटता के निर्माण की दिशा में राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच सक्रिय है. समिति को उम्मीद है की राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग इस महासम्मेलन में शामिल होंगे.
राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति स्थापित है, जबकि संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट के बाहर एक चौराहे के कोने में लगी हुई है. समाज में आज भी मनुस्मृति का शासन चलता दिखाई पड़ता है, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि मनु की मूर्ति हटाने और मनु स्मृति दहन जैसे प्रतीकात्मक कार्यवाहियों को पुन: हाथ में लिया जाये. इसी क्रम में 26 अक्टूबर को गुजरात उना दलित अत्याचार लड़त समिति के संयोजक जिग्नेश मेवाणी की मौजूदगी में जयपुर में जुटे मानवतावादी लोगों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है कि या तो मनुवाद रहेगा या मानवतावाद.
मेवाणी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अगर 56 इंच का सीना है और वह खुद को अम्बेडकर भक्त मानते है तो स्वयं मनु की मूर्ति को तोड़ें और उसका विरोध करें. उन्होंने कहा कि हम मनु की मूर्ति को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे. यह विरोध प्रदर्शन जयपुर में होगा. इस बैठक में फैसला लिया है कि अगामी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा. राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में लोग मनुस्मृति का दहन करेंगे और इसी दिन मनुस्मृति के खिलाफ यात्रा निकालेंगे. यह यात्रा 3 जनवरी 2017 को सावित्री बाई फुले जयंती के अवसर पर जयपुर पहुंचेगी. जहां पर मनु की मूर्ति के विरोध में महासम्मेलन और आक्रोश रैली आयोजित होगी.
गौरतलब है कि जिग्नेश मेवाणी नें उना आन्दोलन के दौरान मनु के पुतले के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की घोषणा की थी. जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि तमाम प्रगतिशील और अम्बेडकराइट ताकतों को दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होना चाहिये. इसी एकजुटता के निर्माण की दिशा में राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच सक्रिय है. समिति को उम्मीद है की राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग इस महासम्मेलन में शामिल होंगे. संविधान में संशोधन पर्याप्त नहीं, समाज को सोच बदलने की जरूरत
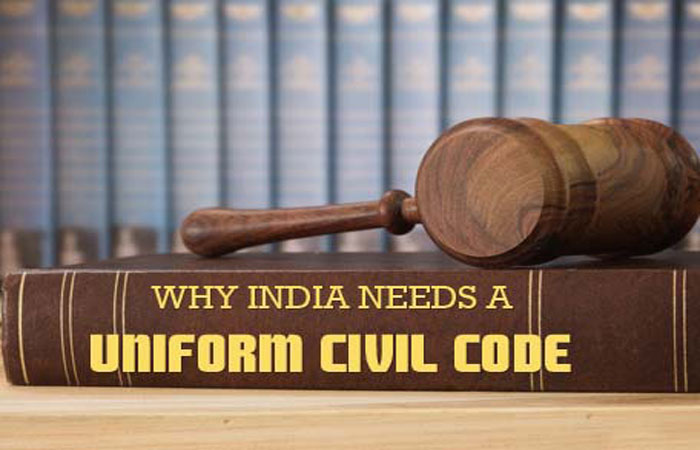 आज कल देश में समान नागरिक संहिता की बहस संसद से लेकर धर्मगुरूओं की पंचायत तक डिबेट का विषय बना हुआ है. लेकिन भारत में संविधान का कानून तो है, मगर जो संविधान धर्मनिरपेक्षता और अस्पृश्यता की बात करता है उसी देश में धर्म और जाति के नाम पर दंगे, हत्यायें और शोषण हो रहे हैं. इसका कारण धर्मों के कट्टर पंथी लोगों का समाज के बड़े हिस्से पर मानसिक रूप से पकड़. भारत का संविधान विश्व का सबसे बडा़ संविधान है. यहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं. ये जरूरी है कि एक देश के संविधान और एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे निवास करने वाले नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान संहिता अवश्य ही होनी चाहिए.
देश के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार दिए गये है. ये मूल अधिकार विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रतायें देश के नागरिकों को प्रदान करते हैं. लेकिन अधिकारों के साथ-साथ भाग 4क के अनुच्छेद 51क में मूल कर्तवय भी दिये गये हैं. देश में समस्याएं इसलिए भी पैदा हो रही हैं कि हम अधिकारों की मांग तो करते हैं मगर कर्तव्यों को नकार देते हैं. मुस्लिम समाज में ज्यादातर सरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून अभी तक हावी रहा है. तलाक के लिए मात्र तीन बार तलाक-तलाक कहकर तलाक को स्वीकार करना संविधान के दायरे से बाहर का कानून है, जिसको अवश्य ही संविधान के कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.
सिर्फ कानून बनाकर और संविधान में संशोधन करके समाज और देश में परिवर्तन नहीं लाया सकता. लोगों को भी अपनी सोच बदलने होग. लोगों को अपनी संकीर्ण मानसिकता में संशोधन कर संविधान के अनुरूप आचरण और व्यवहार करने की जरूरत है. आज मुस्लिम धर्म के लिए समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय बना हुआ है. ये भी हकीकत है कि संविधान में पहले जो 6 मूल अधिकार दिये गये हैं क्या आजादी के 69 वर्ष बाद भी इन कानूनों का क्या हिंदू धर्म के समाज ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन किया है? अनुच्छेद “17” अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बना है. मगर अस्पृश्यता के कारण यहां शहीदों को भी जलाने के लिए दो गज जमीन नसीब नहीं होती है. जबकि अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म-स्थान या इनसे किसी भी आाधार पर विभेद न करें.
आज भी देश में महिलाओं को वो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से हांसिल नहीं हुए हैं. महिलाओं को मंदिर प्रवेश से रोका जाता है. वंचित वर्ग जिसको दलित की उपाधि से नवाजा गया है मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च में तो जा सकता है मगर मंदिर में नहीं. कानून में दहेज देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं मगर देश में हर वर्ष हजारों दुल्हनें उत्पीड़न का शिकार होती हैं. हजारों की निर्मम हत्या कर दी जाती है. ये समाज की संकीर्ण सोच ही तो है. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सन 1994 में एक अधिनियम बनाया गया जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग की जांच करना या करवाना कानूनन अपराध है. मगर इस कानून को भी लोगों ने धन कमाने का जरिया बना लिया है. समाज की संवेदनहीनता के कारण आये दिन कूडे़दानों, झाड़ियों, और नालियों में कन्याभ्रूण फेंक दिये जाते हैं. ये सब हमारी परंपरागत धर्मिक मान्यताओं का ही कारण है जो समाज में बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे कुल का वारिस समझा जाता है. बेटियों को अलग समझा जाता है.
हम संविधान से अधिकारों की ही अपेक्षा रखते हैं पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वास को त्यागना नहीं चाहते. दूसरी बात भारत की वर्तमान राजनीति भी समाज में परिवर्तन को जल्दी नहीं देखना चाहती है. कारण स्पष्ट है कि चुनावी मुद्दों के लिए जाति और धर्म ही एक मात्र सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन चुकी है. एक और कड़वा सच ये भी है कि राजनीति में साधुओं, धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों, को दखल नहीं करनी चाहिए. विज्ञान और तकनीक के युग में देश के युवाओं को बौद्धिक रूप से सशक्त करने, अंधविश्वास से दूर रहने तथा महिलाओं और वंचितों को बराबरी के अधिकार देने हेतु आहवान करने की जरूरत है. सिर्फ हिंदू-हिंदू और इस्लाम-इस्लाम रटाकर देश 21 सवीं सदी के विज्ञान के मुहाने पर खडा़ नहीं हो सकता. अब्दुल कलाम साहब के सपनों का भारत नहीं बन सकता. इसके लिए हम सब को मिलकर रूढी़वाद से लड़ना होगा. भ्रष्टाचार से लड़ना होगा. जातिवाद को खत्म करना होगा. सिर्फ और सिर्फ संविधान के आदर्शों और समाज सुधारकों के आदर्शों पर चलने के लिए नई चेतना देश में जगानी होगी. अन्यथा संविधान में चाहे कितने संशोधन कर नये कानून बनाये जायें, जब तक भारतीय समाज रूढ़ियों और फतवाओं से ऊपर उठ कर अपनी सोच में बदलाव नहीं कर लेता कानून बनाना सार्थक नहीं हो सकता.
आज कल देश में समान नागरिक संहिता की बहस संसद से लेकर धर्मगुरूओं की पंचायत तक डिबेट का विषय बना हुआ है. लेकिन भारत में संविधान का कानून तो है, मगर जो संविधान धर्मनिरपेक्षता और अस्पृश्यता की बात करता है उसी देश में धर्म और जाति के नाम पर दंगे, हत्यायें और शोषण हो रहे हैं. इसका कारण धर्मों के कट्टर पंथी लोगों का समाज के बड़े हिस्से पर मानसिक रूप से पकड़. भारत का संविधान विश्व का सबसे बडा़ संविधान है. यहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं. ये जरूरी है कि एक देश के संविधान और एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे निवास करने वाले नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान संहिता अवश्य ही होनी चाहिए.
देश के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार दिए गये है. ये मूल अधिकार विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रतायें देश के नागरिकों को प्रदान करते हैं. लेकिन अधिकारों के साथ-साथ भाग 4क के अनुच्छेद 51क में मूल कर्तवय भी दिये गये हैं. देश में समस्याएं इसलिए भी पैदा हो रही हैं कि हम अधिकारों की मांग तो करते हैं मगर कर्तव्यों को नकार देते हैं. मुस्लिम समाज में ज्यादातर सरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून अभी तक हावी रहा है. तलाक के लिए मात्र तीन बार तलाक-तलाक कहकर तलाक को स्वीकार करना संविधान के दायरे से बाहर का कानून है, जिसको अवश्य ही संविधान के कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.
सिर्फ कानून बनाकर और संविधान में संशोधन करके समाज और देश में परिवर्तन नहीं लाया सकता. लोगों को भी अपनी सोच बदलने होग. लोगों को अपनी संकीर्ण मानसिकता में संशोधन कर संविधान के अनुरूप आचरण और व्यवहार करने की जरूरत है. आज मुस्लिम धर्म के लिए समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय बना हुआ है. ये भी हकीकत है कि संविधान में पहले जो 6 मूल अधिकार दिये गये हैं क्या आजादी के 69 वर्ष बाद भी इन कानूनों का क्या हिंदू धर्म के समाज ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन किया है? अनुच्छेद “17” अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बना है. मगर अस्पृश्यता के कारण यहां शहीदों को भी जलाने के लिए दो गज जमीन नसीब नहीं होती है. जबकि अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म-स्थान या इनसे किसी भी आाधार पर विभेद न करें.
आज भी देश में महिलाओं को वो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से हांसिल नहीं हुए हैं. महिलाओं को मंदिर प्रवेश से रोका जाता है. वंचित वर्ग जिसको दलित की उपाधि से नवाजा गया है मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च में तो जा सकता है मगर मंदिर में नहीं. कानून में दहेज देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं मगर देश में हर वर्ष हजारों दुल्हनें उत्पीड़न का शिकार होती हैं. हजारों की निर्मम हत्या कर दी जाती है. ये समाज की संकीर्ण सोच ही तो है. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सन 1994 में एक अधिनियम बनाया गया जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग की जांच करना या करवाना कानूनन अपराध है. मगर इस कानून को भी लोगों ने धन कमाने का जरिया बना लिया है. समाज की संवेदनहीनता के कारण आये दिन कूडे़दानों, झाड़ियों, और नालियों में कन्याभ्रूण फेंक दिये जाते हैं. ये सब हमारी परंपरागत धर्मिक मान्यताओं का ही कारण है जो समाज में बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे कुल का वारिस समझा जाता है. बेटियों को अलग समझा जाता है.
हम संविधान से अधिकारों की ही अपेक्षा रखते हैं पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वास को त्यागना नहीं चाहते. दूसरी बात भारत की वर्तमान राजनीति भी समाज में परिवर्तन को जल्दी नहीं देखना चाहती है. कारण स्पष्ट है कि चुनावी मुद्दों के लिए जाति और धर्म ही एक मात्र सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन चुकी है. एक और कड़वा सच ये भी है कि राजनीति में साधुओं, धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों, को दखल नहीं करनी चाहिए. विज्ञान और तकनीक के युग में देश के युवाओं को बौद्धिक रूप से सशक्त करने, अंधविश्वास से दूर रहने तथा महिलाओं और वंचितों को बराबरी के अधिकार देने हेतु आहवान करने की जरूरत है. सिर्फ हिंदू-हिंदू और इस्लाम-इस्लाम रटाकर देश 21 सवीं सदी के विज्ञान के मुहाने पर खडा़ नहीं हो सकता. अब्दुल कलाम साहब के सपनों का भारत नहीं बन सकता. इसके लिए हम सब को मिलकर रूढी़वाद से लड़ना होगा. भ्रष्टाचार से लड़ना होगा. जातिवाद को खत्म करना होगा. सिर्फ और सिर्फ संविधान के आदर्शों और समाज सुधारकों के आदर्शों पर चलने के लिए नई चेतना देश में जगानी होगी. अन्यथा संविधान में चाहे कितने संशोधन कर नये कानून बनाये जायें, जब तक भारतीय समाज रूढ़ियों और फतवाओं से ऊपर उठ कर अपनी सोच में बदलाव नहीं कर लेता कानून बनाना सार्थक नहीं हो सकता.
दलितों को राजनीति में मोहरा बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल
 नई दिल्ली। धर्म, भाषा और जाति के आधार पर वोट मांगने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को जाति और भाषाई आधार पर वोट मांगने पर सवाल पूछे. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने पूछा, कोई उम्मीदवार दलितों के विकास की बात कहकर वोट मांग सकता है या नहीं? क्या यह गलत तरीका माना जाएगा? एक कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दलितों के विकास के नाम पर वोट मांगना सही है. दलितों को संविधान के तहत संरक्षण मिला है. बहुत सी जगहों पर राजनीतिक दल दलितों के विकास को चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं.
चीफ जस्टिस ने पूछा कि किसी भाषा विशेष के लोगों के विकास की बात कहकर वोट मांगने को क्या कहेंगे? जैसे महाराष्ट्र में मराठी-हिंदी विवाद. इस पर सिब्बल ने बताया कि किसी एक भाषा के लोगों के विकास पर वोट मांगने को लेकर कानून स्पष्ट नहीं है. इस मुद्दे पर निर्णय संवैधानिक पीठ को करना है. उन्होंने बताया कि अगर कोई नेता दलित समाज से जुड़ा होने के आधार पर वोट मांगता है तो आरपी एक्ट की धारा 123 के तहत यह गलत है. सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.
चीफजस्टिस ने पूछा कि सोशल मीडिया के जरिये मतदाताओं को लुभाने पर क्या कानून लागू होता है? इस पर सिब्बल ने बताया कि किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट या किसी अन्य द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है. ऐसे में चुनाव रद्द करना चाहिए. हालांकि, चुनाव में सोशल मीडिया या इंटरनेट के प्रयोग पर रोक की बात कानून में नहीं है. इंटरनेट के जमाने में उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी धर्म के नाम पर वोटरों को लुभा सकता है. ऐसे में संविधान पीठ इंटरनेट पर चुनाव के लिए धर्म के प्रयोग पर रोक लगाने पर भी विचार करें.
नई दिल्ली। धर्म, भाषा और जाति के आधार पर वोट मांगने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को जाति और भाषाई आधार पर वोट मांगने पर सवाल पूछे. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने पूछा, कोई उम्मीदवार दलितों के विकास की बात कहकर वोट मांग सकता है या नहीं? क्या यह गलत तरीका माना जाएगा? एक कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दलितों के विकास के नाम पर वोट मांगना सही है. दलितों को संविधान के तहत संरक्षण मिला है. बहुत सी जगहों पर राजनीतिक दल दलितों के विकास को चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं.
चीफ जस्टिस ने पूछा कि किसी भाषा विशेष के लोगों के विकास की बात कहकर वोट मांगने को क्या कहेंगे? जैसे महाराष्ट्र में मराठी-हिंदी विवाद. इस पर सिब्बल ने बताया कि किसी एक भाषा के लोगों के विकास पर वोट मांगने को लेकर कानून स्पष्ट नहीं है. इस मुद्दे पर निर्णय संवैधानिक पीठ को करना है. उन्होंने बताया कि अगर कोई नेता दलित समाज से जुड़ा होने के आधार पर वोट मांगता है तो आरपी एक्ट की धारा 123 के तहत यह गलत है. सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.
चीफजस्टिस ने पूछा कि सोशल मीडिया के जरिये मतदाताओं को लुभाने पर क्या कानून लागू होता है? इस पर सिब्बल ने बताया कि किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट या किसी अन्य द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है. ऐसे में चुनाव रद्द करना चाहिए. हालांकि, चुनाव में सोशल मीडिया या इंटरनेट के प्रयोग पर रोक की बात कानून में नहीं है. इंटरनेट के जमाने में उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी धर्म के नाम पर वोटरों को लुभा सकता है. ऐसे में संविधान पीठ इंटरनेट पर चुनाव के लिए धर्म के प्रयोग पर रोक लगाने पर भी विचार करें. जन्मदिन विशेषः राष्ट्रपति रहते हुए नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में दलितों के प्रवेश का रास्ता खोला
 डॉ. के.आर. नारायणन का प्रारंभिक जीवन अनेक कठिनाइयों, निर्धनता और अभावों से भरा हुआ था. किंतु आपके धैर्य, विश्वास और संघर्ष के कारण उन्होंने हर बाधा पर जीत हासिल कर ली. उनके बचपन का नाम कोचिरिल राम नारायणन था. उनका जन्म केरल राज्य के पूर्व रियासत त्रावणकोर में कोट्यम जिले में स्थित उझाउर गांव में 27 अक्टूबर, 1920 को हुआ था. उनके पिता का नाम रामन वैद्यन था. उनके पिता एवं दादा दोनों आयुर्वेदिक चिकित्सक थे. समाज में उनके पिता की एक सम्मानित पहचान थी. हालांकि परिवार के सामने आर्थिक तंगी हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उनके पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं थे. लेकिन नारायणन की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मां, बहन और भाई ने उन्हें आगे पढ़ाने का निश्चय किया.
छह साल के होने पर नारायणन का दाखिला गांव से चार किलोमीटर दूर स्थित स्थानीय स्कूल में करवा दिया गया. हाई स्कूल के लिए उन्होंने कूराविले गेड़ स्कूल में दाखिला लिया. बाद में अपनी योग्यता के बल पर वह छात्रवृति हासिल करने लगे. उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता उच्च शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ना है. इस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण किया. सन् 1945 में नारायणन ने त्रावणकोर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज, तिरुअनंतपुरम से 60 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी आनर्स में बी.ए की परीक्षा पास की. इसी कॉलेज से 1948 में उन्होंने प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिविजन) से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए पास किया. एम.ए पास करने के बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज में ही अंग्रेजी प्रवक्ता (लेक्चरार) पद के लिए आवेदन किया. लेकिन त्रावणकोर के दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने नारायणन को प्रवक्ता की बजाय क्लर्क के पद पर काम करने को कहा गया. अय्यर के मन में तब जातीय दंभ था और यह विद्वेष की एक दलित आखिरकार प्रवक्ता कैसे हो सकता है. स्वाभिमानी नारायणन ने क्लर्क की नौकरी लेने से साफ मना कर दिया और इसके ठीक बाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विरोधस्वरूप बी.ए की डिग्री लेने से मना कर दिया.
लेकिन चार दशक बाद सन् 1992 में भारत का उपराष्ट्रपति बनने पर उनके गृह राज्य केरल में केरल विश्वविद्यालय के उसी सीनेट में उनका जोरदार स्वागत किया गया, तब उऩ्होंने अपनी बी.ए की डिग्री ली. उस दौरान तात्कालिक जातिवादियों पर तंज कसते हुए के.आर.नारायणन ने कहा, “आज मुझे उन महापुरुषों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने दलित होने के कारण इस विश्वविद्यालय में मुझे प्रवक्ता बनने से वंचित कर दिया था. हालांकि उन्होंने मुझे प्रवक्ता पद पर नहीं चुन कर अच्छा ही किया क्योंकि तब शायद आज मुझे उप राष्ट्रपति बनने का सुनहरा अवसर नहीं मिलता. और न ही केरल राज्य को यह गौरव मिलता. मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं.”
सन् 1948 में एम.ए करने और प्रवक्ता की नौकरी नहीं मिलने के बाद के. आर. नारायणन दिल्ली में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर से मिलने गए. बाबासाहेब वायसराय की काउंसिल में श्रम विभाग के सदस्य थे. नारायणन की योग्यता को देखते हुए बाबासाहेब ने उन्हें दिल्ली में ही भारत ओवरसीज विभाग जिसे अब विदेश विभाग कहा जाता है में 250 रुपये प्रतिमाह पर सरकारी नौकरी दिलवा दी. लेकिन अपनी साहित्यिक रुचि के कारण के.आर. नारायणन पत्रकार बनना चाहते थे इसलिए बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़ कर सौ रुपये प्रतिमाह वेतन पर साप्ताहिक पत्रिका ‘इकॉनामिक्स वीकली ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री’में बतौर पत्रकार नौकरी ज्वाइन कर लिया. बाद में वह कई अन्य समाचार पत्रों से भी जुड़े रहें. राजनयिक के रूप में डॉ. नारायणन टोकियो, लंदन, आस्ट्रेलिया और हनोई में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रतिष्ठित पदों पर रहे. 1970 में वह चीन के राजदूत नियुक्त हुए. 1978 में रिटायर होने के बाद 3 जनवरी 1979 से 14 अक्टूबर 1980 तक वह देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे. सन् 1980-84 तक वो अमेरिका में भारत के राजदूत रहे.
1984 में डॉ. नारायणन ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. अपने गृह राज्य उत्तरी केरल में वह ओटा पल्लम की सुरक्षित लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए. राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वह योजना राज्यमंत्री और विदेश राज्यमंत्री बने. 71 वर्ष की उम्र में वह भारत के उप राष्ट्रपति चुने गए. सभी दलों की सर्वसम्मति से इस पद पर चुने जाने वाले वह शुरुआती उप राष्ट्रपतियों में से थे. 14 जुलाई 1997 को वह भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए. 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे.
नारायणन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए उच्चतम न्यायायल के न्यायाधीश बनने का रास्ता खोला. उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.एस. आनंद ने नियमानुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के लिए दस न्यायविद उच्च न्यायालयों के कानून विशेषज्ञों का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा. आम तौर पर राष्ट्रपति ऐसी सूची पर अपनी मौन स्वीकृति दे देता है, लेकिन नारायणन जी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को यह टिप्पणी लिखते हुए उस फाइल को लौटा दिया कि “क्या इन दस व्यक्तियों के पैनल में रखने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई योग्य न्यायाधीश नहीं है?” देश के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से सरकार से लेकर न्यायालय में हड़कंप मच गया. न्यायालय में दलितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर बहस होने लगी. मामला गंभीर हो गया. राष्ट्रपति की इस टिप्पणी को नकारने या फिर हल्के में लेने की किसी को हिम्मत नहीं हुई. आखिरकार इस टिप्पणी ने सर्वोच्च न्यायालय में दलितों के प्रवेश का रास्ता खोला. यह डॉ. के.आर. नारायणन के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके लिए बहुजन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा.
डॉ. के.आर. नारायणन का प्रारंभिक जीवन अनेक कठिनाइयों, निर्धनता और अभावों से भरा हुआ था. किंतु आपके धैर्य, विश्वास और संघर्ष के कारण उन्होंने हर बाधा पर जीत हासिल कर ली. उनके बचपन का नाम कोचिरिल राम नारायणन था. उनका जन्म केरल राज्य के पूर्व रियासत त्रावणकोर में कोट्यम जिले में स्थित उझाउर गांव में 27 अक्टूबर, 1920 को हुआ था. उनके पिता का नाम रामन वैद्यन था. उनके पिता एवं दादा दोनों आयुर्वेदिक चिकित्सक थे. समाज में उनके पिता की एक सम्मानित पहचान थी. हालांकि परिवार के सामने आर्थिक तंगी हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उनके पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं थे. लेकिन नारायणन की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मां, बहन और भाई ने उन्हें आगे पढ़ाने का निश्चय किया.
छह साल के होने पर नारायणन का दाखिला गांव से चार किलोमीटर दूर स्थित स्थानीय स्कूल में करवा दिया गया. हाई स्कूल के लिए उन्होंने कूराविले गेड़ स्कूल में दाखिला लिया. बाद में अपनी योग्यता के बल पर वह छात्रवृति हासिल करने लगे. उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता उच्च शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ना है. इस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण किया. सन् 1945 में नारायणन ने त्रावणकोर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज, तिरुअनंतपुरम से 60 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी आनर्स में बी.ए की परीक्षा पास की. इसी कॉलेज से 1948 में उन्होंने प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिविजन) से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए पास किया. एम.ए पास करने के बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज में ही अंग्रेजी प्रवक्ता (लेक्चरार) पद के लिए आवेदन किया. लेकिन त्रावणकोर के दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने नारायणन को प्रवक्ता की बजाय क्लर्क के पद पर काम करने को कहा गया. अय्यर के मन में तब जातीय दंभ था और यह विद्वेष की एक दलित आखिरकार प्रवक्ता कैसे हो सकता है. स्वाभिमानी नारायणन ने क्लर्क की नौकरी लेने से साफ मना कर दिया और इसके ठीक बाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विरोधस्वरूप बी.ए की डिग्री लेने से मना कर दिया.
लेकिन चार दशक बाद सन् 1992 में भारत का उपराष्ट्रपति बनने पर उनके गृह राज्य केरल में केरल विश्वविद्यालय के उसी सीनेट में उनका जोरदार स्वागत किया गया, तब उऩ्होंने अपनी बी.ए की डिग्री ली. उस दौरान तात्कालिक जातिवादियों पर तंज कसते हुए के.आर.नारायणन ने कहा, “आज मुझे उन महापुरुषों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने दलित होने के कारण इस विश्वविद्यालय में मुझे प्रवक्ता बनने से वंचित कर दिया था. हालांकि उन्होंने मुझे प्रवक्ता पद पर नहीं चुन कर अच्छा ही किया क्योंकि तब शायद आज मुझे उप राष्ट्रपति बनने का सुनहरा अवसर नहीं मिलता. और न ही केरल राज्य को यह गौरव मिलता. मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं.”
सन् 1948 में एम.ए करने और प्रवक्ता की नौकरी नहीं मिलने के बाद के. आर. नारायणन दिल्ली में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर से मिलने गए. बाबासाहेब वायसराय की काउंसिल में श्रम विभाग के सदस्य थे. नारायणन की योग्यता को देखते हुए बाबासाहेब ने उन्हें दिल्ली में ही भारत ओवरसीज विभाग जिसे अब विदेश विभाग कहा जाता है में 250 रुपये प्रतिमाह पर सरकारी नौकरी दिलवा दी. लेकिन अपनी साहित्यिक रुचि के कारण के.आर. नारायणन पत्रकार बनना चाहते थे इसलिए बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़ कर सौ रुपये प्रतिमाह वेतन पर साप्ताहिक पत्रिका ‘इकॉनामिक्स वीकली ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री’में बतौर पत्रकार नौकरी ज्वाइन कर लिया. बाद में वह कई अन्य समाचार पत्रों से भी जुड़े रहें. राजनयिक के रूप में डॉ. नारायणन टोकियो, लंदन, आस्ट्रेलिया और हनोई में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रतिष्ठित पदों पर रहे. 1970 में वह चीन के राजदूत नियुक्त हुए. 1978 में रिटायर होने के बाद 3 जनवरी 1979 से 14 अक्टूबर 1980 तक वह देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे. सन् 1980-84 तक वो अमेरिका में भारत के राजदूत रहे.
1984 में डॉ. नारायणन ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. अपने गृह राज्य उत्तरी केरल में वह ओटा पल्लम की सुरक्षित लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए. राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वह योजना राज्यमंत्री और विदेश राज्यमंत्री बने. 71 वर्ष की उम्र में वह भारत के उप राष्ट्रपति चुने गए. सभी दलों की सर्वसम्मति से इस पद पर चुने जाने वाले वह शुरुआती उप राष्ट्रपतियों में से थे. 14 जुलाई 1997 को वह भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए. 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे.
नारायणन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए उच्चतम न्यायायल के न्यायाधीश बनने का रास्ता खोला. उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.एस. आनंद ने नियमानुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के लिए दस न्यायविद उच्च न्यायालयों के कानून विशेषज्ञों का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा. आम तौर पर राष्ट्रपति ऐसी सूची पर अपनी मौन स्वीकृति दे देता है, लेकिन नारायणन जी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को यह टिप्पणी लिखते हुए उस फाइल को लौटा दिया कि “क्या इन दस व्यक्तियों के पैनल में रखने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई योग्य न्यायाधीश नहीं है?” देश के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से सरकार से लेकर न्यायालय में हड़कंप मच गया. न्यायालय में दलितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर बहस होने लगी. मामला गंभीर हो गया. राष्ट्रपति की इस टिप्पणी को नकारने या फिर हल्के में लेने की किसी को हिम्मत नहीं हुई. आखिरकार इस टिप्पणी ने सर्वोच्च न्यायालय में दलितों के प्रवेश का रास्ता खोला. यह डॉ. के.आर. नारायणन के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके लिए बहुजन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा. बाबा साहेब के आर्थिक मॉडल पर चुप क्यों हैं पार्टियां
 आने वाले वक्त में देश के महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं. देश 1952 से चुनावी पर्व मना रहा है. हर बार दलों ने तरह-तरह के वादे किए. वोटरों ने यकीन भी किया. केंद्र में किसी न किसी दल की सरकार बनी और उन्हें अपने वादे को पूरा करने के लिए मौका भी मिला, लेकिन गरीबी नहीं मिटी, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, अशिक्षा दूर नहीं हुई, सबको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली, पानी-बिजली-सड़क की कमी दूर नहीं हो पाई, गरीबों-वंचितों-मजलूमों के लिए न्याय सपना ही रहा, जातिवाद का कलंक नहीं मिटा.
ये सभी समस्याएं देश के पहले आम चुनाव के समय भी विद्यमान थे और इस समय भी मौजूद हैं. उल्टे कालांतर में भ्रष्टाचार और महंगाई के मसले जुड़ गए. सामाजिक न्याय का लक्ष्य जटिल होता गया. गरीब और अमीर के बीच खाई और बढ़ गई. आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना ही गुनाह है. इससे साफ है कि किसी भी दल की सरकार ने न ही अपने वादे पूरे किए और न ही संविधान के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में ही काम किया. चाहे और जितने चुनाव हो जाए, जनता के प्रति दलों का जो रवैया है, उससे जाहिर होता है कि देश की मौलिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी. आखिर ऐसा क्यों? फिर इसका हल क्या है? एक शब्द में कहें तो देश के दलों के द्वारा डॉ. अंबेडकर के अर्थशास्त्र (आर्थिक विचारों) की अनदेखी इसकी वजह है और गरीबी दूर करने के लिए बाबा साहेब द्वारा सुझाए गए तरीकों पर अमल इसका हल है.
बाबा साहेब समाज से गरीबी को खत्म करना चाहते थे. इसके लिए वे आर्थिक आजादी की बात करते थे और जातिवाद का खात्मा चाहते थे. उन्हें लगता था कि जातिवाद भी गरीबी का एक बड़ा कारण है. अधिकांश दलित-पिछड़ी जातियां छोटे कामों पर निर्भर हैं, जिसके चलते उनकी आमदनी भी छोटी ही है, जिससे उनका जीवन स्तर उठ नहीं पाता है. इसलिए जातियों की दीवार को गिराना जरूरी है. उनका मानना था कि यह काम शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के सहारे संभव है. दोनों ही लक्ष्य पाने में वे राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका देखते थे. वे जानते थे कि राज्य सरकार लक्ष्य तभी पूरा कर सकेगी, जब उसके खजाने भरे होंगे. इसके लिए उन्होंने उपाय भी सुझाए थे, जिस पर सरकारों को अमल करना था.
डॉ. अंबेडकर ने सबसे अधिक सार्वजनिक वित्त पोषण पर काम किया. वे राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे. इसके लिए वे सरकारी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे. ब्रिटिश शासन में क्या था कि सरकारी धन पर अधिकार सेंट्रल (केंद्र) का होता था, जबकि खर्च प्रोविंस (आज के राज्य) करते थे. इसमें क्या होता था कि सरकार के पास धन कहां से आएगा, इसके लिए सेंट्रल को सोचना पड़ता था, जबकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रोविंस खर्च करता था. इसमें प्रोविंस अक्सर अधिक पैसे की मांग करता था, जिसे केंद्र को पूरा करना होता था. बाबा साहेब ने इस व्यवस्था की खामियों के तरफ लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने आगाह किया कि प्रोविंस पर आय की जिम्मेदारी नहीं है, खर्च करने में वह गैर जिम्मेदार हो सकता है. इस कारण सरकारी धन के नियंत्रण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और अपना संसाधन जुटाने कि लिए राज्यों को स्वायत्त होना चाहिए.
विडंबना यह है कि आज भी केंद्र और राज्य की वित्त व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की तरह है. राज्य सीमित संसाधन ही जुटा पाता है और अपने खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर है. इसका दुष्परिणाम है कि केंद्र तरह-तरह के टैक्स लगाकर धन जमा करता है. इससे कृषि, उद्योग, व्यापार और गरीब नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं. गरीबों में सबसे अधिक दलित ही हैं, जबकि जनता की इस गाढ़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा सैलरी, रक्षा, सेना प्रशासनिक जैसे अनुत्पादक मदों पर खर्च हो जाता है. जिससे शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च कम हो जाता है. अंबेडकर इस अनुत्पादक खर्च को समीति करना चाहते थे और सरकारी धन का उपयोग जनहित में सुनिश्चित करना चाहते थे. उनका मानना था कि केंद्र और राज्यों के बीच सरकारी धन के स्रोतों का समझदारी से बंटवारा नहीं होने के कारण कई राज्य पिछड़ जाएंगे. आज उनका अंदाजा सही निकला है. देश में राज्यों का असमान विकास हुआ है. कई राज्य पिछड़े हैं. इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता विकसित करने की जरूरत है. बाबा का यह सपना अभी अपूर्ण है.
इसके पूरे होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है. कारण राजनीति ही एक ऐसी चीज है, जिसमें राष्ट्र को आगे ले जाने की ताकत है, लेकिन अभी वह अटकी हुई प्रतीत हो रही है. इस आम चुनाव के प्रचार अभियानों पर गौर करें तो किसी भी दल के एजेंडे में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि अगले पांच साल में हमारा देश कैसा होगा. हम तरक्की की राह पर किस तरह जाएंगे. हम किस क्षेत्र में कितना विकास करेंगे. नागरिकों को कैसे खुशहाल बनाया जाए, महंगाई कैसे दूर होगी, भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है. राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एजेंडा किसी भी दल के प्रचार अभियान में शामिल नहीं है. बाबा साहेब ने राज्य सरकार के स्वामित्व में सहकारी खेती और उद्योग का मॉडल पेश किया था. वे राज्य की सहायता से हर परिवार को आय के स्थाई स्रोत मुहैया कराना चाहते थे. वे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समतावादी-कल्याणकारी समाज का निर्माण करना चाहते थे. यह राजनीति से ही संभव था. संविधान में उन्होंने इसकी व्यवस्था भी की, लेकिन लगता है आज उनका सपना राजनीति के बियाबान में कहीं बिला गया है. हालांकि उम्मीद कायम रहेगी, अगला आम चुनाव भी तो है.
– लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।
आने वाले वक्त में देश के महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं. देश 1952 से चुनावी पर्व मना रहा है. हर बार दलों ने तरह-तरह के वादे किए. वोटरों ने यकीन भी किया. केंद्र में किसी न किसी दल की सरकार बनी और उन्हें अपने वादे को पूरा करने के लिए मौका भी मिला, लेकिन गरीबी नहीं मिटी, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, अशिक्षा दूर नहीं हुई, सबको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली, पानी-बिजली-सड़क की कमी दूर नहीं हो पाई, गरीबों-वंचितों-मजलूमों के लिए न्याय सपना ही रहा, जातिवाद का कलंक नहीं मिटा.
ये सभी समस्याएं देश के पहले आम चुनाव के समय भी विद्यमान थे और इस समय भी मौजूद हैं. उल्टे कालांतर में भ्रष्टाचार और महंगाई के मसले जुड़ गए. सामाजिक न्याय का लक्ष्य जटिल होता गया. गरीब और अमीर के बीच खाई और बढ़ गई. आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना ही गुनाह है. इससे साफ है कि किसी भी दल की सरकार ने न ही अपने वादे पूरे किए और न ही संविधान के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में ही काम किया. चाहे और जितने चुनाव हो जाए, जनता के प्रति दलों का जो रवैया है, उससे जाहिर होता है कि देश की मौलिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी. आखिर ऐसा क्यों? फिर इसका हल क्या है? एक शब्द में कहें तो देश के दलों के द्वारा डॉ. अंबेडकर के अर्थशास्त्र (आर्थिक विचारों) की अनदेखी इसकी वजह है और गरीबी दूर करने के लिए बाबा साहेब द्वारा सुझाए गए तरीकों पर अमल इसका हल है.
बाबा साहेब समाज से गरीबी को खत्म करना चाहते थे. इसके लिए वे आर्थिक आजादी की बात करते थे और जातिवाद का खात्मा चाहते थे. उन्हें लगता था कि जातिवाद भी गरीबी का एक बड़ा कारण है. अधिकांश दलित-पिछड़ी जातियां छोटे कामों पर निर्भर हैं, जिसके चलते उनकी आमदनी भी छोटी ही है, जिससे उनका जीवन स्तर उठ नहीं पाता है. इसलिए जातियों की दीवार को गिराना जरूरी है. उनका मानना था कि यह काम शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के सहारे संभव है. दोनों ही लक्ष्य पाने में वे राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका देखते थे. वे जानते थे कि राज्य सरकार लक्ष्य तभी पूरा कर सकेगी, जब उसके खजाने भरे होंगे. इसके लिए उन्होंने उपाय भी सुझाए थे, जिस पर सरकारों को अमल करना था.
डॉ. अंबेडकर ने सबसे अधिक सार्वजनिक वित्त पोषण पर काम किया. वे राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे. इसके लिए वे सरकारी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे. ब्रिटिश शासन में क्या था कि सरकारी धन पर अधिकार सेंट्रल (केंद्र) का होता था, जबकि खर्च प्रोविंस (आज के राज्य) करते थे. इसमें क्या होता था कि सरकार के पास धन कहां से आएगा, इसके लिए सेंट्रल को सोचना पड़ता था, जबकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रोविंस खर्च करता था. इसमें प्रोविंस अक्सर अधिक पैसे की मांग करता था, जिसे केंद्र को पूरा करना होता था. बाबा साहेब ने इस व्यवस्था की खामियों के तरफ लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने आगाह किया कि प्रोविंस पर आय की जिम्मेदारी नहीं है, खर्च करने में वह गैर जिम्मेदार हो सकता है. इस कारण सरकारी धन के नियंत्रण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और अपना संसाधन जुटाने कि लिए राज्यों को स्वायत्त होना चाहिए.
विडंबना यह है कि आज भी केंद्र और राज्य की वित्त व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की तरह है. राज्य सीमित संसाधन ही जुटा पाता है और अपने खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर है. इसका दुष्परिणाम है कि केंद्र तरह-तरह के टैक्स लगाकर धन जमा करता है. इससे कृषि, उद्योग, व्यापार और गरीब नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं. गरीबों में सबसे अधिक दलित ही हैं, जबकि जनता की इस गाढ़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा सैलरी, रक्षा, सेना प्रशासनिक जैसे अनुत्पादक मदों पर खर्च हो जाता है. जिससे शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च कम हो जाता है. अंबेडकर इस अनुत्पादक खर्च को समीति करना चाहते थे और सरकारी धन का उपयोग जनहित में सुनिश्चित करना चाहते थे. उनका मानना था कि केंद्र और राज्यों के बीच सरकारी धन के स्रोतों का समझदारी से बंटवारा नहीं होने के कारण कई राज्य पिछड़ जाएंगे. आज उनका अंदाजा सही निकला है. देश में राज्यों का असमान विकास हुआ है. कई राज्य पिछड़े हैं. इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता विकसित करने की जरूरत है. बाबा का यह सपना अभी अपूर्ण है.
इसके पूरे होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है. कारण राजनीति ही एक ऐसी चीज है, जिसमें राष्ट्र को आगे ले जाने की ताकत है, लेकिन अभी वह अटकी हुई प्रतीत हो रही है. इस आम चुनाव के प्रचार अभियानों पर गौर करें तो किसी भी दल के एजेंडे में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि अगले पांच साल में हमारा देश कैसा होगा. हम तरक्की की राह पर किस तरह जाएंगे. हम किस क्षेत्र में कितना विकास करेंगे. नागरिकों को कैसे खुशहाल बनाया जाए, महंगाई कैसे दूर होगी, भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है. राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एजेंडा किसी भी दल के प्रचार अभियान में शामिल नहीं है. बाबा साहेब ने राज्य सरकार के स्वामित्व में सहकारी खेती और उद्योग का मॉडल पेश किया था. वे राज्य की सहायता से हर परिवार को आय के स्थाई स्रोत मुहैया कराना चाहते थे. वे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समतावादी-कल्याणकारी समाज का निर्माण करना चाहते थे. यह राजनीति से ही संभव था. संविधान में उन्होंने इसकी व्यवस्था भी की, लेकिन लगता है आज उनका सपना राजनीति के बियाबान में कहीं बिला गया है. हालांकि उम्मीद कायम रहेगी, अगला आम चुनाव भी तो है.
– लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 
