 ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’
इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.
आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!
भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.
बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.
प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.
बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.
फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’
तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.
यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.
इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.
इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.
1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.
इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.
इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?
अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?
साभारः जनसत्ता
ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’
इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.
आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!
भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.
बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.
प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.
बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.
फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’
तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.
यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.
इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.
इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.
1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.
इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.
इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?
अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?
साभारः जनसत्ता क्रिकेट में दलित हिस्सेदारी
 ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’
इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.
आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!
भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.
बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.
प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.
बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.
फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’
तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.
यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.
इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.
इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.
1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.
इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.
इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?
अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?
साभारः जनसत्ता
ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’
इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.
आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!
भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.
बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.
प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.
बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.
फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’
तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.
यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.
इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.
इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.
1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.
इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.
इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?
अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?
साभारः जनसत्ता देश में हॉकी को स्टार खिलाड़ी देने वाला कोच, गलियों में बेच रहा है स्पोर्ट्स किट्स
 गोरखपुर। देश को हॉकी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले गोरखपुर के इमरान की जिंदगी खेल के मैदान से निकल सड़कों पर आकर ठहर गई है. जो अब दो जून की रोटी की जुगाड़ में घर-घर जाकर स्पोर्ट्स किट्स बेचने को मजबूर है. पूर्वांचल की माटी से देश के लिए हॉकी को 8 अंतरराष्ट्रीय और 50 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ी देने का गौरव हासिल है. इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रहीं निधि खुल्लर, संजू ओझा, रजनी चौधरी, रीता पांडेय, प्रवीन शर्मा, सनवर अली, जनार्दन गुप्ता और प्रतिभा चौधरी जैसे कई खिलाड़ियों को हॉकी की ट्रेनिंग दी है.
बता दें, कि 1973 में रोजी रोटी की तलाश में इमरान गोरखपुर आ गए. यहां के खाद्य कारखाने में स्पोटर्स कोटे से नौकरी मिल गई.जहां उन्होंने नौकरी के साथ हॉकी की ट्रेनिंग देना भी जारी रखा. लेकिन अचानक 31 दिसंबर 2002 में खाद्य कारखाना बंद हो गया और नौकरी चली गई. इमरान ने बताया कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से 900 रूपए पेंशन मिलता है, लेकिन आज की महंगाई में इतने कम पैसे में क्या घर की दाल रोटी चल सकती है. वहीं हमने खिलाड़ियों के लिए लोअर बनाने का कारखाना शुरू किया, लेकिन पैसे के अभाव में यह भी बंद हो गया.
आज के दौर में ये हौनहार कोच घर-घर जाकर स्पोर्ट किट बेचते हैं. वैसे ज्यादारतर किट वहां ले जाकर बेचते हैं, जहां कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है. किट बेचने पर कमीशन मिलता है. जिससे वो अपने परिवार की जिंदगी की डगर को धक्का दे रहे हैं. इमरान के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. बेटा आमिर प्राइवेट फर्म में 6 हजार की नौकरी करता है, तो दूसरी तरफ बेटी उज्मा की पढ़ाई पैसों की वजह से पूरी नहीं हो पाई.
गोरखपुर। देश को हॉकी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले गोरखपुर के इमरान की जिंदगी खेल के मैदान से निकल सड़कों पर आकर ठहर गई है. जो अब दो जून की रोटी की जुगाड़ में घर-घर जाकर स्पोर्ट्स किट्स बेचने को मजबूर है. पूर्वांचल की माटी से देश के लिए हॉकी को 8 अंतरराष्ट्रीय और 50 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ी देने का गौरव हासिल है. इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रहीं निधि खुल्लर, संजू ओझा, रजनी चौधरी, रीता पांडेय, प्रवीन शर्मा, सनवर अली, जनार्दन गुप्ता और प्रतिभा चौधरी जैसे कई खिलाड़ियों को हॉकी की ट्रेनिंग दी है.
बता दें, कि 1973 में रोजी रोटी की तलाश में इमरान गोरखपुर आ गए. यहां के खाद्य कारखाने में स्पोटर्स कोटे से नौकरी मिल गई.जहां उन्होंने नौकरी के साथ हॉकी की ट्रेनिंग देना भी जारी रखा. लेकिन अचानक 31 दिसंबर 2002 में खाद्य कारखाना बंद हो गया और नौकरी चली गई. इमरान ने बताया कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से 900 रूपए पेंशन मिलता है, लेकिन आज की महंगाई में इतने कम पैसे में क्या घर की दाल रोटी चल सकती है. वहीं हमने खिलाड़ियों के लिए लोअर बनाने का कारखाना शुरू किया, लेकिन पैसे के अभाव में यह भी बंद हो गया.
आज के दौर में ये हौनहार कोच घर-घर जाकर स्पोर्ट किट बेचते हैं. वैसे ज्यादारतर किट वहां ले जाकर बेचते हैं, जहां कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है. किट बेचने पर कमीशन मिलता है. जिससे वो अपने परिवार की जिंदगी की डगर को धक्का दे रहे हैं. इमरान के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. बेटा आमिर प्राइवेट फर्म में 6 हजार की नौकरी करता है, तो दूसरी तरफ बेटी उज्मा की पढ़ाई पैसों की वजह से पूरी नहीं हो पाई. … और जब बसपा के एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए तो कांशीराम जी ने कहा…
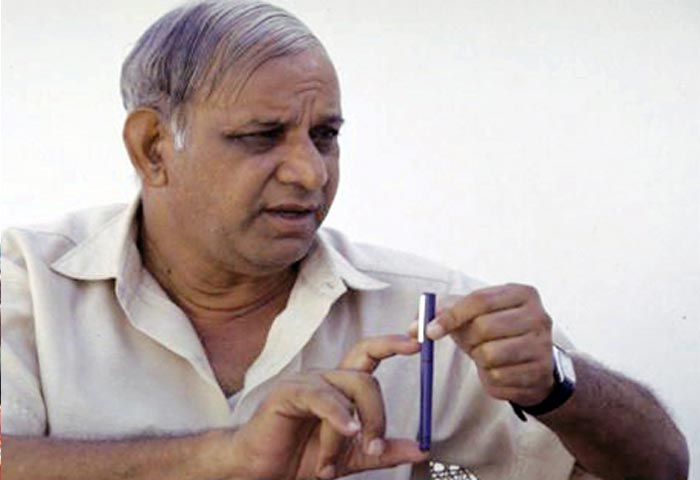 कांशीराम जी जब बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने में लगे थे उस दौरान एक बार एक बड़ा आदिवासी चेहरा अरविन्द नेताम पार्टी से अलग हो गए. नेताम बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए. आमतौर पर किसी बड़े चेहरे के पार्टी से अलग हो जाने के बाद कुछ दिनों तक पार्टी में हलचल रहती है. लेकिन नेताम के कांग्रेस से अलग हो जाने के बावजूद भी कांशीराम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा. पार्टी में भी सबकुछ सामान्य तौर पर चलता रहा. पत्रकार जो इसे मुद्दा बनाने में लगे थे, उन्हें बड़ी निराशा हुई. उन्हें चटपटी खबरें बनाने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि कांशीराम जी उस नेता पर कोई भड़ास नहीं निकाल रहे थे.
पत्रकारों से नहीं रहा गया. कांशीराम जी से पत्रकारों ने पूछा- साहब आपकी पार्टी का दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चला गया, लेकिन आपको चिंता ही नहीं है. आप उसको मना क्यों नहीं लेते? साहब ने जवाब में कहा- भाई पहली बात तो वो माना हुआ होता तो पार्टी छोड़ता ही नहीं. दूसरी बात अब आप लोगों ने उसको दिग्गज़ बना दिया तो अब उसको मनाने की रेट भी दिग्गज़ हो गयी है जो कि मेरे पास है नहीं. इसीलिए मैं इसके जाने की विदाई पार्टी देता हूं ताकि किसी दूसरी पार्टी में रहकर मेरी सिखाई बातों पर थोड़ा बहुत तो अमल करेगा. वो भी मेरे मिशन का ही हिस्सा है.
कांशीराम जी ने कहा कि बसपा में किसी को लालची रस्सी से बांधकर नहीं रखा जाता और ना ही किसी नेता को नोट की कोर दिखाकर बुलाया जाता है. इसीलिए जिस किसी को बसपा समझ में आये वो यहां काम करे. यहां आने जाने वालों के लिए दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं.
कांशीराम जी जब बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने में लगे थे उस दौरान एक बार एक बड़ा आदिवासी चेहरा अरविन्द नेताम पार्टी से अलग हो गए. नेताम बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए. आमतौर पर किसी बड़े चेहरे के पार्टी से अलग हो जाने के बाद कुछ दिनों तक पार्टी में हलचल रहती है. लेकिन नेताम के कांग्रेस से अलग हो जाने के बावजूद भी कांशीराम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा. पार्टी में भी सबकुछ सामान्य तौर पर चलता रहा. पत्रकार जो इसे मुद्दा बनाने में लगे थे, उन्हें बड़ी निराशा हुई. उन्हें चटपटी खबरें बनाने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि कांशीराम जी उस नेता पर कोई भड़ास नहीं निकाल रहे थे.
पत्रकारों से नहीं रहा गया. कांशीराम जी से पत्रकारों ने पूछा- साहब आपकी पार्टी का दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चला गया, लेकिन आपको चिंता ही नहीं है. आप उसको मना क्यों नहीं लेते? साहब ने जवाब में कहा- भाई पहली बात तो वो माना हुआ होता तो पार्टी छोड़ता ही नहीं. दूसरी बात अब आप लोगों ने उसको दिग्गज़ बना दिया तो अब उसको मनाने की रेट भी दिग्गज़ हो गयी है जो कि मेरे पास है नहीं. इसीलिए मैं इसके जाने की विदाई पार्टी देता हूं ताकि किसी दूसरी पार्टी में रहकर मेरी सिखाई बातों पर थोड़ा बहुत तो अमल करेगा. वो भी मेरे मिशन का ही हिस्सा है.
कांशीराम जी ने कहा कि बसपा में किसी को लालची रस्सी से बांधकर नहीं रखा जाता और ना ही किसी नेता को नोट की कोर दिखाकर बुलाया जाता है. इसीलिए जिस किसी को बसपा समझ में आये वो यहां काम करे. यहां आने जाने वालों के लिए दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं. अठावले ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता नागपुर में गिरवी रख दी है
 भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय रामदास अठावले का एक बयान आया है. अठावले के लिए लिखते समय उनका इतना विस्तृत परिचय देने की एक वजह है. शायद वह इन्हीं संबोधनों के भूखे हैं. क्योंकि मंत्रीपद मिलने के बाद उनके तेवर और सुर बदले हुए हैं. अपने ताजा बयान में उन्होंने सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की है. उन्होंने नौकरी और शिक्षा में अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए 25 फीसदी आरक्षण की वकालत की है. मंत्री महोदय का कहना है कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षण देने से दलितों और अन्य जातियों को कोई परेशानी नहीं होगी.
अठावले जी के इस तर्क से मैं भी सहमत हूं कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. लेकिन अठावले जी से मेरा सवाल यह है कि अगड़ों के लिए आरक्षण की बांग देने से पहले क्या उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सामाजिक न्याय के तहत दलितों को सारे संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं? क्या अठावले इस बात को लेकर आवश्वस्त हैं कि सारे विभागों में बैकलॉग भरा जा चुका है और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा के तहत उन्हें निर्धारित सीटें मिल रही हैं? क्या अठावले ने इस बात की तफ्तीश कर ली है कि मंत्रालयों में सचिव और मुख्य सचिव के पद पर वंचित तबके के अधिकारियों को उनका हक मिल रहा है? क्या अठावले दलित समाज के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं? अगर अठावले को लगता है कि ये सारी बातें हो चुकी है या फिर इन बातों के लिए आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी अगड़ों के लिए आरक्षण की मांग करना है तो फिर और बात है.
अठावले जब से भाजपा के रथी बने हैं, उनका अंदाज बदला सा है. याद रहे कि ये वही अठावले हैं जो गुजरात के उना में दलितों के मान मर्दन पर चुप्पी साध लेते हैं. ये वही अठावले हैं जो बिहार में दलित छात्रों पर लाठी भांजे जाने पर कुछ नहीं बोलते. ये वही अठावले हैं जिनकी आवाज संसद में दलित हितों के सवालों पर सुनाई नहीं देती. ये वही अठावले हैं जो तब भी खामोश रह जाते हैं जब महाराष्ट्र में मोबाइल में बाबासाहेब के गाने की रिंगटोन रखने पर एक युवक को मार दिया जाता है. ये वही अठावले हैं जो अपने ‘आका’ के इशारे पर बहुजन नेत्री और दलित हितों को लेकर संसद में गरजने वाली बसपा प्रमुख मायावती से यह पूछ बैठते हैं कि वो बौद्ध धम्म कब अपनाएंगी. और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद सूंड वाले भगवान गणेश के आगे नतमस्तक हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.
मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को बतौर पत्रकार करीब से देखा है. मैंने अठावले को ‘किसी भी कीमत पर’ संसद में पहुंचने के लिए छटपटाते देखा है. जिस वक्त अठावले को राज्यसभा में लाने की बात चल रही थी, उस समय मैं एक अखबार से बतौर राजनीतिक संवाददाता जुड़ा था. भाजपा के दफ्तर में रविशंकर प्रसाद इस पर चर्चा कर रहे थे और हम जैसे तमाम पत्रकार बैठे थे. महाराष्ट्र के कुछ सीनियर पत्रकारों ने रविशंकर प्रसाद को चेताया था कि अठावले को राज्यसभा में लाकर वह गलत कर रहे हैं, क्योंकि अठावले को संभाल पाना मुश्किल होगा. तब रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे. लगता है भाजपा ने सचमुच में अठावले को संभाल लिया है. अठावले के पिछले कुछ बयानों और कुछ खामोशियों को देखें तो यह साफ हो गया है कि अठावले अपनी स्वतंत्रता नागपुर में गिरवी रख कर तब दिल्ली पहुंचे हैं.
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय रामदास अठावले का एक बयान आया है. अठावले के लिए लिखते समय उनका इतना विस्तृत परिचय देने की एक वजह है. शायद वह इन्हीं संबोधनों के भूखे हैं. क्योंकि मंत्रीपद मिलने के बाद उनके तेवर और सुर बदले हुए हैं. अपने ताजा बयान में उन्होंने सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की है. उन्होंने नौकरी और शिक्षा में अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए 25 फीसदी आरक्षण की वकालत की है. मंत्री महोदय का कहना है कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षण देने से दलितों और अन्य जातियों को कोई परेशानी नहीं होगी.
अठावले जी के इस तर्क से मैं भी सहमत हूं कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. लेकिन अठावले जी से मेरा सवाल यह है कि अगड़ों के लिए आरक्षण की बांग देने से पहले क्या उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सामाजिक न्याय के तहत दलितों को सारे संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं? क्या अठावले इस बात को लेकर आवश्वस्त हैं कि सारे विभागों में बैकलॉग भरा जा चुका है और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा के तहत उन्हें निर्धारित सीटें मिल रही हैं? क्या अठावले ने इस बात की तफ्तीश कर ली है कि मंत्रालयों में सचिव और मुख्य सचिव के पद पर वंचित तबके के अधिकारियों को उनका हक मिल रहा है? क्या अठावले दलित समाज के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं? अगर अठावले को लगता है कि ये सारी बातें हो चुकी है या फिर इन बातों के लिए आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी अगड़ों के लिए आरक्षण की मांग करना है तो फिर और बात है.
अठावले जब से भाजपा के रथी बने हैं, उनका अंदाज बदला सा है. याद रहे कि ये वही अठावले हैं जो गुजरात के उना में दलितों के मान मर्दन पर चुप्पी साध लेते हैं. ये वही अठावले हैं जो बिहार में दलित छात्रों पर लाठी भांजे जाने पर कुछ नहीं बोलते. ये वही अठावले हैं जिनकी आवाज संसद में दलित हितों के सवालों पर सुनाई नहीं देती. ये वही अठावले हैं जो तब भी खामोश रह जाते हैं जब महाराष्ट्र में मोबाइल में बाबासाहेब के गाने की रिंगटोन रखने पर एक युवक को मार दिया जाता है. ये वही अठावले हैं जो अपने ‘आका’ के इशारे पर बहुजन नेत्री और दलित हितों को लेकर संसद में गरजने वाली बसपा प्रमुख मायावती से यह पूछ बैठते हैं कि वो बौद्ध धम्म कब अपनाएंगी. और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद सूंड वाले भगवान गणेश के आगे नतमस्तक हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.
मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को बतौर पत्रकार करीब से देखा है. मैंने अठावले को ‘किसी भी कीमत पर’ संसद में पहुंचने के लिए छटपटाते देखा है. जिस वक्त अठावले को राज्यसभा में लाने की बात चल रही थी, उस समय मैं एक अखबार से बतौर राजनीतिक संवाददाता जुड़ा था. भाजपा के दफ्तर में रविशंकर प्रसाद इस पर चर्चा कर रहे थे और हम जैसे तमाम पत्रकार बैठे थे. महाराष्ट्र के कुछ सीनियर पत्रकारों ने रविशंकर प्रसाद को चेताया था कि अठावले को राज्यसभा में लाकर वह गलत कर रहे हैं, क्योंकि अठावले को संभाल पाना मुश्किल होगा. तब रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे. लगता है भाजपा ने सचमुच में अठावले को संभाल लिया है. अठावले के पिछले कुछ बयानों और कुछ खामोशियों को देखें तो यह साफ हो गया है कि अठावले अपनी स्वतंत्रता नागपुर में गिरवी रख कर तब दिल्ली पहुंचे हैं. बसपा की रैलियों पर प्रो. विवेक कुमार की टिप्पणी
 बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में अब तक दो चुनावी रैलियां कर चुकी हैं. इन दोनों चुनावी रैलियों में लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए. चुनावों के नजरिए से बसपा का रूख सकारात्मक है. बसपा अपना एजेंडा सेट कर रही है. आगरा रैली और आजमगढ़ रैली में लोगों ने बसपा को भारी समर्थन दिया और आने वाली रैलियों में समर्थकों की सुनामी आएगी. हालांकि मुख्यधारा की मीडिया इसे कवर नहीं कर रही है, फिर भी लोगों की भीड़ स्वतः निकलकर आ रही है. लोगों का यह हुजूम प्रमाणित करता है कि ये रैलियां काफी सफल हो रही है.
आजमगढ़ की रैली में बसपा सुप्रीमो ने तिलक तराजू का नारे के बारे में बहुत दिनों बाद कुछ कहा है. उनका कहना बिल्कुल ठीक है. मैंने जब मान्यवर कांशीराम का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने यह बात कही थी कि यह नारा मेरा या फिर बसपा का नहीं है. मान्यवर कांशीराम उस समय इटावा से चुनाव लड़ रहे थे. जब सपा और बसपा का गठबंधन था और सपा के लोगों ने यह नारा लगाया था. पहली बार यह नारा 1993 में सपा के लोगों द्वारा दिया गया. कांशीराम ने कहा था कि मेरे नारे तो सिद्धांतवादी होते हैं जिसके अंदर हम प्रजातंत्र को दिखाते हैं. जैसे हमारे शुरूआत के नारे “वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा”, “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी”, “वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम”. ये नारे हमारे थे और इसी पर हम टिके हुए हैं. इसलिए तिलक-तराजू वाला नारा बसपा के मंच से कभी नहीं निकला. जनता ने अगर लगाया हो तो लगाया हो.
बसपा से निकाले गए नेताओं को भाजपा जिस तरह अपना रही है, इस पर बहनजी ने भाजपा की यथास्थति को बताया है. उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे रिजेक्टेड माल को भाजपा बड़ी अहमियत दे रही है. इसका मतलब यह हुआ कि उसके अपने कैडर और कैंडिडेट नहीं हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी जोकि दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे है और विरोधी पार्टी के 25 साल पुराने नेता को अपनाकर इज्जत दे रही है. भाजपा का यह कदम उसकी जमीनी हकीकत और संगठनात्मक हकीकत का कहीं न कहीं पोल खोलती है.
अब तक दो रैलियां हो चुकी हैं. रैली में समर्थकों का हूजुम देखकर बसपा सुप्रीमों ने इसे समुद्री रैली बोला है. मेरा मानना है कि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल यूपी में रैली नहीं करेगा. वो रथ यात्रा निकाल सकता है, वो रोड शो कर सकता है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वह रैली नहीं करेगा. क्योंकि इससे उसके जनाधार की पोल खुलने का खतरा रहेगा. इसलिए बसपा प्रमुख ने इन जनसैलाबी रैली को कर के एक नई स्थापना कर दी है. दूसरे दल रैली न कर सके और अपने जनाधार का परचम ना लहरा पाए. तो इसे बसपा की राजनैतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है.
बसपा की अपनी एक नीति रही है. बसपा लगातार अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि कंवर्टेड माइनोरिटीज और अपर कास्ट में गरीब तबके को सर्वजन हिताय के तहत संगठित करती रहीं हैं. लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को अकलियत समाज, कनवर्टेड माइनोरोटीज जिन्हें रिलिजियस माइनोरिटीज कहा जाता है, उसके लिए दो कदम और चलना पडेगा. उनके अंदर विश्वास बनाना पड़ेगा. उनके लीडरों के माध्यम से उनको मनाना पड़ेगा कि आपका भविष्य सपा में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस और किसी अन्य दल में सुरक्षित नहीं है. आज अल्पसंख्यक समाज सिर्फ बसपा में सुरक्षित है. इसके लिए उनको एक कदम आगे आना पड़ेगा, उनके संगठन को मनाना पड़ेगा. जिससे की वो बसपा की तरफ तेजी से उन्मुख हो सके.
बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में अब तक दो चुनावी रैलियां कर चुकी हैं. इन दोनों चुनावी रैलियों में लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए. चुनावों के नजरिए से बसपा का रूख सकारात्मक है. बसपा अपना एजेंडा सेट कर रही है. आगरा रैली और आजमगढ़ रैली में लोगों ने बसपा को भारी समर्थन दिया और आने वाली रैलियों में समर्थकों की सुनामी आएगी. हालांकि मुख्यधारा की मीडिया इसे कवर नहीं कर रही है, फिर भी लोगों की भीड़ स्वतः निकलकर आ रही है. लोगों का यह हुजूम प्रमाणित करता है कि ये रैलियां काफी सफल हो रही है.
आजमगढ़ की रैली में बसपा सुप्रीमो ने तिलक तराजू का नारे के बारे में बहुत दिनों बाद कुछ कहा है. उनका कहना बिल्कुल ठीक है. मैंने जब मान्यवर कांशीराम का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने यह बात कही थी कि यह नारा मेरा या फिर बसपा का नहीं है. मान्यवर कांशीराम उस समय इटावा से चुनाव लड़ रहे थे. जब सपा और बसपा का गठबंधन था और सपा के लोगों ने यह नारा लगाया था. पहली बार यह नारा 1993 में सपा के लोगों द्वारा दिया गया. कांशीराम ने कहा था कि मेरे नारे तो सिद्धांतवादी होते हैं जिसके अंदर हम प्रजातंत्र को दिखाते हैं. जैसे हमारे शुरूआत के नारे “वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा”, “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी”, “वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम”. ये नारे हमारे थे और इसी पर हम टिके हुए हैं. इसलिए तिलक-तराजू वाला नारा बसपा के मंच से कभी नहीं निकला. जनता ने अगर लगाया हो तो लगाया हो.
बसपा से निकाले गए नेताओं को भाजपा जिस तरह अपना रही है, इस पर बहनजी ने भाजपा की यथास्थति को बताया है. उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे रिजेक्टेड माल को भाजपा बड़ी अहमियत दे रही है. इसका मतलब यह हुआ कि उसके अपने कैडर और कैंडिडेट नहीं हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी जोकि दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे है और विरोधी पार्टी के 25 साल पुराने नेता को अपनाकर इज्जत दे रही है. भाजपा का यह कदम उसकी जमीनी हकीकत और संगठनात्मक हकीकत का कहीं न कहीं पोल खोलती है.
अब तक दो रैलियां हो चुकी हैं. रैली में समर्थकों का हूजुम देखकर बसपा सुप्रीमों ने इसे समुद्री रैली बोला है. मेरा मानना है कि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल यूपी में रैली नहीं करेगा. वो रथ यात्रा निकाल सकता है, वो रोड शो कर सकता है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वह रैली नहीं करेगा. क्योंकि इससे उसके जनाधार की पोल खुलने का खतरा रहेगा. इसलिए बसपा प्रमुख ने इन जनसैलाबी रैली को कर के एक नई स्थापना कर दी है. दूसरे दल रैली न कर सके और अपने जनाधार का परचम ना लहरा पाए. तो इसे बसपा की राजनैतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है.
बसपा की अपनी एक नीति रही है. बसपा लगातार अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि कंवर्टेड माइनोरिटीज और अपर कास्ट में गरीब तबके को सर्वजन हिताय के तहत संगठित करती रहीं हैं. लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को अकलियत समाज, कनवर्टेड माइनोरोटीज जिन्हें रिलिजियस माइनोरिटीज कहा जाता है, उसके लिए दो कदम और चलना पडेगा. उनके अंदर विश्वास बनाना पड़ेगा. उनके लीडरों के माध्यम से उनको मनाना पड़ेगा कि आपका भविष्य सपा में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस और किसी अन्य दल में सुरक्षित नहीं है. आज अल्पसंख्यक समाज सिर्फ बसपा में सुरक्षित है. इसके लिए उनको एक कदम आगे आना पड़ेगा, उनके संगठन को मनाना पड़ेगा. जिससे की वो बसपा की तरफ तेजी से उन्मुख हो सके.
गुड़गांव में बुद्ध विहार गिराना चाहता है सरपंच
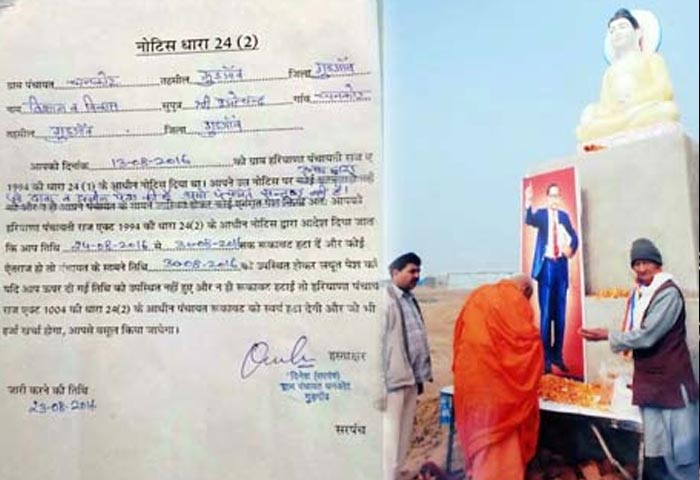 गुड़गांव। गुड़गांव से सटा एक गांव है धनकोट. बौद्ध धम्म के जानकार बताते हैं कि कालांतर में तथागत बुद्ध यहां आ चुके हैं. इसी धनकोट में एक सामलात जमीन है. खाली पड़ी इस जमीन पर तत्कालीन सरपंच के कहने पर और सहमति लेकर गांव के लोगों ने एक बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई और इस जमीन पर एक बुद्ध विहार बना दिया. लेकिन वर्तमान सरपंच को यह बुद्ध विहार पसंद नहीं है. वह इसे तोड़ना चाहता है. जिसके लिए उसने पंचायती राज एक्ट, सेक्शन 24 के तहत बुद्धिस्ट सोसायटी को एक नोटिस दे दिया है. इसके बाद सोसाइटी के लोग और तथागत एवं धम्म को मानने वाले लोगों में रोष है.
स्थानीय निवासी एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभा के पूर्व अध्यक्ष जितेन्दर कुमार का कहना है कि यह जमीन वर्षों से हमारी है. इस जमीन का बहुत पहले से दलित समाज के हमारे लोग इस्तेमाल करते रहे हैं. यहां तक की तहसीलदार के पास जो रेवेन्यू रिकार्ड होता है, उसमें भी साफ-साफ इस जमीन की मिल्कियत सामलात भूमि हरिजन (रिकार्ड में यही शब्द है) के पास है. सालों से यह जमीन खाली और बेकार पड़ी थी. 2013 में तात्कालीन सरपंच की सहमति से हमने इस जमीन के गड्ढे को भरा और यहां बौद्ध विहार बनाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी. बाकी की जमीन में पेड़-पौधे लगाकर इसको सुंदर बनाया.
यह सबके लिए खुला है लेकिन वर्तमान सरपंच को यह अच्छा नहीं लगता. वह बुद्ध की प्रतिमा को हटाना चाहता है. उसने नोटिस दिया है इसे खाली कर दिया जाए लेकिन यह जमीन पंचायती राज में है ही नहीं इसलिए वह इस पर कोई नोटिस नहीं दे सकता है. हमने जवाब दे दिया है लेकिन वह उस पर संतुष्ट नहीं है. ग्राम पंचायत की कार्यकारीणी उसके साथ हैं. उसकी मेज्योरिटी है. वह अपने हिसाब से काम करवाता है.
गांव के सरपंच दिनेश सहरावत का कहना है कि यह जमीन पंचायत की है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन से जुड़े दस्तावेज भी है. दलित दस्तक ने जब उनसे दस्तावेज मांगें तो वो आनाकानी करने लगे.
गुड़गांव। गुड़गांव से सटा एक गांव है धनकोट. बौद्ध धम्म के जानकार बताते हैं कि कालांतर में तथागत बुद्ध यहां आ चुके हैं. इसी धनकोट में एक सामलात जमीन है. खाली पड़ी इस जमीन पर तत्कालीन सरपंच के कहने पर और सहमति लेकर गांव के लोगों ने एक बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई और इस जमीन पर एक बुद्ध विहार बना दिया. लेकिन वर्तमान सरपंच को यह बुद्ध विहार पसंद नहीं है. वह इसे तोड़ना चाहता है. जिसके लिए उसने पंचायती राज एक्ट, सेक्शन 24 के तहत बुद्धिस्ट सोसायटी को एक नोटिस दे दिया है. इसके बाद सोसाइटी के लोग और तथागत एवं धम्म को मानने वाले लोगों में रोष है.
स्थानीय निवासी एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभा के पूर्व अध्यक्ष जितेन्दर कुमार का कहना है कि यह जमीन वर्षों से हमारी है. इस जमीन का बहुत पहले से दलित समाज के हमारे लोग इस्तेमाल करते रहे हैं. यहां तक की तहसीलदार के पास जो रेवेन्यू रिकार्ड होता है, उसमें भी साफ-साफ इस जमीन की मिल्कियत सामलात भूमि हरिजन (रिकार्ड में यही शब्द है) के पास है. सालों से यह जमीन खाली और बेकार पड़ी थी. 2013 में तात्कालीन सरपंच की सहमति से हमने इस जमीन के गड्ढे को भरा और यहां बौद्ध विहार बनाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी. बाकी की जमीन में पेड़-पौधे लगाकर इसको सुंदर बनाया.
यह सबके लिए खुला है लेकिन वर्तमान सरपंच को यह अच्छा नहीं लगता. वह बुद्ध की प्रतिमा को हटाना चाहता है. उसने नोटिस दिया है इसे खाली कर दिया जाए लेकिन यह जमीन पंचायती राज में है ही नहीं इसलिए वह इस पर कोई नोटिस नहीं दे सकता है. हमने जवाब दे दिया है लेकिन वह उस पर संतुष्ट नहीं है. ग्राम पंचायत की कार्यकारीणी उसके साथ हैं. उसकी मेज्योरिटी है. वह अपने हिसाब से काम करवाता है.
गांव के सरपंच दिनेश सहरावत का कहना है कि यह जमीन पंचायत की है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन से जुड़े दस्तावेज भी है. दलित दस्तक ने जब उनसे दस्तावेज मांगें तो वो आनाकानी करने लगे. गली-गली में बुद्ध
 ईसा की प्रथम शताब्दी तक एशिया महादेश के अधिकतर देशों में बुद्ध धम्म स्थापित हो चुका था. इसकी आधारशिला ईसा पूर्व 250 के आस पास मौर्य वंश के यशस्वी सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म-प्रचार के लिए श्रीलंका भेजकर रख दी थी. ईसा की छठी शताब्दी के आस पास जब एशिया के देशों के मध्य सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संक्रमण का दौर शुरू हुआ तो अरबी-तुर्की यात्रियों व्यापारियों को जगह जगह बुद्ध मिलते. वे यात्री व्यापारी चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका आदि जहां भी जाते, वहां के पगोडा, मठ या विहार और स्तूपों में उन्हें आंखे मूंदे, मुस्कुराती हुई एक सौम्य मूर्ति अवश्य दिखाई देती. यदि स्थानीय व्यक्तियों से वो मूर्तियों के विषय में अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते तो केवल एक ही उतर मिलता, यह ‘बुद्ध’ हैं. अन्ततः बुद्ध शब्द अरबी, फ़ारसी भाषा में अपभ्रंशित हो बुत हो गया, जिसका अर्थ ही मान लिया गया मूर्ति. बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग पांच सौ वर्षो के पश्चात भारत में महायानी शाखा ने बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना शुरू की और कालांतर में लगभग पूरे पश्चिम एशिया में बुद्ध फ़ैल गये. चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि सभी जगह. भारत में बुद्ध संस्कृति का प्रभाव एवं विस्तार देश के कोने कोने में है. यह बात प्रमाणिकता से इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में अब तक सबसे ज्यादा साक्ष्य बुद्ध धम्म के होने के ही मिले हैं. खुदाई की सतत प्रक्रिया और बुद्ध धम्म के विश्व व्यापकता के स्वतः प्रमाण इसी खुदाई में मिलते रहे हैं. बुद्ध धम्म के कारण आज भी भारत विश्व गुरु के बैभव से विभूषित है. सम्राट अशोक के काल में भारत बुद्ध धम्ममय एक अखंड देश था. भारत सांस्कृतिक, राजनीतिक (प्रजातांत्रिक) एवं आर्थिक रूप से समृद्ध था. इस धम्म का प्रसार भी यहीं से अन्य देशों में हुआ और खुदाई इसका प्रमाण भी देती हैं. आज दुनिया के 170 देशों में बौद्ध धम्म विद्यमान है. बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र में एक करोड़ बुद्धिस्ट हैं. इस आंकड़े से बौद्ध धम्म के प्रसार का अंदाजा लगाया जा सकता है. जहां तक भारत में बौद्ध धम्म के विभिन्न प्रमुख स्थलों की बात है तो यह देश बौद्धमय था और आज भी है. जागृत स्थल का विवरण केवल बुद्ध धम्म की एक छोटी सी भूमिका मात्र है.
बिहार
बोधगया: बिहार प्रदेश में स्थित यह वह स्थान है, जहां सिद्धार्थ को सम्यक सम्बोधि की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाये. उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. आज बोधगया में अनेक देशों ने अपने बुद्ध विहार बनाए हैं. बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व सिद्धार्थ निरंजना नदी के दुसरे किनारे पर स्थित डुंगेश्वरी गुफा में कठिन तपस्या व ध्यान किया करते थे. यह गुफाएं आज भी मौजूद हैं. महाबोधि विहार यहां सबसे पवित्र और दुनिया के बौद्ध शिल्पों में से सबसे सुन्दर व भव्य निर्माणों में से एक है.
राजगीर: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल को बुद्ध के काल में राजगृह अथवा राजगढ़ भी कहा जाता था. पांच पर्वतो से घिरे होने के कारण सुरक्षित यह मगध राज्य की राजधानी भी थी. बुद्ध के समय यहां बिम्बिसार का शासन था. बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा व चतुर्थ वर्षावास यहीं बिताया था. राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था, वहां विशाल विहार बनवाया था जो आज भी विद्यमान है. जापान के सहयोग से यहां राजगीर के गृज्झकूट पर्वत पर विशाल विश्व शांति स्तूप व भव्य विहार निर्मित हुआ है.
वैशाली: बिहार राज्य में स्थित यह स्थल बुद्ध के काल खंड में लिच्छिवी वंश की राजधानी के तौर पर विश्व का प्रथम प्रजातांत्रिक राज्य था. बुद्धत्व प्राप्ति के पांचवें वर्षावास में बुद्ध प्रथम बार वैशाली आएं. उन्होंने पांचवा वर्षावास भी यहीं गुजारा. भगवान बुद्ध ने भिक्खुणी संघ की स्थापना यहीं की, नगरवधू आम्रपाली यहीं पर संघ में शामिल हुई. बुद्ध ने तेवज्ज सूत, महाली सूत, रतन सूत सहित अनेक सुतों की देशना यही की थी. बिहार राज्य की राजधानी पटना से 40 किमी की दुरी पर स्थित इसी वैशाली में बुद्ध ने अपने निर्वाण की पूर्व घोषणा की थी.
केसरिया: बिहार के ही पटना से 105 किमी की दुरी पर व चंपारण जिले में स्थित 104 फीट ऊंचा यह स्तूप विश्व के सबसे बड़े व ऊंचे स्तूपों में से एक है. सन् 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई कर इसके अस्तित्व को दुनिया के समक्ष अनावृत किया गया. ऐसी मान्यता है की बुद्ध जब वैशाली से केसरिया के लिए विदा हो रहे थे तब वैशाली के लोगों को भिक्षापात्र दान में दिया था. इसके पश्चात इस भिक्षापात्र को वैशाली के मठ में रखा गया जहां किसान और फल व्यापारी अपनी फसल काटने के बाद सर्वप्रथम इसी पात्र को समर्पित करते थे.
नालंदा: बिहार के पटना से 80 किमी की दूरी पर स्थित नालंदा विश्विद्यालय के रूप में विश्व विख्यात नालंदा महाविहार कभी पूरे विश्व समूह का गौरव था. यह मानव के विकास और प्रकृति से समन्वय से जुड़े शुद्ध ज्ञान का केंद्र था. अपने पूर्ण वैभव में यहां 10 हजार विद्यार्थी और 2 हजार अध्यापक थे. यहां के कुछ प्रसिद्ध छात्रों में इत्सिंग, ह्वेनसांग, फ़ो–ताऊ-माऊ, ताओ शिंग, हुएं चाओ, धर्मस्वामिन, आर्यभट् आदि प्रमुख हैं. शिक्षकों में यहां 1 हजार शिक्षक ऐसे थे जो 30 विषयों के ज्ञाता थे व शिक्षा दे सकते थे. नालंदा के प्राचीन खंडहरों से 12 किमी. दूर राजगीर में 433 एकड़ भूमि में निर्माणधीन व संचालित नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः दुहराने की दिशा में अग्रसर है.
विक्रमशिला महाविहार: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल की खुदाई में एक पुस्तकालय, स्तूप और वृहद् मठ प्राप्त हुआ है.
उत्तर प्रदेश
सारनाथ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित व वाराणसी रेलवे स्टेशन से 5 किमी. की दुरी पर यह स्थल बुद्ध धम्म में एक प्रतीक स्थल के रूप में विश्व विख्यात है. यही वह पवित्र स्थल है, जहां बुद्ध ने अपनी प्रथम देशना (उपदेश) की थी. बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबके कल्याण हेतु बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच पुराने मित्रो को धम्मोप्देश दिए. पहली बार बताया की उन्होंने कल्याणकारी आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज लिया है. इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्खु संघ की स्थापना भी की.
कुशीनगर: उतर प्रदेश का यह जिला बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है. यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है. यहीं भगवान बुद्ध ने अंतिम सांसे ली थी. यहां भगवान बुद्ध ने दो साल वृक्षों के बीच में लेटकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. यहां भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण नामक विशाल स्तूप विद्यमान है. जहां बुद्ध ने अंतिम सांसे ली वह स्थल भी मौजूद है. पुराने खंडहर आज भी अपने इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं.
जौनपुर: मुख्यालय से 55 किमी दूर मादरडीह गांव में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व में उत्खनन कार्य संपन्न हो रहा है. सर्वेक्षण कर रही टीम को स्तूप व बुद्ध विहार होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. बुद्ध विहार की दीवार के अवशेष भी मिले हैं. अब तक के उत्खनन से यह ध्वनित हो रहा है की लगभग ढ़ाई हज़ार वर्ष पूर्व यहां नगरीय सभ्यता मौजूद थी. संभव है कि यह स्थान विशेष व्यापार–वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा हो.
उत्तर प्रदेश में ही बुद्ध के अन्य तीर्थस्थलों में श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी एवं मथुरा आदि है.
मध्य प्रदेश
साँची: मध्य प्रदेश में स्थित साँची बौद्ध स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है. स्तूपों के लिए प्रसिद्ध यहां कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं. ईसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवी सदी के दरम्यान बने स्तूप, मठों, विहार और स्तंभों के लिए जाना जाता है. यहां निर्मित स्तूप तोरणों से घिरे हैं. स्तूप के द्वार की मेहराब पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र खुदा है. यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है. साँची में कुल 36 मठ, 18 विहार, एक स्तूप के साथ ही एक अशोक स्तंभ मौजूद है. 1854 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग ने यहां खुदाई करवाई थी.
उज्जैन: भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को संचित कर बने स्तुप 2500 वर्ष से ज्यादा प्राचीन हैं. यह स्तूप उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किमी दुरी पर ही अवस्थित है.
भरहुत स्तूप: प्रदेश के सतना जिले में स्थित यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है. इस स्तूप को सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी सदी में निर्मित करवाया था. इस स्तूप में बुद्ध को बौद्ध प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है. जैसे बुद्ध के पद चिन्ह, धम्मचक्र, बोधिवृक्ष इत्यादि.
ग्वालियरः हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर में शिवपुरी जिले के राजापुर गांव में करीब 2200 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है. यह ईसा पूर्व शुंग वंश के काल का बताया जा रहा है. ग्रामीण इसे अंचल का पहला बौद्ध स्तूप बता रहे हैं. गांव के लोग अब तक इस स्तूप को कुटिया मठ्ठ के नाम से पहचानते आ रहे थे. पुरातत्वविदों का मानना है कि स्तूप के नीचे तांबे का कलश हो सकता है और उसमें सम्राट अशोक की अस्थियां एवं राख हो सकती है. ग्वालियर चंबल संभाग में पहला बौद्ध स्तूप ज्यादातर बपाल, विदिशा, देवास, होशंगाबाद के आस-पास के क्षेत्रों में मिले हैं.
ओडिशा
यह स्थान बुद्ध धम्म संस्कृति के प्रमुख स्थलों में से एक है. प्राचीन बौद्ध विरासत से समृद्ध ओडिशा (उड़िसा) में क्षतिग्रस्त बुद्ध विहार एव स्तूप सर्वत्र विद्यमान हैं. वोलंगीर, ढ़ेनकनाल, फूलबनी, कालाहांडी, संभलपुर, क्योंझार, गंजम, वालासोर और पूरी आदि जिलों में कई महत्वपूर्ण शोध किये गए है, जहां बुद्ध अवशेष या तो मौजूद हैं या प्रमाण मिला है. इस राज्य में बुद्ध धम्म स्मारकों की सर्वोत्तम निधि कटक और जाजपुर जिलों में केद्रित है. इस परिक्षेत्र में ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरि एवं लान्गुली में बुद्ध विहारों, स्तूपों और शिलालेखों के रूप में बौद्ध अवशेषों की विशाल निधि है.
ललितगिरी: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 85 किमी. की दुरी पर स्थित यह स्थल प्रथम ईस्वी सदी में स्थापित किया गया था. यह ओडिशा का सबसे उत्कृष्ट कलात्मक, प्राचीन एवं भव्य स्थलों में से है. खंडहरों में तब्दील हो चुके इस स्थल की खोज 1985 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी थी. यहां उत्खनन में भगवान् बुद्ध की अस्थिधातु प्राप्त हुई थी. मुख्य स्तूप के अतिरिक्त यहां तीन विशाल विहार, बहुकक्षों वाले चैत्यगृहों के अवशेष विद्यमान हैं.
उदयगिरी: सातवीं सदी में यहां ओडिशा का सबसे वृहद् बौद्ध परिसर था जो करीब करीब 400 एकड़ में विस्तारित था. यहां दो विशाल विहार है तथा दोनों एक साथ मिलकर अपने समय की सबसे वृहद् बौद्ध स्थापनाएं हैं. यह स्थल भुवनेश्वर से 93 किमी. की दुरी पर स्थित है.
रत्नगिरि: यह स्थान बुद्ध धम्म की अन्य शाखा जैसे महायान एवं वज्रयान परंपरा का प्रमुख तीर्थस्थल है. इसमें विहार के दरवाजों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गयी है. रत्नगिरि बौद्ध शिल्पकला के दृष्टिकोण से अत्यंत उनन्त थी, यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालय में अनेकों प्रकार के पत्थर की शिल्पकला व अवशेष संरक्षित हैं. भुवनेश्वर से 91 किमी. की दुरी पर स्थित रत्नगिरि में तारा, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री और ध्यानी बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं.
लान्गुली: ओडिशा के प्राचीनतम बौद्ध स्थल के रूप में दर्ज इस स्थल की खोज बाद में हुई. जैपोर जिला मुख्यालय से 6 किमी. की दुरी पर स्थित इस स्थल की खोज के उपरांत ये सर्वविदित हुआ की यहाँ ह्वेनसांग का वैभवशाली पुष्पगिरी महाविहार हैं. यह शिक्षा के महानतम केन्द्रों में से एक था.
धौली: भुवनेश्वर से 8 किमी. की दुरी पर स्थित धौली कलिंग युद्ध का मूक साक्षी है जिसने शासनप्रिय अशोक को धम्मानुरागी में परिवर्तित कर दिया. कलिंग युद्ध के बाद ही बुद्ध धम्म का गौरव पुरे भारत में फैला और भारत विश्व गुरु हो अखंड बना. जापान के सहयोग से यहां एक विशाल स्तूप निर्मित है.
हरियाणा
कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य के धम्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक बुद्ध स्तूपों का वर्णन कई ग्रंथों में है. थानेसर के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में यहां आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कुरुभूमि में स्तूपों का वर्णन किया है. भारतवर्ष के महान सम्राट अशोक द्वरा निर्मित बौद्ध स्तूपों के बारे में पुरातत्वविदों का भी एकमत है. वर्तमान में ब्रह्म सरोवर के प्राचीन शेरोन वाले घाट के ठीक सामने पुरातत्व महत्व के एक स्थल पर आज भी जीर्णशीर्ण हालत में एक बौद्ध स्तूप मौजूद है. यहीं (कमल के फूलों के एक झुण्ड) अनोता झील पर बुद्ध ने दीक्षा दी थी. हरियाणा में दूसरा स्तूप पड़ोसी जिला यमुनानगर का चनौती का स्तूप है. अभी इन स्तूपों के संरक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी है.
झारखंड
चतरा: इंटखोरी चतरा में स्थित यह बौद्ध स्तूप भद्रकाली मंदिर परिसर में है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां बुद्ध धम्म अनुयायिओं की भीड़ उमड़ी रहती है. माना जाता है कि पहले यहां बौद्ध स्तूप था, जिसे छिपाने के लिए यहां मंदिर का निर्माण किया गया.
महाराष्ट्र
एलोरा: छठीं एवं नौवीं सदी के दौरान निर्मित गुफा विहार कलचुरी, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के शासनकाल के लिए जाना जाता है. पत्थरों को नक्काशी कर निर्मित गुफाएं, विहार, बड़े हॉल, छोटे आवास अपनी महान शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है.
धम्म्गिरी: यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में स्थित है. यह स्थल मुंबई महानगरी से 135 किमी. की दुरी पर स्थित है. यह अन्तराष्ट्रीय विपस्सना अकादमी का मुख्यालय है. बुद्ध धम्म के बड़े शोध केन्द्रों में से एक यहां पुरे साल विपस्सना शिविरों का आयोजन होता रहता है.
ड्रैगन पैलेस विहार: यह बुद्ध विहार कामठी, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है. 14 एकड़ भूमि में फैले इस विहार में एक विशाल म्यूजियम, वातानुकूलित सभागार, एक सामुदायिक भवन एवं एक पुस्तकालय है.
कान्हेरी गुफा एवं अन्य स्थल: कान्हेरी गुफा मुंबई के बोरीवली में स्थित है. इसके आलावा महाराष्ट्र में दादर, चैत्यभूमि, राजगढ़, सतारा, पुणे, औरंगाबाद जिले में दर्शनीय स्तूप एवं अन्य बौद्ध अवशेष विद्यमान हैं.
छत्तीसगढ़
सिरपुर: रायपुर से 78 किमी. की दुरी पर महासमुंद जिले में स्थित यह स्थान छठी एवं 10वीं सदी में एक प्रमुख बौद्ध स्थल था और यहां चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भ्रमण किया था. सन् 2013 में परम पावन दलाई लामा के आने से इस स्थल का गौरव पुनः स्थापित हुआ है. उत्खनन से यहां 10 बुद्ध विहार व दस हजार बौद्ध भिक्खुओं के अध्ययन के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त कई बौद्ध स्तूप व नागार्जुन के आने के प्रमाण भी मिले हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है. नालंदा में चार बुद्ध विहार मिले हैं जबकि यहां अब तक 10 बुद्ध विहार के होने के साक्ष्य प्राप्त हो चुके है.
आंध्र प्रदेश
अमरावती स्तूप: गुंटूर जिले में स्थित इसी स्तूप से स्तूप उपासना की शुरुआत हुई थी. यह भारत में निर्मित सबसे वृहद् स्तूप था, हालांकि अब इसके अवशेष ही बचे हैं. बुद्ध धम्म के विख्यात आचार्य बुद्धघोष का पता यहीं से मिलता है. आन्ध्र प्रदेश में अब तक 150 बौद्ध स्थलों की खुदाई हो चुकी है. प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध धम्म यहां दूसरी सदी ईसा पूर्व से 14 वीं सदी तक अपने पुरे वैभव में मौजूद था व पुरे दक्षिण भारत में फैला.
चंदावरम स्तूप: यह दुर्लभ स्तूप आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम् जिले के चंद्रवरम में स्थित है. भारत के उतर से दक्षिण कांचीपुरम जाने के लिए एक पड़ाव था, संभवतः इसलिए यहां बुद्ध विहार बनवाया गया था.
विजयवाड़ा: बौद्ध विरासत को समेटे यहां उंडवल्ली गुफा है जो की उंडवल्ली ग्राम का ही हिस्सा है. गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित इस गुफा को भिक्खुओं के मठ के रूप में उपयोग में लाया जाता था.
कर्नाटक
सनाती: कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के चितापुर तहसील में स्थित सनाती बौद्ध वास्तुशिल्प के उत्कृष्टतम स्थलों में से एक है. भीमा नदी के तट पर स्थित सनाती को 1954 में पहचाना गया. 1964 से 1966 के दरम्यान पुरातत्व विभाग द्वारा इसका विधिवत सर्वेक्षण पूरा हुआ. उत्खनन से शिलालेख, पक्की मिटटी की भृतिकाएं आदि प्राप्त हुए हैं. इसी इलाके में मौजूद अनेक स्तूपों से यहां बुद्ध धम्म के विस्तार की पुष्टि होती है.
कंगनाहल्ली: यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये गए उत्खनन से भीमा नदी के तट पर विशाल स्तूप, बाएं तट पर एक विहार परिसर तथा उसके समीप एक चैत्यगृह प्रकट हुए हैं.
गुजरात
जूनागढ़: तीसरी व चौथी सदी में निर्मित खपरा कोडिय गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है. जूनागढ़ जिला अशोक के काल से ही एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था. यहां अनेकों बौद्ध स्तूप, मठ, प्रस्तर गुफाएं व विशाल चैत्य हैं. अहमदाबाद से करीब 128 किमी. दूर बनास और रुपेन नदी के बीच मौजूद एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, जहां 12 सेलनुमा संरचना है जो पूर्व में बुद्ध विहार रहा होगा. चीनी यात्री वडनगर के आसपास के इलाको में आये थे जिन्होंने इन इलाकों का विस्तृत वर्णन भी किया है. पुरातत्विदों ने बुद्ध मूर्ति सहित करीब 2000 कलाकृतियां खोजी है, जो अब महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा के पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है.
हिमाचल प्रदेश
धनकर बौद्ध मठ: यह बौद्ध मठ धनकर ग्राम में हिमाचल के स्पिति में 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. स्पीति और पिन नदी के संगम पर स्थित यह स्थल दुनियां में बुद्ध धम्म के ऐतिहासिक विरासतों में स्थान रखता है.
कश्मीर
परिहासपुर: श्रीनगर से 26 किमी. की दुरी पर बारामुला के पास स्थित इस स्थल पर कई बुद्ध विहार, चैत्य व स्तूप पाए गए हैं.
हारवन बौद्ध स्तूप: श्रीनगर में स्थित इस विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल की खोज सर अर्ल स्टेन ने की थी. यहां चौथी सदी में तृतीय बुद्ध धम्म संगीति का आयोजन हुआ था. यहां निर्मित स्तूप कुषाण काल के हैं. इस स्तूप का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है. खुदाई में प्राप्त अवशेषों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने म्यूजियम में रखा है वहीं कुछ अवशेष विश्व म्यूजियम में संरक्षित है.
अरुणाचल प्रदेश
तक्त्सांग मठ: यहां महान बौद्ध गुरु पद्मसंभव ने ध्यान साधना की थी. इस मठ का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था. छोटी सी पहाड़ी के टीले पर स्थित यह मठ हरे भरे वन से घिरा हुआ है. यहां का शांत निर्मल माहौल मन को सुकून देता है.
गोरसम चोरटेन: तवांग कस्बे से 90 किमी. दूर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तूप है. ऐसी मान्यता है कि इस स्तूप का निर्माण 12वीं सदी में एक लामा प्राधार द्वारा किया गया था. गली गली में विस्तार लिए हुए अरुणाचल प्रदेश में आज अनेक मठ विद्धमान हैं, जिनमें उर्गेलिंग मठ, बोमडिला मठ इत्यादि प्रमुख हैं.
दो द्रुल चोर्टन स्तूप: यह गंगटोक के प्रमुख आकर्षण में एक है. इसे सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है. इसकी स्थापना त्रुलुसी रिम्पोचे ने 1945 ईस्वी में की थी. सिक्किम में भी अनेकों मठ मौजूद हैं.
पंजाब
संघोल: फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित एक गांव है जो चंडीगढ़ से 40 किमी दूर है. यहां प्रथम सदी में निर्मित बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं एवं एक महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्खु के अस्थि अवशेष और बौद्ध मठ भी सामने आए हैं.
गोवा
लेमगांव गुफा: लेमगांव गुफा भिक्खुओं द्वारा ध्यान व निवास स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता था. लेमगांव शब्द का मतलब है, लामाओं का निवास. यह स्थल उतरी गोवा के बिचोलिम शहर से 2 किमी दूर है.
राज्स्थान
विराट बौद्ध मठ: जयपुर में स्थित इस स्थल पर सम्राट अशोक यहां स्वयं आये थे. वर्षों तक यह बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा. यहां एक बौद्ध स्तूप भी है जिसका आकार सांची के स्तूप के कलाशिल्प से मिलता है.
तामिलनाडु
कवेरीपुमपट्टीनम: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में कवेरीपुमपट्टीनम के एक मंदिर में अनेको बुद्ध मूर्ति एवं कांस्य कलाकृतियों के प्राप्त होने से राज्य में बुद्ध धम्म के प्रभाव का पता चलता है. राज्य के ही नागपट्टीनम बुद्ध के काल के उन्नत भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए है जो विदेशी सहयोग से निर्मित थे.
तथागत बुद्ध से जुड़ी स्मृतियों, अवशेषों व धरोहरों की खोज निरंतर जारी है. उपरोक्त जानकारी से यह बात सामने है कि कि भारत देश में जहां देशों वहीं बुद्ध विद्यमान हैं. यह स्थिति तब है, जब बौद्ध धम्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया. भारतवर्ष का एक-एक ईंट, एक-एक पत्थर कहता है की भारत बुद्धमय है. बुद्ध का शासन हमारे मन पर है. दुनिया के सभी देशों में खुदाई से बुद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं. कभी कभी तो युद्ध में विध्वंस के पश्चात बुद्ध की मुर्तिया भूमि के गर्भ से निकली. एक कहावत भी है कि ‘हुआ युद्ध निकले बुद्ध’. बुद्ध शालीनता से देश के हर राज्य में हर गांव-मुहल्ले में मौजूद हैं.
ईसा की प्रथम शताब्दी तक एशिया महादेश के अधिकतर देशों में बुद्ध धम्म स्थापित हो चुका था. इसकी आधारशिला ईसा पूर्व 250 के आस पास मौर्य वंश के यशस्वी सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म-प्रचार के लिए श्रीलंका भेजकर रख दी थी. ईसा की छठी शताब्दी के आस पास जब एशिया के देशों के मध्य सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संक्रमण का दौर शुरू हुआ तो अरबी-तुर्की यात्रियों व्यापारियों को जगह जगह बुद्ध मिलते. वे यात्री व्यापारी चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका आदि जहां भी जाते, वहां के पगोडा, मठ या विहार और स्तूपों में उन्हें आंखे मूंदे, मुस्कुराती हुई एक सौम्य मूर्ति अवश्य दिखाई देती. यदि स्थानीय व्यक्तियों से वो मूर्तियों के विषय में अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते तो केवल एक ही उतर मिलता, यह ‘बुद्ध’ हैं. अन्ततः बुद्ध शब्द अरबी, फ़ारसी भाषा में अपभ्रंशित हो बुत हो गया, जिसका अर्थ ही मान लिया गया मूर्ति. बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग पांच सौ वर्षो के पश्चात भारत में महायानी शाखा ने बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना शुरू की और कालांतर में लगभग पूरे पश्चिम एशिया में बुद्ध फ़ैल गये. चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि सभी जगह. भारत में बुद्ध संस्कृति का प्रभाव एवं विस्तार देश के कोने कोने में है. यह बात प्रमाणिकता से इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में अब तक सबसे ज्यादा साक्ष्य बुद्ध धम्म के होने के ही मिले हैं. खुदाई की सतत प्रक्रिया और बुद्ध धम्म के विश्व व्यापकता के स्वतः प्रमाण इसी खुदाई में मिलते रहे हैं. बुद्ध धम्म के कारण आज भी भारत विश्व गुरु के बैभव से विभूषित है. सम्राट अशोक के काल में भारत बुद्ध धम्ममय एक अखंड देश था. भारत सांस्कृतिक, राजनीतिक (प्रजातांत्रिक) एवं आर्थिक रूप से समृद्ध था. इस धम्म का प्रसार भी यहीं से अन्य देशों में हुआ और खुदाई इसका प्रमाण भी देती हैं. आज दुनिया के 170 देशों में बौद्ध धम्म विद्यमान है. बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र में एक करोड़ बुद्धिस्ट हैं. इस आंकड़े से बौद्ध धम्म के प्रसार का अंदाजा लगाया जा सकता है. जहां तक भारत में बौद्ध धम्म के विभिन्न प्रमुख स्थलों की बात है तो यह देश बौद्धमय था और आज भी है. जागृत स्थल का विवरण केवल बुद्ध धम्म की एक छोटी सी भूमिका मात्र है.
बिहार
बोधगया: बिहार प्रदेश में स्थित यह वह स्थान है, जहां सिद्धार्थ को सम्यक सम्बोधि की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाये. उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. आज बोधगया में अनेक देशों ने अपने बुद्ध विहार बनाए हैं. बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व सिद्धार्थ निरंजना नदी के दुसरे किनारे पर स्थित डुंगेश्वरी गुफा में कठिन तपस्या व ध्यान किया करते थे. यह गुफाएं आज भी मौजूद हैं. महाबोधि विहार यहां सबसे पवित्र और दुनिया के बौद्ध शिल्पों में से सबसे सुन्दर व भव्य निर्माणों में से एक है.
राजगीर: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल को बुद्ध के काल में राजगृह अथवा राजगढ़ भी कहा जाता था. पांच पर्वतो से घिरे होने के कारण सुरक्षित यह मगध राज्य की राजधानी भी थी. बुद्ध के समय यहां बिम्बिसार का शासन था. बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा व चतुर्थ वर्षावास यहीं बिताया था. राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था, वहां विशाल विहार बनवाया था जो आज भी विद्यमान है. जापान के सहयोग से यहां राजगीर के गृज्झकूट पर्वत पर विशाल विश्व शांति स्तूप व भव्य विहार निर्मित हुआ है.
वैशाली: बिहार राज्य में स्थित यह स्थल बुद्ध के काल खंड में लिच्छिवी वंश की राजधानी के तौर पर विश्व का प्रथम प्रजातांत्रिक राज्य था. बुद्धत्व प्राप्ति के पांचवें वर्षावास में बुद्ध प्रथम बार वैशाली आएं. उन्होंने पांचवा वर्षावास भी यहीं गुजारा. भगवान बुद्ध ने भिक्खुणी संघ की स्थापना यहीं की, नगरवधू आम्रपाली यहीं पर संघ में शामिल हुई. बुद्ध ने तेवज्ज सूत, महाली सूत, रतन सूत सहित अनेक सुतों की देशना यही की थी. बिहार राज्य की राजधानी पटना से 40 किमी की दुरी पर स्थित इसी वैशाली में बुद्ध ने अपने निर्वाण की पूर्व घोषणा की थी.
केसरिया: बिहार के ही पटना से 105 किमी की दुरी पर व चंपारण जिले में स्थित 104 फीट ऊंचा यह स्तूप विश्व के सबसे बड़े व ऊंचे स्तूपों में से एक है. सन् 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई कर इसके अस्तित्व को दुनिया के समक्ष अनावृत किया गया. ऐसी मान्यता है की बुद्ध जब वैशाली से केसरिया के लिए विदा हो रहे थे तब वैशाली के लोगों को भिक्षापात्र दान में दिया था. इसके पश्चात इस भिक्षापात्र को वैशाली के मठ में रखा गया जहां किसान और फल व्यापारी अपनी फसल काटने के बाद सर्वप्रथम इसी पात्र को समर्पित करते थे.
नालंदा: बिहार के पटना से 80 किमी की दूरी पर स्थित नालंदा विश्विद्यालय के रूप में विश्व विख्यात नालंदा महाविहार कभी पूरे विश्व समूह का गौरव था. यह मानव के विकास और प्रकृति से समन्वय से जुड़े शुद्ध ज्ञान का केंद्र था. अपने पूर्ण वैभव में यहां 10 हजार विद्यार्थी और 2 हजार अध्यापक थे. यहां के कुछ प्रसिद्ध छात्रों में इत्सिंग, ह्वेनसांग, फ़ो–ताऊ-माऊ, ताओ शिंग, हुएं चाओ, धर्मस्वामिन, आर्यभट् आदि प्रमुख हैं. शिक्षकों में यहां 1 हजार शिक्षक ऐसे थे जो 30 विषयों के ज्ञाता थे व शिक्षा दे सकते थे. नालंदा के प्राचीन खंडहरों से 12 किमी. दूर राजगीर में 433 एकड़ भूमि में निर्माणधीन व संचालित नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः दुहराने की दिशा में अग्रसर है.
विक्रमशिला महाविहार: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल की खुदाई में एक पुस्तकालय, स्तूप और वृहद् मठ प्राप्त हुआ है.
उत्तर प्रदेश
सारनाथ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित व वाराणसी रेलवे स्टेशन से 5 किमी. की दुरी पर यह स्थल बुद्ध धम्म में एक प्रतीक स्थल के रूप में विश्व विख्यात है. यही वह पवित्र स्थल है, जहां बुद्ध ने अपनी प्रथम देशना (उपदेश) की थी. बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबके कल्याण हेतु बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच पुराने मित्रो को धम्मोप्देश दिए. पहली बार बताया की उन्होंने कल्याणकारी आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज लिया है. इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्खु संघ की स्थापना भी की.
कुशीनगर: उतर प्रदेश का यह जिला बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है. यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है. यहीं भगवान बुद्ध ने अंतिम सांसे ली थी. यहां भगवान बुद्ध ने दो साल वृक्षों के बीच में लेटकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. यहां भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण नामक विशाल स्तूप विद्यमान है. जहां बुद्ध ने अंतिम सांसे ली वह स्थल भी मौजूद है. पुराने खंडहर आज भी अपने इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं.
जौनपुर: मुख्यालय से 55 किमी दूर मादरडीह गांव में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व में उत्खनन कार्य संपन्न हो रहा है. सर्वेक्षण कर रही टीम को स्तूप व बुद्ध विहार होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. बुद्ध विहार की दीवार के अवशेष भी मिले हैं. अब तक के उत्खनन से यह ध्वनित हो रहा है की लगभग ढ़ाई हज़ार वर्ष पूर्व यहां नगरीय सभ्यता मौजूद थी. संभव है कि यह स्थान विशेष व्यापार–वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा हो.
उत्तर प्रदेश में ही बुद्ध के अन्य तीर्थस्थलों में श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी एवं मथुरा आदि है.
मध्य प्रदेश
साँची: मध्य प्रदेश में स्थित साँची बौद्ध स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है. स्तूपों के लिए प्रसिद्ध यहां कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं. ईसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवी सदी के दरम्यान बने स्तूप, मठों, विहार और स्तंभों के लिए जाना जाता है. यहां निर्मित स्तूप तोरणों से घिरे हैं. स्तूप के द्वार की मेहराब पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र खुदा है. यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है. साँची में कुल 36 मठ, 18 विहार, एक स्तूप के साथ ही एक अशोक स्तंभ मौजूद है. 1854 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग ने यहां खुदाई करवाई थी.
उज्जैन: भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को संचित कर बने स्तुप 2500 वर्ष से ज्यादा प्राचीन हैं. यह स्तूप उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किमी दुरी पर ही अवस्थित है.
भरहुत स्तूप: प्रदेश के सतना जिले में स्थित यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है. इस स्तूप को सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी सदी में निर्मित करवाया था. इस स्तूप में बुद्ध को बौद्ध प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है. जैसे बुद्ध के पद चिन्ह, धम्मचक्र, बोधिवृक्ष इत्यादि.
ग्वालियरः हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर में शिवपुरी जिले के राजापुर गांव में करीब 2200 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है. यह ईसा पूर्व शुंग वंश के काल का बताया जा रहा है. ग्रामीण इसे अंचल का पहला बौद्ध स्तूप बता रहे हैं. गांव के लोग अब तक इस स्तूप को कुटिया मठ्ठ के नाम से पहचानते आ रहे थे. पुरातत्वविदों का मानना है कि स्तूप के नीचे तांबे का कलश हो सकता है और उसमें सम्राट अशोक की अस्थियां एवं राख हो सकती है. ग्वालियर चंबल संभाग में पहला बौद्ध स्तूप ज्यादातर बपाल, विदिशा, देवास, होशंगाबाद के आस-पास के क्षेत्रों में मिले हैं.
ओडिशा
यह स्थान बुद्ध धम्म संस्कृति के प्रमुख स्थलों में से एक है. प्राचीन बौद्ध विरासत से समृद्ध ओडिशा (उड़िसा) में क्षतिग्रस्त बुद्ध विहार एव स्तूप सर्वत्र विद्यमान हैं. वोलंगीर, ढ़ेनकनाल, फूलबनी, कालाहांडी, संभलपुर, क्योंझार, गंजम, वालासोर और पूरी आदि जिलों में कई महत्वपूर्ण शोध किये गए है, जहां बुद्ध अवशेष या तो मौजूद हैं या प्रमाण मिला है. इस राज्य में बुद्ध धम्म स्मारकों की सर्वोत्तम निधि कटक और जाजपुर जिलों में केद्रित है. इस परिक्षेत्र में ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरि एवं लान्गुली में बुद्ध विहारों, स्तूपों और शिलालेखों के रूप में बौद्ध अवशेषों की विशाल निधि है.
ललितगिरी: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 85 किमी. की दुरी पर स्थित यह स्थल प्रथम ईस्वी सदी में स्थापित किया गया था. यह ओडिशा का सबसे उत्कृष्ट कलात्मक, प्राचीन एवं भव्य स्थलों में से है. खंडहरों में तब्दील हो चुके इस स्थल की खोज 1985 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी थी. यहां उत्खनन में भगवान् बुद्ध की अस्थिधातु प्राप्त हुई थी. मुख्य स्तूप के अतिरिक्त यहां तीन विशाल विहार, बहुकक्षों वाले चैत्यगृहों के अवशेष विद्यमान हैं.
उदयगिरी: सातवीं सदी में यहां ओडिशा का सबसे वृहद् बौद्ध परिसर था जो करीब करीब 400 एकड़ में विस्तारित था. यहां दो विशाल विहार है तथा दोनों एक साथ मिलकर अपने समय की सबसे वृहद् बौद्ध स्थापनाएं हैं. यह स्थल भुवनेश्वर से 93 किमी. की दुरी पर स्थित है.
रत्नगिरि: यह स्थान बुद्ध धम्म की अन्य शाखा जैसे महायान एवं वज्रयान परंपरा का प्रमुख तीर्थस्थल है. इसमें विहार के दरवाजों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गयी है. रत्नगिरि बौद्ध शिल्पकला के दृष्टिकोण से अत्यंत उनन्त थी, यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालय में अनेकों प्रकार के पत्थर की शिल्पकला व अवशेष संरक्षित हैं. भुवनेश्वर से 91 किमी. की दुरी पर स्थित रत्नगिरि में तारा, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री और ध्यानी बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं.
लान्गुली: ओडिशा के प्राचीनतम बौद्ध स्थल के रूप में दर्ज इस स्थल की खोज बाद में हुई. जैपोर जिला मुख्यालय से 6 किमी. की दुरी पर स्थित इस स्थल की खोज के उपरांत ये सर्वविदित हुआ की यहाँ ह्वेनसांग का वैभवशाली पुष्पगिरी महाविहार हैं. यह शिक्षा के महानतम केन्द्रों में से एक था.
धौली: भुवनेश्वर से 8 किमी. की दुरी पर स्थित धौली कलिंग युद्ध का मूक साक्षी है जिसने शासनप्रिय अशोक को धम्मानुरागी में परिवर्तित कर दिया. कलिंग युद्ध के बाद ही बुद्ध धम्म का गौरव पुरे भारत में फैला और भारत विश्व गुरु हो अखंड बना. जापान के सहयोग से यहां एक विशाल स्तूप निर्मित है.
हरियाणा
कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य के धम्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक बुद्ध स्तूपों का वर्णन कई ग्रंथों में है. थानेसर के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में यहां आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कुरुभूमि में स्तूपों का वर्णन किया है. भारतवर्ष के महान सम्राट अशोक द्वरा निर्मित बौद्ध स्तूपों के बारे में पुरातत्वविदों का भी एकमत है. वर्तमान में ब्रह्म सरोवर के प्राचीन शेरोन वाले घाट के ठीक सामने पुरातत्व महत्व के एक स्थल पर आज भी जीर्णशीर्ण हालत में एक बौद्ध स्तूप मौजूद है. यहीं (कमल के फूलों के एक झुण्ड) अनोता झील पर बुद्ध ने दीक्षा दी थी. हरियाणा में दूसरा स्तूप पड़ोसी जिला यमुनानगर का चनौती का स्तूप है. अभी इन स्तूपों के संरक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी है.
झारखंड
चतरा: इंटखोरी चतरा में स्थित यह बौद्ध स्तूप भद्रकाली मंदिर परिसर में है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां बुद्ध धम्म अनुयायिओं की भीड़ उमड़ी रहती है. माना जाता है कि पहले यहां बौद्ध स्तूप था, जिसे छिपाने के लिए यहां मंदिर का निर्माण किया गया.
महाराष्ट्र
एलोरा: छठीं एवं नौवीं सदी के दौरान निर्मित गुफा विहार कलचुरी, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के शासनकाल के लिए जाना जाता है. पत्थरों को नक्काशी कर निर्मित गुफाएं, विहार, बड़े हॉल, छोटे आवास अपनी महान शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है.
धम्म्गिरी: यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में स्थित है. यह स्थल मुंबई महानगरी से 135 किमी. की दुरी पर स्थित है. यह अन्तराष्ट्रीय विपस्सना अकादमी का मुख्यालय है. बुद्ध धम्म के बड़े शोध केन्द्रों में से एक यहां पुरे साल विपस्सना शिविरों का आयोजन होता रहता है.
ड्रैगन पैलेस विहार: यह बुद्ध विहार कामठी, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है. 14 एकड़ भूमि में फैले इस विहार में एक विशाल म्यूजियम, वातानुकूलित सभागार, एक सामुदायिक भवन एवं एक पुस्तकालय है.
कान्हेरी गुफा एवं अन्य स्थल: कान्हेरी गुफा मुंबई के बोरीवली में स्थित है. इसके आलावा महाराष्ट्र में दादर, चैत्यभूमि, राजगढ़, सतारा, पुणे, औरंगाबाद जिले में दर्शनीय स्तूप एवं अन्य बौद्ध अवशेष विद्यमान हैं.
छत्तीसगढ़
सिरपुर: रायपुर से 78 किमी. की दुरी पर महासमुंद जिले में स्थित यह स्थान छठी एवं 10वीं सदी में एक प्रमुख बौद्ध स्थल था और यहां चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भ्रमण किया था. सन् 2013 में परम पावन दलाई लामा के आने से इस स्थल का गौरव पुनः स्थापित हुआ है. उत्खनन से यहां 10 बुद्ध विहार व दस हजार बौद्ध भिक्खुओं के अध्ययन के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त कई बौद्ध स्तूप व नागार्जुन के आने के प्रमाण भी मिले हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है. नालंदा में चार बुद्ध विहार मिले हैं जबकि यहां अब तक 10 बुद्ध विहार के होने के साक्ष्य प्राप्त हो चुके है.
आंध्र प्रदेश
अमरावती स्तूप: गुंटूर जिले में स्थित इसी स्तूप से स्तूप उपासना की शुरुआत हुई थी. यह भारत में निर्मित सबसे वृहद् स्तूप था, हालांकि अब इसके अवशेष ही बचे हैं. बुद्ध धम्म के विख्यात आचार्य बुद्धघोष का पता यहीं से मिलता है. आन्ध्र प्रदेश में अब तक 150 बौद्ध स्थलों की खुदाई हो चुकी है. प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध धम्म यहां दूसरी सदी ईसा पूर्व से 14 वीं सदी तक अपने पुरे वैभव में मौजूद था व पुरे दक्षिण भारत में फैला.
चंदावरम स्तूप: यह दुर्लभ स्तूप आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम् जिले के चंद्रवरम में स्थित है. भारत के उतर से दक्षिण कांचीपुरम जाने के लिए एक पड़ाव था, संभवतः इसलिए यहां बुद्ध विहार बनवाया गया था.
विजयवाड़ा: बौद्ध विरासत को समेटे यहां उंडवल्ली गुफा है जो की उंडवल्ली ग्राम का ही हिस्सा है. गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित इस गुफा को भिक्खुओं के मठ के रूप में उपयोग में लाया जाता था.
कर्नाटक
सनाती: कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के चितापुर तहसील में स्थित सनाती बौद्ध वास्तुशिल्प के उत्कृष्टतम स्थलों में से एक है. भीमा नदी के तट पर स्थित सनाती को 1954 में पहचाना गया. 1964 से 1966 के दरम्यान पुरातत्व विभाग द्वारा इसका विधिवत सर्वेक्षण पूरा हुआ. उत्खनन से शिलालेख, पक्की मिटटी की भृतिकाएं आदि प्राप्त हुए हैं. इसी इलाके में मौजूद अनेक स्तूपों से यहां बुद्ध धम्म के विस्तार की पुष्टि होती है.
कंगनाहल्ली: यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये गए उत्खनन से भीमा नदी के तट पर विशाल स्तूप, बाएं तट पर एक विहार परिसर तथा उसके समीप एक चैत्यगृह प्रकट हुए हैं.
गुजरात
जूनागढ़: तीसरी व चौथी सदी में निर्मित खपरा कोडिय गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है. जूनागढ़ जिला अशोक के काल से ही एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था. यहां अनेकों बौद्ध स्तूप, मठ, प्रस्तर गुफाएं व विशाल चैत्य हैं. अहमदाबाद से करीब 128 किमी. दूर बनास और रुपेन नदी के बीच मौजूद एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, जहां 12 सेलनुमा संरचना है जो पूर्व में बुद्ध विहार रहा होगा. चीनी यात्री वडनगर के आसपास के इलाको में आये थे जिन्होंने इन इलाकों का विस्तृत वर्णन भी किया है. पुरातत्विदों ने बुद्ध मूर्ति सहित करीब 2000 कलाकृतियां खोजी है, जो अब महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा के पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है.
हिमाचल प्रदेश
धनकर बौद्ध मठ: यह बौद्ध मठ धनकर ग्राम में हिमाचल के स्पिति में 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. स्पीति और पिन नदी के संगम पर स्थित यह स्थल दुनियां में बुद्ध धम्म के ऐतिहासिक विरासतों में स्थान रखता है.
कश्मीर
परिहासपुर: श्रीनगर से 26 किमी. की दुरी पर बारामुला के पास स्थित इस स्थल पर कई बुद्ध विहार, चैत्य व स्तूप पाए गए हैं.
हारवन बौद्ध स्तूप: श्रीनगर में स्थित इस विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल की खोज सर अर्ल स्टेन ने की थी. यहां चौथी सदी में तृतीय बुद्ध धम्म संगीति का आयोजन हुआ था. यहां निर्मित स्तूप कुषाण काल के हैं. इस स्तूप का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है. खुदाई में प्राप्त अवशेषों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने म्यूजियम में रखा है वहीं कुछ अवशेष विश्व म्यूजियम में संरक्षित है.
अरुणाचल प्रदेश
तक्त्सांग मठ: यहां महान बौद्ध गुरु पद्मसंभव ने ध्यान साधना की थी. इस मठ का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था. छोटी सी पहाड़ी के टीले पर स्थित यह मठ हरे भरे वन से घिरा हुआ है. यहां का शांत निर्मल माहौल मन को सुकून देता है.
गोरसम चोरटेन: तवांग कस्बे से 90 किमी. दूर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तूप है. ऐसी मान्यता है कि इस स्तूप का निर्माण 12वीं सदी में एक लामा प्राधार द्वारा किया गया था. गली गली में विस्तार लिए हुए अरुणाचल प्रदेश में आज अनेक मठ विद्धमान हैं, जिनमें उर्गेलिंग मठ, बोमडिला मठ इत्यादि प्रमुख हैं.
दो द्रुल चोर्टन स्तूप: यह गंगटोक के प्रमुख आकर्षण में एक है. इसे सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है. इसकी स्थापना त्रुलुसी रिम्पोचे ने 1945 ईस्वी में की थी. सिक्किम में भी अनेकों मठ मौजूद हैं.
पंजाब
संघोल: फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित एक गांव है जो चंडीगढ़ से 40 किमी दूर है. यहां प्रथम सदी में निर्मित बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं एवं एक महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्खु के अस्थि अवशेष और बौद्ध मठ भी सामने आए हैं.
गोवा
लेमगांव गुफा: लेमगांव गुफा भिक्खुओं द्वारा ध्यान व निवास स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता था. लेमगांव शब्द का मतलब है, लामाओं का निवास. यह स्थल उतरी गोवा के बिचोलिम शहर से 2 किमी दूर है.
राज्स्थान
विराट बौद्ध मठ: जयपुर में स्थित इस स्थल पर सम्राट अशोक यहां स्वयं आये थे. वर्षों तक यह बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा. यहां एक बौद्ध स्तूप भी है जिसका आकार सांची के स्तूप के कलाशिल्प से मिलता है.
तामिलनाडु
कवेरीपुमपट्टीनम: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में कवेरीपुमपट्टीनम के एक मंदिर में अनेको बुद्ध मूर्ति एवं कांस्य कलाकृतियों के प्राप्त होने से राज्य में बुद्ध धम्म के प्रभाव का पता चलता है. राज्य के ही नागपट्टीनम बुद्ध के काल के उन्नत भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए है जो विदेशी सहयोग से निर्मित थे.
तथागत बुद्ध से जुड़ी स्मृतियों, अवशेषों व धरोहरों की खोज निरंतर जारी है. उपरोक्त जानकारी से यह बात सामने है कि कि भारत देश में जहां देशों वहीं बुद्ध विद्यमान हैं. यह स्थिति तब है, जब बौद्ध धम्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया. भारतवर्ष का एक-एक ईंट, एक-एक पत्थर कहता है की भारत बुद्धमय है. बुद्ध का शासन हमारे मन पर है. दुनिया के सभी देशों में खुदाई से बुद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं. कभी कभी तो युद्ध में विध्वंस के पश्चात बुद्ध की मुर्तिया भूमि के गर्भ से निकली. एक कहावत भी है कि ‘हुआ युद्ध निकले बुद्ध’. बुद्ध शालीनता से देश के हर राज्य में हर गांव-मुहल्ले में मौजूद हैं. दयाशंकर मुद्दे पर यूपी के महिला आयोग में चुप्पी क्यों?
 क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा अध्यक्ष मायावती को अपशब्द कहने पर भी देश और उत्तर प्रदेश के महिला आयोगों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है? ऐसा क्यों? जो राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए ही बनाये गए है, उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? इसके निम्न कारण हो सकते है:- (1) महिला आयोगों को इसकी सूचना ही ना हो कि इस प्रकार का कोई अपराध हुआ है. (2) महिला आयोगों को ये लगा होगा कि यह कोई अपराध नहीं है और इसलिए इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जब देश की संसद में यह मामला उठाया गया है तो ऐसा असंभव है कि महिला आयोगों को इसकी सूचना ना हो पायी हो, इसलिए कोई कार्यवाही ना करने का यह कारण नहीं हो सकता कि महिला आयोगों को कोई सूचना ही नहीं मिली. अब दूसरे कारण के विषय में विचार किया जाए, जब राष्ट्रीय महिला आयोग अभिनेता सलमान खान द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर कार्यवाही कर सकता है, तो इस मामले में क्यों नहीं कर सकता. क्या महिला आयोग के शब्दकोष के अनुसार उक्त अपशब्द जिसका दयाशंकर सिंह ने ””बहन जी”” के विरुद्ध उपयोग किया आपत्तिजनक नहीं है? इससे यही सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने के पीछे कोई अन्य कारण होगा.
भारतीय समाज के प्रभुत्वशाली शोषक वर्ग की सामंतवादी- ब्राह्मणवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए यही बात प्रकट होती है कि क्योंकि यह मामला अनुसूचित जाति की महिला से सम्बंधित है इसलिए महिला आयोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की. क्योंकि इन ब्राह्मणवादी शोषकों की नजर में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के सम्मान का कोई महत्व नहीं होता. वास्तव में यह केवल स्त्री से सम्बंधित मामला ही नहीं है बल्कि यह पूरे शोषित वर्ग से सम्बंधित मामला है. शोषक वर्ग यह सहन नहीं कर सकता कि शोषित वर्ग में जागृति उत्पन्न हो, उनमें अपने शोषण के कारणों को लेकर चेतना आये और वो शोषण के खात्मे के लिए संघर्ष करने की स्थिति में आ पाएं. क्योकि ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग जिस धन-दौलत पर ऐशोआराम करता है, अपने महल खड़े करता है, अय्याशियां करता है, वो सब धन दौलत इसी शोषित वर्ग के श्रम और पसीने से उत्पन्न होती है. शोषक वर्ग तो शोषित वर्ग का खून चूसने वाला पिस्सू है जो शोषण वर्ग के श्रम के शोषण पर अय्याशियां कर रहा है. ऐसी शोषणकारी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग सतत प्रयत्नशील रहता है. इसी कारण वो नहीं चाहता कि शोषित वर्ग में चेतना का संचार हो और उनमें जागृति आये. लेकिन क्योंकि अब शोषित वर्ग में चेतना का संचार होने लगा है इसीलिए शोषित वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे है.
शोषित वर्ग की महिलाओं के साथ संगठित बलात्कार किये जा रहे है और पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, फ़ौज, मीडिया और सरकार शोषक वर्ग की कठपुतलियां बने हुए है, क्योंकि इन संस्थाओं में यही ब्राह्मणवादी बैठे हुए हैं. इसीलिए सुश्री मायावती ””””बहन जी”””” का अपमान करने के बावजूद श्री दयाशंकर सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की. वास्तव में यह स्त्री – पुरुष संघर्ष नहीं है, वर्ग संघर्ष है. यह शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का संघर्ष है. इसलिए शोषक वर्ग का प्रत्येक सदस्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस शोषणकारी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कार्य कर रहा है. क्योंकि शोषित वर्ग का शोषण करते रहने में ही उनका हित है. शोषित वर्ग के शोषण करने पर ही तो ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग का अस्तित्व टिका हुआ है.
- फेसबुक पोस्ट से
क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा अध्यक्ष मायावती को अपशब्द कहने पर भी देश और उत्तर प्रदेश के महिला आयोगों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है? ऐसा क्यों? जो राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए ही बनाये गए है, उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? इसके निम्न कारण हो सकते है:- (1) महिला आयोगों को इसकी सूचना ही ना हो कि इस प्रकार का कोई अपराध हुआ है. (2) महिला आयोगों को ये लगा होगा कि यह कोई अपराध नहीं है और इसलिए इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जब देश की संसद में यह मामला उठाया गया है तो ऐसा असंभव है कि महिला आयोगों को इसकी सूचना ना हो पायी हो, इसलिए कोई कार्यवाही ना करने का यह कारण नहीं हो सकता कि महिला आयोगों को कोई सूचना ही नहीं मिली. अब दूसरे कारण के विषय में विचार किया जाए, जब राष्ट्रीय महिला आयोग अभिनेता सलमान खान द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर कार्यवाही कर सकता है, तो इस मामले में क्यों नहीं कर सकता. क्या महिला आयोग के शब्दकोष के अनुसार उक्त अपशब्द जिसका दयाशंकर सिंह ने ””बहन जी”” के विरुद्ध उपयोग किया आपत्तिजनक नहीं है? इससे यही सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने के पीछे कोई अन्य कारण होगा.
भारतीय समाज के प्रभुत्वशाली शोषक वर्ग की सामंतवादी- ब्राह्मणवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए यही बात प्रकट होती है कि क्योंकि यह मामला अनुसूचित जाति की महिला से सम्बंधित है इसलिए महिला आयोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की. क्योंकि इन ब्राह्मणवादी शोषकों की नजर में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के सम्मान का कोई महत्व नहीं होता. वास्तव में यह केवल स्त्री से सम्बंधित मामला ही नहीं है बल्कि यह पूरे शोषित वर्ग से सम्बंधित मामला है. शोषक वर्ग यह सहन नहीं कर सकता कि शोषित वर्ग में जागृति उत्पन्न हो, उनमें अपने शोषण के कारणों को लेकर चेतना आये और वो शोषण के खात्मे के लिए संघर्ष करने की स्थिति में आ पाएं. क्योकि ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग जिस धन-दौलत पर ऐशोआराम करता है, अपने महल खड़े करता है, अय्याशियां करता है, वो सब धन दौलत इसी शोषित वर्ग के श्रम और पसीने से उत्पन्न होती है. शोषक वर्ग तो शोषित वर्ग का खून चूसने वाला पिस्सू है जो शोषण वर्ग के श्रम के शोषण पर अय्याशियां कर रहा है. ऐसी शोषणकारी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग सतत प्रयत्नशील रहता है. इसी कारण वो नहीं चाहता कि शोषित वर्ग में चेतना का संचार हो और उनमें जागृति आये. लेकिन क्योंकि अब शोषित वर्ग में चेतना का संचार होने लगा है इसीलिए शोषित वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे है.
शोषित वर्ग की महिलाओं के साथ संगठित बलात्कार किये जा रहे है और पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, फ़ौज, मीडिया और सरकार शोषक वर्ग की कठपुतलियां बने हुए है, क्योंकि इन संस्थाओं में यही ब्राह्मणवादी बैठे हुए हैं. इसीलिए सुश्री मायावती ””””बहन जी”””” का अपमान करने के बावजूद श्री दयाशंकर सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की. वास्तव में यह स्त्री – पुरुष संघर्ष नहीं है, वर्ग संघर्ष है. यह शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का संघर्ष है. इसलिए शोषक वर्ग का प्रत्येक सदस्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस शोषणकारी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कार्य कर रहा है. क्योंकि शोषित वर्ग का शोषण करते रहने में ही उनका हित है. शोषित वर्ग के शोषण करने पर ही तो ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग का अस्तित्व टिका हुआ है.
- फेसबुक पोस्ट से हरियाणाः जातिवादी गुंडों के डर से किया दलित परिवार ने पलायन
 मेवात। मेवात के नीमखेड़ा गांव में जातिवादी गुंडे दलित परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं. परिवार पर जातिवादी गुंडे न केवल अत्याचार कर है बल्कि उन्हें गांव से पलायन करने पर भी मजबूर कर रहे हैं. जिसके चलते दलित परिवार ने गांव छोड़ दिया है. हालांकि जातिवादी गुंडे इस मामले को सियासी रंग देकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं.
गांव की स्थिति जानने के लिए एसडीएम ने दलितों से मिलने गए. जांच के दौरान केवल एक 60 साल का दलित बुजुर्ग रामजीलाल मिला. जो दहशत के चलते अपना मानसिक संतुलन खोया हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जांच के दौरान जब एसडीएम सुरेंद्र सह बुजुर्ग के पास गए तो बुजुर्ग ने सहमे हुए एसडीएम को सरपंच समझा और हाथ जोड़कर कहा सरपंच साहब मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा. काफी समझाने के बाद उन्हें पता चला कि यह सरपंच नहीं, फिरोजपुर झिरका के एसडीएम हैं और उन्हें बचाने के लिए आए हैं.
बुजुर्ग ने सिसकते हुए कहा साहब हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है. पूरा परिवार जातिवादी गुंडों के डर से गांव छोड़ चुका है. अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बचा लो और इंसाफ दो. एसडीएम ने दोनों तरफ से बयान व मौका मुआयना करने के बाद सहमे हुए बुजुर्ग के इलाज के लिए डाक्टरों की टीम को गांव में जाकर इलाज करने के आदेश दिए. लेकिन बुजुर्ग की हालात शाम को खराब होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा उसे रात साढ़े ग्यारह बजे इलाज के लिए फिरोजपुर झिरका लाया गया.
गौरतलब है गांव नीमखेड़ा में बीते माह दलित परिवार के ऊपर उस समय सरपंच गुट के लोगों ने हमला कर दिया जब दलित महिलाएं बोर पर पीने का पानी लेने के लिए गई थी. आरोप है सरपंच व उनके गुट के लोगों ने दलित परिवार को पानी न भरने दिया और गाली देकर भगा दिया. दलितों ने अपने साथ हुई इस घटना के बाद पुन्हाना थाने में शिकायत दी. लेकिन पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की. एसपी के हस्तक्षेप के बाद पुन्हाना पुलिस ने गांव के सरपंच साकिर सहित 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. दबंगों के लगातार दबाव से 20 सदस्यों का पीड़ित दलित परिवार गांव से पलायन कर गया. घर की रखवाली के लिए मात्र 60 वर्ष का एक बुजुर्ग यहां रह रहा है जो पूरी तरह से सहमा हुआ है. मामला एससी-एसटी आयोग तक पहुंचा तो प्रशासन हरकत में आया.
मेवात। मेवात के नीमखेड़ा गांव में जातिवादी गुंडे दलित परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं. परिवार पर जातिवादी गुंडे न केवल अत्याचार कर है बल्कि उन्हें गांव से पलायन करने पर भी मजबूर कर रहे हैं. जिसके चलते दलित परिवार ने गांव छोड़ दिया है. हालांकि जातिवादी गुंडे इस मामले को सियासी रंग देकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं.
गांव की स्थिति जानने के लिए एसडीएम ने दलितों से मिलने गए. जांच के दौरान केवल एक 60 साल का दलित बुजुर्ग रामजीलाल मिला. जो दहशत के चलते अपना मानसिक संतुलन खोया हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जांच के दौरान जब एसडीएम सुरेंद्र सह बुजुर्ग के पास गए तो बुजुर्ग ने सहमे हुए एसडीएम को सरपंच समझा और हाथ जोड़कर कहा सरपंच साहब मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा. काफी समझाने के बाद उन्हें पता चला कि यह सरपंच नहीं, फिरोजपुर झिरका के एसडीएम हैं और उन्हें बचाने के लिए आए हैं.
बुजुर्ग ने सिसकते हुए कहा साहब हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है. पूरा परिवार जातिवादी गुंडों के डर से गांव छोड़ चुका है. अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बचा लो और इंसाफ दो. एसडीएम ने दोनों तरफ से बयान व मौका मुआयना करने के बाद सहमे हुए बुजुर्ग के इलाज के लिए डाक्टरों की टीम को गांव में जाकर इलाज करने के आदेश दिए. लेकिन बुजुर्ग की हालात शाम को खराब होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा उसे रात साढ़े ग्यारह बजे इलाज के लिए फिरोजपुर झिरका लाया गया.
गौरतलब है गांव नीमखेड़ा में बीते माह दलित परिवार के ऊपर उस समय सरपंच गुट के लोगों ने हमला कर दिया जब दलित महिलाएं बोर पर पीने का पानी लेने के लिए गई थी. आरोप है सरपंच व उनके गुट के लोगों ने दलित परिवार को पानी न भरने दिया और गाली देकर भगा दिया. दलितों ने अपने साथ हुई इस घटना के बाद पुन्हाना थाने में शिकायत दी. लेकिन पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की. एसपी के हस्तक्षेप के बाद पुन्हाना पुलिस ने गांव के सरपंच साकिर सहित 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. दबंगों के लगातार दबाव से 20 सदस्यों का पीड़ित दलित परिवार गांव से पलायन कर गया. घर की रखवाली के लिए मात्र 60 वर्ष का एक बुजुर्ग यहां रह रहा है जो पूरी तरह से सहमा हुआ है. मामला एससी-एसटी आयोग तक पहुंचा तो प्रशासन हरकत में आया. दलितों का आक्रोश जायज है
 ग्यारह जुलाई, 2016 को एक वीडियो सामने आया, जिसने यह दर्शाया कि गुजरात के उना में कुछ लोगों ने एक मृत गाय का चमड़ा उतारने के आरोप में सात दलितों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की. इस घटना के विरोध में बहुत-से दलितों ने गाय के शव को हाथ लगाने से मना कर दिया है. ‘गऊ रक्षकों’ को इस पर खुश होना चाहिए, पर वे नाखुश हैं. ‘गऊ रक्षकों’ समेत कई गैर-दलितों ने, बदले में और भी हिंसा की है- इस बार गाय का शव न उठाने के कारण- सामतेर (16 अगस्त), भावरा (20 अगस्त) और राजकोट (24 अगस्त). ये सभी वाकये गुजरात के हैं. दलित के सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति है- वह काम करे तो भी मुसीबत, न करे तो भी. कहा जाता है कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को धर्मग्रथों ने पवित्र बताया है, पर यह हिंदू समाज का अभिशाप है. इस व्यवस्था ने अधिकांश हिंदू समाज को समाहित और वर्गीकृत किया, पर इसने एक बड़ी संख्या को बाहर रखा. बाहर रखे गए लोग जाति-बहिष्कृत या अछूत थे. जन्मना गैर-बराबरी इस व्यवस्था की बुनियाद थी. यह गैर-बराबरी आपके साथ जीवन भर बनी रहती थी. दलित के खिलाफ हिंसा, इस व्यवस्था के नियमों का पालन न करने की सजा है. रोहित वेमुला ने इसी को सार-रूप में कहा: ‘मेरा जन्म मेरे साथ घटी भयानक दुर्घटना है.’
दलित एकजुटता
दलित इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बस, अब बहुत हो चुका. उन्होंने एकजुट होने का फैसला किया है. दलितों की जैसी सामाजिक एकजुटता गुजरात और महाराष्ट्र में, और कुछ हद तक देश के अन्य हिस्सों में भी हुई है, वैसी हाल के वर्षों में पहले कभी नहीं दिखी थी. हालांकि अधिकांश मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा है, पर बड़ी-बड़ी रैलियां और जुलूस आयोजित हो रहे हैं. दलित समुदाय का आक्रोश प्रत्यक्ष है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में वे ऐसी हिंसा के शिकार हैं जिसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जा रहा है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुताबिक, वर्ष 2015 में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा गुजरात में रही, फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में।मौजूदा अति-राष्ट्रवाद के खोखलेपन को लेकर दलित गुस्से में हैं, जहां भारत से जुड़ी हर चीज महान बताई जाती है और हरेक आलोचना पर राष्ट्र-विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है. जिस तरह उना कांड और ऐसी अन्य घटनाओं को अलग-थलग घटना या षड्यंत्र कह कर झुठलाया जा रहा है उससे भी वे गुस्से में हैं. यह गौरतलब है कि गाय के शव का बहिष्कार, रैलियां और जुलूस राजनीति के स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता के तौर पर आयोजित किए गए.
लंबी चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री छह अगस्त को बोले. उन्होंने कहा, ‘मैं उन लोगों पर बहुत कुपित हूं जो गऊ रक्षा के धंधे में लगे हैं… मैंने देखा है कि कुछ लोग रात भर जुर्म में लगे रहते हैं और दिन में गऊ रक्षक का चोला धारण कर लेते हैं.’ इसके दूसरे रोज एक रैली में उन्होंने कहा, ‘दलितों को निशाना बनाने के बजाय आप मुझे गोली मार सकते हैं.’ एक प्रधानमंत्री का ऐसा कहना विचित्र है: उन्हें तमाम अधिकार हासिल हैं, हिंसा करने वालों को दंडित करने के लिए उन अधिकारों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए.
बदलाव की पीड़ादायी सुस्ती
बदलाव हो रहा है, पर इसकी गति पीड़ादायी होने की हद तक धीमी है. शहरी इलाकों में, जहां आर्थिक और पेशेवर पहचान को तवज्जो मिलती है, और देश के कुछ ऐसे हिस्सों में, जहां सामाजिक आंदोलनों की वजह से बदलाव आया, अधिकांश हिंदू जाति-व्यवस्था को लेकर उत्साही नहीं हैं. बहुतेरे हिंदू अब भी जाति के भीतर विवाह को वरीयता देते हैं, पर उनके दोस्त दलितों में भी हैं. कई लोग आरक्षण को लेकर नाराजगी जताते हैं, पर दलितों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जो एक सीमित तवज्जो मिली हुई है उससे डाह नहीं करते. अलबत्ता हिंदू समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो जाति के दबदबे के दिनों को बड़े मोह-भाव से याद करता है. उनमें से बहुतों को 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपने दिन फिरने के संकेत दिखे. गोरक्षा की ठेकेदारी सदियों के वचर्स्ववाद का नया इजहार है. गोवध और बीफ की खपत पर पाबंदी के सिलसिले और आक्रामक बहुसंख्यकवादी धारणाओं ने उनमें नया जोश पैदा किया है.
ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने जातिवादी एजेंडे को डॉ आंबेडकर और ‘पेरियार’ ईवी रामास्वामी से ज्यादा साफ ढंग से समझा होगा? दोनों हिंदू समाज के सुधार की बाबत निराश थे. आंबेडकर का खयाल था कि हिंदू धर्म के ढांचे में दलित गरिमापूर्ण ढंग से नहीं रह सकते, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए दलितों का आह्वान किया. पेरियार का रास्ता निरीश्वरवाद और बुद्धिवाद का था. तीसरा रास्ता हिंदू सामाजिक व्यवस्था के सुधार का तथा उन रुझानों को तेज करने का था जो एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाएं- शिक्षा, उद्योगीकरण, शहरीकरण, संचार और तकनीकी प्रगति.
संवैधानिक लक्ष्य
हिंदू अति-राष्ट्रवादियों के लिए, हिंदू राष्ट्र का विचार, संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य से अधिक वरेण्य है. वे जाति के दंश के इतिहास को दबा-छिपा देना चाहते हैं. वे सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र के विचार को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि इसके दोषों को नगण्य करके देखा जाए और करोड़ों दलितों तथा अल्पसंख्यकों ने जो कीमत चुकाई है उसे अनदेखा कर दिया जाए. दूसरी तरफ, संविधान निर्माताओं ने कभी इन समस्याओं के वजूद से इनकार नहीं किया: उन्होंने जातिगत विषमता और जातिगत भेदभाव की हकीकत को माना, और अपने हिसाब से बीच के समाधान तलाशे, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और अल्पसंख्यकों के अधिकार.
संविधान का असल फोकस हरेक भारतीय के लिए कुछ नैसर्गिक अधिकारों को सुनिश्चित करना और इन अधिकारों को ऐतिहासिक अन्यायों से अप्रभावित रखना है. संविधान की यह बुनियाद जाति, धर्म, लिंग को नागरिकता और नागरिक अधिकारों के आड़े नहीं आने देती. इस विशाल और जटिलता भरे देश में समान नागरिकता के बोध का विकास अब भी ठीक से नहीं हो पाया है. हिंदू अति-राष्ट्रवाद, जो प्रकारांतर से बहुसंख्यकवाद है, संवैधानिक संकल्पना से मेल नहीं खाता. हमारी आंखों के सामने यह टकराव जारी है, दिनोंदिन अधिक उग्र रूप में. लंबे टकराव के नतीजे हमारे देश तथा एक शांतिमय व खुशहाल राष्ट्र के लक्ष्य की दिशा में इसकी प्रगति के लिए भयावह साबित होंगे.
ग्यारह जुलाई, 2016 को एक वीडियो सामने आया, जिसने यह दर्शाया कि गुजरात के उना में कुछ लोगों ने एक मृत गाय का चमड़ा उतारने के आरोप में सात दलितों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की. इस घटना के विरोध में बहुत-से दलितों ने गाय के शव को हाथ लगाने से मना कर दिया है. ‘गऊ रक्षकों’ को इस पर खुश होना चाहिए, पर वे नाखुश हैं. ‘गऊ रक्षकों’ समेत कई गैर-दलितों ने, बदले में और भी हिंसा की है- इस बार गाय का शव न उठाने के कारण- सामतेर (16 अगस्त), भावरा (20 अगस्त) और राजकोट (24 अगस्त). ये सभी वाकये गुजरात के हैं. दलित के सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति है- वह काम करे तो भी मुसीबत, न करे तो भी. कहा जाता है कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को धर्मग्रथों ने पवित्र बताया है, पर यह हिंदू समाज का अभिशाप है. इस व्यवस्था ने अधिकांश हिंदू समाज को समाहित और वर्गीकृत किया, पर इसने एक बड़ी संख्या को बाहर रखा. बाहर रखे गए लोग जाति-बहिष्कृत या अछूत थे. जन्मना गैर-बराबरी इस व्यवस्था की बुनियाद थी. यह गैर-बराबरी आपके साथ जीवन भर बनी रहती थी. दलित के खिलाफ हिंसा, इस व्यवस्था के नियमों का पालन न करने की सजा है. रोहित वेमुला ने इसी को सार-रूप में कहा: ‘मेरा जन्म मेरे साथ घटी भयानक दुर्घटना है.’
दलित एकजुटता
दलित इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बस, अब बहुत हो चुका. उन्होंने एकजुट होने का फैसला किया है. दलितों की जैसी सामाजिक एकजुटता गुजरात और महाराष्ट्र में, और कुछ हद तक देश के अन्य हिस्सों में भी हुई है, वैसी हाल के वर्षों में पहले कभी नहीं दिखी थी. हालांकि अधिकांश मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा है, पर बड़ी-बड़ी रैलियां और जुलूस आयोजित हो रहे हैं. दलित समुदाय का आक्रोश प्रत्यक्ष है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में वे ऐसी हिंसा के शिकार हैं जिसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जा रहा है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुताबिक, वर्ष 2015 में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा गुजरात में रही, फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में।मौजूदा अति-राष्ट्रवाद के खोखलेपन को लेकर दलित गुस्से में हैं, जहां भारत से जुड़ी हर चीज महान बताई जाती है और हरेक आलोचना पर राष्ट्र-विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है. जिस तरह उना कांड और ऐसी अन्य घटनाओं को अलग-थलग घटना या षड्यंत्र कह कर झुठलाया जा रहा है उससे भी वे गुस्से में हैं. यह गौरतलब है कि गाय के शव का बहिष्कार, रैलियां और जुलूस राजनीति के स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता के तौर पर आयोजित किए गए.
लंबी चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री छह अगस्त को बोले. उन्होंने कहा, ‘मैं उन लोगों पर बहुत कुपित हूं जो गऊ रक्षा के धंधे में लगे हैं… मैंने देखा है कि कुछ लोग रात भर जुर्म में लगे रहते हैं और दिन में गऊ रक्षक का चोला धारण कर लेते हैं.’ इसके दूसरे रोज एक रैली में उन्होंने कहा, ‘दलितों को निशाना बनाने के बजाय आप मुझे गोली मार सकते हैं.’ एक प्रधानमंत्री का ऐसा कहना विचित्र है: उन्हें तमाम अधिकार हासिल हैं, हिंसा करने वालों को दंडित करने के लिए उन अधिकारों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए.
बदलाव की पीड़ादायी सुस्ती
बदलाव हो रहा है, पर इसकी गति पीड़ादायी होने की हद तक धीमी है. शहरी इलाकों में, जहां आर्थिक और पेशेवर पहचान को तवज्जो मिलती है, और देश के कुछ ऐसे हिस्सों में, जहां सामाजिक आंदोलनों की वजह से बदलाव आया, अधिकांश हिंदू जाति-व्यवस्था को लेकर उत्साही नहीं हैं. बहुतेरे हिंदू अब भी जाति के भीतर विवाह को वरीयता देते हैं, पर उनके दोस्त दलितों में भी हैं. कई लोग आरक्षण को लेकर नाराजगी जताते हैं, पर दलितों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जो एक सीमित तवज्जो मिली हुई है उससे डाह नहीं करते. अलबत्ता हिंदू समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो जाति के दबदबे के दिनों को बड़े मोह-भाव से याद करता है. उनमें से बहुतों को 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपने दिन फिरने के संकेत दिखे. गोरक्षा की ठेकेदारी सदियों के वचर्स्ववाद का नया इजहार है. गोवध और बीफ की खपत पर पाबंदी के सिलसिले और आक्रामक बहुसंख्यकवादी धारणाओं ने उनमें नया जोश पैदा किया है.
ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने जातिवादी एजेंडे को डॉ आंबेडकर और ‘पेरियार’ ईवी रामास्वामी से ज्यादा साफ ढंग से समझा होगा? दोनों हिंदू समाज के सुधार की बाबत निराश थे. आंबेडकर का खयाल था कि हिंदू धर्म के ढांचे में दलित गरिमापूर्ण ढंग से नहीं रह सकते, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए दलितों का आह्वान किया. पेरियार का रास्ता निरीश्वरवाद और बुद्धिवाद का था. तीसरा रास्ता हिंदू सामाजिक व्यवस्था के सुधार का तथा उन रुझानों को तेज करने का था जो एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाएं- शिक्षा, उद्योगीकरण, शहरीकरण, संचार और तकनीकी प्रगति.
संवैधानिक लक्ष्य
हिंदू अति-राष्ट्रवादियों के लिए, हिंदू राष्ट्र का विचार, संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य से अधिक वरेण्य है. वे जाति के दंश के इतिहास को दबा-छिपा देना चाहते हैं. वे सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र के विचार को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि इसके दोषों को नगण्य करके देखा जाए और करोड़ों दलितों तथा अल्पसंख्यकों ने जो कीमत चुकाई है उसे अनदेखा कर दिया जाए. दूसरी तरफ, संविधान निर्माताओं ने कभी इन समस्याओं के वजूद से इनकार नहीं किया: उन्होंने जातिगत विषमता और जातिगत भेदभाव की हकीकत को माना, और अपने हिसाब से बीच के समाधान तलाशे, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और अल्पसंख्यकों के अधिकार.
संविधान का असल फोकस हरेक भारतीय के लिए कुछ नैसर्गिक अधिकारों को सुनिश्चित करना और इन अधिकारों को ऐतिहासिक अन्यायों से अप्रभावित रखना है. संविधान की यह बुनियाद जाति, धर्म, लिंग को नागरिकता और नागरिक अधिकारों के आड़े नहीं आने देती. इस विशाल और जटिलता भरे देश में समान नागरिकता के बोध का विकास अब भी ठीक से नहीं हो पाया है. हिंदू अति-राष्ट्रवाद, जो प्रकारांतर से बहुसंख्यकवाद है, संवैधानिक संकल्पना से मेल नहीं खाता. हमारी आंखों के सामने यह टकराव जारी है, दिनोंदिन अधिक उग्र रूप में. लंबे टकराव के नतीजे हमारे देश तथा एक शांतिमय व खुशहाल राष्ट्र के लक्ष्य की दिशा में इसकी प्रगति के लिए भयावह साबित होंगे.
साभारः जनसत्ता. लेखक पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री हैं.
शिक्षा, ज्ञान एवं शक्ति के सन्दर्भ में डॉ. अंबेडकर
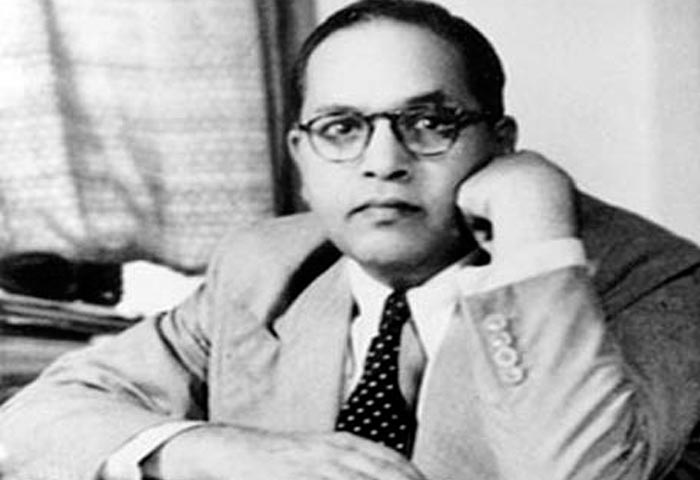 दलित एवं पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मूलभूत कारक है. यह उनके सामाजिक मुक्ति एवं आर्थिक विकास के लिये एक मात्र कारक है. दलित, जनजातीय एवं घुमंतू समुदायों में साक्षरता या आधुनिक शिक्षा जैसी व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है. जब हम शिक्षा के बारे में डा. अंबेडकर के विचारों एवं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके संर्घर्षों पर नजर डालते हैं तो हमारे मन में सहज ही उनके प्रति सम्मान का भाव जागता है. जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से के विचार को आगे बढ़ाते हुए फूको ने अपनी सभी कृतियों में ज्ञान, शक्ति एवं व्यक्ति के बीच स्थित त्रिकोणीय संबंधों का विश्लेषण किया है. इसी त्रिकोण के आधार डॉ. अंबेडकर के शिक्षा के लिये किए संघर्ष एवं ज्ञान प्रप्ति के उपरान्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व के माध्यम से भारतीय समाज में उनके द्वारा लाये गए परिवर्तनों का विश्लेषण करने पर इसकी महत्ता साफ दिखती है.
लगभग 100 वर्ष पूर्व 4 जून 1913 को डॉ. अंबेडकर और बड़ौदा नरेश के बीच के हुए करार के बाद उन्हें अमेरिका में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्ति मिली. यह एक ऐतिहासिक घटना थी. जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में वह न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिये पहुंचे. इस दौरान उन्हें पहली बार बराबरी का अनुभव हुआ. वह वहां के विद्यार्थियों के साथ बराबरी के साथ वार्तालाप करते, भोजन करते और घूमते थे. सभी जगह समता का वातावरण था. उस नये जगत ने उनके मन का क्षितिज विशाल किया. इसके बाद से डॉ. अंबेडकर ने गंभीरता पूर्वक सोचना शुरू किया कि पददलित समाज में शिक्षा के प्रसार से ही सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सकते हैं. डॉ. अंबेडकर ने प्राप्त अवसर का पूरा लाभ उठाया. विश्वविद्यालय में उपाधि हासिल करने के उद्देश्य के साथ ही अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास़्त्र और मानव शास्त्र अदि विषयों में प्रवीणता प्राप्त करने की उनकी प्रबल महात्वाकाक्षा थी, जिसे उन्होंने पूरा किया.
अपने गुरू सेंलिगमैन के निर्देशन में दो साल की कड़ी मेहनत से प्राचीन भारत में व्यापार (Ancient Indian Commerce) विषय पर प्रबंध (THESIS) लिखकर 1915 में एमए की उपाधि हासिल की. एक और प्रबंध भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवाराः एक ऐतिहासिक और विवेवचात्मक अध्ययन (National Dividend of India A History and Analytical Study) जून 1916 में पूरा किया. उनकी इस उपलब्धि पर उनके सहपाठियों ने पार्टी देकर उनका सम्मान किया. सन् 1924 में उनका यह प्रबंध पुस्तक के रूप में लंदन से (The Evolution of Provincial Finance in British India) के शीर्षक से प्रकाशित हुआ. तदुपरान्त कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें विधिवत रूप से पी.ए.चडी (डाक्टरेट) की उपाधि प्रदान की. आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉ. अंबेडकर की विशाल मूर्ति एवं अध्ययन पीठ स्थापित है और वहां उनके विचारों पर आधारित पाठयक्रम की शिक्षा दी जाती है एवं शोध किया जाता है. सन 2012 के ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर में जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग के प्रध्यापक एवं प्रसिद्व समाजशास्त्री डॉ. विवेक कुमार ने विजटिंग प्रोफेसर के रूप में कोलबिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था.
कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ-साथ डॉ. अंबेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी की परीक्षा 1921 में उतीर्ण की तथा (The Problem of Rupees) पर प्रबंध लिखकर लंदन विश्वविद्यालय डॉ. ऑफ सांइस की उपाधि प्राप्ति की. वहीं पर बैरिस्टरी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की. सर्वथा विपरीत परिस्थतियों में संघर्ष करते हुए चुनौतियों का अदम्य साहस से सामना करते हुए डा. अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक बुद्विमान एवं शक्तिशाली व्यक्ति बने और विषमता मूलक भारतीय समाज में दलितों-शोषितों के उत्थान के लिये प्रवृत्त हुए.
उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त डॉ. अंबेडकर ने स्वदेश लौटकर अर्जित ज्ञान का उपयोग असमानता पर आधारित भारतीय समाज एवं सदियों से शोषित, पीड़ित दलित समाज के उद्वार के प्रयासों में किया. इसके कारण उन्हें दलित चेतना के प्रतीक पुरूष के रूप में जाना जाता है. अपने गहन अध्ययन एवं प्रखर बुद्वि के बल पर उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किये. मसलन, उनका कहना था कि जब तक जाति के दानव से नहीं लड़ा जायेगा तब तक न इस देश में समाजवाद आयेगा और न ही लोकतन्त्र स्थपित होगा. अपनी पुस्तक (Annihilations of Caste) में डॉ. अंबेडकर ने जातियों की समाप्ति की बात कही है. उनका मत था कि जाति को समाप्त करने के लिए जाति से संबंधित धार्मिक धारणाओ को समाप्त करना होगा जो शास्त्रों में वर्णित है. उनका मानना था कि अन्तरजातिय विवाहों के द्वारा लोगों में मौलिक साझा एकता का विकास कर जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है. शान्तिपूर्ण साधनों से जब तक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सुधार संभव न हो तो कानूनों का निर्माण कर परिवर्तन लाया जा सकता है. यही वजह रही कि उन्होंने संसद एवं विधान मण्डलों, संविधान में पिछड़े दलित वर्गों की शिक्षा एवं नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के आवश्यक प्रावधान किये.
यह डॉ. अंबेडकर की विद्वता ही थी कि उन्होंने कम समय में विभिन्न विषयों पर ढेर सारा लेखन कार्य किया. आज उनकी कृतियों पर बहुत सारा साहित्य लिखा जा रहा है. उनकी कृतियां सामाजिक परिवर्तन का हथियार बन चुकी है. अत्यंत सशक्त भाषा में अपने स्पष्ट लेखन से डॉ. अंबेडकर ने प्रतिक्रिया वादी ताकतों पर करारा प्रहार किया है. उनकी कृतियां एवं विचार बहुजन समाज की अमूल्य धरोहर है. डॉ. अंबेडकर के योगदानो पर विस्तृत शोध करने वाली शोधकर्ता इलिनौर जिलेट ने लिखा है डॉ. अंबेडकर एक मात्र ऐसे भारतीय व्यक्तित्व हैं, जिनकी मृत्यु के बाद उनका महत्व और भी वढ़ता गया और उनकी स्वीकार्यता एवं अनुकरण करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है.
दलित एवं पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मूलभूत कारक है. यह उनके सामाजिक मुक्ति एवं आर्थिक विकास के लिये एक मात्र कारक है. दलित, जनजातीय एवं घुमंतू समुदायों में साक्षरता या आधुनिक शिक्षा जैसी व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है. जब हम शिक्षा के बारे में डा. अंबेडकर के विचारों एवं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके संर्घर्षों पर नजर डालते हैं तो हमारे मन में सहज ही उनके प्रति सम्मान का भाव जागता है. जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से के विचार को आगे बढ़ाते हुए फूको ने अपनी सभी कृतियों में ज्ञान, शक्ति एवं व्यक्ति के बीच स्थित त्रिकोणीय संबंधों का विश्लेषण किया है. इसी त्रिकोण के आधार डॉ. अंबेडकर के शिक्षा के लिये किए संघर्ष एवं ज्ञान प्रप्ति के उपरान्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व के माध्यम से भारतीय समाज में उनके द्वारा लाये गए परिवर्तनों का विश्लेषण करने पर इसकी महत्ता साफ दिखती है.
लगभग 100 वर्ष पूर्व 4 जून 1913 को डॉ. अंबेडकर और बड़ौदा नरेश के बीच के हुए करार के बाद उन्हें अमेरिका में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्ति मिली. यह एक ऐतिहासिक घटना थी. जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में वह न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिये पहुंचे. इस दौरान उन्हें पहली बार बराबरी का अनुभव हुआ. वह वहां के विद्यार्थियों के साथ बराबरी के साथ वार्तालाप करते, भोजन करते और घूमते थे. सभी जगह समता का वातावरण था. उस नये जगत ने उनके मन का क्षितिज विशाल किया. इसके बाद से डॉ. अंबेडकर ने गंभीरता पूर्वक सोचना शुरू किया कि पददलित समाज में शिक्षा के प्रसार से ही सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सकते हैं. डॉ. अंबेडकर ने प्राप्त अवसर का पूरा लाभ उठाया. विश्वविद्यालय में उपाधि हासिल करने के उद्देश्य के साथ ही अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास़्त्र और मानव शास्त्र अदि विषयों में प्रवीणता प्राप्त करने की उनकी प्रबल महात्वाकाक्षा थी, जिसे उन्होंने पूरा किया.
अपने गुरू सेंलिगमैन के निर्देशन में दो साल की कड़ी मेहनत से प्राचीन भारत में व्यापार (Ancient Indian Commerce) विषय पर प्रबंध (THESIS) लिखकर 1915 में एमए की उपाधि हासिल की. एक और प्रबंध भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवाराः एक ऐतिहासिक और विवेवचात्मक अध्ययन (National Dividend of India A History and Analytical Study) जून 1916 में पूरा किया. उनकी इस उपलब्धि पर उनके सहपाठियों ने पार्टी देकर उनका सम्मान किया. सन् 1924 में उनका यह प्रबंध पुस्तक के रूप में लंदन से (The Evolution of Provincial Finance in British India) के शीर्षक से प्रकाशित हुआ. तदुपरान्त कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें विधिवत रूप से पी.ए.चडी (डाक्टरेट) की उपाधि प्रदान की. आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉ. अंबेडकर की विशाल मूर्ति एवं अध्ययन पीठ स्थापित है और वहां उनके विचारों पर आधारित पाठयक्रम की शिक्षा दी जाती है एवं शोध किया जाता है. सन 2012 के ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर में जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग के प्रध्यापक एवं प्रसिद्व समाजशास्त्री डॉ. विवेक कुमार ने विजटिंग प्रोफेसर के रूप में कोलबिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था.
कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ-साथ डॉ. अंबेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी की परीक्षा 1921 में उतीर्ण की तथा (The Problem of Rupees) पर प्रबंध लिखकर लंदन विश्वविद्यालय डॉ. ऑफ सांइस की उपाधि प्राप्ति की. वहीं पर बैरिस्टरी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की. सर्वथा विपरीत परिस्थतियों में संघर्ष करते हुए चुनौतियों का अदम्य साहस से सामना करते हुए डा. अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक बुद्विमान एवं शक्तिशाली व्यक्ति बने और विषमता मूलक भारतीय समाज में दलितों-शोषितों के उत्थान के लिये प्रवृत्त हुए.
उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त डॉ. अंबेडकर ने स्वदेश लौटकर अर्जित ज्ञान का उपयोग असमानता पर आधारित भारतीय समाज एवं सदियों से शोषित, पीड़ित दलित समाज के उद्वार के प्रयासों में किया. इसके कारण उन्हें दलित चेतना के प्रतीक पुरूष के रूप में जाना जाता है. अपने गहन अध्ययन एवं प्रखर बुद्वि के बल पर उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किये. मसलन, उनका कहना था कि जब तक जाति के दानव से नहीं लड़ा जायेगा तब तक न इस देश में समाजवाद आयेगा और न ही लोकतन्त्र स्थपित होगा. अपनी पुस्तक (Annihilations of Caste) में डॉ. अंबेडकर ने जातियों की समाप्ति की बात कही है. उनका मत था कि जाति को समाप्त करने के लिए जाति से संबंधित धार्मिक धारणाओ को समाप्त करना होगा जो शास्त्रों में वर्णित है. उनका मानना था कि अन्तरजातिय विवाहों के द्वारा लोगों में मौलिक साझा एकता का विकास कर जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है. शान्तिपूर्ण साधनों से जब तक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सुधार संभव न हो तो कानूनों का निर्माण कर परिवर्तन लाया जा सकता है. यही वजह रही कि उन्होंने संसद एवं विधान मण्डलों, संविधान में पिछड़े दलित वर्गों की शिक्षा एवं नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के आवश्यक प्रावधान किये.
यह डॉ. अंबेडकर की विद्वता ही थी कि उन्होंने कम समय में विभिन्न विषयों पर ढेर सारा लेखन कार्य किया. आज उनकी कृतियों पर बहुत सारा साहित्य लिखा जा रहा है. उनकी कृतियां सामाजिक परिवर्तन का हथियार बन चुकी है. अत्यंत सशक्त भाषा में अपने स्पष्ट लेखन से डॉ. अंबेडकर ने प्रतिक्रिया वादी ताकतों पर करारा प्रहार किया है. उनकी कृतियां एवं विचार बहुजन समाज की अमूल्य धरोहर है. डॉ. अंबेडकर के योगदानो पर विस्तृत शोध करने वाली शोधकर्ता इलिनौर जिलेट ने लिखा है डॉ. अंबेडकर एक मात्र ऐसे भारतीय व्यक्तित्व हैं, जिनकी मृत्यु के बाद उनका महत्व और भी वढ़ता गया और उनकी स्वीकार्यता एवं अनुकरण करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. 6 दिसंबर को जयपुर हाईकोर्ट में मनुस्मृति फूंकने की तैयारी
 गुजरात में उना आंदोलन की कमान संभालने वाले जिग्नेश मेवाणी अब मनुस्मृति फूंकने की तैयारी में है. मेवाणी ने घोषणा की है कि 6 दिसंबर को जयपुर हाईकोर्ट में मनुस्मृति जलाया जाएगा. बताते चलें कि जयपुर हाई कोर्ट के परिसर में मनु की मूर्ति लगी हुई है. जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि दलित आदोलन का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए बाबासाहेब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को देश भर के दलित राजस्थान में एकत्र होकर जयपुर हाईकोर्ट तक मार्च करेंगे.
इस दौरान दलित समाज के लोग कोर्ट परिसर में स्थापित मनु की मूर्ति के सामने मनु स्मृति जलाएंगे. मेवाणी ने यह बात शनिवार को लखनऊ में आयोजित अम्बेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में कही. गौरतलब है कि दलित संगठन काफी पहले से जयपुर हाईकोर्ट में मौजूद मनु की मूर्ति को वहां से हटाने की मांग करते रहे हैं. दलित संगठनों का तर्क रहता है कि जब देश संविधान से चलता है तो एक राज्य के उच्च न्यायालय में मनु की मूर्ति स्थापित होना कितना जायज है?
गुजरात में उना आंदोलन की कमान संभालने वाले जिग्नेश मेवाणी अब मनुस्मृति फूंकने की तैयारी में है. मेवाणी ने घोषणा की है कि 6 दिसंबर को जयपुर हाईकोर्ट में मनुस्मृति जलाया जाएगा. बताते चलें कि जयपुर हाई कोर्ट के परिसर में मनु की मूर्ति लगी हुई है. जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि दलित आदोलन का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए बाबासाहेब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को देश भर के दलित राजस्थान में एकत्र होकर जयपुर हाईकोर्ट तक मार्च करेंगे.
इस दौरान दलित समाज के लोग कोर्ट परिसर में स्थापित मनु की मूर्ति के सामने मनु स्मृति जलाएंगे. मेवाणी ने यह बात शनिवार को लखनऊ में आयोजित अम्बेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में कही. गौरतलब है कि दलित संगठन काफी पहले से जयपुर हाईकोर्ट में मौजूद मनु की मूर्ति को वहां से हटाने की मांग करते रहे हैं. दलित संगठनों का तर्क रहता है कि जब देश संविधान से चलता है तो एक राज्य के उच्च न्यायालय में मनु की मूर्ति स्थापित होना कितना जायज है? सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय बसपा का नारा नहीं, नीति है- आजमगढ़ में मायावती
 पूर्वांचल के प्रमुख हिस्सों को ध्यान में रखकर आजमगढ़ में आयोजित की गई बसपा की महारैली में पार्टी अध्यक्ष मायावती आगरा से बदले अंदाज में दिखीं. अपने भाषण के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा तो यह भी साफ कर दिया कि अगर बसपा सरकार में नहीं आई तो उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश ही बना रहेगा. अपने भाषण में बसपा मुखिया ने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में बसपा की सरकार आने पर पूर्वांचल के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. सपा मुखिया मुलायम सिंह के क्षेत्र में उन्हें ललकारते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने सपा मुखिया को इसलिए यहां से जीताया था क्योंकि उनको भरोसा था कि आजमगढ़ भी सैफई और इटावा की तरह चमकने लगेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने आजमगढ़ के लोगों का आवाहन करते हुए कहा कि इसका बदला आजमगढ़ और पूर्वांचल के सभी विधानसभा सीटों पर यूपी चुनाव में हरा कर लेना है. रविवार 28 अगस्त की यह रैली आजमगढ़, बलिया, और अम्बेडकर नगर क्षेत्रों की संयुक्त रैली थी.
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा नहीं, बसपा का सिद्धांत
आजमगढ़ की रैली में बसपा प्रमुख ने साफ किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बसपा का सिर्फ नारा नहीं है बल्कि हमारी पार्टी इसी सिद्धांत पर चलती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बसपा में सिर्फ बहुजन नहीं बल्कि सर्व समाज का हित सुरक्षित है. सवर्ण वोटरों को भड़काने के लिए विपक्ष द्वारा तिलक-तराजू … वाले नारे का प्रचार किए जाने पर मायावती ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ऊंची जाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखते. उन्हें एमएलसी और अन्य पदों पर नहीं बिठाते.
अच्छे दिन लाने के वायदे बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं
केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के अच्छे दिन के नारे अब बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं. देश का अल्पसंख्यक और दलित खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से दिल्ली की कानून व्यवस्था तो संभल नहीं रही है, यूपी की क्या संभालेगी.
कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा कर ले यूपी में सरकार नहीं बना सकती
पूर्वांचल के लोगों को कांग्रेस की असलियत बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान मैं पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा देना चाहती थी लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को दबा दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, वह दिल्ली को गंदा होने के लिए पूर्वांचल के लोगों को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं. पहले सोनिया गांधी के रोड शो और अब राहुल गांधी का रोड शो और पदयात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी भी पदयात्रा कर ले, यूपी में सरकार नहीं बना सकती.
यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं
रैली में महिलाओं की उपस्थिति भी अच्छी खासी थी. उन्हें भावनात्मक सहारा देते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. हर दिन आबरु लूट रही है. प्रदेश में 75 जिलों हैं, हर दिन किसी न किसी जिले में बहनों-बेटियों की आबरु लूट रही है.
भाजपा की हालत खऱाब, कैंडिडेंट नहीं मिल रहे
बसपा द्वारा निकाले गए नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की हालत खराब है. भाजपा को यूपी में कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं. यही वजह है कि वह दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर और बसपा द्वारा निकाले गए नेताओं को टिकट दे रही है और उन्हें साथ लेकर घूम रही है.
स्वार्थी बागी नेताओं पर निशाना
बसपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए स्वार्थी नेताओं पर वार करते हुए बसपा प्रमुख ने उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी से अलग होने के लिए मैं उनका आभार जताती हूं. यह हमारे पार्टी और आंदोलन के हित में अच्छा हुआ. उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि यह गंदगी बीजेपी में चली गई है.
विपक्षियों की साजिश से रहें सावधान
कुछ महीने पहले सर्वे में बसपा को नंबर वन बताए जाने और फिर हाल ही में उसे नीचे दिखाए जाने को साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा को समर्थन देने वाले मीडिया वालों की साजिश है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बसपा के समर्थक ढीले पर जाए और भाजपा को इसका फायदा मिले.
दलितों को जमीन के पट्टे दिलाए जाएंगे, दोषियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
सपा सरकार में जिन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बसपा सरकार आने पर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा. जिन पीड़ित लोगों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. दलितों को जमीन के पट्टे दिलवाए जाएंगे. जिन जिलों और पार्कों आदि के जो नाम बदले गए हैं, उनको फिर बहाल कराया जाएगा.
पूर्वांचल के प्रमुख हिस्सों को ध्यान में रखकर आजमगढ़ में आयोजित की गई बसपा की महारैली में पार्टी अध्यक्ष मायावती आगरा से बदले अंदाज में दिखीं. अपने भाषण के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा तो यह भी साफ कर दिया कि अगर बसपा सरकार में नहीं आई तो उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश ही बना रहेगा. अपने भाषण में बसपा मुखिया ने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में बसपा की सरकार आने पर पूर्वांचल के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. सपा मुखिया मुलायम सिंह के क्षेत्र में उन्हें ललकारते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने सपा मुखिया को इसलिए यहां से जीताया था क्योंकि उनको भरोसा था कि आजमगढ़ भी सैफई और इटावा की तरह चमकने लगेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने आजमगढ़ के लोगों का आवाहन करते हुए कहा कि इसका बदला आजमगढ़ और पूर्वांचल के सभी विधानसभा सीटों पर यूपी चुनाव में हरा कर लेना है. रविवार 28 अगस्त की यह रैली आजमगढ़, बलिया, और अम्बेडकर नगर क्षेत्रों की संयुक्त रैली थी.
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा नहीं, बसपा का सिद्धांत
आजमगढ़ की रैली में बसपा प्रमुख ने साफ किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बसपा का सिर्फ नारा नहीं है बल्कि हमारी पार्टी इसी सिद्धांत पर चलती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बसपा में सिर्फ बहुजन नहीं बल्कि सर्व समाज का हित सुरक्षित है. सवर्ण वोटरों को भड़काने के लिए विपक्ष द्वारा तिलक-तराजू … वाले नारे का प्रचार किए जाने पर मायावती ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ऊंची जाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखते. उन्हें एमएलसी और अन्य पदों पर नहीं बिठाते.
अच्छे दिन लाने के वायदे बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं
केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के अच्छे दिन के नारे अब बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं. देश का अल्पसंख्यक और दलित खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से दिल्ली की कानून व्यवस्था तो संभल नहीं रही है, यूपी की क्या संभालेगी.
कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा कर ले यूपी में सरकार नहीं बना सकती
पूर्वांचल के लोगों को कांग्रेस की असलियत बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान मैं पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा देना चाहती थी लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को दबा दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, वह दिल्ली को गंदा होने के लिए पूर्वांचल के लोगों को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं. पहले सोनिया गांधी के रोड शो और अब राहुल गांधी का रोड शो और पदयात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी भी पदयात्रा कर ले, यूपी में सरकार नहीं बना सकती.
यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं
रैली में महिलाओं की उपस्थिति भी अच्छी खासी थी. उन्हें भावनात्मक सहारा देते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. हर दिन आबरु लूट रही है. प्रदेश में 75 जिलों हैं, हर दिन किसी न किसी जिले में बहनों-बेटियों की आबरु लूट रही है.
भाजपा की हालत खऱाब, कैंडिडेंट नहीं मिल रहे
बसपा द्वारा निकाले गए नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की हालत खराब है. भाजपा को यूपी में कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं. यही वजह है कि वह दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर और बसपा द्वारा निकाले गए नेताओं को टिकट दे रही है और उन्हें साथ लेकर घूम रही है.
स्वार्थी बागी नेताओं पर निशाना
बसपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए स्वार्थी नेताओं पर वार करते हुए बसपा प्रमुख ने उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी से अलग होने के लिए मैं उनका आभार जताती हूं. यह हमारे पार्टी और आंदोलन के हित में अच्छा हुआ. उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि यह गंदगी बीजेपी में चली गई है.
विपक्षियों की साजिश से रहें सावधान
कुछ महीने पहले सर्वे में बसपा को नंबर वन बताए जाने और फिर हाल ही में उसे नीचे दिखाए जाने को साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा को समर्थन देने वाले मीडिया वालों की साजिश है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बसपा के समर्थक ढीले पर जाए और भाजपा को इसका फायदा मिले.
दलितों को जमीन के पट्टे दिलाए जाएंगे, दोषियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
सपा सरकार में जिन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बसपा सरकार आने पर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा. जिन पीड़ित लोगों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. दलितों को जमीन के पट्टे दिलवाए जाएंगे. जिन जिलों और पार्कों आदि के जो नाम बदले गए हैं, उनको फिर बहाल कराया जाएगा. रमणिका गुप्ता और अंतरंगता का उत्सव
 मैं रमणिका गुप्ता (जी) को नहीं जानता. मतलब बहुत अच्छे से नहीं जानता. उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उनके बारे में जानता हूं. उनकी मैग्जीन, उनके प्रकाशन और आदिवासियों के लिए किए गए उनके काम के बारे में जानता हूं. उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानने का कारण यह भी हो सकता है कि उनके और मेरे उम्र का अंतर काफी ज्यादा है. 2016 के विश्व पुस्तक मेले में पहली बार उनको देखा था. बमुश्किल एक 18-19 साल के नवयुवा का सहारा लिए वह पुस्तक मेले में घूम रही थीं. पीछे कुछ और लोग भी थे. सोशल मीडिया और कुछ किताबों में उनकी तस्वीर देखी थी सो उन्हें पहचान गया. हां, बात और मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी से भी एकदम से जाकर मिल लेने में मैं हमेशा से सकुचाता रहा हूं.
31 अगस्त वाले इंडिया टुडे के अंक में उनकी एक किताब की चर्चा ने इतने दिनों बाद मुझे उनका जिक्र करने पर मजबूर किया है. उनकी आत्मकथा आई है, ‘आपहुदरी… एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा’ के नाम से. इससे पहले उनकी आत्मकथा का पहला खंड ‘हादसे’ के नाम से आ चुका है. फिलहाल चर्चा दूसरे खंड आपहुदरी की. इंडिया टुडे में इसी का जिक्र है. पत्रिका ने इसे अपना एक शीर्षक दिया है, ‘अंतरंगता का उत्सव.’ और इसी ‘उत्सव’ की झांकी ने मुझे यह लेख लिखने पर मजबूर कर दिया. क्योंकि बहुत संक्षिप्त में दिए गए पुस्तक के कुछ अंश मेरे मन में सवाल छोड़ गए. यहां गुप्ता जी के आत्मकथा के अंश का जिक्र करते हुए लिखा है, “मैं अब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी. सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है, सीमा तोड़ने का आभाष ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है. मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूं… अपनी देह की मैं खुद मालिक हूं. मैं संचालक हूं. संचालित नहीं.”
उनकी आत्मकथा के एक अन्य अंश को भी देखिए, “यौन के बारे में भक्ष्य-अभक्ष्य क्या है, समाज इसका फैसला तो करता रहा है, पर उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले… व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएं, सुख की व्याख्या, यौन का दायरा सब तो देशकाल के अनुरूप बदलता है. रिश्ते भी सापेक्ष होते हैं. दुर्भाग्यवश समाज ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला खासकर भारतीय समाज ने.” कुछ लाइनें इस किताब को पढ़ने (शायद) के बाद समीक्षक मनोज मोहन ने लिखी है. मनोज लिखते हैं, “इस भारतीय समाज के जिन पुरुषों से रमणिका गुप्ता का साबका पड़ता है उनमें उनका पति, पति के दोस्त, नेता, नेता के साथ चलने वाले छुटभैये, ओहदेदार पुरुषों की भी लंबी फेहरिस्त है.”
इतनी लंबी फेहरिस्त को लांघने के बाद इस शिखर पर पहुंची रमणिका गुप्ता अपनी उम्र के 86वें वर्ष में हैं. मुझे नहीं पता कि आज वो अपने जीवन के तीसरे और चौथे दशक को किस तरह देखती हैं. मेरे मन में बस इतना सा सवाल भर है कि जिन परिस्थितियों को लांघ कर वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और उन्होंने जो सफलता अर्जित की है, वह सफलता उनकी अपनी कितनी है? अपनी आगे बढ़ने की अकांक्षाओं और सीमाओं को तोड़ने को तैयार एक मनुष्य के लिए क्या सफलता आसान नहीं हो जाती है? जब वो औरत हो तो तब तो कई मामलों में सफलता चल कर आती है. ऐसे में क्या उसकी सफलता में उन लोगों का भी हिस्सा नहीं हो जाता जिनको लांघ कर उसने वह सफलता पाई होती है.
मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई स्त्री विमर्श नहीं कर रहा हूं, और न ही स्त्री के देह और वर्जनाओं पर सवाल उठा रहा हूं. मैं रमणिका गुप्ता जी की इन लाइनों का विरोध नहीं करता कि स्त्री अपनी देह की मालिक खुद है. निस्संदेह यह उसकी अपनी ‘स्वतंत्रता’ हो सकती है. मैं तो बस उस सफलता की बात कर रहा हूं जो उसे तमाम रास्तों से गुजरने के बाद मिलती है, क्योंकि जब कोई सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर पहुंचने में सीढ़ियों का भी योगदान होता है. मेरी समझ से ऐसी सफलता अकेले की सफलता नहीं है. और जहां तक व्यक्तिगत जीवन और देह की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने की बात है तो आत्मकथा के बहाने जीवन के निजी पलों और संबंधों को बेचना कुछ साहित्यकारों का शगल बनता जा रहा है.
मैं रमणिका गुप्ता (जी) को नहीं जानता. मतलब बहुत अच्छे से नहीं जानता. उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उनके बारे में जानता हूं. उनकी मैग्जीन, उनके प्रकाशन और आदिवासियों के लिए किए गए उनके काम के बारे में जानता हूं. उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानने का कारण यह भी हो सकता है कि उनके और मेरे उम्र का अंतर काफी ज्यादा है. 2016 के विश्व पुस्तक मेले में पहली बार उनको देखा था. बमुश्किल एक 18-19 साल के नवयुवा का सहारा लिए वह पुस्तक मेले में घूम रही थीं. पीछे कुछ और लोग भी थे. सोशल मीडिया और कुछ किताबों में उनकी तस्वीर देखी थी सो उन्हें पहचान गया. हां, बात और मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी से भी एकदम से जाकर मिल लेने में मैं हमेशा से सकुचाता रहा हूं.
31 अगस्त वाले इंडिया टुडे के अंक में उनकी एक किताब की चर्चा ने इतने दिनों बाद मुझे उनका जिक्र करने पर मजबूर किया है. उनकी आत्मकथा आई है, ‘आपहुदरी… एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा’ के नाम से. इससे पहले उनकी आत्मकथा का पहला खंड ‘हादसे’ के नाम से आ चुका है. फिलहाल चर्चा दूसरे खंड आपहुदरी की. इंडिया टुडे में इसी का जिक्र है. पत्रिका ने इसे अपना एक शीर्षक दिया है, ‘अंतरंगता का उत्सव.’ और इसी ‘उत्सव’ की झांकी ने मुझे यह लेख लिखने पर मजबूर कर दिया. क्योंकि बहुत संक्षिप्त में दिए गए पुस्तक के कुछ अंश मेरे मन में सवाल छोड़ गए. यहां गुप्ता जी के आत्मकथा के अंश का जिक्र करते हुए लिखा है, “मैं अब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी. सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है, सीमा तोड़ने का आभाष ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है. मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूं… अपनी देह की मैं खुद मालिक हूं. मैं संचालक हूं. संचालित नहीं.”
उनकी आत्मकथा के एक अन्य अंश को भी देखिए, “यौन के बारे में भक्ष्य-अभक्ष्य क्या है, समाज इसका फैसला तो करता रहा है, पर उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले… व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएं, सुख की व्याख्या, यौन का दायरा सब तो देशकाल के अनुरूप बदलता है. रिश्ते भी सापेक्ष होते हैं. दुर्भाग्यवश समाज ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला खासकर भारतीय समाज ने.” कुछ लाइनें इस किताब को पढ़ने (शायद) के बाद समीक्षक मनोज मोहन ने लिखी है. मनोज लिखते हैं, “इस भारतीय समाज के जिन पुरुषों से रमणिका गुप्ता का साबका पड़ता है उनमें उनका पति, पति के दोस्त, नेता, नेता के साथ चलने वाले छुटभैये, ओहदेदार पुरुषों की भी लंबी फेहरिस्त है.”
इतनी लंबी फेहरिस्त को लांघने के बाद इस शिखर पर पहुंची रमणिका गुप्ता अपनी उम्र के 86वें वर्ष में हैं. मुझे नहीं पता कि आज वो अपने जीवन के तीसरे और चौथे दशक को किस तरह देखती हैं. मेरे मन में बस इतना सा सवाल भर है कि जिन परिस्थितियों को लांघ कर वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और उन्होंने जो सफलता अर्जित की है, वह सफलता उनकी अपनी कितनी है? अपनी आगे बढ़ने की अकांक्षाओं और सीमाओं को तोड़ने को तैयार एक मनुष्य के लिए क्या सफलता आसान नहीं हो जाती है? जब वो औरत हो तो तब तो कई मामलों में सफलता चल कर आती है. ऐसे में क्या उसकी सफलता में उन लोगों का भी हिस्सा नहीं हो जाता जिनको लांघ कर उसने वह सफलता पाई होती है.
मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई स्त्री विमर्श नहीं कर रहा हूं, और न ही स्त्री के देह और वर्जनाओं पर सवाल उठा रहा हूं. मैं रमणिका गुप्ता जी की इन लाइनों का विरोध नहीं करता कि स्त्री अपनी देह की मालिक खुद है. निस्संदेह यह उसकी अपनी ‘स्वतंत्रता’ हो सकती है. मैं तो बस उस सफलता की बात कर रहा हूं जो उसे तमाम रास्तों से गुजरने के बाद मिलती है, क्योंकि जब कोई सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर पहुंचने में सीढ़ियों का भी योगदान होता है. मेरी समझ से ऐसी सफलता अकेले की सफलता नहीं है. और जहां तक व्यक्तिगत जीवन और देह की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने की बात है तो आत्मकथा के बहाने जीवन के निजी पलों और संबंधों को बेचना कुछ साहित्यकारों का शगल बनता जा रहा है. जाति का एशियाई संदर्भ
 एक पत्रिका के लेख में प्रसिद्ध उद्योगपति वॉरेन बफेट ने एक सवाल उठाया था कि “एक ही मां के गर्भ से जन्में जुड़वों का समान रुप से चुस्ती, शक्ति-सामर्थ्य है. उनमें से एक का जन्म बांग्लादेश में और दूसरे का अमेरिका में होगा तो क्या होगा? उनका नसीब कैसा रहेगा? व्यक्तियों के सामाजिक स्तर के अनुसार उसके भविष्य का निर्माण कैसा होगा?” उन्होंने विनम्रता के साथ गहरे और गंभीर विषय को सामने रखते हुए कहा है कि अमेरिका में जन्म के स्तर पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं मेरा जीवन है. मुझे किसी भी व्यवसाय को चुनने की आजादी इस धरती और देश ने प्रदान की है. अगर मैं कहीं दूसरी जगह जन्म लेता तो कभी भी इस स्थान तक नहीं पहुंच सकता था. लेकिन एक बात तो विचारणीय है कि अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देश में भी नस्लगत भेद-भाव उस देश की छवि को धूल-धूसरित करता है.
कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि व्यक्तियों के भविष्य निर्माण में देशगत, प्रांतीय, धार्मिक और जातीय आधारों की विशिष्ट भूमिका रहती है. भारतीय समाज व्यवस्था की स्थिति बहुस्तरीय है. भारतीय समाज व्यवस्था के ऊपरी पायदान पर ‘सवर्ण’ केंद्रित है तो दूसरी और निचले पायदान पर ‘अंत्यज’ या ‘दलित’. क्या दलितों को इस समाज-व्यवस्था ने मानवीय दर्जा दिया है? भारत जैसे देश की संस्कृति की गाथा हजारों वर्षों से गायी जा रही है. जबकि इस देश की समाज-व्यवस्था ने क्रूरता, बर्बरता एवं अमानवीयता का परिचय कर्म और व्यवहार के स्तर पर दलितों के संदर्भ में दिया है. श्रमशील तबकों को हाशिये पर रखा गया है. मेहनतकश लोगों के श्रम की बुनियाद पर ही यह समाज-व्यवस्था टिकी हुई है. जबकि जातीय अहंकार और दंभ के कारण निर्दोष भारतीय नागरिक समुदाय का एक हिस्सा निरंतर उपेक्षा, अपमान और नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. क्या सभ्य संस्कृति का यह अर्थ लगाया जाए कि मनुष्य का मनुष्य पर अत्याचार एक श्रेष्ठ सभ्यता का विशेष गुण है?
भारत सरकार के एक अध्ययन के अनुसार भारत में दलित तबकों के बच्चे जीवन की आधारभूत सुविधाओं विशेषकर पोषण की कमी की वजह से जन्म लेने के बावजूद भी अन्य तबकों के बच्चों की तुलना में औसत आयु के स्तर पर चार साल कम जीवित रह पाते हैं. जन्म लेने वालों में से आधे से ज्यादा बच्चे पौष्टिक आहार की कमी से जूझ रहे हैं. भारत की औसत बाल जन्म दर में हर सौ बच्चों के आंकड़े को देखा जाय तो उनमें से 12 बच्चे पांच वर्ष की अवस्था से पूर्व ही अकाल काल के ग्रास बन रहे हैं. दलित तबकों के हर पांच बच्चों में से एक ही ठीक से स्कूल जा पाता है. हर 3 बच्चों में से एक बर्बर गरीबी का शिकार हो रहा है. दलित तबकों की 31% महिलाएं रक्त की कमी से परेशान हैं. भारत देश में छः हजार जातियां हैं. उसमें भी अस्सी फीसदी से अधिक दबी-कुचली जा रही जातियां हैं. हजारों वर्षों से तड़पते हुए वर्ण-व्यवस्था के लोहे के शिकंजे के पिंजरे में फंसकर, अवसरों से वंचित होकर निचले पायदान पर ही जीते जा रहे जन-समुदायों की स्थिति कैसी होगी? भारत के संविधान निर्माताओं ने जो स्वप्न देखने की आकांक्षा चाही थी उसे जाति-प्रथा से युक्त समाज-व्यवस्था ने साकार नहीं होने दिया. जाति-प्रथा से पीड़ित तबकों के सुधार में असफलताओं की गणना संभव ही नहीं है. आज भी सरकारी, गैर-सरकारी शौचालयों में अमानुषिक कृत्य करने वाले ‘मेहतर’ (भंगी) या ‘सफाईकर्मियों’ की संख्या दस लाख से अधिक होने की संभावना की सूचना सरकारी गणना के स्तर पर सामने आयी है. आंध्रप्रदेश के साथ-साथ देश के अनेक राज्यों में आज भी भेद-भाव पूर्ण ‘दो गिलास’ की पद्धति व्यवहार में है. दलितों का मंदिरों में प्रवेश न होने देना और सवर्णों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे कुंओं से पानी पीने की सुविधा नहीं देना जैसे अमानवीय कार्य केवल जन्मगत आधार पर ही तो हो रहे हैं. जाति-व्यवस्था के कारण ही वैश्विक स्तर पर 26 करोड़ आबादी कष्ट सह रही है. दृढ़ कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी वे सामाजिक न्याय से मोहताज हैं. विशेष रुप से दक्षिण एशिया के देशों में यह प्रथा व्यवस्थीकृत होकर जड़ें जमा चुकी हैं.
संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति की स्वतंत्र समिति ने चिंता व्यक्त की है कि आज भी दक्षिण एशिया के देशों में दलितों के साथ अछूत व्यवहार किया जा रहा है. यह विचारणीय और सोचनीय बिंदु है कि कैसे भारत विश्व की चौथी अर्थ-व्यवस्था होने पर गुमान कर रहा है और उसी के देश में मानव समुदायों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है.
पाकिस्तान जैसे देश में भी जाति-व्यवस्था का एक रुप दिखाई दिया है. पाकिस्तान में कानूनन शेड्यूल्ड कॉस्ट के नाम से घोषित किये गये हिंदुओं में निम्न जातियों को ‘कहूट्स’(अस्पृश्य) कहा जाता है. ‘कहूट्स’ एक सामाजिक वर्ग है. इस वर्ग के लोग मछली, सफाई एवं ईट के भट्टों पर काम करने वाले किसानों की जमीन पर भूमिहीन मजदूर के रुप में काम करते हैं. यह वर्ग पाकिस्तान के समाज में बिल्कुल सम्मानहीन होकर रह गया है. हिंदुओं की निम्न जातियों में से 93% लोग पाकिस्तान के ग्रामीण प्रांतों से ही हैं. पाकिस्तान के थरपर्कर जिले में निम्न जाति की जनसंख्या 45 फीसदी है. इस आबादी के सात व्यक्तियों में से केवल एक ही पढ़ पा रहा है. विभिन्न प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार, पाक में लगभग बीस लाख लोग दलित बनकर तरह-तरह की यातनाओं के शिकार होने लगे हैं. बांग्लादेश और श्रीलंका में पिछड़ी हुई जातियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है. मगर पाकिस्तान में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन्हें 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. लेकिन यह प्रावधान कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है. पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में अत्यधिक संख्या में दलित बंधुआ मज़दूर बनकर नारकीय जीवन जी रहे हैं. हिंदुओं की निम्न जाति के 83.6% जनता के पास एक गज जमीन भी नहीं है. धर्म के रुप में इस्लाम समानता की बात तो करता है, लेकिन हिंदुओं की निम्न जातियों के लोगों को आज भी वहां के हज्जाम की दुकानों में प्रवेश नहीं मिला है. अगर किसी होटल में जायें तो नीचे बैठकर खाने के साथ, थाली, गिलास भी धोने को मजबूर होना पड़ता है. मुसलमानों में भी सल्ला, सच्चि, मोच्चि, पथेर, भंगी वर्गों को निम्न से निम्न जाति कहकर हीनता के भाव से देखने की स्थिति भी बदस्तूर जारी है.
छूआछूत के मामले में नेपाल भी पीछे नहीं है. नेपाल में लगभग 45 लाख दलित आबादी आज भी अग्रवर्णों के दमन को मौन रुप से सह रही है. निम्न जाति के द्वारा छुए गए पानी को भी फेंके जाने की अमानवीय प्रथा नेपाल में आज भी जारी है. मंदिर में प्रवेश करना, दूसरे वर्ग के शादियों में जाना और अंतर्जातीय विवाह जैसी बातें नेपाल दलित सपने में भी नहीं सोच सकता. वहां के शासन द्वारा 1963 में जातिगत अस्पृश्यता का निषेध किया जा चुका है. बावजूद इसके व्यवहार में आज तक जारी है. 1990 के संविधान में उसे दंड दिया जाने वाला अपराध माना गया है. 2007 तक के (तात्कालिक) संविधान में उसमें और कुछ जोड़कर जाति व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया गया था. लेकिन वे सारे नियम आचरण में व्यर्थ ही सिद्ध हुए हैं. गरीबी दलितों को कहीं का नहीं छोड़ रही है. नेपाल में 53% साक्षरता होने पर भी वहां के दलितों की साक्षरता दर 33.8 फीसदी ही है. नेपाल की जनता में 3.4% के पास डिग्री है तो, दलितों में वह संख्या केवल 0.4%ही है. राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की औसत आयु 58.9 वर्ष है, वहीं दलित महिलाओं का औसत स्तर 50.8 वर्ष ही है. उस देश के दलितों में आधे से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे ही गिड़गिडा रहे हैं. नेपाल की राज्य सभा में दलितों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% से ज्यादा नहीं हो पाया है.
जाति-व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश के संविधान में स्पष्ट रुप से प्रावधान होने के बावजूद भी वह कागजों पर ही दिखाई दे रहा है. बांग्लादेश में लगभग आधे करोड़ से भी ज्यादा दलितों के होने का अनुमान है. कहां जीना है? किन जगहों पर खेलना है? किन होटलों में खाना है? कहां चाय पीनी है? कैसे पीना है? कौन से श्मशान घाटों का उपयोग करना है? ऐसे नियमों से भरी लंबी तालिका होने पर भी बांग्लादेश में दशकों से जाति-प्रथा का आचरण में व्यवहार हो रहा है. यह सब कुछ किसी लिखित अधिनियम के अनुसार नहीं चल रहा है. घृणा भरी नज़रों से, खुलेआम ही यह सब चल रहा है. हिंदू दलितों में 64 फीसदी अनपढ़ हैं. हिंदू-मुस्लिम धर्मों से जुड़े पिछड़ी जातियों के लोग बर्बर प्रथा का सामना करने का मुख्य कारण आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध न होना ही है. वहां के दलितों का आर्थिक स्तर का एक आंकड़ा निम्न वस्तुओं के उपयोग के स्तर पर देखा जा सकता है. टेलिफोन, रेडियो का 9% और सायकिल का 14.5% उपयोग वहां की दलित आबादी करती है. बांग्लादेश के स्वतंत्र होने पर (1971) 1974 में वेस्टेड प्रापर्टी एक्ट बना. इसके अनुसार, राज्य के लिए दुश्मन बनकर रहने वाले व्यक्तियों के ज़मीन को बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर ही सरकार अपने क्षेत्र/ वश में कर सकती है. इसके चलते हिंदुओं के जमीन को उनमें भी विशेष रुप से निस्सहाय दलितों के ज़मीन को बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा हड़प लिया गया है. इस कारण से गरीबी के शिकंजे में फंस कर वहां के दलितों के जीवन और अस्तित्व को इस कानून ने सड़क पर ला दिया है.
एक अन्य एशियाई देश श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों का प्रभुत्व है. देश के उत्तर-पूरब प्रांत के तमिल चाय के बागानों (खेतों) में 150 वर्षों से काम कर रहे भारतीय तमिलों में तीन प्रकार की जाति व्यवस्थाएं चल रही है. दक्षिण एशिया में जातिगत असमानताएं थोड़ी बहुत कम दिखाई देने वाला देश श्रीलंका ही है. जातियों के बीच चले तीव्र संघर्ष के बावजूद कहना होगा कि इस देश में जाति-प्रथा का क्रूर रूप उतना अधिक नहीं हो पाया है. प्रतिदिन युद्ध के माहौल से जूझते हुए जाफ़ना समाज में जाति आधारित व्यवस्था पर टॉयगर्स के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था. श्रीलंका के चाय के बागानों में काम करने वाले तमिल श्रमिकों पर वहां की व्यवस्था ने निम्न वर्ग के होने का चस्पा लगा दिया है. बहुत से अध्ययनों के अनुसार अवगत होता है कि श्रीलंका की आबादी में लगभग 30% (पचास लाख) लोग किसी न किसी रुप में एक ही स्थान पर जातिगत विषमता का सामना कर रहे हैं. ‘वेलक्लॉर’ नाम की अग्रवर्ण के वर्चस्व वाली जाति के प्रार्थनालयों में ‘पंचमार’ नाम की निम्न जाति के लिए आज भी प्रवेश वर्जित है.
तमाम आंकलन को देखने के बाद कहा जा सकता है कि पूरे दक्षिण एशिया में जाति प्रथा का जहर इस स्तर तक फैलने का कारण भारत की समाजिक व्यवस्था ही है. जाति और उसके साथ जुड़कर विभाजित हुए पेशों ने भारत की अधिसंख्यक जनता के जीवन में अंधकार भरने का कार्य किया है. यह न मिटा देने वाला एक सामाजिक सच है.
भारतीय राष्ट्रीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक युग के महत्वपूर्ण सामाजिक चिंतक डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस कड़वे सच को बखूबी देखा था. शायद यही वजह थी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत में ‘स्वतंत्रता-आंदोलन से भी ज्यादा कठिन जाति-उन्मूलन का कार्य है.’
– लेखक हैदराबाद विवि हैदराबाद में दलित-आदिवासी अध्ययन एवं अनुवाद केंद्र में अतिथि अध्यापक हैं. संपर्कः- 09059379268
एक पत्रिका के लेख में प्रसिद्ध उद्योगपति वॉरेन बफेट ने एक सवाल उठाया था कि “एक ही मां के गर्भ से जन्में जुड़वों का समान रुप से चुस्ती, शक्ति-सामर्थ्य है. उनमें से एक का जन्म बांग्लादेश में और दूसरे का अमेरिका में होगा तो क्या होगा? उनका नसीब कैसा रहेगा? व्यक्तियों के सामाजिक स्तर के अनुसार उसके भविष्य का निर्माण कैसा होगा?” उन्होंने विनम्रता के साथ गहरे और गंभीर विषय को सामने रखते हुए कहा है कि अमेरिका में जन्म के स्तर पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं मेरा जीवन है. मुझे किसी भी व्यवसाय को चुनने की आजादी इस धरती और देश ने प्रदान की है. अगर मैं कहीं दूसरी जगह जन्म लेता तो कभी भी इस स्थान तक नहीं पहुंच सकता था. लेकिन एक बात तो विचारणीय है कि अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देश में भी नस्लगत भेद-भाव उस देश की छवि को धूल-धूसरित करता है.
कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि व्यक्तियों के भविष्य निर्माण में देशगत, प्रांतीय, धार्मिक और जातीय आधारों की विशिष्ट भूमिका रहती है. भारतीय समाज व्यवस्था की स्थिति बहुस्तरीय है. भारतीय समाज व्यवस्था के ऊपरी पायदान पर ‘सवर्ण’ केंद्रित है तो दूसरी और निचले पायदान पर ‘अंत्यज’ या ‘दलित’. क्या दलितों को इस समाज-व्यवस्था ने मानवीय दर्जा दिया है? भारत जैसे देश की संस्कृति की गाथा हजारों वर्षों से गायी जा रही है. जबकि इस देश की समाज-व्यवस्था ने क्रूरता, बर्बरता एवं अमानवीयता का परिचय कर्म और व्यवहार के स्तर पर दलितों के संदर्भ में दिया है. श्रमशील तबकों को हाशिये पर रखा गया है. मेहनतकश लोगों के श्रम की बुनियाद पर ही यह समाज-व्यवस्था टिकी हुई है. जबकि जातीय अहंकार और दंभ के कारण निर्दोष भारतीय नागरिक समुदाय का एक हिस्सा निरंतर उपेक्षा, अपमान और नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. क्या सभ्य संस्कृति का यह अर्थ लगाया जाए कि मनुष्य का मनुष्य पर अत्याचार एक श्रेष्ठ सभ्यता का विशेष गुण है?
भारत सरकार के एक अध्ययन के अनुसार भारत में दलित तबकों के बच्चे जीवन की आधारभूत सुविधाओं विशेषकर पोषण की कमी की वजह से जन्म लेने के बावजूद भी अन्य तबकों के बच्चों की तुलना में औसत आयु के स्तर पर चार साल कम जीवित रह पाते हैं. जन्म लेने वालों में से आधे से ज्यादा बच्चे पौष्टिक आहार की कमी से जूझ रहे हैं. भारत की औसत बाल जन्म दर में हर सौ बच्चों के आंकड़े को देखा जाय तो उनमें से 12 बच्चे पांच वर्ष की अवस्था से पूर्व ही अकाल काल के ग्रास बन रहे हैं. दलित तबकों के हर पांच बच्चों में से एक ही ठीक से स्कूल जा पाता है. हर 3 बच्चों में से एक बर्बर गरीबी का शिकार हो रहा है. दलित तबकों की 31% महिलाएं रक्त की कमी से परेशान हैं. भारत देश में छः हजार जातियां हैं. उसमें भी अस्सी फीसदी से अधिक दबी-कुचली जा रही जातियां हैं. हजारों वर्षों से तड़पते हुए वर्ण-व्यवस्था के लोहे के शिकंजे के पिंजरे में फंसकर, अवसरों से वंचित होकर निचले पायदान पर ही जीते जा रहे जन-समुदायों की स्थिति कैसी होगी? भारत के संविधान निर्माताओं ने जो स्वप्न देखने की आकांक्षा चाही थी उसे जाति-प्रथा से युक्त समाज-व्यवस्था ने साकार नहीं होने दिया. जाति-प्रथा से पीड़ित तबकों के सुधार में असफलताओं की गणना संभव ही नहीं है. आज भी सरकारी, गैर-सरकारी शौचालयों में अमानुषिक कृत्य करने वाले ‘मेहतर’ (भंगी) या ‘सफाईकर्मियों’ की संख्या दस लाख से अधिक होने की संभावना की सूचना सरकारी गणना के स्तर पर सामने आयी है. आंध्रप्रदेश के साथ-साथ देश के अनेक राज्यों में आज भी भेद-भाव पूर्ण ‘दो गिलास’ की पद्धति व्यवहार में है. दलितों का मंदिरों में प्रवेश न होने देना और सवर्णों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे कुंओं से पानी पीने की सुविधा नहीं देना जैसे अमानवीय कार्य केवल जन्मगत आधार पर ही तो हो रहे हैं. जाति-व्यवस्था के कारण ही वैश्विक स्तर पर 26 करोड़ आबादी कष्ट सह रही है. दृढ़ कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी वे सामाजिक न्याय से मोहताज हैं. विशेष रुप से दक्षिण एशिया के देशों में यह प्रथा व्यवस्थीकृत होकर जड़ें जमा चुकी हैं.
संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति की स्वतंत्र समिति ने चिंता व्यक्त की है कि आज भी दक्षिण एशिया के देशों में दलितों के साथ अछूत व्यवहार किया जा रहा है. यह विचारणीय और सोचनीय बिंदु है कि कैसे भारत विश्व की चौथी अर्थ-व्यवस्था होने पर गुमान कर रहा है और उसी के देश में मानव समुदायों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है.
पाकिस्तान जैसे देश में भी जाति-व्यवस्था का एक रुप दिखाई दिया है. पाकिस्तान में कानूनन शेड्यूल्ड कॉस्ट के नाम से घोषित किये गये हिंदुओं में निम्न जातियों को ‘कहूट्स’(अस्पृश्य) कहा जाता है. ‘कहूट्स’ एक सामाजिक वर्ग है. इस वर्ग के लोग मछली, सफाई एवं ईट के भट्टों पर काम करने वाले किसानों की जमीन पर भूमिहीन मजदूर के रुप में काम करते हैं. यह वर्ग पाकिस्तान के समाज में बिल्कुल सम्मानहीन होकर रह गया है. हिंदुओं की निम्न जातियों में से 93% लोग पाकिस्तान के ग्रामीण प्रांतों से ही हैं. पाकिस्तान के थरपर्कर जिले में निम्न जाति की जनसंख्या 45 फीसदी है. इस आबादी के सात व्यक्तियों में से केवल एक ही पढ़ पा रहा है. विभिन्न प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार, पाक में लगभग बीस लाख लोग दलित बनकर तरह-तरह की यातनाओं के शिकार होने लगे हैं. बांग्लादेश और श्रीलंका में पिछड़ी हुई जातियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है. मगर पाकिस्तान में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन्हें 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. लेकिन यह प्रावधान कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है. पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में अत्यधिक संख्या में दलित बंधुआ मज़दूर बनकर नारकीय जीवन जी रहे हैं. हिंदुओं की निम्न जाति के 83.6% जनता के पास एक गज जमीन भी नहीं है. धर्म के रुप में इस्लाम समानता की बात तो करता है, लेकिन हिंदुओं की निम्न जातियों के लोगों को आज भी वहां के हज्जाम की दुकानों में प्रवेश नहीं मिला है. अगर किसी होटल में जायें तो नीचे बैठकर खाने के साथ, थाली, गिलास भी धोने को मजबूर होना पड़ता है. मुसलमानों में भी सल्ला, सच्चि, मोच्चि, पथेर, भंगी वर्गों को निम्न से निम्न जाति कहकर हीनता के भाव से देखने की स्थिति भी बदस्तूर जारी है.
छूआछूत के मामले में नेपाल भी पीछे नहीं है. नेपाल में लगभग 45 लाख दलित आबादी आज भी अग्रवर्णों के दमन को मौन रुप से सह रही है. निम्न जाति के द्वारा छुए गए पानी को भी फेंके जाने की अमानवीय प्रथा नेपाल में आज भी जारी है. मंदिर में प्रवेश करना, दूसरे वर्ग के शादियों में जाना और अंतर्जातीय विवाह जैसी बातें नेपाल दलित सपने में भी नहीं सोच सकता. वहां के शासन द्वारा 1963 में जातिगत अस्पृश्यता का निषेध किया जा चुका है. बावजूद इसके व्यवहार में आज तक जारी है. 1990 के संविधान में उसे दंड दिया जाने वाला अपराध माना गया है. 2007 तक के (तात्कालिक) संविधान में उसमें और कुछ जोड़कर जाति व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया गया था. लेकिन वे सारे नियम आचरण में व्यर्थ ही सिद्ध हुए हैं. गरीबी दलितों को कहीं का नहीं छोड़ रही है. नेपाल में 53% साक्षरता होने पर भी वहां के दलितों की साक्षरता दर 33.8 फीसदी ही है. नेपाल की जनता में 3.4% के पास डिग्री है तो, दलितों में वह संख्या केवल 0.4%ही है. राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की औसत आयु 58.9 वर्ष है, वहीं दलित महिलाओं का औसत स्तर 50.8 वर्ष ही है. उस देश के दलितों में आधे से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे ही गिड़गिडा रहे हैं. नेपाल की राज्य सभा में दलितों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% से ज्यादा नहीं हो पाया है.
जाति-व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश के संविधान में स्पष्ट रुप से प्रावधान होने के बावजूद भी वह कागजों पर ही दिखाई दे रहा है. बांग्लादेश में लगभग आधे करोड़ से भी ज्यादा दलितों के होने का अनुमान है. कहां जीना है? किन जगहों पर खेलना है? किन होटलों में खाना है? कहां चाय पीनी है? कैसे पीना है? कौन से श्मशान घाटों का उपयोग करना है? ऐसे नियमों से भरी लंबी तालिका होने पर भी बांग्लादेश में दशकों से जाति-प्रथा का आचरण में व्यवहार हो रहा है. यह सब कुछ किसी लिखित अधिनियम के अनुसार नहीं चल रहा है. घृणा भरी नज़रों से, खुलेआम ही यह सब चल रहा है. हिंदू दलितों में 64 फीसदी अनपढ़ हैं. हिंदू-मुस्लिम धर्मों से जुड़े पिछड़ी जातियों के लोग बर्बर प्रथा का सामना करने का मुख्य कारण आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध न होना ही है. वहां के दलितों का आर्थिक स्तर का एक आंकड़ा निम्न वस्तुओं के उपयोग के स्तर पर देखा जा सकता है. टेलिफोन, रेडियो का 9% और सायकिल का 14.5% उपयोग वहां की दलित आबादी करती है. बांग्लादेश के स्वतंत्र होने पर (1971) 1974 में वेस्टेड प्रापर्टी एक्ट बना. इसके अनुसार, राज्य के लिए दुश्मन बनकर रहने वाले व्यक्तियों के ज़मीन को बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर ही सरकार अपने क्षेत्र/ वश में कर सकती है. इसके चलते हिंदुओं के जमीन को उनमें भी विशेष रुप से निस्सहाय दलितों के ज़मीन को बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा हड़प लिया गया है. इस कारण से गरीबी के शिकंजे में फंस कर वहां के दलितों के जीवन और अस्तित्व को इस कानून ने सड़क पर ला दिया है.
एक अन्य एशियाई देश श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों का प्रभुत्व है. देश के उत्तर-पूरब प्रांत के तमिल चाय के बागानों (खेतों) में 150 वर्षों से काम कर रहे भारतीय तमिलों में तीन प्रकार की जाति व्यवस्थाएं चल रही है. दक्षिण एशिया में जातिगत असमानताएं थोड़ी बहुत कम दिखाई देने वाला देश श्रीलंका ही है. जातियों के बीच चले तीव्र संघर्ष के बावजूद कहना होगा कि इस देश में जाति-प्रथा का क्रूर रूप उतना अधिक नहीं हो पाया है. प्रतिदिन युद्ध के माहौल से जूझते हुए जाफ़ना समाज में जाति आधारित व्यवस्था पर टॉयगर्स के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था. श्रीलंका के चाय के बागानों में काम करने वाले तमिल श्रमिकों पर वहां की व्यवस्था ने निम्न वर्ग के होने का चस्पा लगा दिया है. बहुत से अध्ययनों के अनुसार अवगत होता है कि श्रीलंका की आबादी में लगभग 30% (पचास लाख) लोग किसी न किसी रुप में एक ही स्थान पर जातिगत विषमता का सामना कर रहे हैं. ‘वेलक्लॉर’ नाम की अग्रवर्ण के वर्चस्व वाली जाति के प्रार्थनालयों में ‘पंचमार’ नाम की निम्न जाति के लिए आज भी प्रवेश वर्जित है.
तमाम आंकलन को देखने के बाद कहा जा सकता है कि पूरे दक्षिण एशिया में जाति प्रथा का जहर इस स्तर तक फैलने का कारण भारत की समाजिक व्यवस्था ही है. जाति और उसके साथ जुड़कर विभाजित हुए पेशों ने भारत की अधिसंख्यक जनता के जीवन में अंधकार भरने का कार्य किया है. यह न मिटा देने वाला एक सामाजिक सच है.
भारतीय राष्ट्रीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक युग के महत्वपूर्ण सामाजिक चिंतक डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस कड़वे सच को बखूबी देखा था. शायद यही वजह थी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत में ‘स्वतंत्रता-आंदोलन से भी ज्यादा कठिन जाति-उन्मूलन का कार्य है.’
– लेखक हैदराबाद विवि हैदराबाद में दलित-आदिवासी अध्ययन एवं अनुवाद केंद्र में अतिथि अध्यापक हैं. संपर्कः- 09059379268 बाबा साहेब के ब्राह्मणीकरण की साजिश
 भारत में जो भी ज्ञानी-ध्यानी लोग पैदा होते हैं…. वो किसी भी जाति में पैदा हों….. ये ब्राह्मण उन्हें अपनी संतान कहने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं…. इस जन्म की बात घोषित करें या पूर्वजन्म की….. यानि कि चित भी मेरी….पट भी मेरी……ये हिन्दू को मुसलमान और मुसलमान को हिन्दू बनाने में तनिक भी देर नहीं करते…… साईं बाबा मुसलमान थे….. उन्हें अपना ईष्ट बना लिया और ……. हो गई पौबारा…. वर्ष भर में इतना दान किसी और देवता के नाम पर नहीं आता जितना साईं बाबा के मन्दिर पर आता है……और ये अधम अपने आपको उनकी कृपा पर ही छोड़ देते हैं……. यही कारण है कि भारत से कभी भी दास प्रथा जाने वाली नहीं लगती…एक कारण और भी है कि अधम समाज में पैदा हुए तथाकथित समाज सुधारक अपना पेट भरने में ही जुटे रहे और आज भी वैसा ही हो रहा है.
उल्लिखित है कि साईंबाबा जिन्हें शिरडी साईंबाबा भी कहा जाता है और जिन्हें मुसलमान जाति का बताया जाता है….. पिछले महीनों हिन्दू मठाधीशों ने साईंबाबा की जाति को लेकर काफी हौ-हल्ला भी किया था. कहा गया था वो एक फकीर थे जिन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है. उन्हें भगवान कैसे माना जा सकता है किंतु हिन्दुओं के बड़े तबके ने शोर मचाने वालों की एक नहीं सुनी और साईंबाबा भगवान ही बने हुए है. कारण यह नहीं कि हिन्दू मुसलमनों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, कारण ये है कि साईंबाबा बाबा के शिरडी स्थित मन्दिर में इतना चढ़ावा आता है जो कई हिन्दू देवताओं के नाम पर बने मन्दिरों में आने वाले चढ़ावे से भी कई गुना होता है. ब्राह्मण जो कभी राम-कृष्ण का भक्त हुआ करता था, अब अब साईं बाबा का पक्का भक्त बन गया है क्यूं की वो साईं के बड़ते हुए भक्तो की संख्या और उसपे चढ़ने वाले चढ़ावे के लालच को कैसे छोड़ सकता है …इसलिए अब हर मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित करता है, पर ये वही ब्रह्माण वर्ग है जिसने साईं को जीते-जी कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया …और अब उनकी मूर्ति मंदिर में स्थापित करता है और दिन रात साईं के गुण गाने में मग्न है.
बड़े-बड़े तथाकथित दलित राजनेता पालतू कुत्ता बने रहकर कुर्सी पाने के लालच में वर्चस्वशाली राजनैतिक दलों के नेताओं न केवल तलुए चाटने पर लगे होते हैं… सत्ता में कुर्सी पाने के बाद “ब्राह्मण” हो जाते हैं. कमजोर और निरीह जनता को तो केवल मोहरा बनाए रखने का काम करते हैं. कहना न अतिश्योक्ति न होगा कि समाज के कमजोर और निरीह समाज में पैदा हुए बुद्धिजीवी ब्राह्मणवाद के शिकार होने से नहीं बच पाते. और जो बच जाते हैं, उनको ब्राह्मण घोषित करने के प्रयास बार-बार किया जाता रहा है. 21 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ब्राहमण चेतना मंच के कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा, “बाबा साहेब अंबेडकर दलित नहीं थे, वो सनाड्य ब्राह्मण थे. वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित थे, उन्होंने लोगों को ऊपर उठाने का काम किया, इसलिए उन्होंने संविधान लिखा. उनका नाम अंबेडकर नहीं था उनका नाम था भीमराव, लेकिन अब उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है.” भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल का यह बयान यूं ही नहीं आया होगा अपितु इस बयान के पीछे बाबा साहेब के ब्राह्मणीकरण की बू आती है.
उन्होंने बसपा का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए आगे कहा कि इस देश में ब्राह्मणों ने इतिहास रचा था, लेकिन आज यहां अम्बेडकर के नाम पर राजनीति होती है. जरा भी कुछ हो जाता है तो दंगे शुरू हो जाते हैं. लेकिन अंबेडकर का नाम भीमराव न कहकर बाबा साहब अंबेडकर कहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि भीमराव को उनकी प्राथमिक शिक्षा दिलाने का काम किसने किया था, उन्हें यूरोप में शिक्षा दिलाने का काम किसने किया था. भीमराव अपने नाम के आगे अंबेडकर की उपाधि लगाए थे, यह उनका नाम नहीं था… सांसद शिव प्रताप शुक्ल के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि उनको बाबा साहेब के जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है. जब उन्हें इतना ही पता नहीं है कि बाबा साहेब की प्राथमिक और उच्च शिक्षा दिलाने के पीछे कौन-कौन लोग रहे तो उन्हें और क्या पता होगा. उनका यह बयान हवा में पत्थर उछालने जैसा ही है. बिना सिरपैर की बयानबाजी करना ही ब्राह्मण की सबसे बड़ी खूबी है जिसके जाल में अज्ञानी लोग आराम से फंस जाते हैं.
आरएसएस और अब उसके द्वारा पोषित भाजपा का यह कोई पहला अवसर नहीं है कि जब उसने किसी न किसी के जरिए बाबा साहेब को अपने पाले में करने और अनुसूचित जातियों में फूट डालने का प्रयास किया है. इससे पूर्व भी ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ पहले भी ऐसे कार्य कर चुकी है. संघ के झंडेवालान द्वारा प्रकाशित डा. कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक “ राष्ट्र पुरूष: बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर” में अनेक ऐसे झूठे प्रसंग है. जिनके कोई हाथ-पैर तो क्या कोई जमीन तक भी नहीं है. इन प्रसंगों के जरिए बाबा साहब को पूरा-का-पूरा सनातनी नेता, गीता का संरक्षक, यज्ञोपवीत कर्ता, महारों को जनेऊ धारण कराने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बाबा साहब के प्रारंम्भिक जीवन काल के हैं. दुख तो ये है कि संदर्भित पुस्तक के रचियता ने 1929 और 1949 के बीच के वर्षों पर कोई चर्चा नहीं की है जबकि बाबा साहब का मुख्य कार्यकारी दौर वही था.
पुस्तक के लेखक ने सबसे ज्यादा जोर बाबा साहब को मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने पर लगाया है जो दुराग्रह पूर्ण कार्य है. इतना ही नहीं, डा. कृष्ण गोपाल के मन का मैल पुस्तक के पेज 5 पर उल्लिखित इन शब्दों में स्पष्ट झलकता है– “एक अपृश्य परिवार में जन्मा बालक सम्पूर्ण भारतीय समाज का विधि-विधाता बन गया. धरती की धूल उड़कर आकाश और मस्तक तक जा पहुंची”. इस पंक्ति का लिखना-भर ही सीधे-सीधे बाबा साहेब का अपमान करना है, और कुछ नहीं. इन पंक्तियों में पूरा का पूरा मनुवाद भरा पड़ा है.
लेखक तेजपाल सिंह तेज एक लेखक हैं. तेजपाल सिंह तेज को (हिन्दी अकादमी (दिल्ली) ने बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. इनका संपर्क सूत्र tejpaltej@gmail.com है.
भारत में जो भी ज्ञानी-ध्यानी लोग पैदा होते हैं…. वो किसी भी जाति में पैदा हों….. ये ब्राह्मण उन्हें अपनी संतान कहने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं…. इस जन्म की बात घोषित करें या पूर्वजन्म की….. यानि कि चित भी मेरी….पट भी मेरी……ये हिन्दू को मुसलमान और मुसलमान को हिन्दू बनाने में तनिक भी देर नहीं करते…… साईं बाबा मुसलमान थे….. उन्हें अपना ईष्ट बना लिया और ……. हो गई पौबारा…. वर्ष भर में इतना दान किसी और देवता के नाम पर नहीं आता जितना साईं बाबा के मन्दिर पर आता है……और ये अधम अपने आपको उनकी कृपा पर ही छोड़ देते हैं……. यही कारण है कि भारत से कभी भी दास प्रथा जाने वाली नहीं लगती…एक कारण और भी है कि अधम समाज में पैदा हुए तथाकथित समाज सुधारक अपना पेट भरने में ही जुटे रहे और आज भी वैसा ही हो रहा है.
उल्लिखित है कि साईंबाबा जिन्हें शिरडी साईंबाबा भी कहा जाता है और जिन्हें मुसलमान जाति का बताया जाता है….. पिछले महीनों हिन्दू मठाधीशों ने साईंबाबा की जाति को लेकर काफी हौ-हल्ला भी किया था. कहा गया था वो एक फकीर थे जिन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है. उन्हें भगवान कैसे माना जा सकता है किंतु हिन्दुओं के बड़े तबके ने शोर मचाने वालों की एक नहीं सुनी और साईंबाबा भगवान ही बने हुए है. कारण यह नहीं कि हिन्दू मुसलमनों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, कारण ये है कि साईंबाबा बाबा के शिरडी स्थित मन्दिर में इतना चढ़ावा आता है जो कई हिन्दू देवताओं के नाम पर बने मन्दिरों में आने वाले चढ़ावे से भी कई गुना होता है. ब्राह्मण जो कभी राम-कृष्ण का भक्त हुआ करता था, अब अब साईं बाबा का पक्का भक्त बन गया है क्यूं की वो साईं के बड़ते हुए भक्तो की संख्या और उसपे चढ़ने वाले चढ़ावे के लालच को कैसे छोड़ सकता है …इसलिए अब हर मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित करता है, पर ये वही ब्रह्माण वर्ग है जिसने साईं को जीते-जी कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया …और अब उनकी मूर्ति मंदिर में स्थापित करता है और दिन रात साईं के गुण गाने में मग्न है.
बड़े-बड़े तथाकथित दलित राजनेता पालतू कुत्ता बने रहकर कुर्सी पाने के लालच में वर्चस्वशाली राजनैतिक दलों के नेताओं न केवल तलुए चाटने पर लगे होते हैं… सत्ता में कुर्सी पाने के बाद “ब्राह्मण” हो जाते हैं. कमजोर और निरीह जनता को तो केवल मोहरा बनाए रखने का काम करते हैं. कहना न अतिश्योक्ति न होगा कि समाज के कमजोर और निरीह समाज में पैदा हुए बुद्धिजीवी ब्राह्मणवाद के शिकार होने से नहीं बच पाते. और जो बच जाते हैं, उनको ब्राह्मण घोषित करने के प्रयास बार-बार किया जाता रहा है. 21 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ब्राहमण चेतना मंच के कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा, “बाबा साहेब अंबेडकर दलित नहीं थे, वो सनाड्य ब्राह्मण थे. वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित थे, उन्होंने लोगों को ऊपर उठाने का काम किया, इसलिए उन्होंने संविधान लिखा. उनका नाम अंबेडकर नहीं था उनका नाम था भीमराव, लेकिन अब उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है.” भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल का यह बयान यूं ही नहीं आया होगा अपितु इस बयान के पीछे बाबा साहेब के ब्राह्मणीकरण की बू आती है.
उन्होंने बसपा का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए आगे कहा कि इस देश में ब्राह्मणों ने इतिहास रचा था, लेकिन आज यहां अम्बेडकर के नाम पर राजनीति होती है. जरा भी कुछ हो जाता है तो दंगे शुरू हो जाते हैं. लेकिन अंबेडकर का नाम भीमराव न कहकर बाबा साहब अंबेडकर कहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि भीमराव को उनकी प्राथमिक शिक्षा दिलाने का काम किसने किया था, उन्हें यूरोप में शिक्षा दिलाने का काम किसने किया था. भीमराव अपने नाम के आगे अंबेडकर की उपाधि लगाए थे, यह उनका नाम नहीं था… सांसद शिव प्रताप शुक्ल के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि उनको बाबा साहेब के जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है. जब उन्हें इतना ही पता नहीं है कि बाबा साहेब की प्राथमिक और उच्च शिक्षा दिलाने के पीछे कौन-कौन लोग रहे तो उन्हें और क्या पता होगा. उनका यह बयान हवा में पत्थर उछालने जैसा ही है. बिना सिरपैर की बयानबाजी करना ही ब्राह्मण की सबसे बड़ी खूबी है जिसके जाल में अज्ञानी लोग आराम से फंस जाते हैं.
आरएसएस और अब उसके द्वारा पोषित भाजपा का यह कोई पहला अवसर नहीं है कि जब उसने किसी न किसी के जरिए बाबा साहेब को अपने पाले में करने और अनुसूचित जातियों में फूट डालने का प्रयास किया है. इससे पूर्व भी ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ पहले भी ऐसे कार्य कर चुकी है. संघ के झंडेवालान द्वारा प्रकाशित डा. कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक “ राष्ट्र पुरूष: बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर” में अनेक ऐसे झूठे प्रसंग है. जिनके कोई हाथ-पैर तो क्या कोई जमीन तक भी नहीं है. इन प्रसंगों के जरिए बाबा साहब को पूरा-का-पूरा सनातनी नेता, गीता का संरक्षक, यज्ञोपवीत कर्ता, महारों को जनेऊ धारण कराने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बाबा साहब के प्रारंम्भिक जीवन काल के हैं. दुख तो ये है कि संदर्भित पुस्तक के रचियता ने 1929 और 1949 के बीच के वर्षों पर कोई चर्चा नहीं की है जबकि बाबा साहब का मुख्य कार्यकारी दौर वही था.
पुस्तक के लेखक ने सबसे ज्यादा जोर बाबा साहब को मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने पर लगाया है जो दुराग्रह पूर्ण कार्य है. इतना ही नहीं, डा. कृष्ण गोपाल के मन का मैल पुस्तक के पेज 5 पर उल्लिखित इन शब्दों में स्पष्ट झलकता है– “एक अपृश्य परिवार में जन्मा बालक सम्पूर्ण भारतीय समाज का विधि-विधाता बन गया. धरती की धूल उड़कर आकाश और मस्तक तक जा पहुंची”. इस पंक्ति का लिखना-भर ही सीधे-सीधे बाबा साहेब का अपमान करना है, और कुछ नहीं. इन पंक्तियों में पूरा का पूरा मनुवाद भरा पड़ा है.
लेखक तेजपाल सिंह तेज एक लेखक हैं. तेजपाल सिंह तेज को (हिन्दी अकादमी (दिल्ली) ने बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. इनका संपर्क सूत्र tejpaltej@gmail.com है. बिहारः अम्बेडकर छात्रावास में सवर्ण छात्र!
 पटना। अम्बेडकर छात्रावास अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक सहारे की तरह रहा है. गरीब वर्ग के दलित छात्र यहीं अपने जीवन के सपने बुनते हैं. अपने समाज के अन्य छात्रों के बीच रहकर उनका विकास होता है. लेकिन बिहार सरकार इसमें सेंधमारी करने जा रही है. बिहार सरकार ने अम्बेडकर छात्रावास में सवर्ण छात्रों को रहने की इजाजत दे दी है. सरकार ने इसके लिए कागजी फरमान भी जारी कर दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रावास में एससी/एसटी छात्रों की सीटें खाली रहने पर ओबीसी (पिछड़ा) और फिर जनरल (सामान्य) छात्र अम्बेडकर हॉस्टल में रह सकते हैं.
बिहार सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव प्रेम सिंह मीणा के द्वारा इस आशय का आदेश 15-07-2016 पत्रांक- 4680 को जारी किया जा चुका है. बिहार सरकार के इस फैसले ने दलितों को एक और झटका दिया है. पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे एवं वर्तमान में लेखन और पत्रकारिता में सक्रिय बुद्ध शरण हंस ने सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा कर रही है तो यह पूरी तरह से दलित विरोधी षड्यंत्र है. अम्बेडकर छात्रावास स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत एससी/एसटी वेलफेयर के लिए जारी पैसे से बनता है. यह छात्रावास सिर्फ एससी/एसटी छात्रों के लिए होता है. इसमें दूसरे वर्ग के छात्र कैसे रह सकते हैं. बुद्ध शरण हंस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अम्बेडकर हॉस्टल में सीटें खाली रहने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब तो ज्यादा बच्चे आ रहे हैं. मुझे शक है कि कहीं सरकार बाद में यह न कहने लगे कि छात्रावास सिर्फ योग्य एससी छात्रों को ही दिया जाएगा. इसी सरकार ने हाल ही में एससी वर्ग के कर्मचारियों का आरक्षण में प्रोमोशन हटाया है वह भी सबके सामने हैं. नीतीश असल में भाजपा के आदमी हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं. नीतीश और लालू की यह सरकार दलितों का काफी नुकसान कर रही है.
गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में दलित छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा था. हकीकत यह भी है कि विधानसभा चुनाव में दलितों के वोट से ही चुनाव में पिछड़ रहे नीतीश-लालू गठबंधन को जीत मिल पाई थी. लेकिन सरकार आने के बाद से लेकर अब तक सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिससे दलित समाज के छात्रों और कर्मचारियों के हित की अनदेखी हुई है. इससे पहले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दलितों की सीट सवर्णों को दिया जा चुका है. इस पूरे मामले पर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला से उनका पक्ष जानने के लिए उनके नंबर पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. दलित दस्तक द्वारा उन्हें मैसेज भी किया गया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला.
पटना। अम्बेडकर छात्रावास अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक सहारे की तरह रहा है. गरीब वर्ग के दलित छात्र यहीं अपने जीवन के सपने बुनते हैं. अपने समाज के अन्य छात्रों के बीच रहकर उनका विकास होता है. लेकिन बिहार सरकार इसमें सेंधमारी करने जा रही है. बिहार सरकार ने अम्बेडकर छात्रावास में सवर्ण छात्रों को रहने की इजाजत दे दी है. सरकार ने इसके लिए कागजी फरमान भी जारी कर दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रावास में एससी/एसटी छात्रों की सीटें खाली रहने पर ओबीसी (पिछड़ा) और फिर जनरल (सामान्य) छात्र अम्बेडकर हॉस्टल में रह सकते हैं.
बिहार सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव प्रेम सिंह मीणा के द्वारा इस आशय का आदेश 15-07-2016 पत्रांक- 4680 को जारी किया जा चुका है. बिहार सरकार के इस फैसले ने दलितों को एक और झटका दिया है. पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे एवं वर्तमान में लेखन और पत्रकारिता में सक्रिय बुद्ध शरण हंस ने सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा कर रही है तो यह पूरी तरह से दलित विरोधी षड्यंत्र है. अम्बेडकर छात्रावास स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत एससी/एसटी वेलफेयर के लिए जारी पैसे से बनता है. यह छात्रावास सिर्फ एससी/एसटी छात्रों के लिए होता है. इसमें दूसरे वर्ग के छात्र कैसे रह सकते हैं. बुद्ध शरण हंस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अम्बेडकर हॉस्टल में सीटें खाली रहने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब तो ज्यादा बच्चे आ रहे हैं. मुझे शक है कि कहीं सरकार बाद में यह न कहने लगे कि छात्रावास सिर्फ योग्य एससी छात्रों को ही दिया जाएगा. इसी सरकार ने हाल ही में एससी वर्ग के कर्मचारियों का आरक्षण में प्रोमोशन हटाया है वह भी सबके सामने हैं. नीतीश असल में भाजपा के आदमी हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं. नीतीश और लालू की यह सरकार दलितों का काफी नुकसान कर रही है.
गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में दलित छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा था. हकीकत यह भी है कि विधानसभा चुनाव में दलितों के वोट से ही चुनाव में पिछड़ रहे नीतीश-लालू गठबंधन को जीत मिल पाई थी. लेकिन सरकार आने के बाद से लेकर अब तक सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिससे दलित समाज के छात्रों और कर्मचारियों के हित की अनदेखी हुई है. इससे पहले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दलितों की सीट सवर्णों को दिया जा चुका है. इस पूरे मामले पर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला से उनका पक्ष जानने के लिए उनके नंबर पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. दलित दस्तक द्वारा उन्हें मैसेज भी किया गया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला. झारखण्डः 15 आदिवासी संगठनों ने किया सरकार का विरोध, कहा-जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे
 रांची। झारखण्ड राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर बना, वे तमाम उद्देश्य झारखण्ड वासियों के लिए सपने बन कर रह गए हैं. सरकार विकास के नाम पर सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का अध्यादेश ले आयी है. जमीन लूट की नीति के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते हुए 15 आदिवासी संगठनों ने आदिवासी अस्तित्व और भूमि कानून के मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजन किया. मुंडारी खूंटकटी परिषद, एभन मांझी वैसी पाकुड़, जनाधिकार मंच बोकारो, आदिवासी-मूलवासी अस्तित्व मंच, सोनात संताल समाज, एआईपीएफ इंसाफ और अन्य आदिवासी संगठन भी इस सम्मेलन में शामिल हुए. इस सम्मेलन में काश्तकारी कानून में संशोधन, अधिवास नीति एवं आदिवासी और मूल निवासी समुदायों के बीच संसाधनों का असमान वितरण आदि मुद्दों पर बात की गई.
सम्मेलन में दयामनी बारला ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर सरकार आखिर किसको बेवकूफ बनाना चाहती है. झारखंड का आदिवासी समुदाय अब जाग चुका है. अब उनका एक ही नारा है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे. लड़ेंगे और जीतेंगे. सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन को आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों देने का जरिया बताया. उन्होंने कहा कि एक्ट में संशोधन से झारखण्ड के आदिवासियों का विकास नहीं, विनाश होगा. उन्होंने इसे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व खत्म करने की साजिश बताया. सरकार को याद रखना चाहिए कि झारखंड के किसान खेती और जमीन के बिना नहीं रह सकते हैं.
एक आदिवासी संगठन के सदस्य ओनिल ने कहा कि गांव-गांव में संगठन बना कर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. बिरसाइत समाज के मंगरा ने कहा कि पुरखों ने हमारे अस्तित्व पहचान की विरासत जल, जंगल, जमीन के रूप में दी है, जिसे बेचने नहीं, बल्कि बचाने की जरूरत है. वामपंथी नेता केडी सिंह ने भाजपा सरकार को हाईफाई सरकार बताते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप और बुलेट ट्रेन जैसी घोषणाएं यहां के भोले-भाले आदिवासी-मूलवासियों को भुलावे में डालने वाली हैं. यह सरकार लोगों को आपस में लड़ा कर राज करने और किसानों की जमीन लूटने की साजिश रच रही है.
रांची। झारखण्ड राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर बना, वे तमाम उद्देश्य झारखण्ड वासियों के लिए सपने बन कर रह गए हैं. सरकार विकास के नाम पर सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का अध्यादेश ले आयी है. जमीन लूट की नीति के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते हुए 15 आदिवासी संगठनों ने आदिवासी अस्तित्व और भूमि कानून के मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजन किया. मुंडारी खूंटकटी परिषद, एभन मांझी वैसी पाकुड़, जनाधिकार मंच बोकारो, आदिवासी-मूलवासी अस्तित्व मंच, सोनात संताल समाज, एआईपीएफ इंसाफ और अन्य आदिवासी संगठन भी इस सम्मेलन में शामिल हुए. इस सम्मेलन में काश्तकारी कानून में संशोधन, अधिवास नीति एवं आदिवासी और मूल निवासी समुदायों के बीच संसाधनों का असमान वितरण आदि मुद्दों पर बात की गई.
सम्मेलन में दयामनी बारला ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर सरकार आखिर किसको बेवकूफ बनाना चाहती है. झारखंड का आदिवासी समुदाय अब जाग चुका है. अब उनका एक ही नारा है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे. लड़ेंगे और जीतेंगे. सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन को आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों देने का जरिया बताया. उन्होंने कहा कि एक्ट में संशोधन से झारखण्ड के आदिवासियों का विकास नहीं, विनाश होगा. उन्होंने इसे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व खत्म करने की साजिश बताया. सरकार को याद रखना चाहिए कि झारखंड के किसान खेती और जमीन के बिना नहीं रह सकते हैं.
एक आदिवासी संगठन के सदस्य ओनिल ने कहा कि गांव-गांव में संगठन बना कर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. बिरसाइत समाज के मंगरा ने कहा कि पुरखों ने हमारे अस्तित्व पहचान की विरासत जल, जंगल, जमीन के रूप में दी है, जिसे बेचने नहीं, बल्कि बचाने की जरूरत है. वामपंथी नेता केडी सिंह ने भाजपा सरकार को हाईफाई सरकार बताते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप और बुलेट ट्रेन जैसी घोषणाएं यहां के भोले-भाले आदिवासी-मूलवासियों को भुलावे में डालने वाली हैं. यह सरकार लोगों को आपस में लड़ा कर राज करने और किसानों की जमीन लूटने की साजिश रच रही है. डॉ. अम्बेडकर और मातृत्व अवकाश
 मातृत्व लाभ बिल 2016 को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी. लोकसभा की मंजूरी अभी बाकी है. बिल से सरकारी और निजी क्षेत्रा में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि तमिलनाडू में 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश का प्रावधान पहले से ही है. नये विधेयक के अनुसार मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन भी मिलेगा और तीन हजार रुपये का मातृत्व बोनस भी. 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश सिर्फ दो बच्चों के जन्म तक ही मिलेगा. दो से अधिक बच्चे होने पर अवकाश सिर्फ 12 हफ्ते का ही रहेगा. बच्चे को गोद लेने वाली महिला को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा. महिलाओं को सार्वजनिक मातृत्व अवकाश देने वाला भारत दुनिया का तीसरे नंबर का देश होगा. मातृत्व अवकाश के मामले में भारतीय महिलाओं की स्थिति अमेरिका से काफी बेहतर कही जा सकती है. अमेरिका दुनिया का एक मात्रा ऐसा देश है जहां महिलाओं को मातृत्व के दौरान वेतन नहीं मिलता. यदि अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं म्यांमार में 12 हफ्ते, अफगानिस्तान व इंडोनेशिया में 13 हफ्ते, चीन में 14 हफ्ते, बांग्लादेश व सिंगापुर में 16 हफ्ते, ईरान में 17 हफ्ते और वियतनाम में 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है.
सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा. राज्यसभा में पारित हो चुके इस विधेयक का दायरा उन सभी कंपनियों तक फैला हुआ है जहां 10 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं. अनुमान है कि 18 लाख महिलाएं उक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगी. यह उन सामाजिक संगठनों की जीत है जो लम्बे अर्से से संघर्ष कर रहे थे. क्या निजी संस्थान महिलाओं को मातृत्व अवकाश दे पायेंगे? सच तो यह है कि आरोप-प्रत्यारोप लगा कर ऐसी महिलाओं को पहले ही संस्थान से निकाल देते हैं या फिर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं. जहां नीयत में खोट हो वहां नियम क्या करेगा?
19 जुलाई 1937 में बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर ने बंबई विधानसभा के सदस्य की शपथ लेने के बाद कहा था कि महोदय! प्रेसिडेंसी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंसी में निरक्षरता, मलेरिया, गनोरिया, सिफलिस तथा अन्य बीमारियों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए मुझे यह पूछने का तनिक भी संकोच नहीं है कि क्या सरकार अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभा रही है? उसने मात्र सैंतीस लाख ग्यारह हजार रुपये का बजट पेश किया है. कामकाजी महिलाओं की कवायद करते हुए बाबा साहेब डॉ.आंबेडकर ने कहा कि ‘कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है. यानी वहां वे हालात नहीं हैं जो फैक्टरियों में हैं. जो हालात फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऐसी स्थिति में जच्चा का कुछ समय के लिए प्रसव से पूर्व तथा कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए.
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत महिला प्रसूति लाभ अधिनियम 1941 पर चर्चा करते हुए बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर ने कहा था कि वर्तमान खदान प्रसूति लाभ विधेयक के तहत खदान की एक महिला कर्मचारी 8 हफ्तों का लाभ आठ आना प्रतिदिन की दर से ले सकती है. यह आठ हफ्ते का समय चार-चार हफ्ते के दो भागों में बांटा गया है. पहला भाग प्रसव के पहले और दूसरा प्रसव के बाद. पहले भाग में महिला स्वैच्छिक आराम कर सकती है और चाहे तो निरंतर काम करके पूरा वेतन अर्जित कर सकती है. आराम के लिए काम से गैर हाजिर रहने पर वह प्रसूति लाभ पा सकती है. प्रसूति के बाद का चार हफ्ते का समय आवश्यक आराम का समय है, जिसमें किसी महिला को काम नहीं करना चाहिए. वास्तव में इस अवस्था में उसका काम करना गैर कानूनी और आपराधिक है. उसे केवल प्रसूति लाभ पर ही संतुष्ट होना है. प्रसूति लाभ विधेयक की धारा 5 में प्रसूति लाभ की आदायगी का प्रावधान किया गया है. यदि माननीय सदस्य इस प्रावधान की पंक्ति 9 में काम के संदर्भ में वर्णित शब्दों की ओर ध्यान दे तो पायेंगे कि शब्दावली काम से गैर हाजिर का प्रयोग या फिर काम से शब्द अस्पष्ट है. मैं संक्षेप में स्पष्ट करूंगा कि इनमें क्या अस्पष्टता है? मान लीजिए कि खदान के मालिक ने किसी विशेष दिन खदान बंद कर दी तो क्या उस दिन से महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ पाने का अधिकर है? कहा जाता है कि नहीं. क्योंकि काम से गैरहाजरी शब्दों की जटिलता का यह भी अर्थ निकलता है कि काम तो है किन्तु जब खदान बंद कर दी गई तो काम नहीं.
प्रवर समिति द्वारा जो संशोधन हुआ उस विषय में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर कहते हैं. प्रवर समिति ने जो पहला परिर्वतन किया है कि गर्भवती स्त्री को धरातल के नीचे कार्यों पर भेजे जाने की अवधि संबंधी प्रतिबंध है. मूल विधेयक में प्रसूति से 10 सप्ताह पूर्व ओर प्रसूति से चार सप्ताह बाद तक प्रतिबंध था. प्रवर समिति ने मूल से प्रसूति पूर्व की प्रस्तावित अवधि में परिवर्तन नहीं किया परन्तु प्रसूति उपरांत की अवधि में जो परिवर्तन किए गए हैं वे व्यापक हैं. यह प्रतिबंध अवधि चार सप्ताह से बढ़ा कर छत्तीस सप्ताह कर दी है. धरातल के नीचे कार्य कारने वाली स्त्रियों को प्रसूति लाभ के प्रवर समिति ने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं. मूल विधेयक में धरातल के नीचे कार्य करने वाली स्त्रियों की प्रसूति लाभ की पात्राता की दो शर्तें रखी गई थीं. वे शर्तें थीं प्रसूति से न्यूनतम छह महीने पहले खदान में कार्यरत होना और इन छह महीनों में 90 दिन तक धरातल के नीचे कार्य. प्रवर समिति ने पहली शर्त हटा दी है अर्थात खदान में न्यूनतम छह माह की सेवा ताकि संशोधित विधयेक में बस इतना ही पर्याप्त माना जाए कि स्त्री ने प्रसूति से पूर्व के छह महीना में नब्बे दिन तक तल के नीचे कार्य किया है. उस स्थिति में वह प्रसूति लाभ की पात्र होगी.
प्रवर समिति ने लाभ की अवधि में भी संशोधन किए हैं. मूल विधेयक में प्रसूति लाभ की अवधि प्रसूति से दस सप्ताह पूर्व और प्रसूति उपरांत चार थी. प्रवर समिति ने प्रसूति उपरांत लाभ प्राप्त करने की अवधि चार से बढ़ा कर छह सप्ताह कर दी है. साथ ही लाभ राशि में भी परिवर्तन कर दिया गया है. मूल रूप से लाभ राशि आठ आना प्रतिदिन थी. प्रवर समिति ने इसे बढ़ा कर छह रुपये प्रति सप्ताह कर दिया है. जो चौदह आना प्रतिदिन से कुछ कम है. फिर दूसरी अवधि को अधिकृत छुट्टी घोषित कर दिया गया. ताकि इस काल के दौरान कोई मालिक इस विधेयक के अधीन आने वाली स्त्री को निकाल न सके.
प्रवार समिति ने जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किया है वह लाभ की पात्र स्त्री की मांग पर उसकी डॉक्टरी जांच महिला डॉक्टर से कराई जाएगी. यह प्रावधान मूल विधेयक में नहीं था. मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि नीचे कार्य छत्तीस प्रतिबंधित सप्ताहों के बीच कोई स्त्री बत्तीस सप्ताहों के दौरान धरातल के नीचे कार्य को छोड़कर अपनी आमदनी के लिए अन्य कार्य कर सकती है. यह व्यवस्था मूल विधेयक में नहीं थी.
सरकारी या निजी स्तर की महिला कर्मचारियों ने मातृत्व अवकाश के लिए दावेदारी की पर किसी ने यह नहीं सोचा कि इस विधेयक को प्रस्तुति करने वाला कौन था? यह विधेयक किसी उच्चवर्णीय द्वारा प्रस्तुत किया होता तो वह इस देश में भगवान या देवी बना जाती है. गैर दलित की तो बात ही छोड़िए अधिकांश दलित भी नहीं जानते कि यह विधेयक बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने पहली बार प्रस्तुत किया था. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का मूल्यांकन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप में इतना किया कि सौ से अधिक शीर्षक से हिन्दी बाजार में पुस्तक देखी जा सकती हैं पर स्वास्थ्य के संबंध में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को लेकर कोई किताब नहीं लिखी गई. डॉ. जुगल किशोर ने डॉ. अम्बेडकर और स्वास्थ्य को लेकर आलेख सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका में जरूर लिखा.
मातृत्व लाभ बिल 2016 को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी. लोकसभा की मंजूरी अभी बाकी है. बिल से सरकारी और निजी क्षेत्रा में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि तमिलनाडू में 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश का प्रावधान पहले से ही है. नये विधेयक के अनुसार मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन भी मिलेगा और तीन हजार रुपये का मातृत्व बोनस भी. 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश सिर्फ दो बच्चों के जन्म तक ही मिलेगा. दो से अधिक बच्चे होने पर अवकाश सिर्फ 12 हफ्ते का ही रहेगा. बच्चे को गोद लेने वाली महिला को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा. महिलाओं को सार्वजनिक मातृत्व अवकाश देने वाला भारत दुनिया का तीसरे नंबर का देश होगा. मातृत्व अवकाश के मामले में भारतीय महिलाओं की स्थिति अमेरिका से काफी बेहतर कही जा सकती है. अमेरिका दुनिया का एक मात्रा ऐसा देश है जहां महिलाओं को मातृत्व के दौरान वेतन नहीं मिलता. यदि अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं म्यांमार में 12 हफ्ते, अफगानिस्तान व इंडोनेशिया में 13 हफ्ते, चीन में 14 हफ्ते, बांग्लादेश व सिंगापुर में 16 हफ्ते, ईरान में 17 हफ्ते और वियतनाम में 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है.
सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा. राज्यसभा में पारित हो चुके इस विधेयक का दायरा उन सभी कंपनियों तक फैला हुआ है जहां 10 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं. अनुमान है कि 18 लाख महिलाएं उक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगी. यह उन सामाजिक संगठनों की जीत है जो लम्बे अर्से से संघर्ष कर रहे थे. क्या निजी संस्थान महिलाओं को मातृत्व अवकाश दे पायेंगे? सच तो यह है कि आरोप-प्रत्यारोप लगा कर ऐसी महिलाओं को पहले ही संस्थान से निकाल देते हैं या फिर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं. जहां नीयत में खोट हो वहां नियम क्या करेगा?
19 जुलाई 1937 में बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर ने बंबई विधानसभा के सदस्य की शपथ लेने के बाद कहा था कि महोदय! प्रेसिडेंसी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंसी में निरक्षरता, मलेरिया, गनोरिया, सिफलिस तथा अन्य बीमारियों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए मुझे यह पूछने का तनिक भी संकोच नहीं है कि क्या सरकार अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभा रही है? उसने मात्र सैंतीस लाख ग्यारह हजार रुपये का बजट पेश किया है. कामकाजी महिलाओं की कवायद करते हुए बाबा साहेब डॉ.आंबेडकर ने कहा कि ‘कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है. यानी वहां वे हालात नहीं हैं जो फैक्टरियों में हैं. जो हालात फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऐसी स्थिति में जच्चा का कुछ समय के लिए प्रसव से पूर्व तथा कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए.
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत महिला प्रसूति लाभ अधिनियम 1941 पर चर्चा करते हुए बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर ने कहा था कि वर्तमान खदान प्रसूति लाभ विधेयक के तहत खदान की एक महिला कर्मचारी 8 हफ्तों का लाभ आठ आना प्रतिदिन की दर से ले सकती है. यह आठ हफ्ते का समय चार-चार हफ्ते के दो भागों में बांटा गया है. पहला भाग प्रसव के पहले और दूसरा प्रसव के बाद. पहले भाग में महिला स्वैच्छिक आराम कर सकती है और चाहे तो निरंतर काम करके पूरा वेतन अर्जित कर सकती है. आराम के लिए काम से गैर हाजिर रहने पर वह प्रसूति लाभ पा सकती है. प्रसूति के बाद का चार हफ्ते का समय आवश्यक आराम का समय है, जिसमें किसी महिला को काम नहीं करना चाहिए. वास्तव में इस अवस्था में उसका काम करना गैर कानूनी और आपराधिक है. उसे केवल प्रसूति लाभ पर ही संतुष्ट होना है. प्रसूति लाभ विधेयक की धारा 5 में प्रसूति लाभ की आदायगी का प्रावधान किया गया है. यदि माननीय सदस्य इस प्रावधान की पंक्ति 9 में काम के संदर्भ में वर्णित शब्दों की ओर ध्यान दे तो पायेंगे कि शब्दावली काम से गैर हाजिर का प्रयोग या फिर काम से शब्द अस्पष्ट है. मैं संक्षेप में स्पष्ट करूंगा कि इनमें क्या अस्पष्टता है? मान लीजिए कि खदान के मालिक ने किसी विशेष दिन खदान बंद कर दी तो क्या उस दिन से महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ पाने का अधिकर है? कहा जाता है कि नहीं. क्योंकि काम से गैरहाजरी शब्दों की जटिलता का यह भी अर्थ निकलता है कि काम तो है किन्तु जब खदान बंद कर दी गई तो काम नहीं.
प्रवर समिति द्वारा जो संशोधन हुआ उस विषय में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर कहते हैं. प्रवर समिति ने जो पहला परिर्वतन किया है कि गर्भवती स्त्री को धरातल के नीचे कार्यों पर भेजे जाने की अवधि संबंधी प्रतिबंध है. मूल विधेयक में प्रसूति से 10 सप्ताह पूर्व ओर प्रसूति से चार सप्ताह बाद तक प्रतिबंध था. प्रवर समिति ने मूल से प्रसूति पूर्व की प्रस्तावित अवधि में परिवर्तन नहीं किया परन्तु प्रसूति उपरांत की अवधि में जो परिवर्तन किए गए हैं वे व्यापक हैं. यह प्रतिबंध अवधि चार सप्ताह से बढ़ा कर छत्तीस सप्ताह कर दी है. धरातल के नीचे कार्य कारने वाली स्त्रियों को प्रसूति लाभ के प्रवर समिति ने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं. मूल विधेयक में धरातल के नीचे कार्य करने वाली स्त्रियों की प्रसूति लाभ की पात्राता की दो शर्तें रखी गई थीं. वे शर्तें थीं प्रसूति से न्यूनतम छह महीने पहले खदान में कार्यरत होना और इन छह महीनों में 90 दिन तक धरातल के नीचे कार्य. प्रवर समिति ने पहली शर्त हटा दी है अर्थात खदान में न्यूनतम छह माह की सेवा ताकि संशोधित विधयेक में बस इतना ही पर्याप्त माना जाए कि स्त्री ने प्रसूति से पूर्व के छह महीना में नब्बे दिन तक तल के नीचे कार्य किया है. उस स्थिति में वह प्रसूति लाभ की पात्र होगी.
प्रवर समिति ने लाभ की अवधि में भी संशोधन किए हैं. मूल विधेयक में प्रसूति लाभ की अवधि प्रसूति से दस सप्ताह पूर्व और प्रसूति उपरांत चार थी. प्रवर समिति ने प्रसूति उपरांत लाभ प्राप्त करने की अवधि चार से बढ़ा कर छह सप्ताह कर दी है. साथ ही लाभ राशि में भी परिवर्तन कर दिया गया है. मूल रूप से लाभ राशि आठ आना प्रतिदिन थी. प्रवर समिति ने इसे बढ़ा कर छह रुपये प्रति सप्ताह कर दिया है. जो चौदह आना प्रतिदिन से कुछ कम है. फिर दूसरी अवधि को अधिकृत छुट्टी घोषित कर दिया गया. ताकि इस काल के दौरान कोई मालिक इस विधेयक के अधीन आने वाली स्त्री को निकाल न सके.
प्रवार समिति ने जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किया है वह लाभ की पात्र स्त्री की मांग पर उसकी डॉक्टरी जांच महिला डॉक्टर से कराई जाएगी. यह प्रावधान मूल विधेयक में नहीं था. मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि नीचे कार्य छत्तीस प्रतिबंधित सप्ताहों के बीच कोई स्त्री बत्तीस सप्ताहों के दौरान धरातल के नीचे कार्य को छोड़कर अपनी आमदनी के लिए अन्य कार्य कर सकती है. यह व्यवस्था मूल विधेयक में नहीं थी.
सरकारी या निजी स्तर की महिला कर्मचारियों ने मातृत्व अवकाश के लिए दावेदारी की पर किसी ने यह नहीं सोचा कि इस विधेयक को प्रस्तुति करने वाला कौन था? यह विधेयक किसी उच्चवर्णीय द्वारा प्रस्तुत किया होता तो वह इस देश में भगवान या देवी बना जाती है. गैर दलित की तो बात ही छोड़िए अधिकांश दलित भी नहीं जानते कि यह विधेयक बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने पहली बार प्रस्तुत किया था. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का मूल्यांकन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप में इतना किया कि सौ से अधिक शीर्षक से हिन्दी बाजार में पुस्तक देखी जा सकती हैं पर स्वास्थ्य के संबंध में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को लेकर कोई किताब नहीं लिखी गई. डॉ. जुगल किशोर ने डॉ. अम्बेडकर और स्वास्थ्य को लेकर आलेख सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका में जरूर लिखा.
डॉ. रूपचंद गौत्तम पत्रकार हैं.
यूपीः पुलिस के डर से जंगलों में रात बिता रहे हैं दलित!
 सहारनपुर। पंद्रह अगस्त के बाद से सहारनपुर के उसंद गांव के दलित लोग पास के जंगल में रात गुजार रहे हैं. गांव की दलित महिलाएं रात भर देखा करती हैं कि कहीं पुलिस की जीप तो नहीं आ रही है. पिछले एक हफ्ते में तीन दलितों की पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई. हालांकि पुलिस इस बात से इनकार करती है. गांव वालों का आरोप है कि पुलिस और पीएसी के लोगों ने उनपर लाठियां बरसाईं.
तनाव की स्थिति तब शुरू हुई जब किसी और जाति के एक शख्स ने दलित से कर्ज के बदले इसकी बेटी को अपने घर रखने के लिए कहा. इस बात पर दो समूह जब आमने-सामने आए तो पुलिस को बुलाया गया. पुलिस के अनुसार दंगे जैसी स्थिति को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया. लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस ने केवल दलितों को ही टारगेट किया.
एक ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें जानवरों की तरह पीटा. उन्होंने कहा, हमें बुरी तरह से पीटा गया. गांव के किसी भी दलित का ऐसा घर नहीं बचा जहां पुलिस ने घुसकर तोड़ फोड़ न की हो. कम से कम सौ पुलिस और पीएसी के लोगों ने उपद्रव किया और यह घटना स्वतंत्रता दिवस पर हुई. सरिता देवी, राकेश कुमार और चमन सिंह को बहुत बुरी तरह पीटा गया और उसी रात उन तीनों ने दम तोड़ दिया. वे सभी दलित थे. इन हालात में हम लोगों ने अब जंगल में रात बितानी शुरू कर दी है जबकि घर की महिलाएं रात भर पुलिस को आहट देखती रहती हैं. यहां तक की एंबुलेंस की आवाज सुन कर भी हम डर जाते हैं.
सहारनपुर के एसएसपी मनोज तिवारी ने कहा,”मुझे पता चला है कि दो समूह के लोगों में अनबन हो गई थी. कुछ लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया इसलिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा. हमने 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने के लिए केस दर्ज किया है. हो सकता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग जंगल में सो रहे हैं. जहां तक लोगों के डर का मामला है तो हम गांव जाकर उन्हें आश्वासन देंगे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है.”
सहारनपुर। पंद्रह अगस्त के बाद से सहारनपुर के उसंद गांव के दलित लोग पास के जंगल में रात गुजार रहे हैं. गांव की दलित महिलाएं रात भर देखा करती हैं कि कहीं पुलिस की जीप तो नहीं आ रही है. पिछले एक हफ्ते में तीन दलितों की पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई. हालांकि पुलिस इस बात से इनकार करती है. गांव वालों का आरोप है कि पुलिस और पीएसी के लोगों ने उनपर लाठियां बरसाईं.
तनाव की स्थिति तब शुरू हुई जब किसी और जाति के एक शख्स ने दलित से कर्ज के बदले इसकी बेटी को अपने घर रखने के लिए कहा. इस बात पर दो समूह जब आमने-सामने आए तो पुलिस को बुलाया गया. पुलिस के अनुसार दंगे जैसी स्थिति को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया. लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस ने केवल दलितों को ही टारगेट किया.
एक ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें जानवरों की तरह पीटा. उन्होंने कहा, हमें बुरी तरह से पीटा गया. गांव के किसी भी दलित का ऐसा घर नहीं बचा जहां पुलिस ने घुसकर तोड़ फोड़ न की हो. कम से कम सौ पुलिस और पीएसी के लोगों ने उपद्रव किया और यह घटना स्वतंत्रता दिवस पर हुई. सरिता देवी, राकेश कुमार और चमन सिंह को बहुत बुरी तरह पीटा गया और उसी रात उन तीनों ने दम तोड़ दिया. वे सभी दलित थे. इन हालात में हम लोगों ने अब जंगल में रात बितानी शुरू कर दी है जबकि घर की महिलाएं रात भर पुलिस को आहट देखती रहती हैं. यहां तक की एंबुलेंस की आवाज सुन कर भी हम डर जाते हैं.
सहारनपुर के एसएसपी मनोज तिवारी ने कहा,”मुझे पता चला है कि दो समूह के लोगों में अनबन हो गई थी. कुछ लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया इसलिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा. हमने 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने के लिए केस दर्ज किया है. हो सकता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग जंगल में सो रहे हैं. जहां तक लोगों के डर का मामला है तो हम गांव जाकर उन्हें आश्वासन देंगे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है.” 

