 पंजाब के चुनाव में सिद्धू के कांग्रेस में जाने की चर्चा जोरो पर है जो भाजपा-अकाली और आम आदमी के चुनावी मुद्दे का भी मीडिया में खूब जोर-शोर से प्रचार चल रहा है. लेकिन पंजाब की जिस दलित आबादी के भरोसे वहां की सत्ता का सारा समीकरण टिका हुआ है, मीडिया उसी मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है. पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया दलितों के मुद्दों की ओर से आंखे मूंदे हैं तो वहीं उस आंदोलन का भी जिक्र नहीं कर रही है, जो 29 जनवरी को हुआ.
बीते रविवार यानि 29 जनवरी को संगरूर की अनाज मंडी में हजारों भूमिहीन दलितों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी, लेकिन यह मुद्दा तमाम चैनलों और अखबारों की सुर्खियों से गायब रहा. ये लोग पंजाब में 33 फीसदी पंचायत जमीन में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे. अपने हक के लिए पंजाब के दलित काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं. अपने हक़ की ज़मीन पर कब्ज़ाा लेने की कोशिश करने वाले दलितों को संगरूर जिले के झलूर गांव में अक्टूबर की पांच तारीख को जाट सिक्खों और उनके समर्थित एक अन्यस समूह द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, औरतों पर हमला किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आईं और बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा गया.
यहां भी झलूर कांड के खिलाफ़ 21 अक्टूनबर को एक लंबी प्रतिरोध यात्रा दलितों ने निकाली. इस संघर्ष में दलित गुरदेव कौर की मौत हो गई. उनके समर्थक लाश को लाल झंडे में लपेट कर दो हफ्ते तक चक्का जाम किए रहे पर नतीजा सिफर रहा. लिहाजा आज चुनाव के मौसम में इनके गांव के गांव नोटा का बटन दबाने का फैसला कर चुके हैं.
हालांकि पंजाब का दलित भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है जिससे उसकी ताकत भी बंट जाती है. एक हिस्साि वह है जिसके पास राजनीतिक नुमाइंदगी के रूप में मायावती हैं या फिर जिसे अकाली या अन्यस दलों की सरपरस्तीत हासिल है. दूसरा तबका वह है जो इनमें से किसी को अपना तारणहार नहीं मानता. वह हक़ की बात करता है. हक़ उस 33 फीसदी पंचायती ज़मीन पर, जो 1961 के पंजाब जमीन नियमन कानून में उसे मिला था, लेकिन आज तक असलियत में नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि मायावती ज़मीन के प्रश्न को नज़रंदाज करती हैं. 30 जनवरी को फगवाड़ा की अनाज मंडी में उन्होंाने ज़मीन का सवाल तो उठाया, हालांकि इतना ही कहा कि दलितों को उनका वाजिब हक तभी मिल पाएगा जब \””पंजाब में मेरी सरकार आएगी.\””
इस बात की संभावना है कि 11 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में आई नई सरकार को सबसे पहले इसी सवाल से जूझना पड़ेगा, क्योंंकि अप्रैल से 33 फीसदी पंचायती ज़मीन की नई बोली लगने वाली है.
पंजाब के चुनाव में सिद्धू के कांग्रेस में जाने की चर्चा जोरो पर है जो भाजपा-अकाली और आम आदमी के चुनावी मुद्दे का भी मीडिया में खूब जोर-शोर से प्रचार चल रहा है. लेकिन पंजाब की जिस दलित आबादी के भरोसे वहां की सत्ता का सारा समीकरण टिका हुआ है, मीडिया उसी मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है. पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया दलितों के मुद्दों की ओर से आंखे मूंदे हैं तो वहीं उस आंदोलन का भी जिक्र नहीं कर रही है, जो 29 जनवरी को हुआ.
बीते रविवार यानि 29 जनवरी को संगरूर की अनाज मंडी में हजारों भूमिहीन दलितों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी, लेकिन यह मुद्दा तमाम चैनलों और अखबारों की सुर्खियों से गायब रहा. ये लोग पंजाब में 33 फीसदी पंचायत जमीन में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे. अपने हक के लिए पंजाब के दलित काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं. अपने हक़ की ज़मीन पर कब्ज़ाा लेने की कोशिश करने वाले दलितों को संगरूर जिले के झलूर गांव में अक्टूबर की पांच तारीख को जाट सिक्खों और उनके समर्थित एक अन्यस समूह द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, औरतों पर हमला किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आईं और बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा गया.
यहां भी झलूर कांड के खिलाफ़ 21 अक्टूनबर को एक लंबी प्रतिरोध यात्रा दलितों ने निकाली. इस संघर्ष में दलित गुरदेव कौर की मौत हो गई. उनके समर्थक लाश को लाल झंडे में लपेट कर दो हफ्ते तक चक्का जाम किए रहे पर नतीजा सिफर रहा. लिहाजा आज चुनाव के मौसम में इनके गांव के गांव नोटा का बटन दबाने का फैसला कर चुके हैं.
हालांकि पंजाब का दलित भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है जिससे उसकी ताकत भी बंट जाती है. एक हिस्साि वह है जिसके पास राजनीतिक नुमाइंदगी के रूप में मायावती हैं या फिर जिसे अकाली या अन्यस दलों की सरपरस्तीत हासिल है. दूसरा तबका वह है जो इनमें से किसी को अपना तारणहार नहीं मानता. वह हक़ की बात करता है. हक़ उस 33 फीसदी पंचायती ज़मीन पर, जो 1961 के पंजाब जमीन नियमन कानून में उसे मिला था, लेकिन आज तक असलियत में नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि मायावती ज़मीन के प्रश्न को नज़रंदाज करती हैं. 30 जनवरी को फगवाड़ा की अनाज मंडी में उन्होंाने ज़मीन का सवाल तो उठाया, हालांकि इतना ही कहा कि दलितों को उनका वाजिब हक तभी मिल पाएगा जब \””पंजाब में मेरी सरकार आएगी.\””
इस बात की संभावना है कि 11 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में आई नई सरकार को सबसे पहले इसी सवाल से जूझना पड़ेगा, क्योंंकि अप्रैल से 33 फीसदी पंचायती ज़मीन की नई बोली लगने वाली है. पंजाब के दलितों के सवालों को दबा रहा है मीडिया
 पंजाब के चुनाव में सिद्धू के कांग्रेस में जाने की चर्चा जोरो पर है जो भाजपा-अकाली और आम आदमी के चुनावी मुद्दे का भी मीडिया में खूब जोर-शोर से प्रचार चल रहा है. लेकिन पंजाब की जिस दलित आबादी के भरोसे वहां की सत्ता का सारा समीकरण टिका हुआ है, मीडिया उसी मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है. पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया दलितों के मुद्दों की ओर से आंखे मूंदे हैं तो वहीं उस आंदोलन का भी जिक्र नहीं कर रही है, जो 29 जनवरी को हुआ.
बीते रविवार यानि 29 जनवरी को संगरूर की अनाज मंडी में हजारों भूमिहीन दलितों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी, लेकिन यह मुद्दा तमाम चैनलों और अखबारों की सुर्खियों से गायब रहा. ये लोग पंजाब में 33 फीसदी पंचायत जमीन में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे. अपने हक के लिए पंजाब के दलित काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं. अपने हक़ की ज़मीन पर कब्ज़ाा लेने की कोशिश करने वाले दलितों को संगरूर जिले के झलूर गांव में अक्टूबर की पांच तारीख को जाट सिक्खों और उनके समर्थित एक अन्यस समूह द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, औरतों पर हमला किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आईं और बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा गया.
यहां भी झलूर कांड के खिलाफ़ 21 अक्टूनबर को एक लंबी प्रतिरोध यात्रा दलितों ने निकाली. इस संघर्ष में दलित गुरदेव कौर की मौत हो गई. उनके समर्थक लाश को लाल झंडे में लपेट कर दो हफ्ते तक चक्का जाम किए रहे पर नतीजा सिफर रहा. लिहाजा आज चुनाव के मौसम में इनके गांव के गांव नोटा का बटन दबाने का फैसला कर चुके हैं.
हालांकि पंजाब का दलित भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है जिससे उसकी ताकत भी बंट जाती है. एक हिस्साि वह है जिसके पास राजनीतिक नुमाइंदगी के रूप में मायावती हैं या फिर जिसे अकाली या अन्यस दलों की सरपरस्तीत हासिल है. दूसरा तबका वह है जो इनमें से किसी को अपना तारणहार नहीं मानता. वह हक़ की बात करता है. हक़ उस 33 फीसदी पंचायती ज़मीन पर, जो 1961 के पंजाब जमीन नियमन कानून में उसे मिला था, लेकिन आज तक असलियत में नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि मायावती ज़मीन के प्रश्न को नज़रंदाज करती हैं. 30 जनवरी को फगवाड़ा की अनाज मंडी में उन्होंाने ज़मीन का सवाल तो उठाया, हालांकि इतना ही कहा कि दलितों को उनका वाजिब हक तभी मिल पाएगा जब \””पंजाब में मेरी सरकार आएगी.\””
इस बात की संभावना है कि 11 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में आई नई सरकार को सबसे पहले इसी सवाल से जूझना पड़ेगा, क्योंंकि अप्रैल से 33 फीसदी पंचायती ज़मीन की नई बोली लगने वाली है.
पंजाब के चुनाव में सिद्धू के कांग्रेस में जाने की चर्चा जोरो पर है जो भाजपा-अकाली और आम आदमी के चुनावी मुद्दे का भी मीडिया में खूब जोर-शोर से प्रचार चल रहा है. लेकिन पंजाब की जिस दलित आबादी के भरोसे वहां की सत्ता का सारा समीकरण टिका हुआ है, मीडिया उसी मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है. पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया दलितों के मुद्दों की ओर से आंखे मूंदे हैं तो वहीं उस आंदोलन का भी जिक्र नहीं कर रही है, जो 29 जनवरी को हुआ.
बीते रविवार यानि 29 जनवरी को संगरूर की अनाज मंडी में हजारों भूमिहीन दलितों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी, लेकिन यह मुद्दा तमाम चैनलों और अखबारों की सुर्खियों से गायब रहा. ये लोग पंजाब में 33 फीसदी पंचायत जमीन में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे. अपने हक के लिए पंजाब के दलित काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं. अपने हक़ की ज़मीन पर कब्ज़ाा लेने की कोशिश करने वाले दलितों को संगरूर जिले के झलूर गांव में अक्टूबर की पांच तारीख को जाट सिक्खों और उनके समर्थित एक अन्यस समूह द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, औरतों पर हमला किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आईं और बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा गया.
यहां भी झलूर कांड के खिलाफ़ 21 अक्टूनबर को एक लंबी प्रतिरोध यात्रा दलितों ने निकाली. इस संघर्ष में दलित गुरदेव कौर की मौत हो गई. उनके समर्थक लाश को लाल झंडे में लपेट कर दो हफ्ते तक चक्का जाम किए रहे पर नतीजा सिफर रहा. लिहाजा आज चुनाव के मौसम में इनके गांव के गांव नोटा का बटन दबाने का फैसला कर चुके हैं.
हालांकि पंजाब का दलित भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है जिससे उसकी ताकत भी बंट जाती है. एक हिस्साि वह है जिसके पास राजनीतिक नुमाइंदगी के रूप में मायावती हैं या फिर जिसे अकाली या अन्यस दलों की सरपरस्तीत हासिल है. दूसरा तबका वह है जो इनमें से किसी को अपना तारणहार नहीं मानता. वह हक़ की बात करता है. हक़ उस 33 फीसदी पंचायती ज़मीन पर, जो 1961 के पंजाब जमीन नियमन कानून में उसे मिला था, लेकिन आज तक असलियत में नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि मायावती ज़मीन के प्रश्न को नज़रंदाज करती हैं. 30 जनवरी को फगवाड़ा की अनाज मंडी में उन्होंाने ज़मीन का सवाल तो उठाया, हालांकि इतना ही कहा कि दलितों को उनका वाजिब हक तभी मिल पाएगा जब \””पंजाब में मेरी सरकार आएगी.\””
इस बात की संभावना है कि 11 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में आई नई सरकार को सबसे पहले इसी सवाल से जूझना पड़ेगा, क्योंंकि अप्रैल से 33 फीसदी पंचायती ज़मीन की नई बोली लगने वाली है. आदिवासी संगठनों ने किया आरएसएस के हिन्दू सम्मेलन का बहिष्कार
 मध्यप्रदेश। प्रदेश में आदिवासी संगठन आरएसएस के विरोध में खड़े हो गए हैं. आदिवासी संगठनों ने आरएसएस द्वारा आयोजित हिन्दू सम्मेलन के विरोध पर उतर गए हैं. साथ ही प्रदेश के आदिवासियों से अपील कर उन्हें इस हिन्दू सम्मेलन में शामिल नहीं होने की अपील की है. राजधानी भोपाल में यह सम्मेलन आठ फरवरी को आयोजित होना है.
प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी संगठनों ने विरोध कर जिले के आदिवासियों से हिन्दू सम्मलेन में शामिल नहीं होने की अपील की है. इस अपील के बाद से संगठनों ने आदिवासी समाज में अपील जारी की है कि कोई भी हिन्दू सम्मेलन में न जाए. इस सम्मेलन में आरएसएस के सर संघ संचालक मोहन भागवत को बैतूल पहुंचना है. जिसके लिए भीड़ जुटाने में सत्ता और संगठन को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है. लेकिन आदिवासियों के ताजा फैसले से आरएसएस को बड़ा झटका लग सकता है. यही नहीं संगठनों ने आदिवासियों की घर वापसी अभियान भी चलाने का फैसला किया है.
आदिवासी संगठनों का कहना है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं इसलिए उन्हें सम्मेलन में न जाने के लिए समझाया जा रहा है. बैतूल में आयोजित आदिवासी संगठन की एक बैठक में साफ एलान किया गया है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं, इसलिए वे आठ फरवरी को आयोजित हिन्दू सम्मेलन का हिस्सा न बनें. इसके लिए गांव-गांव फरमान भी जारी कर दिया है. समाज के युवा भी मानते हैं कि उनके रीति-रिवाज और संस्कृति हिन्दू समाज से भिन्न है. उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आदिवासी हिन्दू नही हैं. इसलिए वे सम्मेलन में नही जायेंगे. आदिवासी समाज के इस फैसले से हिन्दू सम्मलेन को लेकर आरएसएस की योजना खटाई में पड़ सकती है. बताते चलें कि बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है.
मध्यप्रदेश। प्रदेश में आदिवासी संगठन आरएसएस के विरोध में खड़े हो गए हैं. आदिवासी संगठनों ने आरएसएस द्वारा आयोजित हिन्दू सम्मेलन के विरोध पर उतर गए हैं. साथ ही प्रदेश के आदिवासियों से अपील कर उन्हें इस हिन्दू सम्मेलन में शामिल नहीं होने की अपील की है. राजधानी भोपाल में यह सम्मेलन आठ फरवरी को आयोजित होना है.
प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी संगठनों ने विरोध कर जिले के आदिवासियों से हिन्दू सम्मलेन में शामिल नहीं होने की अपील की है. इस अपील के बाद से संगठनों ने आदिवासी समाज में अपील जारी की है कि कोई भी हिन्दू सम्मेलन में न जाए. इस सम्मेलन में आरएसएस के सर संघ संचालक मोहन भागवत को बैतूल पहुंचना है. जिसके लिए भीड़ जुटाने में सत्ता और संगठन को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है. लेकिन आदिवासियों के ताजा फैसले से आरएसएस को बड़ा झटका लग सकता है. यही नहीं संगठनों ने आदिवासियों की घर वापसी अभियान भी चलाने का फैसला किया है.
आदिवासी संगठनों का कहना है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं इसलिए उन्हें सम्मेलन में न जाने के लिए समझाया जा रहा है. बैतूल में आयोजित आदिवासी संगठन की एक बैठक में साफ एलान किया गया है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं, इसलिए वे आठ फरवरी को आयोजित हिन्दू सम्मेलन का हिस्सा न बनें. इसके लिए गांव-गांव फरमान भी जारी कर दिया है. समाज के युवा भी मानते हैं कि उनके रीति-रिवाज और संस्कृति हिन्दू समाज से भिन्न है. उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आदिवासी हिन्दू नही हैं. इसलिए वे सम्मेलन में नही जायेंगे. आदिवासी समाज के इस फैसले से हिन्दू सम्मलेन को लेकर आरएसएस की योजना खटाई में पड़ सकती है. बताते चलें कि बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है. नोटबंदी से बदहाल किसान को बजट से आश
 भारत एक कृषि प्रधान देश है. इसके चलते यहां की अर्थव्यवस्था का आधार भी खेती-किसानी है. आज भी गांव व शहर की आबादी को मिला कर अस्सी फीसदी तक लोग खेती-किसानी के काम में जुटे है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार जो भी काम करेगी या निर्णय लेगी इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रख कर ही लेगी, लेकिन मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय इस पूरी आबादी को नजर अंदाज कर दिया. हालात ये बने कि देश का तमाम किसान दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया. नोटबंदी को लेकर जैसे-जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी सच्चाई सामने आती जा रही है. नोटबंदी के चलते आम नागरिकों ने जो नरक भोगा है उसका जिक्र करना तो यहां लाजिमी नहीं लगता है लेकिन किसानों ने जो भोगा है उस पर काफी कम चर्चा हुई है.
फिलहाल हम नोटबंदी से किसान को होने वाले नुकसान और परेशानी पर बात करते है. नोटबंदी को लेकर हाल ही में देश के किसान नेताओं का एक आंकलन सामने आया है. यह आंकलन बताता है कि इसके चलते हर किसान को एक एकड़ के पीछे करीब पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ है. कृषि संगठनों से जुड़े नेताओं का ये भी मानना है कि फल और सब्जी उपजाने वाले किसानों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने हाल ही में अपने बयान में ये कहा है कि ज्यादातर किसान फल और सब्जियां बोते हैं नोटबंदी के कारण उन्हें औसतन 20 से 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का नुकसान झेलना पड़ा है. यह नुकसान बहुत ज्यादा है. किसान जागृति मंच के अध्यक्ष सुधीर पंवार की माने तो नोटबंदी ने तो किसानों की कमर ही तोडकर रख दी है. किसानों की हालत बहुत खराब है. किसानों को उम्मीद है कि एक फरवरी को आम बजट में उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी के चलते कृषि क्षेत्र पर तगड़ी मार पड़ी है और वह अभी तक इससे उबर नहीं पाया है. इस परेशानी के चलते ही अब किसानों से जुड़े संगठन और उनके नेता नुकसान की भरपाई बजट में विशेष योजना बना कर करने की मांग कर रहे. सभी किसान नेता एक सुर में ये बात दोहरा रहे है कि मोदी सरकार को किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष योजना का ऐलान करना चाहिए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके.
काबिलेगौर हो कि नोटबंदी के समय देश के अनेक राज्यों से ये खबरें भी आ रही थी कि किसानों को उसकी उपज का सही भाव नहीं मिलने के कारण फसल को ओने-पौने दाम में बेचना पड़ रहा है. खबरें तो ये भी सामने आई थी कि किसानों ने सब्जियों को फ्री में बांट दी या फिर सडक़ों पर फेक दी. जब किसान अपनी उपज को बाजार में ले जाता है और वह नहीं बिकती है या कीमत कम मिलती है तो वह उसे फेंकने के सिवाय क्या कर पाएगा. उसके पास दो ही रास्ते हैं या तो मामूली कीमत पर उपज बेचे या फेंके. नोटबंदी के दौरान आलम यह था कि मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में किसानों को आलू सडक़ों पर फैकने पड़े. किसानों को छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में टमाटर और मटर सहित दूसरी सब्जियों को सडक़ों पर फेंकना पड़ा. हालाकि इस स्थिति के निर्मित होने का खास कारण कृषकों की फसल खरीदने वाले व्यापारियों के पास नगदी का अभाव रहा है. व्यापारियों की भी एक ही पीड़ा थी कि उनके पास उपज को खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे. चेक भी काम नहीं आ रहे थे, बैंकों में भी नगदी का खासा अभाव जो था.
सच पूछो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया आर्थिक तंत्र (कैशलेस) का प्रस्ताव रखा उसे किसान अपना ही नहीं पा रहे हैं. नतीजा सामने है. फसल की कीमतें जमीन पर आ रही है और किसान मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. अब तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जब किसान को बुवाई की लागत के बराबर भी पैसा नहीं मिलेगा तो वह खेती कैसे करेगा. गौरतलब हो कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले से रबी की बुवाई पर भी गहरा असर पड़ा है. हालांकि सरकार का कहना है कि इस साल रबी की बुवाई बढ़ी है. सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि किसानों पर इसका विपरित प्रभाव पड़ा है. बहरहाल इस साल रबी की बुवाई बढऩे का जो दावा सरकार कर रही है वह पिछले साल से तुलना के चलते ही कर रही है, जबकि पिछले साल सूखा पड़ा था और इसके चलते बुवाई कम हुई थी. असल में सरकार रबी की बुवाई बढऩे का आंकड़ा बताकर अप्रत्यक्ष रूप से यह जताना चाहती है कि बुवाई के लिए पैसों की जरुरत नहीं है.
खैर नोटबंदी ने सहकारी बैंकों के माध्यम से भी किसानों की कमर तोडऩे का काम किया है. नोटबंदी ने सहकारी बैंकों को अपने मकडज़ाल में फंसा कर किसानों की परेशानी बढ़ाई. यह सर्वविदित है कि किसानों का अधिकतर लेन -देन सहकारी बैंकों से होता है. किसानों के पचास फीसद से ज्यादा खाते इन्हीं बैंकों में होते है. इन बैंकों से वे एक ओर कृषि-कार्य के लिए कर्ज लेते हैं तो दूसरी तरफ अपनी बचत भी जमा कराते हैं. हजारों किसानों का मानना है कि मोदी सरकार ने हजार और पांच सौ के नोटबंद करके न केवल सहकारी बैंकों को तबाह किया बल्कि किसान को भी मरने के लिए मजबूर कर दिया. यह एक सच है कि किसानों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के मकसद से शुरू किए गए सहकारी बैंकों की देश के ग्रामीण इलाकों में दूर-दूर तक पहुंच है. दूरदराज तक जहां सरकारी और व्यावसायिक बैंकों की मौजूदगी नहीं होती है वहां सहकारी बैंकों ने लोगों को वित्तीय सहारा देने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार ने इन बैंकों को ही लेनदेन से दूर कर दिया.
दरअसल, सहकारी बैंकों को भी हजार और पांच सौ के पुराने नोट बदलने की प्रक्रिया में शामिल किया गया होता तो हालात शायद इतने बुरे नहीं होते. हालाकि सरकार ने सहकारी बैंकों को नोटों की अदलाबदली से अलग रखा तो कोई हर्ज नहीं, पर किसानों को संकट से बचाने की उसके पास क्या योजना थी? नोटबंदी के फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा हाल रहा. ग्रामीण इलाकों में कई किलोमीटर जाने पर किसी बैंक शाखा या एटीएम के दर्शन होते हैं, पर नोटबंदी के समय वहां नगदी के दर्शन नहीं हो रहे थे. रबी की बुआई के समय किसानों ने पुराने नोट बदलने की गुहार सहाकरी बैंकों में लगाई लेकिन उनको वहां निराशा का ही सामना करना पड़ा. किसान जिन सहकारी बैंकों से फरियाद कर रहे थे उनसे मोदी सरकार ने फरियाद सुनने तक का हक ही छीन लिया था.
इस तरह के माहौल में किसान ने कैसे खुद को संभाला, परेशानी होने पर उसका कैसे सामना किया ये सवाल आज भी प्रासंगिक है. उस समय किसान पर क्या बीती होगी?संकट में काम न आने पर क्या अब सहकारी बैंक अपने ग्राहकों का भरोसा कायम रख पाएंगे? क्या इस नोटबंदी से सरकार ने सहकारी बैंकों को अनुपयोगी मान कर उनकी विदाई का फैसला भी कर लिया था. असल में नोटबंदी से न केवल खेती-किसानी बल्कि दूसरे कामों जैसे कारीगर, मकान निर्माण मजूदर पर भी विपरीत असर पड़ा है. यह जीडीपी का 45 प्रतिशत है और 80 प्रतिशत रोजगार इसी से आता है. यह सही बात है कि इस सेक्टर से टैक्स नहीं जाता लेकिन यहां से रोजगार मिलता है. नोटबंदी के चलते यह लगभग रूक गया है. हालांकि नकदी की स्थिति सुधर रही है लेकिन युवाओं की नौकरियों और किसान की बदहाली पर समस्या और सवाल बरकरार है. अब किसान को नोटबंदी से होने वाले नुकसान की भरपाई की बजट से है.
– लेखक मीडिय़ा रिलेशन पत्रिका के संपादक हैं. सम-सामयिक विषयों पर भी लिखते रहते हैं. संपर्क 9827277518
भारत एक कृषि प्रधान देश है. इसके चलते यहां की अर्थव्यवस्था का आधार भी खेती-किसानी है. आज भी गांव व शहर की आबादी को मिला कर अस्सी फीसदी तक लोग खेती-किसानी के काम में जुटे है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार जो भी काम करेगी या निर्णय लेगी इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रख कर ही लेगी, लेकिन मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय इस पूरी आबादी को नजर अंदाज कर दिया. हालात ये बने कि देश का तमाम किसान दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया. नोटबंदी को लेकर जैसे-जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी सच्चाई सामने आती जा रही है. नोटबंदी के चलते आम नागरिकों ने जो नरक भोगा है उसका जिक्र करना तो यहां लाजिमी नहीं लगता है लेकिन किसानों ने जो भोगा है उस पर काफी कम चर्चा हुई है.
फिलहाल हम नोटबंदी से किसान को होने वाले नुकसान और परेशानी पर बात करते है. नोटबंदी को लेकर हाल ही में देश के किसान नेताओं का एक आंकलन सामने आया है. यह आंकलन बताता है कि इसके चलते हर किसान को एक एकड़ के पीछे करीब पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ है. कृषि संगठनों से जुड़े नेताओं का ये भी मानना है कि फल और सब्जी उपजाने वाले किसानों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने हाल ही में अपने बयान में ये कहा है कि ज्यादातर किसान फल और सब्जियां बोते हैं नोटबंदी के कारण उन्हें औसतन 20 से 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का नुकसान झेलना पड़ा है. यह नुकसान बहुत ज्यादा है. किसान जागृति मंच के अध्यक्ष सुधीर पंवार की माने तो नोटबंदी ने तो किसानों की कमर ही तोडकर रख दी है. किसानों की हालत बहुत खराब है. किसानों को उम्मीद है कि एक फरवरी को आम बजट में उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी के चलते कृषि क्षेत्र पर तगड़ी मार पड़ी है और वह अभी तक इससे उबर नहीं पाया है. इस परेशानी के चलते ही अब किसानों से जुड़े संगठन और उनके नेता नुकसान की भरपाई बजट में विशेष योजना बना कर करने की मांग कर रहे. सभी किसान नेता एक सुर में ये बात दोहरा रहे है कि मोदी सरकार को किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष योजना का ऐलान करना चाहिए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके.
काबिलेगौर हो कि नोटबंदी के समय देश के अनेक राज्यों से ये खबरें भी आ रही थी कि किसानों को उसकी उपज का सही भाव नहीं मिलने के कारण फसल को ओने-पौने दाम में बेचना पड़ रहा है. खबरें तो ये भी सामने आई थी कि किसानों ने सब्जियों को फ्री में बांट दी या फिर सडक़ों पर फेक दी. जब किसान अपनी उपज को बाजार में ले जाता है और वह नहीं बिकती है या कीमत कम मिलती है तो वह उसे फेंकने के सिवाय क्या कर पाएगा. उसके पास दो ही रास्ते हैं या तो मामूली कीमत पर उपज बेचे या फेंके. नोटबंदी के दौरान आलम यह था कि मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में किसानों को आलू सडक़ों पर फैकने पड़े. किसानों को छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में टमाटर और मटर सहित दूसरी सब्जियों को सडक़ों पर फेंकना पड़ा. हालाकि इस स्थिति के निर्मित होने का खास कारण कृषकों की फसल खरीदने वाले व्यापारियों के पास नगदी का अभाव रहा है. व्यापारियों की भी एक ही पीड़ा थी कि उनके पास उपज को खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे. चेक भी काम नहीं आ रहे थे, बैंकों में भी नगदी का खासा अभाव जो था.
सच पूछो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया आर्थिक तंत्र (कैशलेस) का प्रस्ताव रखा उसे किसान अपना ही नहीं पा रहे हैं. नतीजा सामने है. फसल की कीमतें जमीन पर आ रही है और किसान मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. अब तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जब किसान को बुवाई की लागत के बराबर भी पैसा नहीं मिलेगा तो वह खेती कैसे करेगा. गौरतलब हो कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले से रबी की बुवाई पर भी गहरा असर पड़ा है. हालांकि सरकार का कहना है कि इस साल रबी की बुवाई बढ़ी है. सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि किसानों पर इसका विपरित प्रभाव पड़ा है. बहरहाल इस साल रबी की बुवाई बढऩे का जो दावा सरकार कर रही है वह पिछले साल से तुलना के चलते ही कर रही है, जबकि पिछले साल सूखा पड़ा था और इसके चलते बुवाई कम हुई थी. असल में सरकार रबी की बुवाई बढऩे का आंकड़ा बताकर अप्रत्यक्ष रूप से यह जताना चाहती है कि बुवाई के लिए पैसों की जरुरत नहीं है.
खैर नोटबंदी ने सहकारी बैंकों के माध्यम से भी किसानों की कमर तोडऩे का काम किया है. नोटबंदी ने सहकारी बैंकों को अपने मकडज़ाल में फंसा कर किसानों की परेशानी बढ़ाई. यह सर्वविदित है कि किसानों का अधिकतर लेन -देन सहकारी बैंकों से होता है. किसानों के पचास फीसद से ज्यादा खाते इन्हीं बैंकों में होते है. इन बैंकों से वे एक ओर कृषि-कार्य के लिए कर्ज लेते हैं तो दूसरी तरफ अपनी बचत भी जमा कराते हैं. हजारों किसानों का मानना है कि मोदी सरकार ने हजार और पांच सौ के नोटबंद करके न केवल सहकारी बैंकों को तबाह किया बल्कि किसान को भी मरने के लिए मजबूर कर दिया. यह एक सच है कि किसानों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के मकसद से शुरू किए गए सहकारी बैंकों की देश के ग्रामीण इलाकों में दूर-दूर तक पहुंच है. दूरदराज तक जहां सरकारी और व्यावसायिक बैंकों की मौजूदगी नहीं होती है वहां सहकारी बैंकों ने लोगों को वित्तीय सहारा देने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार ने इन बैंकों को ही लेनदेन से दूर कर दिया.
दरअसल, सहकारी बैंकों को भी हजार और पांच सौ के पुराने नोट बदलने की प्रक्रिया में शामिल किया गया होता तो हालात शायद इतने बुरे नहीं होते. हालाकि सरकार ने सहकारी बैंकों को नोटों की अदलाबदली से अलग रखा तो कोई हर्ज नहीं, पर किसानों को संकट से बचाने की उसके पास क्या योजना थी? नोटबंदी के फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा हाल रहा. ग्रामीण इलाकों में कई किलोमीटर जाने पर किसी बैंक शाखा या एटीएम के दर्शन होते हैं, पर नोटबंदी के समय वहां नगदी के दर्शन नहीं हो रहे थे. रबी की बुआई के समय किसानों ने पुराने नोट बदलने की गुहार सहाकरी बैंकों में लगाई लेकिन उनको वहां निराशा का ही सामना करना पड़ा. किसान जिन सहकारी बैंकों से फरियाद कर रहे थे उनसे मोदी सरकार ने फरियाद सुनने तक का हक ही छीन लिया था.
इस तरह के माहौल में किसान ने कैसे खुद को संभाला, परेशानी होने पर उसका कैसे सामना किया ये सवाल आज भी प्रासंगिक है. उस समय किसान पर क्या बीती होगी?संकट में काम न आने पर क्या अब सहकारी बैंक अपने ग्राहकों का भरोसा कायम रख पाएंगे? क्या इस नोटबंदी से सरकार ने सहकारी बैंकों को अनुपयोगी मान कर उनकी विदाई का फैसला भी कर लिया था. असल में नोटबंदी से न केवल खेती-किसानी बल्कि दूसरे कामों जैसे कारीगर, मकान निर्माण मजूदर पर भी विपरीत असर पड़ा है. यह जीडीपी का 45 प्रतिशत है और 80 प्रतिशत रोजगार इसी से आता है. यह सही बात है कि इस सेक्टर से टैक्स नहीं जाता लेकिन यहां से रोजगार मिलता है. नोटबंदी के चलते यह लगभग रूक गया है. हालांकि नकदी की स्थिति सुधर रही है लेकिन युवाओं की नौकरियों और किसान की बदहाली पर समस्या और सवाल बरकरार है. अब किसान को नोटबंदी से होने वाले नुकसान की भरपाई की बजट से है.
– लेखक मीडिय़ा रिलेशन पत्रिका के संपादक हैं. सम-सामयिक विषयों पर भी लिखते रहते हैं. संपर्क 9827277518
26 जनवरी को डा. अम्बेडकर को सम्मान क्यों नहीं?
 तकरीबन ढाई दशक पहले आरपीआई के एक नेता ने संसद में यह प्रश्न उठाया था कि जिस तरह 15 अगस्त से पहले लाल किले पर झंडोत्तोलन के लिए जाते वक्त प्रधानमंत्री राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, उसी तरह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति इंडिया गेट पर जाने से पहले संसद भवन स्थित संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर को याद क्यों नहीं करती? सवाल सीधा और सपाट था सो सरकार ने भी इसका सीधा सा जवाब दे दिया. सरकार का कहना था कि इस मौके पर किसी भी राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, इसलिए डा. अम्बेडकर को भी सम्मानित नहीं किया जाता है.
जवाब आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया. इस बीच रतनलाल केन नाम के एक व्यक्ति इसके लिए लड़ते रहे, हर साल राष्ट्रपति को चिठ्ठी लिखते रहे. आरटीआई ने अब इन्हें नया हथियार दे दिया था और उनकी लड़ाई भी धारदार हो गई. लेकिन जब जवाब सरकार से मांगना हो और वह ना देना चाहे तो कोई सूचना का अधिकार भी कुछ नहीं कर सकता. खासतौर पर भारत जैसे देश में. सवाल है कि प्रधानमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के पहले जब इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है तो अपने कर्मवीरों और राष्ट्रनेताओं को जिन्होंने देश को संविधान दिया उनको क्यों भूल जाते हैं?
हालांकि आरटीआई के माध्यम से केन ने कई नई चीजें निकाली हैं, जो चौंकाने वाली है. रतनलाल के अपने तर्क हैं. अपनी मुहिम को जारी रखते हुए केन ने 13 दिसंबर 2011 को महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिख कर उनसे इस मामले में एनओसी की मांग की है. केन का कहना है कि हमें एनओसी दिया जाए कि सरकार हमारे इस मामले को सुलझाने में असफल रही है, ताकि हम इसे यूएनओ में उठा सके. हालांकि 13 दिसंबर के इस पत्र के इंतजार में वह अब तक हैं. जाहिर है उन्हें इसका जवाब नहीं मिला है. संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के बारे में सरकार के दृष्टिकोण का एक चौंकाने वाला यह पहलू भी सामने आया है कि सरकार डा. अम्बेडकर को जहां स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती, वहीं उनके संविधान निर्माता होने के सवाल पर चुप्पी साध लेती है. आरटीआई के माध्यम से केन ने गृह मंत्रालय से यह सवाल किया कि क्या डा. अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी हैं? या फिर क्या वह संविधान निर्माता हैं? तो गृह मंत्रालय के डीओपीटी से जवाब आया कि डा. अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानियों के वर्ग में नहीं आतें, तो वहीं संविधान निर्माता मानने के बारे में उसने चुप्पी साध ली.
गांधी और अम्बेडकर के बीच आजादी के समय से ही उभरे मतभेद यहां भी साफ दिखाई देते हैं. यहीं से एक सवाल यह भी उठता है कि फिर महात्मा गांधी जी को किस नीति और नियम के तहत राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई. गड़बड़झाला की सूचना यहां भी है. केन द्वारा गृह मंत्रालय से महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता होने के संबंध में जानकारी मांगने पर 2002 में तात्कालिन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जवाब दिया कि जैसे दूसरे लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे मैं भी कहता हूं लेकिन गृह मंत्रालय के रिकार्ड के मुताबिक आज तक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करने का कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. ना ही संविधान में ऐसा कोई अलंकरण देने की व्यवस्था है. सरकार किसी को ऐसा अलंकरण नहीं दे सकती. महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता न होने के बावजूद सरकार उन्हें विशेष अलंकरण और स्वतंत्रता दिवस के पहले सम्मान देती है जबकि देश को संविधान देने वाले डा. भीमराव अम्बेडकर का नाम संविधान की संक्षिप्त रुपरेखा तक में नहीं है.
इसके विपरीत्त महात्मा गांधी का वास्ता न तो संविधान निर्माण से था और न संविधान सभा से था, फिर भी उनका नाम और उनके फोटो संविधान के अंदर है. केन की मांग है कि संविधान निर्माता होने के कारण डा. अम्बेडकर को भी वाजिब सम्मान मिले. क्या इस गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संविधान का गुणगान करने वाली सरकार और राजनीतिक दल इस बारे में सोचेंगे?
तकरीबन ढाई दशक पहले आरपीआई के एक नेता ने संसद में यह प्रश्न उठाया था कि जिस तरह 15 अगस्त से पहले लाल किले पर झंडोत्तोलन के लिए जाते वक्त प्रधानमंत्री राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, उसी तरह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति इंडिया गेट पर जाने से पहले संसद भवन स्थित संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर को याद क्यों नहीं करती? सवाल सीधा और सपाट था सो सरकार ने भी इसका सीधा सा जवाब दे दिया. सरकार का कहना था कि इस मौके पर किसी भी राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, इसलिए डा. अम्बेडकर को भी सम्मानित नहीं किया जाता है.
जवाब आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया. इस बीच रतनलाल केन नाम के एक व्यक्ति इसके लिए लड़ते रहे, हर साल राष्ट्रपति को चिठ्ठी लिखते रहे. आरटीआई ने अब इन्हें नया हथियार दे दिया था और उनकी लड़ाई भी धारदार हो गई. लेकिन जब जवाब सरकार से मांगना हो और वह ना देना चाहे तो कोई सूचना का अधिकार भी कुछ नहीं कर सकता. खासतौर पर भारत जैसे देश में. सवाल है कि प्रधानमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के पहले जब इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है तो अपने कर्मवीरों और राष्ट्रनेताओं को जिन्होंने देश को संविधान दिया उनको क्यों भूल जाते हैं?
हालांकि आरटीआई के माध्यम से केन ने कई नई चीजें निकाली हैं, जो चौंकाने वाली है. रतनलाल के अपने तर्क हैं. अपनी मुहिम को जारी रखते हुए केन ने 13 दिसंबर 2011 को महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिख कर उनसे इस मामले में एनओसी की मांग की है. केन का कहना है कि हमें एनओसी दिया जाए कि सरकार हमारे इस मामले को सुलझाने में असफल रही है, ताकि हम इसे यूएनओ में उठा सके. हालांकि 13 दिसंबर के इस पत्र के इंतजार में वह अब तक हैं. जाहिर है उन्हें इसका जवाब नहीं मिला है. संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के बारे में सरकार के दृष्टिकोण का एक चौंकाने वाला यह पहलू भी सामने आया है कि सरकार डा. अम्बेडकर को जहां स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती, वहीं उनके संविधान निर्माता होने के सवाल पर चुप्पी साध लेती है. आरटीआई के माध्यम से केन ने गृह मंत्रालय से यह सवाल किया कि क्या डा. अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी हैं? या फिर क्या वह संविधान निर्माता हैं? तो गृह मंत्रालय के डीओपीटी से जवाब आया कि डा. अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानियों के वर्ग में नहीं आतें, तो वहीं संविधान निर्माता मानने के बारे में उसने चुप्पी साध ली.
गांधी और अम्बेडकर के बीच आजादी के समय से ही उभरे मतभेद यहां भी साफ दिखाई देते हैं. यहीं से एक सवाल यह भी उठता है कि फिर महात्मा गांधी जी को किस नीति और नियम के तहत राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई. गड़बड़झाला की सूचना यहां भी है. केन द्वारा गृह मंत्रालय से महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता होने के संबंध में जानकारी मांगने पर 2002 में तात्कालिन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जवाब दिया कि जैसे दूसरे लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे मैं भी कहता हूं लेकिन गृह मंत्रालय के रिकार्ड के मुताबिक आज तक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करने का कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. ना ही संविधान में ऐसा कोई अलंकरण देने की व्यवस्था है. सरकार किसी को ऐसा अलंकरण नहीं दे सकती. महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता न होने के बावजूद सरकार उन्हें विशेष अलंकरण और स्वतंत्रता दिवस के पहले सम्मान देती है जबकि देश को संविधान देने वाले डा. भीमराव अम्बेडकर का नाम संविधान की संक्षिप्त रुपरेखा तक में नहीं है.
इसके विपरीत्त महात्मा गांधी का वास्ता न तो संविधान निर्माण से था और न संविधान सभा से था, फिर भी उनका नाम और उनके फोटो संविधान के अंदर है. केन की मांग है कि संविधान निर्माता होने के कारण डा. अम्बेडकर को भी वाजिब सम्मान मिले. क्या इस गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संविधान का गुणगान करने वाली सरकार और राजनीतिक दल इस बारे में सोचेंगे? आज का राष्ट्रवाद : एक राजनीतिक प्रपंच
 समय के परिवर्तन के साथ-साथ बहुत कुछ बदल जाता है. यहाँ तक कि शब्द भी और शब्दों के अर्थ भी. इसे यूँ समझ सकते हैं कि बहुत पुराने समय में ‘वेदना’ शब्द को दो तरह से जाना जाता था, यथा… सुखद वेदना और दुखद वेदना. लेकिन वर्तमान में ‘वेदना’ शब्द को केवल और केवल एक ही अर्थ में जाना जाने लगा है…वह है ‘पीड़ा’. इसी संदर्भ में यदि ‘राष्ट्रवाद’ शब्द को समझना है तो हमें विगत से होकर गुजरने की जरूरत है. वीकिपीडिया के अनुसार 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज के आपसी सम्बन्ध पर वाद-विवाद शुरू हुआ बताया जाता है तथा 20वीं शताब्दी में द्वितिय विश्वयुद्ध के बाद सामाजिक विज्ञानों में विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण की उदित प्रवृत्ति तथा राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रान्ति और अन्तः अनुशासनात्मक उपागम के बढ़े हुए महत्व के परिणामस्वरूप जर्मन और अमरीकी विद्वानों में राजनीतिक विज्ञान के समाजोन्मुख अध्ययन की एक नूतन प्रवृत्ति शुरू हुई.
इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप राजनीतिक समस्याओं की समाजशास्त्रीय खोज एवं जांच की जाने लगी. ये खोजें एवं जांच न तो पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय ही थीं और न ही पूर्णतः राजनीतिक. अतः ऐसे अध्ययनों को ‘राजनीतिक समाजशास्त्र’ के नाम से पुकारा जाने लगा. एक नया विषय होने के कारण ‘राजनीतिक समाजशास्त्र’ की परिभाषा करना थोड़ा कठिन है. राजनीतिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत हम सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं अर्थात राजनीतिक कारकों तथा सामाजिक कारकों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा इनके एक-दूसरे पर प्रभाव एवं प्रतिच्छेदन का अध्ययन करते हैं. इतना ही नहीं समय के साथ-साथ ‘राजनीतिक समाजशास्त्र’ की भी भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषा की जाने लगी. इस विषय को यही छोड़ना ज्यादा महत्त्वपूर्ण महसूस इस लिए हो रहा है क्योंकि हमें यथोक्त के आलोक में मूलत: ‘राष्ट्रवाद’ की परिभाषा को समझना है. इस बात को तो केवल संदर्भ के रूप में लिया गया है ताकि यहाँ यह समझा जा सके कि समय के साथ-साथ ‘राष्ट्रवाद’ की परिभाषा ने भी कई रूप धारण किए हैं.
आज के समय में ‘राष्ट्रवाद’ की भावना के साथ आज की राजनीति जैसे बलात्कार कर रही है, ऐसा लगता है. यह समझने की जरूरत है कि संघ का राष्ट्रवाद क्या रहा है और आज क्या है? इसे सावरकर के अनुसार ”हिंदुत्व” कहा जाता है…उनके इस ‘हिंदुत्व का अर्थ ‘हिन्दू धर्म’ से नहीं है. उनके अनुसार ‘हिन्दू धर्म’ धार्मिक आस्था पर आधारित एक जीवन-चर्या है, जबकि ”हिंदुत्व ” की अवधारणा ”हिन्दुओं” को एक राजनीतिक श्रेणी या समुदाय में समेटने के लिए की गयी है. यहाँ यह कहा जा सकता है संघ का ‘हिन्दुत्व’ ही उनका आज का ‘राष्ट्रवाद’ है जिसमें सामाजिक सद्भावना की जगह राजनीतिक भावना ज्यादा परिलक्षित होती है. असल में धर्म ‘राष्ट्रवाद’ के बदले ‘धार्मिक अवधारणा’ का ज्यादा समर्थन करता है. और ‘हिन्दुत्व’ के ‘राष्ट्रवाद’ का सीधा अर्थ तो ये है कि जन्म के आधार पर खुद को हिन्दू कहने वाले या कहलाने वाले लोग ही भारतीय राष्ट्र के प्रथम नागरिक हो सकते हैं. इस तर्क के आधार पर सभी गैर-हिन्दूओं को भारत के दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है. संघ की दृष्टि में गैर-हिन्दुओं की भारतीयता और देशभक्ति स्वतः संदिग्ध हो जाती है. इनको अपनी देशभक्ति साबित करके दिखाने की जरूरत है. संघ की राजनीतिक इकाई बीजेपी के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो खुलेआम ये स्वीकार किया था कि उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन भाग लेने का कभी कोई गुनाह नहीं किया. इसका अर्थ ये हुआ कि वो और उनकी पैत्रिक संस्था आर एस एस ने अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया था. यहाँ तक कि ???
आज ये भी कहा जा सकता है कि संघ का राष्ट्रवाद यानी ”हिंदुत्व ” पर आधारित ‘राष्ट्रवाद’ मोदी का राष्ट्रवाद है. कोई इसे मंजूर करे या ना करे, लेकिन कम से कम इसे ठीक- ठीक समझ लेना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठर नेताओं से कहा कि राष्ट्रवाद हमारी पहचान है और उनको राष्ट्रीवाद के संदेश और एजेंडे पर फोकस करना चाहिए क्योंेकि दो साल पहले उनकी रिकॉर्ड जीत में यह प्रमुख कारण रहा है. हैरत अंगेज बात तो ये रही कि उन्होंलने अपने नेताओं से कहा कि बी जे पी का चुनाव जीतना ही उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है. अब आप संघ परिवार के राष्ट्रवाद की परिभाषा सहज ही समझ सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए किए गए स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े लोगों को राष्ट्र-भक्त की श्रेणी में रखा जाता था. अर्थात राष्ट्र से प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है. उस समय भी आर एस एस ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग नहीं लिया… इसके विपरीत अंग्रेजों की गुलामी को इस हद तक स्वीकार किया कि उनके लिए मुखबरी का काम भी किया. अंग्रेजी न्यायालयों में स्वतंत्रता-सेनानियों खिलाफ गवाहियां भी दी. फलत: बहुत से राष्ट्रप्रेमियों को फांसी के फन्दे तक को चूमना पड़ा. किंतु उस समय गांधी और कांग्रेस ने कभी भी आर एस एस को देशद्रोही नहीं कहा. इतना जरूर था कि जो-जो स्वतंत्रता आन्दोलन में शरीक हो रहे थे…. उन्हें देशभक्त जरूर कहा गया था. अंग्रेजों के समय में उनका विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोही थे और अंग्रेजों के समर्थक ….. जाहिर है देशभक्त. यानी सत्ता के विरोध में मत रखने वाले देशद्रोही और सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले राष्ट्रवादी.
यहाँ राष्ट्रवाद को विस्तार से समझने की आवश्कता महसूस हो रही है. दरअसल राष्ट्रवाद को अगर आसान शब्दों में राष्ट्र से प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है. लेकिन सत्ता की मारामारे में भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषाएं भी बदल गयी हैंI आज का राष्ट्रवाद सत्ताशीन पार्टी विशेष के लोगो के लिए ही है. अगर आप उस पार्टी के समर्थक नहीं है तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते. राष्ट्रवाद के नए-नए मायने भी निकल आये हैंI एक सच्चे राष्ट्रवादी बनने के लिए पहले तो आपको आँखें मूंदना सीखना पड़ेगा . सरकार के किसी भी कार्यक्रम में किंतु-परंतु लगाने की हिमाकत नहीं करनी जो सही हुआ वो भी सही और जो गलत हुआ या हो रहा है वो भी सही… बस आज के राष्ट्रवाद की यही परिभाषा शेष रह गई है. यूँ भी कहा जा सकता है कि आज के राष्ट्रवादियों ने बुर देखने, बुरा सुनने, बुरा बोलने, बुरा करने जैसी तमाम बुराइयों को दिल से लगा लिया हैI राष्ट्रवादी बनने के लिए अगला रूल ये है कि आपको हर उस इंसान की आलोचना करनी है जो समाज की बुराइयों पर बात करना चाहता है. उन्हें देशद्रोही बोलकर खुद को राष्ट्रवादी सिद्ध करना है. इतना ही नहीं एक सच्चे राष्ट्रवादी को दलितों पर सदियों से हो रहे अत्याचार और औरतों के साथ हो रहे अमानुषिक व्यवहार /शोषण पर भी आँखें मूंद लेनी हैI आज के राष्ट्रवादियों का ध्येय समाज के उन लोगों से लड़ना है जो समाज को सुधारने की दिशा में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं… और उनसे जो लोग हमें हिन्दू-धर्म में फैली बुराइयों का खुलासा करते हैं … आज के दौर में आप समाज और देश के हित में बात करने वाले लोगों का सामाजिक तिरस्कार करने पर ही आप सच्चे राष्ट्रवादी कहलायेंगेI
असल में राष्ट्रवाद आज के युग में ‘राजनीतिक राष्ट्रवाद’ हो गया है. दुनिया भर में सरकारों के कामकाज़ का तरीका बदल रहा है. सरकारें बदल रही हैं. राजनीतिक और सामाजिक अवधरणा बदल रही है. फलत: राष्ट्रवाद का नया मोडल हमारे सामने है. राष्ट्रवाद आज की राजनीति का अभिन्न अंग हो गया है. दुनिया भर की सरकारें मीडिया को कबजाने का प्रयास कर रही हैं. हर जगह मीडिया का राजनीतिकरण हो गया है. यह केवल भारत की ही बात नहीं है अपितु फ्रांस लंदन, पोलैंड, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया के नेता राजनीतिक मुद्दों पर ही सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देने के मूड में ही देखी जाती हैं.
थोड़ा-बहुत पुराने राष्ट्रवाद को बचाकर रखती हैं, बयानों या कागज़ों में ही सही, ताकि जनता में लोकतंत्र का भ्रम बना रहे. लगातार विज्ञापनों और भाषणों के जरिए यह दिखाने की प्रक्रिया कि कुछ तो हो रहा है, बेशक जमीन पर कुछ भी न हो रहा हो…जोर पकड़ती जा रही है. कहना अतिशयोक्ति नहीं कि आज का राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने-अपने हिसाब से की जाने लगी है….. यानी सबका अपना-अपना राष्ट्रवाद… इस बात को गहनता से समझने के लिए मैं फेसबुक पर आई ईश कुमार गंगानिया की एक पोस्ट का उल्लेख करना चाहूँगा. वो लिखते हैं, ‘आजकल देश-भक्ति व संस्कृति की नई-नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं. कोई तेल-साबुन, दंत-मंजन, मैगी, बिस्किट व चाकलेट आदि की दुकान सजाकर अपनी देश-भक्ति का प्रदर्शन करता है. कोई तीन-चार बच्चे पैदा करने का आह्वान कर अपनी देश-भक्ति का ढोल पीटता है. कोई महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिएं, कब घर से निकलना चाहिए और कब नहीं आदि पर फतवे जारी कर देश-भक्ति व संस्कृति की अपनी नई मिसाल कायम करने पर तुला है. फहरिस्त बड़ी लम्बी है, किस-किस की देश-भक्ति और संस्कृति के किस्से गिनाऊं और किसके नहीं, समझ में नहीं आ रहा है. मुझे लगता है कि इन महानुभावों ने देश-भक्ति और संस्कृति को महाभारत की द्रोपदी बना दिया है. जहां कोई स्त्री उसे अपने पांच-पांच पुत्रों की बीवी बनाकर अपनी देश-भक्ति व संस्कृति की स्थापना करती है. कोई धर्मराज उसे जुएं में दांव पर लगाकर अपनी देश-भक्ति और संस्कृति का परिचय देता है. कोई राजा अपने दरबार में उसके चीरहरण को देश-भक्ति व संस्कृति की नई मिसाल मानता है. आज इक्कीसवीं सदी में देश का राजा धर्मराज भी है और वह चक्रवर्ती भी. उसके दरबार में मंत्री भी हैं और संत्री भी. उसके पास सेना भी है, अस्त्र भी है और शस्त्र भी. लेकिन नहीं बच पा रही है द्रोपदी की अस्मिता… निरंतर लहुलुहान होने से. कोई शम्बूक इसके जख्मों पर निरंतर मरहम लगाने का जोखिम उठाए जा रहा है. क्या रोक पाएगा वह इक्कीसवीं सदी के कुरुक्षेत्र को? आप क्या कहते हो मित्रों…..’ है किसी के पास इसका जवाब? क्या आप गंगानिया जी के इस मत से सहमत नहीं? यदि नहीं तो आपके राष्ट्रवाद की भी अपनी अलग ही परिभाषा होगी. ठीक वैसे ही जैसे योग गुरू बाबा रामदेव के राष्ट्रवाद की परिभाषा. अन्ना के राष्ट्रवाद को कोई समझ ही पाता…उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा तो समय के साथ-साथ बदलती ही रहती है.
पुन: उल्लिखित है कि अंग्रजों के शासनकाल में जो अंग्रेजों के खिलाफ जन-आन्दोलन करते थे …वो राष्ट्रद्रोही और जो उनकी गुलामी को चाहे जैसे स्वीकार कर रहे थे या उनके लिए मुखबरी कर रहे थे …. वो राष्ट्रप्रेमी. ठीक वही हालत आज की है… जो लोग सरकार के कामों पर किंतु-परंतु करते हैं या किसी भी प्रकार का प्रश्नचिन्द लगाते दिखते हैं …वो राष्ट्रद्रोही और वो जो सरकार के उल्टे-सीधे कामों पर आँख मून्दकर सरकार के पक्षधर बने रहते हैं…वो राष्ट्रप्रेमी. कहा जा सकता है कि देश के साथ जो भी अच्छा-बुरा हो रहा है, उसकी राजनीतिक दलों को कोई भी चिंता नहीं रह गई है. राजनीतिक दलों का तो येनकेन-प्रकारेण सत्ता में बने रहना मात्र ही ध्येय रह गया है. वास्तव में आज का राष्ट्रवाद एक राजनीतिक प्रपंच बनकर रह गया है. क्या ऐसा राष्ट्रवाद भारत के विनाश की गारंटी नहीं है? क्या 21वीं सदी में ऐसे राष्ट्रवाद के साथ भारत आगे बढ़ सकता है?
समय के परिवर्तन के साथ-साथ बहुत कुछ बदल जाता है. यहाँ तक कि शब्द भी और शब्दों के अर्थ भी. इसे यूँ समझ सकते हैं कि बहुत पुराने समय में ‘वेदना’ शब्द को दो तरह से जाना जाता था, यथा… सुखद वेदना और दुखद वेदना. लेकिन वर्तमान में ‘वेदना’ शब्द को केवल और केवल एक ही अर्थ में जाना जाने लगा है…वह है ‘पीड़ा’. इसी संदर्भ में यदि ‘राष्ट्रवाद’ शब्द को समझना है तो हमें विगत से होकर गुजरने की जरूरत है. वीकिपीडिया के अनुसार 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज के आपसी सम्बन्ध पर वाद-विवाद शुरू हुआ बताया जाता है तथा 20वीं शताब्दी में द्वितिय विश्वयुद्ध के बाद सामाजिक विज्ञानों में विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण की उदित प्रवृत्ति तथा राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रान्ति और अन्तः अनुशासनात्मक उपागम के बढ़े हुए महत्व के परिणामस्वरूप जर्मन और अमरीकी विद्वानों में राजनीतिक विज्ञान के समाजोन्मुख अध्ययन की एक नूतन प्रवृत्ति शुरू हुई.
इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप राजनीतिक समस्याओं की समाजशास्त्रीय खोज एवं जांच की जाने लगी. ये खोजें एवं जांच न तो पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय ही थीं और न ही पूर्णतः राजनीतिक. अतः ऐसे अध्ययनों को ‘राजनीतिक समाजशास्त्र’ के नाम से पुकारा जाने लगा. एक नया विषय होने के कारण ‘राजनीतिक समाजशास्त्र’ की परिभाषा करना थोड़ा कठिन है. राजनीतिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत हम सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं अर्थात राजनीतिक कारकों तथा सामाजिक कारकों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा इनके एक-दूसरे पर प्रभाव एवं प्रतिच्छेदन का अध्ययन करते हैं. इतना ही नहीं समय के साथ-साथ ‘राजनीतिक समाजशास्त्र’ की भी भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषा की जाने लगी. इस विषय को यही छोड़ना ज्यादा महत्त्वपूर्ण महसूस इस लिए हो रहा है क्योंकि हमें यथोक्त के आलोक में मूलत: ‘राष्ट्रवाद’ की परिभाषा को समझना है. इस बात को तो केवल संदर्भ के रूप में लिया गया है ताकि यहाँ यह समझा जा सके कि समय के साथ-साथ ‘राष्ट्रवाद’ की परिभाषा ने भी कई रूप धारण किए हैं.
आज के समय में ‘राष्ट्रवाद’ की भावना के साथ आज की राजनीति जैसे बलात्कार कर रही है, ऐसा लगता है. यह समझने की जरूरत है कि संघ का राष्ट्रवाद क्या रहा है और आज क्या है? इसे सावरकर के अनुसार ”हिंदुत्व” कहा जाता है…उनके इस ‘हिंदुत्व का अर्थ ‘हिन्दू धर्म’ से नहीं है. उनके अनुसार ‘हिन्दू धर्म’ धार्मिक आस्था पर आधारित एक जीवन-चर्या है, जबकि ”हिंदुत्व ” की अवधारणा ”हिन्दुओं” को एक राजनीतिक श्रेणी या समुदाय में समेटने के लिए की गयी है. यहाँ यह कहा जा सकता है संघ का ‘हिन्दुत्व’ ही उनका आज का ‘राष्ट्रवाद’ है जिसमें सामाजिक सद्भावना की जगह राजनीतिक भावना ज्यादा परिलक्षित होती है. असल में धर्म ‘राष्ट्रवाद’ के बदले ‘धार्मिक अवधारणा’ का ज्यादा समर्थन करता है. और ‘हिन्दुत्व’ के ‘राष्ट्रवाद’ का सीधा अर्थ तो ये है कि जन्म के आधार पर खुद को हिन्दू कहने वाले या कहलाने वाले लोग ही भारतीय राष्ट्र के प्रथम नागरिक हो सकते हैं. इस तर्क के आधार पर सभी गैर-हिन्दूओं को भारत के दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है. संघ की दृष्टि में गैर-हिन्दुओं की भारतीयता और देशभक्ति स्वतः संदिग्ध हो जाती है. इनको अपनी देशभक्ति साबित करके दिखाने की जरूरत है. संघ की राजनीतिक इकाई बीजेपी के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो खुलेआम ये स्वीकार किया था कि उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन भाग लेने का कभी कोई गुनाह नहीं किया. इसका अर्थ ये हुआ कि वो और उनकी पैत्रिक संस्था आर एस एस ने अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया था. यहाँ तक कि ???
आज ये भी कहा जा सकता है कि संघ का राष्ट्रवाद यानी ”हिंदुत्व ” पर आधारित ‘राष्ट्रवाद’ मोदी का राष्ट्रवाद है. कोई इसे मंजूर करे या ना करे, लेकिन कम से कम इसे ठीक- ठीक समझ लेना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठर नेताओं से कहा कि राष्ट्रवाद हमारी पहचान है और उनको राष्ट्रीवाद के संदेश और एजेंडे पर फोकस करना चाहिए क्योंेकि दो साल पहले उनकी रिकॉर्ड जीत में यह प्रमुख कारण रहा है. हैरत अंगेज बात तो ये रही कि उन्होंलने अपने नेताओं से कहा कि बी जे पी का चुनाव जीतना ही उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है. अब आप संघ परिवार के राष्ट्रवाद की परिभाषा सहज ही समझ सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए किए गए स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े लोगों को राष्ट्र-भक्त की श्रेणी में रखा जाता था. अर्थात राष्ट्र से प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है. उस समय भी आर एस एस ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग नहीं लिया… इसके विपरीत अंग्रेजों की गुलामी को इस हद तक स्वीकार किया कि उनके लिए मुखबरी का काम भी किया. अंग्रेजी न्यायालयों में स्वतंत्रता-सेनानियों खिलाफ गवाहियां भी दी. फलत: बहुत से राष्ट्रप्रेमियों को फांसी के फन्दे तक को चूमना पड़ा. किंतु उस समय गांधी और कांग्रेस ने कभी भी आर एस एस को देशद्रोही नहीं कहा. इतना जरूर था कि जो-जो स्वतंत्रता आन्दोलन में शरीक हो रहे थे…. उन्हें देशभक्त जरूर कहा गया था. अंग्रेजों के समय में उनका विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोही थे और अंग्रेजों के समर्थक ….. जाहिर है देशभक्त. यानी सत्ता के विरोध में मत रखने वाले देशद्रोही और सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले राष्ट्रवादी.
यहाँ राष्ट्रवाद को विस्तार से समझने की आवश्कता महसूस हो रही है. दरअसल राष्ट्रवाद को अगर आसान शब्दों में राष्ट्र से प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है. लेकिन सत्ता की मारामारे में भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषाएं भी बदल गयी हैंI आज का राष्ट्रवाद सत्ताशीन पार्टी विशेष के लोगो के लिए ही है. अगर आप उस पार्टी के समर्थक नहीं है तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते. राष्ट्रवाद के नए-नए मायने भी निकल आये हैंI एक सच्चे राष्ट्रवादी बनने के लिए पहले तो आपको आँखें मूंदना सीखना पड़ेगा . सरकार के किसी भी कार्यक्रम में किंतु-परंतु लगाने की हिमाकत नहीं करनी जो सही हुआ वो भी सही और जो गलत हुआ या हो रहा है वो भी सही… बस आज के राष्ट्रवाद की यही परिभाषा शेष रह गई है. यूँ भी कहा जा सकता है कि आज के राष्ट्रवादियों ने बुर देखने, बुरा सुनने, बुरा बोलने, बुरा करने जैसी तमाम बुराइयों को दिल से लगा लिया हैI राष्ट्रवादी बनने के लिए अगला रूल ये है कि आपको हर उस इंसान की आलोचना करनी है जो समाज की बुराइयों पर बात करना चाहता है. उन्हें देशद्रोही बोलकर खुद को राष्ट्रवादी सिद्ध करना है. इतना ही नहीं एक सच्चे राष्ट्रवादी को दलितों पर सदियों से हो रहे अत्याचार और औरतों के साथ हो रहे अमानुषिक व्यवहार /शोषण पर भी आँखें मूंद लेनी हैI आज के राष्ट्रवादियों का ध्येय समाज के उन लोगों से लड़ना है जो समाज को सुधारने की दिशा में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं… और उनसे जो लोग हमें हिन्दू-धर्म में फैली बुराइयों का खुलासा करते हैं … आज के दौर में आप समाज और देश के हित में बात करने वाले लोगों का सामाजिक तिरस्कार करने पर ही आप सच्चे राष्ट्रवादी कहलायेंगेI
असल में राष्ट्रवाद आज के युग में ‘राजनीतिक राष्ट्रवाद’ हो गया है. दुनिया भर में सरकारों के कामकाज़ का तरीका बदल रहा है. सरकारें बदल रही हैं. राजनीतिक और सामाजिक अवधरणा बदल रही है. फलत: राष्ट्रवाद का नया मोडल हमारे सामने है. राष्ट्रवाद आज की राजनीति का अभिन्न अंग हो गया है. दुनिया भर की सरकारें मीडिया को कबजाने का प्रयास कर रही हैं. हर जगह मीडिया का राजनीतिकरण हो गया है. यह केवल भारत की ही बात नहीं है अपितु फ्रांस लंदन, पोलैंड, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया के नेता राजनीतिक मुद्दों पर ही सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देने के मूड में ही देखी जाती हैं.
थोड़ा-बहुत पुराने राष्ट्रवाद को बचाकर रखती हैं, बयानों या कागज़ों में ही सही, ताकि जनता में लोकतंत्र का भ्रम बना रहे. लगातार विज्ञापनों और भाषणों के जरिए यह दिखाने की प्रक्रिया कि कुछ तो हो रहा है, बेशक जमीन पर कुछ भी न हो रहा हो…जोर पकड़ती जा रही है. कहना अतिशयोक्ति नहीं कि आज का राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने-अपने हिसाब से की जाने लगी है….. यानी सबका अपना-अपना राष्ट्रवाद… इस बात को गहनता से समझने के लिए मैं फेसबुक पर आई ईश कुमार गंगानिया की एक पोस्ट का उल्लेख करना चाहूँगा. वो लिखते हैं, ‘आजकल देश-भक्ति व संस्कृति की नई-नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं. कोई तेल-साबुन, दंत-मंजन, मैगी, बिस्किट व चाकलेट आदि की दुकान सजाकर अपनी देश-भक्ति का प्रदर्शन करता है. कोई तीन-चार बच्चे पैदा करने का आह्वान कर अपनी देश-भक्ति का ढोल पीटता है. कोई महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिएं, कब घर से निकलना चाहिए और कब नहीं आदि पर फतवे जारी कर देश-भक्ति व संस्कृति की अपनी नई मिसाल कायम करने पर तुला है. फहरिस्त बड़ी लम्बी है, किस-किस की देश-भक्ति और संस्कृति के किस्से गिनाऊं और किसके नहीं, समझ में नहीं आ रहा है. मुझे लगता है कि इन महानुभावों ने देश-भक्ति और संस्कृति को महाभारत की द्रोपदी बना दिया है. जहां कोई स्त्री उसे अपने पांच-पांच पुत्रों की बीवी बनाकर अपनी देश-भक्ति व संस्कृति की स्थापना करती है. कोई धर्मराज उसे जुएं में दांव पर लगाकर अपनी देश-भक्ति और संस्कृति का परिचय देता है. कोई राजा अपने दरबार में उसके चीरहरण को देश-भक्ति व संस्कृति की नई मिसाल मानता है. आज इक्कीसवीं सदी में देश का राजा धर्मराज भी है और वह चक्रवर्ती भी. उसके दरबार में मंत्री भी हैं और संत्री भी. उसके पास सेना भी है, अस्त्र भी है और शस्त्र भी. लेकिन नहीं बच पा रही है द्रोपदी की अस्मिता… निरंतर लहुलुहान होने से. कोई शम्बूक इसके जख्मों पर निरंतर मरहम लगाने का जोखिम उठाए जा रहा है. क्या रोक पाएगा वह इक्कीसवीं सदी के कुरुक्षेत्र को? आप क्या कहते हो मित्रों…..’ है किसी के पास इसका जवाब? क्या आप गंगानिया जी के इस मत से सहमत नहीं? यदि नहीं तो आपके राष्ट्रवाद की भी अपनी अलग ही परिभाषा होगी. ठीक वैसे ही जैसे योग गुरू बाबा रामदेव के राष्ट्रवाद की परिभाषा. अन्ना के राष्ट्रवाद को कोई समझ ही पाता…उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा तो समय के साथ-साथ बदलती ही रहती है.
पुन: उल्लिखित है कि अंग्रजों के शासनकाल में जो अंग्रेजों के खिलाफ जन-आन्दोलन करते थे …वो राष्ट्रद्रोही और जो उनकी गुलामी को चाहे जैसे स्वीकार कर रहे थे या उनके लिए मुखबरी कर रहे थे …. वो राष्ट्रप्रेमी. ठीक वही हालत आज की है… जो लोग सरकार के कामों पर किंतु-परंतु करते हैं या किसी भी प्रकार का प्रश्नचिन्द लगाते दिखते हैं …वो राष्ट्रद्रोही और वो जो सरकार के उल्टे-सीधे कामों पर आँख मून्दकर सरकार के पक्षधर बने रहते हैं…वो राष्ट्रप्रेमी. कहा जा सकता है कि देश के साथ जो भी अच्छा-बुरा हो रहा है, उसकी राजनीतिक दलों को कोई भी चिंता नहीं रह गई है. राजनीतिक दलों का तो येनकेन-प्रकारेण सत्ता में बने रहना मात्र ही ध्येय रह गया है. वास्तव में आज का राष्ट्रवाद एक राजनीतिक प्रपंच बनकर रह गया है. क्या ऐसा राष्ट्रवाद भारत के विनाश की गारंटी नहीं है? क्या 21वीं सदी में ऐसे राष्ट्रवाद के साथ भारत आगे बढ़ सकता है?
– लेखक तेजपाल सिंह तेज स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर इन दिनों स्वतंत्र लेखन में रत हैं. आपको हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार ( 1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से सम्मानित किया जा चुका है.
यूपी चुनावः ग्लैमर बनाम संघर्ष
 उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होने के बाद एक चर्चा आम है. चर्चा है कि यहां चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी. खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि दोनों साथ उतर सकती हैं और ऐसे में वे दोनों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के लिए चुनौती बन सकती हैं. तर्क यह दिया जा रहा है कि लोगों के बीच इन दोनों का ग्लैमर ज्यादा काम करेगा और ये युवाओं को जोर पाएंगी.
असल में यह तमाम अखबारों और वेबसाइटों पर चल रहा यह तर्क बेहद बेकार है. क्योंकि अगर लोग किसी नेता की सुंदर छवि को देख कर वोट देते तो फिर इस देश की सत्ता पर मॉडल और फिल्मी हस्तियों का राज होता. इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि जनता जिन चेहरों को रुपहले पर्दे पर देखती है, सामने आने पर उनसे प्रभावित हो जाती है. लेकिन यह लंबे वक्त के लिए नहीं होता. वैसे भी अगर साउथ को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत की चुनावी राजनीति में आए फिल्मी हस्तियों ने जनता को निराश ही किया है. ऐसे में किसी भी राजनीतिक परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति के ग्लैमर के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की बात बेमानी है. प्रभावित हो भी जाए तो इससे चुनावी जीत संभव नहीं है.
एक तथ्य यह भी है कि चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा नहीं बल्कि विचारधारा मायने रखती है. और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी विचारधारा की ही लड़ाई है. एक तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो समाज के हर नागरिक को साथ लेकर चलने और संविधान के अनुरूप काम करने को तव्वजो देती है तो दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा का हाल आज क्या है, यह जगजाहिर है. इन दोनों विचारधाराओं की बात करें तो समाजवाद माने मुलायम परिवार और कांग्रेस माने गांधी परिवार होता है.
अगर डिंपल यादव और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरती भी हैं तो सिवाय भीड़ जुटाने के वह कुछ और कर पाएं इसमें संदेह है. और अगर प्रियंका गांधी में उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की उतनी ही क्षमता होती तो कांग्रेस का यह हाल नहीं होता. इन दोनों के पास जो भी है वह इनके परिवार की मेहनत से उपजा है, न कि इन दोनों का इसमें अपना कोई व्यक्तिगत योगदान है. जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने जो कुछ भी अर्जित किया है उसमें उनकी मेहनत, संघर्ष और त्याग की भूमिका है. और बसपा और मायावती जितना जनसमर्थन जुटाने में जब भाजपा जैसी बड़ी पार्टी औऱ देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक का पसीना छूट गया और इसके बाद भी वो सफल नहीं हो सके तो फिर अन्य नाम कहां ठहरते हैं.
फिर भी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यह भ्रम पाले हैं कि बसपा प्रमुख मायावती के सामने वह डिंपल यादव और प्रियंका गांधी को उतार कर बसपा को रोक सकते हैं तो यह संभव नहीं दिखता. क्योंकि जीत हमेशा संघर्ष की होती है.
उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होने के बाद एक चर्चा आम है. चर्चा है कि यहां चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी. खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि दोनों साथ उतर सकती हैं और ऐसे में वे दोनों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के लिए चुनौती बन सकती हैं. तर्क यह दिया जा रहा है कि लोगों के बीच इन दोनों का ग्लैमर ज्यादा काम करेगा और ये युवाओं को जोर पाएंगी.
असल में यह तमाम अखबारों और वेबसाइटों पर चल रहा यह तर्क बेहद बेकार है. क्योंकि अगर लोग किसी नेता की सुंदर छवि को देख कर वोट देते तो फिर इस देश की सत्ता पर मॉडल और फिल्मी हस्तियों का राज होता. इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि जनता जिन चेहरों को रुपहले पर्दे पर देखती है, सामने आने पर उनसे प्रभावित हो जाती है. लेकिन यह लंबे वक्त के लिए नहीं होता. वैसे भी अगर साउथ को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत की चुनावी राजनीति में आए फिल्मी हस्तियों ने जनता को निराश ही किया है. ऐसे में किसी भी राजनीतिक परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति के ग्लैमर के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की बात बेमानी है. प्रभावित हो भी जाए तो इससे चुनावी जीत संभव नहीं है.
एक तथ्य यह भी है कि चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा नहीं बल्कि विचारधारा मायने रखती है. और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी विचारधारा की ही लड़ाई है. एक तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो समाज के हर नागरिक को साथ लेकर चलने और संविधान के अनुरूप काम करने को तव्वजो देती है तो दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा का हाल आज क्या है, यह जगजाहिर है. इन दोनों विचारधाराओं की बात करें तो समाजवाद माने मुलायम परिवार और कांग्रेस माने गांधी परिवार होता है.
अगर डिंपल यादव और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरती भी हैं तो सिवाय भीड़ जुटाने के वह कुछ और कर पाएं इसमें संदेह है. और अगर प्रियंका गांधी में उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की उतनी ही क्षमता होती तो कांग्रेस का यह हाल नहीं होता. इन दोनों के पास जो भी है वह इनके परिवार की मेहनत से उपजा है, न कि इन दोनों का इसमें अपना कोई व्यक्तिगत योगदान है. जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने जो कुछ भी अर्जित किया है उसमें उनकी मेहनत, संघर्ष और त्याग की भूमिका है. और बसपा और मायावती जितना जनसमर्थन जुटाने में जब भाजपा जैसी बड़ी पार्टी औऱ देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक का पसीना छूट गया और इसके बाद भी वो सफल नहीं हो सके तो फिर अन्य नाम कहां ठहरते हैं.
फिर भी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यह भ्रम पाले हैं कि बसपा प्रमुख मायावती के सामने वह डिंपल यादव और प्रियंका गांधी को उतार कर बसपा को रोक सकते हैं तो यह संभव नहीं दिखता. क्योंकि जीत हमेशा संघर्ष की होती है. जन्मदिन विशेषः बहनजी का धम्म कारवां
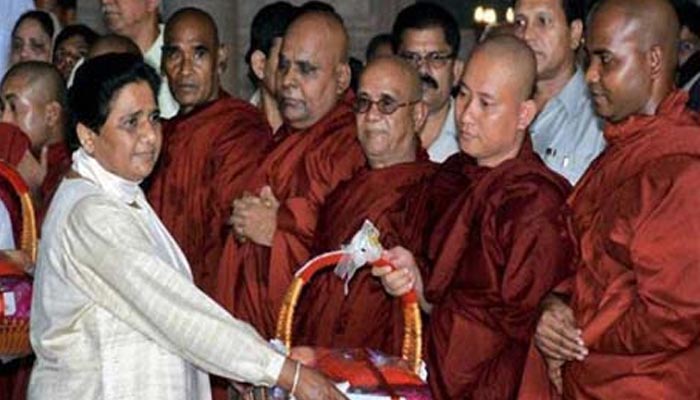 भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण उपरान्त लगभग 218 वर्षों के बाद विश्व के तमाम देशों को अपने धम्म-विजय अभियान द्वारा विजित करने वाले महान सम्राट अशोक ने इसी भारत-भूमि पर राज्य करना प्रारम्भ किया. न्यग्रोध नामक सात वर्षीय श्रामणेर के ‘अप्पमाद’ (अप्रमाद) से संबंधित धर्मोपदेश को सुनकर सम्राट अशोक के मन में बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति श्रद्धा व भक्ति उत्पन्न हुई. जब सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में आस्था उत्पन्न हुई तो सम्राट ने युद्ध-विजय को त्यागकर अहिंसा व धम्म-विजय का अभियान शुरू किया. सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में बहुजनों के सुख व हित के लिए बहुत सा धम्म-कार्य करने के तद्नन्तर अपने आचार्य मोग्गलिपुत्ततिस्स से पूछा,‘‘भगवान बुद्ध के कितने उपदेश हैं?’’ तब मोग्गलीपुत्ततिस्स ने बताया-‘‘राजन् भगवान बुद्ध के 84000 उपदेश हैं.’’ सम्राट अशोक ने 84000 धर्म-स्कन्धों की पूजा करने व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सम्पूर्ण जम्बुद्वीप के 84000 नगरों में विहार, स्तूप व चैत्य बनवाकर एक ही दिन सबकी पूजा की और सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में दीप प्रज्जवलित करवाया गया. तमाम विद्वानों का ऐसा मनाना है कि इसी घटना के बाद इसी दिन हमारे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है. जो राजा पहले ‘चण्डासोक’ था इसी घटना के बाद से अब ‘धम्मासोक’ नाम से प्रसिद्ध हो गया. प्रव्रज्या को राज्याभिषेक से ऊंचा जानकर सम्राट ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को बहुत बड़े समारोह के साथ प्रव्रजित करवाया. इतना ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक के ही संरक्षण में सुप्रसिद्ध तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन देश की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई इसी तृतीय बौद्ध संगीति के परिणामस्वरूप ही मोग्गलिपुत्ततिस्स की अध्यक्षता एवं महान सम्राट अशोक के संरक्षण में विदेशों में भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार व प्रसार की योजना बनायी गयी. बाह्य देशों में धम्म के प्रचार व प्रसार के लिए नौ समूह बनाकर भेजे गये. इस प्रकार सम्राट अशोक का धम्म-दायित्व पूर्ण हुआ.
15 मार्च 1934 को पंजाब प्रान्त के रोपण जिले में ख्वासपुर गांव में जन्में मान्यवर कांशीराम बाबा साहेब के ऐसे श्रेष्ठ अनुयायी हुए कि उन्हें डॉ. अम्बेडकर के आन्दोलन का उत्तराधिकारी कह सकते हैं. बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण उपरान्त एक वर्ष के बाद ही सन् 1957 में अपनी 23 वर्ष की उम्र में ही कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के आन्दोलन को बड़ी तीव्रता के साथ समझने का प्रयास किया. उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत के बहुसंख्यक समाज को राजनीति करने के तौर-तरीके सिखाने एवं निष्कर्ष के रूप में बौद्ध धम्म की तरफ प्रेरित करने में लगाया.
भगवान तथागत गौतम बुद्ध के धम्म-सिद्धान्त ‘बहुजन हिताय- बहुजन सुखाय’ से प्रभावित होकर और इसे ही आदर्श मानते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को ‘बहुजन समाज पार्टी’ की स्थापना की. मान्यवर कांशीराम जी ने सम्पूर्ण भारत देश को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया परन्तु उत्तर प्रदेश को अपने आन्दोलन के लिए अधिक उर्वरा प्रदेश मानते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को कहा- ‘‘मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक के भारत जैसा होगा, यदि मानवतावाद को इस देश में लाना है तो मानवता लाने के लिए भारत को बौद्धमय बनाना जरूरी है.’’ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार अपने संघर्षों के निचोड़ के रूप में उन्होंने 30 मार्च 2002 को नागपुर के उॅटखाना में एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था- ‘‘मैंने फैसला किया है कि 2006 में जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के 50 साल पूरे होंगे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में चमार समाज के लोगों को ‘सलाह देंगे’ कि आप लोग ‘बौद्ध धर्म अपनाएँ’ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी सलाह को मानकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा चमार समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनायेंगे इसलिए बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का जो दूसरा काम आज तक भी अधूरा रहा है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ायेंगे.’’
वर्तमान समय में मान्यवर कांशीराम जी के भी करोड़ों अनुयायी हैं. मान्यवर कांशीराम जी ने अपने उन करोड़ों अनुयायियों में से अपनी परम शिष्या कुमारी मायावती जी को 15 दिसम्बर 2001 को अपने आन्दोलन की जिम्मेवारी देते हुए अपने आन्दोलन का उत्तराधिकारी घोषित किया. अपने आन्दोलन की जिम्मेवारी कुमारी मायावती के कन्धें पर डालते हुए उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार व संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया. अपने परिनिर्वाण से पूर्व मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी वसीयत लिखी- ‘‘मेरी मृत्यु के बाद मेरा अन्तिम संस्कार बौद्ध रीति से ही होना चाहिए.’’ मान्यवर कांशीराम जी ने नागपुर, महाराष्ट्र में यह उद्घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर 2006 को जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर 1956 कि स्वर्ण जयंती मनायी जायेगी तो उस अवसर पर वे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ चमारों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे. परन्तु 2003 ई. में ही उन्हें ब्रेन अटैक जैसी खतरनाक बीमारी हो गयी और वे अस्वस्थ हो गये. लगातार 3 वर्षों के इलाज के बाद 14 अक्टूबर 2006 से पाँच दिन पहले ही 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वाण हो गया. इस प्रकार मान्यवर कांशीराम बौद्ध धर्मान्तरण की अपनी की हुई भविष्यवाणी पूर्ण नहीं कर सके.
डॉ. अम्बेडकर प्रणीत नवबौद्धों के आन्दोलन के मुखिया मान्यवर कांशीराम की शिष्या कुमारी मायावती वर्ष 1995, 1997, 2002 और 2007 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने मान्यवर कांशीराम के उत्तराधिकार को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1997 ई. में सुप्रसिद्ध इन बौद्ध तीर्थ-स्थलों के नाम पर नवीन जिलों का गठन किया. तीर्थ-स्थलों के नाम पर नवनिर्मित जनपदों की ही प्राथमिक प्रेरणा से तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने भगवान बुद्ध और उनकी माँ के नाम पर भी नये जिलों का गठन किया. इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के पुर्नरुद्धारक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर व उनकी पत्नी रमाबाई और उनके बौद्धमय भारत बनाने के सपने को साकार करने वाले मान्यवर कांशीराम के नाम पर भी नये जनपदों का निर्माण किया. बहन कुमारी मायावती ने भगवान बुद्ध के मानवतावादी श्रमण संस्कृति को अपना आदर्श बनाने वाले सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों के नाम पर भी नये जनपदों का गठन कर उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया.
इस प्रकार बहन कुमारी मायावती ने 20 सितम्बर सन् 1995 को सिद्धार्थ नगर की स्थापना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 25 मई सन् 1997 को जिला श्रावस्ती की स्थापना, 4 अप्रैल सन् 1997 को जिला कौशाम्बी और 22 मई सन् 1997 को पडरौना का नाम बदल कर कुशीनगर कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर दिनांक 6 मई सन् 1997 को जिला गौतम बुद्ध नगर की स्थापना एवं दिनांक 6 मई सन् 1997 को भगवान गौतम बुद्ध की माँ महामाया के नाम पर जिला महामाया नगर की स्थापना किया. बुद्धकाल में कण्णकुज्ज नगर के रूप में विख्यात बौद्ध तीर्थ-स्थल के परिक्षेत्र में 18 सितम्बर सन् 1997 को जिला कन्नौज की स्थापना किया. भारत में बौद्ध धर्म का पुर्नरुत्थान करने वाले डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और उनकी पत्नी के नाम पर नवनिर्मित जनपद डॉ. अम्बेडकर नगर (20 सितम्बर सन् 1995), भीम नगर (28 सितम्बर सन् 2011) एवं रमाबाई नगर (18 सितम्बर सन् 1997) का गठन किया. मान्यवर कांशीराम के नाम पर नवनिर्मित जनपद कांशीराम नगर (सन् 2009) और बौद्ध सिद्धान्तों एवं बौद्ध शब्दावली के नाम पर नवनिर्मित जनपद पंचशील नगर (28 सितम्बर सन् 2011) एवं प्रबुद्ध नगर (28 सितम्बर सन् 2011) का ऐतिहासिक गठन किया. इतना ही नहीं बल्कि श्रमण-संस्कृति को मानने वाले संतों-गुरूओं व महापुरुषों के नाम पर भी नवीन जिलों का गठन किया गया है जिसमें संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ज्योतिबाराव फूले नगर एवं छत्रपति शाहू जी महाराज नगर इत्यादि प्रमुख हैं.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्देशन में बौद्ध तीर्थ-स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संग्रहालय 1910 ई. में बौद्ध तीर्थ-स्थल सारनाथ (षिपत्तन मृगदाववन) में स्थापित हुआ था, जिसमें बुद्धकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के पुरावशेष संग्रहित हैं. सन् 1910 के बाद इस दिशा में किसी भी सरकार ने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया. पहली बार बहन कुमारी मायावती ने संग्रहालयों के विकास के क्रम में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य किया. 31 अगस्त 2002 को संग्रहालय निदेशालय के रूप में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना किया. राज्य संग्रहालय, बनारसी बाग, लखनउ के परिसर के पुराने भवन में इस निदेशालय को स्थापित किया गया. इस निदेशालय की स्थापना के पूर्व ही कुमारी मायावती जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी पुरातात्विक सम्पदा के संग्रह, संरक्षण, अभिलेखीकरण व प्रदर्शन के लिए एवं शोध के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनाँक 04 मई, 1997 को ‘राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर’ की स्थापना किया. पूर्वी उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास का हृदय स्थल रहा है. बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल लुम्बिनी, देवदह, कोलियों का रामग्राम एवं तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर इत्यादि इसी क्षेत्र से संबंधित हैं.
भारत के बौद्ध स्थलों में कुशीनगर (कुशीनारा) का प्रमुख स्थान है. भगवान बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अपनी चारिका पूर्ण करने के पश्चात कुशीनारा के उपवत्तन नामक शालवन में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, जिसे आज कुशीनगर कहा जाता है. इस पवित्र स्थल पर असंख्य पर्यटक एवं बौद्ध धर्मानुयायी प्रति वर्ष भगवान बुद्ध को श्रद्धाजंलि अर्पित करने आते हैं. कुशीनगर की धार्मिक महत्ता एवं समृद्ध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर ने कई देशों एवं विभागों को इस क्षेत्र में अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापित करने की प्रेरणा दी और परिणामस्वरूप यह स्थल सम्पूर्ण विश्व में आकर्षण का केन्द्र बन गया. कुशीनगर की पुरातात्विक सम्पदा सहित भारतीय संस्कृति को संकलित तथा सुरक्षित करने के उद्देश्य से कुमारी मायावती ने शासन द्वारा 04 मई, 1997 को कुशीनगर में ‘राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर’ की स्थापना किया.
भगवान बुद्ध की क्रीड़ास्थली एवं युवावस्था तक कर्मस्थली होने के कारण कपिलवस्तु भी बौद्ध तीर्थ-स्थल के रूप में प्रसिद्ध है. जिसकी पहचान सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित पिपरहवाँ नामक स्थान से की गयी है. जहाँ पर देश-विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पर्यटन हेतु आते हैं. पिपरहवाँ में ही बुद्ध के अस्थि-अवशेषों से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ. जिस पर ब्राह्मी एवं खरोष्ठी, दोनों लिपियों में लेख लिपिबद्ध हैं. बौद्ध तीर्थ-स्थल कपिलवस्तु की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए बौद्ध हैरिटेज सेन्टर, पिपरहवाँ की योजनान्तर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी ने ‘राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवाँ, सिद्धार्थनगर’ की स्थापना करवाया. इसी श्रृंखला में कुमारी मायावती ने रामपुर जनपद में ‘भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय’ का भी निर्माण करवाया. इस संग्रहालय के मुख्य द्वार पर डॉ. अम्बेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कालाक्रमानुसार लिपिबद्ध कर प्रदर्शित किया गया है.
शैक्षणिक विकास के क्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की दृष्टि से तकनीकी एवं प्रबंधन में डिग्री एवं डिप्लोमा देने वाले समस्त महाविद्यालयों को दो भागों में विभाजित कर उन्हें ‘गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय (Goutam Buddh Technical University) एवं ‘महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय (Mahamaya Technical University) से सम्बद्ध कर दिया. शिक्षा की दृष्टि से ‘महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना’ का निर्माण किया गया जिसके तहत प्रत्येक वर्ष लगभग पांच लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया. इसके अलावा ‘महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना’ के तहत बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है. डॉ. अम्बेडकर के नाम पर भी और इतना ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित और मानवता के लिए काम करने वाले और कई सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर सैकड़ों शैक्षणिक संस्थान खोले गये. कुमारी मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें संचालित किया गया, जिनके माध्यम से डॉ. अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने के लिए बल प्रदान किया गया.
बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अभिप्रेत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का भगवान बुद्ध के नाम पर मात्र नामकरण ही नहीं किया बल्कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रहने के लिये पंचशील आवासीय परिसर का निर्माण, परिसर में निर्मित महामाया शांति सरोवर के नाम से दर्शनीय स्थल का निर्माण, विश्वविद्यालय के मुख्य मार्ग का नामकरण सिद्धार्थ गौतम मार्ग, बाह्य परिधि मार्ग को बौद्ध परिपथ तथा आन्तरिक परिधि मार्ग को महामाया परिपथ का नाम दिया जाना, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का नामकरण महामाया द्वार और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में विपस्सना विद्या के अभ्यास हेतु महात्मा ज्योतिबाराव फूले विपस्सना ध्यान भावना केन्द्र की स्थापना इत्यादि का कार्य बहन कुमारी मायावती जी के बौद्ध धर्म के पुर्नरुत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कार्य है.
सामाजिक कल्याण के विकास के क्रम में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण की कई योजनाओं में भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित ‘बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय’ की नीति का अनुसरण किया है. भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के पुर्नरुद्धारक डॉ. अम्बेडकर के ‘समता मूलक समाज की स्थापना’ के सिद्धान्तों के आधार पर कुमारी मायावती जी ने अपनी योजनाएं निर्मित की और उन योजनाओं का नामकरण भगवान बुद्ध की मां महामाया व डॉ. अम्बेडकर के नाम पर किया. सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निर्मित योजनाओं का नामकरण भी बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में बहन जी के योगदान को परिभाषित करता है.
आवासीय व्यवस्था के विकास के क्रम में देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नवनिर्मित जनपद गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विकास कार्य किया गया. उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले नागारिकों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए ‘डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना’ का कार्यान्वयन भी बहन जी की सरकारों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और इतना ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की मां महामाया के नाम पर ‘महामाया सर्वजन आवास योजना’ का निर्माण किया गया और इस योजना के तहत समाज के सभी वर्गों को जो आवास विहीन थे, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया गया. इन योजनाओं के अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री कांशीराम जी के नाम पर निर्मित ‘मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना’ एवं ‘मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना’ के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आवासीय व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया गया.
पर्यटन की दृष्टि से बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं. उत्तर प्रदेश में अधिकांश विदेशी पर्यटकों का आवागमन बौद्ध तीर्थ-स्थलों के कारण ही होता है. बौद्ध तीर्थ-स्थलों की दृष्टि से पर्यटन का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘बौद्ध परिपथ से मथुरा और संकिसा को जोड़ने के क्रम में ब्रज परिपथ, सारनाथ के लिए वाराणसी-विन्ध्य परिपथ, श्रावस्ती के लिए लखनउ-अवध परिपथ का चिन्हांकन किया. पर्यटन के विकास के क्रम में इन परिपथों के विकास के लिए बहन जी ने विभिन्न योजनाएँ निर्मित की हैं.
सन् 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘बौद्ध परिपथ’ के महत्व को स्वीकारते हुए इसकी अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाने की प्राथमिकता दी गई और भगवान गौतम बुद्ध एवं बौद्ध परिपथ से जुड़े स्थानों के विकास के क्रम में गोरखपुर परिक्षेत्र में बौद्ध परिपथ का विकास विशेष रूप से किया गया. गोरखपुर परिक्षेत्र में भगवान बुद्ध से संबंधित राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण/ब्रिजवर्क कराया गया. इसके अलावा कुशीनगर में पर्यटक आवास गृह का विस्तारीकरण/उच्चीकरण, कपिलवस्तु में लैण्डस्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण, कपिलवस्तु में भारतीय बौद्ध महाविहार में यात्री निवास का निर्माण, बौद्ध हेरिटेज सेंटर/वाणिज्यिक परिसर का निर्माण, कपिलवस्तु में बौद्ध संग्रहालय का निर्माण, हेरिटेज पार्क एवं विपश्यना केन्द्र की स्थापना, बौद्ध कला वीथिका की स्थापना एवं कुशीनगर में हवाई पट्टी का निर्माण इत्यादि के कार्य अत्यन्त उल्लेखनीय हैं. फैज़ाबाद परिक्षेत्र में बौद्ध पर्यटन के विकास के क्रम में जनपद श्रावस्ती में स्थित बौद्ध तीर्थ-स्थल का विकास बड़े पैमाने पर किया गया.
वाराणसी परिक्षेत्र में बौद्ध पर्यटन के विकास हेतु बौद्ध तीर्थ-स्थल सारनाथ में तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी के निर्देश पर तमाम उल्लेखनीय कार्य किए गए. इस प्रकार हम देखते हैं कि वाराणसी एवं फैजाबाद परिक्षेत्र में बौद्ध परिपथ का विकास विशेष रूप से किया गया. पर्यटन-व्यवसाय एवं रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लखनउ में मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, चिनहट की स्थापना की गई.
लखनउ में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने एवं बौद्ध धर्म के पुर्नरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनउ में बौद्ध स्थापत्य के आधार पर कई बौद्ध विहारों एवं बौद्ध स्मारकों के निर्माण करवाये गये. उनमें बौद्ध विहार शान्ति उपवन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुजन नायक पार्क, रमाबाई मूलक चौक, रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की चौमुखी प्रतिमा, गोमती विहार खण्ड-1 इत्यादि प्रमुख स्थल ऐतिहासिक रूप से बहन जी योगदान को व्याख्यायित कर रहे हैं.
बौद्ध तीर्थ-स्थलों को जोड़ने के क्रम में ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन वाली ‘गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना’ का निर्माण किया गया. इस मार्ग के निर्माण हो जाने पर बौद्ध तीर्थ-स्थल संकिसा, सारनाथ एवं कुशीनगर की यात्रा आसान व सुलभ हो जाएगी. सड़क परिवहन के साथ ही साथ रेल परिवहन, जल परिवहन एवं उड्डयन परिवहन का विकास भी बौद्ध तीर्थ-स्थलों की दृष्टि से किया गया. नागारिक उड्डयन सेवा की दृष्टि से हवाई पट्टी श्रावस्ती, हवाई पट्टी गौतम बुद्ध नगर एवं अर्न्तराष्ट्रीय एयर पोर्ट कुशीनगर का निर्माण उल्लेखनीय है.
ब्रिटिश-भारत के कुछ महान अन्वेषकों ने और भारतीय पुरातत्व विभाग ने जिन पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कर, उन्हें बौद्ध तीर्थ-स्थल के रूप में घोषित किया उनमें से कुछ पर भारतीय सरकारों ने ध्यान दिया और उनका विकास भी किया परन्तु अपने मुख्यमन्त्रित्व काल में बहन कुमारी मायावती जी ने उन तीर्थ-स्थलों के परिक्षेत्र में बौद्ध तीर्थ-स्थलों के नाम पर नवीन जिलों का निमार्ण एवं भगवान बुद्ध व उनके महान अनुयायियों के नाम पर भी नवनिर्मित जिलों की स्थापना करके और भगवान बुद्ध की विचारधारा के आधार पर कई योजनाएँ निर्मित कर बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का ऐतिहासिक कार्य किया है.
उत्तर प्रदेश के नागरिकों के रहन-सहन, आचार-व्यवहार इत्यादि का अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ के लोग शताब्दियों से चली आ रही वर्णवाद, जातिवाद एवं छुआछूत इत्यादि की परम्परा से ग्रसित रहते थे परन्तु आधुनिक समय में जब नवबौद्धों द्वारा बुद्ध की शिक्षा-दीक्षा का प्रचार-प्रसार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तो इसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के ऐसे कई समुदाय हैं जो वर्णवाद, जातिवाद एवं छुआछूत इत्यादि जैसी कुरीतियों से उपर उठकर भगवान बुद्ध के आदर्शों पर आधारित अपनी संस्कृति के विकास में उन्नति कर रहे हैं. अंधविश्वास तथा ढोंग-ढकोसला एवं पाखण्डों के जाल से मुक्त होने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग अथक प्रयास कर रहे हैं. कुछ समुदायों के लोगों की पूजा-पाठ, रीति-रिवाज में बदलाव आया है. इन लोगों के शादी-विवाह एवं मृतक इत्यादि संस्कारों में भगवान बुद्ध के आदर्शों का परिपालन किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के कई समुदायों के लोगों ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को समाहित कर अपनी संस्कृति और संस्कारों में सुधार किया है. सामाजिक-राजनैतिक विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न समाजों और उनके द्वारा निर्मित राजनैतिक दलों के सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है. भौतिक विकास ही नहीं बल्कि धर्मिक, सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक व राजनैतिक विकास में सामन्जस्य स्थापित हुआ है.
– लेखक बौद्ध विद्वान हैं. एम.एससी/ एम.ए./ एम.फिल/पी.एचडी हैं. राजनीति में भी सक्रिय हैं.
नोट- यह आलेख दलित दस्तक के जनवरी, 2017 अंक की कवर स्टोरी का अंश है। बिना मैगजीन की अनुमति के इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता।
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण उपरान्त लगभग 218 वर्षों के बाद विश्व के तमाम देशों को अपने धम्म-विजय अभियान द्वारा विजित करने वाले महान सम्राट अशोक ने इसी भारत-भूमि पर राज्य करना प्रारम्भ किया. न्यग्रोध नामक सात वर्षीय श्रामणेर के ‘अप्पमाद’ (अप्रमाद) से संबंधित धर्मोपदेश को सुनकर सम्राट अशोक के मन में बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति श्रद्धा व भक्ति उत्पन्न हुई. जब सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में आस्था उत्पन्न हुई तो सम्राट ने युद्ध-विजय को त्यागकर अहिंसा व धम्म-विजय का अभियान शुरू किया. सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में बहुजनों के सुख व हित के लिए बहुत सा धम्म-कार्य करने के तद्नन्तर अपने आचार्य मोग्गलिपुत्ततिस्स से पूछा,‘‘भगवान बुद्ध के कितने उपदेश हैं?’’ तब मोग्गलीपुत्ततिस्स ने बताया-‘‘राजन् भगवान बुद्ध के 84000 उपदेश हैं.’’ सम्राट अशोक ने 84000 धर्म-स्कन्धों की पूजा करने व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सम्पूर्ण जम्बुद्वीप के 84000 नगरों में विहार, स्तूप व चैत्य बनवाकर एक ही दिन सबकी पूजा की और सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में दीप प्रज्जवलित करवाया गया. तमाम विद्वानों का ऐसा मनाना है कि इसी घटना के बाद इसी दिन हमारे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है. जो राजा पहले ‘चण्डासोक’ था इसी घटना के बाद से अब ‘धम्मासोक’ नाम से प्रसिद्ध हो गया. प्रव्रज्या को राज्याभिषेक से ऊंचा जानकर सम्राट ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को बहुत बड़े समारोह के साथ प्रव्रजित करवाया. इतना ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक के ही संरक्षण में सुप्रसिद्ध तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन देश की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई इसी तृतीय बौद्ध संगीति के परिणामस्वरूप ही मोग्गलिपुत्ततिस्स की अध्यक्षता एवं महान सम्राट अशोक के संरक्षण में विदेशों में भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार व प्रसार की योजना बनायी गयी. बाह्य देशों में धम्म के प्रचार व प्रसार के लिए नौ समूह बनाकर भेजे गये. इस प्रकार सम्राट अशोक का धम्म-दायित्व पूर्ण हुआ.
15 मार्च 1934 को पंजाब प्रान्त के रोपण जिले में ख्वासपुर गांव में जन्में मान्यवर कांशीराम बाबा साहेब के ऐसे श्रेष्ठ अनुयायी हुए कि उन्हें डॉ. अम्बेडकर के आन्दोलन का उत्तराधिकारी कह सकते हैं. बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण उपरान्त एक वर्ष के बाद ही सन् 1957 में अपनी 23 वर्ष की उम्र में ही कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के आन्दोलन को बड़ी तीव्रता के साथ समझने का प्रयास किया. उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत के बहुसंख्यक समाज को राजनीति करने के तौर-तरीके सिखाने एवं निष्कर्ष के रूप में बौद्ध धम्म की तरफ प्रेरित करने में लगाया.
भगवान तथागत गौतम बुद्ध के धम्म-सिद्धान्त ‘बहुजन हिताय- बहुजन सुखाय’ से प्रभावित होकर और इसे ही आदर्श मानते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को ‘बहुजन समाज पार्टी’ की स्थापना की. मान्यवर कांशीराम जी ने सम्पूर्ण भारत देश को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया परन्तु उत्तर प्रदेश को अपने आन्दोलन के लिए अधिक उर्वरा प्रदेश मानते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को कहा- ‘‘मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक के भारत जैसा होगा, यदि मानवतावाद को इस देश में लाना है तो मानवता लाने के लिए भारत को बौद्धमय बनाना जरूरी है.’’ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार अपने संघर्षों के निचोड़ के रूप में उन्होंने 30 मार्च 2002 को नागपुर के उॅटखाना में एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था- ‘‘मैंने फैसला किया है कि 2006 में जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के 50 साल पूरे होंगे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में चमार समाज के लोगों को ‘सलाह देंगे’ कि आप लोग ‘बौद्ध धर्म अपनाएँ’ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी सलाह को मानकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा चमार समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनायेंगे इसलिए बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का जो दूसरा काम आज तक भी अधूरा रहा है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ायेंगे.’’
वर्तमान समय में मान्यवर कांशीराम जी के भी करोड़ों अनुयायी हैं. मान्यवर कांशीराम जी ने अपने उन करोड़ों अनुयायियों में से अपनी परम शिष्या कुमारी मायावती जी को 15 दिसम्बर 2001 को अपने आन्दोलन की जिम्मेवारी देते हुए अपने आन्दोलन का उत्तराधिकारी घोषित किया. अपने आन्दोलन की जिम्मेवारी कुमारी मायावती के कन्धें पर डालते हुए उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार व संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया. अपने परिनिर्वाण से पूर्व मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी वसीयत लिखी- ‘‘मेरी मृत्यु के बाद मेरा अन्तिम संस्कार बौद्ध रीति से ही होना चाहिए.’’ मान्यवर कांशीराम जी ने नागपुर, महाराष्ट्र में यह उद्घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर 2006 को जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर 1956 कि स्वर्ण जयंती मनायी जायेगी तो उस अवसर पर वे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ चमारों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे. परन्तु 2003 ई. में ही उन्हें ब्रेन अटैक जैसी खतरनाक बीमारी हो गयी और वे अस्वस्थ हो गये. लगातार 3 वर्षों के इलाज के बाद 14 अक्टूबर 2006 से पाँच दिन पहले ही 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वाण हो गया. इस प्रकार मान्यवर कांशीराम बौद्ध धर्मान्तरण की अपनी की हुई भविष्यवाणी पूर्ण नहीं कर सके.
डॉ. अम्बेडकर प्रणीत नवबौद्धों के आन्दोलन के मुखिया मान्यवर कांशीराम की शिष्या कुमारी मायावती वर्ष 1995, 1997, 2002 और 2007 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने मान्यवर कांशीराम के उत्तराधिकार को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1997 ई. में सुप्रसिद्ध इन बौद्ध तीर्थ-स्थलों के नाम पर नवीन जिलों का गठन किया. तीर्थ-स्थलों के नाम पर नवनिर्मित जनपदों की ही प्राथमिक प्रेरणा से तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने भगवान बुद्ध और उनकी माँ के नाम पर भी नये जिलों का गठन किया. इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के पुर्नरुद्धारक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर व उनकी पत्नी रमाबाई और उनके बौद्धमय भारत बनाने के सपने को साकार करने वाले मान्यवर कांशीराम के नाम पर भी नये जनपदों का निर्माण किया. बहन कुमारी मायावती ने भगवान बुद्ध के मानवतावादी श्रमण संस्कृति को अपना आदर्श बनाने वाले सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों के नाम पर भी नये जनपदों का गठन कर उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया.
इस प्रकार बहन कुमारी मायावती ने 20 सितम्बर सन् 1995 को सिद्धार्थ नगर की स्थापना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 25 मई सन् 1997 को जिला श्रावस्ती की स्थापना, 4 अप्रैल सन् 1997 को जिला कौशाम्बी और 22 मई सन् 1997 को पडरौना का नाम बदल कर कुशीनगर कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर दिनांक 6 मई सन् 1997 को जिला गौतम बुद्ध नगर की स्थापना एवं दिनांक 6 मई सन् 1997 को भगवान गौतम बुद्ध की माँ महामाया के नाम पर जिला महामाया नगर की स्थापना किया. बुद्धकाल में कण्णकुज्ज नगर के रूप में विख्यात बौद्ध तीर्थ-स्थल के परिक्षेत्र में 18 सितम्बर सन् 1997 को जिला कन्नौज की स्थापना किया. भारत में बौद्ध धर्म का पुर्नरुत्थान करने वाले डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और उनकी पत्नी के नाम पर नवनिर्मित जनपद डॉ. अम्बेडकर नगर (20 सितम्बर सन् 1995), भीम नगर (28 सितम्बर सन् 2011) एवं रमाबाई नगर (18 सितम्बर सन् 1997) का गठन किया. मान्यवर कांशीराम के नाम पर नवनिर्मित जनपद कांशीराम नगर (सन् 2009) और बौद्ध सिद्धान्तों एवं बौद्ध शब्दावली के नाम पर नवनिर्मित जनपद पंचशील नगर (28 सितम्बर सन् 2011) एवं प्रबुद्ध नगर (28 सितम्बर सन् 2011) का ऐतिहासिक गठन किया. इतना ही नहीं बल्कि श्रमण-संस्कृति को मानने वाले संतों-गुरूओं व महापुरुषों के नाम पर भी नवीन जिलों का गठन किया गया है जिसमें संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ज्योतिबाराव फूले नगर एवं छत्रपति शाहू जी महाराज नगर इत्यादि प्रमुख हैं.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्देशन में बौद्ध तीर्थ-स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संग्रहालय 1910 ई. में बौद्ध तीर्थ-स्थल सारनाथ (षिपत्तन मृगदाववन) में स्थापित हुआ था, जिसमें बुद्धकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के पुरावशेष संग्रहित हैं. सन् 1910 के बाद इस दिशा में किसी भी सरकार ने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया. पहली बार बहन कुमारी मायावती ने संग्रहालयों के विकास के क्रम में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य किया. 31 अगस्त 2002 को संग्रहालय निदेशालय के रूप में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना किया. राज्य संग्रहालय, बनारसी बाग, लखनउ के परिसर के पुराने भवन में इस निदेशालय को स्थापित किया गया. इस निदेशालय की स्थापना के पूर्व ही कुमारी मायावती जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी पुरातात्विक सम्पदा के संग्रह, संरक्षण, अभिलेखीकरण व प्रदर्शन के लिए एवं शोध के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनाँक 04 मई, 1997 को ‘राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर’ की स्थापना किया. पूर्वी उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास का हृदय स्थल रहा है. बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल लुम्बिनी, देवदह, कोलियों का रामग्राम एवं तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर इत्यादि इसी क्षेत्र से संबंधित हैं.
भारत के बौद्ध स्थलों में कुशीनगर (कुशीनारा) का प्रमुख स्थान है. भगवान बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अपनी चारिका पूर्ण करने के पश्चात कुशीनारा के उपवत्तन नामक शालवन में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, जिसे आज कुशीनगर कहा जाता है. इस पवित्र स्थल पर असंख्य पर्यटक एवं बौद्ध धर्मानुयायी प्रति वर्ष भगवान बुद्ध को श्रद्धाजंलि अर्पित करने आते हैं. कुशीनगर की धार्मिक महत्ता एवं समृद्ध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर ने कई देशों एवं विभागों को इस क्षेत्र में अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापित करने की प्रेरणा दी और परिणामस्वरूप यह स्थल सम्पूर्ण विश्व में आकर्षण का केन्द्र बन गया. कुशीनगर की पुरातात्विक सम्पदा सहित भारतीय संस्कृति को संकलित तथा सुरक्षित करने के उद्देश्य से कुमारी मायावती ने शासन द्वारा 04 मई, 1997 को कुशीनगर में ‘राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर’ की स्थापना किया.
भगवान बुद्ध की क्रीड़ास्थली एवं युवावस्था तक कर्मस्थली होने के कारण कपिलवस्तु भी बौद्ध तीर्थ-स्थल के रूप में प्रसिद्ध है. जिसकी पहचान सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित पिपरहवाँ नामक स्थान से की गयी है. जहाँ पर देश-विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पर्यटन हेतु आते हैं. पिपरहवाँ में ही बुद्ध के अस्थि-अवशेषों से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ. जिस पर ब्राह्मी एवं खरोष्ठी, दोनों लिपियों में लेख लिपिबद्ध हैं. बौद्ध तीर्थ-स्थल कपिलवस्तु की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए बौद्ध हैरिटेज सेन्टर, पिपरहवाँ की योजनान्तर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी ने ‘राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवाँ, सिद्धार्थनगर’ की स्थापना करवाया. इसी श्रृंखला में कुमारी मायावती ने रामपुर जनपद में ‘भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय’ का भी निर्माण करवाया. इस संग्रहालय के मुख्य द्वार पर डॉ. अम्बेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कालाक्रमानुसार लिपिबद्ध कर प्रदर्शित किया गया है.
शैक्षणिक विकास के क्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की दृष्टि से तकनीकी एवं प्रबंधन में डिग्री एवं डिप्लोमा देने वाले समस्त महाविद्यालयों को दो भागों में विभाजित कर उन्हें ‘गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय (Goutam Buddh Technical University) एवं ‘महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय (Mahamaya Technical University) से सम्बद्ध कर दिया. शिक्षा की दृष्टि से ‘महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना’ का निर्माण किया गया जिसके तहत प्रत्येक वर्ष लगभग पांच लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया. इसके अलावा ‘महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना’ के तहत बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है. डॉ. अम्बेडकर के नाम पर भी और इतना ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित और मानवता के लिए काम करने वाले और कई सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर सैकड़ों शैक्षणिक संस्थान खोले गये. कुमारी मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें संचालित किया गया, जिनके माध्यम से डॉ. अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने के लिए बल प्रदान किया गया.
बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अभिप्रेत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का भगवान बुद्ध के नाम पर मात्र नामकरण ही नहीं किया बल्कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रहने के लिये पंचशील आवासीय परिसर का निर्माण, परिसर में निर्मित महामाया शांति सरोवर के नाम से दर्शनीय स्थल का निर्माण, विश्वविद्यालय के मुख्य मार्ग का नामकरण सिद्धार्थ गौतम मार्ग, बाह्य परिधि मार्ग को बौद्ध परिपथ तथा आन्तरिक परिधि मार्ग को महामाया परिपथ का नाम दिया जाना, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का नामकरण महामाया द्वार और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में विपस्सना विद्या के अभ्यास हेतु महात्मा ज्योतिबाराव फूले विपस्सना ध्यान भावना केन्द्र की स्थापना इत्यादि का कार्य बहन कुमारी मायावती जी के बौद्ध धर्म के पुर्नरुत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कार्य है.
सामाजिक कल्याण के विकास के क्रम में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण की कई योजनाओं में भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित ‘बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय’ की नीति का अनुसरण किया है. भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के पुर्नरुद्धारक डॉ. अम्बेडकर के ‘समता मूलक समाज की स्थापना’ के सिद्धान्तों के आधार पर कुमारी मायावती जी ने अपनी योजनाएं निर्मित की और उन योजनाओं का नामकरण भगवान बुद्ध की मां महामाया व डॉ. अम्बेडकर के नाम पर किया. सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निर्मित योजनाओं का नामकरण भी बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में बहन जी के योगदान को परिभाषित करता है.
आवासीय व्यवस्था के विकास के क्रम में देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नवनिर्मित जनपद गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विकास कार्य किया गया. उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले नागारिकों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए ‘डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना’ का कार्यान्वयन भी बहन जी की सरकारों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और इतना ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की मां महामाया के नाम पर ‘महामाया सर्वजन आवास योजना’ का निर्माण किया गया और इस योजना के तहत समाज के सभी वर्गों को जो आवास विहीन थे, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया गया. इन योजनाओं के अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री कांशीराम जी के नाम पर निर्मित ‘मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना’ एवं ‘मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना’ के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आवासीय व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया गया.
पर्यटन की दृष्टि से बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं. उत्तर प्रदेश में अधिकांश विदेशी पर्यटकों का आवागमन बौद्ध तीर्थ-स्थलों के कारण ही होता है. बौद्ध तीर्थ-स्थलों की दृष्टि से पर्यटन का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘बौद्ध परिपथ से मथुरा और संकिसा को जोड़ने के क्रम में ब्रज परिपथ, सारनाथ के लिए वाराणसी-विन्ध्य परिपथ, श्रावस्ती के लिए लखनउ-अवध परिपथ का चिन्हांकन किया. पर्यटन के विकास के क्रम में इन परिपथों के विकास के लिए बहन जी ने विभिन्न योजनाएँ निर्मित की हैं.
सन् 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘बौद्ध परिपथ’ के महत्व को स्वीकारते हुए इसकी अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाने की प्राथमिकता दी गई और भगवान गौतम बुद्ध एवं बौद्ध परिपथ से जुड़े स्थानों के विकास के क्रम में गोरखपुर परिक्षेत्र में बौद्ध परिपथ का विकास विशेष रूप से किया गया. गोरखपुर परिक्षेत्र में भगवान बुद्ध से संबंधित राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण/ब्रिजवर्क कराया गया. इसके अलावा कुशीनगर में पर्यटक आवास गृह का विस्तारीकरण/उच्चीकरण, कपिलवस्तु में लैण्डस्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण, कपिलवस्तु में भारतीय बौद्ध महाविहार में यात्री निवास का निर्माण, बौद्ध हेरिटेज सेंटर/वाणिज्यिक परिसर का निर्माण, कपिलवस्तु में बौद्ध संग्रहालय का निर्माण, हेरिटेज पार्क एवं विपश्यना केन्द्र की स्थापना, बौद्ध कला वीथिका की स्थापना एवं कुशीनगर में हवाई पट्टी का निर्माण इत्यादि के कार्य अत्यन्त उल्लेखनीय हैं. फैज़ाबाद परिक्षेत्र में बौद्ध पर्यटन के विकास के क्रम में जनपद श्रावस्ती में स्थित बौद्ध तीर्थ-स्थल का विकास बड़े पैमाने पर किया गया.
वाराणसी परिक्षेत्र में बौद्ध पर्यटन के विकास हेतु बौद्ध तीर्थ-स्थल सारनाथ में तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी के निर्देश पर तमाम उल्लेखनीय कार्य किए गए. इस प्रकार हम देखते हैं कि वाराणसी एवं फैजाबाद परिक्षेत्र में बौद्ध परिपथ का विकास विशेष रूप से किया गया. पर्यटन-व्यवसाय एवं रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लखनउ में मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, चिनहट की स्थापना की गई.
लखनउ में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने एवं बौद्ध धर्म के पुर्नरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनउ में बौद्ध स्थापत्य के आधार पर कई बौद्ध विहारों एवं बौद्ध स्मारकों के निर्माण करवाये गये. उनमें बौद्ध विहार शान्ति उपवन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुजन नायक पार्क, रमाबाई मूलक चौक, रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की चौमुखी प्रतिमा, गोमती विहार खण्ड-1 इत्यादि प्रमुख स्थल ऐतिहासिक रूप से बहन जी योगदान को व्याख्यायित कर रहे हैं.
बौद्ध तीर्थ-स्थलों को जोड़ने के क्रम में ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन वाली ‘गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना’ का निर्माण किया गया. इस मार्ग के निर्माण हो जाने पर बौद्ध तीर्थ-स्थल संकिसा, सारनाथ एवं कुशीनगर की यात्रा आसान व सुलभ हो जाएगी. सड़क परिवहन के साथ ही साथ रेल परिवहन, जल परिवहन एवं उड्डयन परिवहन का विकास भी बौद्ध तीर्थ-स्थलों की दृष्टि से किया गया. नागारिक उड्डयन सेवा की दृष्टि से हवाई पट्टी श्रावस्ती, हवाई पट्टी गौतम बुद्ध नगर एवं अर्न्तराष्ट्रीय एयर पोर्ट कुशीनगर का निर्माण उल्लेखनीय है.
ब्रिटिश-भारत के कुछ महान अन्वेषकों ने और भारतीय पुरातत्व विभाग ने जिन पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कर, उन्हें बौद्ध तीर्थ-स्थल के रूप में घोषित किया उनमें से कुछ पर भारतीय सरकारों ने ध्यान दिया और उनका विकास भी किया परन्तु अपने मुख्यमन्त्रित्व काल में बहन कुमारी मायावती जी ने उन तीर्थ-स्थलों के परिक्षेत्र में बौद्ध तीर्थ-स्थलों के नाम पर नवीन जिलों का निमार्ण एवं भगवान बुद्ध व उनके महान अनुयायियों के नाम पर भी नवनिर्मित जिलों की स्थापना करके और भगवान बुद्ध की विचारधारा के आधार पर कई योजनाएँ निर्मित कर बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का ऐतिहासिक कार्य किया है.
उत्तर प्रदेश के नागरिकों के रहन-सहन, आचार-व्यवहार इत्यादि का अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ के लोग शताब्दियों से चली आ रही वर्णवाद, जातिवाद एवं छुआछूत इत्यादि की परम्परा से ग्रसित रहते थे परन्तु आधुनिक समय में जब नवबौद्धों द्वारा बुद्ध की शिक्षा-दीक्षा का प्रचार-प्रसार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तो इसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के ऐसे कई समुदाय हैं जो वर्णवाद, जातिवाद एवं छुआछूत इत्यादि जैसी कुरीतियों से उपर उठकर भगवान बुद्ध के आदर्शों पर आधारित अपनी संस्कृति के विकास में उन्नति कर रहे हैं. अंधविश्वास तथा ढोंग-ढकोसला एवं पाखण्डों के जाल से मुक्त होने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग अथक प्रयास कर रहे हैं. कुछ समुदायों के लोगों की पूजा-पाठ, रीति-रिवाज में बदलाव आया है. इन लोगों के शादी-विवाह एवं मृतक इत्यादि संस्कारों में भगवान बुद्ध के आदर्शों का परिपालन किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के कई समुदायों के लोगों ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को समाहित कर अपनी संस्कृति और संस्कारों में सुधार किया है. सामाजिक-राजनैतिक विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न समाजों और उनके द्वारा निर्मित राजनैतिक दलों के सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है. भौतिक विकास ही नहीं बल्कि धर्मिक, सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक व राजनैतिक विकास में सामन्जस्य स्थापित हुआ है.
– लेखक बौद्ध विद्वान हैं. एम.एससी/ एम.ए./ एम.फिल/पी.एचडी हैं. राजनीति में भी सक्रिय हैं.
नोट- यह आलेख दलित दस्तक के जनवरी, 2017 अंक की कवर स्टोरी का अंश है। बिना मैगजीन की अनुमति के इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता।
बाप-बेटे के बीच झगड़ा नहीं रगड़ा हो रहा है जो चुनाव से ऐन पहले सुलझ जाएगा
 समाजवादी पार्टी का झगड़ा जिसे मैं रगड़ा कह रहा हूं, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया है. दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश मेरा बेटा है उससे मतभेद दूर कर लेंगे. असल में मुलायम सिंह ने बाप-बेटे के रिश्ते की दुहाई देकर जो विश्वास जताया है वह विश्वास कभी टूटा ही नहीं था. आप पिछले तकरीबन तीन महीने जबसे समाजवादी पार्टी के परिवार का झगड़ा चल रहा है, कि मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए. इस बीच कभी भी न तो समाजवादी पार्टी के गुंडई की बात हुई न ही भ्रष्टाचार की, और न ही परिवारवाद की. बस बाप-बेटे और परिवार के बीच इमोशन झगड़े की चर्चा ही होती रही.
इस बीच चुनाव की तारीख घोषित होने तक यह ड्रामारूपी झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया. जब आर-पार की तयशुदा लड़ाई सामने आई तो एक चीज चौंकाने वाली यह थी कि 80 फीसदी लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए, जबकि जिस मुलायम सिंह ने इस पार्टी की नींव रखी और उसे अपने खून-पसीने से सींचा उनके साथ बस गिने-चुने लोग ही नजर आए. एक और बात ध्यान खिंचने वाली रही. युवा नेता अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े युवा नेता तो समझ में आते हैं लेकिन जब रेवती रमन सरीखे दर्जन भर पुराने नेता मुलायम सिंह को छोड़कर अखिलेश के पीछे चलते दिखते हैं तो यह बात समझ से परे है, क्योंकि ये वो लोग हैं, जिसे मुलायम सिंह ने आम ‘इंसान’ से ‘नेता’ बनाया. और ऐसे में जब मुलायम सिंह यादव पिता-पुत्र प्रेम और बेटे को समझा लेने की बात करते हैं तो सारा परिदृश्य साफ हो जाता है. यह साफ हो जाता है कि पटकथा रची हुई है जिसके पटाक्षेप का वक्त आ गया है.
यूपी चुनाव को लेकर एक और बात साफ है. इस चुनाव में बसपा को छोड़ कर अभी तक किसी के पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है. सपा इन पांच सालों में अपने ”लोगों” को फायदा पहुंचाने और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया. जबकि भाजपा के पास यूपी चुनाव के लिए न तो कोई चाल है, न चरित्र, न कोई चेहरा और न ही कोई मुद्दा.
समाजवादी पार्टी का झगड़ा जिसे मैं रगड़ा कह रहा हूं, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया है. दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश मेरा बेटा है उससे मतभेद दूर कर लेंगे. असल में मुलायम सिंह ने बाप-बेटे के रिश्ते की दुहाई देकर जो विश्वास जताया है वह विश्वास कभी टूटा ही नहीं था. आप पिछले तकरीबन तीन महीने जबसे समाजवादी पार्टी के परिवार का झगड़ा चल रहा है, कि मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए. इस बीच कभी भी न तो समाजवादी पार्टी के गुंडई की बात हुई न ही भ्रष्टाचार की, और न ही परिवारवाद की. बस बाप-बेटे और परिवार के बीच इमोशन झगड़े की चर्चा ही होती रही.
इस बीच चुनाव की तारीख घोषित होने तक यह ड्रामारूपी झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया. जब आर-पार की तयशुदा लड़ाई सामने आई तो एक चीज चौंकाने वाली यह थी कि 80 फीसदी लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए, जबकि जिस मुलायम सिंह ने इस पार्टी की नींव रखी और उसे अपने खून-पसीने से सींचा उनके साथ बस गिने-चुने लोग ही नजर आए. एक और बात ध्यान खिंचने वाली रही. युवा नेता अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े युवा नेता तो समझ में आते हैं लेकिन जब रेवती रमन सरीखे दर्जन भर पुराने नेता मुलायम सिंह को छोड़कर अखिलेश के पीछे चलते दिखते हैं तो यह बात समझ से परे है, क्योंकि ये वो लोग हैं, जिसे मुलायम सिंह ने आम ‘इंसान’ से ‘नेता’ बनाया. और ऐसे में जब मुलायम सिंह यादव पिता-पुत्र प्रेम और बेटे को समझा लेने की बात करते हैं तो सारा परिदृश्य साफ हो जाता है. यह साफ हो जाता है कि पटकथा रची हुई है जिसके पटाक्षेप का वक्त आ गया है.
यूपी चुनाव को लेकर एक और बात साफ है. इस चुनाव में बसपा को छोड़ कर अभी तक किसी के पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है. सपा इन पांच सालों में अपने ”लोगों” को फायदा पहुंचाने और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया. जबकि भाजपा के पास यूपी चुनाव के लिए न तो कोई चाल है, न चरित्र, न कोई चेहरा और न ही कोई मुद्दा. ”चुप रहता है पर चौंकाता है मायावती का वोटर”
 बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की और दावा किया कि वो प्रदेश में ”अकेले दम पर सरकार” बनाएंगी. विरोधियों ने उनके दावे पर प्रश्नचिन्ह लगाने में देर नहीं की लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को उनके बयानों में ”गंभीरता” नज़र आती है.
अख़बार जदीद ख़बर के संपादक मासूम मुरादाबादी कहते हैं, ”मायावती की पार्टी चुनाव के लिए तैयार है. बाक़ी दलों में टिकट बंटवारों का मुहुर्त नहीं आया है. समाजवादी पार्टी में सिर फुटव्वल हो रहा है. इसका समाजवादी पार्टी को नुक़सान पहुंचने का अंदेशा है.” हालांकि, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और बाकी नेता लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मुक़ाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है. सपा का अखिलेश यादव धड़ा भी दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश के विकास कार्यों के दम पर पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी. ये दोनों दल विभिन्न चुनाव सर्वेक्षणों का भी हवाला देते हैं तो मायावती बीजेपी और सपा के बीच ”गठजोड़” का आरोप लगाती हैं.
इस पर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह कहते हैं, ”आज़ादी के बाद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव है जिसे त्रिकोणीय कहा जा सकता है. फ़िलहाल ये कहना जोखिम भरा होगा कि सपा, बीएसपी और बीजेपी में से कौन जीत सकता है?” रामकृपाल सिंह की राय है कि मायावती की पार्टी के पास तैयारी के लिहाज़ से बढ़त है. और, उनका वोट बैंक भी स्थिर है.
वो कहते हैं, ”कई बार मायावती का वोट बैंक बहुत चौंकाता है. वजह ये है कि वो चुप रहता है. यही हाल अल्पसंख्यकों का भी है. अगर सपा पुराने स्वरुप में लड़ती तो भी एडवांटेज मायावती के पास था. वो ये भी कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का जो तबक़ा क़ानून-व्यवस्था को अहमियत देता है, वो भी मायावती का समर्थन कर सकता है.”
समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण भी बीएसपी की चुनाव पूर्व तैयारी को उसके लिए बढ़त की वजह बताते हैं. वो कहते हैं, ”मायावती की प्लानिंग बहुत सॉलिड है. मीडिया उसे देख नहीं पाती है. मायावती अनौपचारिक तौर पर बहुत पहले से अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी थीं. उनके उम्मीदवारों को काफ़ी समय मिला है.”
बीएसपी के उम्मीदवारों के चयन में जातिगत के साथ-साथ सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश साफ़ नज़र आती है. मायावती के मुताबिक़ उनकी पार्टी ने अनुसूचित जाति के 87, मुस्लिम समुदाय के 97, अन्य पिछड़ा वर्ग के 106 और 113 स्वर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं.
मायावती का ख़ास ज़ोर मुस्लिम-दलित समीकरण को साधने पर है. वो कहती हैं, ”मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अकेले मुस्लिम और दलित वोट के साथ आने से बीएसपी उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे.” सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर विरोधी मायावती के ऐसे बयानों पर सवालिया निशान लगाते हैं लेकिन वो इस आपत्ति को नज़रअंदाज़ करती हैं, और वोटरों को आगाह करती हैं, ”अल्पसंख्यक वोटर सपा के दोनों धड़ों और कांग्रेस को देकर बांटे नहीं.”
लेकिन क्या अल्पसंख्यक वोटर मायावती का साथ देंगे, इस सवाल पर रामकृपाल सिंह कहते हैं, ”वर्तमान में ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं. उसके सामने जब ये तस्वीर साफ़ होती है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, वो उसकी तरफ़ चला जाता है, चाहे वो बीएसपी हो या फिर सपा.”
वो कहते हैं कि सपा में जारी तकरार का फ़ायदा बीएसपी को मिल सकता है. रामकृपाल सिंह की राय है, ”मायावती के यहां परिवार में कोई झगड़ा नहीं है. मायावती को ये देखना नहीं है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए तब हम जारी करें. लगातार वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ही हूं जो बीजेपी को हरा सकती हूं.”
हालांकि मासूम मुरादाबादी की राय अलग है. उनका आंकलन है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है. वो कहते हैं, ”अगर सपा बंटी तो मुसलमानों का बड़ा हिस्सा अखिलेश के साथ जा सकता है. लेकिन फ़ायदा मायावती को भी मिलेगा.”
मासूम मुरादाबादी ये भी कहते हैं, ”मायावती ने मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं लेकिन इससे वोट मिलने की गारंटी नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमानों के साथ सत्ता बांटने की बात नहीं करती हैं.”
सवाल नोटबंदी का भी है. मायावती नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ लगातार आक्रामक रुख़ अपनाए हुए हैं. बीजेपी का दावा है कि नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल में मायावती की पार्टी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ की रैली में इस मुद्दे को लेकर मायावती पर ”हमला” कर चुके हैं. लेकिन बद्री नारायण की राय है कि नोटबंदी से परेशान हुए लोग बीएसपी का समर्थन कर सकते हैं. रामकृपाल सिंह कहते हैं, “मायावती के वोट बैंक का दृष्टिकोण बड़ा सा़फ है. जो 18 फ़ीसदी दलित हैं, उन्हें नोटबंदी और विकास से ज्यादा लेना देना नहीं है.” वो ये भी कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का जो तबक़ा क़ानून-व्यवस्था को अहमियत देता है, वो भी मायावती का समर्थन कर सकता है.
रामकृपाल सिंह की राय है, ”क़ानून व्यवस्था के मामले में मध्यवर्ग का बड़ा तबक़ा मायावती को मानता है. लेकिन उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ना मायवती का माइनस प्वाइंट है.” वहीं बद्री नारायण की राय में मायावती के ख़िलाफ़ जो बात जाती है, वो ये है कि वो अखिलेश यादव या फिर बीजेपी की तरह मध्य वर्ग तक अपनी ख़ास छवि नहीं गढ़ पाती हैं. उन्हें किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर पाने का नुक़सान भी हो सकता है.
वहीं, मायावती के विरोधी ये भी याद दिलाते हैं कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सकी थी. इसे लेकर मासूम मुरादाबादी कहते हैं, ”लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बहुत अंतर होता है. मुद्दे अलग होते हैं और नतीजे भी अलग होते हैं.” वो कहते हैं कि मायावती को भले ही कमतर करके आंका जा रहा हो लेकिन वो बढ़त बना सकती हैं.
– बीबीसी हिन्दी से साभार
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की और दावा किया कि वो प्रदेश में ”अकेले दम पर सरकार” बनाएंगी. विरोधियों ने उनके दावे पर प्रश्नचिन्ह लगाने में देर नहीं की लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को उनके बयानों में ”गंभीरता” नज़र आती है.
अख़बार जदीद ख़बर के संपादक मासूम मुरादाबादी कहते हैं, ”मायावती की पार्टी चुनाव के लिए तैयार है. बाक़ी दलों में टिकट बंटवारों का मुहुर्त नहीं आया है. समाजवादी पार्टी में सिर फुटव्वल हो रहा है. इसका समाजवादी पार्टी को नुक़सान पहुंचने का अंदेशा है.” हालांकि, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और बाकी नेता लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मुक़ाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है. सपा का अखिलेश यादव धड़ा भी दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश के विकास कार्यों के दम पर पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी. ये दोनों दल विभिन्न चुनाव सर्वेक्षणों का भी हवाला देते हैं तो मायावती बीजेपी और सपा के बीच ”गठजोड़” का आरोप लगाती हैं.
इस पर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह कहते हैं, ”आज़ादी के बाद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव है जिसे त्रिकोणीय कहा जा सकता है. फ़िलहाल ये कहना जोखिम भरा होगा कि सपा, बीएसपी और बीजेपी में से कौन जीत सकता है?” रामकृपाल सिंह की राय है कि मायावती की पार्टी के पास तैयारी के लिहाज़ से बढ़त है. और, उनका वोट बैंक भी स्थिर है.
वो कहते हैं, ”कई बार मायावती का वोट बैंक बहुत चौंकाता है. वजह ये है कि वो चुप रहता है. यही हाल अल्पसंख्यकों का भी है. अगर सपा पुराने स्वरुप में लड़ती तो भी एडवांटेज मायावती के पास था. वो ये भी कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का जो तबक़ा क़ानून-व्यवस्था को अहमियत देता है, वो भी मायावती का समर्थन कर सकता है.”
समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण भी बीएसपी की चुनाव पूर्व तैयारी को उसके लिए बढ़त की वजह बताते हैं. वो कहते हैं, ”मायावती की प्लानिंग बहुत सॉलिड है. मीडिया उसे देख नहीं पाती है. मायावती अनौपचारिक तौर पर बहुत पहले से अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी थीं. उनके उम्मीदवारों को काफ़ी समय मिला है.”
बीएसपी के उम्मीदवारों के चयन में जातिगत के साथ-साथ सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश साफ़ नज़र आती है. मायावती के मुताबिक़ उनकी पार्टी ने अनुसूचित जाति के 87, मुस्लिम समुदाय के 97, अन्य पिछड़ा वर्ग के 106 और 113 स्वर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं.
मायावती का ख़ास ज़ोर मुस्लिम-दलित समीकरण को साधने पर है. वो कहती हैं, ”मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अकेले मुस्लिम और दलित वोट के साथ आने से बीएसपी उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे.” सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर विरोधी मायावती के ऐसे बयानों पर सवालिया निशान लगाते हैं लेकिन वो इस आपत्ति को नज़रअंदाज़ करती हैं, और वोटरों को आगाह करती हैं, ”अल्पसंख्यक वोटर सपा के दोनों धड़ों और कांग्रेस को देकर बांटे नहीं.”
लेकिन क्या अल्पसंख्यक वोटर मायावती का साथ देंगे, इस सवाल पर रामकृपाल सिंह कहते हैं, ”वर्तमान में ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं. उसके सामने जब ये तस्वीर साफ़ होती है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, वो उसकी तरफ़ चला जाता है, चाहे वो बीएसपी हो या फिर सपा.”
वो कहते हैं कि सपा में जारी तकरार का फ़ायदा बीएसपी को मिल सकता है. रामकृपाल सिंह की राय है, ”मायावती के यहां परिवार में कोई झगड़ा नहीं है. मायावती को ये देखना नहीं है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए तब हम जारी करें. लगातार वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ही हूं जो बीजेपी को हरा सकती हूं.”
हालांकि मासूम मुरादाबादी की राय अलग है. उनका आंकलन है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है. वो कहते हैं, ”अगर सपा बंटी तो मुसलमानों का बड़ा हिस्सा अखिलेश के साथ जा सकता है. लेकिन फ़ायदा मायावती को भी मिलेगा.”
मासूम मुरादाबादी ये भी कहते हैं, ”मायावती ने मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं लेकिन इससे वोट मिलने की गारंटी नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमानों के साथ सत्ता बांटने की बात नहीं करती हैं.”
सवाल नोटबंदी का भी है. मायावती नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ लगातार आक्रामक रुख़ अपनाए हुए हैं. बीजेपी का दावा है कि नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल में मायावती की पार्टी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ की रैली में इस मुद्दे को लेकर मायावती पर ”हमला” कर चुके हैं. लेकिन बद्री नारायण की राय है कि नोटबंदी से परेशान हुए लोग बीएसपी का समर्थन कर सकते हैं. रामकृपाल सिंह कहते हैं, “मायावती के वोट बैंक का दृष्टिकोण बड़ा सा़फ है. जो 18 फ़ीसदी दलित हैं, उन्हें नोटबंदी और विकास से ज्यादा लेना देना नहीं है.” वो ये भी कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का जो तबक़ा क़ानून-व्यवस्था को अहमियत देता है, वो भी मायावती का समर्थन कर सकता है.
रामकृपाल सिंह की राय है, ”क़ानून व्यवस्था के मामले में मध्यवर्ग का बड़ा तबक़ा मायावती को मानता है. लेकिन उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ना मायवती का माइनस प्वाइंट है.” वहीं बद्री नारायण की राय में मायावती के ख़िलाफ़ जो बात जाती है, वो ये है कि वो अखिलेश यादव या फिर बीजेपी की तरह मध्य वर्ग तक अपनी ख़ास छवि नहीं गढ़ पाती हैं. उन्हें किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर पाने का नुक़सान भी हो सकता है.
वहीं, मायावती के विरोधी ये भी याद दिलाते हैं कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सकी थी. इसे लेकर मासूम मुरादाबादी कहते हैं, ”लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बहुत अंतर होता है. मुद्दे अलग होते हैं और नतीजे भी अलग होते हैं.” वो कहते हैं कि मायावती को भले ही कमतर करके आंका जा रहा हो लेकिन वो बढ़त बना सकती हैं.
– बीबीसी हिन्दी से साभार गुजरात के चुनाव एवं आदिवासी समस्याएं
 गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हो गये हैं. ये चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं वहीं दूसरों दलों को भाजपा को हराने की सकारात्मक संभावनाएं दिखाई दे रही है. पिछले तीन चुनावों से शानदार जीत का सेहरा बांधने वाली भाजपा के लिए आखिर ये चुनाव चुनौती क्यों बन रहे हैं? एक अहम प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशना जरूरी है. इस बार गुजरात के इन चुनावों में आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका हो सकती है. मैं पिछले चार चुनावों से गुजरात के बड़ौदा एवं छोटा उदयपुर से जुड़े आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं. आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में मैं आदिवासी समस्याओं और उनके समाधान में सकारात्मक वातावरण को निर्मित करने की आवश्यकता महसूस करता हूं.
आजादी के सात दशक बाद भी गुजरात के आदिवासी उपेक्षित, शोषित और पीड़ित नजर आते हैं. राजनीतिक पार्टियां और नेता आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते. आज इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार एवं विकास का जो वातावरण निर्मित होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है, इस पर चिंतन अपेक्षित है. अक्सर आदिवासियों की अनदेखी कर तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने वाली बातों को हवा देना एक परम्परा बन गयी है. इस परम्परा को बदले बिना देश को वास्तविक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं किया जा सकता. देश के विकास में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को सही अर्थां में स्वीकार करना वर्तमान की बड़ी जरूरत है और इसके लिए चुनाव का समय निर्णायक होता है.
गुजरात में अभी भी आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक जैसा जीवनयापन कर रहे हैं. नक्सलवाद हो या अलगाववाद, पहले शिकार आदिवासी ही होते हैं. नक्सलवाद की समस्या आतंकवाद से कहीं बड़ी है. आतंकवाद आयातित है, जबकि नक्सलवाद देश की आंतरिक समस्या है. यह समस्या देश को अंदर ही अंदर घुन की तरह खोखला करती जा रही है. नक्सली अत्याधुनिक विदेशी हथियारों और विस्फोटकों से लैस होते जा रहे हैं. नक्सली सरकारों को मजबूती के साथ आंख भी दिखा रहे हैं. राजनीतिक पार्टियों को बाहरी ताकतों से लड़ने की बातें छोड़कर पहले देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास और रणनीति बनाना चाहिए. उनके वादे देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने के होने चाहिए. केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करती है. इसके बाद भी 7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है. स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए वे आज भी तरस रहे हैं.
गुजरात को हम भले ही समृद्ध एवं विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल कर लें, लेकिन यहां आदिवासी अब भी समाज की मुख्य धारा से कटे नजर आते हैं. इसका फायदा उठाकर मध्यप्रदेश से सटे नक्सली उन्हें अपने से जोड़ लेते हैं. सरकार आदिवासियों को लाभ पहुँचाने के लिए उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझे बिना ही योजना बना लेती हैं. ऐसी योजनाओं का आदिवासियों को लाभ नहीं होता, अलबत्ता योजना बनाने वाले जरूर फायदे में रहते हैं. महंगाई के चलते आज आदिवासी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं. वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं. अतः गुजरात की बहुसंख्य आबादी आदिवासियों पर विशेष ध्यान देना होगा.
अब जबकि आदिवासी क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर जागृति का माहौल बना है और कुछ शिक्षा के अधिकार का कानून भी आ गया है और यह अपने क्रियान्वयन की तरफ अग्रसर है तो यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आदिवासी बच्चों की स्थिति में इससे क्या बदलाव आता है. जो पिछले 70 सालों में नहीं आ पाया. आदिवासी समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति काफी बुरी है. आदिवासी समुदाय में शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल आबादी का 10 प्रतिशत से भी कम प्राथमिक से आगे की पढ़ाई कर पाए हैं. सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों को इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनानी चाहिए. जैसाकि मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर में सुखी परिवार फाउंडेशन के द्वारा गणि राजेन्द्र विजयजी के नेतृत्व में बालिका शिक्षा एवं शिक्षा की दृष्टि से एक अभिनव क्रांति घटित हुई है. लेकिन आदिवासी समुदाय की शिक्षा राज्य एवं केन्द्र सरकार के लिए एक चुनौती का प्रश्न है. आदिवासी समुदाय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना एवं इसे सुनिश्चित करना जरूरी है. यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमें समग्रता से हल ढूंढना होगा, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम उन समस्याओं को सुलझाएं जिनके कारण आदिवासी बच्चों का स्कूलों में ठहराव नहीं हो पा रहा है, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा, पाठशाला से बाहर होने की दर, खासकर लड़कियों में लगातार बढ़ती जा रही है. बच्चे घरों में, होटलों या ढाबों पर या खेतों के काम कर रहे हैं. कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल हमें समस्या की जड़ तक ले जाएगा. इससे निपटने के लिए समाज, राज्य एवं केन्द्र को सघन प्रयास करने होंगे.
हमें यह समझना होगा कि एक मात्र शिक्षा की जागृति से ही आदिवासियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा. बदलाव के लिए जरूरत है उनकी कुछ मूल समस्याओं के हल ढूंढना. कोई परिवार ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे स्कूल जाने के बजाये काम करें. ऐसे समुदाय जिन्हें विकास की सीमाओं पर छोड़ दिया गया है वो सारा दिन अपनी पूरी ताकत से सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि वो दो वक्त का भोजन जुटा सकें पर कई बार इसमें भी सफल नहीं हो पाते हैं. अशिक्षा की समस्या एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जड़ काफी गहरी जमीं हुई है. नीतियों ओर कानून बना देने से ही ये समस्या हल हो जाएगी ये एक बचकानी सोच है. इसके लिए पहले हमें उन कारणों को समझना होगा जिनकी वजह से बच्चों को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है. इसकी जड़ में वो व्यवस्था है जो व्यक्ति एवं समुदायों को आम और खास में बांटता है. अब इस व्यवस्था के परिवर्तन की बात होनी चाहिए.
आदिवासियों की खुदकी एक अपनी सभ्यता और संस्कृति है जिसमे वह जीते हैं. उनका एक तौर तरीका है, उनका रहन सहन खुद का है, भाषा है, बोली है, संस्कृति है तथा अपना एक अलग तरीका है जीवन को जीने तथा समझने का, वो जिस हालत में हैं, वो खुश हैं उनके अपने स्कूल या शिक्षा तंत्र हैं, उनके खुद के खेल या प्रथाएं हैं, खुद के ही देवी देवता हैं तथा खुद की ही परंपरा और सभ्यता है. इसी तरह सदियों से जंगल में रहते हुए उन्होंने खुद का ही एक स्वास्थ्य का या उपचार करने का तंत्र भी है जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तथाकथित विकसित स्वास्थ्य सेवाओं से वे आज भी वंचित हैं. आज भी उनके बच्चों का जन्म परम्परागत तरीकों से ही दाई ही करती है. बुखार या ऐसी ही छोटी-मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों की शरण नहीं लेते. इस तरह सरकार द्वारा उनके लिए जो सुविधाएं एवं सेवाएं सुलभ करायी जा रही हैं उनका वे लाभ नहीं ले पा रहे हैं. तकलीफ और परेशानी में जीना उनकी आदत सी है. ऐसी स्थितियों से उन्हें मुक्ति दिलाना वर्तमान समय की बहुत अपेक्षा है.
भारत के जंगल समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से भी. देश के जंगलों की कीमत खरबों रुपये आंकी गई है. ये भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तो कम है लेकिन कनाडा, मेक्सिको और रूस जैसे देशों के सकल उत्पाद से ज्यादा है. इसके बावजूद यहां रहने वाले आदिवासियों के जीवन में आर्थिक दुश्वारियां मुंह बाये खड़ी रहती हैं. आदिवासियों की विडंबना यह है कि जंगलों के औद्योगिक इस्तेमाल से सरकार का खजाना तो भरता है लेकिन इस आमदनी के इस्तेमाल में स्थानीय आदिवासी समुदायों की भागीदारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. जंगलों के बढ़ते औद्योगिक उपयोग ने आदिवासियों को जंगलों से दूर किया है. आर्थिक जरूरतों की वजह से आदिवासी जनजातियों के एक वर्ग को शहरों का रुख करना पड़ा है. विस्थापन और पलायन ने आदिवासी संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज और संस्कार को बहुत हद तक प्रभावित किया है. गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते आज का विस्थापित आदिवासी समाज, खासतौर पर उसकी नई पीढ़ी, अपनी संस्कृति से लगातार दूर होती जा रही है. आधुनिक शहरी संस्कृति के संपर्क ने आदिवासी युवाओं को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां वे न तो अपनी संस्कृति बचा पा रहे हैं और न ही पूरी तरह मुख्यधारा में ही शामिल हो पा रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी कॉर्निवल में आदिवासी उत्थान और उन्नयन की चर्चाएं की और वे इस समुदाय के विकास के लिए तत्पर भी हैं.
आदिवासियों का हित केवल आदिवासी समुदाय का हित नहीं है प्रत्युतः सम्पूर्ण देश व समाज के कल्याण का मुद्दा है जिस पर व्यवस्था से जुड़े तथा स्वतन्त्र नागरिकों को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए. और इस बार के गुजरात चुनाव इसकी एक सार्थक पहल बनकर प्रस्तुत हो, यह अपेक्षित है.
– लेखक गुजरात से लोकसभा सांसद हैं.
गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हो गये हैं. ये चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं वहीं दूसरों दलों को भाजपा को हराने की सकारात्मक संभावनाएं दिखाई दे रही है. पिछले तीन चुनावों से शानदार जीत का सेहरा बांधने वाली भाजपा के लिए आखिर ये चुनाव चुनौती क्यों बन रहे हैं? एक अहम प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशना जरूरी है. इस बार गुजरात के इन चुनावों में आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका हो सकती है. मैं पिछले चार चुनावों से गुजरात के बड़ौदा एवं छोटा उदयपुर से जुड़े आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं. आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में मैं आदिवासी समस्याओं और उनके समाधान में सकारात्मक वातावरण को निर्मित करने की आवश्यकता महसूस करता हूं.
आजादी के सात दशक बाद भी गुजरात के आदिवासी उपेक्षित, शोषित और पीड़ित नजर आते हैं. राजनीतिक पार्टियां और नेता आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते. आज इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार एवं विकास का जो वातावरण निर्मित होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है, इस पर चिंतन अपेक्षित है. अक्सर आदिवासियों की अनदेखी कर तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने वाली बातों को हवा देना एक परम्परा बन गयी है. इस परम्परा को बदले बिना देश को वास्तविक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं किया जा सकता. देश के विकास में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को सही अर्थां में स्वीकार करना वर्तमान की बड़ी जरूरत है और इसके लिए चुनाव का समय निर्णायक होता है.
गुजरात में अभी भी आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक जैसा जीवनयापन कर रहे हैं. नक्सलवाद हो या अलगाववाद, पहले शिकार आदिवासी ही होते हैं. नक्सलवाद की समस्या आतंकवाद से कहीं बड़ी है. आतंकवाद आयातित है, जबकि नक्सलवाद देश की आंतरिक समस्या है. यह समस्या देश को अंदर ही अंदर घुन की तरह खोखला करती जा रही है. नक्सली अत्याधुनिक विदेशी हथियारों और विस्फोटकों से लैस होते जा रहे हैं. नक्सली सरकारों को मजबूती के साथ आंख भी दिखा रहे हैं. राजनीतिक पार्टियों को बाहरी ताकतों से लड़ने की बातें छोड़कर पहले देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास और रणनीति बनाना चाहिए. उनके वादे देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने के होने चाहिए. केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करती है. इसके बाद भी 7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है. स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए वे आज भी तरस रहे हैं.
गुजरात को हम भले ही समृद्ध एवं विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल कर लें, लेकिन यहां आदिवासी अब भी समाज की मुख्य धारा से कटे नजर आते हैं. इसका फायदा उठाकर मध्यप्रदेश से सटे नक्सली उन्हें अपने से जोड़ लेते हैं. सरकार आदिवासियों को लाभ पहुँचाने के लिए उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझे बिना ही योजना बना लेती हैं. ऐसी योजनाओं का आदिवासियों को लाभ नहीं होता, अलबत्ता योजना बनाने वाले जरूर फायदे में रहते हैं. महंगाई के चलते आज आदिवासी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं. वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं. अतः गुजरात की बहुसंख्य आबादी आदिवासियों पर विशेष ध्यान देना होगा.
अब जबकि आदिवासी क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर जागृति का माहौल बना है और कुछ शिक्षा के अधिकार का कानून भी आ गया है और यह अपने क्रियान्वयन की तरफ अग्रसर है तो यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आदिवासी बच्चों की स्थिति में इससे क्या बदलाव आता है. जो पिछले 70 सालों में नहीं आ पाया. आदिवासी समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति काफी बुरी है. आदिवासी समुदाय में शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल आबादी का 10 प्रतिशत से भी कम प्राथमिक से आगे की पढ़ाई कर पाए हैं. सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों को इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनानी चाहिए. जैसाकि मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर में सुखी परिवार फाउंडेशन के द्वारा गणि राजेन्द्र विजयजी के नेतृत्व में बालिका शिक्षा एवं शिक्षा की दृष्टि से एक अभिनव क्रांति घटित हुई है. लेकिन आदिवासी समुदाय की शिक्षा राज्य एवं केन्द्र सरकार के लिए एक चुनौती का प्रश्न है. आदिवासी समुदाय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना एवं इसे सुनिश्चित करना जरूरी है. यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमें समग्रता से हल ढूंढना होगा, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम उन समस्याओं को सुलझाएं जिनके कारण आदिवासी बच्चों का स्कूलों में ठहराव नहीं हो पा रहा है, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा, पाठशाला से बाहर होने की दर, खासकर लड़कियों में लगातार बढ़ती जा रही है. बच्चे घरों में, होटलों या ढाबों पर या खेतों के काम कर रहे हैं. कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल हमें समस्या की जड़ तक ले जाएगा. इससे निपटने के लिए समाज, राज्य एवं केन्द्र को सघन प्रयास करने होंगे.
हमें यह समझना होगा कि एक मात्र शिक्षा की जागृति से ही आदिवासियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा. बदलाव के लिए जरूरत है उनकी कुछ मूल समस्याओं के हल ढूंढना. कोई परिवार ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे स्कूल जाने के बजाये काम करें. ऐसे समुदाय जिन्हें विकास की सीमाओं पर छोड़ दिया गया है वो सारा दिन अपनी पूरी ताकत से सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि वो दो वक्त का भोजन जुटा सकें पर कई बार इसमें भी सफल नहीं हो पाते हैं. अशिक्षा की समस्या एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जड़ काफी गहरी जमीं हुई है. नीतियों ओर कानून बना देने से ही ये समस्या हल हो जाएगी ये एक बचकानी सोच है. इसके लिए पहले हमें उन कारणों को समझना होगा जिनकी वजह से बच्चों को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है. इसकी जड़ में वो व्यवस्था है जो व्यक्ति एवं समुदायों को आम और खास में बांटता है. अब इस व्यवस्था के परिवर्तन की बात होनी चाहिए.
आदिवासियों की खुदकी एक अपनी सभ्यता और संस्कृति है जिसमे वह जीते हैं. उनका एक तौर तरीका है, उनका रहन सहन खुद का है, भाषा है, बोली है, संस्कृति है तथा अपना एक अलग तरीका है जीवन को जीने तथा समझने का, वो जिस हालत में हैं, वो खुश हैं उनके अपने स्कूल या शिक्षा तंत्र हैं, उनके खुद के खेल या प्रथाएं हैं, खुद के ही देवी देवता हैं तथा खुद की ही परंपरा और सभ्यता है. इसी तरह सदियों से जंगल में रहते हुए उन्होंने खुद का ही एक स्वास्थ्य का या उपचार करने का तंत्र भी है जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तथाकथित विकसित स्वास्थ्य सेवाओं से वे आज भी वंचित हैं. आज भी उनके बच्चों का जन्म परम्परागत तरीकों से ही दाई ही करती है. बुखार या ऐसी ही छोटी-मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों की शरण नहीं लेते. इस तरह सरकार द्वारा उनके लिए जो सुविधाएं एवं सेवाएं सुलभ करायी जा रही हैं उनका वे लाभ नहीं ले पा रहे हैं. तकलीफ और परेशानी में जीना उनकी आदत सी है. ऐसी स्थितियों से उन्हें मुक्ति दिलाना वर्तमान समय की बहुत अपेक्षा है.
भारत के जंगल समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से भी. देश के जंगलों की कीमत खरबों रुपये आंकी गई है. ये भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तो कम है लेकिन कनाडा, मेक्सिको और रूस जैसे देशों के सकल उत्पाद से ज्यादा है. इसके बावजूद यहां रहने वाले आदिवासियों के जीवन में आर्थिक दुश्वारियां मुंह बाये खड़ी रहती हैं. आदिवासियों की विडंबना यह है कि जंगलों के औद्योगिक इस्तेमाल से सरकार का खजाना तो भरता है लेकिन इस आमदनी के इस्तेमाल में स्थानीय आदिवासी समुदायों की भागीदारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. जंगलों के बढ़ते औद्योगिक उपयोग ने आदिवासियों को जंगलों से दूर किया है. आर्थिक जरूरतों की वजह से आदिवासी जनजातियों के एक वर्ग को शहरों का रुख करना पड़ा है. विस्थापन और पलायन ने आदिवासी संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज और संस्कार को बहुत हद तक प्रभावित किया है. गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते आज का विस्थापित आदिवासी समाज, खासतौर पर उसकी नई पीढ़ी, अपनी संस्कृति से लगातार दूर होती जा रही है. आधुनिक शहरी संस्कृति के संपर्क ने आदिवासी युवाओं को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां वे न तो अपनी संस्कृति बचा पा रहे हैं और न ही पूरी तरह मुख्यधारा में ही शामिल हो पा रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी कॉर्निवल में आदिवासी उत्थान और उन्नयन की चर्चाएं की और वे इस समुदाय के विकास के लिए तत्पर भी हैं.
आदिवासियों का हित केवल आदिवासी समुदाय का हित नहीं है प्रत्युतः सम्पूर्ण देश व समाज के कल्याण का मुद्दा है जिस पर व्यवस्था से जुड़े तथा स्वतन्त्र नागरिकों को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए. और इस बार के गुजरात चुनाव इसकी एक सार्थक पहल बनकर प्रस्तुत हो, यह अपेक्षित है.
– लेखक गुजरात से लोकसभा सांसद हैं. शहीद उधम सिंह के परपोते को एक अदद नौकरी की तलाश
 यह खबर मुझे एक चैनल के वेबसाइट पर पढ़ने को मिली. हेडिंग थी- ‘जनरल डायर को मारने वाले शहीद उधम सिंह के परपोते को नहीं मिल रही चपरासी की नौकरी’ खबर पढकर मुझे लगा कि एक वीर शहीद के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। हो सकता है कि खबर लिखने वाले पत्रकार की ऐसी मंशा ना हो और उसने अपनी खबर को सनसनी बनाने के लिए यह हेडिंग दी हो, लेकिन चूंकि मैं क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के बलिदान के बारे में जानता हूं इसलिए मुझे यह खबर अखर गई. लेकिन पहले उधम सिंह के परपोते जग्गा सिंह के बारे में जानते हैं. फिर दूसरी बात.
यह खबर मुझे एक चैनल के वेबसाइट पर पढ़ने को मिली. हेडिंग थी- ‘जनरल डायर को मारने वाले शहीद उधम सिंह के परपोते को नहीं मिल रही चपरासी की नौकरी’ खबर पढकर मुझे लगा कि एक वीर शहीद के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। हो सकता है कि खबर लिखने वाले पत्रकार की ऐसी मंशा ना हो और उसने अपनी खबर को सनसनी बनाने के लिए यह हेडिंग दी हो, लेकिन चूंकि मैं क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के बलिदान के बारे में जानता हूं इसलिए मुझे यह खबर अखर गई. लेकिन पहले उधम सिंह के परपोते जग्गा सिंह के बारे में जानते हैं. फिर दूसरी बात.
शहीद उधम सिंह के परपोते पंजाब सरकार में नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. नौकरी के नाम पर वह दस साल से पंजाब सरकार द्वारा छले जा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 10 साल पहले उन्हें नौकरी देने का वादा किया था. वह इंतजार करते रहे, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा किया वादा; वादा ही रह गया. क्योंकि कांग्रेस तुरंत सत्ता से बाहर हो गई थी और उसके बाद की भाजपा-अकाली सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया. उधम सिंह की बड़ी बहन आस कौर के प्रपौत्र जग्गा सिंह द्वारा शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सरकार से बार-बार अपील किए जाने का अभी कोई परिणाम नहीं निकला है. यह साफ हो गया है कि भाजपा की सरकार का ‘राष्ट्रवाद’ शायद कुछ ‘खास योग्यता’ वाले लोगों के लिए ही है.
फिलहाल जग्गा सिंह एक दुकान में मजदूरी का काम करते हैं, जहां से उन्हें हर महीने मात्र 2500 रुपये मिलते हैं. इसी पैसे से वह अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ बेहद गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं. इसके अलावा उन्हें 60 वर्षीय पिता जीत सिंह की देखभाल भी करनी पड़ती है.
अब दूसरी बात, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है. जिन सरकारों ने उधम सिंह को उनके बलिदान के मुताबिक इज्जत नहीं दी, उनसे इस बात की उम्मीद लगाना कि वह उनके परपोते को नौकरी देगी, इसकी उम्मीद करना बेमानी है. और यह सरकार की दया है कि वह किसी को नौकरी देना चाहती है या नहीं. क्योंकि सिर्फ किसी का परपोता होने से कोई सरकारी नौकरी के योग्य नहीं हो जाता. लेकिन हां, जिस पंजाब से खबर आई है, मुझे वहां के लोगों से बात करनी है. मैंने सुना है कि पंजाब के लोग धनवान हैं. उनकी बड़ी-बड़ी कोठियां देखने लायक होती है. उस पंजाब के लखपति और करोड़पतियों से मेरा सवाल है कि क्या वो एक क्रांतिकारी के परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का इंतजाम नहीं कर सकते ?. क्या वह उन्हें 15-20 हजार रुपये महीने की नौकरी नहीं दे सकते ?
अगर पंजाब के लोग नहीं कर सकते तो क्या दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र के लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं? क्या समाज के समर्थ लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह एक क्रांतिकारी शहीद के नाम का मान रखते हुए उसके परिवार को मदद करे? अगर यह खबर पढ़ने के बाद किसी के दिमाग में यह सवाल आए कि उधम सिंह कौन थे तो उसके लिए बस इतना जानना काफी है कि उधम सिंह वह शेर थे, जिन्होंने अमृतसर के जलियावाला बाग में सैकड़ों लोगों को गोली मारने का आदेश देने वाले माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मार दी थी और अपनी माटी के अपमान का बदला लिया था. इससे ज्यादा जानना हो तो गूगल है ही.
क्या आप उस युद्ध के बारे में जानते हैं, जिसमें 500 अछूतों ने 28 हजार की पेशवा सेना को धूल चटा दी थी
 1 जनवरी सन् 1818 के दिन एक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसने दलित समाज के शौर्य को दुनिया भर में स्थापित किया था. मुख्यधारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कतराते रहे हैं. क्योंकि यह घटना जहां दलितों की शौर्यगाथा है तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर कालिख. बहुजन समाज के लोगों का इस घटना को जानना बहुत जरूरी है. इस महान गाथा में 500 नायकों ने हिस्सा लिया था. ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक हैं. इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे.
यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी. भारत में अंग्रेज़ी राज़ की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया. लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं-महाराजाओं को अंग्रेज़ी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था. अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि इस देश के ‘अछूत’ कहलाने वाले लोग थे. जानवरों सा जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी मिली तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए. इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वह देश के इतिहास में दर्ज है.
1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी. डॉ. अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस (अंग्रेज़ी) के खंड 12 में ‘द अनटचेबल्स एंड द पेक्स ब्रिटेनिका’ में इस तथ्य का वर्णन किया है. यह कोरेगांव की लड़ाई थी, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया. यहां 500 महार सैनिकों ने पेशवा राव के 28 हजार सैनिकों (घुड़सवारों एवं पैदल) की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत किया.
कोरेगांव भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है. 01 जनवरी 1818 को सर्द मौसम में एक ओर कुल 28 हजार सैनिकों जिनमें 20000 हजार घुड़सवार और 8000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई ‘पेशवा बाजीराव-II कर रहे थे तो दूसरी ओर ‘बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री’ के 500 ‘महार’ सैनिक, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे. आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28 हजार पेशवाओं को धूल चटा दिया. दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओर ‘ब्राह्मण राज’ बचाने की फिराक में ‘पेशवा’ थे तो दूसरी ओर ‘पेशवाओं’ के पशुवत ‘अत्याचारों’ से ‘बदला’ चुकाने की ‘फिराक’ में गुस्से से तमतमाए ‘महार’. आखिरकार इस घमासान युद्ध में ‘ब्रह्मा के मुख से पैदा’ हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई. 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी. भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुंचे. यह वीरता की मिसाल है. इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है. यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है. इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं, जो इस लड़ाई में मारे गए थे. 1851 में इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया.
दलित-आदिवासी समाज को अपने पूर्वज उन 500 महार सैनिकों को नमन करना चाहिए क्योंकि इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद ‘पेशवाई’ खतम हो गयी थी और ‘अंग्रेजों’ को इस भारत देश की ‘सत्ता’ मिली. इसके फलस्वरूप ‘अंग्रेजों’ ने इस भारत देश में ‘शिक्षण’ का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था. जिस तरह बाबासाहेब आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को कोरेगांव जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे, हमें भी उन वीरों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद कर गौरवान्वित होना चाहिए.
1 जनवरी सन् 1818 के दिन एक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसने दलित समाज के शौर्य को दुनिया भर में स्थापित किया था. मुख्यधारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कतराते रहे हैं. क्योंकि यह घटना जहां दलितों की शौर्यगाथा है तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर कालिख. बहुजन समाज के लोगों का इस घटना को जानना बहुत जरूरी है. इस महान गाथा में 500 नायकों ने हिस्सा लिया था. ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक हैं. इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे.
यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी. भारत में अंग्रेज़ी राज़ की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया. लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं-महाराजाओं को अंग्रेज़ी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था. अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि इस देश के ‘अछूत’ कहलाने वाले लोग थे. जानवरों सा जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी मिली तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए. इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वह देश के इतिहास में दर्ज है.
1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी. डॉ. अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस (अंग्रेज़ी) के खंड 12 में ‘द अनटचेबल्स एंड द पेक्स ब्रिटेनिका’ में इस तथ्य का वर्णन किया है. यह कोरेगांव की लड़ाई थी, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया. यहां 500 महार सैनिकों ने पेशवा राव के 28 हजार सैनिकों (घुड़सवारों एवं पैदल) की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत किया.
कोरेगांव भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है. 01 जनवरी 1818 को सर्द मौसम में एक ओर कुल 28 हजार सैनिकों जिनमें 20000 हजार घुड़सवार और 8000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई ‘पेशवा बाजीराव-II कर रहे थे तो दूसरी ओर ‘बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री’ के 500 ‘महार’ सैनिक, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे. आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28 हजार पेशवाओं को धूल चटा दिया. दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओर ‘ब्राह्मण राज’ बचाने की फिराक में ‘पेशवा’ थे तो दूसरी ओर ‘पेशवाओं’ के पशुवत ‘अत्याचारों’ से ‘बदला’ चुकाने की ‘फिराक’ में गुस्से से तमतमाए ‘महार’. आखिरकार इस घमासान युद्ध में ‘ब्रह्मा के मुख से पैदा’ हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई. 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी. भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुंचे. यह वीरता की मिसाल है. इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है. यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है. इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं, जो इस लड़ाई में मारे गए थे. 1851 में इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया.
दलित-आदिवासी समाज को अपने पूर्वज उन 500 महार सैनिकों को नमन करना चाहिए क्योंकि इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद ‘पेशवाई’ खतम हो गयी थी और ‘अंग्रेजों’ को इस भारत देश की ‘सत्ता’ मिली. इसके फलस्वरूप ‘अंग्रेजों’ ने इस भारत देश में ‘शिक्षण’ का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था. जिस तरह बाबासाहेब आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को कोरेगांव जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे, हमें भी उन वीरों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद कर गौरवान्वित होना चाहिए. शिक्षा और ज्ञान से डरता है धार्मिक भारत
 भारत के ग्रामीण या शहरी बच्चों से बात करके देखिये, वे बहुत कुछ जानना चाहते हैं. जैसी जिज्ञासा यूरोप के सभ्य समाज के बच्चे करते हैं वैसी ही जिज्ञासा भारत के बच्चे भी करते हैं. जीवन, मन, शरीर, प्रकृति, मशीनें, समाज व्यवस्था और संबंधों पर उनकी जिज्ञासाएं इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि उनको उत्तर देना कठिन हो जाता है. उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए अक्सर जिन लोगों को समाज द्वारा “अधिकृत” किया गया है उन्होंने इन जिज्ञासाओं की बहुत बारीकी से ह्त्या की है. उनकी जिज्ञासाओं को उत्तर देकर नयी जिज्ञासाओं और नये प्रश्नों की तरफ बढ़ाने का अर्थ होता है पुराने सामाजिक ताने बाने और धर्म से आगे बढना. लेकिन अगर आपका समाज किसी आखिरी किताब, आखिरी मसीहा या अपौरुषेय किताबों या विश्वगुरु होने के अहंकार से पीड़ित है तो इस अहंकार की ठीक बगल में एक भयानक डर से भी वह लगातार पीडित रहेगा. यही पूरे इस्लामिक जगत और भारत की कहानी है.
आसमानी या अपौरुषेय किताबों का या विश्वगुरु के अहंकार का आभामंडल इतना असुरक्षित और डरपोक होता है कि वो बच्चों और स्त्रियों के प्रश्नों से सबसे अधिक डरता है. इसीलिये ऐसे समाज के लोग पठन-पाठन का अधिकार अपनी बड़ी जनसंख्या को और स्त्रियों को नहीं देना चाहते. भारतीय होशियारों ने इस विषय में महारथ हासिल कर ली थी. उन्होंने इस काम लिये वर्ण और जाति व्यवस्था ही बना डाली थी और वर्णाश्रम को ही धर्म बना डाला था, और ये व्यव्वस्था उनके आधिपत्य को बनाये रखने के लिए यह बहुत हद तक सफल भी रही. अलबरूनी ने अपने यात्रा संस्मरणों में लिखा है कि काश भारत जैसी जाति व्यवस्था हमारे पास होती तो हम भी करोड़ों लोगों को सैकड़ों हजारों साल गुलाम रखकर निष्कंटक राज करते और दबी कुचली कौमें कोई आवाज भी न उठा पातीं. अलबरूनी की भारत से ये इर्ष्या बहुत महत्वपूर्ण है. वह स्वयं जिस समाज से आ रहे हैं वहां कभी ज्ञान के फूल खिले थे लेकिन बाद में सब रेगिस्तान हो गया.
भारत में भी श्रमणों (बौद्धों, जैनों), लोकायतों, आजीवकों के युग में ज्ञान विज्ञान की बहुत खोज हुई थी और आज गिनाई जाने वाली सारी सफलताएं उसी दौर की हैं. शून्य, रेखागणित, अंकशास्त्र, खगोल, व्याकरण, भेषज, धातुविज्ञान, आयुर्वेद, योग और मनोविज्ञान (जो कि अध्यात्म में पतित हुआ) की खोज श्रमणों अर्थात बौद्धों और जैनों ने की थी. तांत्रिक अनुशासन के साथ लोकायतों ने भारी काम किया था. लेकिन वेद वेदान्त के प्रसार के साथ ज्ञान विज्ञान की ये प्रेरणाएं समाप्त होने लगीं और खगोलशास्त्र ज्योतिष बन गया, रसायन और भेषज जादूगरी और राजगुरुओं की गोपनीय विद्या बन गयी और एक वर्ण विशेष के लोगों के रोजगार की चिंता ने समूचे दक्षिण एशिया की ज्ञान की परम्पराओं का नाश कर डाला. राजसत्ता और व्यापरसत्ता को लग्न, मुहूर्त, ज्योतिष और कर्मकांड से डराकर गुलाम बनाया गया और शेष समाज को अंधविश्वास के दलदल में ऐसा डुबोया कि वो आज तक बाहर नहीं निकल सका है. खगोल के ज्योतिष में पतन पर अलबरूनी ने विस्तार से चर्चा करते हुए गजब की टिप्पणियाँ की हैं, वे पढ़ने योग्य हैं.
भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों की बात एक तरफ रखते हुए हम अगर समाज विज्ञानों जैसे कला, भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और इतिहास लेखन सहित राजनीति, शासन प्रशासन की भी बातें करें तो हम देखते हैं कि इन विषयों का और अधिक बुरा हाल किया गया है. आज के बच्चे समाजशास्त्र, साहित्य, भाषा, मनोविज्ञान इतिहास या राजनीतिशास्त्र नहीं पढ़ना चाहते. जो बच्चे ये सब पढ़ते हैं उन्हें दयनीय, कमजोर और पिछड़ा समझा जाता है. विषयों की भी जातियां हैं भारत में. विज्ञान, तकनीक, मेनेजमेंट, मेडिसिन आदि सवर्ण विषय हैं और मानविकी,आर्ट्स आदि अछूत विषय हैं. इसी का स्वाभाविक परिणाम ये है कि हमारे स्कूल कैसे हों, राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, शासन प्रशासन का ढंग कैसा हो, पत्रकारिता, सामाजिक विमर्ष, नारीवाद, सबाल्टर्न विमर्श सहित संस्कृति और दर्शन का विमर्श कैसा हो-ये सब हमें यूरोप के सभ्य देशों से सीखना होता है.
याद कीजिये, डॉ. अम्बेडकर ने जो संविधान रचा वो पश्चिमी लोकतंत्र और समाजवाद से प्रेरणा लेता है. भारत के अतीत में भविष्य के समाज को दिशा देने लायक बातें लगभग न के बराबर हैं. आज की संसदीय प्रणाली से लेकर कानून, प्रशासन, चुनाव आदि सभी बातें यूरोप ने विकसित कीं और भारत के गुलामी के दौर में यूरोप अमेरिका में पढ़ने गये वकीलों ने इस देश को यूरोपीय सभ्यता के आदर्शों पर खड़ा किया. इसीलिये हम थोड़ा सा बदलाव, सामाजिक सुधार और विकास भारत में देख पाते हैं.
लेकिन भारत के स्वतंत्र होते ही और आत्मनिर्णय का अधिकार मिलते ही विश्वगुरु का जिन्न फिर से जाग गया. भूमि सुधारों और दलित आंदोलनों के दबाव से पुराने शोषक तिलमिला उठे और उन्होंने फिर से गुरुकुल स्टाइल मूर्खताओं की तारीफ़ शुरू कर दी और बहुत गहरे षड्यंत्र के तहत दलितों, शूद्रों (ओबीसी), आदिवासियों और स्त्रियों को ज्ञान से वंचित करने का काम आरंभ कर दिया. राष्ट्र निर्माण के लिए जितना जरुरी था उतना भर विज्ञान और तकनीक सीखने सिखाने का इन्तेजाम कर लिया. देश को प्रबंधन और तकनीक के बड़े बड़े संस्थान दिए गये लेकिन जनमानस में विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को रोकने के लिए गुप्त रूप से कहीं अधिक शक्ति लगाईं गयी.
आईआईटी और आईआईएम को देखिये. आईआईटी असल में तकनीक के संस्थान हैं. यहां विज्ञान के बाबू पैदा होते हैं जो विज्ञान और मशीनरी के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं. विज्ञान वे कितना जानते हैं इसका उत्तर इन संस्थानों के विद्यार्थियों को अब तक मिले नोबेल पुरस्कारों की संख्या से अंदाजा लगता है. लेकिन इतनी प्रशंसा उनकी की जा सकती है कि उनके यूरोपीय या अमेरीकी शिक्षक जब कुछ खोज लेते हैं तो वे उसका सस्ता संस्करण तैयार कर देते हैं. इतनी प्रतिभा उनमे जरुर है. ऐसे ही हमारे चिकित्सक और मैनेजर हैं. वे नया कुछ नहीं खोज सकते लेकिन एक बार ह्रदय का किडनी का मस्तिष्क के काम करने के विज्ञान को कोई यूरोपीय या अमेरिकन खोज ले तो उसके बाद हमारे डाक्टर आँख, नाक, ह्रदय के आपरेशन का या नसबंदी का विश्वरिकार्ड बना लेते हैं. इस बात के लिए उनकी प्रशंसा हो सकती है.
क्या समाज विज्ञान, मानविकी में भारत कुछ बेहतर कर रहा है? उत्तर है कि समाज विज्ञानों को समझने की भारत की तैयारी ही नहीं है. हजारों साल के विविधतापूर्ण सामाजिक इतिहास में समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान को जन्म दे सकने वाले धार्मिक-सामाजिक बदलाव, आक्रमण, युद्ध, राजनीतिक परिवर्तन आदि घटनाएँ घटती रहीं लेकिन यहाँ समाज विज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ. यूरोप में पुनर्जागरण के बाद औद्योगीकरण और नगरीकरण की छाया में समाजशास्त्र का जन्म हुआ लेकिन भारत में ऐसा बहुत कुछ हो चुकने के बाद भी समाज विज्ञान की कोई प्रेरणा नहीं हुई. ये एक चमत्कार है. भारत के धर्म और अध्यात्म ने नये ज्ञान की संभावना और नए समाज की प्रेरणा को बहुत खूबसूरती से और कुशलता से नष्ट किया है. देश के मानव संसाधन को कैसे नष्ट किया जाता है ये कोई भारत से सीखे. आज मानविकी विषयो में भारत की मौलिक रिसर्च बहुत ही कम है. हां, भारत के समाज, राजनीति और संस्कृति के संबंध में भारतीय लोग लिखते लिखाते रहते हैं लेकिन उनका ये लेखन या शोध विश्व स्तर पर ज्ञान को बढ़ाने में कोई ख़ास योगदान नहीं देता है.
आधुनिक युग के सभी बड़े सिद्धांतकार यूरोपीय हैं. राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, लोकतंत्र, शासन, प्रशासन, पत्रकारिता, व्यापार प्रबंधन, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा व्यवस्था, रिसर्च और यहां तक कि अब वैज्ञानिक अध्यात्म विद्या और कांशियसनेस स्टडीज जैसे एकदम नये विषय भी यूरोप से ही आ रहे हैं. और मजा ये कि भारतीय समाज उसपर भी अपना “सनातन अधिकार” जमाते हुए यह कह रहा है कि ये सब तो हमारे शास्त्रों में न जाने कब से लिखा हुआ है.
भारत में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को गौर से देखिये वे इन प्रश्नों पर ज़रा भी जागरूक नहीं हैं. उपर उपर से लगता है कि वे अनजान हैं. लेकिन थोड़ा कुरेदो तो पता चलेगा कि वे एक बहुत बड़े और प्राचीनतम षड्यंत्र के पुर्जे हैं. उन्हें पता है शिक्षा और ज्ञान को कैसे बर्बाद करना है और शोषक धर्म की सत्ता को कैसे बनाये रखना है. बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल कालेज के लोगों से बात कीजिये आपको लगेगा कि ये किस जमाने के जीवाश्म हैं जो अभी भी जीये जा रहे हैं. ग्रामीण बच्चों की तकदीर जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों के स्तर की तो बात ही करना व्यर्थ है. ऊपर से धर्म और राष्ट्रवाद की जहरीली खिचड़ी ने उन्हें एकदम पागल बना दिया है.
भारत के ग्रामीण या शहरी बच्चों से बात करके देखिये, वे बहुत कुछ जानना चाहते हैं. जैसी जिज्ञासा यूरोप के सभ्य समाज के बच्चे करते हैं वैसी ही जिज्ञासा भारत के बच्चे भी करते हैं. जीवन, मन, शरीर, प्रकृति, मशीनें, समाज व्यवस्था और संबंधों पर उनकी जिज्ञासाएं इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि उनको उत्तर देना कठिन हो जाता है. उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए अक्सर जिन लोगों को समाज द्वारा “अधिकृत” किया गया है उन्होंने इन जिज्ञासाओं की बहुत बारीकी से ह्त्या की है. उनकी जिज्ञासाओं को उत्तर देकर नयी जिज्ञासाओं और नये प्रश्नों की तरफ बढ़ाने का अर्थ होता है पुराने सामाजिक ताने बाने और धर्म से आगे बढना. लेकिन अगर आपका समाज किसी आखिरी किताब, आखिरी मसीहा या अपौरुषेय किताबों या विश्वगुरु होने के अहंकार से पीड़ित है तो इस अहंकार की ठीक बगल में एक भयानक डर से भी वह लगातार पीडित रहेगा. यही पूरे इस्लामिक जगत और भारत की कहानी है.
आसमानी या अपौरुषेय किताबों का या विश्वगुरु के अहंकार का आभामंडल इतना असुरक्षित और डरपोक होता है कि वो बच्चों और स्त्रियों के प्रश्नों से सबसे अधिक डरता है. इसीलिये ऐसे समाज के लोग पठन-पाठन का अधिकार अपनी बड़ी जनसंख्या को और स्त्रियों को नहीं देना चाहते. भारतीय होशियारों ने इस विषय में महारथ हासिल कर ली थी. उन्होंने इस काम लिये वर्ण और जाति व्यवस्था ही बना डाली थी और वर्णाश्रम को ही धर्म बना डाला था, और ये व्यव्वस्था उनके आधिपत्य को बनाये रखने के लिए यह बहुत हद तक सफल भी रही. अलबरूनी ने अपने यात्रा संस्मरणों में लिखा है कि काश भारत जैसी जाति व्यवस्था हमारे पास होती तो हम भी करोड़ों लोगों को सैकड़ों हजारों साल गुलाम रखकर निष्कंटक राज करते और दबी कुचली कौमें कोई आवाज भी न उठा पातीं. अलबरूनी की भारत से ये इर्ष्या बहुत महत्वपूर्ण है. वह स्वयं जिस समाज से आ रहे हैं वहां कभी ज्ञान के फूल खिले थे लेकिन बाद में सब रेगिस्तान हो गया.
भारत में भी श्रमणों (बौद्धों, जैनों), लोकायतों, आजीवकों के युग में ज्ञान विज्ञान की बहुत खोज हुई थी और आज गिनाई जाने वाली सारी सफलताएं उसी दौर की हैं. शून्य, रेखागणित, अंकशास्त्र, खगोल, व्याकरण, भेषज, धातुविज्ञान, आयुर्वेद, योग और मनोविज्ञान (जो कि अध्यात्म में पतित हुआ) की खोज श्रमणों अर्थात बौद्धों और जैनों ने की थी. तांत्रिक अनुशासन के साथ लोकायतों ने भारी काम किया था. लेकिन वेद वेदान्त के प्रसार के साथ ज्ञान विज्ञान की ये प्रेरणाएं समाप्त होने लगीं और खगोलशास्त्र ज्योतिष बन गया, रसायन और भेषज जादूगरी और राजगुरुओं की गोपनीय विद्या बन गयी और एक वर्ण विशेष के लोगों के रोजगार की चिंता ने समूचे दक्षिण एशिया की ज्ञान की परम्पराओं का नाश कर डाला. राजसत्ता और व्यापरसत्ता को लग्न, मुहूर्त, ज्योतिष और कर्मकांड से डराकर गुलाम बनाया गया और शेष समाज को अंधविश्वास के दलदल में ऐसा डुबोया कि वो आज तक बाहर नहीं निकल सका है. खगोल के ज्योतिष में पतन पर अलबरूनी ने विस्तार से चर्चा करते हुए गजब की टिप्पणियाँ की हैं, वे पढ़ने योग्य हैं.
भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों की बात एक तरफ रखते हुए हम अगर समाज विज्ञानों जैसे कला, भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और इतिहास लेखन सहित राजनीति, शासन प्रशासन की भी बातें करें तो हम देखते हैं कि इन विषयों का और अधिक बुरा हाल किया गया है. आज के बच्चे समाजशास्त्र, साहित्य, भाषा, मनोविज्ञान इतिहास या राजनीतिशास्त्र नहीं पढ़ना चाहते. जो बच्चे ये सब पढ़ते हैं उन्हें दयनीय, कमजोर और पिछड़ा समझा जाता है. विषयों की भी जातियां हैं भारत में. विज्ञान, तकनीक, मेनेजमेंट, मेडिसिन आदि सवर्ण विषय हैं और मानविकी,आर्ट्स आदि अछूत विषय हैं. इसी का स्वाभाविक परिणाम ये है कि हमारे स्कूल कैसे हों, राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, शासन प्रशासन का ढंग कैसा हो, पत्रकारिता, सामाजिक विमर्ष, नारीवाद, सबाल्टर्न विमर्श सहित संस्कृति और दर्शन का विमर्श कैसा हो-ये सब हमें यूरोप के सभ्य देशों से सीखना होता है.
याद कीजिये, डॉ. अम्बेडकर ने जो संविधान रचा वो पश्चिमी लोकतंत्र और समाजवाद से प्रेरणा लेता है. भारत के अतीत में भविष्य के समाज को दिशा देने लायक बातें लगभग न के बराबर हैं. आज की संसदीय प्रणाली से लेकर कानून, प्रशासन, चुनाव आदि सभी बातें यूरोप ने विकसित कीं और भारत के गुलामी के दौर में यूरोप अमेरिका में पढ़ने गये वकीलों ने इस देश को यूरोपीय सभ्यता के आदर्शों पर खड़ा किया. इसीलिये हम थोड़ा सा बदलाव, सामाजिक सुधार और विकास भारत में देख पाते हैं.
लेकिन भारत के स्वतंत्र होते ही और आत्मनिर्णय का अधिकार मिलते ही विश्वगुरु का जिन्न फिर से जाग गया. भूमि सुधारों और दलित आंदोलनों के दबाव से पुराने शोषक तिलमिला उठे और उन्होंने फिर से गुरुकुल स्टाइल मूर्खताओं की तारीफ़ शुरू कर दी और बहुत गहरे षड्यंत्र के तहत दलितों, शूद्रों (ओबीसी), आदिवासियों और स्त्रियों को ज्ञान से वंचित करने का काम आरंभ कर दिया. राष्ट्र निर्माण के लिए जितना जरुरी था उतना भर विज्ञान और तकनीक सीखने सिखाने का इन्तेजाम कर लिया. देश को प्रबंधन और तकनीक के बड़े बड़े संस्थान दिए गये लेकिन जनमानस में विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को रोकने के लिए गुप्त रूप से कहीं अधिक शक्ति लगाईं गयी.
आईआईटी और आईआईएम को देखिये. आईआईटी असल में तकनीक के संस्थान हैं. यहां विज्ञान के बाबू पैदा होते हैं जो विज्ञान और मशीनरी के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं. विज्ञान वे कितना जानते हैं इसका उत्तर इन संस्थानों के विद्यार्थियों को अब तक मिले नोबेल पुरस्कारों की संख्या से अंदाजा लगता है. लेकिन इतनी प्रशंसा उनकी की जा सकती है कि उनके यूरोपीय या अमेरीकी शिक्षक जब कुछ खोज लेते हैं तो वे उसका सस्ता संस्करण तैयार कर देते हैं. इतनी प्रतिभा उनमे जरुर है. ऐसे ही हमारे चिकित्सक और मैनेजर हैं. वे नया कुछ नहीं खोज सकते लेकिन एक बार ह्रदय का किडनी का मस्तिष्क के काम करने के विज्ञान को कोई यूरोपीय या अमेरिकन खोज ले तो उसके बाद हमारे डाक्टर आँख, नाक, ह्रदय के आपरेशन का या नसबंदी का विश्वरिकार्ड बना लेते हैं. इस बात के लिए उनकी प्रशंसा हो सकती है.
क्या समाज विज्ञान, मानविकी में भारत कुछ बेहतर कर रहा है? उत्तर है कि समाज विज्ञानों को समझने की भारत की तैयारी ही नहीं है. हजारों साल के विविधतापूर्ण सामाजिक इतिहास में समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान को जन्म दे सकने वाले धार्मिक-सामाजिक बदलाव, आक्रमण, युद्ध, राजनीतिक परिवर्तन आदि घटनाएँ घटती रहीं लेकिन यहाँ समाज विज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ. यूरोप में पुनर्जागरण के बाद औद्योगीकरण और नगरीकरण की छाया में समाजशास्त्र का जन्म हुआ लेकिन भारत में ऐसा बहुत कुछ हो चुकने के बाद भी समाज विज्ञान की कोई प्रेरणा नहीं हुई. ये एक चमत्कार है. भारत के धर्म और अध्यात्म ने नये ज्ञान की संभावना और नए समाज की प्रेरणा को बहुत खूबसूरती से और कुशलता से नष्ट किया है. देश के मानव संसाधन को कैसे नष्ट किया जाता है ये कोई भारत से सीखे. आज मानविकी विषयो में भारत की मौलिक रिसर्च बहुत ही कम है. हां, भारत के समाज, राजनीति और संस्कृति के संबंध में भारतीय लोग लिखते लिखाते रहते हैं लेकिन उनका ये लेखन या शोध विश्व स्तर पर ज्ञान को बढ़ाने में कोई ख़ास योगदान नहीं देता है.
आधुनिक युग के सभी बड़े सिद्धांतकार यूरोपीय हैं. राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, लोकतंत्र, शासन, प्रशासन, पत्रकारिता, व्यापार प्रबंधन, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा व्यवस्था, रिसर्च और यहां तक कि अब वैज्ञानिक अध्यात्म विद्या और कांशियसनेस स्टडीज जैसे एकदम नये विषय भी यूरोप से ही आ रहे हैं. और मजा ये कि भारतीय समाज उसपर भी अपना “सनातन अधिकार” जमाते हुए यह कह रहा है कि ये सब तो हमारे शास्त्रों में न जाने कब से लिखा हुआ है.
भारत में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को गौर से देखिये वे इन प्रश्नों पर ज़रा भी जागरूक नहीं हैं. उपर उपर से लगता है कि वे अनजान हैं. लेकिन थोड़ा कुरेदो तो पता चलेगा कि वे एक बहुत बड़े और प्राचीनतम षड्यंत्र के पुर्जे हैं. उन्हें पता है शिक्षा और ज्ञान को कैसे बर्बाद करना है और शोषक धर्म की सत्ता को कैसे बनाये रखना है. बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल कालेज के लोगों से बात कीजिये आपको लगेगा कि ये किस जमाने के जीवाश्म हैं जो अभी भी जीये जा रहे हैं. ग्रामीण बच्चों की तकदीर जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों के स्तर की तो बात ही करना व्यर्थ है. ऊपर से धर्म और राष्ट्रवाद की जहरीली खिचड़ी ने उन्हें एकदम पागल बना दिया है. सिर्फ कैशलेस ही नहीं ”कास्ट लेस” इंडिया भी जरूरी
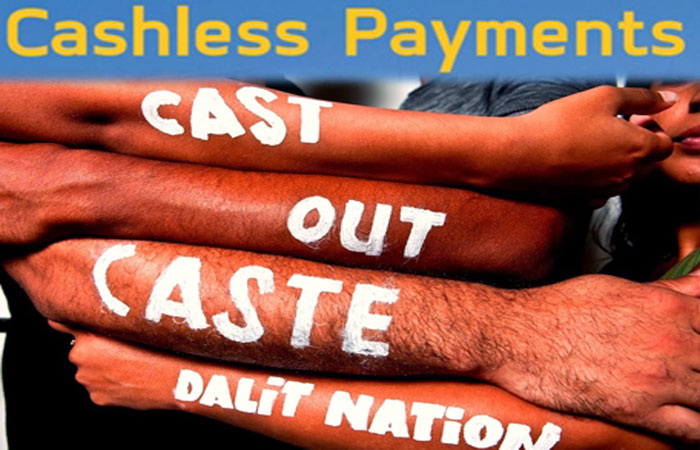 आज जब देश में चारों तरफ नोटबंदी ही चर्चा का विषय बना है तो इस पर एक फिल्म के गाने के कुछ बोल फिट प्रतीत होते हैं “सोने चांदी के महलों में दर्द ज्यादा है चैन थोडा़ है. इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है.”
एक जमाना था जब रोटी कपडा़ और मकान ही लोगों की आवश्यकता हुआ करती थी. इस पर कई फिल्में भी बनीं. आज बदलते युग में दाल और आटा जितना जरूरी है उतना डाटा भी जरूरी बन चुका है. कन्दराओं और गुफाओं से निकला मानव आज चांद और मंगल ग्रह में आशियाना तलासने लगा है. गुफाओं से लेकर मंगल की यात्रा कई हजार सालों के सफर के बाद तय हो पाया है. महीनों में मिलने वाले संदेश आज पल भर में पहुंच जाते हैं. हफ्तों-महीनों का सफर चंद घंटों में तय हो जाता है.
विकास के इस दौर में कई चीजें इतिहास बन कर रह गयीं हैं. आवश्यकताओं ने मनुष्य को आविष्कारक बना डाला है और ये भूख अभी थमी नहीं है. भारत परंपराओं और मान्यताओं का देश रहा है. यहां मंत्रों पर ज्यादा आस्था रही है, और हमने पूरी शक्ति लाखों मंत्रों और टोटकों को खेाजने में लगा दी यही कारण रहा कि देश साहित्य और शास्त्रों में तो आगे रहा मगर साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया.
यहां तक कि गांधीजी भी चरखे और कुटीर उद्योगों से ही देश को आगे ले जाने के पक्षधर थे. नेहरू जी ने देश में साइंस और टेक्नोलॉजी को पहली प्राथमिकता में रखा. आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने “विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों” का एक पृथक मंत्रालय बनाया जिसको नेहरू जी ने अपने पास ही रखा. राजीव गांधी देश को कृषि प्रधान के साथ-साथ कंप्यूटर प्रधान बनाना चाहते थे. देश में सूचना क्रांति का उनको जनक कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. मगर उस वक्त भी देश में कंप्यूटर का ऐसा ही विरोध हुआ था जैसा आजकल डीमोनीटाइजेशन का हो रहा है. जो लोग उस वक्त कंप्यूटर के घोर विरोधी थे वही कंप्यूटर उनकी राजनीति के लिए एक बेहतर लुभावना चुनावी जीत का मंत्र बना.
सूचना क्रांति ने कई ऐसी चीजों को इतिहास बना डाला है जो कभी लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हुआ करते थे यथा चिट्टी पत्री, अंतरदेशीय पत्र, पोस्टकार्ड, आदि. धीरे-धीरे इनके विकल्प मौजूद हो गये तो ये चलन से बाहर हो गये. इसके लिए कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि लैटरलेस हो जाओ, पोस्टकार्डलेस हो जाओ, या मनीआर्डरलैस हो जाओ. और आगे भी बदलाव होता रहा है एसएमएस, ईमेल, मोबाइल फोन आदि की दस्तक ने 165 वर्ष पुरानी टेलीग्राम सेवा को 14 जुलाई 2013 को प्रचलन से पूर्णतः बंद कर दिया. मगर डाकघरों पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है. विकसित भारत और डिजिटल भारत विज्ञान और तकनीक की राह पर चलकर ही संभव हो पायेगा इसमें संदेह की गुंजाइस नहीं है. मगर पल भर में अप्रत्याशित परिणामों की आशा करना जल्दबाजी होगी. हमारा समाज अतीत से पुराने विचारों और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है, इसलिए भारत में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड जैसी क्रांतियां नहीं हो सकी. हम या तो धर्म गुरूओं, साधु संतों के इशारे पर चलने के आदि हो चुके हैं या नेताओं और पार्टियों के डोपिंग का शिकार बनते जा रहे हैं.
नोटबंदी का असली मकसद क्या है? ये दिन प्रतिदिन पहेली बनती जा रही है. 8 नवंबर को जब इसका ऐलान हुआ था तब देश में कालेधन की निकासी और 500 और 1000 के नोटों का पाकिस्तान द्धारा जाली नोट बनाकर आतंकियों को दिया जाना था, के खात्मे के लिए तथा देश से कालेधन की सफाई के लिए नोटबंदी करना अति आवश्यक बताया गया था. 50 दिनों के इस सफर में इसके साथ कई और अध्याय जुड़ते जा रहे हैं यानि कि एक तीर से हजार निशाने साधने की कोशिश हो रही है. कैशलैस योजना में डिजिटल खरीददारी और लेन-देन पर अब इनामी लाटरी भी शामिल की गयी है जो इस योजना को अवश्य ही प्रोत्साहन देने का काम करेगी मगर इसमें 25 दिसंबर अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस और 14 अप्रैल 2017 को बाबासाहेब डा. अंबेडकर की जयंती से जोड़ना क्या विशुद्ध रूप से घूमफिर कर फिर वही दलित वोटों की राजनीति पर आकर नहीं टिक गयी है? जिनके सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता का सुख भोगती रही. दिलचस्प बात ये होगी कि 14 अप्रैल 2017 को कितने गरीबों और दलितों का मेगा शो निकलता है जिससे इनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा. तमाम ऐसी योजनायें स्वतंत्रता के बाद देश में लागू की गयी गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए मगर कोई भी योजना न तो पूर्ण हो सकी न ही अपना उदेदेश्य पूर्ण कर सकी. क्योंकि इनका असली मकसद गरीब और दलितों के हित नहीं मगर इनके वोट रहे है.
70 प्रतिशत गांवों में बसा भारत जो अब भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है, अंगूठा टेक से दस्तखत की ओर 100 प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है और टेक्नोलॅाजी की ओर धीरे-धीरे चलना सीख रहा है. ऐसे में उसको एकदम 100 मीटर की रेस में जापान और चीन की बुलेट ट्रेन के साथ कंप्टीशन में खड़ा करना न्यायसंगत नहीं लगता है. कैशलैस ट्रांजेक्शन असंभव नहीं है. इसके लिए सर्वप्रथम देश को डिजिटल लिटरेट करने की जरूरत है. इस ओर डिजिटल इंडिया महत्वकांक्षी योजना साबित हो सकती थी. डिजिटल इंडिया के मिशन को पूर्ण कर ही डिजिटल ट्रांजेक्शन का रास्ता स्वतः ही निकल सकता था. देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्पीड वाली इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के साथ ही हर हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन का होना भी आवश्यक होगा. बिजली सभी उपकरणों की जननी है इसकी आपूर्ति भी निर्बाध रूप से देश के हर कोने तक पहुंचाने की चुनौती भी हमारे सामने है.
नोटबंदी ने आज राजनीति के शेयर मार्केट में कई पुराने शेयरों को बंद कर दिया है. जिन शेयरों के सहारे भाजपा ने देश की राजनीति में कदम रखा था उनमें सर्व प्रथम राममंदिर तथा हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुख था. 2014 में महंगाई का मुद्दा, एक सिर के बदले दस सिर लाने का वायदा, खातों में लाखों रूपया जमा करने का वायदा, महंगाई को कम करने का वायदा, बेरोजगारी को खत्म करने का वायदा आदि-आदि. हैरानी नहीं चिप की दुनिया है एक छोटी सिलिकॉन चिप ने साइंस और तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी. कभी देश और कलाई की धड़कन समझी जाने वाली एचएमटी घड़ियों को 7 फरवरी 2016 को बंद कर दिया. इसी प्रकार नोटबंदी ने भी कई ज्वलंत मुद्दों को इस वक्त बंद कर दिया है. आज आतंकवाद पर कोई डिबेट नहीं होती, आज गाय और दलित पर बहस नहीं होती, आज महंगाई पर बहस बंद है, आज देशभक्ति और वीर शहीदों पर चर्चा नहीं होती है.
अभी कैशलैस होने मात्र से देश का कायापलट होने वाला नहीं है. कई क्षेत्रों में अभी हमको कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की शख्त जरूरत है. अभी देश को हैंगरलेस, अनटचब्लेटीलेस, अनइम्पलामेन्टईलेस, रेपलेस, क्रप्सनलेस और कास्टलेस भारत बनाना है. अब नोटबंदी भी जाति और मजहब के नाम पर बंटने लगी है, और इसमें भी गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मोहरा बनाकर फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति होने लगी है. तो एक कदम कैशलेस लेन-देन के साथ-साथ कास्टलेस खानपान और मान-सम्मान का माहौल भी देश में बन जाये तो अवश्य ही डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का सही मकसद हासिल किया जा सकता है. सिर्फ अंबेडकर को पूज कर वंचित समाज की दशा बदलने वाली नहीं है. 14 अप्रैल 2017 को मोदी मेगा इनाम की घोषणा अगर पांच सौ और दो हजार के नोटों पर बाबा साहेब डा अम्बेडकर की तस्वीर के साथ करेंगे तो तब सही अर्थ में उनका अम्बेडकर प्रेम प्रदर्शित होगा. वरना देश का दलित वर्ग हमेशा राजनीतिक डोपिंग का शिकार ही होता रहा है.
आज जब देश में चारों तरफ नोटबंदी ही चर्चा का विषय बना है तो इस पर एक फिल्म के गाने के कुछ बोल फिट प्रतीत होते हैं “सोने चांदी के महलों में दर्द ज्यादा है चैन थोडा़ है. इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है.”
एक जमाना था जब रोटी कपडा़ और मकान ही लोगों की आवश्यकता हुआ करती थी. इस पर कई फिल्में भी बनीं. आज बदलते युग में दाल और आटा जितना जरूरी है उतना डाटा भी जरूरी बन चुका है. कन्दराओं और गुफाओं से निकला मानव आज चांद और मंगल ग्रह में आशियाना तलासने लगा है. गुफाओं से लेकर मंगल की यात्रा कई हजार सालों के सफर के बाद तय हो पाया है. महीनों में मिलने वाले संदेश आज पल भर में पहुंच जाते हैं. हफ्तों-महीनों का सफर चंद घंटों में तय हो जाता है.
विकास के इस दौर में कई चीजें इतिहास बन कर रह गयीं हैं. आवश्यकताओं ने मनुष्य को आविष्कारक बना डाला है और ये भूख अभी थमी नहीं है. भारत परंपराओं और मान्यताओं का देश रहा है. यहां मंत्रों पर ज्यादा आस्था रही है, और हमने पूरी शक्ति लाखों मंत्रों और टोटकों को खेाजने में लगा दी यही कारण रहा कि देश साहित्य और शास्त्रों में तो आगे रहा मगर साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया.
यहां तक कि गांधीजी भी चरखे और कुटीर उद्योगों से ही देश को आगे ले जाने के पक्षधर थे. नेहरू जी ने देश में साइंस और टेक्नोलॉजी को पहली प्राथमिकता में रखा. आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने “विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों” का एक पृथक मंत्रालय बनाया जिसको नेहरू जी ने अपने पास ही रखा. राजीव गांधी देश को कृषि प्रधान के साथ-साथ कंप्यूटर प्रधान बनाना चाहते थे. देश में सूचना क्रांति का उनको जनक कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. मगर उस वक्त भी देश में कंप्यूटर का ऐसा ही विरोध हुआ था जैसा आजकल डीमोनीटाइजेशन का हो रहा है. जो लोग उस वक्त कंप्यूटर के घोर विरोधी थे वही कंप्यूटर उनकी राजनीति के लिए एक बेहतर लुभावना चुनावी जीत का मंत्र बना.
सूचना क्रांति ने कई ऐसी चीजों को इतिहास बना डाला है जो कभी लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हुआ करते थे यथा चिट्टी पत्री, अंतरदेशीय पत्र, पोस्टकार्ड, आदि. धीरे-धीरे इनके विकल्प मौजूद हो गये तो ये चलन से बाहर हो गये. इसके लिए कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि लैटरलेस हो जाओ, पोस्टकार्डलेस हो जाओ, या मनीआर्डरलैस हो जाओ. और आगे भी बदलाव होता रहा है एसएमएस, ईमेल, मोबाइल फोन आदि की दस्तक ने 165 वर्ष पुरानी टेलीग्राम सेवा को 14 जुलाई 2013 को प्रचलन से पूर्णतः बंद कर दिया. मगर डाकघरों पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है. विकसित भारत और डिजिटल भारत विज्ञान और तकनीक की राह पर चलकर ही संभव हो पायेगा इसमें संदेह की गुंजाइस नहीं है. मगर पल भर में अप्रत्याशित परिणामों की आशा करना जल्दबाजी होगी. हमारा समाज अतीत से पुराने विचारों और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है, इसलिए भारत में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड जैसी क्रांतियां नहीं हो सकी. हम या तो धर्म गुरूओं, साधु संतों के इशारे पर चलने के आदि हो चुके हैं या नेताओं और पार्टियों के डोपिंग का शिकार बनते जा रहे हैं.
नोटबंदी का असली मकसद क्या है? ये दिन प्रतिदिन पहेली बनती जा रही है. 8 नवंबर को जब इसका ऐलान हुआ था तब देश में कालेधन की निकासी और 500 और 1000 के नोटों का पाकिस्तान द्धारा जाली नोट बनाकर आतंकियों को दिया जाना था, के खात्मे के लिए तथा देश से कालेधन की सफाई के लिए नोटबंदी करना अति आवश्यक बताया गया था. 50 दिनों के इस सफर में इसके साथ कई और अध्याय जुड़ते जा रहे हैं यानि कि एक तीर से हजार निशाने साधने की कोशिश हो रही है. कैशलैस योजना में डिजिटल खरीददारी और लेन-देन पर अब इनामी लाटरी भी शामिल की गयी है जो इस योजना को अवश्य ही प्रोत्साहन देने का काम करेगी मगर इसमें 25 दिसंबर अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस और 14 अप्रैल 2017 को बाबासाहेब डा. अंबेडकर की जयंती से जोड़ना क्या विशुद्ध रूप से घूमफिर कर फिर वही दलित वोटों की राजनीति पर आकर नहीं टिक गयी है? जिनके सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता का सुख भोगती रही. दिलचस्प बात ये होगी कि 14 अप्रैल 2017 को कितने गरीबों और दलितों का मेगा शो निकलता है जिससे इनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा. तमाम ऐसी योजनायें स्वतंत्रता के बाद देश में लागू की गयी गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए मगर कोई भी योजना न तो पूर्ण हो सकी न ही अपना उदेदेश्य पूर्ण कर सकी. क्योंकि इनका असली मकसद गरीब और दलितों के हित नहीं मगर इनके वोट रहे है.
70 प्रतिशत गांवों में बसा भारत जो अब भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है, अंगूठा टेक से दस्तखत की ओर 100 प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है और टेक्नोलॅाजी की ओर धीरे-धीरे चलना सीख रहा है. ऐसे में उसको एकदम 100 मीटर की रेस में जापान और चीन की बुलेट ट्रेन के साथ कंप्टीशन में खड़ा करना न्यायसंगत नहीं लगता है. कैशलैस ट्रांजेक्शन असंभव नहीं है. इसके लिए सर्वप्रथम देश को डिजिटल लिटरेट करने की जरूरत है. इस ओर डिजिटल इंडिया महत्वकांक्षी योजना साबित हो सकती थी. डिजिटल इंडिया के मिशन को पूर्ण कर ही डिजिटल ट्रांजेक्शन का रास्ता स्वतः ही निकल सकता था. देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्पीड वाली इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के साथ ही हर हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन का होना भी आवश्यक होगा. बिजली सभी उपकरणों की जननी है इसकी आपूर्ति भी निर्बाध रूप से देश के हर कोने तक पहुंचाने की चुनौती भी हमारे सामने है.
नोटबंदी ने आज राजनीति के शेयर मार्केट में कई पुराने शेयरों को बंद कर दिया है. जिन शेयरों के सहारे भाजपा ने देश की राजनीति में कदम रखा था उनमें सर्व प्रथम राममंदिर तथा हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुख था. 2014 में महंगाई का मुद्दा, एक सिर के बदले दस सिर लाने का वायदा, खातों में लाखों रूपया जमा करने का वायदा, महंगाई को कम करने का वायदा, बेरोजगारी को खत्म करने का वायदा आदि-आदि. हैरानी नहीं चिप की दुनिया है एक छोटी सिलिकॉन चिप ने साइंस और तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी. कभी देश और कलाई की धड़कन समझी जाने वाली एचएमटी घड़ियों को 7 फरवरी 2016 को बंद कर दिया. इसी प्रकार नोटबंदी ने भी कई ज्वलंत मुद्दों को इस वक्त बंद कर दिया है. आज आतंकवाद पर कोई डिबेट नहीं होती, आज गाय और दलित पर बहस नहीं होती, आज महंगाई पर बहस बंद है, आज देशभक्ति और वीर शहीदों पर चर्चा नहीं होती है.
अभी कैशलैस होने मात्र से देश का कायापलट होने वाला नहीं है. कई क्षेत्रों में अभी हमको कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की शख्त जरूरत है. अभी देश को हैंगरलेस, अनटचब्लेटीलेस, अनइम्पलामेन्टईलेस, रेपलेस, क्रप्सनलेस और कास्टलेस भारत बनाना है. अब नोटबंदी भी जाति और मजहब के नाम पर बंटने लगी है, और इसमें भी गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मोहरा बनाकर फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति होने लगी है. तो एक कदम कैशलेस लेन-देन के साथ-साथ कास्टलेस खानपान और मान-सम्मान का माहौल भी देश में बन जाये तो अवश्य ही डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का सही मकसद हासिल किया जा सकता है. सिर्फ अंबेडकर को पूज कर वंचित समाज की दशा बदलने वाली नहीं है. 14 अप्रैल 2017 को मोदी मेगा इनाम की घोषणा अगर पांच सौ और दो हजार के नोटों पर बाबा साहेब डा अम्बेडकर की तस्वीर के साथ करेंगे तो तब सही अर्थ में उनका अम्बेडकर प्रेम प्रदर्शित होगा. वरना देश का दलित वर्ग हमेशा राजनीतिक डोपिंग का शिकार ही होता रहा है.
5 हजार ओबीसी ने अपनाया बौद्ध धर्म
 नागपुर। सत्यशोधक ओबीसी परिषद के नेतृत्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 हजार लोगों ने मनुस्मृति दहन दिवस ( 25 दिसंबर) पर धम्म दीक्षा ली. इस दिन दीक्षाभूमि पर देशभर से दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए. पहले संविधान चौक से दीक्षा भूमि तक धम्म रैली निकाली गई. उसके बाद 5 हजार ओबीसी दलित ने बौद्ध धर्म को अपनाया.
महाराष्ट्र की सत्यशोधक ओबीसी परिषद पिछले पांच साल से इस योजना को बना रही थी. अंततः 25 दिसंबर को दीक्षाभूमि पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया. परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन अम्बेडकर के धर्मांतरण दिवस पर नागपुर में करने के बारे में सोचा था लेकिन इस दिन दीक्षाभूमि पर होने वाली भीड़ को देखते हुए इसे स्थगित करना पड़ा.
परिषद के एक कार्यकर्ता धानाजी गौरव ने कहा कि हमने तीन कारणों से इस दिन को चुना. इस दिन सावित्री बाई फुले ने पहला महिला स्कूल खोला था, आज के दिन क्रिसमस होता है और आज ही के दिन 1927 में बाबासाहेब ने मनुस्मृति को जलाया था. इस दिन को हम लोग मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते है. उन्होंने कहा की इस मुक्ति दिवस में महिलाओं के समूह भी शामिल है.
धानाजी गौरव ने बताया कि परिषद ने 2011 से ओबीसी लोगों को भर्ती करने का अभियान शुरू किया. परिषद ने ओबीसी को “नागवंशी” के रूप में बताया और उनके इतिहास को जानने पर बल दिया. “नागवंशी” मध्ययुगीन काल में बौद्ध थे. उन्होंने कहा कि अब उनकी सच्ची घर वापसी हो रही है, वह अपने घर आ रहे हैं.
गौरव ने कहा की महाराष्ट्र से सबसे अधिक लोगों ने धर्मांतरण किया. उन्होंने कहा कि पूरे भारत के राज्य से 10-12 संयोजक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे. परिषद को उम्मीद है कि पूरे देश में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा. और जिन्होंने 25 दिसंबर को धर्मांतरण किया है उन्हें धार्मिक शिक्षा की क्लास दी जाएगी.
नागपुर। सत्यशोधक ओबीसी परिषद के नेतृत्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 हजार लोगों ने मनुस्मृति दहन दिवस ( 25 दिसंबर) पर धम्म दीक्षा ली. इस दिन दीक्षाभूमि पर देशभर से दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए. पहले संविधान चौक से दीक्षा भूमि तक धम्म रैली निकाली गई. उसके बाद 5 हजार ओबीसी दलित ने बौद्ध धर्म को अपनाया.
महाराष्ट्र की सत्यशोधक ओबीसी परिषद पिछले पांच साल से इस योजना को बना रही थी. अंततः 25 दिसंबर को दीक्षाभूमि पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया. परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन अम्बेडकर के धर्मांतरण दिवस पर नागपुर में करने के बारे में सोचा था लेकिन इस दिन दीक्षाभूमि पर होने वाली भीड़ को देखते हुए इसे स्थगित करना पड़ा.
परिषद के एक कार्यकर्ता धानाजी गौरव ने कहा कि हमने तीन कारणों से इस दिन को चुना. इस दिन सावित्री बाई फुले ने पहला महिला स्कूल खोला था, आज के दिन क्रिसमस होता है और आज ही के दिन 1927 में बाबासाहेब ने मनुस्मृति को जलाया था. इस दिन को हम लोग मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते है. उन्होंने कहा की इस मुक्ति दिवस में महिलाओं के समूह भी शामिल है.
धानाजी गौरव ने बताया कि परिषद ने 2011 से ओबीसी लोगों को भर्ती करने का अभियान शुरू किया. परिषद ने ओबीसी को “नागवंशी” के रूप में बताया और उनके इतिहास को जानने पर बल दिया. “नागवंशी” मध्ययुगीन काल में बौद्ध थे. उन्होंने कहा कि अब उनकी सच्ची घर वापसी हो रही है, वह अपने घर आ रहे हैं.
गौरव ने कहा की महाराष्ट्र से सबसे अधिक लोगों ने धर्मांतरण किया. उन्होंने कहा कि पूरे भारत के राज्य से 10-12 संयोजक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे. परिषद को उम्मीद है कि पूरे देश में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा. और जिन्होंने 25 दिसंबर को धर्मांतरण किया है उन्हें धार्मिक शिक्षा की क्लास दी जाएगी. दलित-पिछड़ा एकता में बाधक है सामंतवादी सोच
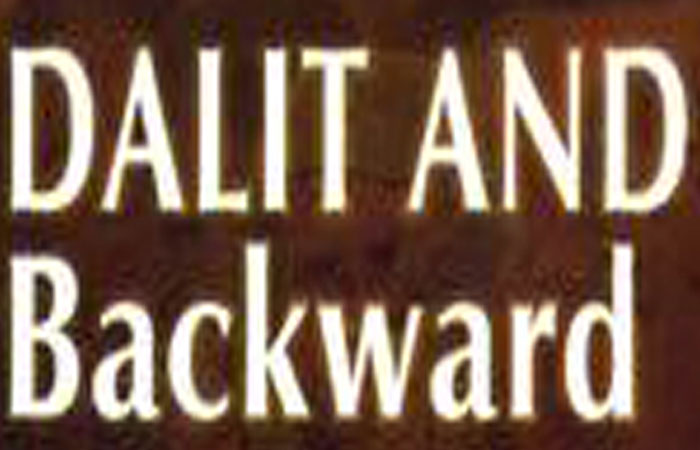 इसमें कोई शक नहीं कि दलितों और पिछड़ों में दूरियां बढ़ी हैं. हालांकि अतिपिछड़ा वर्ग दलितों के थोड़ा करीब दिखता है. लेकिन यह भी सोचना होगा कि जिस गंभीरता से इस विषय पर दलित बुद्धिजीवी सोचते हैं उतनी गंभीरता से पिछड़ों में चर्चा नहीं होती. आज भी पिछड़े अपने को सवर्णों के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश करते हैं. दलित तो शुरू से पिछड़ों को साथ लेकर चलने के हिमायती रहे हैं. चाहे बाबासाहेब का सामाजिक आंदोलन हो, चाहे बिहार में सामाजिक अधिकार की लड़ाई हो या कांशीराम साहब का उत्तर प्रदेश में 85-15 का नारा हो. सर्वदा दलितों ने पिछड़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश की.
1927 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें बाबासाहेब चाहते थे कि पिछड़ा उनका साथ दे और दलित पिछड़ा मिलकर असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़े लेकिन पिछड़ों को अपने को दलित कहलाना मंजूर नहीं था. बाध्य होकर बाबासाहेब को यह लड़ाई दलितों को साथ लेकर अकेले लड़नी पड़ी. मंडल कमीशन के विरोध के चलते जब मुलायम सिंह हाशिये पर आ गए थे, उन्होंने जब अपने निजी स्वार्थवश वीपी सिंह की सरकार गिराकर चंद्रशेखर को पीएम बनाने में मदद की उस समय पिछड़ा उनसे काफी हद तक दूर हो गया था. तब उन्होंने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए मान्यवर कांशीराम से समझौता किया. मुलायम सिंह अपने मकसद में कामयाब तो हो गए लेकिन लेकिन उनके अंदर की सामंतवादी सोच इस एकता में बाधक साबित हुई. नतीजा सपा बसपा का गठबंधन टूट गया.
एक बात यहां स्पष्ट करनी होगी कि उत्तर भारत में जब भी मनुवाद और सामंतवाद की लड़ाई की बात होती है, दलित बढ़-चढ़ कर पिछड़ों का साथ देते हैं लेकिन पिछड़े वर्ग के नेता दलितों को उसी मानसिकता से देखते हैं जैसे सवर्ण देखते हैं. बिहार और यूपी में सत्ता प्राप्ति के बाद से दलितों के अधिकार का जिस तरह से नव सामंतवादी सरकारों ने हनन किया है वैसा तो ब्राह्मणवादी सरकारों ने भी नहीं किया है.
बिहार में जिस प्रकार मनुवादी भाजपा के खिलाफ दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक एकजुट होकर लालू-नीतीश का साथ दिया, सत्ता में आने के बाद वही लालू और नीतीश ने दलितों पर अत्याचार की एक शृंखला प्रारम्भ कर दी है. जिस प्रकार अपने छात्रवृत्ति की मांग करने वाले दलित छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की गई, जिस प्रकार अपनी भूमि को जातिवादी गुंडों से वापस कराने के लिए आन्दोलनरत दलित महिलाओं पर बिहार पुलिस ने नंगा करके लाठी डंडा बरसाया है, वह अप्रत्याशित है.
यूपी में जिस प्रकार दलितों के बल पर पूर्ण बहुमत की अखिलेश सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में दलित विरोधी आदेशों की श्रृंखला को अंजाम दिया. क्या वह दलित पिछड़ा एकता के लिए अच्छा कदम कहा जा सकता है? पूरे पांच साल दलितों पर अत्याचार होते रहे, गुंडागर्दी होती रही और अखिलेश सरकार मूकदर्शक बनी रही. अगर थानों पर लिखी गई दलित उत्पीड़न की केस की जांच कराई जाय तो उसमें अबतक की सबसे कम संख्या दिखेगी.
ऐसे में कोई यह कहे कि दलित पिछड़ा एकता को भंग करने में सवर्ण का हाथ है, वह वास्तविकता से मुंह चुरानेवाली बात होगी. वास्तव में इस एकता में बाधक कुछ नवसामंती मानसिकता वाले पिछड़े हैं. और जबतक वे अपनी सोच नहीं बदलते, यह एकता संभव नहीं है. अब तो एक ही रास्ता बचा है और वह यह कि दलितों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी.
इसमें कोई शक नहीं कि दलितों और पिछड़ों में दूरियां बढ़ी हैं. हालांकि अतिपिछड़ा वर्ग दलितों के थोड़ा करीब दिखता है. लेकिन यह भी सोचना होगा कि जिस गंभीरता से इस विषय पर दलित बुद्धिजीवी सोचते हैं उतनी गंभीरता से पिछड़ों में चर्चा नहीं होती. आज भी पिछड़े अपने को सवर्णों के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश करते हैं. दलित तो शुरू से पिछड़ों को साथ लेकर चलने के हिमायती रहे हैं. चाहे बाबासाहेब का सामाजिक आंदोलन हो, चाहे बिहार में सामाजिक अधिकार की लड़ाई हो या कांशीराम साहब का उत्तर प्रदेश में 85-15 का नारा हो. सर्वदा दलितों ने पिछड़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश की.
1927 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें बाबासाहेब चाहते थे कि पिछड़ा उनका साथ दे और दलित पिछड़ा मिलकर असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़े लेकिन पिछड़ों को अपने को दलित कहलाना मंजूर नहीं था. बाध्य होकर बाबासाहेब को यह लड़ाई दलितों को साथ लेकर अकेले लड़नी पड़ी. मंडल कमीशन के विरोध के चलते जब मुलायम सिंह हाशिये पर आ गए थे, उन्होंने जब अपने निजी स्वार्थवश वीपी सिंह की सरकार गिराकर चंद्रशेखर को पीएम बनाने में मदद की उस समय पिछड़ा उनसे काफी हद तक दूर हो गया था. तब उन्होंने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए मान्यवर कांशीराम से समझौता किया. मुलायम सिंह अपने मकसद में कामयाब तो हो गए लेकिन लेकिन उनके अंदर की सामंतवादी सोच इस एकता में बाधक साबित हुई. नतीजा सपा बसपा का गठबंधन टूट गया.
एक बात यहां स्पष्ट करनी होगी कि उत्तर भारत में जब भी मनुवाद और सामंतवाद की लड़ाई की बात होती है, दलित बढ़-चढ़ कर पिछड़ों का साथ देते हैं लेकिन पिछड़े वर्ग के नेता दलितों को उसी मानसिकता से देखते हैं जैसे सवर्ण देखते हैं. बिहार और यूपी में सत्ता प्राप्ति के बाद से दलितों के अधिकार का जिस तरह से नव सामंतवादी सरकारों ने हनन किया है वैसा तो ब्राह्मणवादी सरकारों ने भी नहीं किया है.
बिहार में जिस प्रकार मनुवादी भाजपा के खिलाफ दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक एकजुट होकर लालू-नीतीश का साथ दिया, सत्ता में आने के बाद वही लालू और नीतीश ने दलितों पर अत्याचार की एक शृंखला प्रारम्भ कर दी है. जिस प्रकार अपने छात्रवृत्ति की मांग करने वाले दलित छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की गई, जिस प्रकार अपनी भूमि को जातिवादी गुंडों से वापस कराने के लिए आन्दोलनरत दलित महिलाओं पर बिहार पुलिस ने नंगा करके लाठी डंडा बरसाया है, वह अप्रत्याशित है.
यूपी में जिस प्रकार दलितों के बल पर पूर्ण बहुमत की अखिलेश सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में दलित विरोधी आदेशों की श्रृंखला को अंजाम दिया. क्या वह दलित पिछड़ा एकता के लिए अच्छा कदम कहा जा सकता है? पूरे पांच साल दलितों पर अत्याचार होते रहे, गुंडागर्दी होती रही और अखिलेश सरकार मूकदर्शक बनी रही. अगर थानों पर लिखी गई दलित उत्पीड़न की केस की जांच कराई जाय तो उसमें अबतक की सबसे कम संख्या दिखेगी.
ऐसे में कोई यह कहे कि दलित पिछड़ा एकता को भंग करने में सवर्ण का हाथ है, वह वास्तविकता से मुंह चुरानेवाली बात होगी. वास्तव में इस एकता में बाधक कुछ नवसामंती मानसिकता वाले पिछड़े हैं. और जबतक वे अपनी सोच नहीं बदलते, यह एकता संभव नहीं है. अब तो एक ही रास्ता बचा है और वह यह कि दलितों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी. मोटिवेशन कैरियर और बुद्ध की अनत्ता
 गौर कीजिए इन शब्दों पर. अक्सर ही हम सोचते हैं कि बुद्ध सिर्फ ध्यान समाधि और निर्वाण जैसी बातों के लिए ही हैं. लेकिन ये बिलकुल गलत बात है. बुद्ध के लिए परलोक या परीलोक का कोई अर्थ नहीं है. वे खालिस इस लोक और इस जीवन के लिए हैं.
एक ख़ास मुद्दे के संदर्भ में इसे देखेंगे तो आसानी से समझ में आयेगा. क्या मोटिवेशन और जीवन में सुधार को अनत्ता से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या वेदांत और ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत और मोटिवेशन या व्यक्तित्व विकास या जीवन के सुधार में आपस में कोई संबन्ध है?
इसका उत्तर है कि वेदांती आत्मा के सिद्धांत से मोटिवेशन या व्यक्तित्व विकास का सीधा संबन्ध नहीं है. बुद्ध की अनत्ता या अनात्मा से न सिर्फ मोटिवेशन का बल्कि जीवन और जगत के सभी सुधारों की संभावना का सीधा संबन्ध है. सनातन आत्मा का सिद्धांत एक भयानक गुलामी और अकर्मण्यता का सिद्धांत है. सनातन आत्मा का सीधा अर्थ पुनर्जन्म से है और हजारों जन्मों के बाद आपका यह जन्म उन अनन्त संस्कारों के सामने तिनके के बराबर है. ओशो रजनीश और आसाराम जैसे वेदांती पंडित प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों की जो व्याख्या करते हैं उसमे भी इस जन्म में करने योग्य या बदलने योग्य अवसर न के बराबर हैं. ये पोंगा पंडित समझाते हैं कि अनन्त जन्मों के अनन्त संस्कार हैं जिनसे आपकी आत्मा बंधी हुई है, उसी से आपका मन या बुद्धि बनी है आपके रुझान और आपकी क्षमताएं या कमजोरियां बनी हैं. इस जन्म में उस प्राचीन ढेर को मिटाना लगभग असंभव है इसलिए आप भाग्य के प्रारब्ध के गुलाम हैं. ये मान्यता जहर की तरह भारतीयों के खून ने घुस गई है.
इसका अर्थ ये हुआ कि आप जीवन, जगत, मन, शरीर, समाज, व्यवस्था आदि को बदलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि करने वाला क्रियानन्द ही प्रारब्ध से बंधा है, मतलब पूरा समाज और राष्ट्र ही एक सामूहिक प्रारब्ध से बंधा है अब उसके अनन्त प्रारब्ध या संचित कर्म को कैसे काटें? एक इंसान के संचित कर्मों के भंडार को जलाना ही जन्मों की तपस्या या साधना से संभव है, इस बीच इन जन्मों में किये पाप और नई कर्म श्रृंखला बनाते हैं. इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति या बदलाव सहित सामूहिक या समाज का बदलाव आत्मा के सिद्धांत के साथ असंभव है. इसीलिये भारत सड़ता रहा है. गुलाम गरीब और अंधविश्वासी होता रहा है.
लेकिन सनातन आत्मा की जगह बुद्ध की अनत्ता को रखकर देखिये. तस्वीर एकदम बदल जाती है.
बुद्ध के अनुसार शरीर बाहर से मिलता है, पहला अणु माँ बाप से फिर बाद में सब कुछ भोजन से निर्मित हुआ, आपका अपना कुछ नहीं. जैसा भोजन मिला वैसा शरीर और स्वास्थ्य बना. भोजन आप रोज करते हैं सही भोजन से स्वस्थ रहेंगे गलत भोजन से बीमार होंगे. गलत भोजन को बंद करके सही भोजन लेने लगेंगे तो शरीर और स्वास्थ्य सुधरने लगेगा. अब इस बात को ओशो रजनीश, जग्गी वासुदेव, आसाराम जैसे वेदांती पंडित भी मानते हैं. लेकिन वे इससे आगे जाने में घबराते हैं.
बुद्ध एक कदम और उठाते हैं और कहते हैं कि शरीर तो बाहर से आया है ही, ये तथाकथित आत्मा या स्व भी बाहर से ही आता है. जैसे शरीर भोजन का ढेर है वैसे ही स्व या व्यक्तित्व या मन या तथाकथित आत्मा भी विचारों, सपनों, स्मृतियों, संस्कारों, शिक्षा, कंडीशनिंग आदि का ढेर मात्र है. आपको गलत समाज, परिवार या संगति मिली है तो आपका स्व या मन गलत ढंग से काम करेगा, खुद के लिए और दूसरों के लिए दुःख पैदा करेगा. इस गलत कंडीशनिंग को सही कंडीशनिंग या विचारों या शिक्षाओं से बदला जा सकता है. और व्यक्ति और समाज को बदला जा सकता है.
चूँकि स्व या व्यक्तित्व भी क़तरा क़तरा बाहरी वातावरण से इकट्ठा करके बनाया जाता है इसलिए नये और अच्छे विचारों, संस्कारों के टुकड़ों को चुनकर मन में सजाते जाने से मन और व्यक्तित्व (जो कि अस्थाई हैं, सनातन नहीं) में बदलाव किया जा सकता है. तो जैसे गलत भोजन बन्द करके सही भोजन से कुछ महीनों में शरीर बदलने लगता है वैसे ही सही विचारों और शिक्षण से मन या व्यक्तित्व भी बदलने लगता है.
लेकिन अगर स्व या व्यक्तित्व या आत्मा सनातन है तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं. इसे ऐसे समझिये, अगर कोई कहे कि आपका शरीर सनातन है, उसने लाखों साल तक जो भोजन किया है उसके कारण कोई बीमारी बनी है. तो इसका अर्थ हुआ कि अब उस लाखों साल के अतीत का परिणाम जब तक मिटाया न जाए तब तक इस शरीर की बीमारी नहीं मिटाई जा सकती. लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर ठीक भोजन और औषधि से कुछ दिनीं या महीनों में बदलने लगता है. इसका मतलब है कि शरीर सनातन नहीं है.
अब मन या स्व पर आइये. हम देखते हैं कि कुछ महीनों में कोई नई भाषा, नई तकनीक, नया हुनर या व्यवहार सीखा जा सकता है. व्यक्तित्व का ढंग ढोल बदला जा सकता है. शिक्षण प्रशिक्षण और मोटिवेशन सहित सेल्फ इम्प्रूवमेंट या समाज के देश के डेवेलपमेंट का सारा ढांचा ही स्व या मन के अस्थाई और परिवर्तनशील होने की संभावना पर खड़ा है. अगर मन या स्व या आत्मा सनातन हुई तो उसमें कोई बदलाव संभव ही नहीं है.
अब ओशो जैसे पोंगा पंडितों की सनातन आत्मा और बुद्ध की अनात्मा के सिद्धांत को जीवन, जगत समाज राष्ट्र और दुनिया के संदर्भ में रखकर देखिये. साफ़ नजर आता है कि अगर सनातन आत्मा और अनन्त संचित कर्म का सिद्धांत माना जाए तो जीवन सिर्फ अतीत और भाग्य की गुलामी बनकर रह जाएगा. और यही भारत का जीवन बन गया है. इसके विपरीत अगर हर जीवन को नया और एकमात्र जीवन माना जाए तो बदलाव सुधार और विकास तेजी से होता है. जैसे यूरोप में हुआ है.
इस तरह जीवन का एक बहुत प्रेक्टिकल आयाम जो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है, मोटिवेशन या सेल्फ इंप्रूवमेंट- उसे बुद्ध की अनत्ता को समझकर और प्रयोग करके आसानी से हासिल किया जा सकता है. अनत्ता यही सिखाती है कि सबकुछ क्षणिक और अस्थाई है. सब कुछ स्वयं ही बदल रहा है आप चाहें तो ये बदलाव सही दिशा में भी जा सकता है. या फिर सभी बदलावों को चुपचाप देखते हुए आप शून्य भी हो सकते है. सेल्फ या स्व को क्षणिक मानना न केवल अतीत से मुक्त कर देता है बल्कि भविष्य का नियंत्रण भी आपके हाथ में दे देता है.
गौर कीजिए इन शब्दों पर. अक्सर ही हम सोचते हैं कि बुद्ध सिर्फ ध्यान समाधि और निर्वाण जैसी बातों के लिए ही हैं. लेकिन ये बिलकुल गलत बात है. बुद्ध के लिए परलोक या परीलोक का कोई अर्थ नहीं है. वे खालिस इस लोक और इस जीवन के लिए हैं.
एक ख़ास मुद्दे के संदर्भ में इसे देखेंगे तो आसानी से समझ में आयेगा. क्या मोटिवेशन और जीवन में सुधार को अनत्ता से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या वेदांत और ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत और मोटिवेशन या व्यक्तित्व विकास या जीवन के सुधार में आपस में कोई संबन्ध है?
इसका उत्तर है कि वेदांती आत्मा के सिद्धांत से मोटिवेशन या व्यक्तित्व विकास का सीधा संबन्ध नहीं है. बुद्ध की अनत्ता या अनात्मा से न सिर्फ मोटिवेशन का बल्कि जीवन और जगत के सभी सुधारों की संभावना का सीधा संबन्ध है. सनातन आत्मा का सिद्धांत एक भयानक गुलामी और अकर्मण्यता का सिद्धांत है. सनातन आत्मा का सीधा अर्थ पुनर्जन्म से है और हजारों जन्मों के बाद आपका यह जन्म उन अनन्त संस्कारों के सामने तिनके के बराबर है. ओशो रजनीश और आसाराम जैसे वेदांती पंडित प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों की जो व्याख्या करते हैं उसमे भी इस जन्म में करने योग्य या बदलने योग्य अवसर न के बराबर हैं. ये पोंगा पंडित समझाते हैं कि अनन्त जन्मों के अनन्त संस्कार हैं जिनसे आपकी आत्मा बंधी हुई है, उसी से आपका मन या बुद्धि बनी है आपके रुझान और आपकी क्षमताएं या कमजोरियां बनी हैं. इस जन्म में उस प्राचीन ढेर को मिटाना लगभग असंभव है इसलिए आप भाग्य के प्रारब्ध के गुलाम हैं. ये मान्यता जहर की तरह भारतीयों के खून ने घुस गई है.
इसका अर्थ ये हुआ कि आप जीवन, जगत, मन, शरीर, समाज, व्यवस्था आदि को बदलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि करने वाला क्रियानन्द ही प्रारब्ध से बंधा है, मतलब पूरा समाज और राष्ट्र ही एक सामूहिक प्रारब्ध से बंधा है अब उसके अनन्त प्रारब्ध या संचित कर्म को कैसे काटें? एक इंसान के संचित कर्मों के भंडार को जलाना ही जन्मों की तपस्या या साधना से संभव है, इस बीच इन जन्मों में किये पाप और नई कर्म श्रृंखला बनाते हैं. इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति या बदलाव सहित सामूहिक या समाज का बदलाव आत्मा के सिद्धांत के साथ असंभव है. इसीलिये भारत सड़ता रहा है. गुलाम गरीब और अंधविश्वासी होता रहा है.
लेकिन सनातन आत्मा की जगह बुद्ध की अनत्ता को रखकर देखिये. तस्वीर एकदम बदल जाती है.
बुद्ध के अनुसार शरीर बाहर से मिलता है, पहला अणु माँ बाप से फिर बाद में सब कुछ भोजन से निर्मित हुआ, आपका अपना कुछ नहीं. जैसा भोजन मिला वैसा शरीर और स्वास्थ्य बना. भोजन आप रोज करते हैं सही भोजन से स्वस्थ रहेंगे गलत भोजन से बीमार होंगे. गलत भोजन को बंद करके सही भोजन लेने लगेंगे तो शरीर और स्वास्थ्य सुधरने लगेगा. अब इस बात को ओशो रजनीश, जग्गी वासुदेव, आसाराम जैसे वेदांती पंडित भी मानते हैं. लेकिन वे इससे आगे जाने में घबराते हैं.
बुद्ध एक कदम और उठाते हैं और कहते हैं कि शरीर तो बाहर से आया है ही, ये तथाकथित आत्मा या स्व भी बाहर से ही आता है. जैसे शरीर भोजन का ढेर है वैसे ही स्व या व्यक्तित्व या मन या तथाकथित आत्मा भी विचारों, सपनों, स्मृतियों, संस्कारों, शिक्षा, कंडीशनिंग आदि का ढेर मात्र है. आपको गलत समाज, परिवार या संगति मिली है तो आपका स्व या मन गलत ढंग से काम करेगा, खुद के लिए और दूसरों के लिए दुःख पैदा करेगा. इस गलत कंडीशनिंग को सही कंडीशनिंग या विचारों या शिक्षाओं से बदला जा सकता है. और व्यक्ति और समाज को बदला जा सकता है.
चूँकि स्व या व्यक्तित्व भी क़तरा क़तरा बाहरी वातावरण से इकट्ठा करके बनाया जाता है इसलिए नये और अच्छे विचारों, संस्कारों के टुकड़ों को चुनकर मन में सजाते जाने से मन और व्यक्तित्व (जो कि अस्थाई हैं, सनातन नहीं) में बदलाव किया जा सकता है. तो जैसे गलत भोजन बन्द करके सही भोजन से कुछ महीनों में शरीर बदलने लगता है वैसे ही सही विचारों और शिक्षण से मन या व्यक्तित्व भी बदलने लगता है.
लेकिन अगर स्व या व्यक्तित्व या आत्मा सनातन है तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं. इसे ऐसे समझिये, अगर कोई कहे कि आपका शरीर सनातन है, उसने लाखों साल तक जो भोजन किया है उसके कारण कोई बीमारी बनी है. तो इसका अर्थ हुआ कि अब उस लाखों साल के अतीत का परिणाम जब तक मिटाया न जाए तब तक इस शरीर की बीमारी नहीं मिटाई जा सकती. लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर ठीक भोजन और औषधि से कुछ दिनीं या महीनों में बदलने लगता है. इसका मतलब है कि शरीर सनातन नहीं है.
अब मन या स्व पर आइये. हम देखते हैं कि कुछ महीनों में कोई नई भाषा, नई तकनीक, नया हुनर या व्यवहार सीखा जा सकता है. व्यक्तित्व का ढंग ढोल बदला जा सकता है. शिक्षण प्रशिक्षण और मोटिवेशन सहित सेल्फ इम्प्रूवमेंट या समाज के देश के डेवेलपमेंट का सारा ढांचा ही स्व या मन के अस्थाई और परिवर्तनशील होने की संभावना पर खड़ा है. अगर मन या स्व या आत्मा सनातन हुई तो उसमें कोई बदलाव संभव ही नहीं है.
अब ओशो जैसे पोंगा पंडितों की सनातन आत्मा और बुद्ध की अनात्मा के सिद्धांत को जीवन, जगत समाज राष्ट्र और दुनिया के संदर्भ में रखकर देखिये. साफ़ नजर आता है कि अगर सनातन आत्मा और अनन्त संचित कर्म का सिद्धांत माना जाए तो जीवन सिर्फ अतीत और भाग्य की गुलामी बनकर रह जाएगा. और यही भारत का जीवन बन गया है. इसके विपरीत अगर हर जीवन को नया और एकमात्र जीवन माना जाए तो बदलाव सुधार और विकास तेजी से होता है. जैसे यूरोप में हुआ है.
इस तरह जीवन का एक बहुत प्रेक्टिकल आयाम जो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है, मोटिवेशन या सेल्फ इंप्रूवमेंट- उसे बुद्ध की अनत्ता को समझकर और प्रयोग करके आसानी से हासिल किया जा सकता है. अनत्ता यही सिखाती है कि सबकुछ क्षणिक और अस्थाई है. सब कुछ स्वयं ही बदल रहा है आप चाहें तो ये बदलाव सही दिशा में भी जा सकता है. या फिर सभी बदलावों को चुपचाप देखते हुए आप शून्य भी हो सकते है. सेल्फ या स्व को क्षणिक मानना न केवल अतीत से मुक्त कर देता है बल्कि भविष्य का नियंत्रण भी आपके हाथ में दे देता है. वाया बीबीसी कौशल पंवार की कहानी
 वर्जीनिया वुल्फ की किताब ”A Room of One””s Own” का प्रकाशन 1929 में हुआ था, उसका केन्द्रीय स्वर है कि एक स्त्री का अपने लेखन के लिए अपना कमरा होना चाहिए, अपने निज को सुरक्षित रखने के लिए भी अपना कमरा, इसके लिए उसकी आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है. अपने कमरे को हासिल करने की इसी छटपटाहट को कौशल पंवार ने बीबीसी से साझा किया, जिसे साभार यहां प्रकाशित किया जा रहा है.
मेरा भी घर मे एक कोना होता, उसमें एक टेबल और कुर्सी होती, मै हमेशा इसके लिए तरसती थी. पर मेरे लिए वह कोना सुनिश्चित होना घर के एक हिस्से को घेरे रखने के बराबर होता.
इसमें मेरे मां- बाप की कोई ग़लती नहीं थी, उन्होंने भी तो सारी उम्र घर की इसी कोठरी में बिता दी थी. यह घर ही इसलिए कहलाया गया था क्योंकि इसी घर में सब मिलकर रहते थे, चाहे वह बकरी हो, मुर्गे हों या फ़िर एक कोने में रखा चूल्हा ही क्यों न हो, उसी के साथ सटे रहते थे एल्मुनियम के कुछ बर्तन.
उसी कोठरी में एक कोने में पीने के पानी के लिए एक मटका रखा रहता था, और एक कोने में अनाज को रखने का एक खुटला (एक तरह से मिट्टी की बनी अनाज को संग्रहित करने की टंकी) तो ये थी हमारी कोठरी, जो अन्दर और बाहर से थी जिसका हर एक कोना निश्चित था, इसलिए मेरे लिए उस कोठरी में एक कोना स्थाई रूप से बनना ही बहुत मुश्किल था.
उस समय का ये मेरा सबसे बड़ा सपना बन गया था कि मुर्गे और बकरी की तरह ही सही मेरा भी एक कोना बना रहे, जो हर दिन मुझे बदलना न पड़े पर नहीं बन सका था. उसी कमरे में मां, दादी और मेरे लिए भी एक कोना नहाने का बन जाता था, जिससे नहाने के बाद साफ़ कर दिया जाता था और उसी में चूल्हे पर खाना भी बनता था.
मैं अपने पढने के लिए खाट पर बैठकर घुटनों को मोड़कर ही उस पर किताब रख कर पढ़ लिया करती थी.
पढ़ने का जुनून बचपन से ही मैने पाल लिया था. घर में बाहर से कोई सामान कागज में लपेट कर भी आता था तो मैं उस मुड़े-तुड़े कागज को पढने में लग जाती थी.
मेरे चाचा ( मेरे पिता को मैं चाचा ही कहती थी) मेरी इस लगन से बहुत प्रभावित थे. जब भी उनके आगे मैं बैठकर घुटना मोड़कर कभी इधर, कभी उधर करती और किताब लिए घूमना पड़ता तो उनको देखकर अच्छा नहीं लगता था.
एक दिन चाचा ने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मैंने मना कर दिया कि मुझे तो किसी चीज की कोई ज़रूरत नहीं है. वे उठकर बाहर चले गये. कैसे उनको बताती कि मुझे एक कुर्सी और मेज चाहिए जिस पर मैं बैठकर कुछ लिख सकूं और पढ़ सकूं. घर के हालात ऐसे थे नहीं कि मैं उन्हें कह पाती.
यह घर के लिए भी अनावश्यक चीज थी, जिसे रखने के लिए जगह निश्चित करना भी मुश्किल था. चाचा शाम को घर लौटे तो उनके हाथ में छोटा सा स्टूल था और छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी. मुझे देखकर बहुत हंसी आई. मैं पेट पकड़कर हंसती रही.
चाचा चुपचाप मेरी ओर देखते रहे. जब मैं चुप हुई तो उन्होंने कहा ये लो इस पर पढ़ा करो. ज़मीन पर रखकर बाहर चले गये थे. मैं हंसने के बाद रोने लगी थी, मुझे अजीब सी ग्लानि हुई थी उस वक़्त. जब घर में खाने तक के लाले पड़े थे तो चाचा ये सब मेरे लिए कर रहे थे.
सोचती रही थी कि कही मेरे हंसने से चाचा को बुरा न लगा हो. पर फिर भी मैं बहुत खुश हुई थी, अब मेरा कोना घर में निश्चित हो गया था. हांलाकि स्टूल और कुर्सी का साइज़ छोटा था और मैं अब बड़ी हो चुकी थी, पर चाचा के लिए मैं आज भी छोटी ही थी.
मां ने कहा भी कि अब ये छोटी नहीं रही इस स्टूल में से पैर बाहर निकल रहे हैं और कुर्सी पर धंस कर बैठी है. चाचा हंसी का कारण समझ गये थे और खुद भी मुस्कराने लगे थे. पर मैं बहुत खुश थी, मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी.
इस तरह मेरा कमरा, यानी वह प्लास्टिक की कुर्सी और छोटा स्टूल , बन गया था पर \मल्टी परपज\ भी बना साथ मे ही. जब भी कोई मेहमान आता था मेरी किताबों को वहां से उतारकर उस पर चाय रखने के लिए दे दी जाती, जिससे मुझे बड़ा खराब लगता था. चाय पी लेने के बाद फ़िर वह मेरा ही बन जाता.
समय गुजरता चला गया और मैं दसवीं में आ गयी थी, पर पढ़ाई के साथ – साथ में अब जो भी आस-पास घट रहा होता, मेरे घर परिवार में जो भी हो रहा होता मैं उसे अब कागजों पर उतारने लगी थी.
जब अपने गुस्से को शांत कर जाती, यूं कहे कि वो पल गुजर जाते, जो मन को बहुत विचलित करते थे, तो उन्हीं कागजों को फ़ाड़ देती थी. मेरे हम उम्र सब जानते थे कि मैं कुछ न कुछ पढ़ाई के अलावा लिखती भी रहती हूं, कभी-कभार वे पढ़ते और मुझे कहते कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो बहुत मारेंगे तुझे, स्कूल से निकाल लेंगे और मैं ओर भी डर जाती और फ़ाड़ देती.
अपने मन की बात कहने और घर के आए दिन झगड़ों से परेशान होकर अपने मन की भड़ास मैं इन कागज के टुकड़ों पर ही निकालती और इसके अलावा अपने भाई सुभाष, जो मुझे दूर रहता था उसे चिट्ठी लिखती रहती. उसमें सब का ज़िक्र होता.
उससे पिछली बार मिलने के बाद की सारी आस -पास घटी घटनाओं को बहुत विस्तार से वर्णन होता, और जब भी वह मिलता तो मैं उसे दे देती थी. ऐसे ही वह भी करता. हमारा एक दूसरे को लिखे पत्र-व्यवहार आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं.
मैं और मेरा वह स्टूल और कुर्सी, जो अब केवल किताबें रखने के काम आता था, एक ज़रूर और आवश्यक अंग बन गए थे घर का. पर जिसे एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता था, ठीक उसी तरह जैसे मैं भी अब उसे छोड़कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पीछे बनी झुग्गी में रहने के लिए आ गयी थी. पर पूरे परिवार में वह स्टूल मेरे नाम से ही जाना गया था.
मैं अब गांव में नहीं थी, पर मेरा स्टूल, मेरा वह कोना, दोनों मैं अपनी विरासत के रूप में अपनी पहचान के रूप में छोड़कर चली आयी थी. विश्वविद्यालय के छात्रावास की फ़ीस बहुत ज्यादा थी, जो मेरे और चाचा के बूते की बात नहीं ही थी.
एमए करना ही था तो पहले कुछ महीने राजौंद और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ने वाले फ़रल, पुंडरी में नानकों के घर पर बिताए जहां पर नानी दूसरों के घरों में काम करके अपनी ज़िन्दगी बिता रही थी.
मुझे भी नानी के साथ बहुत बार सफ़ाई और मैला उठाने के लिए जाना पड़ता था. हम दोनों के लिए रोटी और आचार या कभी कभी सब्जी भी उस गंध को अपने सिर पर ढोकर ले जाने के बदले मिल जाती थी. इस पर विस्तार से कभी फिर लिखूंगी.
ऐसे में मेरी पढ़ाई को नुकसान हो रहा था, तो मैंने चाचा के साथ बात करके वहीं विश्वविद्यालय के छात्रावास के पीछे पड़ने वाली झुग्गी में रहकर पढ़ने की बात की. घर से राशन पानी और छोटा स्टोव और एक थाली, चम्मच, गिलास आदि ये सब लेकर गई.
जितने कम से कम खर्च हो पाए इसकी मेरी कोशिश रही. मां और चाचा की आर्थिक स्थिति क्या है, मैं जानती थी. सबने मना किया था आगे पढ़ने के लिए, बहुत सारे कारणों के साथ एक कारण यह भी तो था कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं होगा, यह बात मैं और चाचा दोनों ही जानते थे, पर दोनों को ही दृढ़ विश्वास था कि कम से कम खर्च में मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ.
किताबों पर खर्च करने के अलावा ऐसा कोई खर्च था भी नहीं जो झेला न जा सके. ना कभी अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए प्रयोग होने वाले क्रीम आदि का मुझे शौक था न किसी और चीज का ही शौक़ था, और न ही तन ढकने के अलावा कपड़ों का ही शौक़ था, इसलिए चाचा की सहमति से मैं आ गई थी इस झुग्गी बस्ती में जो चूहड़ों की बस्ती के नाम से भी जानी जाती थी.
पूरी बस्ती का एक ही टायलेट था और एक ही नल, सुबह के समय बहुत परेशानी होती थी. इन सब का सामना करते हुए मैं अपने बारे में बहुत कुछ लिखती थी. कई डायरियां भर दी. जब कभी सुभाष आता तो उसे दे देती पढ़ने के लिए, जिसमें हर दिन गुजरने वाली पीड़ा, दुःख -तकलीफ़ अभाव भरा हुआ था.
कुछ मन की कोमल भावनाएं होतीं और वह अगली बार मिलता तो खूब रो लेता और अपनी असमर्थता जता जाता, हौसला देता, अपने सपने पूरे करने की कसमें दे जाता, चाचा के खून-पसीने से निकलने और मेरे लिए उंचाई पर पंहुचने के उनके अरमानों को पूरा करने की दुहाई दे जाता. बस अब यही उद्देश्य बन चुका था.
अब मेरा कमरा था मेरे पास, मेरी वह चालीस रुपये में किराये पर ली झुग्गी, जिसे मैं वहीं आस-पास के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर दे दिया करती थी, उन छात्रों के हालत भी मेरे जैसे ही रहती थी, इसलिए कई बार इस कमरे का किराया भी नहीं दे पाती थी. जिसके कारण बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था.
एमए के इस कठिन दौर में मेरे सुख-दुख का साथी, मेरा भाई, मुझे छोड़कर चला गया- टूट गया था, बहुत कुछ अंदर से, कदम भी लड़खड़ा गये थे, पर उसका वह वाक्य कि ”अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, कुछ बनना है, सपनों को पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए, थकना नहीं, हारना नहीं.”
बहुत कुछ लिखा इस दौरान, मेरे पाठयक्रम की पढ़ाई के अलावा मैं और भी बहुत कुछ करती, यूपीएससी की तैयारी के साथ कविता, कहानियां बल्कि यूं कहूं कि अपना दर्द कागजों पर उतारने लगी थी. पर इनको सहेजने का ख्याल न मुझे पहले आया था, और न इस दौरान, बस अगर इधर-उधर कॉपियों पर लिखा रह गया था थोड़ा बहुत.
अभी समय को एक और झटका देना बाकी था. एमए का पहला साल पास कर लिया था, फ़ाइनल में प्रवेश ले लिया था. मेरे इस झुग्गी वाले कमरे के हर कोने में कुछ साहित्यक पत्र पत्रिकाएं जमा होने लगी थीं. नेट की तैयारी दिन रात कर रही थी.
लाइब्रेरी खुलते ही दूसरे तले के कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती थी और बन्द होने तक वहीं रहती थी. साथ ही साथ यूपीएससी, जो मेरे अपना -सपना था, उसकी भी तैयारी चल रही थी.
चाचा स्कूल में मैडम और सबसे बड़ी डिग्री लेने का सपना देख रहे थे, सुभाष कॉलेज के लेक्चर स्टैंड पर लेक्चर देते हुए देखना चाहते थे और नीचे पटरी रखकर उस पर चढकर भाषण देने का सपना देखते थे- मेरी हाइट छोटी थी, इसलिए पटरी का साहरा लेकर लेक्चर देने का बिम्ब रचते. और मैं- मेरा सपना था यूपीएससी पास करना और बड़ी अधिकारी बनना, जिसके लिए मुफ़्त में चलने वाली कोचिंग भी मैंने चाचा को बिना बताये शुरु कर रखी थी.
और एक दिन वह भी अपने सपने के साथ इस सफ़र में साथ छोड़कर चले गये अनजान दुनिया में, कभी वापिस न आने के लिए.
बस अब मैं और मेरा कमरा ही रह गये थे, मतलब वह किराये की झुग्गी. अब कुछ भी करने का मतलब नहीं रह गया था, न अब सुभाष का साथ था और न चाचा. बाकी जितने भी रिश्ते थे, वे खून के रिश्ते जरूर थे पर उनसे कभी अपनेपन के दो शब्द नहीं मिले.
अगर कुछ भी मिला था तो वह शक करने वाली निगाहें थीं, जो मेरे गांव आने पर मानो एक ही सवाल पूछती थी कि मैं …मेरे अन्दर लड़की होने का शेष कुछ बचा भी है या …सब. और मैं मानो तसल्ली देने के लिए उनसे अपनी सफ़ाई देती कि मैं पढ़ रही हूं और बहुत मेहनत कर रही हूँ- हर बार कि अग्नि परीक्षा, जो मेरे हौसले को तोड़ने के लिए काफ़ी होती थी.
पर अब क्या? सब कुछ ख़त्म… तीन महीने लगे मुझे इस सदमे से बाहर आने के लिए. पर सबने जैसे अब मेरा साथ देने का मन भी बना लिया था, और सबसे ज्यादा मां मेरे साथ पूरी तरह से जुट गई थी, मानो चाचा ने मां को अब उनकी जगह लेने की कसम दे दी हो, दोनों भाई भी अब मेरे फ़ैसले के साथ थे.
और इस सफ़र में हमसफ़र बनकर आया मेरी जिन्दगी में मुकेश, जिसने मेरे अन्दर के खालीपन को भर दिया, उन्होंने चाचा और भाई का प्यार तो नहीं दिया पर कमी जरूर पूरी कर दी थी, उस मंजिल और सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया.
फिर चाचा के सपने को ज़िन्दगी का मकसद बना लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. हारना मानो मैंने बिसरा ही दिया. चाचा का एक एक शब्द अब मेरे जीने के लिए काफ़ी था.
झुग्गी अब छूट गयी थी, एमए के बाद अब बीएड करने करनाल आ गयी थी. यहां पर भी किराये का अपना कमरा ले लिया था, जब भी मकान मालिक को पता चलता कि मैं ”चूहड़े” समाज की हूं, कमरा छोड़ना पडता. इसी दौरान हमसफ़र को ताउम्र हमसफ़र बनाने का निर्णय लिया और हमने शादी कर ली. शादी के दूसरे दिन ही वापिस उसी कमरे में लौटना हुआ. बीएड करने के बाद एम फ़िल रोहतक से किया और फिर जेएनयू तक का सफ़र. अपना कमरा न होते हुए भी इन्हीं कमरों में लेखन कार्य चलता रहा.
अब मैं एक अध्यापिका बन गई थी, वो भी चंडीगढ़ जैसे बडे शहर में. पर यहां भी अपना कमरा तो था, लेकिन किराये का. कभी रामदरबार का कमरा तो कभी डड्डूमाजरा का कमरा.
इन सब को पार करते हुए पंहुच गयी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में. पर यहां भी कमरा तो मिला पर अपना नहीं, और इसी दौरान जाति व्यवस्था से जूझते हुए अपना घर, अपना कमरा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा-पर अटल निश्चय था और सामने मंज़िल.
मैंने सहूलियत न होते हुए भी अपना घर और उस घर में मेरा कमरा हो, ऐसा ठान लिया था. और आज मेरे पास अपना कमरा है, उस कमरे में अपनी पसंद की कुर्सी और टेबल है, पूरा कमरा ही मेरी लाइब्रेरी है, जिसमें पूरे घर के सामान को मिलाकर सबसे ज्यादा जो बनता है, वह पुस्तकें ही हैं. अब मेरे पास मेरा कमरा है, और उसके साथ चाचा की यादे हैं, जो मुझे निरन्तर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं.
– बीबीसी हिन्दी की वेबसाइट से साभार
वर्जीनिया वुल्फ की किताब ”A Room of One””s Own” का प्रकाशन 1929 में हुआ था, उसका केन्द्रीय स्वर है कि एक स्त्री का अपने लेखन के लिए अपना कमरा होना चाहिए, अपने निज को सुरक्षित रखने के लिए भी अपना कमरा, इसके लिए उसकी आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है. अपने कमरे को हासिल करने की इसी छटपटाहट को कौशल पंवार ने बीबीसी से साझा किया, जिसे साभार यहां प्रकाशित किया जा रहा है.
मेरा भी घर मे एक कोना होता, उसमें एक टेबल और कुर्सी होती, मै हमेशा इसके लिए तरसती थी. पर मेरे लिए वह कोना सुनिश्चित होना घर के एक हिस्से को घेरे रखने के बराबर होता.
इसमें मेरे मां- बाप की कोई ग़लती नहीं थी, उन्होंने भी तो सारी उम्र घर की इसी कोठरी में बिता दी थी. यह घर ही इसलिए कहलाया गया था क्योंकि इसी घर में सब मिलकर रहते थे, चाहे वह बकरी हो, मुर्गे हों या फ़िर एक कोने में रखा चूल्हा ही क्यों न हो, उसी के साथ सटे रहते थे एल्मुनियम के कुछ बर्तन.
उसी कोठरी में एक कोने में पीने के पानी के लिए एक मटका रखा रहता था, और एक कोने में अनाज को रखने का एक खुटला (एक तरह से मिट्टी की बनी अनाज को संग्रहित करने की टंकी) तो ये थी हमारी कोठरी, जो अन्दर और बाहर से थी जिसका हर एक कोना निश्चित था, इसलिए मेरे लिए उस कोठरी में एक कोना स्थाई रूप से बनना ही बहुत मुश्किल था.
उस समय का ये मेरा सबसे बड़ा सपना बन गया था कि मुर्गे और बकरी की तरह ही सही मेरा भी एक कोना बना रहे, जो हर दिन मुझे बदलना न पड़े पर नहीं बन सका था. उसी कमरे में मां, दादी और मेरे लिए भी एक कोना नहाने का बन जाता था, जिससे नहाने के बाद साफ़ कर दिया जाता था और उसी में चूल्हे पर खाना भी बनता था.
मैं अपने पढने के लिए खाट पर बैठकर घुटनों को मोड़कर ही उस पर किताब रख कर पढ़ लिया करती थी.
पढ़ने का जुनून बचपन से ही मैने पाल लिया था. घर में बाहर से कोई सामान कागज में लपेट कर भी आता था तो मैं उस मुड़े-तुड़े कागज को पढने में लग जाती थी.
मेरे चाचा ( मेरे पिता को मैं चाचा ही कहती थी) मेरी इस लगन से बहुत प्रभावित थे. जब भी उनके आगे मैं बैठकर घुटना मोड़कर कभी इधर, कभी उधर करती और किताब लिए घूमना पड़ता तो उनको देखकर अच्छा नहीं लगता था.
एक दिन चाचा ने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मैंने मना कर दिया कि मुझे तो किसी चीज की कोई ज़रूरत नहीं है. वे उठकर बाहर चले गये. कैसे उनको बताती कि मुझे एक कुर्सी और मेज चाहिए जिस पर मैं बैठकर कुछ लिख सकूं और पढ़ सकूं. घर के हालात ऐसे थे नहीं कि मैं उन्हें कह पाती.
यह घर के लिए भी अनावश्यक चीज थी, जिसे रखने के लिए जगह निश्चित करना भी मुश्किल था. चाचा शाम को घर लौटे तो उनके हाथ में छोटा सा स्टूल था और छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी. मुझे देखकर बहुत हंसी आई. मैं पेट पकड़कर हंसती रही.
चाचा चुपचाप मेरी ओर देखते रहे. जब मैं चुप हुई तो उन्होंने कहा ये लो इस पर पढ़ा करो. ज़मीन पर रखकर बाहर चले गये थे. मैं हंसने के बाद रोने लगी थी, मुझे अजीब सी ग्लानि हुई थी उस वक़्त. जब घर में खाने तक के लाले पड़े थे तो चाचा ये सब मेरे लिए कर रहे थे.
सोचती रही थी कि कही मेरे हंसने से चाचा को बुरा न लगा हो. पर फिर भी मैं बहुत खुश हुई थी, अब मेरा कोना घर में निश्चित हो गया था. हांलाकि स्टूल और कुर्सी का साइज़ छोटा था और मैं अब बड़ी हो चुकी थी, पर चाचा के लिए मैं आज भी छोटी ही थी.
मां ने कहा भी कि अब ये छोटी नहीं रही इस स्टूल में से पैर बाहर निकल रहे हैं और कुर्सी पर धंस कर बैठी है. चाचा हंसी का कारण समझ गये थे और खुद भी मुस्कराने लगे थे. पर मैं बहुत खुश थी, मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी.
इस तरह मेरा कमरा, यानी वह प्लास्टिक की कुर्सी और छोटा स्टूल , बन गया था पर \मल्टी परपज\ भी बना साथ मे ही. जब भी कोई मेहमान आता था मेरी किताबों को वहां से उतारकर उस पर चाय रखने के लिए दे दी जाती, जिससे मुझे बड़ा खराब लगता था. चाय पी लेने के बाद फ़िर वह मेरा ही बन जाता.
समय गुजरता चला गया और मैं दसवीं में आ गयी थी, पर पढ़ाई के साथ – साथ में अब जो भी आस-पास घट रहा होता, मेरे घर परिवार में जो भी हो रहा होता मैं उसे अब कागजों पर उतारने लगी थी.
जब अपने गुस्से को शांत कर जाती, यूं कहे कि वो पल गुजर जाते, जो मन को बहुत विचलित करते थे, तो उन्हीं कागजों को फ़ाड़ देती थी. मेरे हम उम्र सब जानते थे कि मैं कुछ न कुछ पढ़ाई के अलावा लिखती भी रहती हूं, कभी-कभार वे पढ़ते और मुझे कहते कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो बहुत मारेंगे तुझे, स्कूल से निकाल लेंगे और मैं ओर भी डर जाती और फ़ाड़ देती.
अपने मन की बात कहने और घर के आए दिन झगड़ों से परेशान होकर अपने मन की भड़ास मैं इन कागज के टुकड़ों पर ही निकालती और इसके अलावा अपने भाई सुभाष, जो मुझे दूर रहता था उसे चिट्ठी लिखती रहती. उसमें सब का ज़िक्र होता.
उससे पिछली बार मिलने के बाद की सारी आस -पास घटी घटनाओं को बहुत विस्तार से वर्णन होता, और जब भी वह मिलता तो मैं उसे दे देती थी. ऐसे ही वह भी करता. हमारा एक दूसरे को लिखे पत्र-व्यवहार आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं.
मैं और मेरा वह स्टूल और कुर्सी, जो अब केवल किताबें रखने के काम आता था, एक ज़रूर और आवश्यक अंग बन गए थे घर का. पर जिसे एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता था, ठीक उसी तरह जैसे मैं भी अब उसे छोड़कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पीछे बनी झुग्गी में रहने के लिए आ गयी थी. पर पूरे परिवार में वह स्टूल मेरे नाम से ही जाना गया था.
मैं अब गांव में नहीं थी, पर मेरा स्टूल, मेरा वह कोना, दोनों मैं अपनी विरासत के रूप में अपनी पहचान के रूप में छोड़कर चली आयी थी. विश्वविद्यालय के छात्रावास की फ़ीस बहुत ज्यादा थी, जो मेरे और चाचा के बूते की बात नहीं ही थी.
एमए करना ही था तो पहले कुछ महीने राजौंद और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ने वाले फ़रल, पुंडरी में नानकों के घर पर बिताए जहां पर नानी दूसरों के घरों में काम करके अपनी ज़िन्दगी बिता रही थी.
मुझे भी नानी के साथ बहुत बार सफ़ाई और मैला उठाने के लिए जाना पड़ता था. हम दोनों के लिए रोटी और आचार या कभी कभी सब्जी भी उस गंध को अपने सिर पर ढोकर ले जाने के बदले मिल जाती थी. इस पर विस्तार से कभी फिर लिखूंगी.
ऐसे में मेरी पढ़ाई को नुकसान हो रहा था, तो मैंने चाचा के साथ बात करके वहीं विश्वविद्यालय के छात्रावास के पीछे पड़ने वाली झुग्गी में रहकर पढ़ने की बात की. घर से राशन पानी और छोटा स्टोव और एक थाली, चम्मच, गिलास आदि ये सब लेकर गई.
जितने कम से कम खर्च हो पाए इसकी मेरी कोशिश रही. मां और चाचा की आर्थिक स्थिति क्या है, मैं जानती थी. सबने मना किया था आगे पढ़ने के लिए, बहुत सारे कारणों के साथ एक कारण यह भी तो था कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं होगा, यह बात मैं और चाचा दोनों ही जानते थे, पर दोनों को ही दृढ़ विश्वास था कि कम से कम खर्च में मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ.
किताबों पर खर्च करने के अलावा ऐसा कोई खर्च था भी नहीं जो झेला न जा सके. ना कभी अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए प्रयोग होने वाले क्रीम आदि का मुझे शौक था न किसी और चीज का ही शौक़ था, और न ही तन ढकने के अलावा कपड़ों का ही शौक़ था, इसलिए चाचा की सहमति से मैं आ गई थी इस झुग्गी बस्ती में जो चूहड़ों की बस्ती के नाम से भी जानी जाती थी.
पूरी बस्ती का एक ही टायलेट था और एक ही नल, सुबह के समय बहुत परेशानी होती थी. इन सब का सामना करते हुए मैं अपने बारे में बहुत कुछ लिखती थी. कई डायरियां भर दी. जब कभी सुभाष आता तो उसे दे देती पढ़ने के लिए, जिसमें हर दिन गुजरने वाली पीड़ा, दुःख -तकलीफ़ अभाव भरा हुआ था.
कुछ मन की कोमल भावनाएं होतीं और वह अगली बार मिलता तो खूब रो लेता और अपनी असमर्थता जता जाता, हौसला देता, अपने सपने पूरे करने की कसमें दे जाता, चाचा के खून-पसीने से निकलने और मेरे लिए उंचाई पर पंहुचने के उनके अरमानों को पूरा करने की दुहाई दे जाता. बस अब यही उद्देश्य बन चुका था.
अब मेरा कमरा था मेरे पास, मेरी वह चालीस रुपये में किराये पर ली झुग्गी, जिसे मैं वहीं आस-पास के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर दे दिया करती थी, उन छात्रों के हालत भी मेरे जैसे ही रहती थी, इसलिए कई बार इस कमरे का किराया भी नहीं दे पाती थी. जिसके कारण बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था.
एमए के इस कठिन दौर में मेरे सुख-दुख का साथी, मेरा भाई, मुझे छोड़कर चला गया- टूट गया था, बहुत कुछ अंदर से, कदम भी लड़खड़ा गये थे, पर उसका वह वाक्य कि ”अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, कुछ बनना है, सपनों को पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए, थकना नहीं, हारना नहीं.”
बहुत कुछ लिखा इस दौरान, मेरे पाठयक्रम की पढ़ाई के अलावा मैं और भी बहुत कुछ करती, यूपीएससी की तैयारी के साथ कविता, कहानियां बल्कि यूं कहूं कि अपना दर्द कागजों पर उतारने लगी थी. पर इनको सहेजने का ख्याल न मुझे पहले आया था, और न इस दौरान, बस अगर इधर-उधर कॉपियों पर लिखा रह गया था थोड़ा बहुत.
अभी समय को एक और झटका देना बाकी था. एमए का पहला साल पास कर लिया था, फ़ाइनल में प्रवेश ले लिया था. मेरे इस झुग्गी वाले कमरे के हर कोने में कुछ साहित्यक पत्र पत्रिकाएं जमा होने लगी थीं. नेट की तैयारी दिन रात कर रही थी.
लाइब्रेरी खुलते ही दूसरे तले के कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती थी और बन्द होने तक वहीं रहती थी. साथ ही साथ यूपीएससी, जो मेरे अपना -सपना था, उसकी भी तैयारी चल रही थी.
चाचा स्कूल में मैडम और सबसे बड़ी डिग्री लेने का सपना देख रहे थे, सुभाष कॉलेज के लेक्चर स्टैंड पर लेक्चर देते हुए देखना चाहते थे और नीचे पटरी रखकर उस पर चढकर भाषण देने का सपना देखते थे- मेरी हाइट छोटी थी, इसलिए पटरी का साहरा लेकर लेक्चर देने का बिम्ब रचते. और मैं- मेरा सपना था यूपीएससी पास करना और बड़ी अधिकारी बनना, जिसके लिए मुफ़्त में चलने वाली कोचिंग भी मैंने चाचा को बिना बताये शुरु कर रखी थी.
और एक दिन वह भी अपने सपने के साथ इस सफ़र में साथ छोड़कर चले गये अनजान दुनिया में, कभी वापिस न आने के लिए.
बस अब मैं और मेरा कमरा ही रह गये थे, मतलब वह किराये की झुग्गी. अब कुछ भी करने का मतलब नहीं रह गया था, न अब सुभाष का साथ था और न चाचा. बाकी जितने भी रिश्ते थे, वे खून के रिश्ते जरूर थे पर उनसे कभी अपनेपन के दो शब्द नहीं मिले.
अगर कुछ भी मिला था तो वह शक करने वाली निगाहें थीं, जो मेरे गांव आने पर मानो एक ही सवाल पूछती थी कि मैं …मेरे अन्दर लड़की होने का शेष कुछ बचा भी है या …सब. और मैं मानो तसल्ली देने के लिए उनसे अपनी सफ़ाई देती कि मैं पढ़ रही हूं और बहुत मेहनत कर रही हूँ- हर बार कि अग्नि परीक्षा, जो मेरे हौसले को तोड़ने के लिए काफ़ी होती थी.
पर अब क्या? सब कुछ ख़त्म… तीन महीने लगे मुझे इस सदमे से बाहर आने के लिए. पर सबने जैसे अब मेरा साथ देने का मन भी बना लिया था, और सबसे ज्यादा मां मेरे साथ पूरी तरह से जुट गई थी, मानो चाचा ने मां को अब उनकी जगह लेने की कसम दे दी हो, दोनों भाई भी अब मेरे फ़ैसले के साथ थे.
और इस सफ़र में हमसफ़र बनकर आया मेरी जिन्दगी में मुकेश, जिसने मेरे अन्दर के खालीपन को भर दिया, उन्होंने चाचा और भाई का प्यार तो नहीं दिया पर कमी जरूर पूरी कर दी थी, उस मंजिल और सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया.
फिर चाचा के सपने को ज़िन्दगी का मकसद बना लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. हारना मानो मैंने बिसरा ही दिया. चाचा का एक एक शब्द अब मेरे जीने के लिए काफ़ी था.
झुग्गी अब छूट गयी थी, एमए के बाद अब बीएड करने करनाल आ गयी थी. यहां पर भी किराये का अपना कमरा ले लिया था, जब भी मकान मालिक को पता चलता कि मैं ”चूहड़े” समाज की हूं, कमरा छोड़ना पडता. इसी दौरान हमसफ़र को ताउम्र हमसफ़र बनाने का निर्णय लिया और हमने शादी कर ली. शादी के दूसरे दिन ही वापिस उसी कमरे में लौटना हुआ. बीएड करने के बाद एम फ़िल रोहतक से किया और फिर जेएनयू तक का सफ़र. अपना कमरा न होते हुए भी इन्हीं कमरों में लेखन कार्य चलता रहा.
अब मैं एक अध्यापिका बन गई थी, वो भी चंडीगढ़ जैसे बडे शहर में. पर यहां भी अपना कमरा तो था, लेकिन किराये का. कभी रामदरबार का कमरा तो कभी डड्डूमाजरा का कमरा.
इन सब को पार करते हुए पंहुच गयी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में. पर यहां भी कमरा तो मिला पर अपना नहीं, और इसी दौरान जाति व्यवस्था से जूझते हुए अपना घर, अपना कमरा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा-पर अटल निश्चय था और सामने मंज़िल.
मैंने सहूलियत न होते हुए भी अपना घर और उस घर में मेरा कमरा हो, ऐसा ठान लिया था. और आज मेरे पास अपना कमरा है, उस कमरे में अपनी पसंद की कुर्सी और टेबल है, पूरा कमरा ही मेरी लाइब्रेरी है, जिसमें पूरे घर के सामान को मिलाकर सबसे ज्यादा जो बनता है, वह पुस्तकें ही हैं. अब मेरे पास मेरा कमरा है, और उसके साथ चाचा की यादे हैं, जो मुझे निरन्तर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं.
– बीबीसी हिन्दी की वेबसाइट से साभार हमारे यहां सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन चलाने वालों का आपसी तालमेल नहीं है- एड. सुरेश राव
 उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हेमपुर गांव के ग्रांट नंबर-18 में 1969 के मई महीने में एक बच्चे का जन्म होता है. लेकिन उसकी बदनसीबी ऐसी होती है कि उसके जन्म के दो महीने पहले ही उसके पिता गुजर जाते हैं. जन्म के बाद मां की दूसरी शादी हो जाती है और उस बच्चे को उसके दादा-दादी पालते हैं. जब वह अबोध 11 साल का होता है तो उसके दादा चल बसते हैं और 18 साल का होते-होते उसकी दादी भी साथ छोड़ जाती हैं. और वह अठारह साल का नवयुवा अपने जीवन में अकेला रह जाता है. कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन सच है.
आप कल्पना करिए कि कोई आम नवयुवक होता तो ऐसे में क्या करता? शायद वह जिंदगी से निराश हो जाता. ज्यादा संभावना थी कि वह गलत संगत में पर जाता. अगर ये न भी होता तो वह इस दुनिया की भीड़ में तो जरूर खो गया होता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि इन तमाम नाकारात्मक घटनाओं में एक अच्छी घटना यह हुई कि वह बालक बचपन में ही प्रभुदयाल नामक एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति के संपर्क में आ गया. असल में उस बच्चे के पिता एक जागरुक व्यक्ति थे और किसानी के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते रहते थे. उनके पिता के घनिष्ट मित्र थे- प्रभुदयाल, जो कासगंज के कट्टर अम्बेडकरवादी बाबूलाल बौद्ध की संगत में थे. चूंकि प्रभुदयाल और उस बालक के पिता अच्छे मित्र थे, सो अम्बेडकरवाद और आंदोलन की बात उन दोनों से होते हुए उस बालक तक भी पहुंचने लगी.
आखिरकार जीवन में तमाम झटके खाने के बावजूद भटकने की बजाय इस युवा ने अम्बेडकरवाद की राह चुनी और उसी में रम गया. आगे चलकर उसने ‘भारतीय बहुजन महासभा’ (BBM) नाम के एक संगठन की नींव रखी. जी हां, हम जो हकीकत बयां कर रहे हैं वह भारतीय बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश राव की है, जिन्होंने भारत भर में अम्बेडकरवाद की मशाल को जला रखा है और मान्यवर कांशीराम के सपने को साकार करने में जुटे हैं. 28 नवंबर 2016 को इस संगठन के पांच साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर जब ‘दलित दस्तक’ ने एड. राव के संघर्ष के बारे में जानने की कोशिश की तो उनके सामाजिक और आंदोलन के जीवन के साथ-साथ उनके जीवन का जो व्यक्तिगत पक्ष निकल कर सामने आया, उसने एक बार झकझोर कर रख दिया. उनका जीवन कईयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है, इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन का जिक्र करना भी जरूरी था.
राव कहते हैं, “प्रभुदयाल मेरे ताऊ जैसे थे. पिताजी के गुजर जाने के बाद उनका भी पारिवारिक जीवन से मोहभंग हो गया और वह अकेले ही रहे. जब मैं 10-12 साल का था तभी से उनके साथ सभा-सम्मेलनों में जाने लगा. वो अनपढ़ थे, लेकिन मिशन को लेकर समर्पित थे. उन्हें बहुजन आंदोलन और महापुरुषों के बारे में जानने का बहुत शौक था. वह किताबें खरीद कर लातें और हमें पैसे देते कि पढ़कर सुनाओ. उन्होंने अपनी जमीनें बेंच दी और बहुजन आंदोलन की किताबें खरीदकर लोगों में बांटने लगे. उनका यह समर्पण देखकर मेरे जीवन में काफी प्रभाव पड़ा. मैंने सोचा कि जब वो अनपढ़ होकर इतना सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं?”
राव बताते हैं, “मैंने लखीमपुर से ग्रेजुएशन किया. 1993 में लखनऊ से वकालत की पढ़ाई पूरी की. मैंने बी.एड भी किया और सोशल वर्क में एम.ए भी किया. इस बीच 1990 में ही मैं बामसेफ से जुड़ चुका था. 1990 से लेकर 2005 तक मैं बामसेफ में बहुत सक्रिय रहा. 2005 में बामसेफ में काफी गुटबाजी दिखने लगी. 2006 में जब साहब का परिनिर्वाण हुआ तो एक बार सोचा कि अब क्या करना चाहिए.” राव कहते हैं कि मुझे साहब के सोशल इंजीनियरिंग वाली बात ज्यादा समझ में आती थी. क्योंकि अगर मैं धार्मिक आंदोलन को चुनता तो फिर मुसलमान भाईयों से कैसे जुड़ता? सन् 1963-83 तक साहब ने बंद कमरे में लोगों के बीच कैडर कैंप के जरिए काफी काम किया. मैंने भी वही शुरु किया और ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण दिवस पर 28 नवंबर 2011 को लखनऊ में प्रेस क्लब में ‘भारतीय बहुजन महासभा’ की घोषणा की और यह घोषणा किया कि मान्यवर कांशीराम ने 20 सालों तक जो काम किया, उसी को आगे बढ़ाऊंगा.
राव के काम करने का तरीका भी निराला है. उनकी क्लास (कैडर) पांच घंटे की होती है. वह लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पांच घंटे के लिए एक बंद कमरे में बैठा लेते हैं, फिर शुरू होती है उनकी क्लास और वह ज्यों-ज्यों भारतीय सामाजिक व्यवस्था की परतों को उधेरते जाते हैं, उनके कैडर में मौजूद लोगों के आंखों के सामने से अंधविश्वास का परदा दरकने लगता है. हालांकि एक ही बार में लोग बदल नहीं जाते लेकिन राव सामने वाले के मन में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, बहुजन समाज का इतिहास और मनगढ़ंत धारणाओं और परंपराओं को लेकर कई सवाल छोड़ जाते हैं. फिर दो-तीन मीटिंग के बाद कैडर लेने वाला व्यक्ति अंधविश्वास और मानसिक गुलामी से बाहर निकल चुका होता है.
बहुजन महापुरुषों का जिक्र करते हुए राव कहते हैं कि जितने भी बहुजन नायक हैं, उनके आंदोलन का उद्देश्य मनुवादी व्यवस्था को खतम करके मानवतावादी व्यवस्था की स्थापना करना और उसे बनाए रखना था, क्योंकि इसमें किसी का अहित नहीं था. मैंने भी उसी उद्देश्य को लेकर काम करना शुरु किया. बहुजन समाज की समस्या क्या है?, पूछने पर राव कहते हैं, “असल में मनुवाद की जड़ अंधविश्वास है. यहां लोगों को खुद से ज्यादा भरोसा पत्थर और पेड़ में है. हम इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं.”
भारतीय इतिहासकारों की साजिशों को लेकर भी राव काफी गुस्से में दिखते हैं. बाबासाहेब का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि बाबासाहेब का कहना था कि भारत का इतिहास ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच हुए संघर्ष का इतिहास है. हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि ‘गुप्तकाल’ सवर्ण काल था, मेरा सवाल है कि जिस काल में देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव और भुखमरी में जी रहे थी, वह सवर्ण काल कैसे हो सकता है? इतिहासकार मौर्य काल को सवर्णिम काल क्यों नहीं कहते जब इस देश में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे.
भारतीय बहुजन महासभा (BBM) का उद्देश्य क्या है, पूछने पर राव कहते हैं, “बहुजन समाज के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना, उनको उनका इतिहास बताना, बहुजन महापुरुषों के संघर्ष और संघर्ष के इतिहास को बताना है. बहुजन समाज को इकट्ठा करना उद्देश्य है क्योंकि सारे बहुजन 2200 साल पहले बौद्ध थे. बाद में वो विभिन्न जातियों में बंट गए. पांच साल काम करने के बाद बहुजन समाज की स्थिति को वह कैसे आंकते हैं? इस सवाल के जवाब में राव कहते हैं कि बाबासाहेब के तीन मुख्य आंदोलन थे. (1) सामाजिक (2) राजनैतिक और (3) धार्मिक. ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब और शाहूजी महाराज ने इस पर काफी काम किया. लेकिन सामाजिक आंदोलन बहुत बड़ा है. देश के 85 फीसदी लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें मानसिक गुलामी से बाहर निकालना है. असल में लोग बाबासाहेब को भी मान रहे हैं और हिन्दू धर्म को भी मानते हैं. लोग बीच में हैं; इस वजह से सांस्कृतिक क्रांति नहीं हो पा रही है. वंचितों-बहुजनों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है. उन्हें यह समझना होगा कि जिस बजट में वे सालों भर तीर्थ करते हैं, उस बजट में वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं.
इन पांच सालों में कितनी सफलता मिली, पूछने पर राव कहते है कि लोग अंधविश्वास और परंपराओं से बाहर आ रहे हैं. असल में दिक्कत यह है कि मेहनत व्यक्ति करता है और क्रेडिट धागा और पत्थर ले जाता है. हम इसी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं. संगठन कहां-कहां सक्रिय है के जवाब में बताते हैं कि संगठन 15 राज्यों में है और हमारा संगठन फिलहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मणिपुर में ज्यादा सक्रिय है. आने वाले पांच सालों में वह अपने नेटवर्क को 20-25 राज्यों तक पहुंचाने की बात करते हैं.
बीबीएम राजनैतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के करीब है लेकिन राव का मानना है कि बहुजन राजनीति में ट्रेंड लोगों की कमी है. इसकी वजह सोशल मूवमेंट का कम होना है. अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के संघर्ष में राव बहुजन आंदोलन में एक और कमी की ओर इशारा करते हैं. कहते हैं, “हमारे यहां सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन चलाने वालों का आपसी तालमेल नहीं है, जबकि हमारे विरोधी पक्ष का अंदरखाने गहरा तालमेल है. मनुवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष में अम्बेडकरवादियों को बहुत सी बातें सीखने की जरूरत है. मनुवादी आंदोलन में सोशल मूवमेंट श्रेष्ठ है और राजनीतिक मूवमेंट दूसरे नंबर पर है, जबकि हमारे यहां उल्टा है, यह बड़ी दिक्कत है.”
हालांकि राव अपने संगठन के जरिए अपनी पूरी ताकत से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतिकार और बहुजन समाज के लोगों को जगाने में जुटे हैं. इस मुहिम में उनकी पत्नी इंदिरा राव और संगठन के सभी सहयोगी राव की ताकत हैं. राव कहते हैं, “अंतिम उद्देश्य बहुजन समाज को शासक बनाना है. या यूं कहें कि अंतिम उद्देश्य सम्राट अशोक जैसा भारत बनाने का है, क्योंकि वह हमारा स्वर्णिम काल था. सत्ता इसका माध्यम है.”
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हेमपुर गांव के ग्रांट नंबर-18 में 1969 के मई महीने में एक बच्चे का जन्म होता है. लेकिन उसकी बदनसीबी ऐसी होती है कि उसके जन्म के दो महीने पहले ही उसके पिता गुजर जाते हैं. जन्म के बाद मां की दूसरी शादी हो जाती है और उस बच्चे को उसके दादा-दादी पालते हैं. जब वह अबोध 11 साल का होता है तो उसके दादा चल बसते हैं और 18 साल का होते-होते उसकी दादी भी साथ छोड़ जाती हैं. और वह अठारह साल का नवयुवा अपने जीवन में अकेला रह जाता है. कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन सच है.
आप कल्पना करिए कि कोई आम नवयुवक होता तो ऐसे में क्या करता? शायद वह जिंदगी से निराश हो जाता. ज्यादा संभावना थी कि वह गलत संगत में पर जाता. अगर ये न भी होता तो वह इस दुनिया की भीड़ में तो जरूर खो गया होता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि इन तमाम नाकारात्मक घटनाओं में एक अच्छी घटना यह हुई कि वह बालक बचपन में ही प्रभुदयाल नामक एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति के संपर्क में आ गया. असल में उस बच्चे के पिता एक जागरुक व्यक्ति थे और किसानी के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते रहते थे. उनके पिता के घनिष्ट मित्र थे- प्रभुदयाल, जो कासगंज के कट्टर अम्बेडकरवादी बाबूलाल बौद्ध की संगत में थे. चूंकि प्रभुदयाल और उस बालक के पिता अच्छे मित्र थे, सो अम्बेडकरवाद और आंदोलन की बात उन दोनों से होते हुए उस बालक तक भी पहुंचने लगी.
आखिरकार जीवन में तमाम झटके खाने के बावजूद भटकने की बजाय इस युवा ने अम्बेडकरवाद की राह चुनी और उसी में रम गया. आगे चलकर उसने ‘भारतीय बहुजन महासभा’ (BBM) नाम के एक संगठन की नींव रखी. जी हां, हम जो हकीकत बयां कर रहे हैं वह भारतीय बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश राव की है, जिन्होंने भारत भर में अम्बेडकरवाद की मशाल को जला रखा है और मान्यवर कांशीराम के सपने को साकार करने में जुटे हैं. 28 नवंबर 2016 को इस संगठन के पांच साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर जब ‘दलित दस्तक’ ने एड. राव के संघर्ष के बारे में जानने की कोशिश की तो उनके सामाजिक और आंदोलन के जीवन के साथ-साथ उनके जीवन का जो व्यक्तिगत पक्ष निकल कर सामने आया, उसने एक बार झकझोर कर रख दिया. उनका जीवन कईयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है, इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन का जिक्र करना भी जरूरी था.
राव कहते हैं, “प्रभुदयाल मेरे ताऊ जैसे थे. पिताजी के गुजर जाने के बाद उनका भी पारिवारिक जीवन से मोहभंग हो गया और वह अकेले ही रहे. जब मैं 10-12 साल का था तभी से उनके साथ सभा-सम्मेलनों में जाने लगा. वो अनपढ़ थे, लेकिन मिशन को लेकर समर्पित थे. उन्हें बहुजन आंदोलन और महापुरुषों के बारे में जानने का बहुत शौक था. वह किताबें खरीद कर लातें और हमें पैसे देते कि पढ़कर सुनाओ. उन्होंने अपनी जमीनें बेंच दी और बहुजन आंदोलन की किताबें खरीदकर लोगों में बांटने लगे. उनका यह समर्पण देखकर मेरे जीवन में काफी प्रभाव पड़ा. मैंने सोचा कि जब वो अनपढ़ होकर इतना सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं?”
राव बताते हैं, “मैंने लखीमपुर से ग्रेजुएशन किया. 1993 में लखनऊ से वकालत की पढ़ाई पूरी की. मैंने बी.एड भी किया और सोशल वर्क में एम.ए भी किया. इस बीच 1990 में ही मैं बामसेफ से जुड़ चुका था. 1990 से लेकर 2005 तक मैं बामसेफ में बहुत सक्रिय रहा. 2005 में बामसेफ में काफी गुटबाजी दिखने लगी. 2006 में जब साहब का परिनिर्वाण हुआ तो एक बार सोचा कि अब क्या करना चाहिए.” राव कहते हैं कि मुझे साहब के सोशल इंजीनियरिंग वाली बात ज्यादा समझ में आती थी. क्योंकि अगर मैं धार्मिक आंदोलन को चुनता तो फिर मुसलमान भाईयों से कैसे जुड़ता? सन् 1963-83 तक साहब ने बंद कमरे में लोगों के बीच कैडर कैंप के जरिए काफी काम किया. मैंने भी वही शुरु किया और ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण दिवस पर 28 नवंबर 2011 को लखनऊ में प्रेस क्लब में ‘भारतीय बहुजन महासभा’ की घोषणा की और यह घोषणा किया कि मान्यवर कांशीराम ने 20 सालों तक जो काम किया, उसी को आगे बढ़ाऊंगा.
राव के काम करने का तरीका भी निराला है. उनकी क्लास (कैडर) पांच घंटे की होती है. वह लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पांच घंटे के लिए एक बंद कमरे में बैठा लेते हैं, फिर शुरू होती है उनकी क्लास और वह ज्यों-ज्यों भारतीय सामाजिक व्यवस्था की परतों को उधेरते जाते हैं, उनके कैडर में मौजूद लोगों के आंखों के सामने से अंधविश्वास का परदा दरकने लगता है. हालांकि एक ही बार में लोग बदल नहीं जाते लेकिन राव सामने वाले के मन में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, बहुजन समाज का इतिहास और मनगढ़ंत धारणाओं और परंपराओं को लेकर कई सवाल छोड़ जाते हैं. फिर दो-तीन मीटिंग के बाद कैडर लेने वाला व्यक्ति अंधविश्वास और मानसिक गुलामी से बाहर निकल चुका होता है.
बहुजन महापुरुषों का जिक्र करते हुए राव कहते हैं कि जितने भी बहुजन नायक हैं, उनके आंदोलन का उद्देश्य मनुवादी व्यवस्था को खतम करके मानवतावादी व्यवस्था की स्थापना करना और उसे बनाए रखना था, क्योंकि इसमें किसी का अहित नहीं था. मैंने भी उसी उद्देश्य को लेकर काम करना शुरु किया. बहुजन समाज की समस्या क्या है?, पूछने पर राव कहते हैं, “असल में मनुवाद की जड़ अंधविश्वास है. यहां लोगों को खुद से ज्यादा भरोसा पत्थर और पेड़ में है. हम इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं.”
भारतीय इतिहासकारों की साजिशों को लेकर भी राव काफी गुस्से में दिखते हैं. बाबासाहेब का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि बाबासाहेब का कहना था कि भारत का इतिहास ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच हुए संघर्ष का इतिहास है. हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि ‘गुप्तकाल’ सवर्ण काल था, मेरा सवाल है कि जिस काल में देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव और भुखमरी में जी रहे थी, वह सवर्ण काल कैसे हो सकता है? इतिहासकार मौर्य काल को सवर्णिम काल क्यों नहीं कहते जब इस देश में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे.
भारतीय बहुजन महासभा (BBM) का उद्देश्य क्या है, पूछने पर राव कहते हैं, “बहुजन समाज के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना, उनको उनका इतिहास बताना, बहुजन महापुरुषों के संघर्ष और संघर्ष के इतिहास को बताना है. बहुजन समाज को इकट्ठा करना उद्देश्य है क्योंकि सारे बहुजन 2200 साल पहले बौद्ध थे. बाद में वो विभिन्न जातियों में बंट गए. पांच साल काम करने के बाद बहुजन समाज की स्थिति को वह कैसे आंकते हैं? इस सवाल के जवाब में राव कहते हैं कि बाबासाहेब के तीन मुख्य आंदोलन थे. (1) सामाजिक (2) राजनैतिक और (3) धार्मिक. ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब और शाहूजी महाराज ने इस पर काफी काम किया. लेकिन सामाजिक आंदोलन बहुत बड़ा है. देश के 85 फीसदी लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें मानसिक गुलामी से बाहर निकालना है. असल में लोग बाबासाहेब को भी मान रहे हैं और हिन्दू धर्म को भी मानते हैं. लोग बीच में हैं; इस वजह से सांस्कृतिक क्रांति नहीं हो पा रही है. वंचितों-बहुजनों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है. उन्हें यह समझना होगा कि जिस बजट में वे सालों भर तीर्थ करते हैं, उस बजट में वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं.
इन पांच सालों में कितनी सफलता मिली, पूछने पर राव कहते है कि लोग अंधविश्वास और परंपराओं से बाहर आ रहे हैं. असल में दिक्कत यह है कि मेहनत व्यक्ति करता है और क्रेडिट धागा और पत्थर ले जाता है. हम इसी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं. संगठन कहां-कहां सक्रिय है के जवाब में बताते हैं कि संगठन 15 राज्यों में है और हमारा संगठन फिलहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मणिपुर में ज्यादा सक्रिय है. आने वाले पांच सालों में वह अपने नेटवर्क को 20-25 राज्यों तक पहुंचाने की बात करते हैं.
बीबीएम राजनैतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के करीब है लेकिन राव का मानना है कि बहुजन राजनीति में ट्रेंड लोगों की कमी है. इसकी वजह सोशल मूवमेंट का कम होना है. अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के संघर्ष में राव बहुजन आंदोलन में एक और कमी की ओर इशारा करते हैं. कहते हैं, “हमारे यहां सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन चलाने वालों का आपसी तालमेल नहीं है, जबकि हमारे विरोधी पक्ष का अंदरखाने गहरा तालमेल है. मनुवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष में अम्बेडकरवादियों को बहुत सी बातें सीखने की जरूरत है. मनुवादी आंदोलन में सोशल मूवमेंट श्रेष्ठ है और राजनीतिक मूवमेंट दूसरे नंबर पर है, जबकि हमारे यहां उल्टा है, यह बड़ी दिक्कत है.”
हालांकि राव अपने संगठन के जरिए अपनी पूरी ताकत से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतिकार और बहुजन समाज के लोगों को जगाने में जुटे हैं. इस मुहिम में उनकी पत्नी इंदिरा राव और संगठन के सभी सहयोगी राव की ताकत हैं. राव कहते हैं, “अंतिम उद्देश्य बहुजन समाज को शासक बनाना है. या यूं कहें कि अंतिम उद्देश्य सम्राट अशोक जैसा भारत बनाने का है, क्योंकि वह हमारा स्वर्णिम काल था. सत्ता इसका माध्यम है.” 



